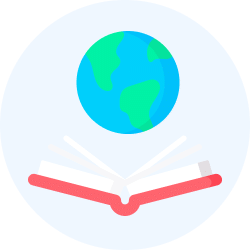Playwriting Grammar (नाटक लिखने का व्याकरण) NCERT Solutions | Hindi Class 12 - Humanities/Arts PDF Download
अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1: नाटक की कहानी बेशक भूतकाल या भविष्य काल से संबंध हो, तब भी उसे वर्तमान काल में ही घटित होना पड़ता है- इस धारणा के पीछे क्या कारण हो सकते हैं?
नाटक को दृश्य काव्य माना जाता है। इसे दर्शकों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। प्रत्येक नाटक का एक निश्चित समय सीमा में समाप्त होना भी आवश्यक है। साहित्य के अन्य विधाओं जैसे कहानी, उपन्यास, कविता, निबंध को पढ़ने के लिए हम अपनी सुविधा के अनुसार समय निकाल सकते हैं। एक ही कहानी को कई दिनों में थोड़ा थोड़ा पढ़ कर समाप्त कर सकते हैं परंतु नाटक को तो दर्शकों ने एक निश्चित समय सीमा में एक ही स्थान पर देखना होता है। नाटककार अपने नाटक का कथ्य भूतकाल से ले अथवा भविष्य काल से उसे उस नाटक को वर्तमान काल में ही संयोजित करना पड़ता है कैसा भी नाटक हो उसे एक विशेष समय में, एक विशेष स्थान पर और वर्तमान काल में ही घटित होना होता है। कोई भी पौराणिक अथवा ऐतिहासिक कथानक भी नाटक के रूप में हमारे सम्मुख, हमारी आंखों के सामने वर्तमान में ही घटित होता है। इसीलिए नाटक के मंच निर्देश वर्तमान काल में ही लिखे जाते हैं। इन्हीं कारणों से नाटक की कहानी बेशक भूतकाल या भविष्य काल से संबंध हो उसे वर्तमान काल में ही घटित होना पड़ता है।
प्रश्न 2: संवाद चाहे कितना भी तत्सम और क्लिष्ट भाषा में क्यों न लिखे गए हो। स्थिति और परिवेश की मांग के अनुसार यदि वे स्वाभाविक जान पड़ते हैं तो उनके दर्शक तक संप्रेषित होने में कोई मुश्किल नहीं है। क्या आप इससे सहमत हैं? पक्ष या विपक्ष में तर्क दीजिए।
हम इस कथन से सहमत है कि सागवान चाहे कितने भी तत्सम और क्लिष्ट भाषा में क्यों न लिखे गए हो। स्थिति और परिवेश की मांग के अनुसार यदि वे स्वाभाविक जान पड़ते हैं तो उनके दर्शक तक संप्रेषित होने में कोई मुश्किल नहीं होती। इसका प्रमुख कारण यह है कि दर्शक नाटक देख रहा है। वह मानसिक रूप से उस युग के परिवेश में पहुंच जाता है जिससे संबंधित वह नाटक हैं। पुरानी कथा ने को पर आधारित नाटकों में तत्सम प्रधान शब्दावली को भी वह अभिनेताओं के अभिनय, हाव भाव, संवाद बोलने के ढंग से समझ जाता है। रामायण और महाभारत के नाटकों में पिता श्री, भ्राता श्री, माता श्री शब्दों का प्रयोग बच्चे बच्चे को स्मरण हो गया था। इसी प्रकार से जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, सुरेंद्र वर्मा आदि के नाटकों में प्रयुक्त शब्दावली भी परिवेश के कारण सहज रूप से हृदयंगम हो जाती है।
प्रश्न 3: समाचार पत्र के किसी कहानीनुमा समाचार से नाटक की रचना करें।
रांची दिनांक 24 मार्च–
पैसों की तंगी के कारण रमेश ने अपनी पुत्री अलका का विवाह रोक दिया था कि उसके मित्र सुरेश ने उसकी बेटी के विवाह पर सारा भार अपने ऊपर ले कर उसका विवाह निश्चित तिथि पर कराया | आज के युग में मित्रता की ऐसी मिसाल कम ही दिखाई देती है। सुरेश की इस पहल पर मोहल्ले वालों ने भी रमेश की सहायता की।
इस समाचार का नाट्य रूपांतरण निम्नलिखित होगा-
(स्थान घर का बरामदा। रमेश सिर पकड़ कर बैठा है। उसकी पत्नी पूनम और पुत्री अलका भी उदास बैठे हैं।)
पूनम – ( रमेश को समझाते हुए ) कोई बात नहीं,धंधे में नफा नुकसान होता रहता है। अभी कुछ दिन की मोहलत मांग लेते हैं। लड़के वाले मान ही जाएंगे।
रमेश – ( रूंधे स्वर में ) अब कुछ नहीं हो सकता | अब तो यह है विवाह रोकना ही होगा। (तभी दौड़ता हुआ सुरेश वहां आता है)
सुरेश-अरे! रमेश! मैं यह क्या सुन रहा हूं? अलका का विवाह नहीं होगा।
रमेश- (मंद स्वर में) क्या करूं—व्यापार में घाटा पड़ गया है। सब कुछ समाप्त हो गया।
सुरेश- (आवेश में) क्या मैं मर गया हूं? अलका मेरी भी तो बेटी है। मैं करूंगा उसका विवाह।
पूनम-इसे कहते हैं मित्र । दिल में कसक उठी तो आया भागा -भागा। (उसी समय वहां मोहल्ले के कुछ लोग आ जाते हैं।)
एक बुजुर्ग-रमेश घबराओ मत अलका हम सब की बेटी है। हम सब मिलकर उसका विवाह करेंगे । क्यों भाइयों? (सब समवेत स्वर में हां करेंगे कहते हैं और पर्दा गिरता है।)
प्रश्न 4: (क) अध्यापक और शिष्य के बीच गृह कार्य को लेकर पांच-पांच संवाद लिखिए।
(ख) एक घरेलू महिला एवं रिक्शा चालक को ध्यान में रखते हुए पांच-पांच संवाद लिखिए।
(क)अध्यापक–रमेश, तुमने कहा कार्य किया है?
शिष्य–नहीं, मास्टर जी।
अध्यापक–क्यों नहीं किया।
शिष्य–मैं किसी कारण से नहीं कर पाया।
अध्यापक–किस कारण से नहीं कर पाए?
शिष्य–कल हमारे घर कुछ अतिथि आ गए थे।
अध्यापक–तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो?
शिष्य–नहीं, मास्टर जी।
अध्यापक–कल गृह कार्य जरूर कर के लाना।
शिष्य–जी, मास्टर जी। जरूर करके आऊंगा।
(ख) घरेलू महिला–रिक्शा! ओ रिक्शा वाले!
रिक्शा चालक–हां! मेम साहब।
घरेलू महिला–अशोका कॉलोनी चलोगे?
रिक्शा चालक–हां, चलूंगा।
घरेलू महिला–कितने पैसे लोगे?
रिक्शा चालक–जी, दस रुपये।
घरेलू महिला–दस रुपये का बहुत ज्यादा है?
रिक्शा चालक–क्या करें मैम साहब, महंगाई बहुत है।
घरेलू महिला–ठीक है, ठीक है। आठ रुपए ले लेना।
रिक्शा चालक–चलो, मेम साहब, आठ ही दे देना।
अति महत्त्वपूर्ण प्रश्न
प्रश्न 1: नाटक किसे कहते हैं ?
साहित्य की वह विधा जिसके पढ़ने के साथ-साथ अभिनय भी किया जा सकता है उसे नाटक कहते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में नाटक को दृश्य काव्य माना जाता है। नाटक रंगमंच की एक प्रमुख विधा है। इसलिए इसे पढ़ा, सुना और देखा भी जा सकता है।
प्रश्न 2: नाटक में चित्रित पात्र कैसे होने चाहिए ?
नाटक में पात्रों का बहुत महत्त्व है नाटक में चित्रित पात्र निम्नलिखित प्रकार के होते हैं:-
(i) पात्र चरित्रवान होने चाहिए।
(ii) पात्र आदर्शवादी होने चाहिए।
(iii) पात्र अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के होने चाहिए।
(iv) पात्र जीवंत तथा जीवन से जुड़े होने चाहिए।
(v) पात्र सामाजिक परिवेश से जुड़े होने चाहिए।
(vi) पात्र कथानक से संबंधित होने चाहिए।
प्रश्न 3: नाटक की भाषा-शैली कैसी होनी चाहिए?
नाटक की भाषा-शैली निम्नलिखित प्रकार की होनी चाहिए :-
(i) नाटक की भाषा-शैली सरल और सहज होनी चाहिए।
(ii) इसकी भाषा-शैली स्वाभाविक तथा प्रसंगानुकूल होनी चाहिए।
(iii) इसकी भाषा-शैली पात्रानुकूल होनी चाहिए।
(iv) इसकी भाषा-शैली विषयानुकूल होनी चाहिए।
(v) इसकी भाषा-शैली संवादों के अनुकूल होनी चाहिए।
(vi) इसकी भाषा-शैली सरस होनी चाहिए।
प्रश्न 4: नाटक और साहित्य की अन्य विधाओं में क्या अंतर है ? संक्षेप में बताइये।
साहित्य में कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध आदि विधाएँ आती हैं। नाटक भी साहित्य की एक प्रमुख विधा है किंतु नाटक तथा अन्य विधाओं में बहुत अंतर है जो इस प्रकार है-
(i) नाटक को दृश्य काव्य कहा जाता है किसी अन्य विधा को नहीं।
(ii) नाटक रंगमंच की एक विधा है किसी अन्य विधाओं के अंतर्गत कोई रंगमंच नहीं आता।
(iii) नाटक का अभिनय होता है जबकि अन्य विधाओं का अभिनय नहीं हो सकता।
(iv) नाटक को पढ़ा, सुना तथा देखा जा सकता है जबकि अन्य विधाओं को केवल पढ़ा तथा सुना जा सकता है।
(v) नाटक में अभिनय का गुण विद्यमान होता है जबकि अन्य विधाओं में यह गुण नहीं होता।
(vi) नाटक का संबंध दर्शकों से है जबकि अन्य विधाओं का संबंध पाठकों से है।
(vii) नाटक एक 'दर्शनीय' विधा है जबकि अन्य पाठनीय विधाएँ हैं।
प्रश्न 5: नाटक के विभिन्न तत्वों पर प्रकाश डालिए।
नाटक की रचना में विभिन्न तत्वों का महत्त्वपूर्ण योगदान है जो निम्नलिखित है :
(i) कथानक / कथावस्तु-नाटक में जो कुछ कहा जाए उसे कथानक अथवा कथावस्तु कहते हैं। यह नाटक का सबसे महत्त्वपूर्ण तत्व है इसी के आधार पर नाटक को आरंभ, मध्य और समापन मुख्यतः तीन भागों में बांटा जा सकता है।
(ii) पात्र योजना / चरित्र-चित्रण-यह नाटक का महत्त्वपूर्ण तत्व है। पात्रों के माध्यम से ही नाटककार कथानक को गतिशीलता प्रदान करता है। इनके माध्यम से ही यह नाटक का उद्देश्य स्पष्ट करता है। नाटक में एक प्रमुख पात्र तथा अन्य उसके सहायक पात्र होते हैं। प्रमुख पात्र को नायक अथवा नायिका कहते हैं।
(iii) संवाद योजना अथवा कथोपकथन-संवाद का शाब्दिक अर्थ है-परस्पर बातचीत अथवा नाटक में पात्रों की परस्पर बातचीत को संवाद अथवा कथोपकथन कहते हैं। संवाद योजना नाटक का प्रमुख तत्व है इसके बिना नाटक की कल्पना भी नहीं की जा सकती। संवाद ही कथानक को गतिशील बनाते हैं तथा पात्रों के चरित्र का उद्घाटन करते हैं। नाटक में संवाद योजना सहज, सरल, स्वाभाविक तथा पात्रानुकूल होना चाहिए।
(iv) अभिनेयता-यह नाटक का महत्त्वपूर्ण तत्व है। इसके द्वारा ही नाटक का मंच पर अभिनय किया जाता है। अभिनेयता के कारण ही नाटक अभिनय के योग्य बनता है।
(v) उद्देश्य-साहित्य की अन्य विधाओं के समान नाटक भी एक उद्देश्य पूर्ण रचना है। नाटककार अपने पात्रों के द्वारा इस उद्देश्य को स्पष्ट करता है।
(vi) भाषा-शैली-यह नाटक का महत्त्वपूर्ण तत्व है क्योंकि इसके माध्यम से ही नाटककार अपनी संवेदनाओं को अभिव्यक्त करता है। नाटक की भाषा-शैली सरल, सहज, स्वाभाविक, पात्रानुकूल तथा प्रसंगानुकूल होनी चाहिए।
प्रश्न 6: कथानक को कितने भागों में बाँटा गया है ?
कथानक को तीन भागों में बाँटा गया है-
(i) आरंभ, (ii) मध्य, (iii) समापन।
प्रश्न 7: नाटक में स्वीकार एवं अस्वीकार की अवधारणा से क्या तात्पर्य है ?
नाटक में स्वीकार के स्थान पर अस्वीकार का अधिक महत्त्व होता है। नाटक में स्वीकार तत्व के आ जाने से नाटक सशक्त हो जाता है। कोई भी दो चरित्र जब आपस में मिलते हैं तो विचारों के आदान-प्रदान में टकराहट पैदा होना स्वाभाविक है। रंगमंच में कभी भी यथास्थिति को स्वीकार नहीं किया जाता। वर्तमान स्थिति के प्रति असंतुष्टि, छटपटाहट, प्रतिरोध और अस्वीकार जैसे नकारात्मक तत्वों के समावेश से ही नाटक सशक्त बनता है। यही कारण है कि हमारे नाटककारों को राम की अपेक्षा रावण और प्रह्लाद की अपेक्षा हिरण्यकश्यप का चरित्र अधिक आकर्षित करता है। इसके विपरीत जब-जब किसी विचार, व्यवस्था या तात्कालिक समस्या को किसी नाटक में सहज स्वीकार किया गया है, वह नाटक अधिक सशक्त और लोगों के आकर्षण का केंद्र नहीं बन पाया है।
|
88 videos|166 docs|36 tests
|