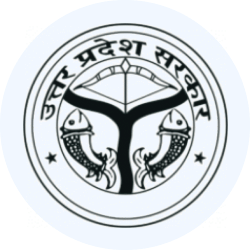संधि और समास | Course for UPPSC Preparation - UPPSC (UP) PDF Download
संधि और समास में अंतर
- संधि:- संधि को दो अक्षरों के मेल से बना विकार कहा जाता है। संधि तोड़ने की क्रिया को संधि-विच्छेद कहते हैं। संधि में वर्णों के योग से वर्ण परिवर्तन हो सकता है। संधि तीन प्रकार की होती है। संधि केवल हिन्दी के तत्सम पदों में होती है। संधि में शब्दों का विभक्ति या लोप नहीं होता है। संधि के लिए, दो वर्णों के संयोजन और विकार की गुंजाइश होती है।
- समास:- समास दो शब्दों के मेल से बना शब्द है। समास को तोड़ने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समास में ऐसा नहीं होता है। समास छह प्रकार का होता है। समास संस्कृत तत्सम, हिन्दी, उर्दू सभी प्रकार के पदों में हो सकता है। समास में शब्दों का विभक्ति हो सकता है। समास के लिए, इस संयोजन या विकार का इससे कोई लेना-देना नहीं होता है।
संधि की परिभाषा
दो या अधिक वर्णों के पास-पास आने के परिणामस्वरूप जो विकार उत्पन्न होता है उसे सन्धि कहते हैं। संधि शब्द सम् + धि से बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ मेल या जोड़ होता है।
जैसे–
- मत + अनुसार = मतानुसार
- अभय + अरण्य = अभयारण्य
- राम + ईश्वर = रामेश्वर
- जगत् + जननी = जगज्जननी
- आशी: + वचन = आशीर्वचन
संधि के प्रकार
संधि के भेद तीन प्रकार होते है-
- स्वर संधि
- व्यंजन संधि
- विसर्ग संधि
स्वर संधि किसे कहते हैं?
किसी स्वर के बाद स्वर आ जाए तो, स्वर के उच्चारण और लेखन में जो परिवर्तन होता है, उसे स्वर संधि (Swar sandhi) कहते हैं।
जैसे-
- कीट + अणु = कीटाणु
- नयन + अभिराम = नयनाभिराम
- हरि + ईश = हरीश
स्वर संधि के भेद
स्वर संधि के पाँच भेद हैं–
- दीर्घ स्वर संधि
यदि किसी स्वर को उसके सजातीय स्वर के साथ जोड़ दिया जाए, तो जो स्वर बनेगा वह दीर्घ स्वर होगा।
अ/आ + अ/आ = आ
इ/ई + इ/ई = ई
उ/ऊ + उ/ऊ= ऊ
राम + अयन रामायण
धर्म + अर्थ धर्मार्थ - गुण स्वर संधि
अ/आ + इ/ई = ए
अ/आ + उ/ऊ = ओ
अ/आ + ऋ = अर् - वृद्धि स्वर संधि
जब ‘अ’, ‘आ’ स्वर के साथ ‘ए’, ‘ऐ’ स्वर मिलते हैं तो 'ऐ' स्वर बनता है और ‘अ’ एवं ‘आ’ स्वरों के साथ 'ओ' और 'औ' स्वर मिलते हैं तो ‘औ’ स्वर बनता है, इसे 'वृद्धि संधि' कहते हैं।
अ/आ + ए/ऐ = ऐ
अ/आ + ओ/औ = औ
परम + ओषधि परमौषधि अ + ओ = औ
जल + ओघ जलौघ अ + ओ = औ - यण् स्वर संधि
'इ, ई, उ, ऊ, ऋ' स्वर से पहले कोई भिन्न स्वर आता है, फिर वह ये 'य, व, र, ल्' में बदल जाता है, इस परिवर्तन को 'यण संधि' कहते हैं।
इ/ई/उ/ऊ/ऋ + असमान स्वर = य्, व्, र्
अधि + आदेश अध्यादेश इ + आ = या
अति + अन्त अत्यन्त इ + अ = य - अयादि स्वर संधि
जब 'ए', 'ऐ', 'ओ' और 'औ' के साथ कोई अन्य स्वर आता है, तो 'ए' का 'अय्', 'ऐ' का 'आय्', 'ओ' का 'अव्' और 'औ' का 'आव्' बन जाता है।
एच् + असमान स्वर
ए/ऐ/ओ/औ + असमान स्वर = अय्, आय्, अव्, आव्
ने + अनम् = नयनम्
व्यंजन संधि किसे कहते हैं?
किसी स्वर के बाद व्यंजन आ जाए या व्यंजन के बाद स्वर आ जाए, व्यंजन के बाद व्यंजन ही आ जाए, तो व्यंजन के उच्चारण और लेखन में जो परिवर्तन होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं।
जैसे–
- तरु + छाया = तरुच्छाया
- वाक् + ईश = वागीश
- उत् + घोष = उद्घोष
विसर्ग संधि किसे कहते हैं?
किसी विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आ जाए तो विसर्ग के उच्चारण और लेखन में जो परिवर्तन होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं।
जैसे–
- सर: + वर = सरोवर
विसर्ग संधि के भेद
- उत्व विसर्ग संधि
- रुत्व विसर्ग संधि
- सत्व विसर्ग संधि
संधि विच्छेद के उदाहरण
- उद्धत – उत् + हत (व्यंजन सन्धि)
- कंठोष्ठ्य – कंठ + ओष्ठ्य (गुण सन्धि)
- अन्वय – अनु + अय (यण् सन्धि)
- किंचित् – किम् + चित् (व्यंजन सन्धि)
- घनानंद – घन + आनन्द (दीर्घ सन्धि)
- एकैक – एक + एक (वृद्धि सन्धि)
- अधीश्वर – अधि + ईश्वर (दीर्घ सन्धि)
- अभ्यागत – अभि + आगत (यण् सन्धि)
- उच्छ्वास – उत् + श्वास (व्यंजन सन्धि)
- जगद्बन्धु – जगत् + बन्धु (व्यंजन सन्धि)
- तपोवन – तपः + वन (विसर्ग सन्धि)
- अब्ज – अप् + ज (व्यंजन सन्धि)
- दृष्टान्त – दृष्ट + अंत (दीर्घ सन्धि)
- दुर्बल – दुः + बल (विसर्ग सन्धि)
- तल्लय – तत् + लय (व्यंजन सन्धि)
समास क्या है?
समास का अर्थ है ‘संक्षिप्तीकरण’। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक सार्थक शब्द को समास कहते हैं। इस विधि से बने शब्दों का समस्त-पद कहते हैं। जब समस्त-पदों को अलग-अलग किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को समास-विग्रह कहते हैं।
समास के भेद
समास के 6 भेद होते है, जो इस प्रकार है-
- अव्ययीभाव समास
- तत्पुरुष समास
- द्विगु समास
- द्वन्द्व समास
- कर्मधारय समास
- बहुव्रीहि समास
अव्ययीभाव समास
इसमें दोनों शब्दों में से पहले होने वाला शब्द कोई अव्यय होता है और उसके बाद का शब्द वास्तविकता में प्रयोग होता है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं।
जैसे-
- आजीवन – जीवन-भर
- यथासामर्थ्य – सामर्थ्य के अनुसार
- यथाशक्ति – शक्ति के अनुसार
- यथाविधि- विधि के अनुसार
- यथाक्रम – क्रम के अनुसार
- भरपेट- पेट भरकर
- हररोज़ – रोज़-रोज़
- हाथोंहाथ – हाथ ही हाथ में
- रातोंरात – रात ही रात में
तत्पुरुष समास
तत्पुरुष समास में उत्तरपद प्रधान होता है, पूर्वपद अप्रधान होता है। इसी के साथ दोनों पदों के मध्य में कारक का लोप रहता है, तो इस प्रकार के समास को तत्पुरुष समास तत्पुरुष समास (Tatpurush samas) कहते हैं। तत्पुरुष समास में विशेषणीय पद और मुख्य पद का संबंध एक निश्चित भावना को प्रकट करता है।
जैसे-
तुलसीदासकृत- तुलसीदास द्वारा कृत (रचित)
तत्पुरुष समास के 6 भेद होते है, जो इस प्रकार है-
- कर्म तत्पुरुष
- करण तत्पुरुष
- संप्रदान तत्पुरुष
- अपादान तत्पुरुष
- संबंध तत्पुरुष
- अधिकरण तत्पुरुष
- कर्म तत्पुरुष समास
कर्म तत्पुरुष समास ‘को’ चिन्ह के लोप से बनता है।
जैसे-
बसचालक - बस को चलाने वाला
गगनचुंबी - गगन को चूमने वाला - करण तत्पुरुष समास-
करण तत्पुरुष समास ‘से’ और ‘के द्वारा’ के लोप से बनता है।
जैसे-
मदांध - मद से अंध
रेखांकित - रेखा द्वारा अंकित - सम्प्रदान तत्पुरुष समास-
सम्प्रदान तत्पुरुष समास ‘के लिए’ के लोप से बनता है।
जैसे-
हथकड़ी - हाथ के लिए कड़ी - अपादान तत्पुरुष समास-
अपादान तत्पुरुष समास ‘से’ के लोप से बनता है।
जैसे-
पथभ्रष्ट- पथ से भ्रष्ट
ऋणमुक्त - ऋण से मुक्त - सम्बन्ध तत्पुरुष समास-
सम्बन्ध तत्पुरुष समास ‘का’, ‘के’ व ‘की’ के लोप से बनता है।
जैसे-
घुड़दौड़ - घोंडों की दौड़
पूँजीपति - पूँजी का मालिक - अधिकरण तत्पुरुष समास-
अधिकरण तत्पुरुष समास ‘में’ और ‘पर’ के लोप से बनता है।
जैसे-
शरणागत - शरण में आगत
आत्मविश्वास - आत्मा पर विश्वास
कर्मधारय समास
इसमें दो शब्दों में से पहले शब्द का अर्थ एक विशेष गुण से लिया जाता है, इसे कर्मधारय समास कहा जाता है।
जैसे –
- चंद्रमुख- चंद्र जैसा मुख
- कमलनयन- कमल के समान नयन
- देहलता- देह रूपी लता
- दहीबड़ा- दही में डूबा बड़ा
- नीलकमल- नीला कमल
- पीतांबर- पीला अंबर (वस्त्र)
द्विगु समास
इसमें पूर्वपद संख्या वचक है, उत्तरपद प्रधान हो, तो द्विगु समास (Digu samas) कहते हैं। इसको विग्रह करने पर संख्या का बोध होता है।
जैसे –
- नवग्रह- नौ ग्रहों का समूह
- दोपहर- दो पहरों का समाहार
- त्रिलोक- तीन लोकों का समाहार
- चौमासा- चार मासों का समूह
द्वन्द्व समास
इसमें दो शब्दों का संयुक्त रूप बनता है, जिनमें से प्रत्येक स्वतंत्र होता है, वह द्वंद्व समास कहलाता है।
जैसे-
- पाप-पुण्य- पाप और पुण्य
- अन्न-जल- अन्न और जल
- सीता-राम- सीता और राम
- खरा-खोटा- खरा और खोटा
बहुव्रीहि समास
इसमें दो शब्दों में से पहले शब्द प्रयोज्य संख्या के रूप में प्रयोग होता है और उसके बाद का शब्द उसी शब्द के लिए प्रयुक्त होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं।
जैसे –
- दशानन- दश है आनन जिसके- रावण
- नीलकंठ- नीला है कंठ जिसका- शिव
- पीतांबर- पीला है अम्बर जिसका- श्रीकृष्ण
|
114 videos|362 docs|105 tests
|
FAQs on संधि और समास - Course for UPPSC Preparation - UPPSC (UP)
| 1. संधि क्या होती है? |  |
| 2. संधि के कितने प्रकार होते हैं? |  |
| 3. समास क्या होता है? |  |
| 4. समास के कितने प्रकार होते हैं? |  |
| 5. संधि और समास का महत्व क्या है? |  |