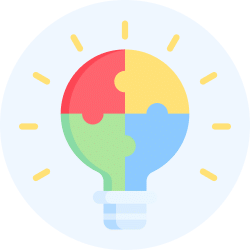Short Question Answers (Passage Based) - वाख | Hindi Class 9 (Kritika and Kshitij) PDF Download
1. निम्नलिखित काव्यांशों को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिये-
रस्सी कच्चे धागे की, खींच रही मैं नाव।
जाने कब सुन मेरी पुकार करें देव भवसागर पार।
पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे।
जी में उठती रह-रह हूक, घर जाने की चाह है घेरे।
प्रश्न (i): ‘रस्सी कच्चे धागे की’ तथा ‘नाव’ में निहित अर्थ स्पष्ट कीजिए।
उत्तर: ‘रस्सी कच्चे धागे की’ का अर्थ कमज़ोर और नाशवान रूपी रस्सी साँस से है जो हर समय चल तो रही है, पर पता नहीं कब तक वह चलेगी। ‘नाव’ शब्द का अर्थ जीवन रूपी नौका से है।
प्रश्न (ii): कवयित्री के हृदय से बार-बार हूक क्यों उत्पन्न होती है?
उत्तर: कवयित्री हर क्षण ईश्वर से एक ही प्रार्थना करती है कि वह परमात्मा की शरण प्राप्त कर इस जीवन को त्याग दे, पर ऐसा हो नहीं रहा।
प्रश्न (iii): कवयित्री किस ‘घर’ में जाना चाहती है?
उत्तर: कवयित्री परमात्मा के पास जाना चाहती है। यह संसार उसका घर नहीं है। उसका घर तो वह है जहाँ परमात्मा है। कवयित्री ने अपने रहस्यवादी वाख में परमात्मा की शरण प्राप्त करने की कामना की है। वह भवसागर को पार कर जाना चाहती है पर ऐसा संभव नहीं हो पा रहा।
प्रश्न (iv): वाख में निहित काव्य-सौंदर्य को प्रतिपादित कीजिए।
उत्तर: कश्मीरी से अनूदित वाख में तत्सम शब्दावली की अधिकता है। लयात्मकता का गुण विद्यमान है। शांत रस और प्रसाद गुण ने कथन को सरसता प्रदान की है। पुनरुक्ति, प्रकाश, रूपक, प्रश्न और अनुप्रास अलंकारों का सहज प्रयोग सराहनीय है।
प्रश्न (v): पानी टपकने से क्या तात्पर्य है?
उत्तर: ‘पानी टपकने’ से तात्पर्य धीरे-धीरे समय का व्यतीत होना है। प्राणी जान भी नहीं पाता और उसकी आयु समाप्त हो जाती है।
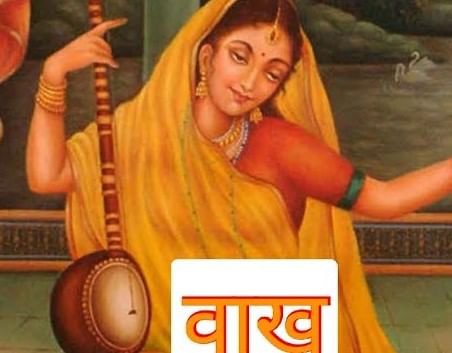
2. निम्नलिखित काव्यांशों को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिये-
खा-खाकर कुछ पाएगा नहीं
न खाकर, बनेगा अहंकारी।
सम खा तभी होगा समभावी,
खुलेगी साँकल बंद द्वार की।
प्रश्न (i): कवयित्री ने ‘न खाकर बनेगा अहंकारी’ कहकर किस तथ्य की ओर संकेत किया है?
उत्तर: कवयित्री ने इस तथ्य की ओर संकेत किया है कि मानव ब्रह्म की प्राप्ति के लिए तरह-तरह के बाह्याडंबर रचते हैं। भूखे रहकर व्रत करते हैं पर इससे उनमें संयमी बनने और अपने शरीर पर नियंत्रण प्राप्त करने का अहंकार मन में आ जाता है।
प्रश्न (ii): ‘सम खा’ से क्या तात्पर्य है?
उत्तर: ‘सम खा’ से तात्पर्य मन का शमन करने से है। इससे अंत: करण और बाह्य इंद्रियों के निग्रह का संबंध है।
प्रश्न (iii): कवयित्री किस द्वार के बंद होने की बात कहती है?
उत्तर: कवयित्री मानव मन के मुक्त न होने तथा उसकी चेतना के संकुचित होने को ‘द्वार के बंद होने से’ संबोधित करती है।
प्रश्न (iv): मनुष्य अहंकारी क्यों बनता है ?
उत्तर: इंद्रियों पर संयम रखने और तपस्या का जीवन जीने से मनुष्य स्वयं को महात्मा और त्यागी मानने लगता है और इससे वह अहंकारी बनता है।
प्रश्न (v): कवयित्री क्या प्रेरणा देना चाहती है ?
उत्तर: कवयित्री प्रेरणा देना चाहती है कि मानव को अपने जीवन में सहजता बनाए रखनी चाहिए। संयम का भाव श्रेष्ठ हो जाता है और इसी से वह ईश्वर की ओर उन्मुख हो सकता है।
3. निम्नलिखित काव्यांशों को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिये-
आई सीधी राह से, गई न सीधी राह।
सुषुम-सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह!
जेब टटोली, कौड़ी न पाई।
माझी को दूँ, क्या उतराई?
प्रश्न (i): ‘माझी’ और ‘उतराई’ क्या है?
उत्तर: ‘माझी’ ईश्वर है; गुरु है जिसने इस संसार में जीवन दिया था और जीने की राह दिखाई थी। ‘उतराई’ सत्कर्म रूपी मेहनताना है जो संसार को त्यागते समय मुझे माझी रूपी ईश्वर को देना होगा।
प्रश्न (ii): कवयित्री को जेब टटोलने पर कौड़ी भी क्यों न मिली?
उत्तर: कवयित्री ने माना है कि उसने कभी आत्मालोचन नहीं किया; सत्कर्म नहीं किए। केवल मोह-माया के संसार में उलझी रही इसलिए अब उसके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसकी मुक्ति का आधार बन सके।
प्रश्न (iii): ‘गई न सीधी राह’ से क्या तात्पर्य है ?
उत्तर: ‘गई न सीधी राह’ से तात्पर्य है कि संसार के मायात्मक बंधनों ने मुझे अपने बस में कर लिया और मैं चाहकर भी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भक्ति मार्ग पर नहीं बढ़ी। मैंने सत्कर्म नहीं किया और दुनियादारी में उलझी रही।
प्रश्न (iv): ‘सुषुम-सेतु’ क्या है ?
उत्तर: हठयोगी सुषुन्ना नाड़ी के माध्यम से कुंडलिनी जागृत कर परमात्मा को पाने की योग साधना करते हैं। ‘सुषुम-सेतु’ सुषुन्ना नाड़ी की साधना को कहते हैं।
प्रश्न (v): कवयित्री का दिन कैसे व्यतीत हो गया ?
उत्तर: कवयित्री ने अपना दिन (जागृत अवस्था) व्यर्थ की हठयोग-साधना में व्यतीत कर दिया।
4. निम्नलिखित काव्यांशों को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिये-
थल-थल में बसता है शिव ही,
भेद न कर क्या हिंदू-मुसलमां।
ज्ञानी है तो स्वयं को जान,
वही है साहिब से पहचान।।
प्रश्न (i): कवयित्री के द्वारा परमात्मा के लिए ‘शिव’ प्रयुक्त किए जाने का मूल आधार क्या है?
उत्तर: कवयित्री शैव मत से संबंधित शैव यौगिनी थी। उसके चिंतन का आधार शैव दर्शन था, इसलिए उसने परमात्मा के लिए ‘शिव’ प्रयुक्त किया है।
प्रश्न (ii): ‘भेद न कर क्या हिंदू-मुसलमां’ में निहित अर्थ स्पष्ट कीजिए।
उत्तर: परमात्मा सभी के लिए एक ही है। चाहे हिंदू हों या मुसलमान- उनके लिए परमात्मा के स्वरूप के प्रति कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उपदेशात्मक स्वर में यही स्पष्ट किया गया है कि धर्म के नाम पर परमात्मा के प्रति आस्था नहीं बदलनी चाहिए।
प्रश्न (iii): ईश्वर वास्तव में कहाँ है?
उत्तर: ईश्वर वास्तव में संसार के कण-कण में समाया हुआ है। वह तो हर प्राणी के शरीर के भीतर भी है, इसलिए उसे कहीं बाहर ढूँढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसे तो अपने भीतर से ही पाने की कोशिश की जानी चाहिए।
प्रश्न (iv): ईश्वर की पहचान कैसे हो सकती है?
उत्तर: ईश्वर की पहचान अपनी आत्मा को पहचानने से संभव हो सकती है। आत्मज्ञान ही उसकी प्राप्ति का एकमात्र रास्ता है।
प्रश्न (v): कवयित्री सांप्रदायिक भेद-भाव को दूर किस प्रकार करती है ?
उत्तर: कवयित्री सर्वकल्याण के भाव से सांप्रदायिक भेद-भाव को दूर करती है। उसके अनुसार हिंदू-मुसलमान दोनों शिव आराधना से आपसी दूरियाँ मिटा सकते हैं।
यहाँ पढ़ें: पठन सामग्री और व्याख्या - वाख
पाठ के NCERT Solutions को यहाँ देखें।
|
16 videos|226 docs|43 tests
|
FAQs on Short Question Answers (Passage Based) - वाख - Hindi Class 9 (Kritika and Kshitij)
| 1. What is the meaning of the word "वाख"? |  |
| 2. Who is Lal Ded and why is she important in Kashmiri literature? |  |
| 3. What are some common themes found in Kashmiri poetry? |  |
| 4. What is the significance of oral tradition in Kashmiri poetry? |  |
| 5. What are some notable Kashmiri poets and their contributions to Kashmiri literature? |  |