नोट्स: जीवन यापन करना | सामाजिक अध्ययन और शिक्षाशास्त्र (SST) CTET & TET Paper 2 - CTET & State TET PDF Download
जीविका किसी भी देश में सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियों में से एक है। भारत जैसे विकासशील अर्थव्यवस्था में, कृषि देश के जीडीपी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। यह आर्थिक गतिविधियों, पैसे के प्रवाह को बढ़ाता है और अर्थव्यवस्था में रोजगार उत्पन्न करता है।
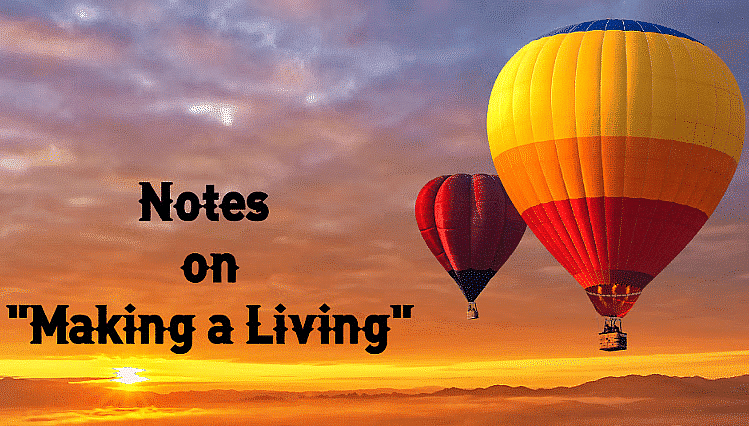
- भारत एक कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था है। हमारी लगभग 60% जनसंख्या कृषि क्षेत्र या उससे संबंधित क्षेत्रों जैसे मछली पकड़ने, वनों की कटाई, मुर्गी पालन, या पशुपालन में कार्यरत है।
- हमारी ग्रामीण जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा कृषि पर अत्यधिक निर्भर है।
जनसंख्या और अर्थशास्त्र के आधार पर, भारतीय समाज में जीविकाएँ दो प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित की जा सकती हैं:
(i) ग्रामीण जीविका
(ii) शहरी जीविका
- ग्रामीण जीविका भारतीय अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख हिस्सा है। यह न केवल सबसे बड़ा क्षेत्र है बल्कि देश की अधिकांश जनसंख्या को भी समाहित करता है।
- हालांकि, अन्य क्षेत्रों की तरह, इस क्षेत्र की भी अपनी समस्याएँ और कमियाँ हैं।
- ग्रामीण जनसंख्या मुख्यतः फसलों से संबंधित गतिविधियों में संलग्न है।
- ग्रामीण क्षेत्र में अन्य गतिविधियों में छोटे पैमाने की उद्योग, हस्तशिल्प और अन्य व्यवसाय शामिल हैं।
आइए हम तमिलनाडु के कल्पट्टू गाँव से एक छोटा सा उदाहरण लें, जो समुद्र तट के करीब है।
- कृषि के अलावा, गाँव वाले छोटे उद्योगों में शामिल हैं जैसे कि टोकरी, बर्तन, ईंटें, बैलगाड़ी आदि बनाना।
- गाँव में आवश्यक सेवाएँ प्रदान करने वाले पेशेवर जैसे कि लोहार, नर्स, शिक्षक, धोबी, मैकेनिक आदि भी उपस्थित हैं।
- सुबह के समय इडली, डोसा, और उपमा जैसे भोजन प्रदान करने वाले लोग भी हैं।
- हर भौगोलिक क्षेत्र की अपनी फसलें होती हैं, इस गाँव में मुख्य फसल धान है।
- गाँव के अधिकांश परिवार अपनी जीविका कृषि के माध्यम से अर्जित करते हैं।
गरीब और भूमिहीन श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर हर दिन बहुत सारा समय जंगल से लकड़ी इकट्ठा करने, पानी लाने, और अपने मवेशियों को चरााने में बिताते हैं।
- इन गतिविधियों से श्रमिकों को कोई पैसा नहीं मिलता लेकिन वे इसे अपने घर के लिए करते हैं।
- परिवार को इस तरह का काम करने में समय बिताना पड़ता है क्योंकि वे जो थोड़ी सी धनराशि कमाते हैं, उससे गुजारा नहीं हो पाता।
हमारे देश में लगभग दो-पाँचवे ग्रामीण परिवार कृषि श्रमिक हैं।
- कुछ छोटे भूखंडों के मालिक होते हैं, जबकि अन्य अभी भी भूमिहीन हैं।
- कठिनाई और चिकित्सा आपात स्थितियों के समय, भूमिहीन परिवारों को गाँव के सुदी से पैसे उधार लेने पड़ते हैं।
- सुदी उनकी स्थिति का अनुचित लाभ उठाते हैं और उन्हें अपने स्वार्थ के लिए शोषित करते हैं।
- कभी-कभी, गाँव वालों को अपने मवेशियों को बेचकर अपने ऋण चुकाने पड़ते हैं।
चूंकि फसलें एक विशेष मौसम में उगाई जाती हैं, भूमिहीन परिवार पूरे वर्ष पैसे नहीं कमा पाते।
- अक्सर, उन्हें काम की तलाश में लंबी यात्रा करनी पड़ती है।
- यह यात्रा या प्रवास विशेष मौसम के दौरान होता है जब उन्हें कृषि क्षेत्र में कोई काम नहीं मिलता।
ऋण में होना
यह अक्सर कहा जाता है कि भारतीय कृषि एक जुआ है। आप कमाएँ या नहीं, यह प्रकृति द्वारा तय किया जाता है। कई बार, जब बारिश पर्याप्त नहीं होती, फसलें भी बर्बाद हो सकती हैं। इसके परिणामस्वरूप, किसान अपने ऋण का भुगतान करने में असमर्थ हो जाते हैं। उन्हें अपने परिवारों के जीवनयापन के लिए पैसे उधार लेने पड़ सकते हैं। जल्द ही, ऋण इतना बड़ा हो जाता है कि चाहे वे कितना भी कमाएँ, वे चुकता नहीं कर पाते और भारतीय किसानों की दयनीय स्थिति बनी रहती है।
उपरोक्त विवरण के आधार पर, हम देखते हैं कि भारत में किसानों की तीन श्रेणियाँ हैं, जिन्हें नीचे समझाया गया है:
- भूमिहीन श्रमिक: इस श्रेणी के किसान भारत की कुल कृषि जनसंख्या का 20% बनाते हैं। वे जीविका कमाने के लिए दूसरों के खेतों में काम करने पर निर्भर होते हैं। इनमें से कई भूमि रहित होते हैं और अन्य के पास बहुत छोटे भूखंड हो सकते हैं।
- छोटे किसान: छोटे किसानों के मामले में, भूमि उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बमुश्किल पर्याप्त होती है। भारत में, 80% किसान इस समूह में आते हैं। वे बहुत कठिन और असुरक्षित जीवन जीते हैं।
- बड़े किसान: बड़े किसान शेष 20% हैं, जो भारत की कृषि वर्ग का निर्माण करते हैं। वे गाँवों में अधिकांश भूमि की खेती करते हैं। उनके उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बाजार में बेचा जाता है। उनमें से कई ने दुकानें, उधारी, व्यापार, छोटे कारखाने आदि जैसे अन्य व्यवसाय शुरू किए हैं।
इसलिए, यह समझा जा सकता है कि देश के अधिकांश किसान काफी गरीब हैं।
ग्रामीण आजीविका: हमने चर्चा की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग विभिन्न तरीकों से अपनी आजीविका कैसे कमाते हैं। कुछ खेतों पर काम करते हैं, जबकि अन्य गैर-कृषि गतिविधियों में जीविका कमाते हैं। खेतों पर काम करने में खरपतवार निकालना और फसल की कटाई जैसी प्रक्रियाएँ शामिल हैं। इसलिए, भारतीय गाँवों में जीवन कृषि के चारों ओर घूमता है। अन्य क्षेत्र उभर रहे हैं लेकिन कृषि ग्रामीण भारत में प्रमुख आजीविका बनी हुई है।
शहरी जीवनयापन आर्थिक गतिविधियों के बढ़ने के साथ, शहरीकरण की व्यापक आवश्यकता है। 1990 के दशक की शुरुआत में उदारीकरण के आगमन के साथ, भारत ने शहरी क्षेत्रों और औद्योगिकीकरण को तेजी से बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की। इसलिए, पिछले 25 वर्षों में, देश के विभिन्न हिस्सों में शहरीकरण कई गुना बढ़ गया है।
शहरी क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए, हमें निम्नलिखित बिंदुओं को समझना होगा:
प्रवासी
कई लोग काम की तलाश में गाँवों से शहरों और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में प्रवासित हुए हैं। यह श्रेणी बड़े कारखानों और अन्य व्यवसायों में कार्यरत श्रमिक वर्ग का अधिकांश हिस्सा बनाती है।
- इनमें से कुछ लोग शहर की जीवन शैली में विभिन्न छोटे सेवाएं प्रदान करते हैं। इनमें विक्रेता, रिक्शा चालक, नाई, मोची, और शहर में अन्य छोटे श्रमिक शामिल हैं। वे अपने आप पर काम करते हैं और किसी के द्वारा नियोजित नहीं होते हैं, इसलिए, उन्हें अपने काम का आयोजन स्वयं करना होता है। उन्हें यह योजना बनानी होती है कि कितनी खरीदारी करनी है, साथ ही अपनी दुकानों को कहाँ और कैसे स्थापित करना है।
- उनकी दुकानें आमतौर पर अस्थायी संरचनाएँ होती हैं; कभी-कभी, बस बोर्ड या कागजों को फेंके गए बक्सों पर फैलाया जाता है या कुछ खंभों पर एक कैनवास की चादर लटकाई जाती है।
- शहर के कुछ हिस्सों में फेरीवालों का प्रवेश निषेध है। यह एक बड़ी अस्पष्टता है और शहरी जीवन के वर्गीय चरित्र को भी दर्शाती है।
- विक्रेता ऐसे सामान बेचते हैं जो अक्सर उनके परिवारों द्वारा घर पर तैयार किए जाते हैं, जो उन्हें खरीदते, साफ करते, छांटते और बेचने के लिए तैयार करते हैं। इनमें वे लोग शामिल हैं जो सड़कों पर खाना या नाश्ता बेचते हैं, जिन्हें अधिकांशतः घर पर ही तैयार किया जाता है।
- देश में लगभग एक करोड़ सड़क विक्रेता हैं जो शहरी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। सड़क विक्रय को पहले यातायात और पैदल चलने वालों के लिए एक बाधा के रूप में देखा जाता था। हालाँकि, कई संगठनों के प्रयासों के साथ, इसे अब एक सामान्य लाभ और लोगों को जीवनयापन कमाने के अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है।
व्यापारी
- व्यवसायी शहरी अर्थव्यवस्था की दूसरी महत्वपूर्ण श्रेणी हैं। शहर में कई लोग विभिन्न बाजारों में दुकानों के मालिक हैं। ये दुकानें छोटी या बड़ी हो सकती हैं और विभिन्न वस्तुओं को बेचती हैं। अधिकांश व्यवसायी अपनी ही दुकानों या व्यवसायों का प्रबंधन करते हैं। वे किसी के लिए काम नहीं करते, बल्कि वे कई अन्य श्रमिकों को पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करते हैं। ये स्थायी दुकानें हैं जिन्हें नगर निगम द्वारा व्यापार करने के लिए लाइसेंस दिया गया है।
कारखाना-कार्यशाला क्षेत्र
- शहरी अर्थव्यवस्था में तीसरी महत्वपूर्ण श्रेणी कारखाना जैसे कार्य हैं। शहर में बड़ी संख्या में लोग अस्थायी श्रमिकों या अस्थायी कर्मचारियों के रूप में काम करते हैं। इस प्रकार के कार्यों का कोई स्थायी दर्जा नहीं होता है। काम करने की परिस्थितियाँ, वेतन, और अन्य कार्य-संबंधित लाभ इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को नहीं दिए जाते हैं। इसमें अस्थायी श्रमिक शामिल हो सकते हैं जो पेंटिंग करते हैं या वे लोग जो छोटे कारखानों या वस्त्र इकाइयों में काम करते हैं। यदि श्रमिक अपने वेतन या कार्य की परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं, तो उनसे छोड़ने के लिए कहा जाता है। यहाँ नौकरी की सुरक्षा या संरक्षण नहीं है यदि उन्हें गलत तरीके से व्यवहार किया जाए। उनसे बहुत लंबे घंटे काम करने की अपेक्षा की जाती है।
कार्यालय क्षेत्र में
- शहरी अर्थव्यवस्था के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्यालय-संबंधित कार्य शामिल हैं। ये कार्य स्थायी दर्जा रखते हैं। किसी संगठन के सभी नियमित कर्मचारियों को हर महीने नियमित वेतन मिलता है। ये कार्य लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। वेतन के अलावा, इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को अन्य लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे:
1. बुढ़ापे के लिए बचत
2. छुट्टियाँ
3. परिवार के लिए चिकित्सा सुविधाएँ
शहर में कई श्रमिक हैं जो कार्यालयों, कारखानों और सरकारी विभागों में नियमित और स्थायी श्रमिक के रूप में काम करते हैं। वे नियमित रूप से उसी कार्यालय या कारखाने में जाते हैं। उनके काम की स्पष्ट पहचान होती है और उन्हें नियमित वेतन मिलता है। आकस्मिक श्रमिकों के विपरीत, उन्हें नहीं कहा जाएगा कि वे चले जाएँ यदि कारखाने में काम कम है। हमने शहरों में लोगों द्वारा की जाने वाली विभिन्न आर्थिक गतिविधियों पर चर्चा की है। यह ध्यान देने योग्य है कि कई लोग शहरों में विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। वे शायद कभी भी एक-दूसरे से नहीं मिले होंगे, लेकिन उनका काम उन्हें एक साथ बांधता है और उन्हें शहरी जीवन का हिस्सा बनाता है।
बाजारों को समझना
क्या हम अपने जीवन को बाजार से अलग कर सकते हैं? निश्चित रूप से नहीं। हमें कई आइटम खरीदने के लिए बाजार जाना पड़ता है चाहे वे कम उपयोग में आएं या रोजमर्रा के जीवन में। हम खाद्य पदार्थ, कपड़े, दवाएँ, कारें, आदि खरीदते हैं। यहाँ साप्ताहिक बाजार, सड़क पर ठेलों वाले, स्थायी दुकानें, स्थानीय बाज़ार, मॉल आदि होते हैं। इन बाजारों का हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
- किसी भी बाजार का मुख्य उद्देश्य लोगों के लिए चीजें उपलब्ध कराना और लाभ कमाना है। एक बाजार को एकल इकाई के रूप में नहीं समझा जा सकता, बल्कि हमें इसे एक सामूहिक एजेंसी के रूप में समझना चाहिए, जैसे एक दुकान मॉल नहीं है, एक दुकान एक दुकान है और न ही यह पूर्ण अर्थ में बाजार है।
- साप्ताहिक बाजार में, लोग कुछ घंटों के लिए दुकानें लगाते हैं और फिर स्थान खाली कर देते हैं। यह प्रक्रिया हर हफ्ते होती है; इसलिए, इसे साप्ताहिक बाजार कहा जाता है। ये बाजार उस दिन के नाम से जाने जाते हैं जिस दिन वे लगते हैं, जैसे बुधवार बाजार, शुक्रवार बाजार, आदि। कई बाजारों को एक स्थान पर विभिन्न दिनों में लगाया जा सकता है। ये बाजार रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए सामान खरीदने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यहाँ से कोई मोलभाव कर सकता है और सस्ते सामान प्राप्त कर सकता है। ऐसे बाजारों के लिए न तो बड़े निवेश की आवश्यकता होती है और न ही लोगों को रोजगार देने की। कोई अपने परिवार के सदस्यों की मदद से इन बाजारों में अपनी दुकान लगा सकता है।
- ऐसे बाजारों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यहाँ सभी आवश्यक वस्तुएँ एक ही स्थान पर मिल सकती हैं। दूसरी ओर, कई पड़ोसी दुकानें स्थायी होती हैं। ये दुकानें भी एक या दो लोगों द्वारा चलाई जाती हैं और आसपास रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। ये दुकानदार अन्य बाजारों से सामान खरीदते हैं और अपनी दुकानों पर बेचते हैं ताकि लोग आसानी से बिना किसी परेशानी के आवश्यक वस्तुएँ प्राप्त कर सकें। ऐसे दुकानों से दूध, किराने का सामान, स्टेशनरी, दवाएँ आदि खरीदी जा सकती हैं। स्टेशनरी या किराने के लिए विशिष्ट दुकान हो सकती है या सामान्य स्टोर हो सकते हैं जो सभी चीजें एक ही दुकान में रखते हैं। ये स्थायी या सड़क के किनारे स्टॉल हो सकते हैं।
- एक मॉल एक बड़ा स्थान है जिसमें विभिन्न दुकानों या ब्रांडों का एक छत के नीचे समावेश होता है। ये बहु-स्तरीय इमारतें होती हैं जहाँ विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए फर्श विभाजित होते हैं, जैसे एक फर्श खाद्य पदार्थों के लिए, दूसरा पुरुषों के वस्त्रों के लिए, एक महिलाओं के वस्त्रों के लिए, आदि। इन्हें यादृच्छिक रूप से भी व्यवस्थित किया जा सकता है। मॉल चीजें अपेक्षाकृत महंगे दाम पर बेचते हैं। भारत में एक शक्तिशाली ब्रांड संस्कृति लोकप्रिय हो गई है। मॉल ने इस संस्कृति को बढ़ावा देने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस ब्रांड संस्कृति ने भारत में पश्चिमी जीवन शैली को भी लोकप्रिय बनाया है।
यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि थोक बाजार अन्य बाजारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लोग थोक बाजार से सामान खरीदते हैं और उन्हें अपनी दुकानों, साप्ताहिक बाजारों या मॉल में बेचते हैं। हालांकि, थोक बाजारों से खरीदने के लिए एक बड़ी मात्रा में खरीदना आवश्यक है।
समानता और बाजार को समझना
- इस अध्याय में विभिन्न प्रकार के बाजारों पर चर्चा की गई है। हालांकि, इन बाजारों को केवल एक ऐसे स्थान के रूप में नहीं देखा जा सकता जहाँ लोग सामान खरीदते हैं, बल्कि इन्होंने समाज में विशिष्ट प्रकार के विभाजन भी उत्पन्न किए हैं, जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, बल्कि हमें मॉल जाने वाली जनसंख्या और मॉल जाने के कारण के संदर्भ में स्थिति का विश्लेषण करना होगा।
- यह भी समझना आवश्यक है कि मध्यवर्ग और निम्नवर्ग का एक व्यक्ति मॉल से सामान खरीदने में असमर्थ है, परंतु समाज ने एक ऐसा विचार प्रक्रिया विकसित की है जहाँ उच्च वर्ग और निम्न वर्ग का निर्धारण बाजार द्वारा किया जाता है। यदि हम मॉल में काम करने वाले व्यक्ति का उदाहरण लेते हैं, तो वह मॉल से सामान नहीं खरीद सकता क्योंकि उसकी सैलरी ऐसा करने की अनुमति नहीं देती। फिर भी, वह लोगों का अवलोकन करता है और इससे एक प्रकार की इच्छा उत्पन्न होती है, जो शायद आवश्यक नहीं है, और उनके जीवन में समस्याएँ पैदा करती है।
- विज्ञापन व्यक्तियों की मनोवृत्ति को प्रभावित करते हैं और विभिन्न समस्याओं का कारण बनते हैं। ऐसे कई बाजारों की समस्याएँ हैं जो समाज में समस्याएँ उत्पन्न करती हैं। इसलिए, हम अर्थशास्त्र को सामाजिक जीवन से अलग नहीं कर सकते।
|
64 videos|68 docs|78 tests
|
















