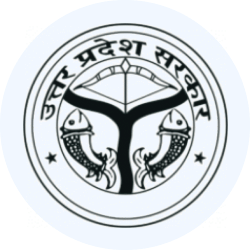वैश्वीकरण की आड़ में संरक्षणवाद | Course for UPPSC Preparation - UPPSC (UP) PDF Download
वैश्वीकरण का आशय विश्व अर्थव्यवस्था में खुलापन, बढ़ती आत्मनिर्भरता तथा आर्थिक एकीकरण के विस्तार से लगाया जाता है। वैश्वीकरण के तहत विश्व बाज़ारों के मध्य पारस्परिक निर्भरता की स्थिति उत्पन्न होती है तथा देश की सीमाओं को पार करते हुए व्यवसायों का स्वरूप विश्वव्यापी हो जाता है। वैश्वीकरण के तहत ऐसे प्रयास किये जाते हैं कि विश्व के सभी देश व्यवसाय एवं उद्योग के क्षेत्र में एक-दूसरे के साथ सहयोग एवं समन्वय स्थापित कर सकें। परंतु वर्तमान समय में वैश्वीकरण के प्रयासों के मध्य संरक्षणवाद ने पनाह ले ली है। संयुक्त राज्य अमेरिका जो स्वंय को वैश्वीकरण का पैरोकार कहता था, आज संरक्षणवादी नीतियों को प्रश्रय देने लगा है। यह बात सोचने वाली है कि एक समय तक वैश्वीकरण का नेतृत्व करने वाला देश अचानक से संरक्षणवादी नीतियों को प्रश्रय क्यों देने लगा है। अमेरिका का यह झुकाव क्या सिर्फ राष्ट्रवाद है या फिर वर्तमान में स्वतंत्र व्यापार का स्वरूप विकृत होने लगा है? क्या स्वतंत्र व्यापार में आई कमियों को सिर्फ संरक्षणवाद से ही दूर किया जा सकता है?
गौरतलब है कि वैश्वीकरण एवं संरक्षणवाद एक-दूसरे की विपरीत अवधारणाएँ हैं। वैश्वीकरण स्वतंत्र व्यापार पर आधारित होता है, जहाँ पर बिना किसी भेदभाव के वस्तुओं एवं सेवाओं का स्वतंत्र व्यापार होता है। परंतु इसके विपरीत संरक्षणवादी नीति में विदेशी उत्पादों के साथ भेदभाव कर उनकी कीमतों या मात्रा आदि को दुष्प्रभावित किया जाता है।
इसकी वजह विदेशी उत्पादों की प्रतिस्पर्द्धात्मकता में कमी एवं उनके बदले स्वदेशी उत्पादों की मांग में वृद्धि करनी होती है।
इस प्रकार सरकारें घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्द्धा से सुरक्षा प्रदान करती है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में संरक्षण के अनेक तरीके प्रचलन में हैं। संरक्षण का प्रथम तरीका है विदेशी उत्पादों पर आयात शुल्क में वृद्धि करना। हम देखते है कि आयात शुल्क बढ़ जाने से विदेशी उत्पाद, घरेलू उत्पादों की तुलना में कम प्रतिस्पर्द्धी हो जाते हैं तथा उनकी मांग कम हो जाती है। संरक्षण का दूसरा तरीका है कोटा निर्धारण। इसके तहत सरकार आयातित वस्तुओं की अधिकतम मात्रा का निर्धारण करती है एवं इस निर्धारित मात्रा से अधिक वस्तुओं का देश में आगमन प्रतिबंधित हो जाता है। इस प्रकार घरेलू उद्योग उन वस्तुओं की प्रतिस्पर्द्धा से बच जाते हैं। संरक्षण का तीसरा तरीका घरेलू उत्पादों को सहायता देकर उनकी कीमतों में कमी लाना है। इससे इन उत्पादों की कीमत विदेशी उत्पादों की तुलना में कम हो जाती है एवं वे सस्ते हो जाते हैं और उनकी मांग में वृद्धि हो जाती है। इसके अतिरिक्त सरकारें इच्छानुसार भी अपनी मुद्रा के मूल्य को विदेशी मुद्रा की तुलना में कम कर देती हैं। इससे भी देश का आयात महँगा होकर हतोत्साहित होता है तथा देश के निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है। अंतत: घरेलू उत्पादों की मांग में वृद्धि होती है। इस प्रकार हम पाते हैं कि अवमूल्यन भी घरेलू उद्योगों के संरक्षण के दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण होता है।
सैद्धांतिक रूप से अगर देखें तो संरक्षणवादी नीति से भले ही विदेशी वस्तुओं के साथ भेदभाव द्वारा घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया जाता है परंतु व्यावहारिक रूप से देखने पर पता चलता है कि संरक्षण संबंधी नीतियों से प्रभावित देश इसके विरोध में प्रतिक्रिया करते हैं जिससे अंतत: व्यापार युद्ध का जन्म होता है। इस व्यापार युद्ध के कारण विदेशी उत्पादों के साथ भेदभाव के स्तर में वृद्धि हो जाती है।
अगर वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गौर करें तो हम पाते हैं कि मौजूदा समय में भी व्यापार युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं चीन जैसे देश अपनी संरक्षणवादी नीतियों के कारण विश्व व्यापार संगठन के नियमों को भी धता बता रहे हैं। मौजूदा व्यापार युद्ध की पृष्ठभूमि पिछले कई वर्षों से तैयार हो रही थी। अमेरिका द्वारा अपने यहाँ आयातित स्टील एवं एल्युमीनियम पर आरोपित आयात कर में वृद्धि ने इसे मुख्यपृष्ठ पर लाकर खड़ा कर दिया है। अमेरिका द्वारा आायात कर में की गई वृद्धि को विश्व समुदाय द्वारा संरक्षणवादी रवैया करार दिया गया। इसके फलस्वरूप चीन सहित अनेक यूरोपीय देशों ने अमेरिका से आयातित अनेक उत्पादों पर आयात कर में वृद्धि कर दी। हालाँकि अमेरिका द्वारा इस पर कड़ा ऐतराज जताया गया।
गौरतलब है कि अमेरिका अपने द्वारा उठाए गए इस कदम को न तो स्वतंत्र व्यापार के खिलाफ मानता है और न ही वैश्वीकरण के विरुद्ध।
अमेरिका के अनुसार, यह कदम उसने व्यापार अधिनियम, 1974 की धारा 301 के तहत अपारदर्शी एवं अनुचित व्यापार गतिविधियों के विरुद्ध उठाया है। उसका तर्क है कि विश्व के अनेक देशों ने अपने यहाँ आयात कर की दर काफी ऊँची कर रखी है, जबकि अमेरिका में यह काफी नीची है। ऐसे में वह मानता है कि वैश्विक स्वतंत्र व्यापार संतुलित नहीं है क्योंकि दूसरे देशों के उत्पाद तो अमेरिका में काफी सुगमता से कम कीमतों पर आ जाते हैं, जबकि अमेरिकी उत्पादों के साथ दूसरे देशों में काफी भेदभाव होता है।
अमेरिका चीन पर भी अनैतिक व्यापार नीतियों के पालन का आरोप लगाता रहा है। उसके अनुसार, चीन भी विश्व व्यापार नियमों के विरुद्ध कार्य करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति वर्तमान में ‘अमेरिका प्रथम’ की नीति का पालन कर रहे है जिसके अनुसार अमेरिकी हितों की पूर्ति पहले होनी चाहिये एवं अन्य देशों के हितों का संरक्षण उसके बाद में होना चाहिये। अमेरिकी राष्ट्रपति की यह नीति अमेरिकी उद्योगों की मंद विकास गति को तीव्र करने तथा वहाँ की बेरोज़गार जनता को रोज़गार दिलाने एवं अमेरिकी आर्थिक संवृद्धि को तीव्र करने हेतु लाई गई है। अमेरिका के संरक्षणवादी रुख को उसके सामरिक सुरक्षा जैसे हितों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। अमेरिका स्टील एवं एल्युमीनियम जैसे सामरिक महत्त्व की धातुओं के उत्पादन हेतु स्वयं चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहता।
इस व्यापार युद्ध के विश्व में गंभीर आर्थिक-राजनीतिक दुष्परिणाम निकलने की आशंका जताई जा रही है। इस व्यापार युद्ध से विश्व पुन: वैश्विक आर्थिक मंदी की ओर जा सकता है। स्वतंत्र प्रतिस्पर्द्धा खत्म होने से उत्पादकता एवं उत्पादन में भी कमी आएगी। इस प्रकार संरक्षणवादी दृष्टिकोण अपनाने से विश्व के उपभोक्ताओं को ऊँची लागत पर कम गुणवत्ता वाली वस्तुएँ प्राप्त होंगी।
व्यापार युद्ध के सकारात्मक पक्ष को देखने वालों का मानना है कि इससे दीर्घकाल में परस्पर सहयोग में वृद्धि होगी। यह व्यापार युद्ध वर्तमान आयात कर की विभेदी संरचना में समानता लाएगा एवं विश्व व्यापार संगठन को और मज़बूत बनाएगा। संरक्षण के मुद्दे पर फ्राँसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का कहना था कि ‘‘दुनिया के लिये अपने दरवाज़े बंद कर लेने से हम दुनिया को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते हैं। यह हमारे नागरिकों के भय को कम नहीं करेगा अपितु उसे और भी बढ़ाएगा। हम अतिवादी राष्ट्रवाद के उन्माद से दुनिया की उम्मीद को नुकसान पहुँचने नहीं दे सकते हैं’’। आज यह कथन सत्य प्रतीत होता है।
भले ही स्वतंत्र व्यापार की विसंगतियों को दूर करने का उद्देश्य पवित्र हो परंतु इसे वैश्विक मंच से समावेशी दृष्टिकोण द्वारा ही दूर किया जा सकता है और तभी WTO जैसी संस्था को पारदर्शी एवं परस्पर सहयोगी बनाया जा सकेगा।
|
114 videos|362 docs|105 tests
|