नोट्स: त्रुटि विश्लेषण | गणित और शिक्षाशास्त्र (Mathematics) CTET & TET Paper 1 - CTET & State TET PDF Download
किसी भौतिक मात्रा का मापन पूरी तरह से सटीक नहीं हो सकता। इसलिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि मापी गई मूल्य वास्तविक, अज्ञात मात्रा के मूल्य से कितना भिन्न हो सकता है। इन भिन्नताओं का अनुमान लगाने की कला को शायद अनिश्चितता विश्लेषण कहा जाना चाहिए, लेकिन ऐतिहासिक कारणों से इसे त्रुटि विश्लेषण कहा जाता है।
त्रुटियों का वर्गीकरण
कुछ विद्वानों ने मापन और मूल्यांकन की त्रुटियों का वर्गीकरण उनके रूप के आधार पर किया है। ये निम्नलिखित प्रकार की हैं:
- व्यक्तिगत त्रुटियाँ: इस प्रकार में मापने वाले और मूल्यांकन करने वाले द्वारा की गई मापन त्रुटियाँ शामिल हैं। यह देखा गया है कि मापने वाले की शारीरिक और मानसिक स्थिति, उसका व्यक्तिगत दृष्टिकोण, उसकी पसंद और पूर्वाग्रह सीधे या परोक्ष रूप से उसके मापन प्रक्रिया पर प्रभाव डालते हैं। इस प्रकार की त्रुटियाँ सामान्यतः निबंध प्रकार के उत्तरों को अंकित करते समय देखी जाती हैं। इन त्रुटियों को वस्तुनिष्ठ परीक्षण करके सुधारा जा सकता है।
- परिवर्तनीय त्रुटियाँ: इस प्रकार में मापन त्रुटियाँ शामिल हैं जो मापन वस्तु, व्यक्ति या गतिविधि, मापन गुणवत्ता (परिवर्तनीय), मापन उपकरण या विधि के प्रशासन के कारण होती हैं। शैक्षिक माप में, त्रुटियाँ छात्रों की असामान्य शारीरिक या मानसिक स्थिति, मापन परिवर्तनीय की अस्पष्टता, मापन उपकरण या विधि की असंगतता और उनके अपर्याप्त प्रशासन के कारण होती हैं। इनका उन्मूलन करने के लिए, छात्रों के साथ सहानुभूति से व्यवहार करना, मापन गुणों को स्पष्ट रूप से समझना, सबसे उपयुक्त मापन विधि का चयन करना और उसका उचित प्रशासन करना आवश्यक है।
- स्थायी त्रुटियाँ: इस प्रकार में मापन उपकरण या विधि के रूप में मापन त्रुटियाँ और उनके उपयोग में त्रुटियाँ शामिल हैं। चूंकि सभी छात्रों द्वारा प्राप्त अंक इन त्रुटियों से प्रभावित होते हैं, इसलिए इन्हें स्थायी त्रुटियाँ कहा जाता है। इन त्रुटियों को मापन विधि को अधिक वैध बनाकर समाप्त किया जा सकता है।
- व्याख्यात्मक त्रुटियाँ: मापन परिणामों के विश्लेषण में होने वाली त्रुटियों को व्याख्यात्मक त्रुटियाँ कहा जाता है। इस प्रकार की त्रुटियों को उपयुक्त मानदंडों के विकास और सही सांख्यिकीय गणनाओं द्वारा समाप्त किया जा सकता है।
- संयोगिक त्रुटियाँ: संयोगिक त्रुटियों से हमारा तात्पर्य उन त्रुटियों से है जो आकस्मिक रूप से होती हैं। ये तीन प्रकार की होती हैं:
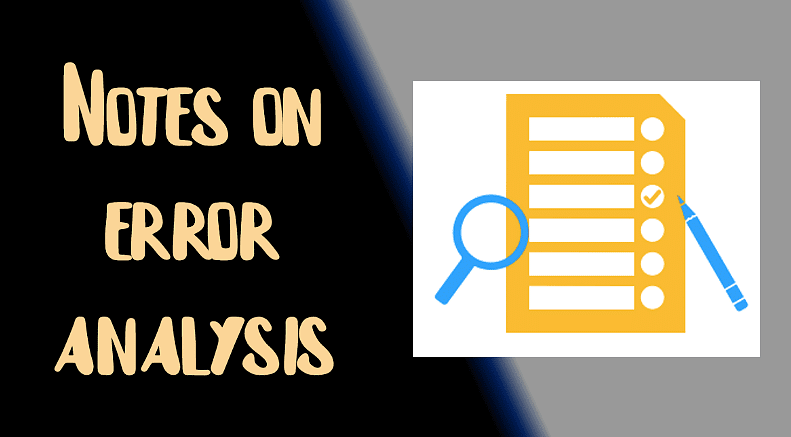
- छात्र उन्मुख त्रुटियाँ: वे त्रुटियाँ जो छात्र के अचानक बीमार होने, उत्तेजित या भयभीत होने के कारण होती हैं, उन्हें छात्र उन्मुख त्रुटियाँ कहा जाता है। इनका समाधान करने के लिए छात्र को सामान्य बनाना आवश्यक है।
- परीक्षा उन्मुख त्रुटियाँ: ऐसी त्रुटियाँ तब उत्पन्न होती हैं जब परीक्षा मान्य, विश्वसनीय और वस्तुनिष्ठ नहीं होती। इन त्रुटियों को परीक्षा को मान्य, विश्वसनीय और वस्तुनिष्ठ बनाकर समाप्त किया जा सकता है।
- मार्किंग में त्रुटियाँ: मार्किंग में त्रुटियाँ उन परीक्षकों द्वारा भिन्न दृष्टिकोण के साथ मार्किंग करने के कारण होती हैं। ये त्रुटियाँ अक्सर निबंध प्रकार के उत्तरों की मार्किंग में होती हैं। ऐसे प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ बनाया जा सकता है। मूल्यांकनकर्ताओं का प्रशिक्षण भी आवश्यक है।
6. सिस्टमेटिक त्रुटियाँ: सिस्टमेटिक त्रुटियों का तात्पर्य उन त्रुटियों से है जो मापन और मूल्यांकन की प्रक्रिया में व्यक्ति द्वारा की जाती हैं। ये त्रुटियाँ भी तीन प्रकार की होती हैं।
- अज्ञानता के कारण त्रुटियाँ: अज्ञानता के कारण त्रुटियाँ छात्रों द्वारा निर्देशों या मैनुअल को ठीक से न देखने पर होती हैं। ऐसी त्रुटियों को दूर किया जा सकता है यदि छात्र सावधानी से कार्य करें।
- भूलने के कारण त्रुटियाँ: कभी-कभी छात्र 0.01 को 0.1 के स्थान पर, या 3.7 को 7.3 के स्थान पर लिख देते हैं। ऐसी त्रुटियों को सावधानी बरतने से नियंत्रित किया जा सकता है।
- पक्षपात के कारण त्रुटियाँ: मापने वाले के पूर्वाग्रह या पसंद के कारण उत्पन्न होने वाली त्रुटियाँ इसमें शामिल होती हैं। ऐसी त्रुटियों को व्यक्तिपरकता के अवसरों को समाप्त करके और मापन उपकरण या विधि को वस्तुनिष्ठ बनाकर हटाया जा सकता है।
शिक्षण विधियाँ:
ज्ञान की दुनिया को छात्रों के मन में व्याख्यायित करने की प्रक्रिया को ‘‘शिक्षण की विधि’’ कहा जाता है। ज्ञान की दुनिया में ज्ञान, रुचि, दृष्टिकोण, कौशल आदि शामिल होते हैं, यानी सभी तीन क्षेत्र—ज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोमोटर।
व्याख्यान विधि
- यह एक शिक्षक-केंद्रित विधि है। इस विधि में शिक्षक एक सक्रिय प्रतिभागी होता है और छात्र एक निष्क्रिय शिक्षार्थी होता है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। इस विधि में शिक्षक किसी विशेष विषय पर व्याख्यान देता है और बच्चे सुनते हैं। यह एकतरफा संचार है क्योंकि शिक्षक विचार देता है और बच्चे उन्हें ग्रहण करते हैं।
- व्याख्यान विधि के कुछ लाभ नीचे दिए गए हैं:
- यह एक आसान, आकर्षक और संक्षिप्त विधि है।
- यह तथ्य आधारित ज्ञान और गणित के ऐतिहासिक विकास को देने के लिए उपयोगी है।
- यह उच्च कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है।
- यह विचारों और अनुभवों की शब्द चित्रण करने की विधि है।
- व्याख्यान विधि के कुछ दोष भी हैं:
- यह एक शिक्षक-केंद्रित विधि है। इसलिए यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के खिलाफ है।
- शिक्षार्थी निष्क्रिय और अनियंत्रित रहता है।
- यह विभिन्न मानसिक क्षमताओं जैसे—युक्ति, तार्किक सोच, गणितीय प्रशिक्षण आदि को विकसित करने के अवसर नहीं प्रदान करता है।
- इस विधि में व्यावहारिक और रचनात्मक कार्य के लिए कोई प्रावधान नहीं है।
- यह आवश्यक नहीं है कि बच्चे शिक्षक/वक्ता द्वारा कही गई सभी बातें समझें और ध्यान दें।
इन्डक्टिव विधि
गणित की शिक्षा और अध्ययन के लिए इंडक्टिव विधि प्रेरणा पर आधारित है। प्रेरणा का अर्थ है किसी सार्वभौमिक सत्य या प्रमेय को इस तरह से साबित करना कि यदि यह किसी विशेष मामले में सही है, तो यह अगले मामले में भी उसी क्रम में सही होगा। यह एक विकास की विधि है जिसमें बच्चे को सत्य को स्वयं खोजने के लिए प्रेरित किया जाता है।
- इंडक्टिव विधि के कुछ लाभ नीचे दिए गए हैं:
- यह एक वैज्ञानिक विधि है क्योंकि इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान वास्तविक तथ्यों पर आधारित होता है।
- इस विधि का उपयोग करके प्राप्त ज्ञान अधिक टिकाऊ होता है क्योंकि इस विधि में बच्चा स्वयं उदाहरणों, अवलोकन और परीक्षण के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है।
- इस विधि द्वारा बच्चों की आलोचनात्मक अवलोकन और तर्कशक्ति विकसित होती है।
- इस विधि में बच्चे स्वयं उदाहरणों की सहायता से ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसलिए उन्हें उदासी या थकावट नहीं होती।
- वे नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सक्रिय रहते हैं।
- यह निश्चित रूप से सच है कि इंडक्टिव विधि गणित की शिक्षा की एक बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी विधि है।
हालांकि इसके इतने सारे लाभ हैं, इसके कुछ हानियां भी हैं:
- यह एक बहुत धीमी प्रक्रिया है, इसलिए इस विधि द्वारा ज्ञान प्राप्त करने में अधिक समय और श्रम लगता है।
- इसका उपयोग करने के लिए तेज दिमाग, उचित योजना और पर्याप्त श्रम की आवश्यकता होती है।
- इसलिए यह सभी स्तरों के छात्रों के लिए इस विधि से ज्ञान प्राप्त करना आसान नहीं है।
- केवल एक अनुभवी और सक्षम शिक्षक ही इस विधि का सफलतापूर्वक उपयोग कर सकता है।
- इस विधि का उपयोग करके समस्या समाधान की क्षमता विकसित नहीं हो सकती।
डेडक्टिव विधि
निष्कर्षात्मक विधि (Deductive method) बिल्कुल सूचकीय विधि (Inductive method) के विपरीत है। इस विधि में निष्कर्षात्मक तर्क (deductive logic) का उपयोग किया जाता है। निष्कर्षात्मक विधि मुख्यतः बीजगणित (algebra), ज्यामिति (geometry) और त्रिकोणमिति (trigonometry) में उपयोग की जाती है क्योंकि इन उप-शाखाओं में विभिन्न संबंध, नियम और सूत्रों का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक नियम और सूत्र को व्यावहारिक रूप से सत्यापित करना असंभव है। इस विधि में गणित के मान्यताएँ (assumptions), पदस्थापनाएँ (postulates) और अक्षीय नियम (axioms) से सहायता ली जाती है। यह विधि उच्च कक्षाओं में गणित पढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है। यह निष्कर्ष (deduction) पर आधारित है।
- निष्कर्षात्मक विधि बिल्कुल सूचकीय विधि के विपरीत है।
- इस विधि में निष्कर्षात्मक तर्क का उपयोग किया जाता है। यह विधि मुख्यतः बीजगणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति में उपयोग होती है।
- प्रत्येक नियम और सूत्र को व्यावहारिक रूप से सत्यापित करना असंभव है।
- इस विधि में गणित के मान्यताएँ, पदस्थापनाएँ और अक्षीय नियम से सहायता ली जाती है।
- यह विधि उच्च कक्षाओं में गणित पढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है।
- यह निष्कर्ष पर आधारित है।
निष्कर्षात्मक विधि के कुछ गुण निम्नलिखित हैं:
- इस विधि का उपयोग करने से ज्ञान अर्जित करने की गति बढ़ जाती है क्योंकि छात्र सीधे समस्या को हल करने के लिए सूत्र का उपयोग करते हैं।
- इस विधि का उपयोग तब किया जाना चाहिए जब समय की कमी हो।
- इस विधि का उपयोग ज्यामिति के थियोरम (theorems) और अक्षीय नियम (axioms) को पढ़ाने, अंकगणित में तालिकाओं आदि को पढ़ाने के लिए किया जाता है।
- शिक्षक और छात्र दोनों को इस विधि का उपयोग करने में कोई कठिनाई नहीं होती है।
- इस विधि के प्रयोग से कम समय में अधिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है।
- यह विधि संक्षिप्त और व्यावहारिक है।
निष्कर्षात्मक विधि के कुछ कमजोरियाँ और सीमाएँ हैं:
- यह विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार नहीं है।
- इस विधि में समझने या खोजने के बजाय रटने पर अधिक जोर दिया जाता है।
- इस विधि में तार्किक सोच और खोज की शक्तियों को विकसित करने का कोई अवसर नहीं है।
- बच्चों को इस विधि का उपयोग करके नए ज्ञान प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलता है।
विश्लेषणात्मक विधि (Analytic Method)
विश्लेषण शब्द का मूल अर्थ है एक साथ जुड़े चीजों को अलग करना। विश्लेषण "हमें क्या पता करना है" से शुरू होता है और इसके और डेटा के बीच संबंध को दर्शाता है। इस विधि की सहायता से किसी भी समस्या के कठिन हिस्सों का विश्लेषण किया जा सकता है ताकि दी गई समस्या का समाधान निकाला जा सके। इस प्रकार, समस्या के विभिन्न हिस्सों का अलगाव विश्लेषण के रूप में जाना जाता है।
- विश्लेषण शब्द का मूल अर्थ है एक साथ जुड़े चीजों को अलग करना।
- विश्लेषण "हमें क्या पता करना है" से शुरू होता है और इसके और डेटा के बीच संबंध को दर्शाता है।
- विश्लेषणात्मक विधि के कुछ लाभ निम्नलिखित हैं: यह विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। विश्लेषण एक व्याख्यात्मक प्रक्रिया है। यह बच्चे में रचनात्मकता और मौलिकता उत्पन्न करता है और विश्लेषणात्मक और तर्कशक्ति को विकसित करता है। यह बच्चे में आत्मविश्वास और तार्किक क्षमताओं को विकसित करता है। यह एक आकारात्मक विधि है और गुणात्मक तर्क पर आधारित है।
विश्लेषणात्मक विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। विश्लेषण एक व्याख्यात्मक प्रक्रिया है। यह बच्चे में रचनात्मकता और मौलिकता उत्पन्न करता है और विश्लेषणात्मक और तर्कशक्ति को विकसित करता है। यह बच्चे में आत्मविश्वास और तार्किक क्षमताओं को विकसित करता है। यह एक आकारात्मक विधि है और गुणात्मक तर्क पर आधारित है।
- यह विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है।
- विश्लेषण एक व्याख्यात्मक प्रक्रिया है।
- यह एक आकारात्मक विधि है और गुणात्मक तर्क पर आधारित है।
- हालांकि यह गणित सिखाने की एक महत्वपूर्ण और उपयोगी विधि है, इसके कुछ सीमाएँ हैं जो निम्नलिखित हैं: हर शिक्षक इस विधि का सफलतापूर्वक उपयोग नहीं कर सकता। पूरे पाठ्यक्रम को निश्चित समय में पूरा नहीं किया जा सकता। विश्लेषणात्मक विधि का उपयोग केवल तभी संभव है जब हमारे पास ज्ञात तथ्यों और अज्ञात निष्कर्षों का ज्ञान हो।
हर शिक्षक इस विधि का सफलतापूर्वक उपयोग नहीं कर सकता है।
- पूरा पाठ्यक्रम निश्चित समय में पूरा नहीं किया जा सकता है।
संश्लेषण विधि
यह विश्लेषणात्मक पद्धति का विपरीत है। संश्लेषण का अर्थ है अलग चीज़ों को एक साथ रखना या "अलग हिस्सों को एकजुट करना"।
- इस पद्धति में हम "ज्ञात से अज्ञात की ओर" बढ़ते हैं या हम परिकल्पना से शुरू करते हैं और निष्कर्षों पर समाप्त करते हैं। इस प्रकार, संश्लेषण डेटा से शुरू होता है और उन्हें निष्कर्ष से जोड़ता है।
- संश्लेषण पद्धति के कुछ लाभ निम्नलिखित हैं:
- यह एक संक्षिप्त और त्वरित पद्धति है।
- यह बच्चे की स्मृति को उजागर करती है।
- यह खोजे गए तथ्यों को संक्षेप में तैयार करती है, रिकॉर्ड करती है और प्रस्तुत करती है।
- यह विश्लेषण की तरह परीक्षणों और त्रुटियों को छोड़ देती है।
- यह एक संक्षिप्त रूप में समाधान प्रस्तुत करने की पद्धति है।
संश्लेषण पद्धति के कुछ दोष निम्नलिखित हैं:
- यह बच्चे के मन में कई संदेह उत्पन्न करती है।
- सोचने, तर्क करने और अन्य मानसिक क्षमताओं को विकसित करने का कोई अवसर नहीं होता।
- हर बच्चे के लिए हर चरण की पुनः स्मरण करना संभव नहीं हो पाता।
प्रयोगशाला पद्धति
गणित को और अधिक दिलचस्प और अर्थपूर्ण बनाने के लिए, प्रयोगशाला विधि का उपयोग गणित की शिक्षा में किया जाता है। इस विधि में छात्रों को व्यक्तिगत रूप से सीधे अनुभवों के माध्यम से तथ्यों से परिचित होने का अवसर मिलता है। इस विधि में छात्र स्वयं प्रयोगों की सहायता से गणित के तथ्यों और कानूनों का सत्यापन करते हैं।
- इस विधि को लागू करने के लिए एक प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है जिसमें गणित से संबंधित उपकरण और अन्य उपयोगी शिक्षण सामग्री उपलब्ध हो।
- प्रयोगशाला विधि के कुछ लाभ निम्नलिखित हैं: यह विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत "करने द्वारा सीखना" पर आधारित है, ताकि छात्र अपने काम में रुचि लें।
- इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान अधिक ठोस और दीर्घकालिक होता है।
- यह खोज और आत्म-अध्ययन की आदत विकसित करने में सहायता करता है।
- यह छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करता है।
- यह विधि समस्या समाधान की क्षमता विकसित करने में मदद करती है।
- बच्चों को सृजनात्मक और व्यावहारिक कार्य करने का अवसर मिलता है।
- बच्चे प्रयोगशाला में सक्रिय रहने के कारण आनंदित होते हैं।
प्रयोगशाला विधि के कुछ नुकसान निम्नलिखित हैं:
- यह एक महंगी विधि है, इसलिए आर्थिक सीमाओं के कारण सभी स्कूल इस विधि को अपनाने में असमर्थ हैं।
- इसे सिखाने में अधिक समय लगता है, इसलिए विशाल पाठ्यक्रम को समय के भीतर पूरा नहीं किया जा सकता।
- इस विधि के लिए विभिन्न उपकरणों से लैस प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है।
- बड़े छात्र वर्गों में व्यक्तिगत ध्यान नहीं दिया जा सकता।
हीयुरिस्टिक विधि
अन्य विधियों की तरह, ह्यूरिस्टिक विधि का गणित शिक्षण में एक विशेष स्थान है।
ह्यूरिस्टिक शब्द का मानना है कि यह ग्रीक शब्द ‘‘Heurisco’’ से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है ‘‘मैं खोजता हूँ’’। इस विधि के प्रवर्तक प्रोफेसर हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग थे।
ह्यूरिस्टिक विधि के कुछ लाभ निम्नलिखित हैं:
- यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है।
- यह आत्म-विश्वास, आत्म-निर्भरता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करती है।
- यह समस्याओं को हल करने के लिए अवलोकन की क्षमता और जिज्ञासा की भावना को विकसित करती है।
- बच्चों में विचारशीलता और जागरूकता बढ़ती है।
- छात्रों को मानसिक और विचार शक्ति विकसित करने का अवसर मिलता है।
- यह विधि गतिविधि के सिद्धांत पर आधारित है।
- शिक्षक का व्यक्तिगत ध्यान संभव है और शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच संबंध अधिक निकटता से बनता है।
ह्यूरिस्टिक विधि के कुछ दोष निम्नलिखित हैं:
- यह निचले कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है।
- यह एक बहुत ही धीमा विधि है।
- ह्यूरिस्टिक दृष्टिकोण पर लिखी गई पाठ्यपुस्तकों की कमी है।
- यह एक रचनात्मक विधि है, सूचना देने वाली नहीं।
|
29 videos|73 docs|72 tests
|
















