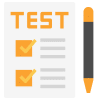UPSC Daily Current Affairs (Hindi) - 2nd April 2024 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly PDF Download
जीएस-I
दूर त्रिभुज
विषय : भूगोल

चर्चा में क्यों?
भूवैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की है कि अफार त्रिभुज में अफ्रीकी महाद्वीप की दरार के परिणामस्वरूप अगले 5 से 10 मिलियन वर्षों में एक नए महासागर का निर्माण हो सकता है।
पृष्ठभूमि
- लंबे समय में, इस दरार के चौड़ा होने और अंततः समुद्री जल से भरने की संभावना है, जिससे एक नया महासागर बन सकता है। वर्तमान भूवैज्ञानिक ज्ञान और पूर्वानुमानों के आधार पर यह परिवर्तन लाखों वर्षों में होने की उम्मीद है।
- यह हमारे ग्रह पर हो रहे निरंतर परिवर्तन और विकास का एक आकर्षक उदाहरण है।
अफ़ार त्रिभुज के बारे में
- अफार त्रिभुज, जिसे अफार अवदाब के नाम से भी जाना जाता है, अफ्रीका के हॉर्न में स्थित एक भूवैज्ञानिक अवदाब है।
- अफ्रीका के उत्तरपूर्वी भाग में स्थित अफार त्रिभुज विश्व स्तर पर सबसे गतिशील रूप से सक्रिय क्षेत्रों में से एक है।
- यह वह बिंदु है जहां अरब, न्युबियन और सोमाली टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से अलग हो रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप एक दरार प्रणाली बन रही है जो अफ्रीकी महाद्वीप को विभाजित कर रही है।
भूवैज्ञानिक संदर्भ
- अफार त्रिभुज अफार ट्रिपल जंक्शन का परिणाम है, जो पूर्वी अफ्रीका में ग्रेट रिफ्ट घाटी का एक हिस्सा है।
- यह इथियोपिया के अफ़ार क्षेत्र में स्थित है।
- यह क्षेत्र अपनी विशिष्ट भूवैज्ञानिक विशेषताओं के कारण विख्यात है और यहां प्राचीनतम होमिनिनों के जीवाश्म अवशेष मिले हैं, जिन्हें मानव वंश का सबसे प्रारंभिक सदस्य माना जाता है।
- कुछ वैज्ञानिक इसे मानव विकास का जन्मस्थान मानते हैं।
भौगोलिक मुख्य आकर्षण
- अफार त्रिभुज जिबूती में असाल झील को घेरता है, जो समुद्र तल से 155 मीटर (509 फीट) नीचे स्थित, अफ्रीका का सबसे निचला बिंदु है।
- इस क्षेत्र को अवाश नदी से पोषण मिलता है, जो एक संकीर्ण हरित पट्टी को सहारा देती है, जो वनस्पति, वन्य जीवन और दानकिल रेगिस्तान में रहने वाले खानाबदोश अफार समुदाय को जीवित रखती है।
- अफार डिप्रेशन के उत्तरी भाग को डानाकिल डिप्रेशन के नाम से भी जाना जाता है।
- यह क्षेत्र अत्यधिक गर्मी, शुष्कता और सीमित वायु परिसंचरण को सहन करता है, जिससे यह वर्ष भर पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थानों में से एक बन जाता है।
स्रोत : टाइम्स ऑफ इंडिया
जीएस-II
रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (रेरा)
विषय : राजनीति एवं शासन

चर्चा में क्यों?
रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (रेरा), जिसे आठ साल पहले संसद द्वारा पारित किया गया था, वर्तमान में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा समीक्षाधीन है।
पृष्ठभूमि
इस समीक्षा के हिस्से के रूप में, वरिष्ठ अधिकारियों ने अधिनियम की प्रभावशीलता पर प्रतिक्रिया एकत्र करने के लिए घर खरीदारों के साथ नियमित बैठकें शुरू की हैं। इन बैठकों का उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही, सूचना प्रसार और शिकायत निवारण जैसे प्रमुख आयामों का आकलन करना है।
रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के बारे में
रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (रेरा) देश में रियल एस्टेट क्षेत्र को विनियमित करने और बढ़ावा देने के लिए भारतीय संसद द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण कानून है।
उद्देश्य और स्थापना
- RERA का उद्देश्य घर खरीदारों की सुरक्षा करना तथा रियल एस्टेट लेनदेन में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाना है।
- यह प्रत्येक राज्य में एक रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (RERA) की स्थापना करता है, जो त्वरित विवाद समाधान के लिए निर्णायक निकाय के रूप में कार्य करता है।
प्रयोज्यता
- RERA निम्नलिखित मानदंडों के साथ निर्माणाधीन परियोजनाओं पर लागू होता है:
- प्लॉट का आकार 500 वर्ग मीटर से अधिक।
- 8 या अधिक अपार्टमेंट वाली परियोजनाएं।
प्रमुख प्रावधान
- अनिवार्य पंजीकरण: निर्दिष्ट मानदंडों के अंतर्गत आने वाली सभी रियल एस्टेट परियोजनाओं को RERA के साथ पंजीकृत होना होगा।
- त्वरित विवाद समाधान: RERA विवादों को कुशलतापूर्वक निपटाने के लिए एक अपीलीय न्यायाधिकरण और समर्पित न्यायाधिकरण अधिकारियों की स्थापना करता है।
- हस्तांतरण के लिए सहमति: यदि कोई प्रमोटर अधिकारों और दायित्वों को किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित करना चाहता है, तो दो-तिहाई आवंटियों की लिखित सहमति और RERA अनुमोदन आवश्यक है।
- शिकायत तंत्र: व्यक्ति प्रमोटरों, खरीदारों या एजेंटों द्वारा किए गए उल्लंघन के संबंध में RERA में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
गैर-अनुपालन के लिए दंड
- RERA के आदेशों का पालन न करने वाले प्रमोटरों को मूल्यांकित संपत्ति की लागत का 5% तक जुर्माना देना पड़ सकता है।
- अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेशों का पालन न करने पर कारावास या जुर्माना हो सकता है।
क्षेत्राधिकार
सिविल न्यायालयों को RERA या अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा कवर किए गए मामलों पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।
स्रोत : इंडियन एक्सप्रेस
सुप्रीम कोर्ट ने रैखिक परियोजनाओं के लिए अनियमित मिट्टी निष्कर्षण पर रोक क्यों लगाई?
विषय : राजनीति एवं शासन

चर्चा में क्यों?
सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरण मंत्रालय की 2020 की अधिसूचना को अमान्य कर दिया, जिसमें सड़क और पाइपलाइन जैसी रैखिक परियोजनाओं के लिए साधारण मिट्टी के निष्कर्षण को पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) से छूट दी गई थी।
रैखिक परियोजनाओं के लिए मिट्टी निष्कर्षण से छूट देने वाली अधिसूचना की पृष्ठभूमि
- 2006 में पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (ईपीए) के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता वाली गतिविधियों को निर्दिष्ट किया।
- इसके बाद 2016 में जारी अधिसूचना में कुछ परियोजनाओं को इस आवश्यकता से छूट दी गयी।
- 2020 की अधिसूचना में रैखिक परियोजनाओं के लिए मिट्टी निष्कर्षण को छूट प्राप्त गतिविधियों की सूची में जोड़ा गया।
अधिसूचना जारी करने के कारण
- केंद्र ने तर्क दिया कि इस छूट का उद्देश्य विभिन्न गैर-खनन गतिविधियों को लाभ पहुंचाना तथा खान एवं खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन के अनुरूप है।
- इसने तर्क दिया कि न्यायिक हस्तक्षेप अनावश्यक था क्योंकि यह एक नीतिगत निर्णय था।
2020 की छूट की चुनौतियाँ
- इस छूट को मनमाना होने तथा अनुच्छेद 14 जैसे संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
- कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक आपत्ति प्रक्रियाओं को दरकिनार कर निजी खनिकों को लाभ पहुंचाने के लिए इसकी आलोचना की गई थी।
- राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने केंद्र से तीन महीने के भीतर उचित सुरक्षा उपायों के साथ अधिसूचना को संशोधित करने का आग्रह किया।
सरकार की प्रतिक्रिया
- केंद्र ने कार्रवाई में देरी की, जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप नहीं किया, जिसके बाद प्रवर्तन तंत्र की रूपरेखा वाला एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया।
- मंत्रालय ने छूट के लिए पर्यावरण सुरक्षा उपायों और प्रक्रियाओं के अनुपालन पर जोर दिया।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
- न्यायालय ने 'रैखिक परियोजनाओं' और निष्कर्षण मापदंडों जैसे शब्दों पर स्पष्टता की कमी के कारण पूर्ण छूट को मनमाना और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना।
- इसने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान, जब निर्माण गतिविधियां रुकी हुई थीं, अधिसूचना को जल्दबाजी में जारी करने की आलोचना की।
समान छूट की पिछली न्यायिक जांच
- पिछले मामलों में, भवन परियोजनाओं के लिए 2016 की अधिसूचना और शैक्षणिक संस्थानों के लिए 2014 की अधिसूचना जैसी छूटों को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था और पर्यावरणीय औचित्य के अभाव में उन्हें रद्द कर दिया गया था।
- न्यायिक निकायों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए ईपीए के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन के महत्व पर बल दिया।
स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस
दो राज्य: जीवन रक्षक सी-सेक्शन तक पहुंच की तुलना
विषय: राजनीति और शासन

चर्चा में क्यों?
आईआईटी मद्रास द्वारा जारी अध्ययन में तमिलनाडु में महिलाओं, विशेषकर निजी अस्पतालों में, सी-सेक्शन प्रसव की उच्च दर से संबंधित चिंताओं पर प्रकाश डाला गया है।
- इससे स्थिति से निपटने के लिए सुधारात्मक उपायों की आवश्यकता का संकेत मिलता है।
सिजेरियन सेक्शन क्या है?
- इसे सी-सेक्शन या सिजेरियन डिलीवरी के नाम से भी जाना जाता है, यह एक शल्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा मां के पेट में चीरा लगाकर एक या एक से अधिक शिशुओं को जन्म दिया जाता है।
- यह प्रक्रिया अक्सर तब अपनाई जाती है जब योनि से प्रसव से मां या बच्चे को खतरा हो सकता है।
सी-सेक्शन दरों में परिवर्तन:
- सार्वजनिक अस्पताल: तमिलनाडु के सार्वजनिक क्षेत्र के अस्पतालों में 2019-21 के दौरान लगभग 40% महिलाओं ने सी-सेक्शन करवाया।
- निजी अस्पताल: 2019-21 के दौरान तमिलनाडु में निजी क्षेत्र के अस्पतालों में करीब 64% महिलाओं ने सी-सेक्शन करवाया, जो राष्ट्रीय औसत और छत्तीसगढ़ की दर दोनों से काफी अधिक है।
- क्षेत्रीय असमानताएं: छत्तीसगढ़ में, किसी महिला के निजी अस्पताल में सी-सेक्शन प्रसव की संभावना, सार्वजनिक अस्पताल की तुलना में दस गुना अधिक है।
सी-सेक्शन दरों को प्रभावित करने वाले कारक:
- सामाजिक-आर्थिक कारक: अध्ययन से पता चलता है कि गरीब परिवार प्रसव के लिए सार्वजनिक अस्पतालों को चुनते हैं, जबकि अमीर परिवार प्रसव के लिए निजी अस्पतालों को प्राथमिकता देते हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं तक असमान पहुंच में योगदान होता है।
- मातृ आयु और वजन की स्थिति: मातृ आयु (35-49) और अधिक वजन की स्थिति जैसे कारक सी-सेक्शन प्रसव की संभावना को बढ़ाते हैं।
- असमानता: भारत में, निजी सुविधाओं में गरीब और गैर-गरीब लोगों के बीच सी-सेक्शन के प्रचलन में अंतर कम हुआ है, लेकिन तमिलनाडु में चिंताजनक प्रवृत्ति देखी गई, जहां गैर-गरीब लोगों की तुलना में गरीबों में सी-सेक्शन का प्रतिशत अधिक है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिशें:
- न्यूनतम मातृ एवं नवजात मृत्यु दर प्राप्त करने के लिए सिजेरियन डिलीवरी की दर आदर्श रूप से 10-15% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- वैश्विक सी-सेक्शन दरें 2021 में 20% से अधिक हो गईं और 2030 तक 30% तक पहुंचने का अनुमान है।
निष्कर्ष:
- तमिलनाडु में सी-सेक्शन तक पहुंच में असमानताएं हैं, सार्वजनिक और निजी दोनों अस्पतालों में दरें ऊंची हैं।
- क्षेत्रीय और सामाजिक-आर्थिक कारकों पर ध्यान देना तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिशों का पालन करना समतामूलक मातृ स्वास्थ्य देखभाल के लिए महत्वपूर्ण है।
स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस
जीएस-III
सफेद खरगोश प्रौद्योगिकी
विषय : विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

चर्चा में क्यों?
हाल ही में, सर्न ने व्हाइट रैबिट सहयोग की शुरुआत की।
पृष्ठभूमि:
- CERN, जिसे आधिकारिक तौर पर यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन के रूप में जाना जाता है, वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध केंद्र है। यह मुख्य रूप से मौलिक भौतिकी के लिए समर्पित है, जिसका मुख्य उद्देश्य ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करना और इसकी संरचना और तंत्र को समझना है।
व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी के बारे में
- व्हाइट रैबिट (डब्ल्यूआर) सर्न में निर्मित एक नवीन प्रौद्योगिकी है, जो विविध अनुप्रयोगों में समन्वयन के लिए उल्लेखनीय उप-नैनोसेकंड सटीकता और पिकोसेकंड परिशुद्धता प्रदान करती है।
- यह प्रौद्योगिकी खुला स्रोत है, मान्यता प्राप्त मानकों का पालन करती है, तथा इसे प्रिसीजन टाइम प्रोटोकॉल (PTP) में एकीकृत किया गया है, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स (IEEE) द्वारा निगरानी किया जाने वाला एक वैश्विक उद्योग मानक है।
- कण भौतिकी से परे, व्हाइट रैबिट ओपन-सोर्स सहयोग और नवाचार का एक उल्लेखनीय उदाहरण है।
कण भौतिकी से परे अनुप्रयोग:
- वित्त क्षेत्र: व्हाइट रैबिट का उपयोग वर्तमान में वित्तीय प्रणालियों में किया जाता है।
- अनुसंधान अवसंरचना: इसका विभिन्न अनुसंधान सुविधाओं में व्यावहारिक अनुप्रयोग होता है।
- भावी क्वांटम इंटरनेट: आगामी क्वांटम इंटरनेट में संभावित उपयोग के लिए मूल्यांकन किया जा रहा है।
- वैश्विक समय प्रसार: यह वैश्विक समय प्रसार प्रौद्योगिकियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जिससे उपग्रहों पर निर्भरता कम हो सकती है।
स्रोत: सर्न
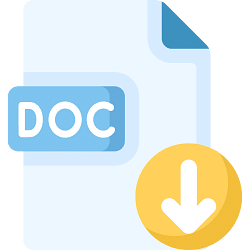 |
Download the notes
UPSC Daily Current Affairs (Hindi) - 2nd April 2024
|
Download as PDF |
भारत में तेंदुओं की स्थिति 2022
विषय : पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

चर्चा में क्यों?
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत में तेंदुओं की स्थिति 2022 पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें भारत के 20 राज्यों को शामिल किया गया है और तेंदुओं के अपेक्षित आवास के लगभग 70% पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
पृष्ठभूमि
- पांचवें चक्र में तेंदुआ जनसंख्या का आकलन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा राज्य वन विभागों के साथ साझेदारी में किया गया।
भारत में तेंदुओं की स्थिति पर 2022 रिपोर्ट की मुख्य बातें
- भारत में तेंदुओं की आबादी 2018 में 12,852 से 8% बढ़कर 2022 में 13,874 हो गई।
- शिवालिक परिदृश्य में तेंदुओं की लगभग 65% आबादी संरक्षित क्षेत्रों के बाहर रहती है, तथा केवल एक तिहाई ही संरक्षित क्षेत्रों के भीतर रहती है।
- मध्य भारत में तेंदुओं की आबादी स्थिर या थोड़ी बढ़ रही है (2018: 8071, 2022: 8820), जबकि शिवालिक पहाड़ियों और गंगा के मैदानों में 3.4% प्रति वर्ष की दर से गिरावट देखी गई (2018: 1253, 2022: 1109)।
- तेंदुए की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश (3,907) में पाई जाती है, इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु का स्थान आता है।
- ओडिशा में तेंदुओं की संख्या 2018 में 760 से घटकर 2022 में 562 हो गई, और उत्तराखंड में तेंदुओं की संख्या 2018 में 839 से घटकर 2022 में 652 हो गई।
- तेंदुओं पर बाघों के कारण नियामक दबाव के बावजूद, संरक्षित क्षेत्रों के बाहर के क्षेत्रों की तुलना में टाइगर रिजर्व में तेंदुओं की संख्या अधिक है।
- सामान्य खतरों में झाड़ी के मांस के लिए शिकार का अवैध शिकार, बाघ और तेंदुए के उत्पादों के लिए लक्षित शिकार, तथा खनन जैसी मानवीय गतिविधियों के कारण आवास का विनाश शामिल है।
- ओडिशा में 2018 से 2023 के बीच वन्यजीव तस्करों को 59 तेंदुओं की खालों के साथ पकड़ा गया, जबकि सड़क दुर्घटनाएं तेंदुओं की मौतों का एक महत्वपूर्ण कारण हैं।
मध्य भारत और पूर्वी घाट परिदृश्य
- इस क्षेत्र में तेंदुओं की सबसे बड़ी आबादी रहती है, जो बाघ संरक्षण ढांचे के तहत संरक्षण प्रयासों के कारण बढ़ रही है।
तेंदुओं को खतरा
- तेंदुओं के समक्ष आने वाले विभिन्न खतरों में अवैध शिकार, आवास का विनाश और सड़क दुर्घटनाएं शामिल हैं, जो उनकी आबादी पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं।
तेंदुओं की आबादी की तुलना
- भारत के विभिन्न क्षेत्रों में तेंदुओं की आबादी के विश्लेषण से अलग-अलग रुझान सामने आए हैं, कुछ क्षेत्रों में उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है, जबकि अन्य क्षेत्रों में गिरावट आ रही है।
संरक्षित क्षेत्रों का प्रभाव
- बाघ अभयारण्यों में तेंदुओं की सघनता चुनौतियों के बावजूद तेंदुओं की आबादी को बनाए रखने में संरक्षित क्षेत्रों के महत्व को उजागर करती है।
स्रोत : टाइम्स ऑफ इंडिया
भारत की एचआईवी/एड्स प्रतिक्रिया का एआरटी
विषय: विज्ञान और प्रौद्योगिकी

चर्चा में क्यों?
1 अप्रैल, 2004 को भारत ने एचआईवी से पीड़ित व्यक्तियों (पीएलएचआईवी) के लिए निःशुल्क एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी (एआरटी) की शुरुआत की, ताकि इसकी पहुंच और सामर्थ्य संबंधी चुनौतियों का समाधान किया जा सके।
एचआईवी/एड्स का उद्भव और प्रारंभिक चुनौतियाँ
- 1980 के दशक में एचआईवी/एड्स के प्रकोप ने वैश्विक स्वास्थ्य संकट को जन्म दिया, जिसका प्रभाव प्रारंभ में हाशिए पर पड़े समूहों पर पड़ा।
- प्रारंभ में इसे जीआरआईडी कहा गया, लेकिन बाद में इसे एचआईवी और एड्स के नाम से जाना जाने लगा, जिससे व्यापक भय और अनिश्चितता फैल गई।
- एचआईवी/एड्स के साथ सामाजिक कलंक, भेदभाव और प्रभावी उपचार विकल्पों का अभाव भी जुड़ा हुआ था।
उपचार उपलब्ध न होने के कारण मौत की सजा
- प्रारंभ में, प्रभावी उपचार के अभाव के कारण एचआईवी/एड्स को अक्सर घातक माना जाता था।
- इस रोग ने मुख्य रूप से हाशिए पर पड़े समुदायों को प्रभावित किया, लेकिन बाद में विविध पृष्ठभूमियों के व्यक्तियों को भी प्रभावित किया।
- एचआईवी/एड्स से पीड़ित लोगों को सामाजिक बहिष्कार, नौकरी छूटने और पारिवारिक अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है।
उपचार तक सीमित पहुंच और उपलब्ध एआरटी की उच्च लागत
- वैश्विक मान्यता के बावजूद, एचआईवी/एड्स के उपचार तक पहुंच सीमित थी, तथा AZT और HAART जैसी एंटीरेट्रोवाइरल दवाएं बहुत महंगी थीं।
- HAART एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन कई लोगों के लिए वह वहनीय नहीं थी, विशेषकर सीमित संसाधनों वाले क्षेत्रों में।
भारत में निःशुल्क कला का शुभारंभ
- 2004 में, भारत ने उपचार की पहुंच और सामर्थ्य में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए निःशुल्क एआरटी की शुरुआत की।
- इस पहल का उद्देश्य सभी पीएलएचआईवी को जीवन रक्षक दवा उपलब्ध कराना था, चाहे उनकी वित्तीय स्थिति कुछ भी हो।
निःशुल्क एआरटी का प्रभाव और महामारी को रोकने में इसकी भूमिका
- निःशुल्क एआरटी कार्यक्रम का दो दशकों में महत्वपूर्ण विस्तार हुआ, जिससे पूरे भारत में 1.8 मिलियन पीएलएचआईवी के लिए उपचार की पहुंच बढ़ी।
- इस पहल के प्रमुख परिणाम थे बेहतर स्वास्थ्य परिणाम, कम मृत्यु दर, तथा कम एचआईवी संक्रमण।
- निःशुल्क एआरटी से न केवल जीवन अवधि बढ़ी, बल्कि जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ, जिससे एचआईवी प्रसार में कमी आई।
पूरक पहल और रोगी-केंद्रित दृष्टिकोण
- निःशुल्क एआरटी की सफलता को निदान, संक्रमण की रोकथाम और अवसरवादी संक्रमण प्रबंधन जैसी अतिरिक्त सेवाओं द्वारा संपूरित किया गया।
- रोगी-केंद्रित दृष्टिकोण, विस्तारित दवा आपूर्ति, उन्नत उपचार अनुपालन प्रदान करना।
चुनौतियाँ और भविष्य की दिशाएँ
- चुनौतियों में उपचार शुरू होने में देरी, अनुवर्ती कार्रवाई के लिए मरीज का अभाव, तथा दूरदराज के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की सीमाएं शामिल हैं।
- आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ाना, निजी क्षेत्र को शामिल करना और स्वास्थ्य कार्यक्रमों को एकीकृत करना भविष्य की सफलता के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- एनएसीपी चरण 5 का लक्ष्य 2025 तक नए संक्रमणों और एड्स से संबंधित मौतों को 80% तक कम करना है, जिसके लिए अधिक परीक्षण और उपचार कवरेज की आवश्यकता होगी।
निष्कर्ष
- भारत की निःशुल्क एआरटी पहल एचआईवी/एड्स से लड़ने में महत्वपूर्ण रही है, जिसमें सुलभ स्वास्थ्य सेवा, निरंतर वित्त पोषण और सामुदायिक भागीदारी पर जोर दिया गया है।
- कार्यक्रम की सफलता संक्रामक रोगों के प्रबंधन में राजनीतिक प्रतिबद्धता और रोगी-केंद्रित देखभाल के महत्व को उजागर करती है।
स्रोत : द हिंदू
अटल सुरंग
विषय : भूगोल

चर्चा में क्यों?
लाहौल और स्पीति जिलों में अटल सुरंग के पास ताजा बर्फबारी के कारण मनाली-लेह राजमार्ग हाल ही में अवरुद्ध हो गया।
अटल सुरंग के बारे में:
- पूर्व में रोहतांग सुरंग के नाम से जानी जाने वाली अटल सुरंग को दुनिया की सबसे लंबी ऊंचाई वाली सुरंग माना जाता है।
- हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला में समुद्र तल से लगभग 3,100 मीटर (10,171 फीट) की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर हिमाचल प्रदेश में स्थित है और रोहतांग दर्रे से होकर गुजरता है।
- 9.02 किलोमीटर की लंबाई में फैली यह सुरंग पूरे वर्ष मनाली और लाहौल एवं स्पीति घाटी के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क स्थापित करती है, जिससे भारी बर्फबारी के कारण लगभग छह महीने तक चलने वाला पिछला मौसमी अलगाव समाप्त हो जाता है।
- घोड़े की नाल के आकार की, दो लेन वाली एकल ट्यूब के रूप में डिजाइन की गई इस सुरंग में अर्ध-अनुप्रस्थ वेंटिलेशन प्रणाली, प्रत्येक 500 मीटर पर आपातकालीन निकास, निकासी प्रकाश व्यवस्था, प्रसारण प्रणाली और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अग्नि हाइड्रेंट की व्यवस्था है।
स्रोत : हिंदुस्तान टाइम्स
|
2698 docs|916 tests
|