लक्ष्मीकांत सारांश: संघ लोक सेवा आयोग | Famous Books for UPSC CSE (Summary & Tests) in Hindi PDF Download
संघ लोक सेवा आयोग
- संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) भारत में सरकारी अधिकारियों की भर्ती के लिए मुख्य संगठन है।
- यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता है, जिसका अर्थ है कि इसे भारत के संविधान द्वारा स्थापित किया गया था।
- UPSC के बारे में जानकारी संविधान के भाग XIV के अनुच्छेद 315 से 323 में उपलब्ध है।
- संविधान के इस हिस्से में विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें शामिल हैं:
- UPSC की संरचना।
- इसके सदस्यों की नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया।
- UPSC की स्वतंत्रता।
- जो शक्तियाँ इसे प्राप्त हैं।
- जो कार्य यह करता है।
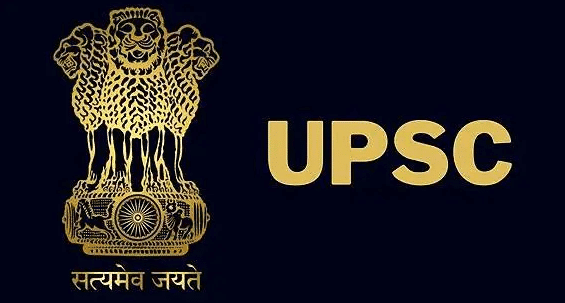
संरचना
- UPSC (संघ लोक सेवा आयोग) का नेतृत्व एक अध्यक्ष और अन्य सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- संविधान आयोग के लिए सदस्यों की संख्या निर्दिष्ट नहीं करता है; इसके बजाय, यह राष्ट्रपति को यह तय करने की अनुमति देता है कि कितने सदस्य होंगे।
- आयोग के सदस्य बनने के लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है, सिवाय इसके कि कम से कम आधे सदस्यों को भारत सरकार या किसी राज्य सरकार में कम से कम दस वर्षों का अनुभव होना चाहिए।
- संविधान राष्ट्रपति को आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें निर्धारित करने का अधिकार भी देता है।
- अतिरिक्त रूप से, राष्ट्रपति यह तय कर सकते हैं कि आयोग के पास कितने कर्मचारियों की संख्या होगी और उनकी कार्य परिस्थितियाँ क्या होंगी।
- अध्यक्ष और सदस्य छह वर्षों की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले हो, सेवा करते हैं।
- वे किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं।
- सदस्यों को उनके कार्यकाल समाप्त होने से पहले हटाया जा सकता है, लेकिन यह संविधान में निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए।
- यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है, या यदि अध्यक्ष किसी कारणवश अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर पाते हैं, तो राष्ट्रपति किसी सदस्य को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकते हैं।
- कार्यकारी अध्यक्ष तब तक कार्य करते रहेंगे जब तक नया अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया जाता या मूल अध्यक्ष अपनी जिम्मेदारियों को फिर से ग्रहण नहीं कर लेते।
हटाना
अगर सदस्य को दिवालिया घोषित किया जाता है (मतलब वे बैंकक्रप्ट हैं)।
- अगर सदस्य अपने आधिकारिक जिम्मेदारियों के बाहर किसी भी भुगतान वाले काम को अपने कार्यकाल के दौरान अपनाता है।
- अगर राष्ट्रपति विश्वास करते हैं कि सदस्य मानसिक या शारीरिक विकलांगता के कारण भूमिका के लिए अयोग्य हैं।
- इसके अतिरिक्त, राष्ट्रपति किसी भी सदस्य को अनुशासनहीनता के लिए हटा सकते हैं। हालांकि, इस मामले में:
- मामले को जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय में भेजा जाना चाहिए।
- अगर सर्वोच्च न्यायालय हटाने का समर्थन करता है और सुझाव देता है, तो राष्ट्रपति इसे आगे बढ़ा सकते हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य है।
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच के दौरान, राष्ट्रपति के पास UPSC के अध्यक्ष या सदस्य को निलंबित करने का अधिकार है।
संविधान अनुशासनहीनता को इस प्रकार परिभाषित करता है:
- अगर सदस्य भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा किए गए किसी भी अनुबंध या समझौते में शामिल हैं।
- अगर सदस्य किसी भी प्रकार से ऐसे अनुबंध या समझौते से लाभान्वित होते हैं, सदस्य के रूप में और एक पंजीकृत कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ समान रूप से।
कार्य
- यह सभी-भारत सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं, और केंद्रीय प्रशासित क्षेत्रों में सार्वजनिक सेवाओं के लिए परीक्षा आयोजित करता है।
- यह राज्यों की मदद करता है, अगर दो या अधिक राज्य इसकी मांग करते हैं, विशेष कौशल वाले उम्मीदवारों की आवश्यकता वाली सेवाओं के लिए संयुक्त भर्ती योजनाएँ बनाने और प्रबंधित करने में।
यह राज्य की जरूरतों को संबोधित करता है जब राज्य के गवर्नर इसकी मांग करते हैं, भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ। यह विभिन्न मामलों पर सलाह प्रदान करता है, जिसमें:
- सिविल सेवाओं और सिविल पदों के लिए भर्ती विधियों।
- सिविल सेवाओं में नियुक्तियों, पदोन्नतियों, और स्थानांतरण के लिए आदर्शों का पालन करना, जिसमें उम्मीदवारों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना शामिल है।
- भारत सरकार के तहत सेवा देने वाले व्यक्तियों के संबंध में अनुशासनात्मक मामले, जिनमें इन मुद्दों से संबंधित स्मारक और याचिकाएँ शामिल हैं।
- सिविल सेवकों द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों से संबंधित कानूनी मामलों में अपनी रक्षा करते समय उठाए गए कानूनी खर्चों की पुनर्भुगतान के लिए दावे।
- भारत सरकार के लिए काम करते समय सिविल सेवकों द्वारा प्राप्त चोटों के लिए पेंशन पुरस्कारों के दावे, साथ ही ऐसे पुरस्कारों की राशि से संबंधित प्रश्न।
- राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित कोई अन्य मामले।
सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया है कि यदि सरकार उपरोक्त मामलों पर UPSC से परामर्श नहीं करती है, तो प्रभावित सिविल सेवक अदालत में remedy की मांग नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि UPSC से परामर्श में कोई भी गलती या इसके बिना कार्य करना सरकार के निर्णयों को अमान्य नहीं बनाता। इस प्रकार, UPSC से परामर्श की आवश्यकता को अनिवार्य के बजाय निर्देशात्मक माना गया है।
इसके अलावा, UPSC द्वारा चयन किसी उम्मीदवार को नौकरी का अधिकार नहीं देता। हालांकि, सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह निष्पक्षता और बिना पूर्वाग्रह या बुरी नीयत के कार्य करे।
संसद UPSC को संघ सेवाओं से संबंधित अतिरिक्त जिम्मेदारियाँ सौंप सकती है। यह किसी भी प्राधिकरण, कॉर्पोरेट निकाय, या सार्वजनिक संस्थान के कर्मियों की प्रणाली को UPSC के अधिकार क्षेत्र में भी रख सकती है। इसका मतलब है कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के माध्यम से UPSC के अधिकार को बढ़ाया जा सकता है।
UPSC अपनी कार्यप्रणाली के बारे में एक वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति फिर इस रिपोर्ट को दोनों सदनों की संसद में प्रस्तुत करते हैं, साथ ही एक ज्ञापन जो यह बताता है कि आयोग की सलाह का पालन क्यों नहीं किया गया और इसके कारण।
सीमाएँ
UPSC कुछ मामलों में शामिल नहीं है, अर्थात् यह निम्नलिखित मुद्दों पर सलाह या इनपुट प्रदान नहीं करता है:
सीमाएं
- UPSC कुछ मामलों में शामिल नहीं है, जिसका अर्थ है कि यह निम्नलिखित मुद्दों पर सलाह या योगदान नहीं देता:
- किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए नौकरियों या पदों के लिए आरक्षण करते समय।
- सेवाओं और पदों में नियुक्तियों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावों पर विचार करते समय।
- यदि:
- व्यक्ति संभवतः एक वर्ष से अधिक उस पद को नहीं धारण करेगा।
- सार्वजनिक हित के लिए नियुक्ति करना आवश्यक है, और UPSC से परामर्श करने में अनावश्यक देरी होगी।
- केंद्रीय सेवाओं के समूह C और समूह D में कई नियुक्तियों के लिए।
- बोर्डों, आयोगों, न्यायाधिकरणों और समान प्राधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियों के लिए।
- विदेश में भारतीय मिशनों के प्रमुखों के पदों के लिए नियुक्तियों के लिए (उदाहरण के लिए, राजदूत, उच्चायुक्त, मंत्री, आयोगकर्ता, महानिदेशक, प्रतिनिधि, एजेंट)।
- राष्ट्रपति कुछ पदों, सेवाओं और मामलों को UPSC की जिम्मेदारियों से बाहर कर सकता है।
- संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति सभी-भारत सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं के लिए नियम बना सकता है जो यह निर्दिष्ट करते हैं कि कब UPSC से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।
- राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए किसी भी नियम को प्रत्येक संसद के सदन में कम से कम 14 दिनों के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- संसद के पास इन नियमों को बदलने या हटाने का अधिकार है।
- इस प्रावधान के आधार पर, राष्ट्रपति ने UPSC (परामर्श से छूट) नियम 1958 के रूप में जाने जाने वाले नियम स्थापित किए हैं।
- ये नियम समय-समय पर अपडेट किए गए हैं।
भूमिका
संविधान के अनुसार, UPSC को भारत में 'मेरिट प्रणाली का प्रहरी' माना जाता है। इसका मुख्य ध्यान अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं - दोनों समूह A और समूह B के लिए भर्ती पर है। जब पूछा जाता है, तो UPSC सरकार को पदोन्नति और अनुशासनात्मक मामलों पर सलाह देती है।
हालांकि, यह सेवाओं के वर्गीकरण, वेतन और सेवा की शर्तों, कैडर प्रबंधन, या प्रशिक्षण जैसे मुद्दों से नहीं निपटती। ये विषय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं, जो कि मंत्रालय के तीन विभागों में से एक है, जो कार्मिक, जनशिकायत और पेंशन से संबंधित हैं। इस प्रकार, UPSC केवल एक केंद्रीय भर्ती एजेंसी के रूप में कार्य करती है, जबकि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग भारत में केंद्रीय कार्मिक एजेंसी है।
UPSC की भूमिका सीमित है; इसकी सिफारिशें केवल सलाहकारी होती हैं और सरकार के लिए अनिवार्य नहीं होती हैं। यह संघ सरकार पर निर्भर करता है कि वह इन सिफारिशों को स्वीकार करे या अस्वीकार करे। सरकार ऐसे नियम भी बना सकती है जो UPSC की सलाहकारी भूमिकाओं को परिभाषित करते हैं।
1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) के गठन ने UPSC की अनुशासनात्मक मामलों में जिम्मेदारियों को प्रभावित किया है। इसका कारण यह है कि दोनों UPSC और CVC सरकार को सिविल सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में सलाह देते हैं। जब ये दो संगठन विरोधाभासी सलाह देते हैं, तो संघर्ष उत्पन्न हो सकता है।
हालांकि, UPSC, एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय होने के नाते, CVC पर एक लाभ में है, जो एक कार्यकारी प्रस्ताव के माध्यम से स्थापित की गई थी और 2003 में वैधानिक स्थिति प्राप्त की थी।
|
125 videos|399 docs|221 tests
|
















