लक्ष्मीकांत सारांश: राज्य मानवाधिकार आयोग | Famous Books for UPSC CSE (Summary & Tests) in Hindi PDF Download
परिचय
मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोगों की स्थापना करता है। राज्य मानवाधिकार आयोग राज्य सरकार द्वारा बनाया जाता है।
राज्य मानवाधिकार आयोग, तमिलनाडु
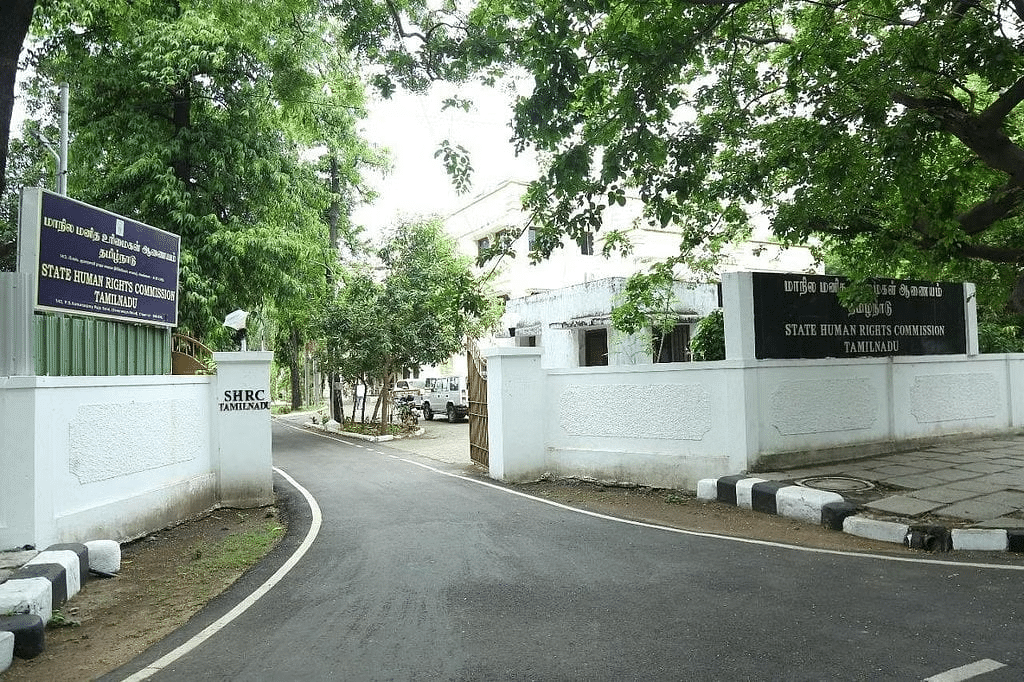
- राज्य मानवाधिकार आयोग केवल उन मामलों की जांच करता है जो संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची (सूची-II) और समवर्ती सूची (सूची-III) में सूचीबद्ध हैं।
- यदि कोई मामला पहले से ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या किसी अन्य वैधानिक आयोग द्वारा जांच में है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग हस्तक्षेप नहीं करता है।
- केंद्र सरकार संघ शासित प्रदेशों (जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख को छोड़कर) में मानवाधिकार से संबंधित कार्यों को राज्य मानवाधिकार आयोगों को सौंप सकती है।
- दिल्ली जैसे संघ शासित प्रदेशों के लिए, मानवाधिकार कार्यों का संचालन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा किया जाता है।
संरचना
आयोग एक बहु-सदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और दो सदस्य होते हैं। अध्यक्ष, जो एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होना चाहिए, और सदस्य, या तो सेवा में या सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय या जिला न्यायाधीश होते हैं जिनके पास जिला न्यायाधीश के रूप में कम से कम सात वर्षों का अनुभव होता है, या ऐसे व्यक्ति जिनके पास व्यावहारिक मानवाधिकार अनुभव होता है।
नियुक्ति प्रक्रिया
राज्यपाल, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति के सिफारिशों के आधार पर अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। समिति में विधानसभा के अध्यक्ष, राज्य गृह मंत्री और विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। जिन राज्यों में विधान परिषद होती है, उनके अध्यक्ष और परिषद में विपक्ष के नेता भी समिति का हिस्सा होते हैं। वर्तमान न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना आवश्यक है।
अवधि और पात्रता
अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा अवधि तीन वर्ष है या 70 वर्ष की आयु तक, जो पहले आए। पुनर्नियुक्ति संभव है। कार्यकाल के बाद, वे राज्य या केंद्रीय सरकारों के तहत आगे की नौकरी नहीं मांग सकते।
निकालना
हालाँकि इन्हें राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन निकालना राष्ट्रपति के अधिकार में है। आधार में दिवालियापन, कार्यों के बाहर भुगतान वाली नौकरी करना, मानसिक या शारीरिक असमर्थता, अस्वस्थ मन, सजा जो कारावास की ओर ले जाती है, या सिद्ध दुराचार शामिल हैं। दुराचार या असमर्थता के मामलों में, राष्ट्रपति मामले को जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय को संदर्भित करते हैं और न्यायालय की सलाह के आधार पर कार्रवाई करते हैं।
सेवा की शर्तें
वेतन, भत्ते, और सेवा की शर्तें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं और नियुक्ति के बाद अध्यक्ष या सदस्यों के लिए अनुकूलता को बदल नहीं सकतीं।
उद्देश्य
ये प्रावधान आयोग के कार्य में स्वायत्तता, स्वतंत्रता, और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए हैं।
कार्य और कार्यप्रणाली
आयोग के कार्य
- जांच: मानवाधिकार उल्लंघनों या सार्वजनिक सेवकों द्वारा रोकथाम में लापरवाही की जांच करना, जो स्वप्रेरणा, याचिकाओं, या न्यायालय के आदेशों पर शुरू की जा सकती है।
- हस्तक्षेप: कथित मानवाधिकार उल्लंघनों से संबंधित चल रही न्यायालय की कार्यवाही में हस्तक्षेप करना।
- निरीक्षण: जेलों और निरोध स्थलों का दौरा करना ताकि जीवन की परिस्थितियों का आकलन किया जा सके और सिफारिशें दी जा सकें।
- सुरक्षा की समीक्षा: मानवाधिकारों के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा की जांच करना, प्रभावी कार्यान्वयन के उपाय सुझाना।
- आतंकवाद का समाधान: मानवाधिकारों के आनंद में बाधा डालने वाले कारकों का आकलन करना, जिसमें आतंकवाद के कृत्य शामिल हैं, और सुधारात्मक उपायों का प्रस्ताव करना।
- अनुसंधान: मानवाधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और बढ़ावा देना।
- मानवाधिकार साक्षरता: मानवाधिकारों के ज्ञान का प्रचार करना, उपलब्ध सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करना।
- एनजीओ समर्थन: मानवाधिकार कार्य में शामिल गैर सरकारी संगठनों (NGOs) का समर्थन करना।
- अतिरिक्त कार्य: मानवाधिकारों के प्रचार के लिए किसी अन्य आवश्यक कार्यों को करना।
आयोग का कार्यप्रणाली
आयोग के पास अपनी प्रक्रियाओं को विनियमित करने का अधिकार है, जिसमें यह एक नागरिक न्यायालय की शक्तियों से युक्त है और इसका कार्य न्यायिक प्रकृति का है। यह राज्य सरकार या किसी अधीनस्थ प्राधिकरण से जानकारी या रिपोर्ट मांग सकता है।
आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप के एक वर्ष के भीतर के मामलों की जांच करने तक सीमित है। इस अवधि के बाद, यह मुद्दे की जांच नहीं कर सकता।
गुजरात राज्य मानवाधिकार आयोग

जांच के दौरान या उसके बाद के चरण:
- मुआवजा: राज्य सरकार को पीड़ित को मुआवजा देने की सिफारिश करें।
- कानूनी कार्रवाई: जिम्मेदार सार्वजनिक सेवक के खिलाफ कार्यवाही या कार्रवाई शुरू करने का सुझाव दें।
- अंतरिम राहत: पीड़ित के लिए तात्कालिक अंतरिम राहत की सिफारिश करें।
- न्यायिक हस्तक्षेप: सर्वोच्च न्यायालय या राज्य उच्च न्यायालय से आवश्यक निर्देश, आदेश या रिट्स की मांग करें।
यह स्पष्ट है कि आयोग के कार्य मुख्यतः सिफारिशात्मक हैं। इसके पास उल्लंघनकर्ताओं को सजा देने या पीड़ितों को राहत देने, जिसमें मौद्रिक मुआवजा शामिल है, की शक्ति नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी सिफारिशें राज्य सरकार या प्राधिकरण पर बाध्यकारी नहीं हैं। हालाँकि, उन्हें एक महीने के भीतर आयोग को उठाए गए कदमों के बारे में सूचित करना चाहिए।
आयोग राज्य सरकार को वार्षिक या विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, जिन्हें राज्य विधान मंडल में पेश किया जाता है। इन रिपोर्टों में आयोग की सिफारिशों पर उठाए गए कदमों का एक ज्ञापन और किसी भी अस्वीकृति के कारण शामिल होते हैं।
मानवाधिकार न्यायालय
मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना:
मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम (1993) प्रत्येक जिले में मानवाधिकार उल्लंघनों के मामलों की सुनवाई की प्रक्रिया को तेज करने के लिए मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना को अनिवार्य करता है।
मुख्य बिंदु:
- अधिकारिता: राज्य सरकारें, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करके, इन न्यायालयों की स्थापना कर सकती हैं।
- अभियोजकों की नियुक्ति: प्रत्येक मानवाधिकार न्यायालय एक सार्वजनिक अभियोजक को नियुक्त करता है, या राज्य सरकार उस न्यायालय में मामलों का संचालन करने के लिए सात वर्षों के अनुभव वाले अधिवक्ता को विशेष सार्वजनिक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है।
2019 संशोधन अधिनियम
मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रावधान:
- अध्यक्ष की पात्रता: संशोधन में यह अनुमति दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके व्यक्ति को, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के अलावा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सके।
- सदस्यता वृद्धि: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में मानवाधिकारों के ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव वाले सदस्यों की संख्या दो से बढ़ाकर तीन कर दी गई है, जिसमें कम से कम एक महिला शामिल है।
- एक्स-ऑफिशियो सदस्य: राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्ष, जैसे कि BCs का राष्ट्रीय आयोग, बाल अधिकारों के संरक्षण का राष्ट्रीय आयोग, और विकलांग लोगों के लिए मुख्य आयुक्त को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एक्स-ऑफिशियो सदस्य के रूप में नामित किया गया है।
- कार्यकाल में कटौती: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल, साथ ही राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्यकाल, पांच से घटाकर तीन वर्ष कर दिया गया है, पुनर्नियुक्ति के लिए पात्रता के साथ।
- राज्य आयोग अध्यक्ष की पात्रता: एक व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है, अब राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है।
- कार्य का हस्तांतरण: केंद्र सरकार मानवाधिकार संबंधी कार्यों को संघ शासित क्षेत्रों में राज्य मानवाधिकार आयोगों को सौंप सकती है, दिल्ली को छोड़कर, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधिकार क्षेत्र में है।
- प्रशासनिक शक्तियाँ: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महासचिव अध्यक्ष के नियंत्रण में प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियाँ (न्यायिक कार्य और विनियमन बनाने को छोड़कर) का प्रयोग करते हैं।
- राज्य आयोग सचिव की शक्तियाँ: राज्य मानवाधिकार आयोग के सचिव अध्यक्ष के नियंत्रण में प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करते हैं।
|
125 videos|399 docs|221 tests
|















