सौंदर्यशास्त्र और साम्राज्य, लगभग 300–600 ईसा पूर्व - 2 | Famous Books for UPSC CSE (Summary & Tests) in Hindi PDF Download
प्राचीन भारतीय राज्यों के राजस्व स्रोत
नारद स्मृति और कमंदक का नीति-सार
- नारद स्मृति (18.48) के अनुसार, विषयों को राजा को सुरक्षा के बदले में राजस्व देना होता है।
- कमंदक का नीति-सार (5.84–85) राजा को सलाह देता है कि वे कर लगाने में एक फूलवाले या दूधवाले की तरह व्यवहार करें। जैसे ये पेशेवर अपने पौधों और जानवरों का सही समय पर ध्यान रखते हैं, वैसे ही राजा को विषयों की मदद पैसों और आवश्यकताओं के साथ करनी चाहिए और अन्य समय में उन पर कर लगाना चाहिए।
- कमंदक यह भी चेतावनी देता है कि जो राजसी अधिकारी भ्रष्टाचार के माध्यम से धनवान बन जाते हैं, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए, जैसे एक शल्य चिकित्सक एक फोड़ा का इलाज करता है।
नीति-सार और अर्थशास्त्र
- नीति-सार, अर्थशास्त्र की तरह, राजसी खजाने और विभिन्न राजस्व स्रोतों के महत्व को उजागर करता है।
- समुद्रगुप्त जैसे राजाओं ने संभवतः अपने सैन्य अभियानों को राजस्व अधिशेषों के माध्यम से वित्तपोषित किया।
गुप्त उत्कीर्णन और राजस्व विभाग
- गुप्त उत्कीर्णन राजस्व विभाग की अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, जिसमें अक्षपातलाधिकृत जैसे भूमिकाएँ शामिल हैं, जो राजसी रिकॉर्ड रखते थे।
- गया की ताम्रपत्र उत्कीर्णन में गोपालस्वामिन का उल्लेख है, जो समुद्रगुप्त के शासनकाल में एक अक्षपातलाधिकृत थे, जिन्होंने ताम्रपत्र की उत्कीर्णन का आदेश दिया।
- रिकॉर्ड रखने वाले, जिन्हें पुस्तपाल कहा जाता है, भूमि हस्तांतरण का ट्रैक रखते थे।
वित्तीय शब्द
- गुप्त उत्कीर्णनों में वित्तीय शब्दों जैसे कर, बाली, उद्रंग, उपरिकर, और हिरण्य का उल्लेख है।
- वकटक उत्कीर्णनों में क्लिप्त और उपक्लिप्त जैसे शब्दों का उल्लेख है, साथ ही विष्टि या मजबूर श्रम भी।
व्याख्या की चुनौतियाँ

- प्राचीन शिलालेखों में कुछ वित्तीय शब्दों के सटीक अर्थों की व्याख्या करना चुनौतीपूर्ण है। भाग शब्द का उल्लेख राजा के अनाज के हिस्से के लिए किया गया था, जो आमतौर पर कृषि उत्पाद का 1/6 था, जैसा कि नारद स्मृति में वर्णित है। पाहारपुर और बैग्राम प्लेटें इसका समर्थन करती हैं, stating कि दान से प्राप्त पुण्य का 1/6 हिस्सा राजा के पास जाएगा। हालांकि, 1/6 एक पारंपरिक आंकड़ा था, और प्राचीन राज्यों द्वारा किसानों से एकत्र की गई वास्तविक मात्रा के बारे में सीमित जानकारी है। पहले की मनुस्मृति (7.130–132) भी इस भिन्नता को दर्शाती है, यह सुझाव देते हुए कि राजा अपने विषयों से फसल की उपज का 1/6, 1/8 या 1/12 ले सकता है।
प्राचीन और प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में भूमि स्वामित्व
प्राचीन और प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में भूमि का स्वामित्व एक विवादित विषय है, जिसमें मुख्यतः तीन प्रकार के स्वामित्व पर विचार किया गया है: सामुदायिक/कॉर्पोरेट स्वामित्व (जहां गांव समुदाय भूमि का मालिक होता है), राजकीय स्वामित्व (जहां राजा भूमि का मालिक होता है), और निजी स्वामित्व (जहां व्यक्तिगत लोग भूमि के मालिक होते हैं)। धर्मशास्त्र परंपरा के विभिन्न ग्रंथों में भूमि अधिकारों पर विभिन्न विचार हैं, और कभी-कभी ये विरोधाभासी बयान भी देते हैं।
- कुछ ग्रंथों का सुझाव है कि गांव समुदाय भूमि से संबंधित मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, जैसे सीमा विवादों का निपटारा और भूमि बिक्री। उदाहरण के लिए, राजा को भूमि दान करते समय गांव समुदाय को सूचित करना अपेक्षित था। विष्णु स्मृति और पहले की मनुस्मृति यह संकेत देती हैं कि चरागाह भूमि को सामुदायिक संपत्ति माना जाता था और इसे विभाजित नहीं किया जा सकता था। गांव समुदाय के पास जल संसाधनों पर भी अधिकार प्रतीत होते हैं।
- पहले के स्रोतों ने भी भूमि संपत्ति की अविभाज्यता पर चर्चा की, यह सुझाव देते हुए कि इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए, गौतम स्मृति कहता है कि जो आजीविका का निर्माण करता है, उसे विभाजित नहीं किया जा सकता, और जैमिनी की मीमांसा सूत्र यह सुझाव देती है कि पृथ्वी सभी के लिए सामान्य है, और यहां तक कि एक सम्राट भी अपनी सभी भूमि नहीं दे सकता। यह विचार बाद में शाबरस्वामिन द्वारा उनके मीमांसा सूत्र पर टिप्पणी में समर्थित किया गया।
- प्राचीन भारत में भूमि स्वामित्व और उसके विभाजन पर विभिन्न दृष्टिकोण थे। कुछ प्रारंभिक स्रोतों का मानना था कि भूमि संपत्ति अविभाज्य होती है और इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए, गौतम स्मृति (28.46) ने सुझाव दिया कि जो योग-क्षेम (आजीविका) का निर्माण करता है, वह अविभाज्य है। इसी प्रकार, जैमिनी का मीमांसा सूत्र (6.7.3) 4/3 सदी BCE से कहता है कि पृथ्वी सभी के लिए सामान्य है और यहां तक कि एक शासक भी अपनी सभी भूमि का वितरण नहीं कर सकता। यह दृष्टिकोण बाद में शाबरस्वामिन द्वारा चौथी शताब्दी CE में दोहराया गया।
- प्राचीन भारत के शिलालेखों से भी संकेत मिलता है कि भूमि को गांव समुदाय की संपत्ति के रूप में देखा जाता था।
- हालांकि, भूमि के राजकीय स्वामित्व के विचार का समर्थन करने वाले अधिक सबूत हैं। मेगस्थनीज का संदर्भ देते हुए ग्रीक ग्रंथों ने दावा किया कि भारत की सभी भूमि राजा के पास थी। कौटिल्य ने भी राजा की भूमि का उल्लेख किया, जिसे sita भूमि कहा जाता था। प्राचीन भारतीय ग्रंथ अक्सर राजा को पृथ्वी से जोड़ते थे, और धर्मशास्त्र ने राजकीय भूमि स्वामित्व के विशिष्ट उदाहरण दिए जो कराधान को उचित ठहराते हैं। उदाहरण के लिए, मनुस्मृति (8.39) ने कहा कि राजा खानों से आधे खनिज का हकदार होता है क्योंकि वह पृथ्वी का स्वामी है और सुरक्षा प्रदान करता है।
- गुप्त काल की कानून की पुस्तकें राजकीय शक्ति और अधिकार के उत्थान को दर्शाती हैं, राजा के भूमि के मालिक होने का दावा करती हैं, हालांकि कुछ अस्पष्टता के साथ। कात्यायन स्मृति (श्लोक 16) ने राजा को भूमि का मालिक (भूमि-स्वामी) घोषित किया, जिसे किसानों की उपज का 1/4 हिस्सा लेने का अधिकार है। फिर भी, अगले श्लोक ने मानवों को भूमि के स्वामी के रूप में मान्यता दी क्योंकि वे वहां निवास करते हैं। नारद स्मृति (11.27, 42) ने राजा को किसानों के खेतों और houses को खाली करने का अधिकार दिया लेकिन ऐसे चरम कार्यों के खिलाफ सलाह दी क्योंकि ये गृहस्थों के जीवित रहने के लिए आवश्यक थे।
- बाद के स्रोतों, जैसे नरसिंह पुराण पर एक टिप्पणी ने स्पष्ट रूप से भूमि के राजकीय स्वामित्व की पुष्टि की, stating कि यह राजा की संपत्ति है, न कि कृषकों की। भट्टस्वामिन की 12वीं शताब्दी की टिप्पणी अर्थशास्त्र पर भी राजकीय भूमि स्वामित्व के आधार पर कराधान को उचित ठहराती है। इसके विपरीत, राजा के भूमि के स्वामित्व को नकारने वाला एक प्रारंभिक विचारधारा भी थी, जिसने तर्क किया कि कराधान राजा का वेतन है जो अपने विषयों की सुरक्षा के लिए है। जैमिनी और शाबरा इस दृष्टिकोण के प्रमुख समर्थक थे।
प्राचीन भारत में भूमि का राजकीय स्वामित्व

- प्राचीन ग्रंथों और शिलालेखों से यह प्रमाण मिलता है कि प्राचीन भारत में भूमि मुख्य रूप से राजा के पास थी। मेगस्थनीज का हवाला देते हुए ग्रीक ग्रंथ और कौटिल्य के राजकीय भूमि स्वामित्व के संदर्भ इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। धर्मशास्त्र, विशेषकर मनुस्मृति, सुझाव देती है कि राजा भूमि का मालिक था और संसाधनों का एक हिस्सा पाने का हकदार था, जो कराधान को उचित ठहराता है।
- हालांकि गुप्त काल की कानून की किताबों ने राजकीय भूमि स्वामित्व के विचार को मजबूत किया, लेकिन विरोधाभासी विचार भी थे। कुछ ग्रंथ, जैसे कात्यायन स्मृति और नारद स्मृति, कृषकों के अधिकारों को मान्यता देते हुए राजकीय दावों का समर्थन करते थे। बाद के स्रोत, जैसे नरसिंह पुराण और अर्थशास्त्र की टिप्पणियाँ, स्पष्ट रूप से भूमि के राजकीय स्वामित्व का उल्लेख करती हैं।
- शिलालेखों और भूमि दान ने राजकीय भूमि स्वामित्व के पक्ष में तर्क किया है। हालाँकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी भूमि राजा की थी। राजा द्वारा धार्मिक दान के लिए भूमि खरीदने के उदाहरण बताते हैं कि राजकीय स्वामित्व निरपेक्ष नहीं था।
- उत्तर भारत में 6वीं सदी BCE तक भूमि में निजी संपत्ति की अवधारणा उभरी और 300-600 CE तक यह स्थापित हो गई। इस अवधि के कानून की किताबों में भूमि के कब्जे, स्वामित्व और कानूनी शीर्षक पर चर्चा की गई है, और कई शिलालेख निजी भूमि लेनदेन को रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें ब्राह्मणों या धार्मिक संस्थानों को दान के लिए भूमि की खरीद शामिल है।
- एक पूर्व अध्याय में उल्लेख किया गया था कि उत्तर भारत में भूमि में निजी संपत्ति की अवधारणा लगभग 6वीं सदी BCE के आस-पास उभरी और लगभग 300-600 CE तक अच्छी तरह से स्थापित हो गई। इस अवधि में, कानूनी ग्रंथों ने संपत्ति, विशेष रूप से भूमि के कब्जे, स्वामित्व और कानूनी शीर्षक के बीच भेद करना शुरू किया।
- इन ग्रंथों ने भूमि के विभाजन, बिक्री और गिरवी रखने के संबंध में कानूनों का विवरण दिया। साहित्य में विभिन्न प्रकार के निजी भूमि लेनदेन का संदर्भ है जो शिलालेखों द्वारा समर्थित हैं। कई शिलालेख ऐसे व्यक्तियों का दस्तावेज करते हैं जो ब्राह्मणों या धार्मिक संस्थानों को दान देने के इरादे से भूमि खरीदते हैं।
- इस अवधि में भूमि में निजी संपत्ति के सबूत को और मजबूत किया गया है क्योंकि कानूनी ग्रंथों में संपत्ति के अधिकारों के विभिन्न पहलुओं के बीच भेद किया गया है। उस समय की कानून की किताबों ने ऐसे मुद्दों को संबोधित किया जैसे कब्जा, स्वामित्व और कानूनी शीर्षक, जो संपत्ति के अधिकारों की विकसित समझ को दर्शाते हैं।
- साहित्य और शिलालेखों में निजी भूमि लेनदेन के संदर्भ, विशेष रूप से उन जो ब्राह्मणों या धार्मिक संस्थानों के लिए दान से संबंधित हैं, निजी भूमि स्वामित्व और धार्मिक उद्देश्यों के लिए भूमि के हस्तांतरण की प्रथा को दर्शाते हैं।
- कुल मिलाकर, कानूनी ग्रंथों, साहित्यिक संदर्भों और शिलालेखों का संयोजन इस अवधि के दौरान उत्तर भारत में भूमि में निजी संपत्ति का एक समग्र चित्र प्रस्तुत करता है।
- उत्तर भारत में लगभग 6वीं सदी BCE में भूमि में निजी संपत्ति उभरी और 300-600 CE तक अच्छी तरह से स्थापित हो गई। इस अवधि के कानूनी ग्रंथों ने भूमि, विशेष रूप से भूमि के कब्जे, स्वामित्व और कानूनी शीर्षक के बीच भेद किया।
- ये ग्रंथ भूमि के विभाजन, बिक्री और गिरवी रखने के संबंध में कानूनों का विवरण देते हैं। साहित्य में विभिन्न प्रकार के निजी भूमि लेनदेन के संदर्भ हैं जो शिलालेखों द्वारा समर्थित हैं, जिसमें कई व्यक्तियों द्वारा ब्राह्मणों या धार्मिक संस्थानों को दान के लिए भूमि खरीदने का दस्तावेज शामिल है।
- कानूनी ग्रंथ संपत्ति के अधिकारों की विकसित समझ को दर्शाते हैं, जो कब्जा, स्वामित्व, और कानूनी शीर्षक जैसे मुद्दों को संबोधित करते हैं। निजी भूमि लेनदेन के संदर्भ निजी भूमि स्वामित्व और धार्मिक उद्देश्यों के लिए भूमि के हस्तांतरण की प्रथा को दर्शाते हैं। कुल मिलाकर, कानूनी ग्रंथों, साहित्य, और शिलालेखों के साक्ष्य इस अवधि के दौरान उत्तर भारत में भूमि में निजी संपत्ति का एक समग्र चित्र प्रस्तुत करते हैं।
- शिलालेखीय साक्ष्य यह सुझाव देते हैं कि कॉर्पोरेट या सामुदायिक भूमि स्वामित्व दुर्लभ था और यह एक पूर्व काल से संबंधित था। जबकि गांव समुदाय का भूमि से संबंधित मामलों में कुछ प्रभाव हो सकता था, यह कॉर्पोरेट या सामुदायिक स्वामित्व के बराबर नहीं था।
- लगभग 300 CE से, राजकीय और निजी भूमि स्वामित्व दोनों साहित्य और शिलालेखीय रिकॉर्ड में अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट हुए। पाठ्य बयानों में भेद विभिन्न दृष्टिकोण दर्शाता है, लेकिन शिलालेखीय साक्ष्य भूमि स्वामित्व की अवधारणाओं में परिवर्तन का संकेत देते हैं।
- 300 CE तक, राजा को सभी भूमि का स्वामी माना गया, लेकिन अनिवार्य रूप से कानूनी मालिक नहीं। भूमि में निजी संपत्ति एक सिद्धांतात्मक ढांचे के अंतर्गत अस्तित्व में थी, जहां राजा के दावे व्यक्तिगत निजी अधिकारों को कमजोर नहीं करते थे।
- कुछ भूमि सीधे राजकीय प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित की जाती थी, जबकि इन राजकीय क्षेत्रों के बाहर निजी स्वामित्व प्रमुख था। यह ढांचा राजकीय निगरानी और निजी भूमि अधिकारों के सह-अस्तित्व की अनुमति देता था।
- प्राचीन और प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में भूमि स्वामित्व का विचार आधुनिक पश्चिमी विचारों से भिन्न था। जबकि भूमि में निजी संपत्ति सामान्य थी, यह अंतिम राजकीय नियंत्रण की सिद्धांतात्मक धारणा के तहत अस्तित्व में थी। इसका अर्थ यह था कि राजा की सभी भूमि पर दावा था, लेकिन यह दावा व्यक्तिगत अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करता था। कुछ भूमि सीधे राजकीय प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित की जाती थी, लेकिन इन क्षेत्रों के बाहर, निजी स्वामित्व सामान्य था।
- भूमि स्वामित्व का विचार निरपेक्ष नहीं था; इसके बजाय, भूमि के अधिकारों की एक श्रेणी थी। उदाहरण के लिए, ऐतिहासिक रिकॉर्ड, जैसे बांग्लादेश में 7वीं या 8वीं शताब्दी CE के अश्रफपुर प्लेटें, इस अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। ये प्लेटें एक भूखंड का उल्लेख करती हैं जिसका आनंद एक व्यक्ति शर्वंतर ने लिया, जिसे अन्य लोगों ने खेती की, और जिसे राजा ने एक बौद्ध भिक्षु संगामित्र को दान किया। यह दर्शाता है कि भूमि के अधिकार जटिल थे और इसमें कई पक्ष शामिल थे।
धर्मशास्त्र में संपत्ति के अधिकार
धर्मशास्त्र ग्रंथ, जिनमें गौतम धर्मसूत्र, मनुस्मृति, बृहस्पति स्मृति, और नारद स्मृति शामिल हैं, प्राचीन भारत में संपत्ति के अधिकारों और संपत्ति अर्जित करने के तरीकों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। यहाँ उनके दृष्टिकोण का सारांश प्रस्तुत है:
- स्वामित्व अधिकार: गौतम धर्मसूत्र और मनुस्मृति के अनुसार, स्वामित्व अधिकारों में संपत्ति को बेचने, दान करने, और गिरवी रखने का अधिकार शामिल था।
- संपत्ति अर्जित करने के तरीके: ग्रंथ विभिन्न तरीकों का उल्लेख करते हैं, जैसे विरासत, खरीदारी, विभाजन, स्वीकृति, और खोज। मनुस्मृति में विजय, ब्याज पर उधार देना, और उपहार स्वीकार करना भी संपत्ति अर्जित करने के तरीके के रूप में उल्लिखित हैं।
- अचल संपत्ति: बृहस्पति स्मृति में अचल संपत्ति अर्जित करने के तरीके के रूप में अध्ययन, खरीद, गिरवी, साहस, विवाह, विरासत, और बिना वारिस के रिश्तेदारों के लिए उत्तराधिकार का उल्लेख किया गया है।
- धन के भेद: नारद स्मृति विभिन्न वर्णों (सामाजिक वर्गों) के लिए धन के प्रकारों में भेद करती है और विरासत, प्रेम उपहार, और पत्नी से प्राप्त उपहार को धन के सामान्य रूपों के रूप में पहचानती है।
भूमि के प्रकार, भूमि माप, और भूमि स्वामित्व
नीतिसार में वैश्य समुदाय के लिए मुख्य आजीविका के स्रोतों के रूप में पशुपालन, कृषि, और व्यापार का उल्लेख किया गया है। यह इस बात पर जोर देता है कि राजा की जिम्मेदारी है कि इन गतिविधियों में कुशल व्यक्तियों को आवश्यकता में न होना चाहिए।
भूमि के प्रकार: अमरकोष 12 विभिन्न प्रकार की भूमि की पहचान करता है, प्रत्येक के अपने विशेष लक्षण हैं:
- उर्वरा: उपजाऊ भूमि।
- उषरा: बंजर भूमि।
- मारु: रेगिस्तानी भूमि।
- अप्रहता: खाली या शुष्क भूमि।
- षड्वाला: घास वाली भूमि।
- पंकिला: कीचड़ भरी भूमि।
- जलप्रयामानुपम: गीली भूमि।
- कच्चा: जल के निकट स्थित भूमि।
- शर्करा: कंकड़ और चूना पत्थर से भरी भूमि।
- शर्कावती: रेत भरी भूमि।
- नदीमात्रिका: नदी द्वारा सिंचित भूमि।
- देवमात्रिका: वर्षा द्वारा सिंचित भूमि।
भूमि की शब्दावली: प्राचीन ग्रंथों से प्राप्त लेख inscripशनों में विभिन्न प्रकार की भूमि को वर्णित करने के लिए विशिष्ट शब्दों का उपयोग किया गया है:
- Kshetra: एक फसल उगाई गई भूमि को संदर्भित करता है।
- Khila: बिना जोते गए भूमि या खेती के लिए उपयुक्त बंजर भूमि।
- Aprahata: Khila के समान, जिसका अर्थ है खेती के लिए उपयुक्त बंजर भूमि।
- Aprada: अनसुलझी भूमि।
- Vastu: आवासीय भूमि।
- Pasture Land: ग्रंथों में ऐसा भूमि जिसका उपयोग जानवरों के चरने के लिए किया जाता है।
कृषि प्रथाएँ और चुनौतियाँ: प्राचीन ग्रंथ जैसे Amarakosha विभिन्न प्रकार के अनाजों को सूचीबद्ध करते हैं, जो उगाए गए फसलों की विविधता को दर्शाते हैं। Varahamihira का Brihatsamhita खराब फसल और अकाल से संबंधित ज्योतिषीय संकेतों पर चर्चा करता है, जो किसानों द्वारा सामना की गई चुनौतियों को दर्शाता है।
जल कार्य: ग्रंथों में पीने के पानी और सिंचाई के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जल कार्यों का उल्लेख किया गया है, जिसमें कुएँ, नहरें, तालाब और बांध शामिल हैं। Junagarh का शिलालेख सुझाव देता है कि राज्य ने इनमें से कुछ जल कार्यों के निर्माण और रखरखाव में भूमिका निभाई।
बंजर भूमि पुनर्वास: कई शिलालेख, जैसे Vainyagupta का Gunaigarh अनुदान और विभिन्न ताम्र पत्र, व्यक्तियों के बंजर भूमि के लिए आवेदन करने का उल्लेख करते हैं। इस प्रवृत्ति के कारण स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन यह कृषि भूमि पर बढ़ते दबाव, बंजर भूमि की अपेक्षाकृत सस्ती कीमत, या ऐसी भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए कर में छूट की उपलब्धता के कारण हो सकता है।
प्राचीन भारत के ग्रंथों और शिलालेखों से भूमि माप के विभिन्न शब्दावली प्रकट होती है, जिससे संकेत मिलता है कि कोई एक मानक माप प्रणाली नहीं थी और विभिन्न क्षेत्रों में अपने-अपने माप थे। पूर्वी भारत में उपयोग किए जाने वाले कुछ भूमि मापों में शामिल हैं:
- अधवाप: 3/8 से 1/2 एकड़
- ड्रोनवाप: 1 1/2 से 2 एकड़
- कूल्यवाप: 12 से 16 एकड़
- पताका: 60 से 80 एकड़
- अन्य शर्तों में प्रवर्तवाप, पदवर्त, और भूमि शामिल हैं। विभिन्न भूमि माप की शर्तों का उपयोग एक समान मानक की अनुपस्थिति और विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न मापों की प्रचलता को दर्शाता है।
बृहस्पति और नारद स्मृतियों में भूमि संपत्ति की सीमाओं को स्पष्ट रूप से चिह्नित करने के महत्व को उजागर किया गया है ताकि विवादों से बचा जा सके। उस समय के शिलालेखों से संकेत मिलता है कि सीमाएँ वास्तव में खाई, खंबों, या प्राकृतिक विशेषताओं जैसे कि पेड़, तालाब, और चूहे के बिल का उपयोग करके चिह्नित की गई थीं। बृहस्पति स्मृति भी सूखे गोबर, हड्डियों, कोयले, भूसे, बर्तन के टुकड़े, ईंटों, गायों की पूंछ, पत्थरों, कपास के बीज, और राख से बने सीमा चिह्नों को सीमाओं पर मिट्टी में दफनाने की सिफारिश करती है। इन चिह्नों को बच्चों और युवा लोगों को दिखाया जाना था, ताकि सीमाएँ सामान्य ज्ञान का हिस्सा बन जाएँ और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित हों।
बृहस्पति और नारद स्मृतियों में भूमि संपत्ति की सीमाओं को स्पष्ट रूप से चिह्नित करने के महत्व को फिर से रेखांकित किया गया है ताकि विवादों से बचा जा सके। ऐतिहासिक शिलालेख बताते हैं कि सीमाएँ वास्तव में चिह्नित की गई थीं, अक्सर खाई, खंबों, या प्राकृतिक विशेषताओं जैसे कि पेड़, तालाब, और चूहे के बिल का उपयोग करके।
बृहस्पति स्मृति सीमा चिह्नित करने के लिए एक अनूठी प्रथा का सुझाव देती है:
- सूखे गोबर, हड्डियाँ, कोयला, भूसा, बर्तन के टुकड़े, ईंटें, गायों की पूंछ, पत्थर, कपास के बीज, और राख जैसे सामान को बर्तन में डालकर सीमा चिन्हों के पास दफनाया जाना था।
- इन चिन्हों को बच्चों और युवाओं को दिखाया जाना था, यह सुनिश्चित करते हुए कि सीमाओं का ज्ञान पीढ़ियों तक पहुंचाया जाए।
- इस प्रथा का उद्देश्य संपत्ति की सीमाओं को समुदाय के ज्ञान का एक साझा और स्थायी हिस्सा बनाना था, जिससे भविष्य में विवादों को रोका जा सके।
भूमि अधिकारों से संबंधित तकनीकी शर्तें:
- इस अवधि के शिलालेखों में भूमि अधिकारों और दान किए गए भूमि पर दानकर्ताओं के अधिकारों से संबंधित विभिन्न तकनीकी शर्तें शामिल हैं।
- निवि-धर्म: यह शब्द संभवतः स्थायी उपयोगाधिकार के अनुदान का संदर्भ देता है, जो दानकर्ता को भूमि के फलों का आनंद लेने की अनुमति देता है।
- अक्षय-निवि और अप्रदा-धर्म: ये शब्द दर्शाते हैं कि दान अचल था, अर्थात इसे नहीं दिया जा सकता था, उपहार नहीं दिया जा सकता था, या बेचा नहीं जा सकता था।
- निवि-धर्म-क्षय: यह शब्द दानकर्ता को भूमि पर पूर्ण अधिकार प्रदान करता है, जिसमें स्थानांतरण और बिक्री के अधिकार शामिल हैं।
- भूमिचित्रणाय: इस शब्द की विभिन्न व्याख्याएँ की गई हैं, लेकिन यह सामान्यतः दानकर्ताओं को दी गई भूमि पर स्थायी और व्यापक अधिकारों को रेखांकित करता है। कुछ विद्वान इसे कृषि योग्य भूमि या गैर-कृषि भूमि के संदर्भ में बताते हैं।
भूमि लेन-देन और मूल्य:
इस अवधि से धर्मनिरपेक्ष बिक्री पत्रों की अनुपस्थिति शायद इस कारण हो सकती है कि ऐसे रिकॉर्ड नाशवान सामग्री पर रखे गए थे, जबकि पत्थर या धातु पर अंकित नहीं किए गए थे। हालांकि, पूर्वी भारत से कुछ शिलालेख हैं जो पवित्र दान के लिए भूमि की खरीद का दस्तावेजीकरण करते हैं, जो स्थानीय सरकारों की प्रक्रिया में भागीदारी को दर्शाते हैं। भूमि खरीदने की मूल प्रक्रिया में स्थानीय अधिकारियों को आवेदन देना, निर्धारित कीमत का भुगतान करना और स्थानीय सरकार द्वारा भूमि का निरीक्षण और सीमांकन करना शामिल था। एक ही क्षेत्र में भूमि की कीमतें काफी भिन्न हो सकती थीं, जैसा कि Pundravardhana भुक्ति के विभिन्न शिलालेखों में देखा गया है।
राजसी भूमि अनुदान
राजाओं द्वारा ब्राह्मणों को भूमि देने की प्रथा समय के साथ अधिक स्वीकार्य हो गई, जैसा कि बाद के वेदिक ग्रंथों में देखा गया है। प्रारंभ में, प्रारंभिक ग्रंथों में कुछ संकोच था, लेकिन अंततः इस प्रथा का मजबूत समर्थन मिला। उदाहरण के लिए, महाभारत राजाओं को ब्राह्मणों को भूमि देने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- ब्राह्मणों का महत्व: महाभारत के दानधर्म खंड में, भीष्म ब्राह्मणों की शक्ति पर जोर देते हैं। वे बताते हैं कि उनके पास देवताओं को बनाने और तोड़ने की क्षमता होती है, और वे राजाओं के भाग्य को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक राजा केवल तभी सत्ता में रह सकता है जब उसके पास ब्राह्मणों का समर्थन हो।
- उपहारों के प्रकार: दानधर्म पर्व में तीन महत्वपूर्ण प्रकार के उपहारों का उल्लेख है: सोना (हिरण्य-दान), मवेशी (गो-दान), और भूमि (पृथ्वी-दान)। इनमें से भूमि का उपहार सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि यह कीमती संसाधनों जैसे जवाहरात, पशुओं, और अनाज का स्रोत है।
- धर्मशास्त्र और पुराणों में समर्थन: ब्राह्मणों को भूमि दान करने की प्रथा को धर्मशास्त्र और पुराणों में भी प्रशंसा प्राप्त है। ये ग्रंथ वादा करते हैं कि जो लोग योग्य ब्राह्मणों को उचित उपहार देते हैं, वे इस जीवन में प्रसिद्धि और परलोक में सुख प्राप्त करेंगे।
- कर छूट और विशेषाधिकार: ब्राह्मण बस्तियों के लिए कर छूट और विशेषाधिकारों के प्रारंभिक प्रमाण आर्थशास्त्र से आते हैं। धर्मशास्त्र में ब्राह्मणों को करों से छूट पाने वालों में शामिल किया गया है और उन्हें भूमि के राजसी उपहारों की प्रशंसा की गई है। हालांकि, यह बृहस्पति स्मृति में है कि इन दोनों विचारों को स्पष्ट रूप से जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया है कि राजाओं द्वारा ब्राह्मणों को दी गई भूमि कर-मुक्त होनी चाहिए।
प्रारंभिक प्रमाण बताते हैं कि कुछ ब्राह्मण बस्तियों के लिए कर छूट और विशेषाधिकार, जो राजकीय आदेश द्वारा स्थापित किए गए थे, आर्थशास्त्र से आते हैं। धर्मशास्त्र भी ब्राह्मणों को करों से छूट पाने वालों में शामिल करता है और उनके लिए भूमि के राजसी उपहारों की प्रशंसा करता है। हालांकि, यह बृहस्पति स्मृति में है कि इन दोनों विचारों को स्पष्ट रूप से जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया है कि राजाओं द्वारा ब्राह्मणों को दी गई भूमि कर-मुक्त होनी चाहिए। ये संदर्भ सुझाव देते हैं कि ब्राह्मणिक परंपरा के संहितागत ग्रंथ, जो ब्राह्मणों द्वारा बनाए और बनाए रखे गए, ने ऐसे उपहारों को सकारात्मक रूप से देखा। सवाल उठता है कि क्या ये बार-बार के आदेश मौजूदा प्रथाओं को दर्शाते थे या इन्हें बढ़ावा देने का उद्देश्य था। अन्य स्रोतों से प्रमाण, जैसे कि बौद्धों के पाली कैनन में बिम्बिसार और कोसला के प्रसेनजीत जैसे राजाओं द्वारा ब्राह्मणों को भूमि देने का उल्लेख, दोनों का मिश्रण दर्शाते हैं।
- राजसी भूमि अनुदानों का प्रारंभिक प्रमाण, साथ ही विशेषाधिकारों और छूट से संबंधित अनुदान, पश्चिमी दक्कन में नानेघाट और नासिक में पाए गए। 4वीं शताब्दी से ऐसे अनुदानों में वृद्धि हुई, और 5वीं/6वीं शताब्दी तक, भारतीय उपमहाद्वीप भर के राजाओं ने इन उपहारों को देने लगे, जो आमतौर पर ताम्र पत्रों पर अंकित थे।
- ब्राह्मणों को दी गई गांवों को अग्रहारा, ब्रह्मादेया, या शासना के नाम से जाना जाता था। इन गांवों के लिए एक अधिक तटस्थ शब्द भट्ट-ग्राम है। जबकि अन्य लाभार्थियों, जैसे बौद्ध और जैन मठों, वैष्णव और शैव मंदिरों, और कुछ धर्मनिरपेक्ष अनुदानों को राजसी अनुदानों के रिकॉर्ड हैं, 10वीं शताब्दी CE तक अधिकांश राजसी भूमि अनुदान ब्राह्मणों को ही दिए गए थे।
भूमि अनुदानों का परिचय
- राजसी भूमि अनुदानों और विशेषाधिकारों और छूट के साथ अनुदानों का प्रारंभिक प्रमाण नानेघाट और नासिक में पश्चिमी दक्कन में पाया गया।
- 4वीं शताब्दी से ऐसे अनुदानों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 5वीं और 6वीं शताब्दी तक, भारतीय उपमहाद्वीप भर के राजाओं ने इन अनुदानों को दिया, जो आमतौर पर ताम्र पत्रों पर अंकित होते थे।
- ब्राह्मणों को दी गई गांवों को अग्रहारा, ब्रह्मादेया, या शासना के नाम से जाना जाता था। इन गांवों के लिए एक अधिक तटस्थ शब्द भट्ट-ग्राम है।
- हालांकि विभिन्न लाभार्थियों को राजसी अनुदानों के रिकॉर्ड हैं, जिनमें बौद्ध और जैन मठ, वैष्णव और शैव मंदिर, और धर्मनिरपेक्ष अनुदान शामिल हैं, 10वीं शताब्दी CE तक अधिकांश राजसी भूमि अनुदान ब्राह्मणों को दिए गए थे।
शाही गुप्तों की भूमिका
- इस अवधि के दौरान साम्राज्यवादी गुप्तों का भूमि अनुदान के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान नहीं था।गुप्त सम्राट द्वारा भूमि अनुदान का एकमात्र प्रामाणिक लेखन स्कंदगुप्त का भीतरी पत्थर का स्तंभ लेख है, जो बिना किसी विशेष शर्त के एक गाँव को विष्णु मंदिर को दिए जाने का उल्लेख करता है। इसके अलावा, समुद्रगुप्त को श्रेय दिया जाने वाले संदिग्ध गया और नालंदा ताम्र पत्र भी हैं। गया पत्र में एक ब्राह्मण, गोपालस्वामिन को रेवातिका गाँव का अनुदान देने का उल्लेख है, जबकि नालंदा पत्र में ब्राह्मण जयभट्टस्वामी को भद्रपुष्करक और पूर्णनाग गाँवों का अनुदान दिया गया है। दोनों अनुदानों में उपरिकर के रूप में ज्ञात शुल्क और गाँववासियों के लिए कर संबंधी दायित्व शामिल थे।
गया और नालंदा पत्रों के चारों ओर विवाद
- कुछ विद्वान इन गया और नालंदा लेखनों को संदिग्ध मानते हैं क्योंकि इनमें कुछ वर्तनी की गलतियाँ, व्याकरणिक त्रुटियाँ और समुद्रगुप्त के लिए प्रयुक्त विशेषण हैं। यह सुझाव दिया गया है कि ये पत्र मौलिक अनुदानों की बाद की प्रतियां हो सकती हैं। हालांकि, छाबड़ा और गई जैसे शोधकर्ताओं का तर्क है कि गया पत्रों की पैलियोग्राफी प्रारंभिक 8वीं सदी की है, जबकि नालंदा पत्र गुप्त काल के हैं। उनका कहना है कि लेखनों में व्याकरणिक दोष, विशेषकर लंबे यौगिक शब्दों में, अनिवार्य रूप से जालसाजी का संकेत नहीं हैं। जबकि गया पत्रों की पैलियोग्राफी को प्रारंभिक 8वीं सदी में रखा गया है, नालंदा पत्रों की पैलियोग्राफी की पुष्टि गुप्त काल की है। वे यह भी बताते हैं कि कई लेखनों में व्याकरणिक त्रुटियाँ हैं, विशेषकर लंबे यौगिक शब्दों में, और इसे एक लेख को जालसाजी मानने का कारण नहीं होना चाहिए। बिहार का पत्थर का लेख, जो संभवतः बुद्धगुप्त या पुरुगुप्त के शासनकाल से है, एक मंत्री द्वारा एक यूप का निर्माण करने का विवरण देता है, जो राजा कुमारगुप्त का साले भी था। इस मंत्री ने स्कंद और सप्त मातृकाएँ (सात दिव्य माताओं) को समर्पित मंदिरों का निर्माण किया। लेख में इन मंदिरों के रखरखाव के लिए दो गाँवों में हिस्सों का दान देने का उल्लेख है। लेख अधूरा है, और दान के किसी विशेष शर्त का उल्लेख समय के साथ खो गया है। गुप्त काल के दौरान, ब्राह्मणों को भूमि दान देना प्रमुख नहीं था, जबकि वाकाटक महत्वपूर्ण दाता थे। वाकाटक लेखनों में कुल 35 दान किए गए गाँवों का उल्लेख है, जिनमें से कई दान प्रवरसेन II के शासनकाल के दौरान किए गए थे, जिन्होंने 20 गाँवों के दान का दस्तावेजीकरण करने वाले 18 या 19 लेख जारी किए। इन अनुदानों में उपहार की गई भूमि से जुड़े छूट और विशेषाधिकारों का उल्लेख करने वाले विभिन्न तकनीकी शब्द शामिल थे। दान की गई भूमि का क्षेत्रफल 20 से 8000 निवर्तनों तक था, और कुछ मामलों में पूर्व के दानों के बदले गाँवों का दान किया गया, जैसे कि प्रवरसेन II के यवत्माल पत्रों में एक पूर्व अनुदान का नवीनीकरण।
- गुप्त काल के दौरान, ब्राह्मणों को भूमि दान देना प्रमुख नहीं था, जबकि वाकाटक महत्वपूर्ण दाता थे। वाकाटक लेखनों में कुल 35 दान किए गए गाँवों का उल्लेख है, जिनमें से कई दान प्रवरसेन II के शासनकाल के दौरान किए गए थे, जिन्होंने 20 गाँवों के दान का दस्तावेजीकरण करने वाले 18 या 19 लेख जारी किए।
- इन अनुदानों में उपहार की गई भूमि से जुड़े छूट और विशेषाधिकारों का उल्लेख करने वाले विभिन्न तकनीकी शब्द शामिल थे। दान की गई भूमि का क्षेत्रफल 20 से 8000 निवर्तनों तक था, और कुछ मामलों में पूर्व के दानों के बदले गाँवों का दान किया गया, जैसे कि प्रवरसेन II के यवत्माल पत्रों में एक पूर्व अनुदान का नवीनीकरण।
- वाकाटक राजवंश, विशेषकर प्रवरसेन II के शासनकाल के दौरान, ब्राह्मणों को उदार भूमि अनुदानों के लिए जाना जाता था। इस अवधि के लेखनों में 35 गाँवों के दान का उल्लेख है, जिसमें प्रवरसेन II के लेखनों में अकेले 20 गाँवों के दान का विवरण है।
- अनुदानों में उल्लेखित भूमि क्षेत्र 20 से 8000 निवर्तनों तक, जो एक शाही माप है। कुछ मामलों में, पूर्व के दानों के बदले गाँवों का दान किया गया, जैसे कि प्रवरसेन II के यवत्माल पत्रों में पूर्व के अनुदानों का नवीनीकरण।
- समय के साथ, इन दान किए गए गाँवों का स्थान वाकाटक साम्राज्य के पूर्वी हिस्से से पश्चिमी हिस्से, विशेषकर तापी घाटी की ओर स्थानांतरित हो गया।
- गुप्तों और वाकाटकों के अधीन उपशासक भी भूमि अनुदान किए। उदाहरण के लिए, गुप्तों के अधीन बघेलखंड में परिव्राजक महाराज और वाकाटक शासक के अंतर्गत मेकेला देश में भारताबाला ने अपने स्वयं के भूमि अनुदान किए।
शहरी इतिहास के पैटर्न
भारतीय उपमहाद्वीप का शहरी इतिहास
आर. एस. शर्मा (1987) ने भारतीय उपमहाद्वीप के शहरी इतिहास पर एक विस्तृत अध्ययन किया, जिसमें सुझाव दिया कि प्रारंभिक ऐतिहासिक शहरीकरण लगभग 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच अपने चरम पर था। इस चरम के बाद, शर्मा ने शहरी गिरावट के दो स्पष्ट चरणों की पहचान की:
- पहला चरण 3वीं सदी या 4वीं सदी ईस्वी के अंत में हुआ।
- दूसरा चरण 6वीं सदी ईस्वी के बाद की गिरावट का था।
शर्मा के अनुसार, उपमहाद्वीप में पुरातात्विक साक्ष्य इन अवधियों के दौरान शहरी गिरावट की व्यापकता का संकेत देते हैं। उन्होंने शिलालेखों में शिल्पकारों और व्यापारियों के संदर्भों में कमी की ओर भी इशारा किया, जो शहरी गिरावट के विचार को और अधिक समर्थन देता है। जबकि शर्मा ने स्वीकार किया कि शहरी गिरावट के लिए साहित्यिक साक्ष्य मजबूत नहीं है, उन्होंने गिरावट को दर्शाने के लिए कई ग्रंथों का उल्लेख किया:
- वराहमिहिर की बृहत्संहिता: विभिन्न नगरों के विनाश या गिरावट की भविष्यवाणी।
- वाल्मीकि रामायण: राम के निर्वासन के बाद अयोध्या की गिरावट का वर्णन।
- कालिदास का रघुवंश: नगर की वीरानी का चित्रण।
शर्मा ने शहरी गिरावट का कारण लंबी दूरी के व्यापार में कमी को बताया और सुझाव दिया कि यह गिरावट का काल कम से कम सात शताब्दियों तक चला। उन्होंने 11वीं सदी के दौरान उपमहाद्वीप के कुछ हिस्सों में हल्की शहरी नवीनीकरण का अवलोकन किया, और 14वीं सदी तक, शहरीकरण एक पहचानने योग्य प्रक्रिया के रूप में उभरा।
वाकाटक साम्राज्य
वाकाटक साम्राज्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए, श्रीमाली (1987) ने इस अवधि के दौरान व्यापार, व्यापारियों और शहरी अर्थव्यवस्था में गिरावट की बात की। उन्होंने वाकाटक काल के शिलालेखों की व्याख्या करते हुए इसे एक गैर-मौद्रिक, छोटे पैमाने की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के रूप में चित्रित किया।
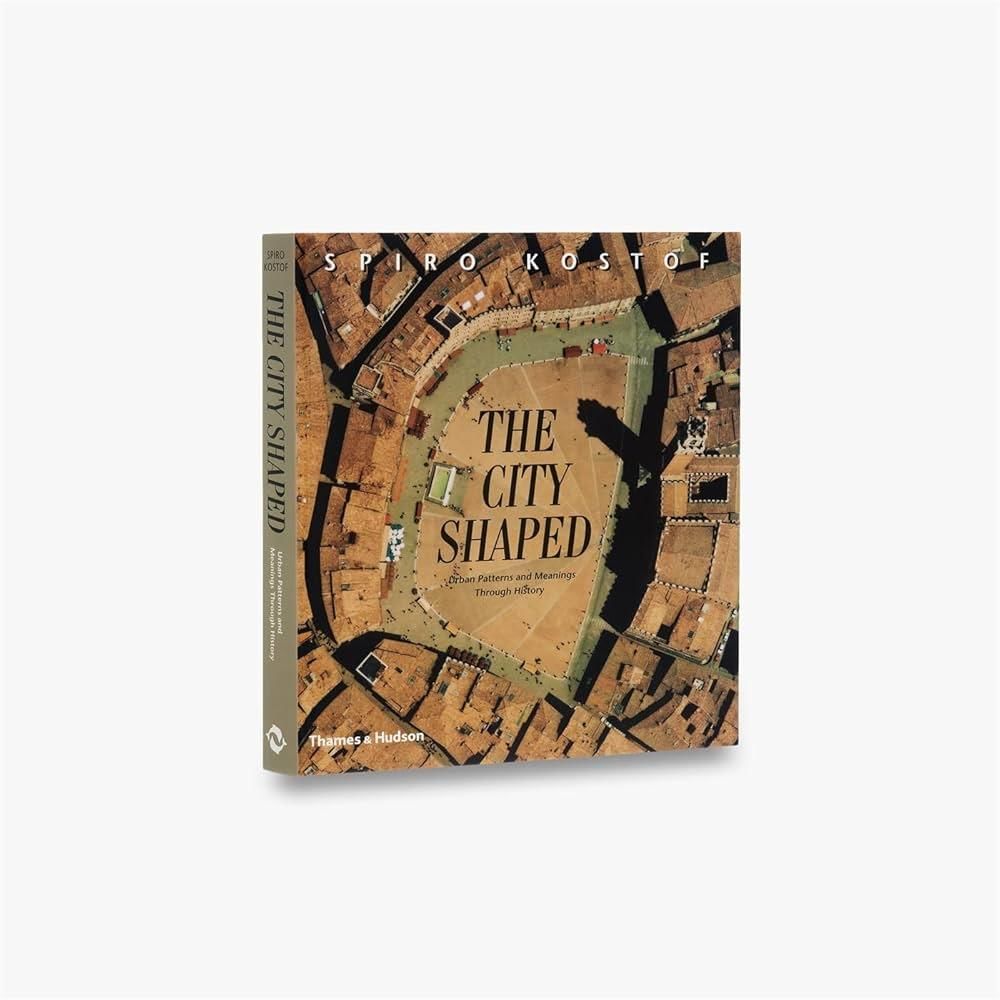
- ग्रामीण बस्तियों का विस्तार।
- शहरीकरण का संकुचन।
- फ्यूडैलिज़्म की प्रारंभिक शुरुआत।
व्यापार और शहरी अर्थव्यवस्था में गिरावट
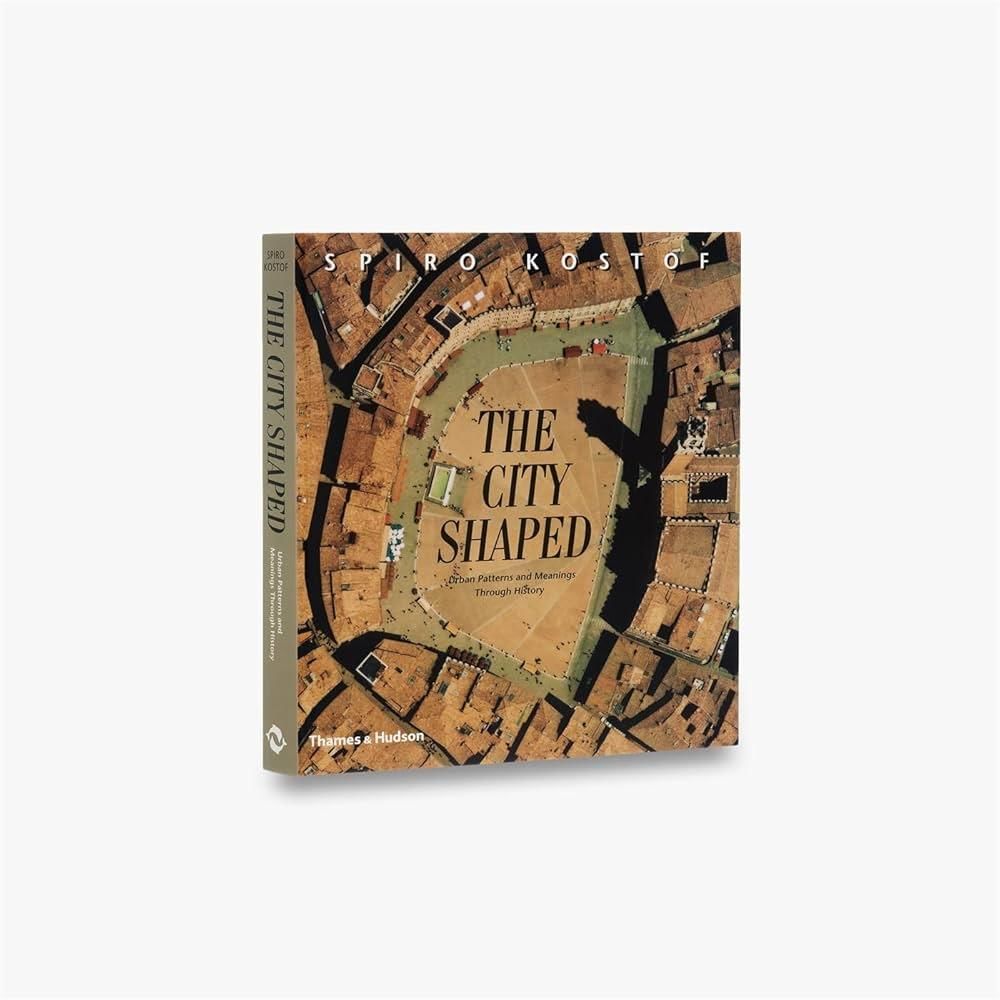
वाकटकों के साम्राज्य ने व्यापार, व्यापारियों और शहरी अर्थव्यवस्था में गिरावट का अनुभव किया। इस अवधि के अभिलेख बताते हैं कि यह एक गैर-मौद्रिक, छोटे पैमाने की ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी।
- ग्रामीण बस्तियों का विस्तार, शहरी क्षेत्रों का संकुचन और फ्यूडैलिज़्म की प्रारंभिक शुरुआत हुई।
- अभिलेखों में शहरी केंद्रों का उल्लेख बहुत कम मिलता है, जो अपेक्षित है क्योंकि ये ग्रामीण भूमि के अनुदान हैं।
- लगभग 16 बस्तियों को ही शहरी विशेषताओं के साथ पहचाना जा सकता है, जैसे कि 'पुरा', 'पुरक' और 'नगर' जैसे उपसर्गों के आधार पर।
शहरी अवनति परिकल्पना पर प्रश्न उठाना

लगभग 300-600 ईसा पूर्व की अवधि के दौरान उपमहाद्वीप में शहरी अवनति की परिकल्पना को कई कारणों से प्रश्नित किया जा सकता है:
- समकालीन ग्रंथों में शहरों और शहरवासियों का लंबा, काव्यात्मक वर्णन मिलता है, जो विकसित शहरी केंद्रों के प्रति जागरूकता को दर्शाता है, भले ही इसे शाब्दिक रूप से न लिया जाए।
- बृहत्संहिता में राजाओं और दरबारों की वैभव का उल्लेख है, जबकि मृच्छकटिक में उज्जयिनी में वसंतसेना के भव्य घर का वर्णन है।
- अमरकोश में विभिन्न आभूषण और वस्त्रों का उल्लेख है, और कामसूत्र नगरक के शहरी जीवन शैली का चित्रण करता है।
- इस अवधि में विभिन्न साहित्यिक, वास्तु और मूर्तिकला के कार्यों का उत्पादन एक शहरी वातावरण और शहरी संरक्षण के स्रोत को दर्शाता है।
दूर दक्षिण में शहरीकरण
तमिल महाकाव्य दूर दक्षिण में शहरी जीवन का जीवंत वर्णन प्रदान करते हैं, जो यह संकेत देता है कि शहरीकरण एक निरंतर प्रक्रिया थी।
- सिलप्पदिकारम में पुहार और मदुरै के हलचल भरे बाजारों का चित्रण किया गया है, जहाँ विभिन्न विक्रेता और कुशल श्रमिक हैं।
- पुहार को दो भागों में बाँटा गया है: आवासीय क्षेत्र (पट्टिनप्पक्कम या अकनागर) और तटीय बंदरगाह क्षेत्र (मरुवुरपक्कम)।
- पुहार का आवासीय क्षेत्र धनवान व्यक्तियों के घरों, भोजनालयों, बागों, बैठक स्थलों, तालाबों, सार्वजनिक स्नानघरों और मंदिरों से भरा हुआ था। श्मशान और दफनाने की जगहें शहर के बाहर स्थित थीं।
- महाकाव्यों में इन शहरों में हिंदू मंदिरों, साथ ही बौद्ध और जैन संस्थानों का भी उल्लेख किया गया है। उदाहरण के लिए, मनिमेकलाई में वंजी में एक विहार और चैत्य का उल्लेख है, जो उस समय के शहरी केंद्रों की धार्मिक विविधता और वास्तुकला का महत्व दर्शाता है।
तमिल महाकाव्यों में शहरी जीवन
तमिल महाकाव्य प्राचीन तमिलनाडु में शहरों और शहरी जीवन का विस्तृत और जीवंत वर्णन प्रदान करते हैं, यह संकेत करते हुए कि शहरी विकास दक्षिण के दूरदराज क्षेत्रों में एक निरंतर प्रक्रिया थी। सिलप्पदिकारम पुहार और मदुरै के हलचल भरे बाजारों का चित्रण करता है, जहाँ विभिन्न विक्रेता और कुशल श्रमिक मौजूद हैं।
पुहार को दो स्पष्ट क्षेत्रों में वर्णित किया गया है:
- पट्टिनप्पक्कम या अकनागर (आवासीय क्षेत्र)
- मरुवुरपक्कम (तटीय बंदरगाह क्षेत्र)
पुहार का आवासीय क्षेत्र धनवान व्यक्तियों के घरों, भोजनालयों, बागों, बैठक स्थलों, तालाबों, सार्वजनिक स्नानघरों और मंदिरों से भरा हुआ था। श्मशान और दफनाने की जगहें शहर के बाहर स्थित थीं।
महाकाव्यों में हिंदू मंदिरों, बौद्ध और जैन संस्थानों की उपस्थिति का भी उल्लेख है। उदाहरण के लिए, मनिमेकलाई में वंजी में एक विहार और चैत्य का उल्लेख है, जो उस समय के शहरी केंद्रों की धार्मिक विविधता और वास्तुकला का महत्व दर्शाता है।
{ "error": { "message": "This model's maximum context length is 128000 tokens. However, your messages resulted in 139270 tokens. Please reduce the length of the messages.", "type": "invalid_request_error", "param": "messages", "code": "context_length_exceeded" } }
अमरकोष में कपास के वस्त्रों के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें बुनकर, हथकरघा, धागा और विभिन्न प्रकार के कपड़े शामिल हैं, जो वस्त्र उत्पादन के महत्व को दर्शाते हैं। प्रारंभिक भारतीय मूर्तियों में सिले हुए कपड़ों के प्रमाण देखे जा सकते हैं, जबकि अजन्ता की पेंटिंग्स में जटिल वस्त्रों का चित्रण किया गया है, जो कुशल दर्जियों और कढ़ाई करने वालों की उपस्थिति का सुझाव देते हैं। कीमती और अर्ध-कीमती पत्थरों से बने आभूषण, साथ ही मूंगा और शंख जैसी सामग्रियों का उपयोग लोकप्रिय था, जैसा कि साहित्य में वर्णित है और मूर्तियों और पेंटिंग्स में दर्शाया गया है। वराहमिहिर की बृहत्संहिता में हीरे, रुबियों और मोती जैसे रत्नों के गुणों का वर्णन किया गया है, जो इन सामग्रियों के प्रति मूल्यांकन को दर्शाता है। कामसूत्र और काव्य साहित्य शहरी निवासियों के जीवन की झलक प्रदान करते हैं, जो माला बनाने वालों और सौंदर्य प्रसाधनों, औषधियों, और इत्र के उत्पादकों के अस्तित्व का सुझाव देते हैं।
प्राचीन भारत में वस्त्र और आभूषण
- अमरकोष में कपास के वस्त्रों के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें बुनकर, हथकरघा, धागा और विभिन्न प्रकार के कपड़े जैसे मोटे और बारीक शामिल हैं।
- प्रारंभिक भारतीय मूर्तियों और अजन्ता की पेंटिंग्स से यह सुझाव मिलता है कि प्राचीन भारत में सिले हुए कपड़े और कुशल दर्जी और कढ़ाई करने वाले थे।
- इस काल का साहित्य और कला विभिन्न कीमती और अर्ध-कीमती पत्थरों जैसे हीरे, रुबियों, और मोतियों से बने सुंदर आभूषणों का चित्रण करते हैं।
- अमरकोष और वराहमिहिर की बृहत्संहिता जैसे ग्रंथ इन पत्थरों और उनके गुणों का विस्तृत वर्णन करते हैं।
- आभूषणों को मूंगा और शंख जैसी सामग्रियों से भी बनाया जाता था।
- कामसूत्र और काव्य साहित्य कला के हस्तशिल्पियों जैसे माला बनाने वालों और सौंदर्य प्रसाधन और इत्र बनाने वालों के अस्तित्व का सुझाव देते हैं।
गिल्ड्स और प्रवासन
मंदसौर की शिलालेख में रेशमी बुनकरों के एक संपन्न गिल्ड के प्रवास और गतिविधियों को उजागर किया गया है, जो सुंदरता बढ़ाने में रेशम के महत्व पर जोर देता है। इंदौर की तांबे की प्लेट, जो स्कंदगुप्त के समय की है, कारीगरी के गिल्डों, जैसे कि तेल व्यापारियों के गिल्ड के प्रवास का संकेत देती है।
- मंदसौर की शिलालेख में रेशमी बुनकरों के एक संपन्न गिल्ड के प्रवास और गतिविधियों को उजागर किया गया है, जो सुंदरता बढ़ाने में रेशम के महत्व पर जोर देता है।
- इंदौर की तांबे की प्लेट, जो स्कंदगुप्त के समय की है, कारीगरी के गिल्डों, जैसे कि तेल व्यापारियों के गिल्ड के प्रवास का संकेत देती है।
धर्मशास्त्र और व्यापार
- धर्मशास्त्र के ग्रंथ शिल्प उत्पादन और व्यापार में साझेदारी, साथ ही नए शिल्पियों की कुशल कारीगरों के साथ शिक्षण पर प्रकाश डालते हैं।
- गोपाचंद्र की फरीदपुर की प्लेट बड़े व्यापारियों (प्राधान-व्यापारिनः) का उल्लेख करती है और व्यापार गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं, जैसे कि परिवहन की व्यवस्था करना और व्यापारियों तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए नियमों को स्पष्ट करती है।
|
125 videos|399 docs|221 tests
|




















