उद्भवशील क्षेत्रीय संरचनाएँ, लगभग 600–1200 ईस्वी - 3 | Famous Books for UPSC CSE (Summary & Tests) in Hindi PDF Download
ग्रामीण समाज
समाज की कृषि नींव
- बर्टन स्टेन ने प्रारंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत को 'किसान समाज' के रूप में वर्णित किया, जहाँ अधिकांश लोग स्थायी कृषि गाँवों में रहते थे।
- किसान कृषि मुख्य जीवनयापन और धन का स्रोत था, जिसमें सामाजिक संबंधों ने सामान्य किसान गतिशीलता को दर्शाया, जिसमें शक्ति असंतुलन शामिल था।
सामाजिक संरचना और कॉर्पोरेट संगठन
- समाज में विकसित कॉर्पोरेट संगठनों और विभिन्न कॉर्पोरेट इकाइयों के बीच प्रभावी गठबंधनों का अस्तित्व था।
- स्टेन ने चोल और पश्चात चोल काल के दौरान दक्षिण भारतीय इतिहास की कृषि आधार को उजागर करने का प्रयास किया, जिसमें किसान को केंद्रीय तत्व के रूप में महत्व दिया।
जाति और किसान जीवन
- जाति पदानुक्रम और असमानता के प्रभाव को स्वीकार करते हुए, स्टेन ने तर्क किया कि ये कारक समाज की किसान प्रकृति को नकारते नहीं हैं।
- किसान जीवन, आंतरिक विभाजनों और शोषण के बावजूद, सामाजिक, अनुष्ठानिक, और राजनीतिक पारस्परिक निर्भरता और सहयोग की विशेषता थी।
स्टेन के दृष्टिकोण पर प्रश्न
- स्टेन की किसान वर्ग का वर्णन एक समान समूह के रूप में, जो केवल निम्न और प्रमुख वर्गों में विभाजित है, समस्या के रूप में देखा जाता है।
- ब्राह्मणों और किसानों के बीच संबंध का वर्णन एक गठबंधन के रूप में संदिग्ध है। स्टेन ने ब्राह्मणों को व्यवस्था और वैधता के प्रमुख मध्यस्थों के रूप में देखा, suggesting कि उनका किसानों के साथ संपर्क ग्रामीण दक्षिण भारत में एक प्राथमिक सांस्कृतिक लिंक था।
ब्राह्मण और किसान
- स्टेन ने प्रस्तावित किया कि ब्राह्मणों ने ग्रामीण क्षेत्रों में अपने प्रभाव को बढ़ाया, जबकि किसानों ने बाहरी खतरों के खिलाफ एकता की तलाश की।
- हालांकि, यह तर्क कुछ विद्वानों द्वारा असंतोषजनक माना जाता है।
दक्षिण भारतीय गाँव का जीवन


- दक्षिण भारतीय गाँव के जीवन में, समाज की मूल इकाई उर थी, जो गाँवों और गाँव की सभाओं को संदर्भित करती थी।
- ये गाँव वेल्लान्वागई गाँव के रूप में जाने जाते थे और ये गैर-ब्रह्मादेया थे।
- लिपियाँ दर्शाती हैं कि इन गाँवों में कृषि खेत, आवास क्षेत्र, पेयजल स्रोत, सिंचाई कार्य, चरागाह भूमि, और शमशान भूमि शामिल थी।
- आवास क्षेत्र के भीतर, विभिन्न समूहों के लिए अलग-अलग क्वार्टर निर्धारित किए गए थे: उर-नट्टम या उर-इरुक्काई भूमि के स्वामित्व वाले किसानों के लिए, कम्मानचेरी कारीगरों के लिए, और परैचेरी कृषि श्रमिकों के लिए।
- गाँव के भीतर अधिकारों और स्थिति की एक पदानुक्रम था, जिसमें सामाजिक और स्थानिक रूप से अलग समूह शामिल थे।
- परैयारों को अनुष्ठानिक रूप से अपवित्र माना जाता था, जबकि वेल्लालर कृषि समूह थे, जिन्हें भूमि स्वामित्व वाले किसान (कनियुदैयर) और किरायेदार किसानों (उलुकुदी) में विभाजित किया गया था।
- वेल्लालर, जो शूद्र वर्ण से संबंधित थे, आर्थिक रूप से शक्तिशाली भूमि धारक थे, जिससे उन्हें ब्राह्मणों के समकक्ष स्थिति मिली।
- सेवा समूह जैसे बर्तन बनाने वाले और लोहार छोटे भूखंडों पर नियंत्रण रखते थे। चोल काल के अंतिम चरण में, आर्थिक रूप से शक्तिशाली और स्थानीय रूप से प्रभावशाली जमींदार उभरने लगे।
गाँव में महिलाओं की नेतृत्व भूमिका
कर्नाटका से प्राप्त शिलालेखों में महिलाओं द्वारा नेतृत्व किए गए गांवों का उल्लेख है, जैसे 902 CE का शिलालेख जिसमें एक महिला का नाम बिट्टैया है, जो भरंगीयूर गांव की प्रमुख है। 1055 CE का एक शिलालेख महिलाओं का उल्लेख करता है जैसे चंदियाब्बे जो एक गांव की मुखिया है और जक्कियाब्बे जो उसकी सलाहकार है। शिलालेखों में यह भी उल्लेख है कि महिलाएं अपने पतियों की मृत्यु के बाद गांव के नेतृत्व के पदों पर सफल होती थीं।
भूमि अनुदान और स्वामित्व के पैटर्न
- दक्षिण भारत में ब्राह्मणों को राजकीय भूमि अनुदान की प्रथा 3/4वीं शताब्दी से शुरू हुई और मध्यकालीन अवधि में फैल गई।
- कराशिमा का सुझाव है कि ब्राह्मादेया और गैर-ब्राह्मादेया गांवों के बीच भूमि धारिता के पैटर्न में अंतर था, जिसमें सामुदायिक धारिता बाद वाले में प्रचलित थी।
- हालांकि, गैर-ब्राह्मादेया गांवों में व्यक्तिगत स्वामित्व का प्रमाण भी मिलता है।
- मध्यकालीन अवधि के दौरान भूमि धारिता के सामान्य रुझान इन पैटर्न को दर्शाते हैं।
भूमि अधिकार और प्रारंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत में कॉर्पोरेट निकाय
चोल काल के दौरान, व्यक्तिगत संपत्ति अधिकारों में उल्लेखनीय मजबूती आई, साथ ही भूमि धारिता के आकार में बढ़ती असमानता भी। इस युग के शिलालेख भूमि हस्तांतरण के विभिन्न उदाहरणों को दर्ज करते हैं, जो अक्सर कानी अधिकारों के हस्तांतरण में शामिल होते थे। कानी अधिकार भूमि के स्वामित्व को संदर्भित करते थे, जो आमतौर पर कुछ जिम्मेदारियों और दायित्वों के साथ होते थे।
- चोल और पांड्य भूमि अनुदानों में विभिन्न प्रकार के भूमि अधिकारों का उल्लेख है, जिनमें करन्मई (कृषि करने का अधिकार) और मिताच्ची (एक श्रेष्ठ स्वामित्व अधिकार) शामिल हैं। जब ये शर्तें एक साथ आती थीं, तो यह भूमि की कृषि करने और इसकी खेती सुनिश्चित करने का अधिकार इंगित करती थीं।
- इसके अलावा कुटिमाई (अधिवास का अधिकार) भी था। करन्मई के दो रूप थे: कुडी निक्की और कुडी निंगा। कुडी निक्की का अर्थ था पूर्ववर्ती निवासियों को हटाना, जबकि कुडी निंगा का मतलब था कि मौजूदा निवासियों को परेशान नहीं किया जाएगा।
- कुछ भूमि अनुदानों में यह भी stipulate किया गया था कि भूमि मजदूरों के साथ प्रदान की गई।
- प्रारंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मजबूत कॉर्पोरेट निकायों की उपस्थिति एक महत्वपूर्ण पहलू था। उर वेल्लन्वागई गांवों में कॉर्पोरेट निकाय था, जिसमें कर चुकाने वाले भूमि मालिक शामिल होते थे। सदस्यता भिन्न होती थी, आमतौर पर दस से कम सदस्यों की होती थी। उर भूमि से संबंधित मामलों जैसे बिक्री, उपहार और कर छूट का प्रबंधन करता था।
- साभा ब्राह्मणों की सभा थी जो ब्राह्मादेया गांवों में पाई जाती थी, जिसमें सदस्यता के मानदंड संपत्ति के स्वामित्व, पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षा और अच्छे आचरण पर आधारित थे। साभा भूमि संपत्ति का प्रबंधन करती थी, जिसमें मंदिर से संबंधित भूमि शामिल होती थी, राजस्व एकत्र करती थी, और खातों को बनाए रखती थी। यह मंदिर से संबंधित धार्मिक गतिविधियों की भी निगरानी करती थी। साभा के निर्णयों का उल्लंघन एक गंभीर अपराध था, जो सामाजिक बहिष्कार की ओर ले जाता था।
- शुरुआत में, कर्नाटका में ब्राह्मण साभाएं छोटी थीं, लेकिन 11वीं-12वीं शताब्दी के शिलालेखों में बड़े साभाओं का उल्लेख है जिनमें सैकड़ों या हजारों सदस्य थे, जो कुछ गांवों में बढ़ती हुई ब्राह्मण जनसंख्या को दर्शाते हैं।
कर्नाटका के कनकट्टे गांव का इतिहास
कनकट्टे, जो दक्षिण कर्नाटक के हासन जिले के अर्सिकेरे तालुक में स्थित है, का एक समृद्ध इतिहास है जिसे B. D. चट्टोपाध्याय ने 15 शिलालेखों के विश्लेषण के माध्यम से पुनर्निर्मित किया है। इन शिलालेखों में, गाँव को कालिकट्टि के रूप में संदर्भित किया गया है।
प्रारंभिक शिलालेख
- सबसे पुराना शिलालेख लगभग 890 ईस्वी का है, जो एक गंगा राजा सत्यवाक्य परमानिदी रचमल्ला के शासन के दौरान लिखा गया था। यह शिलालेख अरेकरे में एक हीरो स्टोन पर पाया गया है और यह उस स्थानीय प्रमुख श्री मुत्तारा की वीरता की मृत्यु को समर्पित है, जिन्होंने नोलंबों के खिलाफ लड़ाई लड़ी।
- मृत्यु के बाद का पुरस्कार: श्री मुत्तारा को पोस्टह्यूमसली दो गाँवों— अरिकेरे और कालिकट्टि का पुरस्कार दिया गया। यह दान संभवतः उनके वंशजों के लिए लाभप्रद था।
हoysala काल
- प्रमुखता में वृद्धि: दो शताब्दियों बाद, कालिकट्टि का उल्लेख होयसाल राजा विश्णुवर्धन (1108–42 ईस्वी) के शासन के शिलालेखों में किया गया। गाँव महत्वपूर्ण बन गया था, इसे 'मागरे 300' के अंतर्गत सबसे प्रमुख के रूप में वर्णित किया गया।
- 1130 ईस्वी का शिलालेख: यह शिलालेख महासामंत सिंगरसा का उल्लेख करता है, जो अर्सिकेरे से कालिकट्टि का अधिग्रहण करते हैं और इसका शासन करते हैं। उन्होंने सिंगेश्वर नामक एक देवता की स्थापना की और शिव मंदिर के रखरखाव के लिए भूमि दान की।
- 1132 ईस्वी का शिलालेख: यह शिलालेख सुझाव देता है कि सिंगरसा को अर्सिकेरे से कालिकट्टि स्थानांतरित किया गया। उन्होंने गाँव में शिव के प्रतीक लिंग नामक बेट्टादाकालिदेवा की स्थापना की और गाँव के तालाब के पास अतिरिक्त भूमि दान की।
कालिकट्टि का वर्णन 1189 ईस्वी में

- 1189 ईस्वी में एक लेखन, होयसाला राजा बल्लाला II के शासनकाल के दौरान, कालिकट्टी को एक जीवंत गाँव (ur) के रूप में वर्णित करता है जिसमें अच्छी तरह से रखे गए टैंक (जल निकाय), सुपारी के पेड़, चावल के खेत, और प्रभावशाली मंदिर हैं।
- टैंक और सिंचाई: लेखन में गाँव के बड़े टैंक और उसके स्लुइसेस का बार-बार उल्लेख किया गया है, जो जल प्रबंधन के महत्व को दर्शाता है। अन्य टैंकों, जैसे अडुवा-गिरे, और व्यक्तियों के नाम पर रखे गए टैंकों जैसे हरियोजा, मंगेय, बोविती, और बिट्टेया से गाँव की सिंचाई प्रयासों का संकेत मिलता है।
- कृषि उत्पादकता: समय के साथ विभिन्न टैंकों की स्थापना ने गाँव की सिंचाई अवसंरचना के विस्तार के लिए पहलों का सुझाव दिया, जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई।
कालिकट्टी में परिवर्तन

12वीं सदी में, लेखन में विभिन्न समंत और महासमंत का उल्लेख है जिन्होंने कालिकट्टी पर शासन किया। इनमें से कुछ शासकों ने मंदिरों की स्थापना की और उन्हें भूमि दान की। 13वीं सदी की शुरुआत में, कालिकट्टी को लेखन में स्थल या नद के रूप में संदर्भित किया गया। इस अवधि में कालिकट्टी के विभिन्न हल्लियों (गाँवों) का उल्लेख, दो नए टैंकों का निर्माण, और मंदिरों में दो नए देवता चित्रों की स्थापना हुई। हिरिया-केरे, एक पुराना जल निकाय, अभी भी पहचाना गया। हालाँकि, इस समय एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ—कालिकट्टी एक अग्रहारा में विकसित हुआ और इसका नाम विजय-नरसिंहपुर रखा गया। लेखन समय के साथ बस्ती में हुए सामाजिक परिवर्तनों की अंतर्दृष्टि भी प्रदान करता है।
ब्राह्मण सभा और चोल Court
- कुछ ब्रह्मणा सभाओं और चोल दरबार के बीच मजबूत संबंध थे। उत्तरमेरी से दो लेख इस बात का संकेत देते हैं कि सभा का निर्णय एक राजकीय अधिकारी की उपस्थिति में लिया गया था, जिसे राजा ने भेजा था। इससे भी अधिक स्पष्ट दो लेख तंजावुर से हैं, जो सुझाव देते हैं कि राजराजा I ने चोलामंडलम की सभाओं को बृहदीश्वर मंदिर में विभिन्न सेवाएँ करने का निर्देश दिया। चोल साम्राज्य में उल्लेखनीय ब्रह्मदेयास को तानियूर स्थिति प्राप्त थी, जिसका अर्थ है कि उन्हें उन नाडुस के भीतर स्वतंत्र गांवों के रूप में माना जाता था जहाँ वे स्थित थे।
ग्रामीण समुदायों के भीतर संघर्ष
- कर्नाटका से प्राप्त लेख ग्रामीण समुदायों के भीतर संघर्ष के स्रोतों को उजागर करते हैं। विवाद तब उत्पन्न हो सकते थे जब ब्रह्मणा दाताओं को एक गांव में शामिल किया जाता था। उदाहरण के लिए, एक मध्य-13वीं सदी का लेख बताता है कि एक गांव के गौडों (खेती करने वाले) ने इसे एक ब्रह्मदेज़ में बदलने के खिलाफ विरोध किया। इसके जवाब में, राजा ने उन्हें दंडित करने के लिए सेना भेजी, जिसने गांव को लूट लिया। संघर्ष अक्सर गांव के संसाधनों के इर्द-गिर्द घूमते थे, जिसमें पानी एक विशेष रूप से संवेदनशील मुद्दा था। 1080 ईस्वी का एक लेख हासन तालुक से एक ब्रह्मणा और एक किसान के परिवार के बीच गांव के तालाब से पानी निकालने के विवाद का वर्णन करता है। इसी प्रकार, एक प्रारंभिक 13वीं सदी का लेख किसानों और एक प्रमुख के बीच एक सिंचाई तालाब पर विवाद का उल्लेख करता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रमुख की मृत्यु हो गई और होयसाला राजा ने उनकी याद में एक नायक पत्थर स्थापित किया और एक नया तालाब बनवाया।
किसानों पर श्रमिक बोझ
- राजराजा III के शासनकाल के दौरान 1231 ईस्वी का एक लेख किसानों पर अनिवार्य श्रम करों के बोझ को उजागर करता है। तानियूर गांव के नत्तार (स्थानीय नेता) ने ब्रह्मणा सभा और महासभा के सामने अत्यधिक श्रम मांगों की शिकायत की। समस्या केवल मात्रा की नहीं थी बल्कि विभिन्न संग्रह एजेंसियों द्वारा एक ही कर की मांग की जा रही थी, जिनमें से कुछ सशस्त्र थीं। लेख में यह भी उल्लेख किया गया है कि गांव वालों पर नेट्टल (अनिवार्य श्रम) लगाया गया था जो राजधानी, राजराजापुरम में मरम्मत कार्य के लिए था, जो कि मन्नारगुडी से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित था। इस तरह के श्रम कर्तव्यों को पूरा करना गांव वालों के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। गांव की सभा और महासभा ने शिकायतों को संबोधित करने और भविष्य में लगाए जा सकने वाले करों को निर्दिष्ट करने के लिए बैठक की।
दक्षिण भारत के प्रारंभिक मध्यकाल में नाडु और नत्तार
- हाल के शोध दर्शाते हैं कि नाडु, जो कि एक स्थानीयता का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें कई बस्तियाँ होती हैं, चाहे वे ग्रामीण हों या शहरी, प्रारंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत में गाँव की तुलना में एक महत्वपूर्ण इकाई थी। नाडु शब्द स्थानीयता की सभा को भी दर्शाता है और इसे आमतौर पर इसके किसी गाँव के नाम पर रखा जाता था।
- हालाँकि चोल साम्राज्य के भीतर नाडुओं की सटीक संख्या निर्धारित करना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन विद्वान सब्बारायालु जैसे शोधकर्ताओं ने चोलामंडलम क्षेत्र में 140 और उत्तरी क्षेत्रों में 65 नाडुओं की पहचान की है। समय के साथ नाडुओं की संख्या निश्चित नहीं थी, जिसमें 9वीं शताब्दी के बाद वृद्धि देखी गई।
- नाडुओं के आकार में महत्वपूर्ण भिन्नता यह सुझाव देती है कि वे राज्य द्वारा लगाए गए मनमाने प्रशासनिक विभाजन नहीं थे।
- पलव और पांड्य साम्राज्य में समान गाँवों के समूह पाए गए थे, जहाँ उन्हें पलव लेखों में कोट्टम के रूप में संदर्भित किया गया था।
- हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि चेरा साम्राज्य में ऐसे इकाइयाँ अनुपस्थित थीं।
नट्टार की भूमिका
{ "error": { "message": "This model's maximum context length is 128000 tokens. However, your messages resulted in 177569 tokens. Please reduce the length of the messages.", "type": "invalid_request_error", "param": "messages", "code": "context_length_exceeded" } }
- कुम्बकोनम और तिरुचिरापल्ली तालुकों में, सिंचाई के लिए नहरों पर काफी निर्भरता थी, जो क्रमशः 85 प्रतिशत और 84 प्रतिशत कार्यों का गठन करती है। कुम्बकोनम कावेरी घाटी के निचले हिस्से में स्थित है, जबकि तिरुचिरापल्ली और ऊपरी हिस्से में है।
- तिरुत्तुरैप्पुंडी तालुक में, नहरों ने उल्लेखित सिंचाई कार्यों का 79 प्रतिशत हिस्सा बनाया, जबकि तालाबों का हिस्सा 15 प्रतिशत था।
- पुदुक्कोट्टई तालुक में, नहरों का 49 प्रतिशत और तालाबों का 38 प्रतिशत उल्लेख किया गया।
- तिरुक्कोयिलुर तालुक में नहरों का 60 प्रतिशत और तालाबों का 23 प्रतिशत उल्लेख था।
- स्लूइस और कुएं कम उल्लेखित हुए, क्रमशः 4.7 प्रतिशत और 5.4 प्रतिशत।
- विभिन्न उपक्षेत्रों में सिंचाई प्रौद्योगिकी के बीच के अंतर मुख्य रूप से पारिस्थितिकी के कारण थे, जो विशेष प्रौद्योगिकियों की उपयुक्तता को निर्धारित करते थे।
- दिलचस्प बात यह है कि, आज इन क्षेत्रों में देखी गई सिंचाई के पैटर्न में उन लेखों में प्रकट पैटर्न के साथ उल्लेखनीय समानताएँ हैं।
प्रारंभिक मध्यकालीन तमिलनाडु में, सिंचाई मुख्य रूप से नहरों और तालाबों के माध्यम से प्रबंधित की जाती थी। समय के साथ, उनके उपयोग में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए: कुम्बकोनम और तिरुक्कोयिलुर तालुकों में नहरों के उल्लेख में वृद्धि हुई और तालाबों के उल्लेख में कमी आई। इसके विपरीत, पुदुक्कोट्टई तालुक में नहरों के उल्लेख में कमी आई।
कुम्बकोनम तालुक: सिंचाई नेटवर्क का विकास चोल काल से पहले हुआ, और इसका मौलिक स्वरूप चोल शासन के दौरान स्थिर रहा।
तिरुक्कोयिलुर तालुक: प्रारंभ में तालाबों पर निर्भरता थी, लेकिन धीरे-धीरे नदी-जलित नहरों पर अधिक निर्भरता की ओर बढ़ा।
पुदुक्कोट्टई तालुक: नहरों का विकास संभवतः 11वीं सदी में अपने चरम पर था और उसके बाद स्थिर हो गया।
तिरुचिरापल्ली तालुक: 11वीं सदी में नहरों में निवेश कम था लेकिन 12वीं सदी में इसमें वृद्धि हुई।
पान के पत्ते और सुपारी
पान के पत्ते और सुपारी चबाना दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में एक सामान्य प्रथा है, जिसकी इतिहास हजारों वर्षों पुरानी है।
पान के पत्ते और सुपारी: एक प्राचीन परंपरा
- उद्भव: पान के पत्ते (तम्बुला संस्कृत में) और सुपारी (गुवक) का दक्षिण-पूर्व एशिया में एक लंबा इतिहास है, जिसमें 10,000–7000 ईसा पूर्व में थाईलैंड में सुपारी के उपयोग के प्रमाण मिलते हैं।
- दक्षिण भारत में प्रवेश: ये वस्तुएं संभवतः पहली शताब्दियों में दक्षिण भारत में आईं।
- ऐतिहासिक उल्लेख: पान के पत्ते चबाने का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों जैसे जataka कथाओं, चारक और सुश्रुत संहिताओं, और कालिदास तथा शुद्रक के कार्यों में मिलता है।
दक्षिण भारत में खेती
- प्रारंभिक खेती: दक्षिण भारत में पान के पत्ते और सुपारी की खेती लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित हो गई थी, जैसा कि पट्टुप्पट्टु में उल्लेखित है।
- लिपि: 11वीं–12वीं शताब्दी की लिपियों से पता चलता है कि यह खेती व्यापक रूप से फैली हुई थी, जिसमें मंदिरों को दिए गए भूमि में अक्सर पान की बेलें और सुपारी के बाग शामिल थे।
बढ़ती मांग
- 11वीं शताब्दी की लिपियाँ: पान के पत्ते और सुपारी का उल्लेख लिपियों में बढ़ता गया, जो बढ़ती मांग को दर्शाता है।
- कटाई और प्रसंस्करण: 11वीं शताब्दी की एक लिपि में सुपारी के कटाई (कोयलासी) और बिक्री के लिए प्रसंस्करण (मोत्ताकारस) में श्रमिकों की भूमिकाओं का उल्लेख किया गया है।
मंदिर अनुष्ठानों में भूमिका
- अनुष्ठानों में एकीकरण: पान के पत्ते और सुपारी मंदिर अनुष्ठानों का अभिन्न हिस्सा बन गए, साथ ही पारंपरिक भेंट जैसे उबले चावल और अगरबत्ती के साथ।
- सामाजिक महत्व: पान के पत्ते दोस्ती और सम्मान का प्रतीक थे, जैसा कि प्रारंभिक अरब लेखकों और चोल काल की लिपियों में उल्लेखित है।
- राजसी पसंद: पान के पत्ते चबाना राजाओं और nobles के बीच लोकप्रिय था, जैसा कि 12वीं शताब्दी के एक चीनी यात्री द्वारा उजागर किया गया है।
पश्चिमी भारत में व्यापार नेटवर्क: पान के पत्ते और सुपारी
- पान के पत्ते और सुपारी पश्चिमी भारत के व्यापार नेटवर्क में महत्वपूर्ण वस्तुएं थीं।
- 1145 CE में मंगरोल, जो सौराष्ट्र तट पर एक बंदरगाह है, से एक लेखन मिलता है जिसमें पान के पत्तों पर एक कर का उल्लेख है, जो संभवतः दक्षिण भारत से बंदरगाह पर आ रहा था।
- यह क्षेत्र में पान के पत्तों को संग्रहित करने के लिए विशेष गोदामों और इसे बेचने वाली दुकानों की उपस्थिति को दर्शाता है।
पान चबाने का प्रसार
- पान (सुपारी के साथ पान का पत्ता) चबाने की आदत पूरे उपमहाद्वीप में तेजी से फैली।
- शुरुआत में, यह एक ऐलीट आदत थी, जैसा कि हेमचंद्र के द्व्याश्रयकाव्य जैसे प्राचीन ग्रंथों में सुझाया गया है।
- राजतरंगिणी की कहानी में राजा अनंत का पान विक्रेता के प्रति ऋणी होना यह संकेत देता है कि कुछ पान विक्रेताओं ने महत्वपूर्ण लाभ कमाए।
औषधीय गुण और फैशनेबल आदत
- प्राचीन चिकित्सा ग्रंथों में पान के पत्तों और सुपारी के औषधीय गुणों का उल्लेख है।
- अल-बिरूनी ने noted किया कि भारतीय रात के खाने के बाद पान के पत्तों को चूने के साथ खाते थे ताकि पाचन में मदद मिले और सुपारी दांतों, मसूड़ों, और पेट के लिए लाभकारी होती है इसके कसैले गुणों के कारण।
- हालांकि, उनकी औषधीय लाभों के अलावा, पान के पत्ते और सुपारी का सेवन उन लोगों के लिए एक फैशनेबल आदत बन गया जो इसे खरीदने में सक्षम थे।
- यह प्रवृत्ति बाद में चाय, कॉफी, और तंबाकू जैसे नशे की लत वाली वस्तुओं की व्यापक लोकप्रियता से तुलनीय है।
भूमि उपयोग और फसल उत्पादन में परिवर्तन
- कृषि के विस्तार, सिंचाई के प्रसार, और बाजार की मांग में परिवर्तनों ने भूमि उपयोग के पैटर्न में बदलाव किया।
- कर्नाटका क्षेत्र में, प्रियांगु (panicum italicum), रागी (eleusine coracana), ज्वार (sorghum vulgare), और बाजरा (bulrush millet) जैसी विभिन्न बाजरा फसलों पर जोर बढ़ा।
- कम गुणवत्ता वाली चावल की किस्मों जैसे श्यामक, निवारा, कंगु, कोद्रवा, और करदुषा की खेती भी बढ़ी।
- नकद फसलें जैसे गन्ना, पान के पत्ते, सुपारी, नारियल, संतरे, और काली मिर्च और अदरक जैसी मसालों की खेती भी बढ़ती गई।
शहरी प्रक्रियाएं
प्रारंभिक मध्यकालीन अवधि दक्षिण भारत में शहरी विकास का एक महत्वपूर्ण चरण है। इस क्षेत्र में शहरी पतन का विचार लागू नहीं होता। इस समय के दौरान शहरों ने विभिन्न भूमिकाएँ निभाईं, जिनमें राजनीतिक, उत्पादन, व्यापार और पवित्र या समारोह केंद्र शामिल हैं।
नगरम: बाजार और वाणिज्यिक केंद्र
- नगरम मुख्यतः वस्तुओं के उत्पादन और व्यापार में संलग्न शहरी स्थान थे, जिसमें कृषि उत्पाद भी शामिल थे, जो स्थानीय, अंतर-क्षेत्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापारित होते थे।
- एक नादु (एक प्रशासनिक इकाई) में कई नगरम हो सकते थे।
- कुछ नगरम, जैसे महत्वपूर्ण ब्राह्मदेय (भूमि अनुदान), को तानीयूर स्थिति दी गई, जिससे वे नादु के अधिकार क्षेत्र से स्वतंत्र हो गए।
- नगरम में व्यापारियों का एक कॉर्पोरेट निकाय था जिसे नगरत्तर कहा जाता था, जो भूमि प्रबंधन में भी शामिल थे। उन्होंने नगरक्कानी के रूप में जानी जाने वाली भूमि का स्वामित्व और प्रबंधन किया, जिससे उन्होंने राजस्व एकत्र किया।
चोल काल में वृद्धि
- चोल काल के दौरान नगरम अधिक महत्वपूर्ण हो गए, नगरत्तर अक्सर शिलालेखों में दाता के रूप में प्रकट होते थे।
- उनका दान, जो ज्यादातर धन, सोना, और चांदी में था, चोल काल के मध्य में अपने चरम पर पहुंच गया।
- इस अवधि में विशेष कॉर्पोरेट संगठनों का उदय भी देखा गया, जैसे कि:
- सालिया नगरम: वस्त्र व्यापार से संबंधित।
- सत्तुम परिषद नगरम: वस्त्रों से भी जुड़ा।
- शंकरप्पडी नगरम: तेल और घी आपूर्तिकर्ताओं का एक कॉर्पोरेट समूह।
- पराग नगरम: समुद्री व्यापारी समूह।
- वाणिया नगरम: तेल व्यापारियों का एक शक्तिशाली संगठन।
कौशल तकनीकों में सुधार
- इस अवधि में शिल्प तकनीकों में महत्वपूर्ण उन्नति हुई, जैसे:
- हाथ से चलने वाले तेल मिल: इन्हें बैल-चलित तेल मिलों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जो तेल को दबाने का काम करती थीं।
- वस्त्र बुनाई: वस्त्र बुनाई उद्योग में भी सुधार हुए, जिसमें लूम स्थापित करने के लिए अनुदानों का उल्लेख शिलालेखों में मिलता है।
शिल्प उत्पादन के केंद्र
- कई शिल्प उत्पादन के केंद्र उभरे, जिनमें से कुछ का प्रारंभिक ऐतिहासिक अवधि से निरंतर विकास हुआ।
- कांचीपुरम: यह शहर एक प्रमुख कपास उगाने वाले क्षेत्र में स्थित था और प्रारंभिक ऐतिहासिक अवधि से सबसे महत्वपूर्ण बुनाई केंद्रों में से एक बन गया।
- विस्तार: कांचीपुरम के चारों ओर और तंजावुर और दक्षिण आर्कोट जिलों में कई अन्य बुनाई केंद्र विकसित हुए।
- भूमि स्वामित्व: 12वीं–13वीं शताब्दी तक, बुनकरों और व्यापारियों ने भूमि में निवेश करना शुरू किया और भूमि स्वामी अभिजात वर्ग का हिस्सा बन गए।
तंजावुर और गंगैकोंडाचोलापुरम
- तंजावुर वडवरू नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित था, जो उपजाऊ कावेरी डेल्टा के दक्षिण-पश्चिमी किनारे पर है, जिसे इसके समृद्ध कृषि के लिए जाना जाता है।
- गंगैकोंडाचोलापुरम, एक और शाही शहर, इस डेल्टा के उत्तरी किनारे पर स्थित था। चोल काल से पहले, तंजाई नामक एक बस्ती थी, जिसे राजराज I के शासन के दौरान एक प्रमुख शाही और मंदिर शहर में बदल दिया गया।
- तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर इस शहर की केंद्रीय विशेषता थी, जो शहर पर हावी था और इसका मूल बनाता था।
शहर की संरचना और अर्थव्यवस्था
- मंदिर के चारों ओर का क्षेत्र शहर के आंतरिक परिपथ का निर्माण करता था, जहाँ राजनीतिक और पुरोहित अभिजात वर्ग निवास करते थे। इसके चारों ओर एक बाहरी आवासीय परिपथ था, जहाँ अन्य शहरी समूह जैसे व्यापारी रहते थे।
- शहर में चार बाजार (अंगड़िस) थे, जो मंदिर की आवश्यकताओं जैसे दूध, घी और फूल, साथ ही पुरोहितों, मंदिर की महिलाओं, संगीतकारों, धोबियों और चौकीदारों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को पूरा करते थे।
बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण और प्रबंधन
- बृहदीश्वर मंदिर एक प्रमुख निर्माण परियोजना थी, जिसे पूरा करने में संभवतः 7 से 8 वर्ष लगे। यह विभिन्न क्षेत्रों और समूहों को अपनी आर्थिक नेटवर्क में आकर्षित करता था, जिसमें लेखों से पता चलता है कि 600 से अधिक कर्मचारी चोल साम्राज्य के विभिन्न भागों से मंदिर में काम करने के लिए आए थे।
- मंदिर के रखरखाव के लिए राजस्व दूरदर्शी गांवों से आया, जिनमें से कुछ श्रीलंका में थे। मंदिर के आर्थिक प्रबंधन की देखरेख कई गांवों के ब्राह्मण सभाओं द्वारा की गई, जबकि स्थानीय किसान, पशुपालक, और कारीगर इसकी कई आवश्यकताओं को पूरा करते थे।
Kudamukku और Palaiyarai, जो उर्वर कावेरी डेल्टा में एक-दूसरे के निकट स्थित हैं, इस अवधि के एक और महत्वपूर्ण शहरी परिसर का प्रतिनिधित्व करते हैं। Kudamukku एक पवित्र केंद्र था, जबकि Palaiyarai चोल महल परिसर का घर था। हालांकि इन बस्तियों का एक लंबा इतिहास है, लेकिन उन्होंने चोल काल के दौरान प्रमुखता प्राप्त की।
- Kudamukku, जो अपने मंदिरों के लिए जाना जाता है और अल्वार्स और नयनार्स के भक्ति गीतों में उल्लिखित है, ने राज परिवार, अधिकारियों, व्यापारियों और कारीगरों द्वारा अनुदानों के कारण विकास किया। यहाँ नगेश्वर मंदिर सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल बन गया।
- Kudamukku व्यापार मार्गों पर एक महत्वपूर्ण बिंदु था, जो सुपारी और सुपारी की खेती, साथ ही धातु कार्य और वस्त्र जैसे शिल्प में विशेषज्ञता रखता था। यहाँ एक चोल टकसाल भी स्थित थी।
- Palaiyarai, जिसका इतिहास 7वीं शताब्दी का है, प्रशासनिक केंद्र और चोलों की आवासीय राजधानी के रूप में प्रमुखता प्राप्त की। Kudamukku और Palaiyarai दोनों अपने ग्रामीण और तटीय Hinterlands से गहराई से जुड़े थे।
Madurai और Kanchipuram का राजनीतिक केंद्र और वस्त्र उत्पादन, विशेष रूप से कपास वस्त्रों, और धार्मिक गतिविधियों के रूप में एक लंबा इतिहास है। प्रारंभिक मध्यकालीन अवधि में, दोनों शहरों का आकार और महत्व बढ़ा। Kanchipuram, जो बुनाई और वाणिज्य का एक प्रमुख केंद्र था, को शिलालेखों और ग्रंथों में मनागरम (बड़ा शहर) के रूप में संदर्भित किया गया।
- Kanchipuram, जो पहले Palar नदी पर Nirppeyyarru के बंदरगाह से जुड़ा था, बाद में Mamallapuram को अपना प्राथमिक बंदरगाह के रूप में पहचानता था।
- Kanchipuram के Hinterland का विस्तार भूमि अनुदानों और बढ़ती मंदिर अर्थव्यवस्था द्वारा सुगम किया गया।
- Kanchipuram की आर्थिक भूमिका के अलावा, यह बौद्ध धर्म, जैन धर्म, विष्णुवाद, और शिववाद के केंद्र के रूप में सांस्कृतिक महत्व रखता था।
प्रारंभिक मध्यकालीन शहरी विकास ने कर्नाटक में जाति संगठन को प्रभावित किया। नए व्यापारिक जातियों जैसे Garvares, जो 10 से 11वीं शताब्दी में दक्षिण की ओर प्रवासित उत्तरी व्यापारियों का समावेश करते हैं, का उदय हुआ। अन्य व्यवसायिक समूह, जैसे गोडास और हेगाडेस, जातियों में विकसित हुए। गोडास, जो प्रारंभ में कृषि करने वाले या गांव के मुखिया थे, और हेगाडेस, जो मूल रूप से राजस्व अधिकारी थे, जातियों के रूप में पहचाने गए। इसके अतिरिक्त, पेशेवर लिपिक जिन्हें कराना कहा जाता था, जो कayasthas के समान थे, भी एक विशिष्ट जाति में विकसित हुए।
प्रारंभिक मध्यकालीन तमिलनाडु में बुनकर और बुनाई

बुनाई समुदायों का अवलोकन
- विजया रामास्वामी द्वारा 10वीं से 17वीं शताब्दी तक दक्षिण भारतीय बुनकरों पर किया गया विस्तृत शोध ऐतिहासिक वस्त्र केंद्रों और आज के केंद्रों के बीच एक निरंतर पैटर्न दर्शाता है। सालीयार और कैक्कोलर समुदाय प्रारंभिक मध्यकालीन तमिलनाडु में सबसे प्रमुख बुनाई समूह थे। चोल काल के दौरान, कैक्कोलर समुदाय ने बुनाई को सैन्य भूमिकाओं के साथ मिलाकर काम किया। बुनकरों के पास नगरों में निर्धारित आवासीय क्षेत्र थे, जो अक्सर मंदिरों के निकट स्थित होते थे, जैसा कि तंजावुर में देखा गया।
वस्त्र और तकनीकें
- ऐतिहासिक ग्रंथ और शिलालेख विभिन्न प्रकार के वस्त्रों और विनिर्माण तकनीकों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। मुसलिन (जिसे सेला कहा जाता है) और चित्त (जिसे विचित्र कहा जाता है) अत्यंत लोकप्रिय थे। प्राकृतिक रंगों जैसे लाल कुसुुम्बो, नीला, और मादर का सामान्य उपयोग होता था। 12वीं शताब्दी से दक्षिण भारत में ब्लॉक प्रिंटिंग लोकप्रिय हो गई। कारीगरों ने ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों प्रकार की ऊनी का उपयोग किया, जिनमें से पैटर्न वाले ऊनी 11वीं शताब्दी में सामान्य हो गए।
संगठन और व्यापार
- वस्त्र उद्योग अच्छी तरह से संगठित था, और वस्त्र आंतरिक और बाह्य व्यापार में महत्वपूर्ण वस्तुएं थीं। बुनकर अपने उत्पादों को स्थानीय मेलों में बेचते थे, जबकि शक्तिशाली व्यापारी संघ वस्त्र व्यापार के उच्च स्तरों को नियंत्रित करते थे। बुनकरों के संघों के विभिन्न नामों के प्रमाण हैं जैसे समया पट्टागरा, सaliya समायंगल, और सेनिया पट्टागरा। रामास्वामी ने दक्षिण भारत में कुछ बुनकर जातियों के प्रवास का उल्लेख किया है, संभवतः विजयनगर काल (15वीं–16वीं शताब्दी) के दौरान, जब बुनाई उद्योग अपने चरम पर था।
चोल संरक्षण और कराधान
- चोल वंश ने वस्त्र बुनाई उद्योग को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया और विभिन्न करों के माध्यम से इससे राजस्व एकत्र किया। शिलालेखों में कई करों का उल्लेख किया गया है जैसे कि तारी इराई या तारी कडामै (बुनाई कर), अच्चु तारी (संभवतः पैटर्न वाले ताने पर कर), तारी पुदवई (संभवतः कपड़े पर कर), पंजुपीली (कॉटन यार्न पर कर), परुत्ति कडामै (कॉटन पर कर), नुलयाम (कॉटन धागे पर कर), और कैबन्ना या बन्निगे (रंगाई वालों पर कर)। रेशमी धागे पर पट्टadai नुलयाम नामक कर लगाया गया था। राज्य ने बुनकरों को नए बस्तियों में आकर्षित करने के लिए कर राहत और छूट भी दी। चोल शासक कुलोत्तुंग I ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बंदरगाहों पर सीमा शुल्क को समाप्त करने के लिए जाने जाते हैं, जिससे उन्हें सुंगम तवीर्त चोलन (सीमा शुल्क हटाने वाला) का उपाधि प्राप्त हुआ।
बुनकरों की आर्थिक भागीदारी
- बुनकर केवल मंदिर दान में शामिल नहीं थे, बल्कि उन्होंने भूमि में भी निवेश किया और पैसे उधार देने के कार्यों में संलग्न थे। मद्रास संग्रहालय के ताम्र पत्रों से पता चलता है कि उत्तम चोल काल में राजा ने कुछ बुनकर समूहों को कांचिपुरम के उरागम मंदिर में उत्सव आयोजित करने के लिए धन सौंपा। कुछ बुनकरों को मंदिरों में प्रबंधकीय भूमिकाएँ सौंपी गईं, जो वित्त का प्रबंधन और खातों को बनाए रखते थे। उनके योगदान के मान्यता के रूप में, उन्हें कुछ करों से छूट दी गई।
जाति समूहों का उदय
- इस अवधि के दौरान एक महत्वपूर्ण विकास इडंगई (बाईं ओर) और वलंगई (दाईं ओर) जाति समूहों के रूप में एक सुप्रा-जाति विभाजन का उदय था। दाईं ओर के समूह में मुख्य रूप से कृषि जातियाँ थीं, जबकि बाईं ओर के समूह में ज्यादातर कारीगर और व्यापारिक समुदाय शामिल थे। प्रारंभ में, ये समूह शत्रुतापूर्ण नहीं थे, लेकिन समय के साथ, उनके बीच संघर्ष के तत्व उभरने लगे।
व्यापार और व्यापारी
व्यापार मार्ग और बंदरगाह: प्राचीन दक्षिण भारत में, व्यापार मार्ग पूर्वी तट पर विभिन्न बंदरगाहों पर एकत्रित होते थे। उल्लेखनीय बंदरगाहों में शामिल थे:
- मामल्लापुरम: पलवों के अधीन समृद्ध हुआ।
- नागापत्तिनम: चोल काल के दौरान प्रमुखता प्राप्त की।
- कावेरीपट्टिनम: महत्वपूर्ण लेकिन 11वीं सदी के बाद नागापत्तिनम से कम महत्वपूर्ण।
- तिरुप्पलैवनम और मयिलार्प्पिल: कांचीपुरम के उत्तर में स्थित तटीय नगर।
- कोवलम और तिरुवदंदाई: मामल्लापुरम के उत्तर में स्थित।
- सद्रास और पुदुपट्टिनम: मामल्लापुरम के दक्षिण में स्थित।
- अन्य तटीय नगर: इनमें पलवपट्टिनम, कडलोर और तिरुवेंदिपुरम शामिल हैं।
व्यापारी संघों की भूमिका: व्यापारियों के कॉर्पोरेट संगठनों ने इन बंदरगाह नगरों में वस्तुओं पर कस्टम शुल्क निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
क्विलोन (कोल्लम): यह पश्चिमी तट का बंदरगाह नगर है जिसमें मणिग्रामम संघ, विदेशी व्यापारियों और राजा के बीच समझौतों के संकेत मिले हैं। इन समझौतों में कर, गोदाम और व्यापारियों और उनकी वस्तुओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
व्यापार के प्रकार: बंदरगाह और बाजार नगर दोनों ही अंतरिक्ष व्यापार और दूरस्थ क्षेत्रों के साथ सीधे व्यापार में लगे हुए थे। व्यापार में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का समावेश था, जिसमें अनाज और विलासिता की वस्तुएं शामिल थीं।
वस्तुएं व्यापारित:
- 11वीं सदी: इस अवधि के शिलालेखों में चावल, दालें, तिल, नमक, काली मिर्च, तेल, कपड़ा, पान का पत्ता, सुपारी, और धातुओं जैसी वस्तुओं का उल्लेख है।
- 12वीं सदी: इस समय में गेहूं, खाद्य अनाज, मूंगफली, गुड़, चीनी, कपास, मसाले, हाथी, और रत्नों जैसी वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला दर्ज की गई।
- विलासिता की वस्तुएं: शिकारपुर (कर्नाटका) जैसे स्थानों के शिलालेखों में व्यापारियों द्वारा चंदन, कमफोर, मस्क, और विभिन्न कीमती रत्नों का परिवहन करने का उल्लेख है।
- आयात: आयात की गई वस्तुओं में अलोएवुड, चंदन, रेशम, गुलाब जल, और घोड़े शामिल थे, जो अक्सर दक्षिण-पूर्व एशिया, अरब और चीन जैसे क्षेत्रों से प्राप्त होते थे।
12वीं शताब्दी का विष्णु मंदिर, अंगकोर वाट, कंबोडिया: भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच सांस्कृतिक परस्पर क्रिया का एक उदाहरण
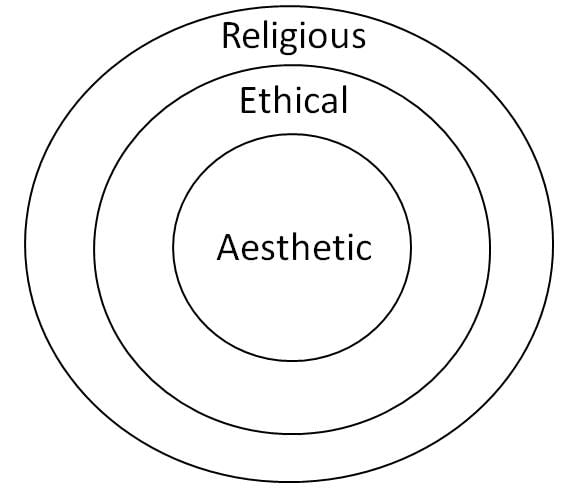
कंबोडिया में अंगकोर वाट का 12वीं शताब्दी का विष्णु मंदिर भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान का एक अद्वितीय उदाहरण है। यह मंदिर उस समय क्षेत्र में भारतीय वास्तुकला और धार्मिक प्रथाओं के प्रभाव को दर्शाता है।
ऐतिहासिक संदर्भ
- दक्षिण, पूर्वी और दक्षिण-पूर्व एशिया के अभिजात वर्ग के बीच बातचीत आपसी थी, जिसमें दोनों पक्षों ने सांस्कृतिक और धार्मिक विकास में योगदान दिया।
- बड़े लीदेन अनुदान में श्री विजया और कादरम के राजा द्वारा नागापट्टिनम में एक बौद्ध मठ के निर्माण के लिए प्रायोजन का उल्लेख है, जिसमें राजराज चोल ने इसके रखरखाव के लिए भूमि भी प्रदान की।
व्यापार और कूटनीतिक संबंध
- लेखों में नागापट्टिनम के मंदिरों में श्री विजया और कादरम के राजाओं द्वारा देवताओं को दिए गए विभिन्न उपहारों का उल्लेख है।
- खमेर राजा ने राजेंद्र I को उपहार भेजे, जबकि राजराज चोल ने चीन के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए, जैसा कि चीनी स्रोतों में चोल श्रद्धा मिशनों का उल्लेख है।
- ये मिशन मूल्यवान वस्तुएं लाए, जैसे हाथी के दांत, गैंडे के सींग, मोती, और वस्त्र, जिनकी चीन में उच्च मांग थी।
व्यापारी संघ और व्यापार
- जे. सी. वैन ल्यूर के सिद्धांत को चुनौती मिलती है कि भारत-पूर्वी एशिया व्यापार छोटे विक्रेताओं द्वारा नियंत्रित था, जबकि प्रारंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत में शक्तिशाली व्यापारी संघों के प्रमाण मिलते हैं।
- कॉर्पोरेट व्यापारी संगठनों, जिन्हें समय के रूप में जाना जाता है, 10वीं शताब्दी से प्रमुख हो गए, जिसमें अय्यावोले और मणिग्रामम संघों का लंबी दूरी के व्यापार में महत्वपूर्ण योगदान था।
- अय्यावोले, जो कर्नाटका के ऐहोल से आया था, एक प्रमुख उच्च-क्षेत्रीय व्यापारी संघ बन गया, जबकि मणिग्रामम, जो तमिलनाडु में आधारित था, 13वीं शताब्दी में अय्यावोले के अधीन हो गया।
- इन संघों की सदस्यता जाति और धार्मिक रेखाओं को पार करती थी, और उनके हस्तशिल्प विशेषज्ञ संघों के साथ संबंध थे।
भौगोलिक प्रसार और प्रभाव
- दक्षिण भारत, श्रीलंका, और पूर्व एवं दक्षिण-पूर्व एशिया में व्यापारी संघों का व्यापक प्रभाव दर्शाते हुए गिल्ड शिलालेख मिले हैं।
- श्रीलंका में पदाविया में मिले एक शिलालेख में अय्यवोले की प्रशंसा की गई थी, और सुमात्रा में 1088 CE का एक गिल्ड शिलालेख मिला था।
- मणिग्रामम ने थाईलैंड के ताकुआपा में एक आधार स्थापित किया, जहां भारतीय कलाकृतियों और शिलालेखों के सबूत हैं, जो तमिल व्यापारियों के स्वायत्त बस्ती का संकेत देते हैं।
- चीन में, क्वांझोउ में हिंदू चित्रों और एक तमिल-चीनी शिलालेख की खोज ने 13वीं/14वीं सदी में एक तमिल व्यापारी उपनिवेश की उपस्थिति को दर्शाया।
धार्मिक क्षेत्र
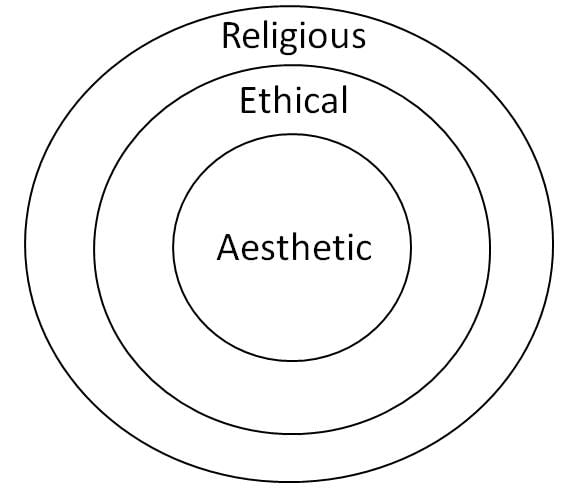
जुन्झांग ने मगध क्षेत्र में कई बड़े और समृद्ध मठों का निरीक्षण किया, जिनमें नालंदा, तिलोदक और बोध गया शामिल हैं। हालांकि, उन्होंने अन्य क्षेत्रों में कई सुनसान या जर्जर मठों का भी उल्लेख किया। चीनी तीर्थयात्री ने नालंदा में योगचार doctrine पर अध्ययन करने के लिए पांच वर्षों से अधिक समय समर्पित किया। इसी प्रकार, यिज़िंग ने बोध गया और तिलोदक का दौरा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि तिलोदक में लगभग 1,000 भिक्षु थे।
जुन्झांग के मठों पर अवलोकन
- निर्माण और डिज़ाइन: जुन्झांग ने उस समय के मठों का एक सामान्य अवलोकन प्रस्तुत किया, जिसमें उनके कुशल निर्माण को उजागर किया। उन्होंने प्रत्येक पक्ष पर तीन मंजिला टॉवर, समृद्ध रंगीन दरवाजे और खिड़कियाँ, और कम ऊँची दीवारों जैसी विशेषताओं का उल्लेख किया।
- भिक्षुओं के कक्ष: भिक्षुओं के कक्ष बाहरी रूप से साधारण लेकिन आंतरिक रूप से भव्य सजाए गए थे।
- सभा हॉल और कक्ष: मठों में आमतौर पर बड़े, ऊँचे सभा हॉल होते थे, जो भवन के मध्य में स्थित होते थे, साथ ही विभिन्न ऊँचाई की मंजिलों वाले कक्ष और टर्रेट, सभी के दरवाजे पूर्व की ओर होते थे।
पाठ्य और पुरातात्विक साक्ष्य
- पाठ्य स्रोत और लेख: ये स्रोत प्रारंभिक मध्यकालीन अवधि के मठों के स्थानों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।
- पुरातात्विक अवशेष: ऐतिहासिक ग्रंथों में उल्लिखित कई मठों की पहचान पुरातात्विक अवशेषों के माध्यम से की गई है, जो उस समय के दौरान उनके अस्तित्व और महत्व की पुष्टि करते हैं।
जुन्झांग का प्रज्ञादेव को उत्तर
645 ईस्वी में चीन लौटने के बाद, जुन्झांग ने चांग'an में त्ज़ु-एन मठ में संस्कृत से चीनी में बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद करने में अपने आप को समर्पित किया। इस दौरान, उन्होंने भारत में मिले कई भिक्षुओं के साथ संपर्क बनाए रखा, जिनमें प्रज्ञादेव भी शामिल थे, जो बोध गया के महाबोधि मठ में एक वरिष्ठ भिक्षु थे। प्रज्ञादेव ने जुन्झांग को एक गीत भेजा, जिसे उन्होंने रचा था, और कपास का cloth भेंट किया, यह प्रस्ताव करते हुए कि यदि जुन्झांग को किसी बौद्ध ग्रंथ की आवश्यकता हो तो वह प्रदान करेंगे। प्रज्ञादेव की इस उदारता के जवाब में, जुन्झांग ने अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और अपने कार्य और विचारों के बारे में अपडेट साझा किए।
प्रज्ञानदेव की कृपा
- शुयांज़ांग को भीखshu धर्मदीर्घा से एक पत्र मिला, जिसमें प्रज्ञानदेव की ओर से कपास के कपड़े और एक भजन शामिल था।
- शुयांज़ांग ने प्रज्ञानदेव की उदारता के कारण शर्म महसूस की, यह मानते हुए कि वह ऐसी कृपा का पात्र नहीं हैं।
शुयांज़ांग का प्रज्ञानदेव पर विचार
- शुयांज़ांग ने प्रज्ञानदेव की प्रशंसा की और फिर से संपर्क करने की इच्छा व्यक्त की, यह बताते हुए कि उन्हें उनकी बातचीत की कितनी याद आती है।
- उन्होंने प्रज्ञानदेव की विभिन्न बौद्ध स्कूलों की गहरी समझ, सही मार्ग पर लोगों को मार्गदर्शित करने की क्षमता, और प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ संवाद करने की कला की सराहना की।
भारत की यादें
- शुयांज़ांग ने भारत में अपने समय को याद किया, विशेष रूप से कanyakubja में हुई बहसों को, जहां उन्होंने महायान और हीनयान स्कूलों के विचारों पर राजकुमारों और बड़े दर्शकों के सामने चर्चा की।
- हालांकि उनकी बहस गर्मागर्मी भरी थी, शुयांज़ांग ने सराहना की कि वे बाद में एक-दूसरे के प्रति द्वेष नहीं रखते थे।
क्षमापना और सम्मान
- शुयांज़ांग ने प्रज्ञानदेव द्वारा किसी भी पूर्व असहमति के लिए क्षमा मांगने को स्वीकार किया, इसे प्रशंसनीय और उनके चरित्र का प्रतीक पाया।
- शुयांज़ांग का एक साथी भिक्षु को पत्र, जिसमें उन्होंने उसकी विशेषताओं की प्रशंसा की और उसे अन्य स्कूलों के बजाय महायान बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया।
- शुयांज़ांग का मानना है कि महायान तर्क और तर्क-वितर्क में श्रेष्ठ है, और भिक्षु से अपनी शंकाओं पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया।
- उन्होंने एक स्मृति चिन्ह भेजने का भी उल्लेख किया और खोई हुई शास्त्रों की वापसी का अनुरोध किया।
भारत में बौद्ध धर्म का पतन और पुनरुत्थान
बौद्ध धर्म का पतन (11वीं सदी के बाद)
- कश्मीर के बौद्ध मठों, जैसे कि जयेंद्र और राजा मठ, 11वीं शताब्दी तक गिरावट का सामना कर रहे थे। इस गिरावट के बावजूद, कुछ मठ जैसे कि रत्नगुप्त और रत्नरश्मि, अनुपमपुरा में 11वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान फल-फूल रहे थे। सांची, अमरावती और सिंध जैसे क्षेत्रों में, बौद्ध धर्म कई शताब्दियों तक फलता-फूलता रहा। बंगाल और बिहार के पालों ने बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण संरक्षक के रूप में कार्य किया, जिन्होंने नालंदा, ओदंतपुरा, विक्रमशिला, और सोमपुर जैसे विभिन्न मठों का समर्थन किया। तिब्बती भिक्षुओं और इन बौद्ध केंद्रों के बीच सक्रिय इंटरएक्शन हुआ, जिससे विचारों और प्रथाओं का आदान-प्रदान संभव हुआ।
अन्य क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान
- प्रारंभिक मध्यकालीन बौद्ध स्तूपों, मठों, और मूर्तियों के अवशेष ओडिशा में, विशेष रूप से ललितगिरी और रत्नगिरी में खोजे गए। नेपाल में इस अवधि के दौरान कई बौद्ध विहारों का निर्माण हुआ, जो बौद्ध प्रथाओं के पुनरुत्थान का संकेत देते हैं। लद्दाख, लाहुल, और स्पीति जैसे क्षेत्रों में भी बौद्ध विहारों की स्थापना हुई, जिसने इन क्षेत्रों में बौद्ध धर्म के फैलाव में योगदान दिया। तांत्रिक बौद्ध धर्म प्रमुख मठ केंद्रों पर एक प्रमुख प्रथा के रूप में उभरा, जो भारत में बौद्ध परंपराओं की विकसित होती प्रकृति को दर्शाता है।
बौद्ध पूजा और अनुष्ठानों का विकास

प्रारंभिक मध्यकालीन अवधि: विविध चित्रकला और भक्ति प्रथाएँ
- प्रारंभिक मध्यकालीन बौद्ध छवियों ने विभिन्न चित्रात्मक रूपों की विस्तृत श्रृंखला का प्रदर्शन किया, जो इस समय के दौरान भक्ति पूजा की विविधता और लोकप्रियता को दर्शाता है। शांति देव द्वारा लिखित 8वीं शताब्दी की ग्रंथ बोधिचार्यवतार में महायान पूजा अनुष्ठानों का वर्णन किया गया है, जिसमें शामिल थे:
- सुगंधित जल से छवि को स्नान कराना
- खाना, फूल और वस्त्र अर्पित करना
- धूपदान और अगरबत्ती जलाना
- गायन और वाद्य संगीत का प्रदर्शन
दान संबंधी शिलालेख और अनुष्ठान प्रावधान
- वालभी के मैत्रक की शिलालेखों से पता चलता है कि धूप, दीपक, तेल, और फूल (धूप-दीप-तैल-पुष्प) के लिए अनुष्ठान के खर्चे को कवर करने के लिए प्रावधान किए गए थे। यह प्रारंभिक मध्यकालीन बौद्ध पूजा में इन बलिदानों के महत्व को उजागर करता है।
तांत्रिक बौद्ध धर्म का उदय
- प्रारंभिक मध्यकालीन काल में तांत्रिक बौद्ध धर्म का उदय हुआ, जिसने अनुष्ठान, जादू और ध्यान को एकीकृत किया। इस परंपरा के सबसे प्रारंभिक ग्रंथ, जैसे कि मञ्जुश्रीमूलकल्प और गुह्यसमाज (5वीं–6वीं शताब्दी), ने तांत्रिक प्रथाओं की नींव रखी।
वज्रयान: बिजली या हीरा वाहन
- तांत्रिक बौद्ध धर्म, जिसे वज्रयान कहा जाता है, ने बिजली और हीरे को शक्ति और ताकत के प्रतीक के रूप में महत्व दिया, जो उन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करते थे जिन्होंने सिद्धि (ज्ञान) प्राप्त किया। वज्र-संकट और घंटी वज्रयान अनुष्ठान उपकरणों में महत्वपूर्ण तत्व बन गए।
मंत्रयान: मंत्रों का वाहन
- तांत्रिक बौद्ध धर्म का एक अन्य पहलू मंत्रयान था, जिसने आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए मंत्रों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया। छः-स्वर वाला मंत्र ओम मणि पद्मे हम, जो Avalokiteshvara से संबंधित है, विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। इस मंत्र में पवित्र ध्वनियाँ और प्रतीकात्मक अर्थ थे, जिन्हें महान आध्यात्मिक शक्ति रखने वाला माना जाता था।
महिला देवताओं और सिद्धों की भूमिका
- महिला देवताओं, विशेष रूप से तारा, ने वज्रयान पैंथियन में एक प्रमुख स्थान प्राप्त किया। सिद्ध या तंत्र-गुरु, जो तांत्रिक बौद्ध धर्म के प्रवक्ता थे, ने इन शिक्षाओं के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
हेवज्र तंत्र और सहजयान
- हेवाज्रा तंत्र ने यौन ऊर्जा के उत्कर्ष के माध्यम से मुक्ति का प्रस्ताव दिया, जिसमें जटिल अनुष्ठान शामिल थे।
- इसके विपरीत, सहजयान मार्ग, जिसे महासिद्ध सरहा ने सिखाया, ने अंतर्दृष्टि और गुरु द्वारा प्रत्यक्ष निर्देश पर जोर दिया, जिससे सांसारिक जीवन में लगे रहते हुए मुक्ति की स्थिति प्राप्त की जा सके।
- सहजियाओं ने, जो विशेष रूप से बंगाल में प्रभावी थे, जटिल दर्शन और भक्ति प्रथाओं को त्यागकर मुक्ति के लिए अंतर्दृष्टिपूर्ण समझ को प्राथमिकता दी।
उपमहाद्वीप में बौद्ध धर्म काDecline
बौद्ध धर्म भारतीय उपमहाद्वीप से पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ, लेकिन इसका अवनति हुआ, जो भूगोलिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिधियों तक सीमित हो गया। इस अवनति को समझाने के लिए कई कारकों का प्रस्ताव किया गया है:
- पहचान संकट: बौद्ध धर्म उभरते हिंदू पंथों के संबंध में एक अलग पहचान बनाए रखने में संघर्ष कर रहा था।
- तांत्रिक प्रभाव: तांत्रिक प्रथाओं का बढ़ता प्रभाव बौद्ध धर्म के भीतर एक 'क्षय' की धारणा में योगदान कर रहा था।
- पुनरुत्थानशील हिंदू धर्म: एक पुनरुत्थानशील हिंदू धर्म, विशेष रूप से शंकरा जैसे विचारकों द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया, बौद्ध प्रथाओं और विश्वासों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत करता था।
- तुर्की आक्रमण: तुर्की आक्रमणों ने कई प्रमुख बौद्ध मठ केंद्रों को नष्ट कर दिया, जो प्रमुख और आसानी से पहचाने जाने योग्य लक्ष्य थे।
इन चुनौतियों के बावजूद, इस अवधि के दौरान तिब्बत और पश्चिमी हिमालय में स्थापित कुछ मठों का एक निरंतर इतिहास है जो वर्तमान दिन तक फैला हुआ है। हालांकि, प्राचीन मध्यकालीन भारत में बौद्ध धर्म के इतिहास के विशेष पहलुओं, विशेष रूप से घटती सामुदायिक समर्थन और प्रायोजन के कारण, स्पष्ट नहीं हैं।
तांत्रिक बौद्ध धर्म के सामाजिक पहलू
मिरांडा शॉ का अध्ययन
- तांत्रिक बौद्ध धर्म में महिलाएं और पुरुष: मिरांडा शॉ के शोध के अनुसार, महिलाएं और पुरुष दोनों तांत्रिक पथ में आवश्यक हैं, जो गैर-शोषणकारी, गैर-बलात्कारी, और आपसी ज्ञानवर्धक संबंध बनाने में सक्षम हैं।
- पुरुष और महिला बुद्धों का संघ: यह विचार एक पुरुष और महिला बुद्ध की छवि में परिलक्षित होता है, जो ज्ञान के प्रतीक के रूप में एकजुट होते हैं।
- महिलाओं की भूमिका: शॉ का तर्क है कि महिलाओं ने तांत्रिक बौद्ध धर्म के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और शिक्षकों, छात्रों, साधकों, और नवप्रवर्तकों के रूप में सक्रिय रूप से भाग लिया।
रोनाल्ड एम. डेविडसन का विश्लेषण
- तांत्रिक बौद्ध धर्म और सामाजिक परिवर्तन: डेविडसन ने तांत्रिक बौद्ध धर्म को प्रारंभिक मध्यकालीन अवधि में व्यापक राजनीतिक, सामाजिक, और आर्थिक परिवर्तनों से जोड़ने का प्रयास किया।
- देवताओं का सामंतकरण: उन्होंने देवताओं के 'सामंतकरण' का सुझाव दिया, जहाँ देवताओं को राजाओं की तरह एक सर्वोच्चता और अधीनता की पदानुक्रम में व्यवस्थित किया गया।
- राजनीतिक गूंज: तांत्रिक बौद्ध धर्म का व्यक्तिगतराजत्व और प्रभुत्व का उपमा उस समय के राजनीतिक विषयों को दर्शाती है।
नए बौद्ध रूपों का विकास
- पुराने समर्थन का पतन: नए बौद्ध रूपों को पारंपरिक समर्थन और संरक्षण के स्त्रोतों के पतन से निपटना पड़ा।
- नए नेटवर्क का निर्माण: सिद्धों (आध्यात्मिक साधकों) ने राजनीतिक संरक्षण के नए नेटवर्क विकसित किए और जनजातीय और अछूत समूहों के साथ संपर्क किया।
- मठों की वृद्धि: कुछ मठ महाविहारों (महान मठों) में विकसित हुए और बड़े ज़मींदार बन गए।
- महिलाओं की भागीदारी में कमी: मठीय और श्रमिक स्तरों पर महिलाओं की भागीदारी में स्पष्ट कमी आई, जो उपमहाद्वीप में उनके भूमिकाओं को दर्शाने वाली लेखों की कमी से स्पष्ट है।
जैन धर्म के प्रमुख केंद्र
जैन धर्म का विकास भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ, जिसमें राजस्थान, गुजरात, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका शामिल हैं। ऐतिहासिक रिकॉर्ड, जैसे कि चीनी भिक्षु शुआनजांग का, यह संकेत देते हैं कि जैन धर्म के दिगंबर सम्प्रदाय का अभ्यास कुछ समय पर श्वेतांबर सम्प्रदाय की तुलना में अधिक व्यापक था।
जैन धर्म को विभिन्न राजवंशों से महत्वपूर्ण शाही संरक्षण प्राप्त हुआ:
- गुजरात में, चापाओं ने महत्वपूर्ण संरक्षक के रूप में कार्य किया।
- मध्य भारत में, परमार राजाओं ने भी जैन संस्थानों का समर्थन किया।
- दक्षिण भारत में, गंग, राष्ट्रकूट, पूर्वी और पश्चिमी चालुक्य, और कादंब राजवंशों ने जैन विद्वानों और संस्थानों को संरक्षण दिया।
इस अवधि के दौरान, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, कन्नड़ और तमिल जैसी विभिन्न भाषाओं में जैन ग्रंथों की एक बड़ी संख्या लिखी गई। इस युग के कुछ प्रमुख जैन दार्शनिक और तर्कशास्त्री हैं:
- अकालंका, जो 8वीं सदी में जीवित थे और जिनका कार्य तत्त्वार्थराजवर्त्तिका जैन तर्कशास्त्र में महत्वपूर्ण पाठ है।
- हरिभद्र, एक अन्य तर्कशास्त्री, जिन्होंने पूर्व के कार्यों पर टिप्पणियाँ लिखीं और जिनका बौद्ध और ब्राह्मणिक सिद्धांतों की आलोचना में योगदान था, जैसे कि अनेकांतजयपत्रक।
- विद्यानंद, जो 9वीं सदी के पाटलीपुत्र के विद्वान थे, जिन्होंने अप्तमिमांसा जैसे कार्यों की रचना की, जो तर्क के सिद्धांतों का अन्वेषण करते हैं।
आदि पुराण, जिसे 8वीं सदी में जिनसेना और गुणभद्र ने लिखा, जीवन-चक्र की संस्कारों (संस्कारों) का एक सेट प्रस्तुत करता है, जो ब्राह्मणिक प्रथाओं के समान होते हुए भी जैन व्याख्याओं को विशेषता देते हैं। इस पाठ ने ब्राह्मणिक पूर्वाग्रहों को भी दर्शाया, stating that शूद्रों को कुछ उच्च धार्मिक प्रथाओं, जिसमें संन्यास भी शामिल था, से बाहर रखा गया था।

श्रवण बेलगोला में गम्मतेश्वर की विशाल प्रतिमा
- श्रवण बेलगोला, कर्नाटका, भारत के हासन जिले के चन्नारायपटना तालुक का एक छोटा शहर है, जो जैनों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है।
- इस शहर का नाम संस्कृत शब्द "श्रमान" से आया है, जिसका अर्थ है 'तपस्वी', और कन्नड़ शब्द "बेला-कोला" से, जिसका अर्थ है 'सफेद टैंक'।
- यह दो चट्टानी पहाड़ियों, चंद्रगिरी (या चिक्काबेट्टा) औरVindhyagiri (या इंद्रगिरी, जिसे डोड्डाबेट्टा भी कहा जाता है) के बीच स्थित है।
- श्रवण बेलगोला में 37 जैन मंदिर हैं, जो 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच बने।
- यहां एक जैन मठ है, जिसमें 17वीं से 18वीं शताब्दी की भित्ति चित्र हैं।
- इस शहर में 500 से अधिक शिलालेख हैं, जो इसके इतिहास का विवरण देते हैं।
- हालांकि, श्रवण बेलगोला अपनी 17.5 मीटर ऊँची गम्मतेश्वर (बाहुबली) की विशाल प्रतिमा के लिए सबसे प्रसिद्ध है। यह प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊँची स्वतंत्र मोनोलिथिक (एकल पत्थर) मूर्ति मानी जाती है।
- जैन परंपरा के अनुसार, गम्मता या बाहुबली आदिनाथ का पुत्र है, जो पहले तीर्थंकर हैं।
- 10वीं शताब्दी के कन्नड़, तमिल और मराठी में शिलालेख, जो प्रतिमा के आधार पर पाए गए, बताते हैं कि इसे गंगा के राजा रचमल्ल (राजामल्ला) के मंत्री चमुंडा राजा द्वारा स्थापित कराया गया था, जो 974 से 984 ईस्वी तक शासन करते थे।
- बाहुबली की प्रतिमा, जो हल्के भूरे ग्रेनाइट से बनी है, एक पहाड़ी के शीर्ष पर स्थित है और इसे 10 किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है, हालांकि यह पहाड़ी के तल से दिखाई नहीं देती।
- प्रतिमा को घेरकर, घुटनों तक गोलाई में तराशा गया है, जहां यह चट्टान के साथ मिलती है। इसकी सतह अत्यधिक चमकदार है।
- बाहुबली को कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े दर्शाया गया है, जिसमें उसके हाथ और पैर सीध में हैं और उसके हाथ उसके शरीर से नहीं छू रहे हैं।
- उसके पैरों के नीचे एक पूर्ण खिलते कमल का फूल है।
- बाहुबली की आकृति चौड़े कंधों, पतले कमर और चौड़े कूल्हों के साथ है।
- उसके बाल घुंघराले हैं, और उसका चेहरा चौड़ा है, जिसमें अच्छी तरह से आकारित ठोड़ी और नाक है।
- उसके लंबे कान की लोब और असामान्य रूप से लंबे हाथ हैं, जो एक महापुरुष (महान व्यक्ति) के लक्षण हैं।
- उसकी बाहों और पैरों पर बेलें लिपटी हुई हैं, और उसके जांघों तक चींटियों के टीले हैं, जो उसकी असाधारण तपस्या का प्रतीक हैं।
- उसकी अभिव्यक्ति शांत और दृढ़ है, जिसमें एक हल्की मुस्कान है, जो आंतरिक शांति को दर्शाती है।
- उसके बगल में एक यक्ष और यक्षी की मूर्तियाँ हैं।
- हर 12 वर्ष में, एक समारोह होता है जिसे महामस्तकाभिषेक कहा जाता है, जिसमें भक्त प्रतिमा के सिर पर दूध, फूल और रत्न जैसे चढ़ावे चढ़ाते हैं।
- हाल का महामस्तकाभिषेक 2006 में हुआ था।
प्रारंभिक मध्यकाल में जैन धर्म
प्रारंभिक मध्यकाल में, जैन धर्म का भारत के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण स्थान था, जिसमें महत्वपूर्ण मंदिरों और शिलालेखों से इसके प्रभाव का संकेत मिलता है।
जैन तीर्थ और मंदिर
- जैन तीर्थों का प्रारंभिक मध्यकालीन दौर आधुनिक उत्तर प्रदेश में पाया गया, विशेषकर देओगढ़ और मथुरा जैसे स्थानों पर।
- दिलवाड़ा मंदिर, माउंट आबू में, इस अवधि के सबसे प्रभावशाली जैन मंदिरों में से एक हैं।
- गुजरात में जैन केंद्रों में भृगुकच्छ, गिरनार और वलभि शामिल थे, जिसमें वलभि चंद्रप्रभ और महावीर को समर्पित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है।
- मध्य भारत में जैन स्थापनाएँ सोनेगिरी और खजुराहो में मौजूद थीं।
- पश्चिमी भारत में नासिक और प्रतिष्ठान में जैन केंद्र स्थापित हुए थे, साथ ही एलोरा में जैन गुफाएँ भी पाई गईं।
- उड़ीसा में उदयगिरी और खंडगिरी में जैन स्थलों ने इस अवधि में अपने विकास को जारी रखा।
कर्नाटका और दक्षिण भारत में जैन धर्म
- कर्नाटका क्षेत्र में जैन धर्म मजबूत था, जैसा कि पुलकेशिन II के ऐहोल लेख से स्पष्ट है, जिसमें कवि राविकीरति का उल्लेख है और उनके मंदिर निर्माण में योगदान का वर्णन है।
- श्रवण बेलगोला, कोप्पाना, और हलैबिड जैसे स्थानों पर जैन मंदिर और लेख पाए गए हैं।
- तमिलनाडु में पलव और चोल तथा पांड्य राजाओं के शासनकाल से संबंधित लेखों में विभिन्न जैन संतों का उल्लेख है, जैसे कि अजयनंदी, इंदुसेना, और मल्लीसेना।
- श्रवण बेलगोला में जैन लेखों में पोंटिफिकल उत्तराधिकार की लंबी सूचियाँ प्रदान की गई हैं, जो सदियों से जैन नेतृत्व की निरंतरता और महत्व को दर्शाती हैं।
निष्कर्ष
- प्रारंभिक मध्यकालीन काल के अंत तक, जैन धर्म गुजरात, राजस्थान और कर्नाटका में एक महत्वपूर्ण उपस्थिति बनाए रखता था, जिसमें मंदिरों, लेखों और धार्मिक नेताओं की निरंतरता का समृद्ध विरासत था।
शंकर और अद्वैत वेदांत
भारत में मध्यकालीन अवधि के दौरान, विभिन्न दर्शनों में दार्शनिक लेखन में वृद्धि हुई। इस समय के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों में से एक शंकर थे, जो 8वीं और 9वीं सदी के अंत में जीवित थे। हालांकि, शंकर के जीवन की कथाओं में ऐतिहासिक तथ्यों को परीकथाओं से अलग करना कठिन है, क्योंकि ये विवरण 14वीं सदी के बाद लिखे गए थे।
- सबसे प्रसिद्ध जीवनी, शंकर-दिग्विजय जो मधव द्वारा लिखी गई है, शंकर को एक भटकते दार्शनिक के रूप में प्रस्तुत करती है, जिन्होंने भारत भर में विभिन्न विरोधियों के साथ बहस की और उन्हें पराजित किया। शंकर को वेदांत में उनके योगदान के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से उनके व्याख्या अद्वैत वेदांत के लिए।
- शब्द "वेदांत" वेदों के अंत (अंत) के भाग को दर्शाता है, और यह उपनिषदों को संदर्भित करता है, जो इस दार्शनिकता का आधार हैं। उपनिषद, साथ ही बादरायण के ब्रह्म सूत्र और भगवद गीता, वेदांत दर्शन का मूल रूप हैं।
- अद्वैत वेदांत की सबसे प्रारंभिक विस्तृत व्याख्या गौडपाद द्वारा 7वीं या 8वीं सदी में की गई थी। उनका काम, मांडूक्यकारिका, मांडूक्य उपनिषद पर एक टिप्पणी है और यह बौद्ध विचारों से प्रभावित है, विशेषकर मध्यमिका और विज्ञानवाद बौद्ध धर्म से।
- गौडपाद ने तर्क किया कि भौतिक वस्तुएं सपनों के समान हैं, यह सुझाव देते हुए कि वास्तविकता मौलिक रूप से एक (अद्वैत) है और विविधता की धारणा माया या भ्रांति से उत्पन्न होती है।
- शंकर ने गौडपाद के विचारों का विस्तार करते हुए दिखाने का प्रयास किया कि उपनिषद और ब्रह्म सूत्र एक सुसंगत दार्शनिक प्रणाली प्रस्तुत करते हैं।
- अपने ब्रह्म सूत्र पर टिप्पणी में, शंकर ने वेदिक बलिदानों के बीच अंतर पर जोर दिया, जो भौतिक लाभ के लिए होते हैं, और उपनिषद, जो अंतिम ज्ञान का मार्ग प्रदान करते हैं।
- शंकर के दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत ब्रह्म है, जिसे अंतिम वास्तविकता माना जाता है, जो गुण रहित (निर्गुण), शुद्ध चेतना, और अपरिवर्तनीय है। उन्होंने प्रस्तावित किया कि परिवर्तन और विविधता केवल प्रकट होते हैं।
- शंकर ने वास्तविकता के दो स्तरों का विचार भी प्रस्तुत किया: पारंपरिक और निरपेक्ष। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति एक कुंडलित रस्सी को सांप समझ लेता है, तो वह पारंपरिक वास्तविकता को निरपेक्ष वास्तविकता के साथ भ्रमित कर रहा है। यह भ्रम अविद्या से उत्पन्न होता है।
- अद्वैत वेदांत का लक्ष्य आत्मा (व्यक्तिगत आत्मा) की ब्रह्म (सार्वभौमिक चेतना) के साथ एकता को पहचानते हुए पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना है।
- कुछ विद्वानों का मानना है कि शंकर का वेदिक परंपरा में स्थिर समर्थन भारत में बौद्ध धर्म केDecline में योगदान करता है।
- दिलचस्प बात यह है कि उनके आलोचकों ने उन्हें "गुप्त बौद्ध" करार दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि दुनिया के प्रति उनका दृष्टिकोण भ्रांति के समान है, जो महायान बौद्ध विचारों के समान है।
- हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उपनिषदों की अपनी व्याख्या का बचाव करते समय, शंकर ने बौद्ध धर्म, सांख्य, न्याय, और मीमांसा सहित अन्य दार्शनिक स्कूलों के विरोधों का भी उत्तर दिया।
- शंकर को दशनामी संप्रदाय की स्थापना का श्रेय दिया जाता है और उन्होंने चार या पांच मठों की स्थापना की, जिन्हें अमनय मठ कहा जाता है।
- हालांकि शंकर की शिक्षाओं को संरक्षित और प्रचारित करने के लिए एक संगठनात्मक रूप उभर कर आया, कई इतिहासकारों का कहना है कि श्रृंगेरी और कांची जैसे मठ कई शताब्दियों बाद स्थापित हुए और उन्हें शंकर के नाम से जोड़ा गया ताकि उनकी प्रतिष्ठा बढ़ सके।
- उदाहरण के लिए, श्रिंगेरी मठ का 14वीं सदी में विजयनगर काल के दौरान स्थापित होने का अनुमान है।
|
125 videos|399 docs|221 tests
|




















