रामेश सिंह संक्षेप: उद्योग और अवसंरचना - 1 | Famous Books for UPSC CSE (Summary & Tests) in Hindi PDF Download
परिचय
पश्चिमी अर्थव्यवस्थाएँ पहले ही औद्योगिकीकरण में सफल हो चुकी थीं, इससे पहले कि भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की। स्वतंत्रता के बाद, भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को एक गंभीर रूप से बिगड़े हुए स्थिति से पुनर्जीवित करने की आवश्यकता थी।
उद्योग एवं अवसंरचना
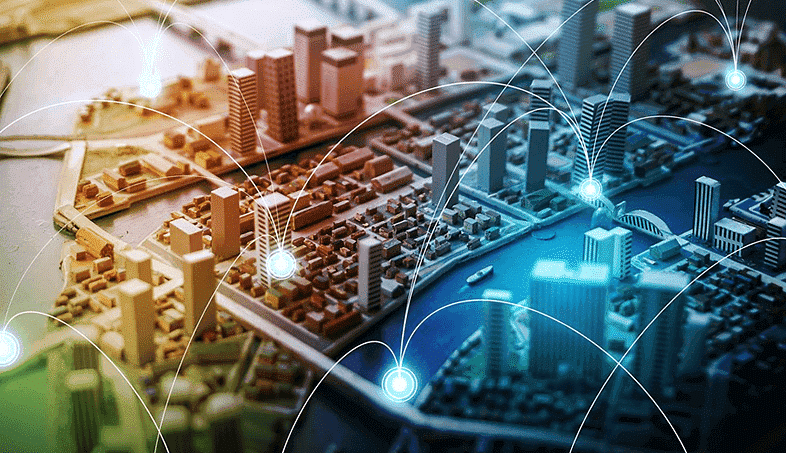
- चुनौतियाँ थीं: व्यापक गरीबी, खाद्य कमी, स्वास्थ्य सेवा की कमियाँ आदि, जो तात्कालिक ध्यान की मांग कर रही थीं।
- केंद्रित क्षेत्रों में उद्योग, अवसंरचना, विज्ञान, तकनीक और उच्च शिक्षा शामिल थे।
- इन क्षेत्रों को उपनिवेशी शासन के दौरान उपेक्षा के कारण महत्वपूर्ण पूंजी निवेश की आवश्यकता थी।
- तेजी से आर्थिक विकास एक आवश्यक आवश्यकता थी। भारत ने तेजी से विकास के लिए औद्योगिक क्षेत्र को 'प्राइम मूविंग फोर्स' के रूप में प्राथमिकता देने का विकल्प चुना।
- द्वितीयक क्षेत्र को अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने के लिए नामित किया गया, यह निर्णय 1930 के दशक में प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा लिया गया।
- सरकार की अर्थव्यवस्था में सक्रिय भूमिका के कारण, औद्योगिक क्षेत्र ने एक प्रमुख राज्य भूमिका ग्रहण की।
- सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों (PSUs) को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
- भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास मुख्यतः सरकारी क्षेत्र की वृद्धि के साथ समानांतर रहा।
- भारी राज्य भागीदारी की विरासत महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों के बावजूद बनी रही।
- सरकार द्वारा घोषित औद्योगिक नीतियों ने अर्थव्यवस्था की मौलिक प्रकृति और संरचना को आकार दिया।
1986 तक औद्योगिक नीतियों की समीक्षा
- औद्योगिक नीति प्रस्तावना, 1948
- (i) 8 अप्रैल, 1948 को घोषित, यह न केवल भारत की पहली औद्योगिक नीति घोषणा थी, बल्कि यह आर्थिक प्रणाली के मॉडल (यानी, मिश्रित अर्थव्यवस्था) को भी तय करती थी।
- (ii) कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों को केंद्रीय सूची में रखा गया जैसे कि कोयला, बिजली, रेलवे, नागरिक उड्डयन, सैन्य सामग्री, रक्षा आदि।
- (iii) कुछ अन्य उद्योगों (आम तौर पर मध्यम श्रेणी के) को राज्य सूची में रखा गया जैसे कि कागज, औषधियाँ, वस्त्र, साइकिल, रिक्शा, दोपहिया आदि।
- (iv) बाकी के उद्योग (जो केंद्रीय या राज्य सूची में शामिल नहीं थे) निजी क्षेत्र के निवेश के लिए खुला छोड़ दिया गया- जिनमें से कई में अनिवार्य लाइसेंसिंग का प्रावधान था।
- औद्योगिक नीति प्रस्तावना, 1956
- (i) सरकार को 1948 की औद्योगिक नीति के प्रभाव से प्रोत्साहित किया गया।
- (ii) उद्योगों का आरक्षण - उद्योगों का स्पष्ट वर्गीकरण (जिसे उद्योगों के आरक्षण के रूप में भी जाना जाता है) तीन अनुसूचियों के साथ किया गया।
- (iii) अनुसूची A - इस अनुसूची में 17 औद्योगिक क्षेत्र शामिल थे जिनमें केंद्र को पूर्ण एकाधिकार दिया गया। इन उद्योगों को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (CPSUs) के रूप में जाना गया, जो बाद में 'PSUs' के रूप में लोकप्रिय हुए।
- (iv) अनुसूची B - इस अनुसूची में 12 औद्योगिक क्षेत्रों को रखा गया, जिसमें राज्य सरकारों को निजी क्षेत्र के साथ अधिक व्यापक पहल करने की जिम्मेदारी दी गई।
- (v) अनुसूची C - सभी औद्योगिक क्षेत्र जो अनुसूची A और B से बाहर थे, उन्हें इस अनुसूची में रखा गया, जिसमें निजी उद्यमों को उद्योग स्थापित करने की अनुमति थी।
- (vi) लाइसेंसिंग का प्रावधान - स्वतंत्र भारत का सबसे महत्वपूर्ण विकास, उद्योगों के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग का प्रावधान इस नीति में स्थापित किया गया।
- (vii) सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार - सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार औद्योगिकीकरण और अर्थव्यवस्था में वृद्धि के लिए वचनबद्ध किया गया।
- औद्योगिक नीति प्रस्तावना, 1969
- (i) यह मूलतः एक लाइसेंसिंग नीति थी जिसका उद्देश्य 1956 की औद्योगिक नीति द्वारा शुरू की गई लाइसेंसिंग नीति की कमियों को हल करना था।
- (ii) विशेषज्ञों और औद्योगिकists (नए आगंतुकों) ने शिकायत की कि औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति उस उद्देश्य के विपरीत काम कर रही थी जिसके लिए इसे प्रस्तावित किया गया था।
- (iii) एक शक्तिशाली औद्योगिक घराना हमेशा नए उद्यमियों की लागत पर नए लाइसेंस प्राप्त करने में सक्षम था।
- (iv) औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति की समीक्षा पर समितियों ने न केवल नीति की कई कमियों को उजागर किया, बल्कि औद्योगिक लाइसेंसिंग की उपयोगी भूमिका को भी स्वीकार किया।
- औद्योगिक नीति प्रस्तावना, 1973
- (i) 1973 की औद्योगिक नीति घोषणा ने अर्थव्यवस्था में कुछ नई सोच को पेश किया।
- (ii) एक नई वर्गीकरण शब्द, यानी, कोर उद्योग बनाया गया।
- (iii) छह कोर उद्योगों में से, निजी क्षेत्र उन उद्योगों के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता था जो 1956 की औद्योगिक नीति के अनुसूची A का हिस्सा नहीं थे।
- (iv) कुछ उद्योगों को आरक्षित सूची में रखा गया जिसमें केवल छोटे या मध्यम उद्योग स्थापित किए जा सकते थे।
- (v) 'संयुक्त क्षेत्र' की अवधारणा विकसित की गई जिससे केंद्र, राज्य और निजी क्षेत्र के बीच साझेदारी की अनुमति मिली।
- (vi) भारत सरकार उस समय विदेशी मुद्रा संकट का सामना कर रही थी।
- औद्योगिक नीति प्रस्तावना, 1977
- (i) 1977 की औद्योगिक नीति का मसौदा एक अलग राजनीतिक सेट अप द्वारा तैयार किया गया था।
- (ii) हम इस नीति में ऐसे तत्व देखते हैं:
- (iii) अनावश्यक क्षेत्रों में विदेशी निवेश पर रोक लगाई गई।
- (iv) ग्रामीण उद्योगों पर जोर दिया गया और छोटे और कुटीर उद्योगों की पुनर्व्याख्या की गई।
- औद्योगिक नीति प्रस्तावना, 1980
- (i) 1980 में उसी राजनीतिक पार्टी की वापसी हुई।
- (ii) नई सरकार ने औद्योगिक नीति 1977 को कुछ अपवादों के साथ संशोधित किया।
- (iii) विदेशी निवेश को फिर से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से अनुमति दी गई।
- औद्योगिक नीति प्रस्तावना, 1985 और 1986
- (i) 1985 और 1986 में सरकारों द्वारा घोषित औद्योगिक नीति प्रस्तावना बहुत समान थी।
- (ii) विदेशी निवेश को और सरल बनाया गया और अधिक औद्योगिक क्षेत्रों को उनके प्रवेश के लिए खोला गया।
- (iii) 'MRTP सीमा' को ₹100 करोड़ तक संशोधित किया गया।
- (iv) औद्योगिक लाइसेंसिंग का प्रावधान सरल किया गया।
- (v) उच्च स्तर का ध्यान उभरते उद्योगों पर दिया गया।
नई औद्योगिक नीति, 1991
यह औद्योगिक नीतियाँ थीं जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति और संरचना को आकार दिया। इस समय की आवश्यकता थी कि 1990 के दशक की शुरुआत में अर्थव्यवस्था की प्रकृति और संरचना को बदल दिया जाए। भारत सरकार ने औद्योगिक नीति की प्रकृति को बदलने का निर्णय लिया, जो स्वतः ही अर्थव्यवस्था की प्रकृति और दायरे में परिवर्तन लाएगा। और इसी के साथ 1991 की नई औद्योगिक नीति आई। इस नीति के साथ सरकार ने अर्थव्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया को शुरू किया, इसलिए इस नीति को एक प्रक्रिया के रूप में अधिक माना जाता है। भारत के गंभीर भुगतान संतुलन संकट से निकटता ने 1991 में भारत की बाजार उदारीकरण उपायों की शुरुआत की, जिसके बाद एक क्रमिक दृष्टिकोण अपनाया गया। नीति के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:
- उद्योगों का डी-आरक्षण
- उद्योगों का डी-लाइसेंसिंग
- MRTP सीमा का उन्मूलन
- विदेशी निवेश को बढ़ावा
- FERA को FEMA द्वारा प्रतिस्थापित किया गया
- चरणबद्ध उत्पादन की बाध्यता समाप्त
- ऋण को शेयरों में परिवर्तित करने की बाध्यता समाप्त
निवेश निकासी
- सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियाँ, अर्थात् सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम (PSUs) और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियाँ (PSEs), भारत के विकास प्रक्रिया में एक मौलिक भूमिका निभाई।
- बदले हुए हालात को समझते हुए, सरकार ने 1991 में सुधार प्रक्रिया शुरू होने पर इन कंपनियों की भूमिका को 'पुनर्परिभाषित' करने का निर्णय लिया।
- उस समय तक, सरकार ने 244 कंपनियों में कुल ₹2.4 लाख करोड़ का निवेश किया था।
- नई सरकारी कंपनियों की स्थापना की प्रक्रिया नहीं रुकी और 2019 तक, सरकार ने 348 ऐसी कंपनियों में ₹16.41 लाख करोड़ का निवेश किया।
- निवेश निकासी एक कंपनी में 'स्वामित्व बेचना' की प्रक्रिया है। तकनीकी रूप से, यह शब्द किसी भी कंपनी (जैसे, निजी स्वामित्व वाली कंपनी) के मामले में उपयोग किया जा सकता है, लेकिन प्रायोगिक रूप से, इसका उपयोग केवल सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों के मामले में किया जाता है।
- नई सरकार (UPA) ने निवेश निकासी मंत्रालय को समाप्त कर दिया और आज केवल निवेश निकासी विभाग इस मामले का ध्यान रखता है, जो वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहा है।
निवेश निकासी के प्रकार
- टोकन निवेश निकासी: भारत में निवेश निकासी उच्च राजनीतिक सतर्कता के साथ प्रारंभ हुई— इसे प्रतीकात्मक तरीके से 'टोकन' निवेश निकासी के रूप में जाना जाता है (वर्तमान में इसे 'माइनॉरिटी स्टेक सेल' कहा जा रहा है)। सामान्य नीति थी कि PSUs के शेयरों को अधिकतम 49 प्रतिशत तक बेचा जाए।
- स्ट्रैटेजिक निवेश निकासी: निवेश निकासी को एक प्रक्रिया बनाने के लिए जिससे PSUs की दक्षता बढ़ाई जा सके और सरकार उन गतिविधियों से खुद को मुक्त कर सके जिसमें निजी क्षेत्र ने बेहतर दक्षता विकसित की है (ताकि सरकार उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर सके जिनमें निजी क्षेत्र के लिए कोई आकर्षण नहीं है, जैसे गरीब जनसंख्या के लिए सामाजिक क्षेत्र का समर्थन), सरकार ने रणनीतिक निवेश निकासी की प्रक्रिया शुरू की।
वर्तमान निवेश निकासी नीति
- भारत की निवेश नीति समय के साथ विकसित हुई है, जो 1991 में शुरू हुई थी। इसमें दो प्रमुख विशेषताएँ हैं— नीति के पीछे की विचारधारा और स्वयं नीति।
- नीति के पीछे की विचारधारा है:
- (i) सार्वजनिक स्वामित्व को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि यह राष्ट्र की संपत्ति है।
- (ii) 'माइनॉरिटी स्टेक सेल' के मामले में सरकार के पास कम से कम 51 प्रतिशत शेयर होने चाहिए।
- (iii) 'स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट' के तहत 50 प्रतिशत या उससे अधिक शेयर बेचे जा सकते हैं।
- सरकार द्वारा अपनाई गई वर्तमान निवेश नीति निम्नलिखित है:
- (i) माइनॉरिटी स्टेक सेल (नवंबर 2009 की नीति जारी है): सूचीबद्ध PSUs को पहले न्यूनतम 25% मानदंड का पालन करने के लिए लिया जाएगा।
- (ii) नए PSUs को सूचीबद्ध किया जाएगा जिन्होंने पिछले तीन लगातार वर्षों में शुद्ध लाभ कमाया है।
- (iii) जब पूंजी निवेश की आवश्यकता हो, तो मामले के आधार पर 'फॉलो-ऑन' सार्वजनिक प्रस्ताव।
- (iv) DIPAM (निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग) PSUs की पहचान करेगा और संबंधित मंत्रालयों के साथ परामर्श करके निवेश का सुझाव देगा।
- स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट यानी PSUs के 50 प्रतिशत या उससे अधिक शेयरों की बिक्री (फरवरी 2016 में घोषित):
- (i) मंत्रालयों/विभागों और NITI आयोग के बीच परामर्श के माध्यम से किया जाएगा।
- (ii) NITI आयोग PSUs की पहचान करेगा और इसके विभिन्न पहलुओं पर सलाह देगा।
- (iii) CGD (डिसइन्वेस्टमेंट पर सचिवों का कोर समूह) NITI आयोग की सिफारिशों पर विचार करेगा ताकि CCEA (कैबिनेट समिति आर्थिक मामलों) द्वारा निर्णय को सुविधाजनक बनाया जा सके और कार्यान्वयन प्रक्रिया की निगरानी करे।
MSME क्षेत्र
SMSE अधिनियम, 2006 के अनुसार, MSME को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है— निर्माण और सेवा उद्यम— और इन्हें संयंत्र और मशीनरी में निवेश के आधार पर परिभाषित किया गया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं— 3.6 करोड़ ऐसे इकाइयाँ 8.05 करोड़ लोगों को रोजगार देती हैं और देश के जीडीपी में 37.5 प्रतिशत का योगदान करती हैं। इस क्षेत्र में संरचनात्मक समस्याओं जैसे कि बेरोजगारी, क्षेत्रीय असंतुलन, और राष्ट्रीय आय और धन का असमान वितरण हल करने की विशाल क्षमता है। तुलनात्मक रूप से कम पूंजी लागत और अन्य क्षेत्रों के साथ उनके अग्रिम-पीछे के लिंक के कारण, वे मेक इन इंडिया पहल की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं।
- (i) UAM (उद्योग आधार मेमोरेंडम): UAM योजना, सितंबर 2015 में अधिसूचित की गई, व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए। इसके तहत, उद्यमियों को एक अद्वितीय उद्योग आधार संख्या (UAN) प्राप्त करने के लिए केवल एक ऑनलाइन उद्यमियों का मेमोरेंडम जमा करना होता है— यह पिछले जटिल और थकाऊ प्रक्रिया की तुलना में एक महत्वपूर्ण सुधार है।
- (ii) उद्योगों के लिए रोजगार एक्सचेंज: संभावित नौकरी की तलाश करने वालों और नियोक्ताओं के बीच मिलान को सुविधाजनक बनाने के लिए, जून 2015 में उद्योगों के लिए एक रोजगार एक्सचेंज स्थापित किया गया (डिजिटल इंडिया की दिशा में)।
- (iii) MSMEs के पुनरुद्धार और पुनर्वास के लिए ढाँचा: इसके तहत (मई 2015) बैंकों को distressed MSMEs के लिए एक सम्प corrective action plan (CAP) तैयार करने के लिए एक समिति का गठन करना आवश्यक है।
- (iv) ASPIRE (नवाचार और ग्रामीण उद्यमियों को बढ़ावा देना): मार्च 2015 में लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी और इंक्यूबेशन केन्द्रों का एक नेटवर्क स्थापित करना है ताकि उद्यमिता को तेज किया जा सके और ग्रामीण और कृषि आधारित उद्योग में नवाचार और उद्यमिता के लिए स्टार्ट-अप को बढ़ावा दिया जा सके।
औद्योगिक क्षेत्र
(i) स्टील उद्योग
- वैश्विक और घरेलू कारणों के चलते भारतीय स्टील उद्योग हाल के समय में कुछ समस्याओं का सामना कर रहा है।
- भारत, चीन के बाद, विश्व में स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, हालांकि वैश्विक स्टील उत्पादन में उनके योगदान के बीच बड़ा अंतर है (भारत का हिस्सेदारी 6 प्रतिशत जबकि चीन का 53.8 प्रतिशत)।
- इसने प्रमुख वैश्विक स्टील उत्पादकों को भारतीय बाजार में स्टील उत्पादों को 'धकेलने' के लिए प्रेरित किया है, जिससे दो मुख्य चिंताएँ उठी हैं:
- (i) स्टील आयात में वृद्धि,
- (ii) घरेलू स्टील उद्योग का हित प्रभावित हुआ।
(ii) एल्युमिनियम उद्योग
- हालांकि भारत वैश्विक एल्युमिनियम उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी रहा है, पिछले कुछ वर्षों में इसे वैश्विक कारणों के कारण कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।
- भारत एल्युमिनियम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक (चीन के बाद) और तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता (चीन के बाद) है।
- आज, भारत लगभग 4.5 एमटी का उत्पादन करता है (चीन-22 एमटी) और 3.8 एमटी का उपभोग करता है (चीन-23 एमटी, अमेरिका-5.5 एमटी)।
- वैश्विक एल्युमिनियम की कीमतें अन्य धातुओं की कीमतों की तरह चक्रीय होती हैं और यह भविष्यवाणी करना मुश्किल है कि ये कब बढ़ना शुरू होंगी। लेकिन, यह प्रवृत्ति तब बदलने की उम्मीद है जब वैश्विक औद्योगिक विकास में सुधार होगा।
- भारत एल्युमिनियम के आयात को कम करने के लिए कस्टम ड्यूटी से बच रहा है क्योंकि इससे बिजली, परिवहन और निर्माण जैसे डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित हो सकती है।
(iii) वस्त्र और फुटवियर क्षेत्र
- औद्योगिक क्रांति के बाद, कोई भी देश औद्योगिक शक्ति बने बिना एक प्रमुख अर्थव्यवस्था नहीं बना है।
- भारत के संदर्भ में, औद्योगिक विस्तार न केवल रुक गया है बल्कि यह काफी पूंजी-गहन भी रहा है।
- जनसंख्या लाभ के कगार पर बैठा भारत को औपचारिक, उत्पादक और निवेश के अनुकूल नौकरियों का सृजन करने की आवश्यकता है।
- इसके अलावा, अर्थव्यवस्था को विकास, निर्यात और व्यापक सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए वैकल्पिक उपाय खोजने की आवश्यकता है। इस मामले में दो क्षेत्र हैं— वस्त्र और चमड़ा एवं फुटवियर।
PLI योजना
- सरकार ने मार्च 2020 में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और आयात बिलों को कम करने के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना पेश की।
- इस योजना के तहत, कंपनियों को 5 साल की अवधि में उनकी बढ़ी हुई बिक्री पर प्रोत्साहन मिलेगा।
- अप्रैल 2023 तक, 14 क्षेत्रों को इस योजना में शामिल किया गया है जिसमें सरकार द्वारा कुल निधियों का आवंटन किया गया है।
- कवर किए गए क्षेत्रों में मोबाइल विनिर्माण, विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटक, महत्वपूर्ण की प्रारंभिक सामग्री, दवा मध्यवर्ती, सक्रिय फार्मास्यूटिकल सामग्री, चिकित्सा उपकरण, उन्नत रसायन सेल बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी उत्पाद, ऑटोमोबाइल, ऑटो घटक, फार्मास्यूटिकल दवाएं, टेलीकॉम और नेटवर्किंग उत्पाद, वस्त्र उत्पाद, खाद्य उत्पाद, उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल, व्हाइट गुड्स (एसी और एलईडी), विशेष स्टील, ड्रोन और ड्रोन घटक शामिल हैं।
- प्रोत्साहन: कंपनियों को उनके उत्पादन टर्नओवर और निवेश खर्चों के प्रतिशत के रूप में प्रोत्साहन मिलेगा, जिसमें भूमि और भवन के निवेश शामिल नहीं हैं।
- यह योजना भारतीय निर्माताओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने, निवेश आकर्षित करने, दक्षताओं को सुनिश्चित करने, पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण करने और भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला में एकीकृत करने का लक्ष्य रखती है।
- प्रभाव: PLI योजना के तहत आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, भारत की वार्षिक विनिर्माण पूंजी व्यय में 15 से 20 प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद है। यह देश में MSME पारिस्थितिकी तंत्र को लाभान्वित करेगा और विभिन्न क्षेत्रों में नए सप्लायर बेस के विकास की ओर ले जाएगा।
FDI नीति उपाय
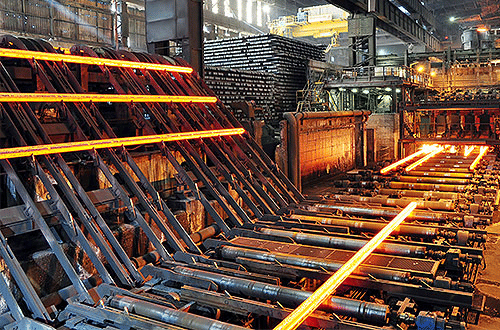

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण चालक है, जो निम्नलिखित में मदद करता है:
- उच्च विकास दर को बनाए रखना
- उत्पादकता बढ़ाना
- गैर-ऋण वित्तीय संसाधनों का एक प्रमुख स्रोत
- रोजगार सृजन
एक अनुकूल नीति प्रणाली और मजबूत व्यापार वातावरण FDI प्रवाह को सुगम बनाते हैं। सरकार ने देश में व्यवसाय करने के लिए अनुकूल माहौल प्रदान करने के लिए FDI नीति को उदार और सरल बनाने के लिए विभिन्न सुधार किए हैं, जिससे बड़े FDI प्रवाह को भी बढ़ावा मिलेगा।
कई क्षेत्रों को उदारीकृत किया गया है, जिनमें शामिल हैं:
- रक्षा
- निर्माण
- ब्रॉडकास्टिंग
- नागरिक उड्डयन
- प्लांटेशन
- व्यापार
- निजी क्षेत्र का बैंकिंग
- सैटेलाइट स्थापना और संचालन
- क्रेडिट सूचना कंपनियाँ
|
125 videos|399 docs|221 tests
|




















