एनसीईआरटी सारांश: कार्यकारी - 1 | UPSC CSE के लिए भारतीय राजनीति (Indian Polity) PDF Download
कार्यकारी - कार्यकारी क्या है?
- सरकार का वह अंग जो मुख्यतः कार्यान्वयन और प्रशासन के कार्यों की देखरेख करता है, उसे कार्यकारी कहा जाता है।
कार्यकारी के मुख्य कार्य क्या हैं?
- कार्यकारी वह सरकारी शाखा है जो कानूनों और नीतियों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी निभाती है, जिन्हें विधायिका द्वारा अपनाया गया है।
- कार्यकारी अक्सर नीति निर्माण में संलग्न होता है। कुछ देशों में राष्ट्रपति होते हैं, जबकि अन्य में चांसलर।
- कार्यकारी शाखा केवल राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और मंत्रियों के बारे में नहीं है। यह प्रशासनिक मशीनरी (सिविल सेवकों) तक भी फैली हुई है।
कार्यकारी के विभिन्न प्रकार
राजनीतिक प्रणालियों के विभिन्न प्रकार हैं जिनमें विभिन्न कार्यकारी विभिन्न राजनीतिक क्षेत्रों का नेतृत्व करते हैं:
- राष्ट्रपति प्रणाली: राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख और सरकार का प्रमुख होता है। इस प्रणाली में, राष्ट्रपति का कार्यालय सिद्धांत और व्यवहार दोनों में बहुत शक्तिशाली होता है।
- देश: संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और लैटिन अमेरिका के अधिकांश देश।
- अर्ध-राष्ट्रपति कार्यकारी: कार्यकारी राष्ट्रपति की प्रणाली के तहत, लोग सीधे राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। यह हो सकता है कि राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री दोनों एक ही राजनीतिक पार्टी से हों या विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से।
- देश: फ्रांस, रूस, श्रीलंका।
- संवैधानिक प्रणाली: प्रधान मंत्री सरकार का प्रमुख होता है। अधिकांश संसदीय प्रणालियों में एक राष्ट्रपति या एक सम्राट होता है जो राज्य का नाममात्र प्रमुख होता है। राष्ट्रपति या सम्राट की भूमिका मुख्यतः औपचारिक होती है, और प्रधान मंत्री तथा मंत्रिमंडल प्रभावी शक्ति धारण करते हैं।
- देश: जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और पुर्तगाल।
भारत में संसदीय कार्यकारी
भारत ने पहले से ही 1919 और 1935 के अधिनियमों के तहत संसदीय प्रणाली चलाने का कुछ अनुभव प्राप्त किया था। इस अनुभव ने दिखाया कि संसदीय प्रणाली में, कार्यकारी को लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है।
भारत ने संसदीय शासन प्रणाली का विकल्प क्यों चुना?
- भारतीय संविधान चाहता था कि सरकार जनता की अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील हो और जिम्मेदार एवं उत्तरदायी हो।
- राष्ट्रपति कार्यकारी प्रणाली में राष्ट्रपति को मुख्य कार्यकारी और सभी कार्यकारी शक्तियों के स्रोत के रूप में रखा जाता है।
- राष्ट्रपति कार्यकारी में व्यक्तित्व पूजा का हमेशा खतरा रहता है।
- कार्यकारी को विधायिका या जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी और नियंत्रित होना चाहिए।
संसदीय प्रणाली क्या है?
- राष्ट्रपति जो भारत का औपचारिक राज्य प्रमुख है और प्रधानमंत्री तथा मंत्रियों का परिषद, जो राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाते हैं।
- राज्य स्तर पर कार्यकारी में राज्यपाल और मुख्यमंत्री तथा मंत्रियों का परिषद शामिल होता है।
राष्ट्रपति
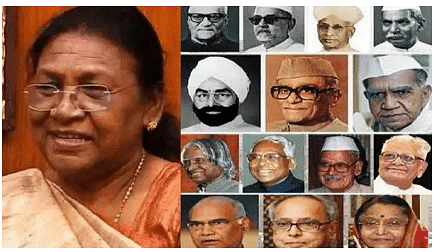
- उच्चतम कार्यकारी अधिकारिता।
- संविधान में उन्हें संघ की सभी कार्यकारी शक्तियाँ दी गई हैं।
- राज्य का प्रमुख और भारत गणराज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- भारत के पहले नागरिक।
- अनुच्छेद 58: भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति की योग्यता से संबंधित है।
- भारत का नागरिक होना चाहिए।
- 35 वर्ष की आयु पूरी की हो।
- लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य होना चाहिए।
- सरकार के तहत किसी लाभकारी पद पर नहीं होना चाहिए।
राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या है?
भारत का राष्ट्रपति सीधे जनता द्वारा नहीं चुना जाता, बल्कि इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों द्वारा चुना जाता है:
- संसद के दोनों सदनों के सदस्य।
- राज्य की विधान सभा के सदस्य।
- दिल्ली और पुडुचेरी की विधान सभा के निर्वाचित सदस्य।
राष्ट्रपति के अधिकार और कार्य क्या हैं?
भारत के राष्ट्रपति की हमारे लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग सामान्य समय में और आपातकाल की अवधि में किया जा सकता है।
राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ
राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित सदस्यों की नियुक्ति की जाती है:
- प्रधान मंत्री और अन्य मंत्रिपरिषद के सदस्य।
- सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश।
- यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य।
- महालेखाकार, अटॉर्नी जनरल।
- मुख्य चुनाव आयुक्त आदि।
विधायी शक्तियाँ
- राष्ट्रपति लोक सभा की बैठक को बुला सकते हैं और भंग कर सकते हैं।
- दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकते हैं।
- राष्ट्रपति संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश भी पारित कर सकते हैं।
न्यायिक शक्तियाँ
- अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों का उल्लेख है।
- राष्ट्रपति केंद्रीय कानूनों के तहत किसी भी दोषी व्यक्ति की सजा माफ कर सकते हैं या उसे कम कर सकते हैं।
राष्ट्रपति की माफी देने की शक्तियाँ
भारत के राष्ट्रपति उस मामले में कार्रवाई करते हैं जिसमें किसी अपराध के लिए दोषी व्यक्ति की सजा या दंड होता है, यह उनकी माफी देने की शक्तियों के रूप में होती है।
ये पाँच प्रकार की होती हैं:
- माफी (Pardon)
- विश्राम (Reprieve)
- छोड़ना (Remit)
- रुकावट (Respite)
- सजा बदलना (Commute)
राष्ट्रपति सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति भी होते हैं।
राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ
भारत में राष्ट्रपति तीन स्थितियों में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं:
- राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352): युद्ध, बाहरी आक्रमण या देश के भीतर सशस्त्र विद्रोह के कारण।
- संविधानिक आपातकाल (अनुच्छेद 356): राज्यों में संविधानिक मशीनरी के विफल होने की स्थिति में। (राष्ट्रपति शासन)
- वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360): भारत की वित्तीय स्थिरता या क्रेडिट को खतरा होने की स्थिति में।
अनुच्छेद 74 (1): राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रियों की परिषद होगी, जो राष्ट्रपति के कार्यों का संचालन करेगी। राष्ट्रपति मंत्रियों की परिषद से ऐसी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकते हैं, और राष्ट्रपति पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेंगे।
राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियाँ क्या हैं?
राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी महत्वपूर्ण मामलों और विचार-विमर्शों से अवगत होने का अधिकार है। प्रधानमंत्री को उन सभी सूचनाओं को प्रदान करने के लिए बाध्य किया जाता है जिनकी राष्ट्रपति मांग कर सकते हैं। राष्ट्रपति अक्सर प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हैं और देश के सामने मौजूद मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करते हैं।
राष्ट्रपति के पास अपने विवेक से उपयोग करने के लिए शक्तियाँ:
- पुनर्विचार
- वेटो शक्ति
- प्रधानमंत्री की नियुक्ति जब स्पष्ट बहुमत न हो।
राष्ट्रपति के पास मंत्रिपरिषद से उनके निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करने का अधिकार है। उनके पास वेटो शक्ति है, जिसके द्वारा वे संसद द्वारा पारित विधेयकों (पैसे के विधेयकों को छोड़कर) को सहमति देने से रोक सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं। कानून बनने से पहले, संसद द्वारा पारित हर विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति के पास विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद में वापस भेजने का अधिकार है। यह 'वेटो शक्ति' सीमित है क्योंकि यदि संसद उसी विधेयक को फिर से पारित करती है और राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो राष्ट्रपति को उस पर सहमति देनी होती है। हालांकि, राष्ट्रपति को विधेयक को पुनर्विचार के लिए कांग्रेस में वापस भेजने के लिए एक निश्चित समय सीमा के भीतर कार्य करना आवश्यक है, जो संविधान में निर्दिष्ट नहीं है। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति विधेयक को अनिश्चितकाल के लिए अपने कार्यालय में लम्बित रख सकते हैं। यह राष्ट्रपति को प्रभावी रूप से वेटो का उपयोग करने के लिए एक अनौपचारिक शक्ति देता है। इसे कुछ लोग "पॉकेट वेटो" के रूप में संदर्भित करते हैं। जब चुनाव के बाद लोकसभा में कोई उम्मीदवार स्पष्ट बहुमत नहीं जीतता है, तो राष्ट्रपति को एक प्रधानमंत्री चुनना होता है। ऐसे में राष्ट्रपति को यह तय करने के लिए अपनी स्वयं की समझ पर निर्भर रहना पड़ता है कि किसके पास बहुमत का समर्थन है या कौन वास्तव में सरकार बना और चला सकता है।
उपाध्यक्ष
- उपाध्यक्ष का चुनाव पांच साल की अवधि के लिए किया जाता है। यह प्रक्रिया राष्ट्रपति के चुनाव के समान है, केवल यह कि राज्य विधानसभाओं के सदस्य इलेक्ट्रोरल कॉलेज में शामिल नहीं होते।
- उन्हें पद से हटाने के लिए राज्य सभा द्वारा बहुमत से पारित एक संकल्प और लोक सभा द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है।
- उपाध्यक्ष राज्य सभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं और मृत्यु, इस्तीफे, महाभियोग या अन्य कारणों से उत्पन्न होने वाली रिक्तता की स्थिति में राष्ट्रपति की भूमिका ग्रहण करते हैं।
- उन्हें एक सीमित समय के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अधिकार होता है जब तक नया राष्ट्रपति चुना नहीं जाता।
प्रधान मंत्री और मंत्रियों की परिषद
- हमारे देश में, प्रधान मंत्री सबसे महत्वपूर्ण सरकारी कार्यकारी बन गए हैं। प्रधान मंत्री को मंत्रियों की परिषद का "मुखिया" भी कहा जाता है।
- राष्ट्रपति केवल मंत्रियों की परिषद की सलाह पर अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं।
- प्रधान मंत्री को संसदीय शासन प्रणाली में लोक सभा के सदस्यों की बहुमत का समर्थन प्राप्त होना चाहिए।
- प्रधान मंत्री बहुमत के समर्थन के कारण अत्यधिक शक्ति रखते हैं।
- मंत्रियों की परिषद में किसे मंत्री के रूप में सेवा करनी है, यह तय करने के अलावा, यह मंत्रियों को रैंक और पोर्टफोलियो भी निर्धारित करती है।
- मंत्रियों को उनकी वरिष्ठता और राजनीतिक महत्व के आधार पर कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, या उप मंत्रियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- इसी तरह, राज्य के मुख्यमंत्री अपने राजनीतिक दल या गठबंधन से मंत्रियों का चयन करते हैं।
- सभी मंत्री, जिसमें प्रधान मंत्री भी शामिल हैं, को संसद का सदस्य होना चाहिए। यदि कोई मंत्री या प्रधान मंत्री बिना संसद में पहले चुने गए बने, तो उन्हें छह महीने के भीतर ऐसा करना होगा।
मंत्रियों की परिषद का आकार
- एक संशोधन किया गया कि मंत्रियों की परिषद सदस्यों की कुल संख्या का 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी (या राज्यों के मामले में विधानसभा)। यह लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार है। इस प्रावधान का अर्थ है कि यदि मंत्रिमंडल को लोक सभा में विश्वास खो देता है, तो उसे इस्तीफा देने के लिए बाध्य होना पड़ता है। यह सिद्धांत बताता है कि मंत्रिमंडल संसद का एक कार्यकारी समिति है और यह संसद की ओर से सामूहिक रूप से शासन करता है।
सामूहिक जिम्मेदारी
- मंत्रिमंडल की एकता के सिद्धांत पर आधारित है।
- इसका अर्थ है कि एक ही मंत्री के खिलाफ अविश्वास का मत भी पूरी मंत्रियों की परिषद के इस्तीफे का कारण बनता है।
- यह भी दर्शाता है कि यदि कोई मंत्री मंत्रिमंडल की नीति या निर्णय से असहमत होता है, तो उसे या तो निर्णय को स्वीकार करना होगा या इस्तीफा देना होगा।
- सभी मंत्रियों पर यह अनिवार्य है कि वे ऐसी नीति का पालन करें या उस पर सहमत हों जिसके लिए सामूहिक जिम्मेदारी है।
जब प्रधानमंत्री की मृत्यु होती है या वह इस्तीफा देते हैं, तो मंत्रियों की परिषद स्वतः समाप्त हो जाती है, लेकिन किसी मंत्री की मृत्यु, बर्खास्तगी, या इस्तीफे से केवल एक मंत्री की रिक्ति उत्पन्न होती है। प्रधानमंत्री, एक ओर, मंत्रियों की परिषद और राष्ट्रपति के बीच एक लिंक के रूप में कार्य करता है, साथ ही संसद के साथ भी।
सभी प्रमुख सरकारी निर्णय प्रधानमंत्री द्वारा लिए जाते हैं, जो सरकार की नीतियों को भी निर्धारित करते हैं।
मंत्रियों की परिषद का नियंत्रण, लोक सभा की नेतृत्व, नौकरशाही मशीन काcommand, मीडिया तक पहुंच, चुनाव के दौरान व्यक्तित्व का प्रक्षेपण, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के दौरान राष्ट्रीय नेता के रूप में प्रक्षेपण, और विदेशी यात्राएं सभी प्रधानमंत्री के लिए शक्ति के स्रोत हैं।
राज्य स्तर पर:
- यहाँ भी एक समान संसदीय कार्यपालिका है, हालांकि इसमें कुछ भिन्नताएँ हैं। सबसे महत्वपूर्ण भिन्नता यह है कि राष्ट्रपति राज्य का गवर्नर (केंद्रीय सरकार की सलाह पर) नियुक्त करते हैं।
- गवर्नर के पास मुख्यमंत्री की तुलना में अधिक विवेकाधीन शक्तियाँ होती हैं, जो, प्रधानमंत्री की तरह, विधानसभा में बहुमत पार्टी के नेता होते हैं।
- हालाँकि, संसदीय प्रणाली के मुख्य सिद्धांत राज्य स्तर पर भी लागू होते हैं।
स्थायी कार्यपालिका क्या है?
- प्रधान मंत्री, मंत्री, और एक बड़ी संगठन जिसे ब्यूरोक्रेसी या प्रशासनिक मशीनरी के रूप में जाना जाता है, सरकार के कार्यकारी अंग का निर्माण करते हैं।
- एक लोकतंत्र में, सरकार का नेतृत्व निर्वाचित प्रतिनिधियों और मंत्रियों द्वारा किया जाता है, और प्रशासन उनके नियंत्रण और पर्यवेक्षण में होता है।
- विधानसभा को कार्यकारी शाखा पर भी अधिकार है। प्रशासनिक अधिकारी विधान के नीतियों के खिलाफ कार्य करने की अनुमति नहीं रखते।
- मंत्री प्रशासन पर राजनीतिक नियंत्रण बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। भारत में एक पेशेवर प्रशासनिक ढाँचा विकसित किया गया है।
- भारतीय ब्यूरोक्रेसी में अखिल भारतीय सेवाएँ, राज्य सेवाएँ, स्थानीय सरकार के कर्मचारी, और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को चलाने वाले तकनीकी और प्रबंधकीय कर्मचारी शामिल हैं।
- संघ लोक सेवा आयोग को भारतीय सरकार के सिविल सेवकों की भर्ती प्रक्रिया आयोजित करने का कार्य सौंपा गया है। राज्य स्तर पर सार्वजनिक सेवा आयोग भी उपलब्ध हैं।
- लोक सेवा आयोग के सदस्य एक निर्धारित समय के लिए सेवा देते हैं। उनकी बर्खास्तगी या निलंबन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा एक गहन जांच के अधीन होता है।
- ब्यूरोक्रेसी एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से सरकार की कल्याणकारी नीतियाँ लोगों तक पहुँचनी चाहिए।
- ब्यूरोक्रेसी आम नागरिक की माँगों और अपेक्षाओं की अनदेखी करती है।
आम नागरिकों की अपेक्षाओं को कैसे संवेदनशील बनाया जा सकता है?
इन समस्याओं में से कुछ केवल तभी हल की जा सकती हैं जब लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार ब्यूरोक्रेसी पर नियंत्रण बनाए रखे। दूसरी ओर, राजनीतिक हस्तक्षेप के अत्यधिक होने पर ब्यूरोक्रेसी नेताओं के हाथों में एक उपकरण बन जाती है।
हालांकि संविधान ने एक स्वतंत्र भर्ती प्रणाली की स्थापना की है, लेकिन कई लोगों का मानना है कि कार्य में राजनीतिक हस्तक्षेप से नागरिक सेवकों की सुरक्षा के लिए कोई उपाय नहीं हैं।
यह भी माना जाता है कि यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं हैं कि ब्यूरोक्रेसी जनता के प्रति जवाबदेह हो। उदाहरण के लिए, सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य ब्यूरोक्रेसी को अधिक उत्तरदायी और जवाबदेह बनाना है।
|
128 videos|631 docs|260 tests
|
















