UPSC Exam > UPSC Notes > इतिहास वैकल्पिक UPSC (नोट्स) > जैन धर्म का प्रसार
जैन धर्म का प्रसार | इतिहास वैकल्पिक UPSC (नोट्स) PDF Download
विभिन्न हेटेरोडॉक्स संप्रदायों का उदय
छठी शताब्दी ई.पू. भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवधि थी, जिसमें नए धर्मों का उदय हुआ। इस समय, ब्राह्मणों के अनुष्ठानिक और पारंपरिक विचारों के प्रति बढ़ती विरोध की भावना ने मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्रों में विभिन्न हेटेरोडॉक्स धार्मिक आंदोलनों के उदय को जन्म दिया। कुल मिलाकर 62 धार्मिक संप्रदायों को पहचाना गया, जिनमें से बौद्ध धर्म और जैन धर्म सबसे लोकप्रिय और संगठित धर्म बने। इस अवधि के नए धार्मिक विचार प्रचलित सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक परिस्थितियों का जवाब थे।
सामाजिक और आर्थिक जीवन में परिवर्तन, जैसे कस्बों का विकास, कारीगर वर्ग का विस्तार और व्यापार और वाणिज्य का तेजी से विकास, धर्म और दार्शनिक विचारों में बदलाव से निकटता से जुड़े थे। इस अवधि में परिव्राजक या श्रमणों की उपस्थिति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्होंने गृहस्थ जीवन का त्याग किया और अपने विचारों को फैलाने के लिए स्थान-स्थान पर घूमे। ये श्रमण बलिदान के culto और सामाजिक प्रमुखता के ब्राह्मणिक दावों के खिलाफ एकजुट थे। उनके विचारों में उच्छेदवाद (Ucchedavada) से लेकर शाश्वतवाद (Sashvatvarda) तक, अजिविकाओं की भाग्यवादिता से लेकर चारवाकों की भौतिकवाद तक फैले हुए थे।
हेटेरोडॉक्स संप्रदायों के उदय और विकास के कारण
सामाजिक स्थिति: वेदों के बाद के समय में, समाज चार वर्णों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रत्येक वर्ण के पास स्पष्ट कार्य थे, जिसमें ब्राह्मणों ने उच्चतम स्थिति का दावा किया और करों और दंड से छूट की मांग की। क्षत्रिय दूसरे स्थान पर थे, जो शासन और युद्ध के लिए जिम्मेदार थे, जबकि वैश्य कृषि, पशुपालन और व्यापार में लगे थे। शूद्रों को अन्य तीन वर्णों की सेवा करने के लिए बनाया गया था और उन्हें वेद अध्ययन से प्रतिबंधित किया गया था। वर्ण विभाजित समाज ने तनाव उत्पन्न किया, विशेष रूप से क्षत्रिय जिन्होंने ब्राह्मणों के अनुष्ठानिक प्रभुत्व के खिलाफ विरोध किया। वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध, दोनों क्षत्रिय जातियों से थे, ने ब्राह्मणों के अधिकार को चुनौती दी।
आर्थिक स्थिति: नए धर्मों का उदय उत्तर-पूर्वी भारत में नए कृषि अर्थव्यवस्था द्वारा प्रेरित था। मध्य गंगा के मैदानी इलाकों में लोहे के औजारों के प्रयोग ने जंगलों की सफाई, कृषि और बड़े बस्तियों के विकास को सक्षम बनाया। कृषि अर्थव्यवस्था पशुपालन पर निर्भर थी, लेकिन वेदिक प्रथाओं के तहत पशु बलिदान ने प्रगति में बाधा डाली। नए किसान समुदायों ने बलिदानों के लिए पशुओं के वध का विरोध किया, जिससे हेटेरोडॉक्स संप्रदायों द्वारा अहिंसा को अपनाया गया। इस अवधि में उत्तर-पूर्वी भारत में शहरों का उदय हुआ, जहां कारीगरों और व्यापारियों ने पहली बार सिक्कों का उपयोग किया, जिसने व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया। वैश्य, जो अपने सामाजिक स्थिति में सुधार करना चाहते थे, ने महावीर और बुद्ध का समर्थन किया, क्योंकि जैनism और बौद्ध धर्म ने प्रारंभिक रूप से वर्ण व्यवस्था की अनदेखी की। ये संप्रदाय अहिंसा का उपदेश देते थे, जो शांति और व्यापार को बढ़ावा देते थे, और वैश्य समुदाय को आकर्षित करते थे। जैनism और बौद्ध धर्म भौतिक संपत्ति को अस्वीकार करते थे, संयमित जीवन का समर्थन करते थे, जो सामाजिक असमानताओं और नए भौतिक जीवन से असंतुष्ट लोगों के साथ प्रतिध्वनित होता था।
धार्मिक स्थिति: वेदिक धार्मिक प्रथाएँ नए सामाजिक संदर्भ में जटिल और अक्सर अर्थहीन हो गईं। बलिदान और अनुष्ठान अधिक विस्तृत और महंगे हो गए, जिससे ब्राह्मणों का प्रभुत्व बढ़ा, जिन्होंने धार्मिक अनुष्ठानों का एकाधिकार किया। इन प्रथाओं के बढ़ते महत्व ने ब्राह्मणों की उच्च स्थिति को स्थापित किया, जिससे समाज अब वर्णों में विभाजित हो गया। वेदिक अनुष्ठान कई लोगों के लिए प्रासंगिकता खो चुके थे, जो वैकल्पिक धार्मिक आदेशों के लिए मार्ग प्रशस्त करता था।
राजनीतिक स्थिति: क्षत्रिय राजतंत्रों और गण-संघों में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने लगे, ब्राह्मणिक प्रभुत्व का विरोध करते हुए। उभरते साम्राज्यों के बीच लगातार युद्धों और असंतोषित व्यापारियों ने लोगों को शांतिपूर्ण, अहिंसक धर्मों की खोज करने के लिए प्रेरित किया। बुद्ध और महावीर पहले नहीं थे जिन्होंने वेदिक विश्वासों की आलोचना की; पहले के उपदेशक जैसे कपिल और मक्कली गोसाल ने भी वेदिक प्रथाओं की निंदा की थी। नए दार्शनिकताएँ प्रचारित की जा रही थीं, लेकिन यह बुद्ध और महावीर थे जिन्होंने एक व्यवहार्य वैकल्पिक धार्मिक क्रम की पेशकश की।
जैन धर्म
उद्गम और विश्वास: जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है जो भारत से है, जो हानिरहितता और त्याग को मुक्ति और सुख के मार्ग के रूप में महत्व देता है। यह ब्रह्मांड के हर प्राणी के कल्याण और स्वयं ब्रह्मांड के स्वास्थ्य पर केंद्रित है। जैनों का विश्वास है कि 24 तीर्थंकर हैं, जो उनके धर्म के नेता हैं। पहले तीर्थंकर ऋषभadev हैं, जो अयोध्या में पैदा हुए थे। इक्कीसवें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं, जिन्होंने राजसी जीवन का त्याग कर एक श्रमण बनने का निर्णय लिया। महावीर को चौबीसवें और अंतिम तीर्थंकर माना जाता है। कुछ तीर्थंकरों के नाम, जैसे ऋषभ और अरिष्टनेमि, प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित हैं जैसे कि ऋग्वेद। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में ऋषभ को नारायण का अवतार बताया गया है। तीर्थंकरों की मिथक, जिनमें से अधिकांश मध्य गंगा क्षेत्र में पैदा हुए और बिहार में निर्वाण प्राप्त किया, शायद जैन धर्म को प्राचीनता का एहसास दिलाने के लिए बनाई गई।
वर्धमान महावीर: वर्धमान महावीर, जिन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है, चौबीसवें और अंतिम तीर्थंकर थे। उनका जन्म 540 ई.पू. में कुंडग्राम में, जो वर्तमान बिहार के वैशाली के निकट है, हुआ। उनके पिता सिद्धार्थ, ज्ञात्रिका जाति के प्रमुख थे, और उनकी माता त्रिशला मगध के शाही परिवार से संबंधित थीं। महावीर का विवाह यशोदा से हुआ और उनके एक बेटी थी जिसका नाम अन्नोजा था।
महावीर ने प्रारंभ में एक गृहस्थ के रूप में जीवन व्यतीत किया, लेकिन 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने परिवार का त्याग किया और सत्य की खोज में एक श्रमण बन गए। बारह वर्षों तक भिक्षाटन और तपस्या करने के बाद, उन्होंने 42 वर्ष की आयु में मुजफ्फरपुर जिले, बिहार में रिजुपालिका नदी के पास एक साल के पेड़ के नीचे सर्वज्ञता (कैवल्य) प्राप्त की। ज्ञान की प्राप्ति के बाद, महावीर को केवली (सर्वज्ञ), जिन (विजेता), और महावीर (महान नायक) के रूप में जाना जाने लगा। उन्होंने निग्रंथ (बंधनमुक्त) नामक एक संप्रदाय का नेतृत्व किया, जो बाद में जैन धर्म के रूप में जाना जाने लगा। अगले 30 वर्षों तक, महावीर ने कोसल, मगध, मिथिला, और चंपा जैसे क्षेत्रों में अपने सिद्धांतों का प्रचार किया। वह हर साल आठ महीने घूमते थे और चार महीनों की बारिश के मौसम में पूर्वी भारत के एक प्रमुख शहर में बिताते थे। उन्होंने अक्सर राजा बिंबिसार और अजातशत्रु के दरबारों का दौरा किया। महावीर की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में पाव (राजगृह के निकट) में आत्म-आहार (Sallekana) द्वारा 468 ई.पू. में हुई।
महावीर के शिक्षाएँ: महावीर ने वेदों, वेदिक अनुष्ठानों और ब्राह्मणों की सर्वोच्चता के अधिकार को खारिज कर दिया। जैनism का ध्यान सही ज्ञान, सही विश्वास, और सही आचरण के माध्यम से सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने पर है, बिना अनुष्ठानों की आवश्यकता के। उन्होंने कैवल्य (निर्वाण या मोक्ष) प्राप्त करने के लिए एक संयमित और सरल जीवन जीने का समर्थन किया। महावीर ने अपने पूर्वज पार्श्व की तुलना में एक अधिक कठोर जीवन का जोर दिया, जिससे जैनism बाद में दो संप्रदायों में विभाजित हो गया: श्वेताम्बर (जो सफेद वस्त्र पहनते हैं) और दिगम्बर (जो नग्न होते हैं)।
बौद्ध धर्म के विपरीत, महावीर ने वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की। उन्होंने विश्वास किया कि किसी व्यक्ति का वर्ण उनके पिछले जन्मों में उनके कार्यों द्वारा निर्धारित होता है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि निम्न जातियों के व्यक्ति भी सदाचारी जीवन द्वारा मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। महावीर ने देवताओं की उपस्थिति को स्वीकार किया, लेकिन उन्हें जिन से नीचे रखा। उन्होंने सिखाया कि ब्रह्मांड का निर्माण, रखरखाव या विनाश किसी व्यक्तिगत देवता द्वारा नहीं, बल्कि सार्वभौमिक कानूनों द्वारा होता है। उन्होंने विश्वास किया कि सभी वस्तुओं, संवेदनशील या असंवेदनशील, में विभिन्न डिग्री की चेतना होती है और जब नुकसान पहुंचता है तो वे दर्द महसूस कर सकते हैं। उन्होंने कर्म और आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांतों पर जोर दिया। कर्म का प्रवाह (Asrav) आत्मा को बाधित करता है, जिससे उसकी शुद्धता का आवरण बनता है, जो जन्म और मृत्यु के चक्र की ओर ले जाता है। जैनism सिखाता है कि मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य आत्मा की शुद्धि और निर्वाण (मोक्ष) की प्राप्ति है, जो जन्म और मृत्यु से मुक्ति का संकेत है।
यह त्रिरत्न (तीन रत्न) और पंचमहाव्रत (पाँच महान व्रत) के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। त्रिरत्न में सही विश्वास, सही ज्ञान, और सही आचरण शामिल हैं, जो मुक्ति के लिए आवश्यक हैं।
सही आचरण पंचमहाव्रत का पालन करने का अर्थ है: अहिंसा (non-violence), सत्य वचन (truthfulness), अस्तेय (non-stealing), ब्रह्मचर्य (continence), और अपरिग्रह (non-possessiveness)।
निर्वाण प्राप्त करने के लिए, एक को सभीAttachments का त्याग करना चाहिए, जिसमें वस्त्र भी शामिल हैं। मुक्ति का मार्ग उपवास, आत्म-पीड़ा, अध्ययन, और ध्यान के माध्यम से है, जो मोक्ष के लिए एक मठीय जीवन को आवश्यक बनाता है। गृहस्थों को इन गुणों के हल्के रूपों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है, जिन्हें अनुव्रत (छोटे व्रत) कहा जाता है।
जबकि ब्राह्मणवाद अनुष्ठान-उन्मुख था, जैनism आचरण-उन्मुख है, जो नैतिक जीवन और व्यक्तिगत आचरण पर ध्यान केंद्रित करता है।
तीन रत्न: जैन जीवन का लक्ष्य आत्मा की मुक्ति प्राप्त करना है, जो जैन नैतिकता के तीन रत्नों का पालन करके प्राप्त किया जा सकता है: सही विश्वास, सही ज्ञान, और सही आचरण।
सही विश्वास (Samyak darshana) का अर्थ है चीजों को स्पष्ट रूप से देखना, पूर्वाग्रहों और अंधविश्वासों से बचना। यह सच्चे पैगम्बरों, सच्ची शास्त्रों, और सच्चे गुरु में विश्वास करने का संबंध रखता है।
सही ज्ञान (Samyak jnana) का अर्थ है वास्तविक ब्रह्मांड का सटीक ज्ञान, जिसमें पांच पदार्थ और नौ सत्य शामिल हैं। इसे पांच श्रेणियों में बांटा गया है: संवेदी ज्ञान, अध्ययन ज्ञान, दूरस्थ ज्ञान, मन पढ़ने का ज्ञान, और सर्वज्ञता।
सही आचरण (Samyak charitra) का अर्थ है जैन नैतिक नियमों के अनुसार जीना, जीवों को नुकसान पहुंचाने से बचना, और स्वयं कोAttachments और अशुद्ध विचारों से मुक्त करना।
सही विश्वास और सही ज्ञान के साथ एक व्यक्ति स्वाभाविक रूप से सही आचरण प्राप्त करेगा। मुख्य लक्ष्य जैन नैतिक कोड का पालन करके आत्मा को मुक्त करना है।
पांच मुख्य व्रत: महावीर ने पार्श्वनाथ द्वारा निर्धारित अहिंसा, सत्य, अस्तेय, और अपरिग्रह के चार व्रतों में ब्रह्मचर्य (continence) का सिद्धांत जोड़ा।
जैनism व्यक्तिगत ज्ञान और आत्म-नियंत्रण के माध्यम से आध्यात्मिक विकास को प्रोत्साहित करता है। अनुपालन के विभिन्न स्तर होते हैं, सख्त अनुयायियों और श्रमणों के लिए।
पांच प्रमुख व्रत हैं:
अस्तित्व के चार मुख्य रूप: जैन सिद्धांत चार मुख्य रूपों को मान्यता देता है: देव (deva), मानव (manushya), नरक beings (naraki), और पशु और पौधे (tiryancha)।
पशु और पौधों की श्रेणी को संवेदनशीलता के आधार पर और विभाजित किया गया है। सबसे निचली श्रेणी एक-संवेदन शरीर (ekendriya) की है।
इनमें से सबसे निचले हैं निगोड (nigodas),tiny जीव जिनमें केवल स्पर्श की संवेदनशीलता होती है। उनकी जीवन अवधि एक सेकंड का एक अंश होती है, और उन्हें हर जगह, यहां तक कि पौधों, जानवरों और लोगों के शरीर में भी रहने का विश्वास किया जाता है।
निगोड के ऊपर एक-संवेदन जीव हैं जो विभिन्न तत्वों (sthavara) में निवास करते हैं, जैसे पृथ्वी के शरीर, जल के शरीर, आग के शरीर, और वायु के शरीर। पौधे, हालांकि केवल एक संवेदना (स्पर्श) रखते हैं, की संरचना अधिक जटिल होती है और उनकी जीवन अवधि निगोड से अधिक होती है।
जानवरों की श्रेणी में दो से पांच संवेदन होते हैं, जिनमें सभी पांच संवेदन रखने वाले जानवरों को प्रेरक और तर्कशील श्रेणियों में और वर्गीकृत किया गया है।
जैन धर्म के अन्य शिक्षाएँ: जैन दर्शन और विश्वास: जैन दर्शन बुनियादी रूप से द्वैतवाद पर आधारित है, जो यह मानता है कि मानव व्यक्तित्व दो आवश्यक तत्वों से बना होता है: जीव (soul) और अजीव (matter)।
जीव (आत्मा): जीव की अवधारणा आत्मा को संदर्भित करती है, जो असीमित संख्या में मानी जाती है और ज्ञान, शक्ति, और आनंद की क्षमता में भिन्न होती है। जीव का सार चेतना, शक्ति, और आनंद है। जीव असीमित और शाश्वत होते हैं, और उनका विकास मुक्ति की ओर ले जाता है।
अजीव (पदार्थ): अजीव में पदार्थ, स्थान, गति (धर्म), विश्राम (अधर्म), और समय (काल) शामिल होता है। जीवों के विपरीत, अजीव नाशवान होते हैं। जीवों और अजीवों के बीच की अंतःक्रिया ऊर्जा उत्पन्न करती है, जो जन्म, मृत्यु, और विभिन्न जीवन अनुभवों का परिणाम होती है। इन ऊर्जा को अनुशासन के माध्यम से नष्ट किया जा सकता है, जिससे मुक्ति या निर्वाण की प्राप्ति होती है।
सात तत्त्व: जीव (आत्मा) और निर्जीव (पदार्थ) के बीच की अंतःक्रिया ऊर्जा उत्पन्न करती है, जिन्हें अनुशासन के माध्यम से नष्ट किया जा सकता है। इस सिद्धांत को सात तत्त्वों या सत्य में संक्षिप्त किया गया है:
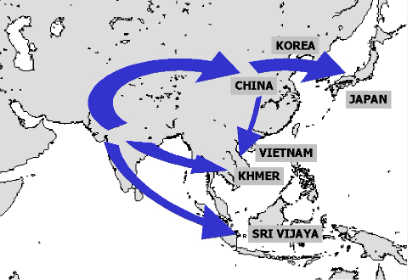

छठी शताब्दी ई.पू. भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवधि थी, जिसमें नए धर्मों का उदय हुआ। इस समय, ब्राह्मणों के अनुष्ठानिक और पारंपरिक विचारों के प्रति बढ़ती विरोध की भावना ने मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्रों में विभिन्न हेटेरोडॉक्स धार्मिक आंदोलनों के उदय को जन्म दिया। कुल मिलाकर 62 धार्मिक संप्रदायों को पहचाना गया, जिनमें से बौद्ध धर्म और जैन धर्म सबसे लोकप्रिय और संगठित धर्म बने। इस अवधि के नए धार्मिक विचार प्रचलित सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक परिस्थितियों का जवाब थे।
सामाजिक और आर्थिक जीवन में परिवर्तन, जैसे कस्बों का विकास, कारीगर वर्ग का विस्तार और व्यापार और वाणिज्य का तेजी से विकास, धर्म और दार्शनिक विचारों में बदलाव से निकटता से जुड़े थे। इस अवधि में परिव्राजक या श्रमणों की उपस्थिति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्होंने गृहस्थ जीवन का त्याग किया और अपने विचारों को फैलाने के लिए स्थान-स्थान पर घूमे। ये श्रमण बलिदान के culto और सामाजिक प्रमुखता के ब्राह्मणिक दावों के खिलाफ एकजुट थे। उनके विचारों में उच्छेदवाद (Ucchedavada) से लेकर शाश्वतवाद (Sashvatvarda) तक, अजिविकाओं की भाग्यवादिता से लेकर चारवाकों की भौतिकवाद तक फैले हुए थे।
हेटेरोडॉक्स संप्रदायों के उदय और विकास के कारण
सामाजिक स्थिति: वेदों के बाद के समय में, समाज चार वर्णों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रत्येक वर्ण के पास स्पष्ट कार्य थे, जिसमें ब्राह्मणों ने उच्चतम स्थिति का दावा किया और करों और दंड से छूट की मांग की। क्षत्रिय दूसरे स्थान पर थे, जो शासन और युद्ध के लिए जिम्मेदार थे, जबकि वैश्य कृषि, पशुपालन और व्यापार में लगे थे। शूद्रों को अन्य तीन वर्णों की सेवा करने के लिए बनाया गया था और उन्हें वेद अध्ययन से प्रतिबंधित किया गया था। वर्ण विभाजित समाज ने तनाव उत्पन्न किया, विशेष रूप से क्षत्रिय जिन्होंने ब्राह्मणों के अनुष्ठानिक प्रभुत्व के खिलाफ विरोध किया। वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध, दोनों क्षत्रिय जातियों से थे, ने ब्राह्मणों के अधिकार को चुनौती दी।
आर्थिक स्थिति: नए धर्मों का उदय उत्तर-पूर्वी भारत में नए कृषि अर्थव्यवस्था द्वारा प्रेरित था। मध्य गंगा के मैदानी इलाकों में लोहे के औजारों के प्रयोग ने जंगलों की सफाई, कृषि और बड़े बस्तियों के विकास को सक्षम बनाया। कृषि अर्थव्यवस्था पशुपालन पर निर्भर थी, लेकिन वेदिक प्रथाओं के तहत पशु बलिदान ने प्रगति में बाधा डाली। नए किसान समुदायों ने बलिदानों के लिए पशुओं के वध का विरोध किया, जिससे हेटेरोडॉक्स संप्रदायों द्वारा अहिंसा को अपनाया गया। इस अवधि में उत्तर-पूर्वी भारत में शहरों का उदय हुआ, जहां कारीगरों और व्यापारियों ने पहली बार सिक्कों का उपयोग किया, जिसने व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया। वैश्य, जो अपने सामाजिक स्थिति में सुधार करना चाहते थे, ने महावीर और बुद्ध का समर्थन किया, क्योंकि जैनism और बौद्ध धर्म ने प्रारंभिक रूप से वर्ण व्यवस्था की अनदेखी की। ये संप्रदाय अहिंसा का उपदेश देते थे, जो शांति और व्यापार को बढ़ावा देते थे, और वैश्य समुदाय को आकर्षित करते थे। जैनism और बौद्ध धर्म भौतिक संपत्ति को अस्वीकार करते थे, संयमित जीवन का समर्थन करते थे, जो सामाजिक असमानताओं और नए भौतिक जीवन से असंतुष्ट लोगों के साथ प्रतिध्वनित होता था।
धार्मिक स्थिति: वेदिक धार्मिक प्रथाएँ नए सामाजिक संदर्भ में जटिल और अक्सर अर्थहीन हो गईं। बलिदान और अनुष्ठान अधिक विस्तृत और महंगे हो गए, जिससे ब्राह्मणों का प्रभुत्व बढ़ा, जिन्होंने धार्मिक अनुष्ठानों का एकाधिकार किया। इन प्रथाओं के बढ़ते महत्व ने ब्राह्मणों की उच्च स्थिति को स्थापित किया, जिससे समाज अब वर्णों में विभाजित हो गया। वेदिक अनुष्ठान कई लोगों के लिए प्रासंगिकता खो चुके थे, जो वैकल्पिक धार्मिक आदेशों के लिए मार्ग प्रशस्त करता था।
राजनीतिक स्थिति: क्षत्रिय राजतंत्रों और गण-संघों में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने लगे, ब्राह्मणिक प्रभुत्व का विरोध करते हुए। उभरते साम्राज्यों के बीच लगातार युद्धों और असंतोषित व्यापारियों ने लोगों को शांतिपूर्ण, अहिंसक धर्मों की खोज करने के लिए प्रेरित किया। बुद्ध और महावीर पहले नहीं थे जिन्होंने वेदिक विश्वासों की आलोचना की; पहले के उपदेशक जैसे कपिल और मक्कली गोसाल ने भी वेदिक प्रथाओं की निंदा की थी। नए दार्शनिकताएँ प्रचारित की जा रही थीं, लेकिन यह बुद्ध और महावीर थे जिन्होंने एक व्यवहार्य वैकल्पिक धार्मिक क्रम की पेशकश की।
जैन धर्म
उद्गम और विश्वास: जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है जो भारत से है, जो हानिरहितता और त्याग को मुक्ति और सुख के मार्ग के रूप में महत्व देता है। यह ब्रह्मांड के हर प्राणी के कल्याण और स्वयं ब्रह्मांड के स्वास्थ्य पर केंद्रित है। जैनों का विश्वास है कि 24 तीर्थंकर हैं, जो उनके धर्म के नेता हैं। पहले तीर्थंकर ऋषभadev हैं, जो अयोध्या में पैदा हुए थे। इक्कीसवें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं, जिन्होंने राजसी जीवन का त्याग कर एक श्रमण बनने का निर्णय लिया। महावीर को चौबीसवें और अंतिम तीर्थंकर माना जाता है। कुछ तीर्थंकरों के नाम, जैसे ऋषभ और अरिष्टनेमि, प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित हैं जैसे कि ऋग्वेद। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में ऋषभ को नारायण का अवतार बताया गया है। तीर्थंकरों की मिथक, जिनमें से अधिकांश मध्य गंगा क्षेत्र में पैदा हुए और बिहार में निर्वाण प्राप्त किया, शायद जैन धर्म को प्राचीनता का एहसास दिलाने के लिए बनाई गई।
वर्धमान महावीर: वर्धमान महावीर, जिन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है, चौबीसवें और अंतिम तीर्थंकर थे। उनका जन्म 540 ई.पू. में कुंडग्राम में, जो वर्तमान बिहार के वैशाली के निकट है, हुआ। उनके पिता सिद्धार्थ, ज्ञात्रिका जाति के प्रमुख थे, और उनकी माता त्रिशला मगध के शाही परिवार से संबंधित थीं। महावीर का विवाह यशोदा से हुआ और उनके एक बेटी थी जिसका नाम अन्नोजा था।
महावीर ने प्रारंभ में एक गृहस्थ के रूप में जीवन व्यतीत किया, लेकिन 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने परिवार का त्याग किया और सत्य की खोज में एक श्रमण बन गए। बारह वर्षों तक भिक्षाटन और तपस्या करने के बाद, उन्होंने 42 वर्ष की आयु में मुजफ्फरपुर जिले, बिहार में रिजुपालिका नदी के पास एक साल के पेड़ के नीचे सर्वज्ञता (कैवल्य) प्राप्त की। ज्ञान की प्राप्ति के बाद, महावीर को केवली (सर्वज्ञ), जिन (विजेता), और महावीर (महान नायक) के रूप में जाना जाने लगा। उन्होंने निग्रंथ (बंधनमुक्त) नामक एक संप्रदाय का नेतृत्व किया, जो बाद में जैन धर्म के रूप में जाना जाने लगा। अगले 30 वर्षों तक, महावीर ने कोसल, मगध, मिथिला, और चंपा जैसे क्षेत्रों में अपने सिद्धांतों का प्रचार किया। वह हर साल आठ महीने घूमते थे और चार महीनों की बारिश के मौसम में पूर्वी भारत के एक प्रमुख शहर में बिताते थे। उन्होंने अक्सर राजा बिंबिसार और अजातशत्रु के दरबारों का दौरा किया। महावीर की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में पाव (राजगृह के निकट) में आत्म-आहार (Sallekana) द्वारा 468 ई.पू. में हुई।
महावीर के शिक्षाएँ: महावीर ने वेदों, वेदिक अनुष्ठानों और ब्राह्मणों की सर्वोच्चता के अधिकार को खारिज कर दिया। जैनism का ध्यान सही ज्ञान, सही विश्वास, और सही आचरण के माध्यम से सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने पर है, बिना अनुष्ठानों की आवश्यकता के। उन्होंने कैवल्य (निर्वाण या मोक्ष) प्राप्त करने के लिए एक संयमित और सरल जीवन जीने का समर्थन किया। महावीर ने अपने पूर्वज पार्श्व की तुलना में एक अधिक कठोर जीवन का जोर दिया, जिससे जैनism बाद में दो संप्रदायों में विभाजित हो गया: श्वेताम्बर (जो सफेद वस्त्र पहनते हैं) और दिगम्बर (जो नग्न होते हैं)।
बौद्ध धर्म के विपरीत, महावीर ने वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की। उन्होंने विश्वास किया कि किसी व्यक्ति का वर्ण उनके पिछले जन्मों में उनके कार्यों द्वारा निर्धारित होता है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि निम्न जातियों के व्यक्ति भी सदाचारी जीवन द्वारा मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। महावीर ने देवताओं की उपस्थिति को स्वीकार किया, लेकिन उन्हें जिन से नीचे रखा। उन्होंने सिखाया कि ब्रह्मांड का निर्माण, रखरखाव या विनाश किसी व्यक्तिगत देवता द्वारा नहीं, बल्कि सार्वभौमिक कानूनों द्वारा होता है। उन्होंने विश्वास किया कि सभी वस्तुओं, संवेदनशील या असंवेदनशील, में विभिन्न डिग्री की चेतना होती है और जब नुकसान पहुंचता है तो वे दर्द महसूस कर सकते हैं। उन्होंने कर्म और आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांतों पर जोर दिया। कर्म का प्रवाह (Asrav) आत्मा को बाधित करता है, जिससे उसकी शुद्धता का आवरण बनता है, जो जन्म और मृत्यु के चक्र की ओर ले जाता है। जैनism सिखाता है कि मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य आत्मा की शुद्धि और निर्वाण (मोक्ष) की प्राप्ति है, जो जन्म और मृत्यु से मुक्ति का संकेत है।
यह त्रिरत्न (तीन रत्न) और पंचमहाव्रत (पाँच महान व्रत) के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। त्रिरत्न में सही विश्वास, सही ज्ञान, और सही आचरण शामिल हैं, जो मुक्ति के लिए आवश्यक हैं।
सही आचरण पंचमहाव्रत का पालन करने का अर्थ है: अहिंसा (non-violence), सत्य वचन (truthfulness), अस्तेय (non-stealing), ब्रह्मचर्य (continence), और अपरिग्रह (non-possessiveness)।
निर्वाण प्राप्त करने के लिए, एक को सभीAttachments का त्याग करना चाहिए, जिसमें वस्त्र भी शामिल हैं। मुक्ति का मार्ग उपवास, आत्म-पीड़ा, अध्ययन, और ध्यान के माध्यम से है, जो मोक्ष के लिए एक मठीय जीवन को आवश्यक बनाता है। गृहस्थों को इन गुणों के हल्के रूपों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है, जिन्हें अनुव्रत (छोटे व्रत) कहा जाता है।
जबकि ब्राह्मणवाद अनुष्ठान-उन्मुख था, जैनism आचरण-उन्मुख है, जो नैतिक जीवन और व्यक्तिगत आचरण पर ध्यान केंद्रित करता है।
तीन रत्न: जैन जीवन का लक्ष्य आत्मा की मुक्ति प्राप्त करना है, जो जैन नैतिकता के तीन रत्नों का पालन करके प्राप्त किया जा सकता है: सही विश्वास, सही ज्ञान, और सही आचरण।
सही विश्वास (Samyak darshana) का अर्थ है चीजों को स्पष्ट रूप से देखना, पूर्वाग्रहों और अंधविश्वासों से बचना। यह सच्चे पैगम्बरों, सच्ची शास्त्रों, और सच्चे गुरु में विश्वास करने का संबंध रखता है।
सही ज्ञान (Samyak jnana) का अर्थ है वास्तविक ब्रह्मांड का सटीक ज्ञान, जिसमें पांच पदार्थ और नौ सत्य शामिल हैं। इसे पांच श्रेणियों में बांटा गया है: संवेदी ज्ञान, अध्ययन ज्ञान, दूरस्थ ज्ञान, मन पढ़ने का ज्ञान, और सर्वज्ञता।
सही आचरण (Samyak charitra) का अर्थ है जैन नैतिक नियमों के अनुसार जीना, जीवों को नुकसान पहुंचाने से बचना, और स्वयं कोAttachments और अशुद्ध विचारों से मुक्त करना।
सही विश्वास और सही ज्ञान के साथ एक व्यक्ति स्वाभाविक रूप से सही आचरण प्राप्त करेगा। मुख्य लक्ष्य जैन नैतिक कोड का पालन करके आत्मा को मुक्त करना है।
पांच मुख्य व्रत: महावीर ने पार्श्वनाथ द्वारा निर्धारित अहिंसा, सत्य, अस्तेय, और अपरिग्रह के चार व्रतों में ब्रह्मचर्य (continence) का सिद्धांत जोड़ा।
जैनism व्यक्तिगत ज्ञान और आत्म-नियंत्रण के माध्यम से आध्यात्मिक विकास को प्रोत्साहित करता है। अनुपालन के विभिन्न स्तर होते हैं, सख्त अनुयायियों और श्रमणों के लिए।
पांच प्रमुख व्रत हैं:
- अहिंसा (nonviolence): जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाना, जानबूझकर और अनजान में होने वाले नुकसान को कम करना।
- सत्य (truth): हमेशा सच बोलना। यदि सच बोलने से हिंसा हो सकती है, तो चुप रहना उचित हो सकता है।
- अस्तेय (not stealing): किसी भी चीज को नहीं लेना जो स्वेच्छा से पेश नहीं की गई है। भौतिक संपत्ति का शोषण या कमजोर का शोषण चोरी माना जाता है।
- ब्रह्मचर्य (continence): इंद्रियों पर नियंत्रण, यौन गतिविधि को सीमित करना।
- अपरिग्रह (non-possessiveness): भौतिकवाद और वस्तुओं, स्थानों, और लोगों के प्रतिAttachments से मुक्ति। जैन श्रमण और नन संपत्ति और सामाजिक संबंधों का पूरी तरह से त्याग करते हैं।
अस्तित्व के चार मुख्य रूप: जैन सिद्धांत चार मुख्य रूपों को मान्यता देता है: देव (deva), मानव (manushya), नरक beings (naraki), और पशु और पौधे (tiryancha)।
पशु और पौधों की श्रेणी को संवेदनशीलता के आधार पर और विभाजित किया गया है। सबसे निचली श्रेणी एक-संवेदन शरीर (ekendriya) की है।
इनमें से सबसे निचले हैं निगोड (nigodas),tiny जीव जिनमें केवल स्पर्श की संवेदनशीलता होती है। उनकी जीवन अवधि एक सेकंड का एक अंश होती है, और उन्हें हर जगह, यहां तक कि पौधों, जानवरों और लोगों के शरीर में भी रहने का विश्वास किया जाता है।
निगोड के ऊपर एक-संवेदन जीव हैं जो विभिन्न तत्वों (sthavara) में निवास करते हैं, जैसे पृथ्वी के शरीर, जल के शरीर, आग के शरीर, और वायु के शरीर। पौधे, हालांकि केवल एक संवेदना (स्पर्श) रखते हैं, की संरचना अधिक जटिल होती है और उनकी जीवन अवधि निगोड से अधिक होती है।
जानवरों की श्रेणी में दो से पांच संवेदन होते हैं, जिनमें सभी पांच संवेदन रखने वाले जानवरों को प्रेरक और तर्कशील श्रेणियों में और वर्गीकृत किया गया है।
जैन धर्म के अन्य शिक्षाएँ: जैन दर्शन और विश्वास: जैन दर्शन बुनियादी रूप से द्वैतवाद पर आधारित है, जो यह मानता है कि मानव व्यक्तित्व दो आवश्यक तत्वों से बना होता है: जीव (soul) और अजीव (matter)।
जीव (आत्मा): जीव की अवधारणा आत्मा को संदर्भित करती है, जो असीमित संख्या में मानी जाती है और ज्ञान, शक्ति, और आनंद की क्षमता में भिन्न होती है। जीव का सार चेतना, शक्ति, और आनंद है। जीव असीमित और शाश्वत होते हैं, और उनका विकास मुक्ति की ओर ले जाता है।
अजीव (पदार्थ): अजीव में पदार्थ, स्थान, गति (धर्म), विश्राम (अधर्म), और समय (काल) शामिल होता है। जीवों के विपरीत, अजीव नाशवान होते हैं। जीवों और अजीवों के बीच की अंतःक्रिया ऊर्जा उत्पन्न करती है, जो जन्म, मृत्यु, और विभिन्न जीवन अनुभवों का परिणाम होती है। इन ऊर्जा को अनुशासन के माध्यम से नष्ट किया जा सकता है, जिससे मुक्ति या निर्वाण की प्राप्ति होती है।
सात तत्त्व: जीव (आत्मा) और निर्जीव (पदार्थ) के बीच की अंतःक्रिया ऊर्जा उत्पन्न करती है, जिन्हें अनुशासन के माध्यम से नष्ट किया जा सकता है। इस सिद्धांत को सात तत्त्वों या सत्य में संक्षिप्त किया गया है:
- कुछ ऐसा है जिसे जीवित कहा जा सकता है।
- कुछ ऐसा है जिसे निर्जीव कहा जा सकता है।
- दोनों एक-दूसरे के संपर्क में आते हैं।
- संपर्क से ऊर्जा का उत्पादन
जीवा का अर्थ आत्मा है, जिसे संख्या में अनंत माना जाता है और यह ज्ञान, शक्ति, और आनंद की क्षमता में भिन्न होता है। जीवा का सार चेतना, शक्ति, और आनंद है। जीवाएँ अ destructible और शाश्वत होती हैं, और उनकी प्रगति मोक्ष की ओर ले जाती है।
- जीवा का अर्थ आत्मा है, जिसे संख्या में अनंत माना जाता है और यह ज्ञान, शक्ति, और आनंद की क्षमता में भिन्न होता है। जीवा का सार चेतना, शक्ति, और आनंद है।
अजीवा में पदार्थ, स्थान, गति (धर्म), विश्राम (अधर्म), और समय (काल) शामिल हैं। जीवों के विपरीत, अजीवाएँ नष्ट होने वाली होती हैं। जीवों और अजीवों के बीच की अंतःक्रिया ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करती है जो जन्म, मृत्यु, और विभिन्न जीवन अनुभवों का परिणाम होती है। इन ऊर्जा को अनुशासन के माध्यम से नष्ट किया जा सकता है, जिससे मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति होती है।
- अजीवा में पदार्थ, स्थान, गति (धर्म), विश्राम (अधर्म), और समय (काल) शामिल हैं। जीवों के विपरीत, अजीवाएँ नष्ट होने वाली होती हैं।
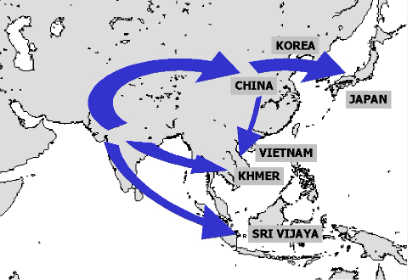

The document जैन धर्म का प्रसार | इतिहास वैकल्पिक UPSC (नोट्स) is a part of the UPSC Course इतिहास वैकल्पिक UPSC (नोट्स).
All you need of UPSC at this link: UPSC
|
28 videos|739 docs|84 tests
|
Related Searches















