प्राचीन भारत में धन उधारी | इतिहास वैकल्पिक UPSC (नोट्स) PDF Download
प्रारंभिक वैदिक और उत्तर वैदिक काल (1500 ईसा पूर्व – 600 ईसा पूर्व)
धन उधारी का प्रारंभिक उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, जहाँ एक सूदखोर या धन उधारी करने वाले को कुसिदिन कहा गया है। यह शब्द पाठ में कई बार आता है और इसे एक ऐसे धन उधारी करने वाले के रूप में समझा जाता है जो ब्याज लेता है।
इस अवधि के दौरान, ऋण पत्रों के रूप रूप में रिनपत्र या रिनलेख्य का सामान्य उपयोग होता था। इन दस्तावेजों में महत्वपूर्ण विवरण शामिल होते थे जैसे:
- ऋणी और ऋणदाता के नाम
- ऋण की राशि
- ब्याज दर
- चुकाने की शर्तें
- चुकाने की समय सीमा
उत्तर वैदिक काल के दौरान, विशेष रूप से 600 से 300 ईसा पूर्व के बीच, भारत ने दूसरे शहरीकरण के चरण की शुरुआत देखी। इस युग में विभिन्न आर्थिक प्रथाओं में महत्वपूर्ण विकास हुआ, विशेष रूप से धन उधारी और व्यापार में।
ऋण प्रथाओं का विकास:
- ऋण पत्र: इस अवधि के दौरान अनिनपन्न के रूप में जाने जाने वाले ऋण पत्रों का निर्माण जारी रहा, जो औपचारिक उधारी प्रथाओं की निरंतरता को दर्शाता है।
- धन उधारी और ब्याज: बाद के सूत्र ग्रंथ (700-100 ईसा पूर्व) और बौद्ध जाटकों (600-400 ईसा पूर्व) में धन उधारी और ब्याज भुगतान के अधिक बार और विस्तृत संदर्भ मिलते हैं, जो वित्तीय लेन-देन की बढ़ती जटिलता का सुझाव देते हैं।
- गौतम धर्मसूत्र धन उधारी को वैश्याओं के चार प्राथमिक व्यवसायों में से एक मानता है, जो समाज में इस पेशे के महत्व को दर्शाता है।
- सिक्कों का परिचय, विशेष रूप से पंच-चिन्हित सिक्के, व्यापार और वाणिज्य में महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक था।
- धन के आगमन के साथ, धन उधारी एक अधिक प्रमुख और संगठित गतिविधि बन गई।
इस अवधि के पाली ग्रंथों में धन उधारी, ऋण उपकरणों और विभिन्न प्रथाओं के कई संदर्भ शामिल हैं, जैसे संपत्तियों का गिरवी रखना और यहां तक कि अत्यधिक दिवालियापन के मामलों में परिवार के सदस्यों को वचन पर रखना।
दिलचस्प बात यह है कि ऋण लेने वालों को बौद्ध संघ (संन्यासी समुदाय) में शामिल होने से वंचित किया गया था जब तक वे अपने ऋण चुकता नहीं कर लेते, जो इस समय के वित्तीय दायित्वों की गंभीरता को दर्शाता है।
सेठियों (श्रेश्ठिनों) की भूमिका:पाली ग्रंथों में सेठियों (श्रेश्ठिनों) की भूमिका को भी उजागर किया गया है, जो व्यापार और धन उधारी में शामिल उच्च स्तर के व्यापारी थे। ये व्यक्ति व्यापारियों, व्यापारी साहसी लोगों और यहां तक कि युद्ध और वित्तीय संकट के समय में राजाओं को वित्तपोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, जो अर्थव्यवस्था में उनके अभिन्न भाग को दर्शाता है।
सूदखोरी के प्रति बदलते दृष्टिकोण:
इस अवधि के दौरान, सूदखोरी और धन उधारी के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में एक स्पष्ट परिवर्तन देखा गया। उदाहरण के लिए, ऋषि वशिष्ठ ने उच्च जातियों, विशेष रूप से ब्राह्मणों (पुजारी) और क्षत्रियों (योद्धाओं) को धन उधारी में संलग्न होने के खिलाफ चेतावनी दी। इसके अतिरिक्त, जाटकों में अक्सर धन उधारी को नकारात्मक रूप में चित्रित किया गया, जो सूदखोरी प्रथाओं के प्रति contempt की उभरती भावना को दर्शाता है।
संक्षेप में, 600 से 300 ईसा पूर्व का उत्तर वैदिक काल भारत में महत्वपूर्ण आर्थिक विकास का समय था। धन उधारी, व्यापार और सिक्कों के परिचय की प्रथाओं ने देश के प्रारंभिक वित्तीय परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
मौर्य काल (3rd – 2nd शताब्दी ईसा पूर्व)कौटिल्य का अर्थशास्त्र:
- सुरक्षित ऋण के लिए अधिकतम कानूनी ब्याज दर 15% और असुरक्षित ऋण के लिए 60% निर्धारित करता है।
- जोखिम कारकों के आधार पर ब्याज दर 120% से 240% प्रति वर्ष तक बढ़ सकती है, जाति की परवाह किए बिना।
- अर्थशास्त्र के अनुरूप, लेकिन धन उधारी में जाति पर जोर देता है।
- वैश्य जाति को धन उधारी में संलग्न होने की अनुमति देता है और ऋणदाता की जाति के आधार पर असुरक्षित ऋण के लिए ब्याज दरें 15% से 60% के बीच निर्धारित करता है।
शहरी अर्थव्यवस्था और धन उधारी:
शहरी अर्थव्यवस्था और धन के माध्यम के रूप में बढ़ती उपयोग ने धन उधारी प्रथाओं को बढ़ावा दिया। मेगस्थनीज के दावे के विपरीत, भारतीयों ने ब्याज के साथ धन उधार लेने और देने में संलग्न थे।
गिल्डों का विकास:
- इस अवधि के दौरान गिल्डों की संख्या में वृद्धि हुई, जिनके शिलालेख बैंकर्स के रूप में उनकी भूमिका को दर्शाते हैं, जो निवेशित धन पर ब्याज का भुगतान करते हैं।
- ऐसे शिलालेखों के उदाहरणों में मथुरा, जुनार, और नासिक शामिल हैं।
- कानूनी सीमा से अधिक ब्याज दरें वसूल नहीं की जा सकतीं, ऐसी उधारी को सूदखोरी के रूप में वर्गीकृत किया गया।
- धन उधारी को एक वैध व्यावसायिक गतिविधि के रूप में मान्यता दी गई।
- धन अर्जन के सात तरीकों में धन उधारी शामिल है:
- विरासत
- मित्र और जमा करने वाले से उपहार
- खरीदना
- विजय करना
- धन उधारी
- श्रम
- अच्छे लोगों से उपहार
मनुस्मृति में कानूनी ब्याज दरें निम्नलिखित निर्धारित की गई हैं:
- ब्राह्मणों के लिए 2% प्रति माह
- योद्धाओं के लिए 3% प्रति माह
- व्यापारियों के लिए 4% प्रति माह
- शूद्रों के लिए 5% प्रति माह
अत्यधिक ब्याज की मनाही:
कानूनी ब्याज से अधिक दर पर धन उधार देना पाप माना जाता है।
अधिकतम ब्याज मार्गदर्शिकाएँ:
गौतम, विष्णु और मनु सहमत होते हैं कि ब्याज की राशि को मुख्यधन से अधिक नहीं होना चाहिए। वे कुछ वस्तुओं जैसे अनाज, फल, ऊन, सोना और कपड़ों के लिए विशिष्ट अधिकतम ब्याज दरें प्रदान करते हैं।
उषवादाता शिलालेख:
दो बुनकर गिल्डों द्वारा गोवर्धन (नासिक) में निर्धारित ब्याज दरें 12% मासिक और 9% वार्षिक हैं, जो अर्थशास्त्र और स्मृतियों में मानकों से कम हैं।
गुप्ता और उत्तर-गुप्ता काल
नारद स्मृति:
धन उधारी के माध्यम से अर्जित धन को 'धब्बेदार धन' और 'काला धन' के रूप में वर्णित करता है।
धर्मशास्त्र ग्रंथ:
सूदखोरी पर विस्तृत विनियम प्रदान करते हैं, जिसमें अनुबंध का निर्माण, ब्याज दरों पर स्थानीय रीति-रिवाजों का प्रभाव, और ऋण सुरक्षा के रूप में स्वीकार्य गिरवी प्रकार शामिल हैं।
सुरक्षित ऋण के लिए सामान्य ब्याज दर 15% प्रति वर्ष की सिफारिश करते हैं, असुरक्षित ऋण के लिए जो ऋणदाता की वर्ण के आधार पर काफी अधिक होती है।
बृहस्पति स्मृति:
यह कहता है कि यदि किसी अचल संपत्ति जैसे ज़मीन ने मुख्यधन से अधिक उपज दी है, तो ऋणी को स्वचालित रूप से गिरवी संपत्ति पुनः प्राप्त करनी चाहिए।
ऋण चुकता न करने के परिणाम:
ऋण न चुकाने के परिणाम अगले जीवन में होते हैं, नारद स्मृति में कहा गया है कि ऋणी को ऋण चुकाने के लिए श्रमिक के रूप में ऋणदाता के घर में पुनर्जन्म लेना होगा।
धन उधारी पर चर्चा:
धन उधारी पर व्यापक चर्चा, जिसमें संयुक्त धन उधारी के उपक्रम शामिल हैं, यह इंगित करता है कि धन का सक्रिय रूप से उपयोग, उधार और लाभ के लिए उधारी की जा रही थी।
सेनकापट शिलालेख:
यह संकेत करता है कि संन्यासियों को ब्याज कमाने और लाभ बनाने के उद्देश्य से उधारी नहीं करनी चाहिए।
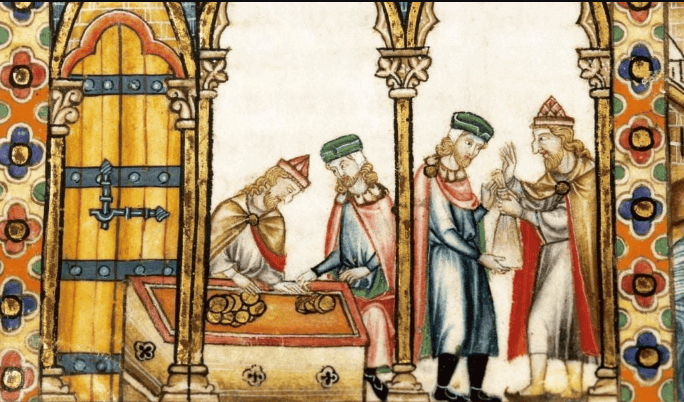
|
28 videos|739 docs|84 tests
|















