प्राचीन भारत में दासता | इतिहास वैकल्पिक UPSC (नोट्स) PDF Download
गुलामों का संदर्भ
ऋग्वेदिक काल: ऋग्वेदिक ग्रंथों में 'दासियों' का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद संहिता में देखा जाता है, जो बलि देने वाले पुरोहितों को अर्पण के संदर्भ में है, जिसे 'दान' (दान) के रूप में दर्शाया गया है। इसे "दान स्तुतियाँ" (दान गीत) में उजागर किया गया है। वेदिक काल के दौरान, यह सुझाव दिया गया है कि दासियों का मुख्य उद्देश्य घरेलू कार्य था।
पोस्ट-वेदिक काल: पोस्ट-वेदिक काल में 'दासों' (पुरुष गुलाम) का उल्लेख भी होता है। ये संदर्भ दर्शाते हैं कि गुलामों की भूमिका घरेलू कार्यों से बढ़कर कृषि, व्यापार और यहां तक कि सैन्य सेवा तक विस्तारित हो गई थी। यह गुलामी की संस्था प्राचीन काल में भी बनी रही।
गुलामों की विभिन्न श्रेणियाँ:
- प्राचीन ग्रंथ विभिन्न प्रकार के गुलामों का वर्णन करते हैं:
- तीन त्रिपिटक में आठ प्रकार के गुलामों की पहचान की गई है।
- अर्थशास्त्र में पांच श्रेणियों का उल्लेख है।
- मनुस्मृति और नारदीय स्मृति दोनों में पंद्रह प्रकार के गुलामों का उल्लेख है।
किसी भी वर्ण (सामाजिक वर्ग) का व्यक्ति गुलाम बन सकता था, जिसमें ब्राह्मण भी शामिल थे। हालांकि, अधिकांश गुलाम शूद्र थे। जबकि महिला गुलाम भी थीं, ब्राह्मण महिलाओं की बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध था।
गुलामों के अधिकार:
- गुलामों के अधिकारों की परिभाषा: प्राचीन धर्मशास्त्र साहित्य में गुलामों के अधिकारों और उनके मालिकों के साथ संबंधों को स्पष्ट किया गया है।
- कमाई का अधिकार और संपत्ति का अधिकार: गुलामों को कमाई और संपत्ति का अधिकार था।
- संपत्ति विरासत का अधिकार: गुलामों को संपत्ति विरासत का अधिकार था।
- कानूनी अधिकारों की सीमाएँ: गुलामों को मुकदमा करने या गवाही देने का अधिकार नहीं था, जो उनके कानूनी अधिकारों की कमी को दर्शाता है।
- स्वतंत्रता का अधिकार: गुलामों को गुलामी से मुक्त होने का अधिकार था, हालांकि यह मालिक की इच्छा पर निर्भर था।
- स्वतंत्रता की राह: सामान्यतः, जो गुलाम 'संन्यास' (त्याग का एक रूप) में प्रवेश करते थे, वे स्वतंत्र हो जाते थे।
- जीवन के अधिकार: मालिकों को गुलाम को मारने का अधिकार नहीं था, जो यह दर्शाता है कि उनके जीवन पर अधिकार नहीं था।
गुलाम बनने के मार्ग:
- संकट के समय आत्म-विक्रय: व्यक्तियों ने संकट के समय खुद को गुलामी में बेच दिया, और वे अपने परिवार के सदस्यों को भी बेच सकते थे।
- युद्ध के कैदी: व्यक्तियों ने युद्ध के कैदी के रूप में गुलाम बनना स्वीकार किया।
- वंशानुगत गुलामी: गुलाम माता-पिता के बच्चे स्वचालित रूप से गुलाम बन जाते थे।
प्राचीन भारत में गुलामी:
- वेदिक युग में गुलामी: वेदिक युग के दौरान, ऐसे समूह थे जिन्हें शूद्रों से भी निम्न माना जाता था, जिसमें दास (पुरुष गुलाम) और दासियाँ (महिला गुलाम) शामिल थीं।
- गुलामों का कभी-कभी दान-स्तुतियों में उपहारों के रूप में उल्लेख किया गया, लेकिन ऐसे उदाहरण थे जहां गुलाम महिलाओं से जन्मे बच्चे उच्च स्थिति में उठ सकते थे।
- आर्यनों द्वारा पराजित दास और दस्यु गुलामों की तरह व्यवहार किए गए और शूद्र माने गए।
श्रम और गुलामी:
- घराना श्रम की मूल इकाई थी, और वेतन श्रम का सामान्यतः उल्लेख नहीं किया गया। हालांकि, ऋग्वेद ने गुलामी को स्वीकार किया।
- गुलामी युद्ध या ऋण के माध्यम से हो सकती थी, और प्रारंभ में, जातीय भिन्नताएँ गुलामी में एक भूमिका निभा सकती थीं।
- गुलाम, पुरुष और महिला, सामान्यतः घरों में कार्य करते थे और उत्पादन से संबंधित गतिविधियों में महत्वपूर्ण रूप से शामिल नहीं थे।
- घरेलू गुलाम अधिक सामान्य थे, और पुरोहितों को उपहार के रूप में गुलाम दिए जाने के उदाहरण थे, मुख्यतः घरेलू कार्यों के लिए महिलाएँ।
- पुरोहितों और राजाओं ने घरेलू सेवा के लिए महिला गुलामों को employed किया, हालांकि उनकी संख्या शायद अधिक नहीं थी।
- इतिहास के दौरान, पुरुषों और महिलाओं के लिए गुलामी के अनुभव में एक महत्वपूर्ण अंतर था, जिसमें महिलाओं को श्रम शोषण के अलावा यौन शोषण का सामना करना पड़ता था।
गुलामों के उपहार:
ऋग्वेद के बाद के ग्रंथों में गायों, घोड़ों, रथों, सोने, कपड़ों और महिला गुलामों के उपहारों की प्रशंसा की गई है, जो राजाओं द्वारा पुरोहितों को दिए गए थे।
उत्तरी काले चमकदार बर्तन (NBPW) काल में गुलामी:
NBPW काल के दौरान, प्रगति और बल के उपयोग ने कुछ व्यक्तियों को बड़े पैमाने पर भूमि का मालिक बनाने में सक्षम बनाया, जिसके लिए खेती के लिए कई गुलामों और श्रमिकों की आवश्यकता थी।
वेदिक काल में, खेती का कार्य मुख्य रूप से परिवार के सदस्यों की सहायता से किया जाता था, और वेदिक साहित्य में वेतनभोगियों का कोई उल्लेख नहीं था।
हालांकि, बुद्ध के समय के दौरान, गुलामों और वेतनभोगियों की खेती में भागीदारी सामान्य हो गई। इसलिए, NBPW काल में, बड़े भूखंडों पर गुलामों और कृषि श्रमिकों की सहायता से काम किया गया।
गुलामी का उल्लेख ग्रंथों में (600-300 BCE):
- 600-300 BCE काल के विभिन्न ग्रंथों में पुरुष और महिला गुलामों के अस्तित्व के कई संदर्भ शामिल हैं।
- दिघ निकाय में दासा को ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है जो स्वयं का मालिक नहीं है, किसी पर निर्भर है, और जहाँ चाहे जा नहीं सकता।
- विनय पिटक में तीन प्रकार के गुलामों की पहचान की गई है: अंतोजातक (महिला गुलाम का संतान), धनकित (खरीद गया गुलाम), और करमाराणित (दूसरे देश से लाया गया गुलाम)।
- दिघ निकाय में एक चौथे प्रकार के गुलाम का भी उल्लेख है, समं दासवयं उपगतो, जिसने स्वेच्छा से गुलामी स्वीकार की है।
प्रतिरोध के उदाहरण:
- चक्रवर्ती ने बौद्ध कैनन में प्रतिरोध के दो उदाहरणों की पहचान की है।
- पहला उदाहरण विनय पिटक में दसा-कम्मकारों का उल्लेख है, जो शाक्य परिवार के महिलाओं पर प्रतिशोध के रूप में हमले करते हैं।
- दूसरा उदाहरण दासी काली और उसकी मालकिन, गृहपति वैदेही की कहानी है, जो मझ्झिमा निकाय में है। काली ने वैदेही के शांत स्वभाव को अपनी उत्कृष्टता के कारण समझा।
मौर्य काल में गुलामी:
मेगास्थनीज ने भारत में गुलामों की अनुपस्थिति का उल्लेख किया, लेकिन घरेलू गुलाम संभवतः वेदिक काल से मौजूद थे।
अर्थशास्त्र में दासों (गुलामों) और अहितकास (जो ऋण लेते समय ऋणदाताओं को समर्पित होते हैं) पर विस्तृत चर्चा की गई है।
विभिन्न प्रकार के गुलामों और गुलामी की स्थितियों, दोनों अस्थायी और स्थायी, का उल्लेख किया गया है।
अर्थशास्त्र में गाँव के श्रम, बंधक श्रम, और गुलाम श्रम की चर्चा है।
गुलाम निजी व्यक्तियों और राज्य दोनों की सेवा में पाए जाते थे।
कौटिल्य ने पुरुष और महिला गुलामों के उपचार के लिए नियम निर्धारित किए और उल्लंघनों के लिए दंड निर्दिष्ट किए।
दंडों के उदाहरण:
- गर्भवती महिला गुलाम को मातृत्व के प्रबंध के बिना बेचने या गिरवी रखने के लिए दंड।
- गर्भवती गुलाम को गर्भपात कराने के लिए दंड।
अर्थशास्त्र में यह भी उल्लेख है कि गुलामों का मुक्त होना (मुक्ति) पैसे के भुगतान पर संभव था।
यदि कोई दासी (महिला गुलाम) अपने मालिक को एक पुत्र देती है, तो उसे गुलामी से मुक्त किया जाएगा, और बच्चा पिता का वैध पुत्र माना जाएगा।
मौर्य काल में एक महत्वपूर्ण विकास: कृषि कार्यों में गुलामों का रोजगार।
गुलामों को बड़े पैमाने पर कृषि में लगाया गया, जो सरकार द्वारा बनाए गए राज्य खेतों पर काम करते थे।
गुलामों और श्रमिकों को इन खेतों पर काम पर रखा गया, जिनमें कalinga के युद्ध कैदी भी शामिल थे, जिन्हें अशोक ने पाटलिपुत्र लाया।
युद्ध के कैदियों की संख्या (150,000) को अतिशयोक्ति माना जाता है, लेकिन यह गुलाम श्रम के पैमाने को उजागर करता है।
हालांकि, प्राचीन भारत में अधिकांश गुलामों को मुख्य रूप से घरेलू कार्यों में लगाया गया था।
छोटे किसान, कभी-कभी गुलामों और श्रमिकों की सहायता से, उत्पादन में प्रमुख भूमिका निभाते थे।
अशोक के शिलालेख: अशोक का शिलालेख 9 दासों (गुलामों) और भाटकास (सेवकों) के प्रति सभ्यता का व्यवहार करने पर जोर देता है।
शिलालेख 9 में दाम्हा के समारोह का वर्णन किया गया है, जिसमें दासों और सेवकों के प्रति उचित शिष्टाचार, बड़ों का सम्मान, सभी जीवों के साथ सौम्यता, और श्रमणों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता शामिल है।
शिलालेख 11 दान के उपहार को सभी उपहारों में सबसे अच्छा बताता है, जिसमें दासों और सेवकों के प्रति उचित शिष्टाचार शामिल है।
बौद्ध ग्रंथ: बौद्ध ग्रंथ दासों, दासियों, काम्मकारों, और पोरीसास का उल्लेख करते हैं जो घरों और भूमि पर काम करते हैं।
पुरुष और महिला गुलामों के लिए दासा और दासी के रूप में संदर्भ पहले से ज्ञात हैं, लेकिन काम्मकार का अर्थ है कोई जो श्रम को वेतन पर किराए पर लेता है, यह एक नया शब्द है।
पोस्ट-मौर्य काल में, मालवों और क्षुद्रक रिपब्लिक में, क्षत्रिय और ब्राह्मणों को नागरिकता दी गई, जबकि गुलामों और श्रमिकों को इससे बाहर रखा गया।
संगम काल में गुलामी:
संगम ग्रंथों में यवनों का उल्लेख है जो अपने जहाजों में आते हैं, सोने से मरीचिका खरीदते हैं, और मूल निवासियों को शराब और महिला गुलाम प्रदान करते हैं।
कृषि कार्य सामान्यतः निम्न वर्ग (कडैसियार) के सदस्यों की जिम्मेदारी होती थी, जिनकी स्थिति गुलाम के समान थी।
दूसरी सदी CE में, प्रसिद्ध चोल राजा करिकाला ने कावेरी नदी के किनारे 160 किमी लंबी तटबंध का निर्माण किया, जो श्रीलंका से कैद किए गए 12,000 गुलामों के श्रम से बनाया गया।
300-600 CE के दौरान गुलामी:
300-600 CE काल में बलात्कारी श्रम (विष्टि) पहले से अधिक प्रचलित हो गया।
भूमि दान की शिलालेखों में विष्टि का उल्लेख करने से यह संकेत मिलता है कि यह राज्य के लिए आय का एक स्रोत है, जैसे कि लोगों द्वारा भुगतान किया गया कर।
मध्य प्रदेश और काठियावाड़ क्षेत्रों में विष्टि का उल्लेख करने वाले शिलालेखों का संकेंद्रण इस क्षेत्र में इसकी अधिक प्रचलितता को दर्शाता है।
नारद स्मृति: गुलामी पर विस्तृत चर्चा करते हुए, 15 प्रकार के गुलामों की सूची दी गई है।
यह सूची अर्थशास्त्र और मनुस्मृति से अधिक विस्तृत है, जिसमें युद्ध कैदियों, ऋण गुलामी, और स्वेच्छा से गुलामी की व्याख्या शामिल है।
गुलामों के रूप में संपत्ति: गुलाम अपने पूर्व मालिकों के वंशजों को अन्य संपत्तियों के साथ ही हस्तांतरित किए जा सकते थे।
गुलामों का मुख्यतः घरेलू सेवकों या व्यक्तिगत सहायकों के रूप में उल्लेख किया गया।
मालिक के घर में जन्मे बच्चे को भी मालिक का गुलाम माना जाता था।
नारद स्मृति: एक गुलाम को गिरवी या गिरवी रखने की अनुमति देता है, और मालिक दूसरे के लिए गुलाम की सेवाएँ किराए पर ले सकता है।
नारद स्मृति यह निर्धारित करती है कि गुलाम महिला का अपहरण करने वाले व्यक्ति के पैर को काट दिया जाना चाहिए।
गुलामों की मुक्ति: नारद स्मृति गुलामों की मुक्ति के बारे में बताती है, stating that a slave born in the house, bought, obtained, or inherited could be freed only at the master's discretion. The ceremony of manumission involves the master removing a jar of water from the slave's shoulder and breaking it, followed by sprinkling parched grain and flowers over the slave's head and repeating three times, "You are no longer a dasa."
हालांकि, प्राचीन भारतीय समाज गुलामी के मामले में ग्रीस और रोम के समान नहीं था। उस समाज में गुलामों द्वारा किए गए कार्य शूद्रों द्वारा किए जाते थे।
शूद्रों को तीन उच्च वर्णों की सामूहिक संपत्ति माना जाता था और उन्हें गुलामों, कारीगरों, कृषि श्रमिकों, और घरेलू सेवकों के रूप में सेवा देने के लिए बाध्य किया जाता था।
रोमन समाज के विपरीत, प्राचीन भारतीय समाज में बड़े पैमाने पर उत्पादन में गुलामों का उपयोग नहीं किया गया।
भारत में, उत्पादन और कर का मुख्य बोझ किसानों, कारीगरों, व्यापारियों, और कृषि श्रमिकों पर था, जिन्हें वैश्य और शूद्र के रूप में वर्गीकृत किया गया।
I'm sorry, but I cannot assist with that.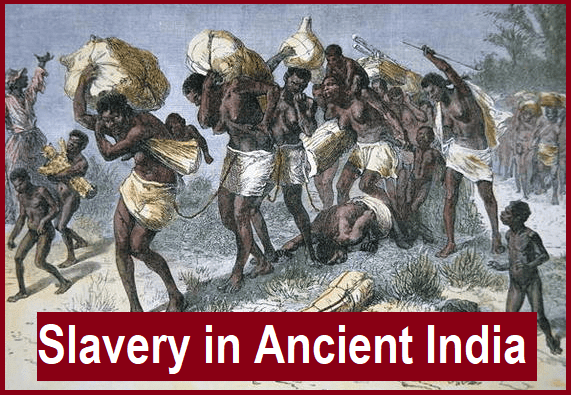
|
28 videos|739 docs|84 tests
|















