1833 और 1855 का चार्टर अधिनियम | इतिहास वैकल्पिक UPSC (नोट्स) PDF Download
चार्टर अधिनियम 1833 का परिचय
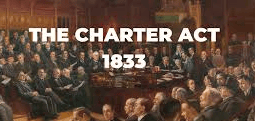
- भारत सरकार अधिनियम 1833, जिसे सेंट हेलेना अधिनियम 1833 या चार्टर अधिनियम 1833 के नाम से भी जाना जाता है, यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित किया गया।
- इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को संचालन के लिए 20 और वर्षों की अनुमति दी, लेकिन इसके साथ महत्वपूर्ण परिवर्तन भी किए गए।
- कंपनी को अब व्यावसायिक कार्यों में संलग्न होने की अनुमति नहीं थी और इसे केवल शासन पर ध्यान केंद्रित करना था।
- चार्टर नवीनीकरण के साथ यह शर्त थी कि कंपनी सभी व्यापार, भारत और चीन सहित, को छोड़ दे और यूरोपीय लोगों को भारत में स्वतंत्र रूप से बसने की अनुमति दे।
- यह अधिनियम पहली बार भारतीयों के लिए न्यायिक पदों को खोलता है और कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए एक कानून आयोग स्थापित करता है।
पृष्ठभूमि:
- चार्टर अधिनियम 1813, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को 20 वर्षों के लिए नवीनीकरण किया, 1833 में समाप्त हो गया।
- 1813 और 1833 के चार्टर अधिनियमों के बीच 20 वर्षों में, इंग्लैंड ने औद्योगिक क्रांति के कारण महत्वपूर्ण परिवर्तनों का सामना किया।
- औद्योगिक क्रांति ने सस्ते सामानों का उत्पादन किया, जिन्हें विदेशों में निर्यात किया गया, जिससे लोगों के दृष्टिकोण में व्यापकता आई।
- एक नई बुद्धिजीवी वर्ग उभरा जिसने श्रमिकों के अधिकारों के लिए वकालत की।
- 1830 में, व्हिग्स (बाद में लिबरल पार्टी) सत्ता में आए, जिन्होंने उदार सिद्धांतों और मानवाधिकारों को बढ़ावा दिया।
- ब्रिटेन में राजनीतिक वातावरण सुधार उत्साह से भरा हुआ था, विशेष रूप से 1832 के सुधार अधिनियम के बाद।
- इन सुधारवादी और उदार विचारों के बीच, संसद को 1833 में कंपनी के चार्टर की समीक्षा करने का कार्य सौंपा गया।
- ब्रिटेन में कंपनी को समाप्त करने और भारतीय प्रशासन को सीधे सरकार को सौंपने की बढ़ती मांग थी।
- इस अशांति के बावजूद, एक संसदीय जांच ने भारत में कंपनी के शासन को एक अलग ढांचे के तहत जारी रखने की सिफारिश की।
- 1833 का अधिनियम, जो मैकॉले और जेम्स मिल जैसे व्यक्तियों द्वारा प्रभावित था, भारत के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण बिंदु को चिह्नित करता है।
- मैकॉले, जो नियंत्रण बोर्ड के सचिव थे, और जेम्स मिल, जो भारत हाउस में बेंथम के अनुयायी थे, ने चार्टर अधिनियम 1833 पर गहरा प्रभाव डाला।
चार्टर अधिनियम 1833 की प्रावधान
भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश: 1813 का चार्टर अधिनियम भारत में ब्रिटिश उपनिवेशीकरण को वैधता प्रदान करता है, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी क्षेत्रीय संपत्तियों का शासन “उसके महाराज के लिए ट्रस्ट में” भारत सरकार के लाभ के लिए करने की अनुमति मिली।
- यह अधिनियम कंपनी को एक वाणिज्यिक इकाई से एक प्रशासनिक निकाय में परिवर्तित करता है, जिससे इसे चीन और चाय व्यापार में अपने एकाधिकार से वंचित किया जाता है।
- कंपनी को अब केवल राजनीतिक कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, जो अपने भारतीय संपत्तियों को ब्रिटिश क्राउन के लिए ट्रस्ट में रखती थी।
- अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर-जनरल को भारत के गवर्नर-जनरल के रूप में पुनर्परिभाषित किया, जो सीधे ब्रिटिश शासन की शुरुआत को दर्शाता है।
- लॉर्ड विलियम बेंटिंक ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर-जनरल बने, जिन्होंने पूरे देश में नागरिक, सैन्य, और राजस्व मामलों का पर्यवेक्षण किया।
- गवर्नर-जनरल इन काउंसिल को भारत में सभी ब्रिटिश क्षेत्रों के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया, जिससे सभी व्यक्तियों, ब्रिटिश या भारतीय के लिए समान कानून सुनिश्चित किया गया।
- राजस्व और व्यय पर केंद्रीय नियंत्रण स्थापित किया गया, जिससे गवर्नर-जनरल इन काउंसिल में वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का केंद्रीकरण हुआ।
- गवर्नर-जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या चार निर्धारित की गई, जिसमें चौथे सदस्य की भूमिका पर विशेष सीमाएँ थीं, जो केवल विधायी कार्यों में भाग ले सकते थे।
लॉर्ड मैकॉले की कानून सदस्य के रूप में नियुक्ति:
- लॉर्ड मैकॉले चौथे व्यक्ति थे जिन्हें परिषद के कानून सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया।
प्रशासनिक शीर्षक में परिवर्तन:
- नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष को भारतीय मामलों के मंत्री के रूप में नामित किया गया।
- बोर्ड को भारत में सभी प्रशासनिक मामलों की निगरानी करने का अधिकार दिया गया।
आव्रजन और भूमि अधिग्रहण:
- भारत में यूरोपीय प्रवासन और यूरोपीय लोगों द्वारा भूमि और संपत्ति के अधिग्रहण पर लगाए गए प्रतिबंध पूरी तरह से हटा दिए गए। इस अधिनियम ने भारत में यूरोपीयों द्वारा उपनिवेशीकरण पर कानूनी बाधा को समाप्त कर दिया।
बंगाल प्रेसीडेंसी में विभाजन:
- 1833 का चार्टर अधिनियम बंगाल प्रेसीडेंसी को दो प्रेसीडेंसियों में विभाजित करने का प्रस्तावित था: फोर्ट विलियम प्रेसीडेंसी और आगरा प्रेसीडेंसी। हालांकि, यह प्रावधान कभी लागू नहीं हुआ और बाद में निलंबित कर दिया गया।
भारत के गवर्नर-जनरल की शक्तियों में वृद्धि:
- गवर्नर-जनरल को ब्रिटिश भारत के लिए सभी विधायी शक्तियाँ दी गईं। गवर्नर-जनरल-इन-काउंसिल किसी भी कानून या विनियम को निरस्त, संशोधित या परिवर्तित कर सकता था जो ब्रिटिश क्षेत्र में सभी व्यक्तियों, स्थानों और वस्तुओं पर लागू होता था। निदेशकों की कोर्ट किसी भी कानून को वेटो कर सकती थी जो गवर्नर-जनरल-इन-काउंसिल द्वारा बनाए गए थे।
कानूनों का संहिताबद्ध करना:
- 1833 का चार्टर अधिनियम भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने का लक्ष्य रखता था। भारत में बनाए गए सभी कानूनों को ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना था और इन्हें अधिनियम के रूप में जाना जाता था। इस अधिनियम ने गवर्नर-जनरल को भारतीय कानून आयोगों की नियुक्ति की अनुमति दी ताकि वे भारत में विभिन्न नियमों और विनियमों का अध्ययन और संहिताबद्ध कर सकें।
पहला भारतीय कानून आयोग:
- 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा स्थापित, जिसमें लॉर्ड मैकौले अध्यक्ष थे। आयोग को न्यायालयों, पुलिस प्रतिष्ठानों, न्यायिक प्रक्रियाओं और कानूनों के अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और नियमों की जांच करने का कार्य सौंपा गया था। आयोग की रिपोर्ट गवर्नर-जनरल-इन-काउंसिल को प्रस्तुत की जानी थी और इसे ब्रिटिश संसद के समक्ष रखा जाना था।
कोडों का कार्यान्वयन:
कानून आयोग ने 1837 तक अपने संहिताकरण कार्य को पूरा कर लिया, लेकिन पूर्ण कार्यान्वयन 1857 के विद्रोह के बाद हुआ। नागरिक प्रक्रिया संहिता 1859 में, भारतीय दंड संहिता 1860 में, और आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1862 में पेश की गई। इन संहिताओं का उद्देश्य वैश्विक न्यायशास्त्र के सिद्धांतों की स्थापना करना था।
भारतीय सरकारी सेवा में:
- 1833 के चार्टर अधिनियम के सेक्शन 87 ने यह घोषित किया कि सरकारी सेवाओं में नियुक्ति का आधार योग्यता होगी, न कि धर्म, जन्मस्थान या जाति।
- यह पहला अधिनियम था जिसने भारत के निवासियों को प्रशासन में भाग लेने की अनुमति दी।
- हालांकि कंपनी की सेवाएं निवासियों के लिए खोली गईं, लेकिन उनकी नियुक्ति के लिए कोई प्रावधान नहीं था।
- अधिनियम ने नागरिक सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की प्रणाली लाने का प्रयास किया।
नागरिक सेवकों के लिए प्रतियोगिता:
- खुली प्रतियोगिता का प्रावधान निदेशक मंडल द्वारा अस्वीकृत किया गया, जिन्होंने कंपनी के अधिकारियों की नियुक्ति के विशेषाधिकार को बनाए रखा।
- प्रतियोगिता केवल निदेशकों द्वारा नामांकित उम्मीदवारों तक सीमित थी, जो स्थिति में सुधार नहीं कर सकी।
- अंततः, 1853 का चार्टर अधिनियम नागरिक सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता की स्थापना करता है, जिसमें परीक्षा के माध्यम से सभी जन्मजात विषयों की भर्ती की जाती है।
दासता का निवारण:
- इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल-इन-काउंसिल को भारत में मौजूद दासता की स्थिति को कम करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया।
- हालांकि ब्रिटेन में 1820 में दासता को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन भारत में उपनिवेशीय प्रशासक विभिन्न रूपों में इसके अस्तित्व को खोजते रहे।
- अंततः, 1843 के अधिनियम V के साथ, भारत में दासता समाप्त कर दी गई।
- गवर्नर जनरल-इन-काउंसिल को नए कानूनों का मसौदा तैयार करते समय विवाह, परिवार के मुखिया के अधिकारों और प्राधिकारों से संबंधित कानूनों पर विचार करने का भी कार्य सौंपा गया।
और बिशप:
भारत में ब्रिटिश निवासियों की संख्या बढ़ने के साथ, 1833 का चार्टर अधिनियम ने भारत में ईसाई संस्थानों की स्थापना को नियंत्रित किया, और बिशपों की संख्या को तीन तक बढ़ा दिया।
1833 के अधिनियम का महत्व
- 1833 का अधिनियम भारत के संविधान में महत्वपूर्ण और दूरगामी परिवर्तन लाया।
- कंपनी को भारत में चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर अपने एकाधिकार से मुक्त किया गया, जो 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा प्रारंभ किए गए कार्य को पूरा करता है।
- व्यापारिक विशेषाधिकार खोने के बाद, कंपनी अब प्रशासन पर ध्यान केंद्रित कर सकती थी।
- कानून के संहिताकरण का प्रावधान महत्वपूर्ण था।
- 1833 से पहले, कानून इतने दोषपूर्ण थे कि यह अक्सर निर्धारित करना असंभव था कि कानून क्या था।
- भारत में लागू कानूनों के विभिन्न प्रकार थे, जिससे यह तय करना कठिन था कि विशिष्ट मामलों में कौन सा कानून लागू होता है।
- अधिनियम के प्रावधानों में गुलामी का उन्मूलन और सभी धर्मों, जन्मस्थान, वंश या रंग के लोगों के लिए भारत में सेवाओं का उद्घाटन शामिल था, जो प्रशंसनीय थे।
धन का प्रवाह:
- भारतीय सरकार ने कंपनी के ऋणों को अपने ऊपर ले लिया, सहमति दी कि अगले 40 वर्षों के लिए भारतीय राजस्व से शेयरधारकों को उनके पूंजी पर 10.5% लाभांश का भुगतान किया जाएगा।
- इससे भारत का बोझ बढ़ गया और यह धन के प्रवाह का एक महत्वपूर्ण पहलू बन गया।
1853 का चार्टर अधिनियम
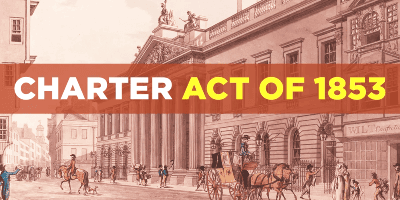
- भारत में कंपनी के शासन को समाप्त करने की बढ़ती मांग थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार अभी भी आश्वस्त नहीं थी।
- कंपनी के चार्टर के नवीनीकरण के समय के करीब आते ही, इंग्लैंड में कंपनी की डबल गवर्नमेंट को समाप्त करने की मांग बढ़ी।
- यह मांग इसलिए उठी क्योंकि: (i) निर्देशक मंडल को अब उपयोगी नहीं समझा जा रहा था। (ii) निर्देशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड की उपस्थिति अनावश्यक देरी और अतिरिक्त लागत का कारण बन रही थी।
- 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा स्थापित विधायी ढांचे की adequacy पर चिंता व्यक्त की गई।
- बंगाल के पक्ष में पक्षपाती होने से बचने के लिए भारत के गवर्नर-जनरल और बंगाल के गवर्नर के कार्यों को अलग करने की मांग की गई।
- 1833 के चार्टर अधिनियम के बाद से महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और राजनीतिक परिवर्तन हुए, जिसमें: (i) 1843 और 1849 में सिंध और पंजाब को कंपनी के क्षेत्रों में शामिल किया गया। (ii) लॉर्ड डलहौसी की नीतियों के तहत कई भारतीय राज्यों का अधिग्रहण। (iii) नए अधिग्रहित क्षेत्रों के लिए संविधान में प्रावधान की आवश्यकता।
- शक्तियों का विकेंद्रीकरण और भारतीयों को अपने मामलों के प्रबंधन में शामिल करने की मांग भी थी, जिसे इंग्लैंड में कुछ समर्थन मिला।
- इन परिस्थितियों में, ब्रिटिश संसद से 1853 में कंपनी के चार्टर को नवीनीकरण के लिए बुलाया गया।
1853 के चार्टर अधिनियम के प्रावधान
- 1833 का चार्टर 1853 में नवीनीकरण किया गया, लेकिन अगले बीस वर्षों के लिए नहीं।
- कंपनी को अपने भारतीय संपत्तियों को "उनकी महारानी, उनके उत्तराधिकारियों और उत्तराधिकारियों के लिए ट्रस्ट में रखना" की अनुमति दी गई, जिससे भविष्य में अधिग्रहण की संभावना खुली रही।
- अधिनियम ने निर्धारित किया कि ब्रिटिश सरकार नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों, उसके सचिव और अन्य अधिकारियों के वेतन निर्धारित करेगी, लेकिन ये वेतन कंपनी द्वारा दिए जाएंगे।
- न्यायालय के निदेशकों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिसमें 6 सदस्य क्राउन द्वारा नामित किए गए।
- अधिनियम ने गवर्नर-जनरल की परिषद के कार्यकारी और विधायी कार्यों को अलग किया, विधायी उद्देश्यों के लिए नए सदस्यों को जोड़ा।
- कानून सदस्य को गवर्नर-जनरल की कार्यकारी परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया।
- विधायी परिषद का विस्तार किया गया, जिसमें छह सदस्य जोड़े गए: (i) कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और एक पुइसने न्यायाधीश। (ii) बंगाल, मद्रास, बंबई और उत्तर पश्चिम प्रांतों से चार प्रतिनिधि, सभी सिविल सेवक जिनकी सेवा का अवधि कम से कम दस वर्ष हो।
- गवर्नर-जनरल परिषद में दो अतिरिक्त सिविल सेवकों की नियुक्ति कर सकता था, हालांकि यह शक्ति शायद ही कभी उपयोग की जाती थी।
- परिषद की प्रक्रियाएं ब्रिटिश संसद के मॉडल पर आधारित थीं, जिसमें मौखिक चर्चाओं और विधायी कार्यों के लिए चयनित समितियों का उपयोग करने की अनुमति थी।
- कंपनी का नियुक्तियों पर नियंत्रण प्रतिस्पर्धात्मक भर्ती को लागू करके कम किया गया।
- (i) न्यायालय के निदेशकों ने अपनी संरक्षण शक्ति खो दी क्योंकि सेवाएं बिना भेदभाव के प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिए खोली गईं।
- (ii) 1854 में मैकॉले की अध्यक्षता में एक समिति इस योजना को लागू करने के लिए स्थापित की गई।
- न्यायालय के निदेशकों को नए प्रेसीडेंसी बनाने या मौजूदा प्रेसीडेंसी को नए अधिग्रहित क्षेत्रों को शामिल करने के लिए संशोधित करने की शक्ति दी गई।
- (i) इस शक्ति का उपयोग 1859 में पंजाब के लिए एक अलग लेफ्टिनेंट-गवर्नरशिप स्थापित करने के लिए किया गया।
- (ii) अधिनियम ने क्राउन को इंग्लैंड में एक कानून आयोग नियुक्त करने की अनुमति भी दी, जो भारतीय कानून आयोग की रिपोर्टों और ड्राफ्टों की समीक्षा करेगा, जो पहले ही भंग हो चुका था, और विधायी उपायों की सिफारिश करेगा।
अधिनियम का महत्व
नियंत्रण का नुकसान: ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो पहले ही अपने व्यावसायिक विशेषाधिकारों से वंचित हो चुकी थी, भारत में नीतियों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही थी।
1863 का अधिनियम: यह अधिनियम दो विरोधी दृष्टिकोणों के बीच एक समझौता था:
- कंपनी शासन के समर्थक: कुछ लोग चाहते थे कि कंपनी भारत में क्राउन के लिए ट्रस्ट के रूप में शासन करना जारी रखे।
- क्राउन नियंत्रण के समर्थक: अन्य लोग सीधे क्राउन नियंत्रण को प्राथमिकता देते थे, जो इस अधिनियम में परिलक्षित हुआ।
शासन में परिवर्तन: अधिनियम ने निदेशकों की संख्या को 24 से घटाकर 18 कर दिया, जिसमें से 6 क्राउन के नामित थे। यह परिवर्तन निर्णय लेने में क्राउन को अधिक प्रभाव देने के उद्देश्य से किया गया था।
विधायी परिषद की शक्ति: नवगठित विधायी परिषद ने कार्यकारी को चुनौती देना शुरू कर दिया, इसके कार्यों पर सवाल उठाते हुए और गोपनीय दस्तावेजों के साथ पारदर्शिता की मांग की।
विधायन की स्वतंत्रता: परिषद ने स्वतंत्र रूप से विधायन करने के अपने अधिकार का दावा किया, जिससे सर चार्ल्स वुड, अधिनियम के लेखक, चिंतित हो गए। उन्होंने स्पष्ट किया कि परिषद का उद्देश्य भारत में संवैधानिक संसद की शुरुआत नहीं थी।
अधिनियम का महत्व: अपनी कमियों के बावजूद, 1853 का अधिनियम 19वीं सदी का एक महत्वपूर्ण संवैधानिक उपाय था, मुख्यतः विधायी परिषद के कार्य करने के कारण।
भारतीयों का बहिष्कार: अधिनियम ने भारतीयों को विधायी प्रक्रिया से बाहर रखने की प्रक्रिया को जारी रखा, जो एक बड़ा नकारात्मक पहलू था।
|
28 videos|739 docs|84 tests
|















