भारत में पश्चिमी शिक्षा का परिचय | इतिहास वैकल्पिक UPSC (नोट्स) PDF Download
सर चार्ल्स वुड का शिक्षा पर डिस्पैच, 1854

- सर चार्ल्स वुड, ब्रिटेन के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष, ने अंग्रेजी नस्ल और संस्थानों की श्रेष्ठता में विश्वास किया, यह सोचते हुए कि वे दुनिया के लिए एक मॉडल के रूप में सेवा कर सकते हैं।
- 1854 में, वुड ने भारत में भविष्य की शिक्षा पर एक व्यापक डिस्पैच तैयार किया, जिसे देश में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया।
- इस डिस्पैच का उद्देश्य भारत भर में एक समन्वित शिक्षा प्रणाली स्थापित करना था।
मुख्य सिफारिशें
- पश्चिमी शिक्षा: डिस्पैच ने पश्चिमी शिक्षा के शिक्षण पर जोर दिया, जिसमें यूरोपीय कला, विज्ञान, दर्शन और साहित्य का प्रसार शामिल था।
- शिक्षण माध्यम: उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को सबसे अच्छा माध्यम माना गया, जबकि स्थानीय भाषाएँ यूरोपीय ज्ञान को जनसामान्य तक पहुँचाने के लिए महत्वपूर्ण थीं।
- शिक्षा प्रणाली के लिए प्रस्ताव:
- स्थानीय प्राथमिक विद्यालय: गाँवों में स्थानीय प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया गया।
- एंग्लो-वर्नाकुलर उच्च विद्यालय: इसके बाद एंग्लो-वर्नाकुलर उच्च विद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया।
- संलग्न कॉलेज: जिला स्तर पर संलग्न कॉलेजों की स्थापना का सुझाव दिया गया।
- अनुदान: शिक्षा में निजी उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान प्रणाली की सिफारिश की गई, जो योग्य शिक्षकों की नियुक्ति और शिक्षण मानकों को बनाए रखने की शर्त पर आधारित थी।
जन शिक्षा विभाग: प्रत्येक प्रांत में जन शिक्षा विभाग की स्थापना की सिफारिश की गई, जो शैक्षणिक प्रगति की समीक्षा करेगा और सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- विश्वविद्यालय: कोलकाता, मुंबई, और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित करने का सुझाव दिया गया, जो लंदन विश्वविद्यालय के मॉडल पर आधारित थे, ताकि परीक्षाएं आयोजित की जा सकें और डिग्रियाँ प्रदान की जा सकें।
- व्यावसायिक शिक्षा: व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया गया और तकनीकी विद्यालय और कॉलेज स्थापित करने की बात की गई।
- शिक्षकों के प्रशिक्षण संस्थान: अंग्रेजी मॉडल पर आधारित शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए संस्थानों की स्थापना की सिफारिश की गई।
- महिलाओं की शिक्षा: महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समर्थन व्यक्त किया गया।
- नई शिक्षा योजना अंग्रेजी मॉडलों की नकल थी, वुड के डेस्पैच से अधिकांश प्रस्ताव लागू किए गए।
क्रियान्वयन: 1855 में सार्वजनिक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई, जिसने पूर्व में सार्वजनिक शिक्षा समिति और शिक्षा परिषद का स्थान लिया।
1857 में कोलकाता, मद्रास, और मुंबई में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई।
बेथुन के प्रयासों के कारण, लड़कियों के विद्यालयों का आधुनिकीकरण किया गया और उन्हें सरकार की अनुदान-आधारित और निरीक्षण प्रणाली के तहत लाया गया।
प्रभुत्व और पश्चिमीकरण: वुड के डेस्पैच के आदर्श लगभग पांच दशकों तक हावी रहे, जिसमें भारत में शिक्षा प्रणाली का तेजी से पश्चिमीकरण हुआ।
स्वदेशी प्रणाली धीरे-धीरे पश्चिमी शिक्षा प्रणाली के प्रति समर्पित हो गई, जिसमें अधिकांश संस्थान यूरोपीय प्रमुखों और प्रिंसिपलों द्वारा शिक्षा विभाग के अधीन संचालित होते थे।
मिशनरी प्रयासों ने भी कई संस्थानों के प्रबंधन में भूमिका निभाई, धीरे-धीरे भारतीय निजी पहलों का विकास इस क्षेत्र में हुआ।
हंटर शिक्षा आयोग का गठन (1882-83)
- 1882 में, भारतीय सरकार ने W.W. Hunter के नेतृत्व में एक आयोग की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत में शिक्षा की स्थिति का आकलन करना था, जो 1854 के डेस्पैच के बाद की प्रगति पर विचार करता था। आयोग का गठन आंशिक रूप से इंग्लैंड में मिशनरी आलोचनाओं के जवाब में किया गया था, जिसमें कहा गया था कि भारत की शिक्षा प्रणाली वुड के डेस्पैच में निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन नहीं कर रही थी।
आयोग के उद्देश्यों:
- यह संकल्प आयोग को भारतीय शिक्षा को पुनर्गठित करने का कार्य सौंपता है ताकि विभिन्न शाखाएँ सार्वजनिक शिक्षा की अधिक समान रूप से और समान गति से प्रगति कर सकें।
- प्राथमिक ध्यान भारतीय साम्राज्य में प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति की जांच करना और इसे विस्तारित तथा सुधारने के तरीकों का अन्वेषण करना था।
- महत्वपूर्ण रूप से, आयोग को भारतीय विश्वविद्यालयों के समग्र कार्यप्रणाली का मूल्यांकन करने का कार्य नहीं सौंपा गया था।
ध्यान केंद्रित क्षेत्र:
- आयोग ने अपने प्रयासों और सिफारिशों को मुख्य रूप से माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा पर केंद्रित किया, विश्वविद्यालय स्तर को छोड़कर।
प्राथमिक शिक्षा:
- राज्य की प्राथमिक शिक्षा में सुधार और विस्तार के प्रति प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- प्राथमिक शिक्षा को जनसामान्य को उनकी मातृभाषा में उन विषयों पर शिक्षित करने के रूप में देखा जाना चाहिए जो उन्हें जीवन के लिए सबसे अच्छा तैयार करते हैं।
- शिक्षा में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया, लेकिन प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय समर्थन के बावजूद प्रदान किया जाना चाहिए।
- आयोग ने प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण नए जिला और नगरपालिका बोर्डों को सौंपने का सुझाव दिया, जो शिक्षा के वित्त पोषण के लिए कर लगा सकते हैं।
माध्यमिक शिक्षा:
- माध्यमिक शिक्षा के दो धारा होनी चाहिए:
- साहित्यिक शिक्षा जो छात्रों को विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षाओं के लिए तैयार करती है।
- व्यावहारिक शिक्षा जो वाणिज्यिक और व्यावसायिक करियर की ओर अग्रसर करती है।
निजी उद्यमों को प्रोत्साहन:
- आयोग ने शिक्षा में निजी पहलों का मजबूत समर्थन करने की सिफारिश की।
- इसे बढ़ावा देने के लिए, इसने अनुशंसा की:
- अनुदान प्रणाली का विस्तार और इसे अधिक लचीला बनाना।
- सहायता प्राप्त स्कूलों को सरकारी संस्थानों के समान स्थिति और लाभों के संदर्भ में मानना।
- सरकार को जितना संभव हो, माध्यमिक और महाविद्यालयीन शिक्षा के प्रत्यक्ष प्रबंधन से पीछे हटने की सलाह दी गई।
महिला शिक्षा:
- आयोग ने प्रमुख शहरों के बाहर महिला शिक्षा के लिए सुविधाओं की कमी को उजागर किया और इसके सुधार के लिए सुझाव दिए।
प्रभाव:
- आयोग की रिपोर्ट के बाद के बीस वर्षों में, माध्यमिक और महाविद्यालयीन शिक्षा में असाधारण वृद्धि और विस्तार हुआ।
- इस विस्तार का एक महत्वपूर्ण पहलू भारतीय परोपकारी गतिविधियों की भागीदारी थी।
- देश भर में कई पंथीय संस्थानों का उदय हुआ।
- भारतीय और ओरिएंटल अध्ययन में नई रुचि के साथ-साथ पश्चिमी ज्ञान की खोज भी बढ़ी।
- इस अवधि के दौरान एक अन्य महत्वपूर्ण विकास शिक्षण-उपयुक्त परीक्षा विश्वविद्यालयों की स्थापना थी।
- पंजाब विश्वविद्यालय 1882 में सर्वोच्च साहित्यिक, शिक्षण, परीक्षा निकाय के रूप में स्थापित हुआ।
- इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में स्थापित किया गया।
कर्ज़न की नीतियाँ और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1904
19वीं सदी की शुरुआत में शैक्षिक विवाद:
- 1800 के दशक की शुरुआत में राजनीतिक अशांति और शैक्षिक नीतियों पर बहसें बढ़ने लगीं।
- राजनीतिक बदलावों ने शैक्षिक विकास को प्रभावित किया और इसके विपरीत भी।
- अधिकारी मानते थे कि शैक्षिक विस्तार गलत दिशा में जा रहा है और गुणवत्ता निजी प्रबंधन के तहत गिर गई है।
- स्कूलों और कॉलेजों में व्यापक अनुशासनहीनता थी, जिसे राजनीतिक क्रांतिकारियों के लिए प्रजनन स्थल माना गया।
- नकारात्मक प्रवृत्तियों को जिम्मेदार निजी उद्यमों द्वारा बिना नियंत्रण के तेजी से विस्तार के लिए दोषी ठहराया गया।
- राष्ट्रीयतावादी दृष्टिकोण ने मानकों में गिरावट को स्वीकार किया, लेकिन तर्क किया कि सरकार निरक्षरता को प्रभावी ढंग से संबोधित करने में विफल रही है।
कर्ज़न के शैक्षिक सुधार:
- कर्ज़न, अपने प्रशासन में सुधार के लिए उत्साह के साथ, भारत में शिक्षा सुधारने का लक्ष्य रखते थे।
- उन्होंने अंग्रेज़ी मॉडल की अंधी नकल और मैकॉले की 'उल्टे पिरामिड' की गलती की आलोचना की, जो भारतीय भाषाओं के प्रति पक्षपाती थी।
- उन्होंने शिक्षकों की खराब गुणवत्ता को उजागर किया और परीक्षा-केंद्रित शिक्षा प्रणाली की आलोचना की।
- कर्ज़न के उद्देश्य मुख्यतः राजनीतिक थे, जबकि शैक्षिक चिंताएँ गौण थीं।
- उन्होंने गुणवत्ता और दक्षता के नाम पर शिक्षा पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाने का औचित्य बताया, लेकिन शिक्षा को सीमित करने और सरकार के प्रति वफादारी को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखा।
- राष्ट्रीयतावादियों ने कर्ज़न की नीतियों को साम्राज्यवाद को मजबूत करने और राष्ट्रीयता की भावनाओं को कमजोर करने के प्रयास के रूप में देखा।
1901 का शिमला सम्मेलन:
- सितंबर 1901 में, कर्ज़न ने भारत भर के उच्च शैक्षिक अधिकारियों और विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों के साथ शिमला में एक गोल मेज सम्मेलन बुलाया।
- सम्मेलन की शुरुआत वायसराय के भाषण से हुई, जिसने भारत के शैक्षिक परिदृश्य की समीक्षा की।
- उन्होंने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय जनता पर लागू करने के लिए एक नया शैक्षिक सुधार योजना बनाना नहीं था।
- हालांकि, बाद की घटनाओं ने इस दावे के पीछे की असत्यता को उजागर किया।
- सम्मेलन के परिणामस्वरूप शिक्षा के लगभग हर पहलू को कवर करने वाले 150 प्रस्तावों को अपनाया गया।
सर थॉमस रैलेघ आयोग:
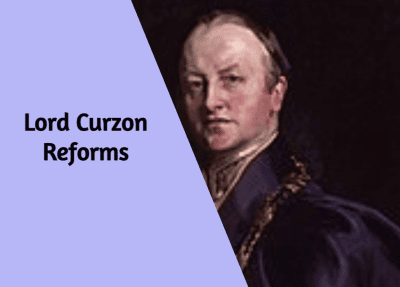
- शिमला सम्मेलन के बाद, 27 जनवरी 1902 को सर थॉमस रॉली की अध्यक्षता में एक आयोग स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य भारत में विश्वविद्यालयों की स्थिति और भविष्य की जांच करना और उनके ढांचे और संचालन में सुधार के लिए सुझाव देना था। आयोग को प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने की अनुमति नहीं थी। आयोग की रिपोर्ट और सिफारिशों के आधार पर, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित किया गया।
भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1904 के मुख्य प्रावधान:
- अध्ययन और अनुसंधान का प्रचार: विश्वविद्यालयों को अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देने, प्रोफेसरों और व्याख्याताओं की नियुक्ति करने, प्रयोगशालाएँ और पुस्तकालय स्थापित करने, और छात्रों को प्रत्यक्ष शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता थी।
- फेलोशिप नियम: किसी विश्वविद्यालय में फेलो की संख्या पचास से एक सौ के बीच होनी चाहिए, और फेलो को जीवन भर के बजाय छह वर्ष की अवधि के लिए सेवा करनी थी।
- सरकारी नामांकन: अधिकांश फेलो को सरकार द्वारा नामांकित किया जाना था। कोलकाता, मद्रास, और बंबई विश्वविद्यालयों में निर्वाचित पदों की संख्या प्रत्येक में बीस निर्धारित की गई, जबकि अन्य विश्वविद्यालयों में पंद्रह।
- सरकारी नियंत्रण में वृद्धि: इस अधिनियम ने विश्वविद्यालयों पर गवर्नर के नियंत्रण को बढ़ा दिया, जिससे सरकार को विश्वविद्यालय की सेनेट द्वारा पारित नियमों को निरस्त करने की अनुमति मिली। सरकार नियमों को संशोधित या नए नियम बनाने की भी अनुमति रखती थी।
- निजी कॉलेजों पर नियंत्रण: अधिनियम ने निजी कॉलेजों पर विश्वविद्यालय के नियंत्रण को मजबूत किया, जिसमें संबद्धता के लिए कठोर शर्तें लगाई गईं और सिंडिकेट द्वारा समय-समय पर निरीक्षण की आवश्यकता थी। निजी कॉलेजों को उचित दक्षता मानक बनाए रखना था, और संबद्धता या असंबद्धता के लिए सरकार की स्वीकृति आवश्यक थी।
- क्षेत्रीय और संबद्धता शक्तियाँ: गवर्नर जनरल इन काउंसिल को विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमाओं को परिभाषित करने और कॉलेजों की विश्वविद्यालयों के साथ संबद्धता को निर्धारित करने का अधिकार दिया गया।
इस उपाय के खिलाफ विरोध:
- राष्ट्रीयता के विचार, जो विधायी परिषद के भीतर और बाहर थे, ने इस उपाय का विरोध किया। श्री जी. के. गोखले ने इस विधेयक की आलोचना करते हुए इसे “प्रतिगामी उपाय” कहा, यह तर्क करते हुए कि यह शिक्षित वर्गों पर अन्यायपूर्ण आरोप लगाता है और “विशेषज्ञों के संकीर्ण, कट्टरपंथी, सस्ते शासन” को स्थायी बनाने का प्रयास करता है। 1917 की सैडलर आयोग ने नोट किया कि 1904 का अधिनियम भारतीय विश्वविद्यालयों को विश्व के सबसे सरकारी विश्वविद्यालयों में से एक बना दिया। भारतीय राय का मानना था कि कर्ज़न का उद्देश्य विश्वविद्यालयों को राज्य विभागों के स्तर पर लाना और शिक्षा में निजी उद्यम के विकास को कमजोर करना था।
कर्ज़न की नीति का सकारात्मक परिणाम:
- आलोचनाओं के बावजूद, कर्ज़न की नीति का एक सकारात्मक परिणाम यह था कि 1902 में उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालयों को सुधारने के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपये की अनुदान राशि की स्वीकृति दी गई। यह उच्च शिक्षा के लिए स्थायी सरकारी अनुदानों की शुरुआत थी।
शिक्षा नीति पर सरकार का प्रस्ताव, 21 फरवरी 1913:
- 1906 में, प्रगतिशील राज्य बारोडा ने अपने क्षेत्र में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू की। राष्ट्रीयता की भावना ने यह सवाल उठाया कि भारत सरकार ब्रिटिश भारत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को लागू क्यों नहीं कर सकती। 1910 से 1913 के बीच, जी. के. गोखले ने विधायी परिषद में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के प्रति सरकार की जिम्मेदारी के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए। 21 फरवरी 1913 के प्रस्ताव में, भारत सरकार ने अनिवार्य शिक्षा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया लेकिन निरक्षरता उन्मूलन के लक्ष्य को स्वीकार किया। सरकार ने प्रांतीय अधिकारियों को गरीब और वंचित समुदायों के लिए मुफ्त प्राथमिक शिक्षा को तेजी से लागू करने का आग्रह किया। इस संदर्भ में निजी पहलों को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया गया। माध्यमिक शिक्षा के संबंध में, प्रस्ताव ने स्कूलों की गुणवत्ता को सुधारने की आवश्यकता को उजागर किया। विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध में, यह कहा गया कि प्रत्येक प्रांत में एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना चाहिए, जिसमें इन विश्वविद्यालयों की शिक्षण गतिविधियों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया।
सैडलर विश्वविद्यालय आयोग (1917-1919)
सैडलर विश्वविद्यालय आयोग (1917-1919)
- 1917 में, भारतीय सरकार ने कोलकाता विश्वविद्यालय द्वारा सामना की जा रही समस्याओं की जांच के लिए एक आयोग स्थापित किया।
- डॉ. एम.ई. सैडलर, लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति, ने इस आयोग की अध्यक्षता की, जिसमें भारतीय सदस्य जैसे सर आसुतोष मुखर्जी और डॉ. जियाउद्दीन अहमद शामिल थे।
- पिछले आयोगों के विपरीत, जो शिक्षा के विशिष्ट पहलुओं पर केंद्रित थे, सैडलर आयोग ने स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक पूरी शिक्षा प्रणाली पर ध्यान केंद्रित किया।
- आयोग का मानना था कि विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए माध्यमिक शिक्षा में सुधार करना महत्वपूर्ण है।
- हालांकि यह कोलकाता विश्वविद्यालय पर केंद्रित था, आयोग की सिफारिशें अन्य भारतीय विश्वविद्यालयों के लिए भी प्रासंगिक थीं।
मुख्य सिफारिशें:
- सैडलर आयोग ने जोर दिया कि उच्च शिक्षा में महत्वपूर्ण परिवर्तन केवल माध्यमिक शिक्षा में सुधार के साथ ही संभव हो सकते हैं।
- इसने सिफारिश की कि माध्यमिक और विश्वविद्यालय शिक्षा के बीच विभाजन इंटरमीडिएट परीक्षा पर होना चाहिए, न कि मैट्रिकुलेशन पर।
- आयोग ने कला, विज्ञान, इंजीनियरिंग, और औद्योगिक शिक्षा में पाठ्यक्रम के साथ इंटरमीडिएट कॉलेजों की स्थापना का प्रस्ताव दिया।
- छात्रों को इंटरमीडिएट परीक्षा पास करने के बाद विश्वविद्यालय में प्रवेश करना चाहिए, इसके बाद तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम होना चाहिए।
- अधिक सक्षम छात्रों के लिए सम्मानित पाठ्यक्रम (Honours courses) प्रदान करने का सुझाव दिया गया, जो पास पाठ्यक्रमों से भिन्न थे।
- माध्यमिक शिक्षा की देखरेख के लिए एक बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन की सिफारिश की गई।
- आयोग ने विश्वविद्यालय के नियमों में अधिक लचीलापन और भारतीय विश्वविद्यालयों के बीच समन्वय के लिए एक इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना की सलाह दी।
- स्वायत्त संस्थानों और केंद्रीकृत आवासीय-शिक्षण विश्वविद्यालयों का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहन दिया गया।
- महिलाओं की शिक्षा को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देने का सुझाव दिया गया, जिसमें कोलकाता विश्वविद्यालय में महिला शिक्षा के लिए एक विशेष बोर्ड की स्थापना शामिल थी।
- शिक्षक प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं और कोलकाता और ढाका विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभाग की स्थापना की सिफारिश की गई।
- आयोग ने केंद्रीकृत एकात्मक शिक्षण स्वायत्त निकायों की वकालत की, जिसमें ढाका में एक एकात्मक शिक्षण विश्वविद्यालय शामिल था, ताकि कोलकाता विश्वविद्यालय पर छात्रों का बोझ कम किया जा सके।
- इसने कस्बों में कॉलेजों के विकास और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नए विश्वविद्यालय केंद्रों की स्थापना की भी सिफारिश की।
इसका प्रभाव:
विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई। सैड्लर विश्वविद्यालय आयोग द्वारा सुझाए गए नए विश्वविद्यालयों की स्थापना पटना, उस्मानिया, आलिगढ़, ढाका, लखनऊ, दिल्ली, आगरा, नागपुर, हैदराबाद, अन्नामलाई जैसे शहरों में की गई। 1930 तक, विश्वविद्यालयों की संख्या 30 हो गई।
- विश्वविद्यालयों में शिक्षण गतिविधियों की शुरुआत की गई।
- भारत के पहले तीन विश्वविद्यालय—कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास—ने संबद्धता, परीक्षा, डिग्री प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया।
- डिग्री कॉलेजों की जिम्मेदारी शिक्षण पर थी, पोस्टग्रेजुएट शिक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं था।
- आयोग की सिफारिशों के बाद, शिक्षण और आवासीय विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई, जिसमें अधिकांश नए स्थापित विश्वविद्यालय शिक्षण विश्वविद्यालय थे।
- सम्मान पाठ्यक्रमों की शुरूआत के साथ विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शैक्षणिक गतिविधियों में वृद्धि हुई।
- विभिन्न भारतीय भाषाओं में अध्ययन की शुरुआत की गई और उच्च अध्ययन तथा अनुसंधान के लिए सुविधाएं बनाई गई।
- विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर का पद स्थापित किया गया और शैक्षणिक दृष्टिकोण को विस्तारित करने के लिए विदेशों से विद्वान को आमंत्रित किया गया।
- कलकत्ता और ढाका विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभाग खोले गए।
- विश्वविद्यालयों के आंतरिक प्रशासन में सुधार के लिए विश्वविद्यालय अदालतें और कार्यकारी परिषदें बनाई गईं, जिससे पूर्व की सेनेट और सिंडिकेट का स्थान लिया गया।
- पाठ्यक्रम निर्माण, परीक्षा, अनुसंधान जैसे शैक्षणिक मामलों के लिए अकादमिक परिषद का गठन किया गया, जिससे शैक्षणिक मानकों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ।
- 1925 में विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों के बीच समन्वय के लिए इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड स्थापित किया गया।
- छात्र कल्याण के लिए प्रावधानों की शुरुआत की गई, जिससे विश्वविद्यालयों का ध्यान इस पहलू पर पहली बार आकर्षित हुआ, और प्रत्येक विश्वविद्यालय में छात्र कल्याण बोर्ड का गठन किया गया।
- 1920 में, भारत सरकार ने सैड्लर रिपोर्ट को प्रांतीय सरकारों को अनुशंसा की।
डायार्की के तहत शिक्षा (1921-37)
- 1919 के मोंटागू-चेल्म्सफोर्ड सुधारों के बाद, शिक्षा विभाग का नियंत्रण प्रांतीय निर्वाचित मंत्रियों को सौंप दिया गया। केंद्र सरकार ने शैक्षणिक मामलों में अपनी सीधी भागीदारी को कम कर दिया, शिक्षा विभाग को अन्य विभागों के साथ मिला दिया। 1902 से प्रदान किए जा रहे केंद्र के विशेष अनुदान शिक्षा के लिए बंद कर दिए गए। वित्तीय सीमाओं ने प्रांतीय सरकारों की महत्वाकांक्षी शैक्षणिक विस्तार या सुधार योजनाओं को लागू करने की क्षमता को सीमित कर दिया। इन चुनौतियों के बावजूद, शिक्षा में महत्वपूर्ण विस्तार हुआ, जो मुख्य रूप से धर्मार्थ प्रयासों द्वारा प्रेरित था।
हार्टोग समिति, 1929
भारत में शिक्षा पर हार्टोग समिति:
भारतीय वैधानिक आयोग द्वारा स्थापित हार्टोग समिति ने भारत में शिक्षा की स्थिति का अध्ययन किया और कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले:
शैक्षणिक गुणवत्ता में गिरावट:
- शैक्षणिक संस्थानों की संख्या में तेजी से वृद्धि ने गुणवत्ता में गिरावट और मानकों में कमी का कारण बना। शैक्षणिक प्रणाली को लेकर व्यापक असंतोष था।
- समिति ने प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय महत्व पर जोर दिया। इसने प्राथमिक शिक्षा के तेजी से विस्तार और इसे अनिवार्य बनाने के प्रयास की आलोचना की। इसके बजाय, समिति ने मौजूदा प्राथमिक शिक्षा सुविधाओं के समेकन और सुधार पर ध्यान केंद्रित करने की सिफारिश की।
- समिति ने noted किया कि माध्यमिक शिक्षा प्रणाली पर मैट्रिक परीक्षा का भारी प्रभाव था, जिसे कई छात्रों ने विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए मुख्य मार्ग के रूप में देखा। इसने माध्यमिक शिक्षा के लिए एक चयनात्मक प्रवेश प्रणाली की सिफारिश की, सुझाव दिया कि ग्रामीण व्यवसायों के लिए नियत छात्रों को मध्य स्थानीय स्कूलों में रहना चाहिए। मध्य स्तर के बाद के छात्रों के लिए, समिति ने औद्योगिक और वाणिज्यिक करियर की ओर ले जाने वाले पाठ्यक्रमों की विविधता को प्रस्तावित किया।
विश्वविद्यालय शिक्षा:
- समिति ने विश्वविद्यालय शिक्षा की कमजोरियों की आलोचना की, विशेष रूप से बिना चयन के प्रवेश नीति की, जिसने मानकों में गिरावट में योगदान दिया। इसने विश्वविद्यालय शिक्षा को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करने की सिफारिश की, यह सुनिश्चित करते हुए कि विश्वविद्यालय केवल उन छात्रों को उन्नत शिक्षा प्रदान करें जो योग्य और सक्षम हैं। समिति ने जोर देकर कहा कि विश्वविद्यालयों को उच्च गुणवत्ता वाली उन्नत शिक्षा प्रदान करने के अपने मुख्य कार्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
वार्धा योजना
- भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतीय स्वायत्तता पेश की, जिसके परिणामस्वरूप 1937 में लोकप्रिय मंत्रालयों की स्थापना हुई।
- कांग्रेस पार्टी ने सात प्रांतों में सत्ता हासिल की।
- 1937 में, कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना विकसित करना शुरू किया।
- महात्मा गांधी ने अपने पत्र 'हरिजन' में वार्धा योजना की प्रस्तावना दी।
- मूल शिक्षा का मुख्य सिद्धांत 'गतिविधि के माध्यम से सीखना' है।
- जाकिर हुसैन समिति ने योजना का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया, विभिन्न शिल्पों के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार किए और शिक्षक प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण, परीक्षा, प्रशासन पर सिफारिशें कीं।
- योजना ने 'हाथ से उत्पादक कार्य' पर ध्यान केंद्रित किया और छात्रों की मातृभाषा में सात वर्षीय पाठ्यक्रम का प्रस्ताव दिया।
- द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत (1939) और कांग्रेस मंत्रालयों के इस्तीफे ने योजना में देरी की।
सरजेंट योजना (Sargeant Plan) 1944
1944 में, केंद्रीय सलाहकार शिक्षा बोर्ड ने एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना का प्रस्ताव रखा, जिसे सरजेंट योजना के नाम से जाना जाता है, जो भारतीय सरकार के शैक्षिक सलाहकार सर जॉन सरजेंट के नाम पर है।
- प्राथमिक और उच्च विद्यालयों (जूनियर और सीनियर बेसिक स्कूल) की स्थापना।
- 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए सार्वजनिक, नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव।
- 11 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए छह वर्ष
- उच्च विद्यालयों को शैक्षणिक और तकनीकी/व्यावसायिक स्कूलों में विभाजित किया जाएगा, जिनके पाठ्यक्रम भिन्न होंगे।
- इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम का उन्मूलन और उच्च विद्यालय तथा कॉलेज स्तर पर एक-एक वर्ष का विस्तार।
सार्जेंट योजना ने देश में शिक्षा पुनर्निर्माण के लिए 40 वर्ष की योजना का खाका प्रस्तुत किया।
|
28 videos|739 docs|84 tests
|















