उभरते क्षेत्रीय विन्यास, लगभग 600–1200 ईस्वी - 2 | UPSC CSE के लिए इतिहास (History) PDF Download
ब्रहमदेय बस्तियों का स्वभाव
ब्रहमदेय बस्तियों का अध्ययन करते समय, तथ्यात्मक विवरणों को सैद्धांतिक दृष्टिकोणों से अलग करना चुनौतीपूर्ण होता है, जो अक्सर महत्वपूर्ण तरीकों से एक-दूसरे के विरोध में होते हैं। इसके अतिरिक्त, जबकि अधिकांश उपमहाद्वीप में सामान्य विशेषताएँ और प्रवृत्तियाँ हैं, विभिन्न क्षेत्रों, उपक्षेत्रों और समय अवधियों में ब्रहमदेय की अपनी अनूठी विशेषताएँ थीं।
- गठन और विशेषताएँ: सभी ब्रह्मण बस्तियाँ शाही भूमि अनुदानों के परिणामस्वरूप नहीं बनी थीं, और ये गाँव कई क्षेत्रों में बस्तियों का केवल एक छोटा हिस्सा constituted करते थे। राज्य के दृष्टिकोण से, ब्रहमदेय का निर्माण अक्सर संभावित राजस्व के स्रोतों को छोड़ने का मतलब था। भूमि अनुदान शिलालेखों में कभी-कभी खजाने, जंगलों और बिना वारिस की संपत्ति पर अधिकारों के हस्तांतरण का उल्लेख किया जाता था, जिन पर theoretically राजा का अधिकार था।
- राज्य के विशेषाधिकार: इन अधिकारों का हस्तांतरण दानकर्ताओं पर राज्य के विशेषाधिकार को प्रभावित करेगा। शिलालेखों से यह भी संकेत मिलता है कि ब्रहमदेय को राज्य, इसके अधिकारियों या सैनिकों द्वारा हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए। चोल साम्राज्य में, कुछ महत्वपूर्ण ब्रहमदेय का स्थानीयता (nadu) के भीतर तनीयूर का एक दर्जा था, जिससे वे नाडु के अधिकार क्षेत्र से स्वतंत्र हो गए।
- स्वायत्तता और राजा के साथ संबंध: यह सुझाव देता है कि ब्रहमदेय, व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, ग्रामीण परिदृश्य में स्वायत्त इकाइयाँ थीं, जहाँ ब्रह्मण दानकर्ताओं को राज्य के हस्तक्षेप के बिना मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता थी। हालाँकि, यह स्वतंत्रता राजा के साथ एक करीबी संबंध द्वारा संतुलित थी।
- कृषि का विस्तार: कुछ मामलों में, भूमि अनुदान ने मौजूदा कृषि सीमाओं के परे ब्रह्मण बस्तियों की स्थापना को शामिल किया, जिससे कृषि क्षेत्रों का विस्तार हुआ। हालाँकि, अधिकांश अनुदान पहले से स्थापित और खेती वाले क्षेत्रों में किए गए थे, जैसा कि बंगाल के 12वीं सदी के बाद के अनुदानों में उपहारित गाँवों और वार्षिक आय एवं आवास भूमि (vastu-bhumi) जैसे विवरणों से स्पष्ट है।
- ब्रह्मण दानकर्ताओं का समावेश: यह दर्शाता है कि अनुदान आमतौर पर ब्रह्मण दानकर्ताओं को पूर्व में मौजूद सामाजिक, आर्थिक, और सांस्कृतिक ढाँचों में एकीकृत करते थे, न कि पूरी तरह से नए बस्तियों का निर्माण करते थे।
ब्रहमदेय भूमि अनुदान का संक्षिप्त अवलोकन
ब्रह्मादेया भूमि अनुदान का आकार विभिन्नता में हो सकता है, जो छोटे भूखंडों से लेकर पूरे गांवों या कई गांवों तक फैला हो सकता है। प्राप्तकर्ताओं या दाताओं की संख्या एक ही ब्राह्मणा से लेकर सैकड़ों तक हो सकती है। कुछ मामलों में एक ही दाता को कई उपहार प्राप्त हुए हैं।
ब्राह्मणों को बड़े अनुदान
- 10वीं शताब्दी के पश्चिमभाग प्लेट में श्रीचंद्र का उदाहरण है, जहां बड़े क्षेत्र को कई ब्राह्मणों को दिया गया।
- इस शिलालेख में 6,000 ब्राह्मणों को अनुदान दिया गया है, साथ ही एक मठ से जुड़े कई व्यक्तियों को भी।
- यह अनुदान श्रीहट्टा मंडल के तीन विशय (जिलों) को शामिल करता है, जिसे राजा की सम्मान में श्रीचंद्रपुर नामक एक ब्रह्मपुरा (ब्राह्मण बस्ती) में परिवर्तित किया गया।
- इन अनुदानों की सीमाओं के विवरण से पता चलता है कि ब्रह्मादेया कभी-कभी एक-दूसरे के निकट होते थे, जो कुछ क्षेत्रों में ब्राह्मण बस्तियों की संख्या और घनत्व में वृद्धि के संकेत देते हैं।
कर-मुक्त स्थिति
- ज्यादातर भूमि अनुदान शिलालेखों ने ब्राह्मण बस्तियों को स्थायी कर-मुक्त स्थिति प्रदान की।
- इसका मतलब था कि भूमि राज्य के करों से मुक्त थी, और किसी भी बकाया राशि जो राज्य वसूल कर सकता था, अब दाता को दी जानी थी।
- ब्रह्मादेया को एक विशेष राजस्व स्थिति का आनंद मिला, जिसमें राजस्व वसूल करने और रखने का अधिकार दाताओं को दिया गया।
कर-शासन और क्रय-शासन
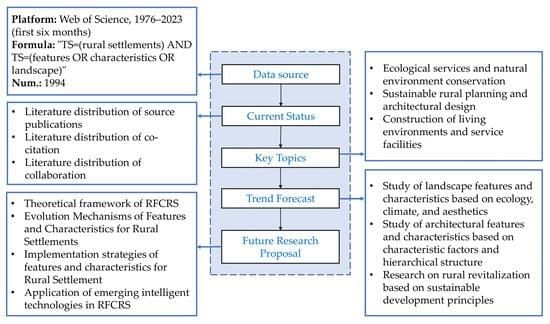
कर-शासन वे भूमि अनुदान शिलालेख हैं जो यह निर्दिष्ट करते हैं कि भूमि करों के अधीन है, जो सामान्य कर-मुक्त अनुदानों के विपरीत है। ये दुर्लभ हैं और ओडिशा, बंगाल, और आंध्र प्रदेश जैसे क्षेत्रों में पाए गए हैं।
- उड़ीसा से उदाहरण:
- बोबिली पट्टे चंदवर्मन के: अनुदान ने गाँव के लिए वार्षिक 200 पानास का भुगतान निर्धारित किया, जो अन्य अग्रहारा की तरह था।
- निंगोंडी पट्टे प्रभंजनवर्मन के: भूमि का शुल्क 200 पानास निर्धारित किया गया, जिसे अग्रिम में भुगतान करना था।
- गंजाम अनुदान पृथिवर्मादेव का: भूमि का अनुदान एक कर आवश्यकता के साथ था, जिसमें 4 पलास चांदी का वार्षिक किराया निर्दिष्ट किया गया।
- कालिंगा के गंगास: विभिन्न अनुदान जो विशिष्ट किराया राशि और भुगतान अवधियों को दर्शाते हैं, जैसे वज्रहस्ता का कलाहांडी अनुदान और अनंतवर्मन का चिकाकोले अनुदान।
- भौमा-कारा रानी धर्ममहादेवी: अंगुल पट्टा जो कर-मुक्त और कर योग्य भूमि अनुदानों का मिश्रण सुझाता है।
- शुल्की शिलालेख: तालचर और पुरी पट्टे जो विशिष्ट कर राशियों को दर्शाते हैं, हालांकि मानक कर-मुक्त भाषा में।
- तुंग राजा गयादतुंगा: तालचर पट्टा और एशियाटिक सोसाइटी पट्टा जो कर राशियों और भूमि अनुदान के प्रकार को विस्तृत करते हैं।
- सोमवंशी राजा जनमेजय महाभवगुप्त: पटना पट्टे जो वार्षिक कर राशियों को निर्दिष्ट करते हैं।
- साम्राज्य गंगास: अनुदान जिनमें स्पष्ट कर-मुक्त संदर्भों की कमी है, संभावित कर दायित्वों का संकेत देते हैं।
दानकर्ताओं के अधिकार:
- जुर्माने की आय: दानकर्ता उन जुर्मानों की आय के हकदार थे जो उन व्यक्तियों पर लगाए गए थे जो विशेष आपराधिक offenses में दोषी पाए गए थे।
- सजा से छूट: एक अन्य व्याख्या का सुझाव है कि दानकर्ताओं को यदि वे खुद ऐसे अपराध करते हैं तो उन्हें सजा से छूट दी गई थी।
- आरोपित व्यक्तियों का परीक्षण करने का अधिकार: कुछ शिलालेख बताते हैं कि दानकर्ताओं को कुछ offenses के लिए आरोपित व्यक्तियों का परीक्षण करने का अधिकार था।
स-चौरोद्ध-रण:
- यह शब्द दो तरीकों से समझा जा सकता है: सजा देने का अधिकार: यह चुराई गई चीज़ों के लिए दोषी पाए गए लोगों को सजा देने के अधिकार को संदर्भित करता है। जुर्माना वसूल करने का अधिकार: यह चुराई गई चीज़ों के लिए दोषी लोगों से जुर्माना वसूल करने के अधिकार को संदर्भित करता है।
दानकर्ताओं का अधिकार:
- विभिन्न क्षेत्रों से मिली लेखन सामग्री यह दिखाती है कि दानकर्ताओं को व्यापक अधिकार प्रदान किए गए थे।
- उड़ीसा का उदाहरण: उड़ीसा के लेखों में ऐसे भूमि दान का उल्लेख है जिसमें निवास भूमि और जंगल (सा-पद्र-अरण्य) दानकर्ताओं को दिया गया।
- बंगाल के साथ तुलना: यह प्रथा 12वीं सदी के बाद बंगाल में उन लेखों के समान है जो निवास भूमि (वास्तु-भूमि) पर दानकर्ताओं को अधिकार स्थानांतरित करते थे।
गांव के चौकी पर नियंत्रण:
- उड़ीसा के लेखन: 9वीं सदी से, उड़ीसा में कुछ लेख (जैसे उदयवराह और भवमा-कार, शुल्की, और तुंगा वंश के) ने कहा कि भूमि के साथ गांव के चौकी, लैंडिंग या स्नान स्थान, और नावों (सा-खेता-घाटा-नदी-तारा-स्थान-आदि-गुल्मक) पर नियंत्रण दिया गया।
- व्याख्या: इसे इन स्थानों पर एकत्रित किए गए करों पर अधिकार या सैन्य चौकियों पर अधिकार के रूप में समझा जा सकता है।
विषयों का दान:
- भवमा-कार, आदि-भंज, शुल्की, और तुंगा के लेख: कुछ लेखों में 'बुनकरों, गोपालकों, शराब बनाने वालों, और अन्य विषयों के साथ भूमि दान' (सा-तानत्रवय-गोकुटा-शौंदिक-आदि-प्राकृतिका) का उल्लेख है।
- शेयरक्रॉपर्स का स्थानांतरण: कर्नाटका में, कुछ भूमि दान यह दर्शाते हैं कि भूमि के साथ शेयरक्रॉपर्स (अद्धिकास) का स्थानांतरण किया गया।
alienation पर प्रतिबंध:
- उपहारित भूमि की असंप्रदायिकता: कई प्राप्तकर्ताओं को भूमि को असंप्रदायिक करने का अधिकार नहीं था, अर्थात् वे इसे किसी भी तरह से स्थानांतरित, बेचना या निपटान नहीं कर सकते थे।
- असंप्रदायिकता का संकेत देने वाले शब्द: उपहारित भूमि की असंप्रदायिकता को निबंधन-धर्म, अक्षय-निबंधन-धर्म, या अप्रदा-धर्म जैसे शब्दों से इंगित किया गया है।
- उड़ीसा के शिलालेख: उड़ीसा के कई शिलालेखों में a-lekhani-praveshataya शब्द शामिल है, जिसका अर्थ है कि भूमि किसी अन्य दस्तावेज का विषय नहीं हो सकती और इसे बेचा नहीं जा सकता।
- ब्राह्मण प्राप्तकर्ताओं के अधिकार: ऐसे मामलों में, उपहारित भूमि पर ब्राह्मण प्राप्तकर्ताओं के अधिकार जमींदारों से अधिक थे लेकिन भूमि मालिकों से कम थे।
ब्राह्मण बस्तियों का कृषि संबंधों पर प्रभाव
दक्षिण भारत में प्रारंभिक मध्यकालीन अवधि के दौरान ब्राह्मण बस्तियों का कृषि संबंधों और विभिन्न ग्रामीण समूहों के अधिकारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इस प्रभाव के संबंध में मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
1. राजसी संरक्षण और ब्राह्मण अभिजात वर्ग
- राजकीय समर्थन ने कुछ ब्राह्मण समुदायों की आर्थिक शक्ति को बढ़ाया, जिससे एक ब्राह्मण भूमि अभिजात वर्ग का उदय हुआ। इस अभिजात वर्ग को 'ब्राह्मण जागीरदारों' या 'ब्राह्मण मध्यस्थों' के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वे राजाओं के लिए सैन्य सेवक या कर संग्रहकर्ता नहीं थे।
2. कृषि विस्तार और भूमि अनुदान
- इतिहासकार आमतौर पर प्रारंभिक मध्यकालीन अवधि को कृषि विस्तार का एक समय मानते हैं, जिसमें भूमि अनुदान का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हालाँकि, इस समय के दौरान कृषि संबंधों की प्रकृति पर अलग-अलग विचार हैं।
3. ग्रामीण समुदाय के अधिकारों पर प्रभाव
- ब्रह्मदेय (Brahmadeyas) के स्थापना ने ग्रामीण समुदाय के विभिन्न वर्गों के अधिकारों के बारे में सवाल उठाए, जिसमें बड़े और छोटे किसान मालिक, किरायेदार, हिस्सेदारी वाले किसान और भूमिहीन श्रमिक शामिल हैं। भूमि अनुदान चार्टर्स में पाए जाने वाले लंबे छूट (pariharas) की सूचियों ने इस पर बहस को जन्म दिया है कि क्या ये किसान वर्ग के प्रति बढ़ती दमन को दर्शाते हैं।
4. विभिन्न ऐतिहासिक दृष्टिकोण
- फ्यूडलिज़्म स्कूल का तर्क है कि भूमि अनुदान ने ग्रामीण समूहों के ब्रह्मण (Brahmana) प्राप्तकर्ताओं द्वारा अधिक अधीनता और दमन का परिणाम दिया।
- बर्टन स्टाइन ने प्रारंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत में ब्रह्मण-किसान गठबंधन का विचार प्रस्तुत किया।
- ‘संविधान’ या ‘प्रक्रियात्मक’ मॉडल के समर्थकों ने इस संदर्भ में कृषि संबंधों की प्रकृति पर व्यापक रूप से विचार नहीं किया है।
5. कृषि संबंधों में परिवर्तन
- गाँवों में ब्रह्मण प्राप्तकर्ताओं का प्रवेश कृषि संबंधों को बदल दिया, जिससे पुराने कुलीनता आधारित उत्पादन संबंध कमजोर हुए।
- ब्रह्मण बस्तियों में अक्सर गैर-परिवार श्रम का उपयोग शामिल था, जिससे उत्पादन में कुलीनता के बंधनों को और भी कमजोर किया गया।
6. कर-मुक्त स्थिति और गाँव के शुल्क
- अधिकांश भूमि अनुदानों में एक कर-मुक्त स्थिति शामिल थी, जिसमें ग्रामीणों को विभिन्न शुल्कों को राज्य के बजाय प्राप्तकर्ताओं को सौंपने की आवश्यकता होती थी।
- अंकन कभी-कभी करों का सामान्य संदर्भ में उल्लेख करते थे या कर छूट की लंबी सूचियों को निर्दिष्ट करते थे, जो कर जिम्मेदारियों में बदलाव को दर्शाता है।
7. संसाधनों पर अधिकार
- प्राप्तकर्ताओं को अक्सर जल संसाधनों, पेड़ों, जंगलों और निवास क्षेत्रों पर अधिकार दिए जाते थे, जो गाँव के समुदाय के अधिकारों को प्रभावित करते थे।
8. विवाद समाधान और न्यायिक अधिकार
गांव के स्तर पर विवादों का समाधान:
- अधिकांश गांव स्तर के विवाद संभवतः गांव समुदाय के एक हिस्से द्वारा सुलझाए जाते थे।
- न्यायिक अधिकारों के हस्तांतरण या आपराधिक offenses के लिए दंड वसूलने के अधिकार के संकेत, इस समुदाय के एक हिस्से के अधिकारों में बदलाव को दर्शाते हैं।
भूमि अनुदान और समाज पर उनका प्रभाव:
- ऐतिहासिक प्रक्रियाएँ: बी. डी. चट्टोपाध्याय ने भारतीय इतिहास में कुछ प्रमुख ऐतिहासिक प्रक्रियाओं की पहचान की, जिनमें राज्य का विस्तार, जनजाति का परिवर्तन, जाति का निर्माण, और प्रारंभिक मध्यकालीन अवधि के दौरान पूजा पद्धतियों का अधिग्रहण शामिल हैं।
- ब्राह्मणों की स्थिति को मजबूत करना: भूमि अनुदान ने ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ ब्राह्मणों की स्थिति को मजबूत किया, जिससे उनकी पारंपरिक उच्च सामाजिक स्थिति को राजनीतिक और आर्थिक शक्ति के साथ बढ़ावा मिला। इससे उन्हें भूमि, संसाधनों, और लोगों पर नियंत्रण मिला, जिससे वे ब्रह्मादेया गांवों में एक प्रमुख जाति बन गए।
- जनजातीय समुदायों के साथ संपर्क: उन क्षेत्रों में जहां ब्रह्मादेया गांव जनजातीय समुदायों के निकट थे, भूमि अनुदान ने इन जनजातियों में हल कृषि के परिचय में सहायता की। कुछ जनजातीय समूह जाति समाज में शामिल हुए, जबकि अन्य को अछूतों या बहिष्कृतों के रूप में हाशिए पर डाल दिया गया।
- जाति का निर्माण और कायस्थ: भूमि अनुदानों की यह प्रक्रिया जातियों के प्रसार में योगदान करती है, जिसमें लेखकों (कायस्थों) का एक व्यावासायिक समूह से जाति में परिवर्तन शामिल है, जो कई भूमि लेन-देन को रिकॉर्ड करने की आवश्यकता के कारण हुआ।
- ब्राह्मणों पर प्रभाव: भूमि अनुदानों में वृद्धि ने ब्राह्मणों के बीच क्षेत्रीय वर्गीकरण और स्थिति पदानुक्रम के उदय का नेतृत्व किया। वे नए सामाजिक नेटवर्क में शामिल हुए, जिसके परिणामस्वरूप उप-जातियों का गठन हुआ, विशेष रूप से प्रवासी ब्राह्मणों के बीच।
- मंदिर धर्म और उप-जातियाँ: तमिल नाडु और कर्नाटका जैसे क्षेत्रों में, मंदिर धर्म के साथ जुड़ाव ने शिव मंदिरों से जुड़े शिव ब्राह्मणों जैसी उप-जातियों को जन्म दिया।
- विवाह प्रथाओं में परिवर्तन: स्थानीय समाजों में समाकलन ने कभी-कभी ब्राह्मणों के बीच विवाह प्रथाओं में बदलाव का कारण बना। उदाहरण के लिए, केरल में, पाय्यानूर के ब्राह्मणों ने मातृसत्तात्मक प्रथाओं को अपनाया, जबकि नंबूद्री ब्राह्मणों ने संपत्ति बनाए रखने के लिए अपनी जाति के भीतर विवाह करने की एक अनूठी प्रथा विकसित की, जो नायर मातृसत्तात्मक समाज के प्रभाव को दर्शाती है।
- मंदिर आधारित संप्रदाय धर्म का उदय: प्रारंभिक मध्यकालीन अवधि में, विशेष रूप से 10वीं शताब्दी से, मंदिर आधारित संप्रदाय धर्म की बढ़ती लोकप्रियता देखी गई, जिसमें मंदिरों के प्रति शाही संरक्षण में वृद्धि हुई।
- ब्राह्मणों और मंदिर प्रबंधन: कुछ ब्राह्मणों ने मंदिर के वातावरण के प्रति अपनी भूमिकाएँ अनुकूलित कीं, और मंदिर प्रबंधक या पुजारी बन गए। दक्षिण भारत की शिलालेखों से पता चलता है कि ब्राह्मणों और ब्राह्मण सभा की मंदिर प्रबंधन में सक्रिय भागीदारी थी, और केरल में ब्राह्मण बस्तियाँ प्रारंभिक समय से मंदिर केंद्रित थीं।
- मंदिर-उन्मुख धर्म का प्रसार: हालांकि शिलालेखों में उनकी वेदिक संबंधों पर जोर दिया गया है, लेकिन ब्रह्मादेयों के ब्राह्मणों ने इस अवधि के दौरान मंदिर-उन्मुख धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
ब्राह्मणिक और जनजातीय संस्कृतियों के बीच अंतःक्रिया:
- ब्राह्मडेस, जो जनजातीय क्षेत्रों में या उनके निकट स्थित थे, ने ब्राह्मणीय और जनजातीय धर्मों के बीच संवाद के बिंदुओं के रूप में कार्य किया, जिससे धार्मिक संश्लेषण के विभिन्न रूपों का विकास हुआ।
- प्रदर्शन और परिवर्तन: जनजातीय समुदायों को ब्राह्मणवाद से अवगत कराया गया, जबकि ब्राह्मणवाद ने भी क्षेत्रीय, स्थानीय और जनजातीय परंपराओं के साथ अपने अंतर्संबंध के माध्यम से परिवर्तन अनुभव किया।
- माइग्रेशन और विवाह: माइग्रेशन के समय में, ब्राह्मणों और स्थानीय महिलाओं के बीच विवाह ने ब्राह्मणीय और जनजातीय संस्कृतियों के बीच संवाद को और बढ़ावा दिया।
- पारस्परिक संवाद: ये संवाद आपसी थे, लेकिन समान या संतुलित नहीं थे, जिसमें ब्राह्मणीय तत्व अंततः प्रमुख बन गए।
- जगन्नाथ का उदाहरण: उड़ीसा में जगन्नाथ की पूजा ने एक जनजातीय देवता के ब्राह्मणीकरण को दर्शाया, जैसा कि विभिन्न विद्वानों द्वारा विश्लेषित किया गया है।
- तंत्र में भूमि अनुदान की भूमिका: आर. एस. शर्मा ने सुझाव दिया कि भूमि अनुदान के माध्यम से ब्राह्मणीय और जनजातीय संस्कृतियों के बीच संवाद तंत्र के उद्भव और विकास में महत्वपूर्ण था।
भूमि अनुदान, ब्राह्मण और संस्कृत साहित्य
- प्रारंभिक मध्यकालीन काल: प्रारंभिक मध्यकालीन काल में ब्राह्मणों को भूमि अनुदानों का प्रसार संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण उत्पादन के साथ मेल खाता है।
- रोजगार के अवसर: इस काल में पढ़े-लिखे और ज्ञानी ब्राह्मणों के लिए प्रशासनिक संरचनाओं में रोजगार के अवसर बढ़े।
- राजकीय दरबारों में संरक्षण: ब्राह्मण विद्वान, कवि, और नाटककारों का इन दरबारों में सम्मान और समर्थन किया गया।
- शोध का संरक्षण: भूमि अनुदानों के माध्यम से संरक्षण ने ब्राह्मण विद्या को बढ़ावा देने और बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- धन और सुरक्षा: भूमि का नियंत्रण और ब्राह्मण विशेषज्ञों द्वारा बसी बस्तियों का उदय ब्राह्मण बुद्धिजीवियों के कुछ वर्गों को निरंतर बौद्धिक गतिविधि के लिए आवश्यक सुरक्षा और धन प्रदान करता है।
ग्रामीण समाज: क्षेत्रीय विशिष्टताएँ
ऐतिहासिक प्रक्रियाएँ और क्षेत्रीय विशिष्टताएँ
- ऐतिहासिक प्रक्रियाओं ने उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में ग्रामीणों के जीवन को प्रभावित किया है।
- इस अवधि के दौरान ग्रामीण जीवन के विवरण के बारे में सीमित प्रत्यक्ष पाठ्य साक्ष्य उपलब्ध हैं।
कृषि-पराशर
- कृषि-पराशर एक महत्वपूर्ण पाठ है जो कृषि संचालन के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित है।
- यह पाठ संभवतः 950 से 1100 ईस्वी के बीच बंगाल क्षेत्र में लिखा गया था।
- इस पाठ को एक लेखक पाराशर के नाम से श्रेय दिया गया है और यह संस्कृत छंद में लिखा गया है जिसमें कुछ गद्य मंत्र भी शामिल हैं।
- कृषि-पराशर की भाषा और शैली सरल और स्पष्ट है।
कृषि प्रथाएँ
- पाठ में कृषि में वर्षा के महत्व पर जोर दिया गया है और ग्रहों के आंदोलन, ऋतुओं, वायु की दिशा, और वर्षा से संबंधित उपदेश दिए गए हैं।
- यह मौसम की स्थिति की निगरानी के लिए वायवीय यंत्रों का उपयोग करने की सिफारिश करता है।
- कृषि-पराशर स्वस्थ धान की फसल के लिए खाद (सारा) के महत्व को उजागर करता है और धान के उत्पादन के लिए जुताई और बुआई की तकनीकों पर विस्तृत निर्देश प्रदान करता है।
बुआई और ट्रांसप्लांटिंग तकनीकें
- बीजों को संरक्षित करने और बुआई के लिए सर्वोत्तम समय के निर्देश दिए गए हैं।
- पाठ में बुआई के बाद धान के खेतों को समतल करने के लिए एक उपकरण 'मयिका' का उपयोग करने का सुझाव दिया गया है।
- नर्सरी के पौधों को ट्रांसप्लांट करने के लिए दिशानिर्देश, जिसमें ग्रहों के संयोग के आधार पर स्थान देना शामिल है, भी शामिल हैं।
कटाई और थ्रेसिंग
- कृषि-पराशर कटाई की अवधि (पौष, दिसंबर-जनवरी) को रेखांकित करता है और थ्रेसिंग फ्लोर स्थापित करने के लिए विवरण प्रदान करता है।
- कटाई और थ्रेसिंग के बाद, किसानों को अनाज को एक मापने के उपकरण 'अधक' का उपयोग करके तौले जाने की सलाह दी जाती है।
प्रारंभिक मध्यकालीन बंगाल की लोकप्रिय कृषि कहावतें
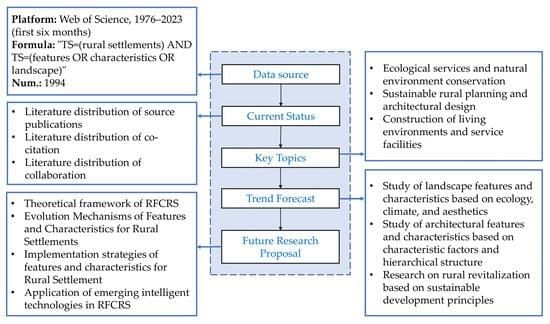
प्रारंभिक बंगाली साहित्य
- बंगाली भाषा पूर्ण रूप से लगभग 1000 ईस्वी के आस-पास विकसित हुई, लेकिन 1300 ईस्वी से पहले का साहित्य बहुत कम है।
- बंगाली में सबसे प्रारंभिक कार्यों में डाक तंत्र शामिल है, जिसे डाकर बचन भी कहा जाता है, जो एक बौद्ध तांत्रिक ग्रंथ है जिसमें पुराने बंगाली में ज्ञानवर्धक कहावतें और सूत्र हैं।
- एक और समान कार्य है खानार बचन, जिसमें समय के साथ अधिक परिवर्तन हुए हैं। लोकप्रिय मान्यता के अनुसार, इस कार्य के लेखक खना थे, जो प्रसिद्ध खगोलज्ञ वराहमिहिर की बहू मानी जाती हैं।
डाकर बचन और खानार बचन
- डाकर बचन और खानार बचन में कहावतें मुख्य रूप से कृषि के मामलों पर केंद्रित हैं, लेकिन वे ज्योतिष, चिकित्सा और घरेलू मुद्दों जैसे विषयों को भी छूती हैं।
- ये कार्य छोटे, छंदबद्ध सूक्तियों का संग्रह हैं जो बंगाल की भूमि और जलवायु से निकटता से जुड़े हुए हैं। आज भी, ये क्षेत्र के किसानों के लिए मूल्यवान कृषि पुस्तिकाएँ हैं।
- डाकर बचन एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ा है जिसे 'डाक' के रूप में जाना जाता है, जो अक्सर एक विनम्र दूध विक्रेता के रूप में कल्पित किया जाता है। कहावतें 'डाक गोआला' के हस्ताक्षर के साथ समाप्त होती हैं, जो इस लोकप्रिय विश्वास को दर्शाती हैं।
अनुवादित कहावतें
- आग्रहायण वर्षा: यदि आग्रहायण (नवम्बर- दिसम्बर) के महीने में बारिश होती है, तो इसे अशुभ माना जाता है, जिसका प्रतीक है राजा का भिक्षाटन करना।
- पौष वर्षा: पौष (दिसम्बर-जनवरी) के महीने में बारिश को अत्यंत लाभदायक माना जाता है, जिससे यहां तक कि भूसा भी बिक्री के लिए मिल सकता है।
- माघ के अंत की वर्षा: माघ (जनवरी-फरवरी) के अंत में बारिश को राजा और उसके राज्य के लिए आशीर्वाद माना जाता है।
- फाल्गुन वर्षा: फाल्गुन (फरवरी-मार्च) में बारिश को चिनी (Panicum miliaceum) के प्रचुर विकास के लिए लाभदायक माना जाता है।
- सूर्य और छाया: खना सलाह देती हैं कि धान (चावल) सूर्य में अच्छा होता है, जबकि पान (पान का पत्ता) छाया में।
- धान के लिए आदर्श स्थिति: खना ने बताया कि धान दिन में पर्याप्त धूप और रात में बारिश के साथ तेजी से बढ़ता है, और कार्तिक (अक्टूबर-नवंबर) में हल्की वर्षा विशेष रूप से लाभकारी होती है।
- धान की सड़न: हल चलाने वालों के लिए एक व्यावहारिक टिप है कि धान की सड़न को झाड़ियों की जड़ों के पास बांस के झाड़ी में डालें ताकि बड़ी भूमि का क्षेत्र कवर हो सके।
- रेतीली मिट्टी में पटोल: पटोल (Trichosanthis dioeca) को रेत वाली मिट्टी में लगाने की सलाह दी गई है।
- सरसों और राई के बीज: सरसों के बीजों को निकटता से और राई के बीजों को दूरी पर बोने की सलाह।
- कपास और जूट के पौधे: कपास के पौधों को एक-दूसरे से दूरी पर लगाने और जूट के पौधों को कपास के पास न लगाने के निर्देश, क्योंकि कपास के पौधे जूट के खेतों की नमी सहन नहीं कर सकते।
- चैत की धुंध और भाद्र धान: चैत (मार्च-अप्रैल) में धुंध और भाद्र (अगस्त-सितंबर) में धान की प्रचुरता से महामारी और आपदाएँ आ सकती हैं।
प्रारंभिक मध्यकालीन पूर्वी भारत में कृषि ज्ञान और अनुष्ठान
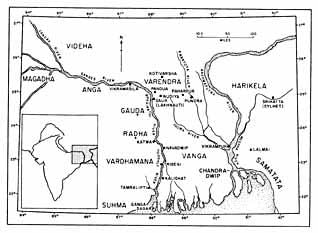
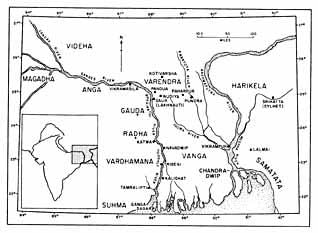
कृषि-पराशर, एक प्राचीन ग्रंथ, प्रारंभिक मध्यकालीन पूर्वी भारत में कृषि प्रथाओं, अनुष्ठानों और विश्वासों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है, विशेष रूप से धान की खेती और कृषि गतिविधियों के समय के संबंध में।
मौसम की भविष्यवाणियाँ और उनका महत्व
- यह पाठ विभिन्न माहों में विशिष्ट वायुमंडलीय स्थितियों के आधार पर मौसम की भविष्यवाणियाँ प्रस्तुत करता है, जो कृषि गतिविधियों की योजना बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
- उदाहरण के लिए, आषाढ़ (जून-जुलाई) में एक दक्षिणी हवा आने का संकेत आगामी बाढ़ का होता है, जबकि कुछ बादल के आकार तात्कालिक वर्षा का सुझाव देते हैं।
- ये भविष्यवाणियाँ किसानों को समय पर कार्रवाई करने में मार्गदर्शन करती हैं, जैसे कि खेतों के चारों ओर पानी संरक्षित करने के लिए रिड्ज़ का निर्माण करना।
कृषि के अनुष्ठान और त्योहार
- कृषि-पराशर में विभिन्न कृषि अनुष्ठानों और त्योहारों का विवरण है, जो कृषि की सफलता को प्रभावित करने वाला माना जाता है।
- उदाहरण के लिए, गो-परवा (गायों का त्योहार) कार्तिक (अक्टूबर-नवंबर) में गायों के स्वास्थ्य को एक वर्ष तक सुनिश्चित करने के लिए कहा जाता है।
- अतिरिक्त रूप से, पाठ में हला-प्रसारणा (पहली हल चलाने का अनुष्ठान) के महत्व पर जोर दिया गया है, जो कृषि के फलों को सुरक्षित करने में सहायक है।
उर्वरा विश्वास और प्रतिबंध
- उर्वरा विश्वासों से संबंधित कुछ विशिष्ट प्रतिबंध हैं, जैसे कि एकत्रित बीजों और उन महिलाओं के बीच संपर्क से बचना जो मासिक धर्म में हैं, बांझ हैं, गर्भवती हैं, या हाल ही में बच्चे को जन्म दिया है।
- पाठ में अंबुवाची का भी उल्लेख है, जो आषाढ़ में एक अवधि है जब पृथ्वी के मासिक धर्म में होने की बात कही जाती है, और बीजों को नहीं बोना चाहिए।
फसलों की सुरक्षा के लिए अनुष्ठान
- कृषि-पराशर में खेतों से पक्षियों और जानवरों को दूर करने और धान के खेतों में रोगों को रोकने के लिए तांत्रिक ग्रंथों से रहस्यमय मंत्रों का उपयोग करने की सलाह दी गई है।
कृषि में समारोह और देवताओं
- पौष (दिसंबर-जनवरी) में धान की कटाई से पहले, एक समारोह जिसे पुष्य-यात्रा कहा जाता है, आयोजित करने की सिफारिश की जाती है, जिसमें भोजन, नृत्य, संगीत और सूर्य की प्रार्थनाएँ शामिल होती हैं। कृषि कार्यों के दौरान विभिन्न देवताओं, जैसे प्रजापति, शची, इंद्र, मारुत, वसुधा, और लक्ष्मी को आह्वान किया जाता है, और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए लक्ष्मी को अंतिम प्रार्थना अर्पित की जाती है।
प्रारंभिक मध्यकालीन बंगाल और बिहार में गांव की जीवनशैली और भूमि अनुदान
- प्रारंभिक मध्यकालीन बंगाल और बिहार की शिलालेख गांव की जीवनशैली, भूमि अनुदान और कृषि प्रथाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। गांवों को ग्राम या पटका कहा जाता था, जिनकी पहचान उनके आवासीय भूमि (वास्तु) और सीमाओं से होती थी, जो अक्सर नदियों, दलदली भूमि और वृक्षों जैसे प्राकृतिक विशेषताओं से निर्धारित होती थीं। चावल मुख्य फसल था, और भूमि अनुदान की शिलालेखों में उपहार में दी गई भूमि के आयाम और वार्षिक राजस्व का विस्तृत विवरण होता था, जो राज्य के राजस्व के रिकॉर्ड को ध्यानपूर्वक बनाए रखने का संकेत देता है। आयामों को सतह और बीज माप में दिया गया था, जो चावल उत्पादन के आधार पर मूल गणनाओं को दर्शाता है। बंगाल और बिहार के भूमि अनुदानों में, प्राप्तकर्ताओं को आमतौर पर कृषक (kshetrakarah) या गांव के निवासियों (prativasinah) के रूप में पहचाना जाता है। ब्राह्मणों, विशेष रूप से उनमें से प्रमुख (Brahmanottarah), का लगातार उल्लेख किया जाता है, जो गांव स्तर पर उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है। कुछ शिलालेखों में अन्य समूहों, जैसे व्यापारियों, क्लर्कों, मज़दूरों, और गांव के नेताओं का भी संदर्भ दिया गया है। कुटुम्बिन शब्द को बढ़ती हुई समझ के अनुसार किसान के रूप में समझा जाता है।
प्रारंभिक मध्यकालीन असम की शिलालेख
- नयनजोत लाहिरी का असम में प्रारंभिक मध्यकालीन लेखों का अध्ययन बताता है कि कृषि गतिविधियाँ और बस्तियाँ मुख्यतः ब्रह्मपुत्र और अन्य नदियों की घाटियों में स्थित थीं, जिनमें तेजपुर और गुवाहाटी जैसे क्षेत्रों में खासा ध्यान दिया गया है।
- इन लेखों में अक्सर गांव की सीमाओं के संदर्भ में नदियों और नालों का उल्लेख किया गया है, जो यह दर्शाता है कि कृषि गांवों के लिए नदी जल संसाधनों पर निर्भरता थी।
- इसके विपरीत, असम घाटी के चारों ओर की पहाड़ियाँ, जैसे कि मिकिर, खासी, गARO, सिंगोरी, हाजी, और सुआलकुची पहाड़ियाँ, इन लेखों में उल्लेखित नहीं हैं।
- नदियों और नालों के अलावा, गांव की सीमाएँ कृषि क्षेत्रों, तटबंधों, तालाबों, पेड़ों, सड़कों, और अन्य गांवों जैसी विशेषताओं से चिह्नित की गई हैं।
- चावल की खेती इन कृषि गांवों में प्रमुख गतिविधि के रूप में उभरती है।
- निवासों को वास्तु के रूप में संदर्भित किया गया है, जिन्हें बांस और फलों के पेड़ों के समूहों के बीच स्थित बताया गया है, जो खेतों से घिरे हुए हैं।
- कभी-कभी, कृषि भूमि के किनारे चरागाह भूमि पाई जाती है, जो पहले कृषि के तहत थी और अब बंजर हो गई है।
- जल प्रबंधन के लिए तटबंधों का सामान्यतः उल्लेख किया गया है।
- चावल के अलावा, लेखों में विभिन्न फलों (जैसे कटहल, अंजीर, काले जामुन, आम, अखरोट, और मीठी जड़ें) और पेड़ों (जैसे पीपल, सप्तपर्णा, झिंगानी, ओडियाम, बांस, और बांस की बेल) का उल्लेख किया गया है।
- व्यावसायिक महत्व वाले पेड़ों, जैसे कि सुपारी, चंदन, और रेशमी कपास, का भी उल्लेख किया गया है, हालाँकि ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हें बागानों में नहीं उगाया गया था।
असम में भूमि दान
- असम में, अन्य क्षेत्रों की तरह, राजाओं ने ब्राह्मणों को भूमि प्रदान की। ग्रामीण समुदाय में ब्राह्मणों, जनजातीय समूहों, और विभिन्न अन्य समुदायों, जैसे कि कैवर्त्त (जो पारंपरिक रूप से मछली पकड़ने और नाव चलाने से जुड़े थे), कुम्हार, और बुनकर शामिल थे, जो कृषि और शिल्प गतिविधियों का मिश्रण दर्शाते हैं।
- घर के इकाईयां कृषि श्रम के लिए केंद्रीय थीं। 9वीं सदी के बाद, जलवायु परिवर्तन के कारण आर्द्र चावल की कृषि पर केंद्रित कृषि बस्तियों में एक महत्वपूर्ण वृद्धि हुई, जो जनसंख्या वृद्धि के साथ संभवतः जुड़ी थी।
प्रारंभिक मध्यकालीन राजस्थान में सिंचाई की भूमिका

- सिंचाई प्रारंभिक मध्यकालीन राजस्थान में कृषि की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण थी।
सिंचाई के स्रोत
- टैंक और कुएं कृत्रिम सिंचाई के प्रमुख स्रोत थे।
- 12वीं-13वीं सदी के कई लेखों में पश्चिम राजस्थान से, जहां पानी की कमी थी, विभिन्न प्रकार के कुएं और टैंकों का उल्लेख है।
कुओं और टैंकों के प्रकार
- लेखों में उल्लेखित विभिन्न प्रकार के कुएं शामिल हैं:
- धिमड़ा/धिवड़ा : एक प्रकार का कुआं।
- वापी : एक सीढ़ी वाला कुआं।
- अराघट्टा/अराघटा/अरहटा : एक प्रकार का कुआं, संभवतः फारसी पहिए से संबंधित।
- उल्लेखित टैंकों और जलाशयों में शामिल हैं: तड़गा, तटकिणी, पुष्करिणी, आदि। कुछ टैंकों का नाम उनके निर्माताओं के नाम पर रखा गया था।
फारसी पहिए पर बहस
- प्रारंभिक मध्यकालीन राजस्थान में फारसी पहिए के उपयोग पर इतिहासकारों में बहस होती है।
- यह बहस अराघट्टा शब्द की व्याख्या के इर्द-गिर्द केंद्रित है और क्या यह फारसी पहिए या नोरिया को संदर्भित करता है।
- नोरिया एक ऐसा पहिया है जिसमें किनारे पर बर्तन या बाल्टियाँ जुड़ी होती हैं, जिसका उपयोग नदियों या उथले स्रोतों से पानी खींचने के लिए किया जाता है।
- फारसी पहिया, जिसमें बर्तनों को ले जाने के लिए गियर और चेन होती है, कुओं से संबंधित था।
- अराघट्टा को फारसी पहिए के समान माना जाता है, जो भारत में इसके प्रारंभिक उपयोग को दर्शाता है।
फसलें और कृषि प्रथाएं
- राजस्थान के अभिलेख विभिन्न फसलों का उल्लेख करते हैं, जिनमें शामिल हैं: चावल, गेंहू, जौ, ज्वार, बाजरा, मोती।
- नकद फसलों में शामिल थे तेल बीज (जैसे तिल) और गन्ना।
- दो फसलों की खेती, या साल में दो फसलें उगाने की प्रथा, 644 CE के डाबोक अभिलेख जैसे अभिलेखों द्वारा सुझाई गई थी।
सिंचाई संसाधनों का नियंत्रण
- सिंचाई संसाधनों पर नियंत्रण विभिन्न समूहों के पास था, जिनमें शामिल हैं: राजा, शाही अधिकारी, कॉर्पोरेट संस्थाएँ (जैसे गोष्ठियां), और व्यक्तिगत कृषि।
सिंचाई कार्यों का विस्तार
- सिंचाई कार्य कम वर्षा वाले क्षेत्रों में विस्तारित हुए: उत्तर गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, और दक्षिण राजस्थान।
- 12वीं सदी के भुवनेदव के आपराजी-तपृच्छा में सिंचाई के लिए विभिन्न जल स्रोतों का उल्लेख है।
- 7वीं-8वीं सदी से लेकर 11वीं-13वीं सदी तक सिंचाई से संबंधित अभिलेखों में वृद्धि हुई।
- 12वीं-13वीं सदी में कई तालाब, कुएं, और सीढ़ी वाले कुंए शासकों, nobles, और व्यापारियों द्वारा बनाए गए।
- अनाहिलवाड़ा के चालुक्य सिंचाई कार्यों के निर्माण में सक्रिय थे और संभवतः उनके पास एक सिंचाई विभाग था।
सिंचाई का कृषि पर प्रभाव
- सिंचाई सुविधाओं का विस्तार संभवतः दो फसलों की खेती और विभिन्न नकद फसलों की खेती को सुगम बनाया।
- बढ़ी हुई सिंचाई ने नकद फसलों जैसे गन्ना, तेल बीज, कपास, और भांग की खेती का समर्थन किया, जो 11वीं से 13वीं सदी के बीच महत्वपूर्ण व्यापारिक वस्तुएँ बन गईं।
अभिलेखों में भूमि माप और सीमाएँ
उड़ीसा की शिलालेखों में, जैसा कि सिंह ने 1994 में उल्लेख किया, भूमि माप से संबंधित विभिन्न शब्दों का उल्लेख किया गया है, जैसे कि तिम्पिरा, मुराजा, नाला, हला, और माला। ये शब्द भूमि को मापने और वर्गीकृत करने के विभिन्न तरीकों को दर्शाते हैं।
- इन शिलालेखों में भूमि की सीमाओं का वर्णन अक्सर संस्कृत, ओड़िया, और तेलुगू जैसी भाषाओं का मिश्रण होता है। यह भाषाई विविधता भूमि सीमाओं के दस्तावेजीकरण में सांस्कृतिक और क्षेत्रीय प्रभावों को इंगित करती है।
- गाँव की सीमाओं को प्राकृतिक और मानव निर्मित विशेषताओं द्वारा चिह्नित किया गया था, जिनमें पेड़, चट्टानें, चींटी के टीले, खाइयाँ, नदियाँ, पहाड़, बाँध, तालाब, कुएँ, और पड़ोसी गाँवों की सीमाएँ और चौराहे शामिल हैं। ये विशेषताएँ कृषि भूमि और गाँवों की सीमाओं को परिभाषित करने के लिए महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करती थीं।
- जल संसाधनों के संदर्भ में, नदियाँ और तालाब सबसे अधिक बार उल्लेखित होते हैं, जबकि कुएँ शिलालेखों में कम बार दिखाई देते हैं। इंद्रवर्मन के अच्युतापुरम ताम्रपत्रों में यह महत्वपूर्णता दर्शाई गई है कि दानकर्ता को तालाब के स्लुइस को खोलने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। यह उपहार में दी गई भूमि के संदर्भ में इन शाही तालाबों के महत्व को दर्शाता है。
ग्रामीण जीवन और कृषि संबंध दक्षिण भारत में ग्रामीण जीवन और कृषि संबंधों की विशेषताओं, जिसमें कृषि, भूमि स्वामित्व, और सामुदायिक संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाएगी, इसे अध्याय के अगले भाग में विस्तृत रूप से बताया जाएगा।
प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में शहरी प्रक्रियाएँ
शहरी पतन, शहरी हस्तशिल्प, व्यापार और धन का विचार प्रारंभिक मध्यकालीन समय में भारतीय सामंतवाद के परिकल्पना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पिछले अध्याय में आर. एस. शर्मा के द्वि-चरणीय शहरी अवनति के सिद्धांत का उल्लेख किया गया था, जिसमें एक चरण 3वीं या 4वीं शताब्दी के दूसरी छमाही में शुरू होता है, और दूसरा चरण 6वीं शताब्दी के बाद शुरू होता है (शर्मा, 1987)।
- शर्मा ने विभिन्न क्षेत्रों के पुरातात्विक डेटा का सारांश प्रस्तुत किया है ताकि अपने सिद्धांत को पुष्ट कर सकें। वह स्वीकार करते हैं कि शहरी अवनति के लिए भारतीय साहित्यिक साक्ष्य मजबूत नहीं है, लेकिन उन्होंने शुआनजांग और अरब लेखकों के विवरणों का उल्लेख किया। उनकी शहरी अवनति की व्याख्या लंबी दूरी के व्यापार में माने जाने वाले गिरावट के चारों ओर केंद्रित है।
- शहरी अवनति ने शहरी आधारित कारीगरों और व्यापारियों की स्थिति को कमजोर किया; कारीगरों को ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा; व्यापारियों को कर चुकाने में कठिनाई हुई; और शहर और गांव के बीच का अंतर धुंधला हो गया। हालांकि, शहरी संकुचन के साथ कृषि विस्तार भी हुआ।
- अन्यत्र, शर्मा ([1965], 1980: 102–5) ने बाजारों पर अधिकार के हस्तांतरण, व्यापारियों द्वारा अपने लाभ का एक भाग मंदिरों को हस्तांतरित करने, और राज्य से मंदिरों को कस्टम शुल्क के हस्तांतरण के शिलालेखीय संदर्भों का उल्लेख किया। इस आधार पर, वह व्यापार और वाणिज्य का सामंतीकरण की बात करते हैं। वह तर्क करते हैं कि उपमहाद्वीप के कुछ हिस्सों में 11वीं सदी में हल्का शहरी नवीनीकरण शुरू हुआ, और शहरी प्रक्रियाएं 14वीं सदी तक अच्छी तरह स्थापित हो गई थीं।
- जैसा कि अध्याय 9 में उल्लेख किया गया है, शहरी अवनति का परिकल्पना विभिन्न आधारों पर प्रश्नांकित किया जा सकता है। चट्टोपाध्याय (1986, 1997) ने तर्क किया है कि प्रारंभिक मध्यकालीन अवधि में कुछ शहरी केंद्रों का अवनति हुई, लेकिन अन्य ऐसे भी थे जो फलते-फूलते रहे, साथ ही कुछ नए भी उभरे।
- शुआनजांग का सुझाव है कि कौशांबी, श्रावस्ती, वैशाली, और कपिलवस्तु जैसे शहर अवनति में थे। लेकिन वह थानेश्वर, वाराणसी, और कन्यकुब्जा जैसे फलते-फूलते शहरों का भी उल्लेख करते हैं। उस अवधि के बस्तियों पर पुरातात्विक डेटा असंगठित और अपर्याप्त है। लेकिन कुछ प्रारंभिक ऐतिहासिक शहर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में भी बसे रहे, जैसे अहीछात्र, अत्रांजिखेड़ा, राजघाट, और चिरंद।
- चट्टोपाध्याय ने इंडो-गंगेटिक विभाजन, ऊपरी गंगा बेसिन, और मालवा पठार से शिलालेखीय साक्ष्य भी प्रस्तुत किए हैं, विशेष रूप से पृथुदक (आधुनिक पेहोआ, करनाल जिला, हरियाणा), तत्तन-दापुर (आहर, बुलंदशहर के निकट, उत्तर प्रदेश), सियादोनी (ललितपुर, झाँसी जिला, मध्य प्रदेश के निकट), और गोपागिरी (ग्वालियर) स्थलों पर।
प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में व्यापार और मौद्रिक इतिहास

मौद्रिक इतिहास:
- जॉन एस. डेयेल के शोध से पता चलता है कि प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में धन की कमी नहीं थी, और राज्यों को वित्तीय संकटों का सामना नहीं करना पड़ा। हालांकि सिक्कों के प्रकारों में कमी आई और सिक्कों की सौंदर्य गुणवत्ता में गिरावट आई, लेकिन चलन में सिक्कों की मात्रा स्थिर रही। डेयेल का तर्क है कि सिक्कों की गिरावट वित्तीय या आर्थिक संकट का संकेत नहीं थी। इसके बजाय, यह सीमित कीमती धातुओं की आपूर्ति के समय सिक्कों की बढ़ती मांग को दर्शा सकता है। उत्तरी भारत में लगभग 1000 ईस्वी (कुछ क्षेत्रों में 750 ईस्वी के रूप में पहले) के आसपास चांदी की निरंतर कमी का सामना करना पड़ा, जिसके कारण सिक्कों में चांदी की मात्रा को घटाना आवश्यक हो गया।
व्यापारिक अंतःक्रियाएँ:
- भारतीय उपमहाद्वीप के व्यापारी एक व्यापक व्यापार नेटवर्क का हिस्सा थे, जो अफ्रीका, यूरोप और एशिया के विभिन्न हिस्सों को जोड़ता था। 7वीं शताब्दी के बाद, अरबों ने उत्तरी अफ्रीका, भूमध्य सागर, मध्य एशिया और सिंध में अपने राजनीतिक नियंत्रण का विस्तार किया। इसने उन्हें भारतीय महासागर व्यापार पर रणनीतिक नियंत्रण प्रदान किया। अरब आक्रमणों और उमय्यद तथा अब्बासिद खलीफाओं की स्थापना ने अरब व्यापारियों को यूरोप को पूर्वी एशिया से जोड़ने वाले व्यापार मार्गों में प्रमुख खिलाड़ियों के रूप में स्थापित किया।
समुद्री व्यापार:
- 9वीं शताब्दी के 'अहबार अस-सिन वा’l-हिंद' जैसे ग्रंथों में अरब व्यापारियों द्वारा ओमान से केरल के क्विलोन (कोल्लम) और फिर चीन तक की लंबी समुद्री यात्राओं का वर्णन है। 11वीं शताब्दी तक, भारतीय महासागर व्यापार छोटे मार्गों में विभाजित हो गया, जिसमें इन खंडों के जंक्शनों पर व्यापार केंद्र उभरे। उल्लेखनीय व्यापार केंद्रों में अदन, होर्मुज, कंबे, कालीकट, सातगाँव, मलक्का, ग्वांगझू और क्वांझौ शामिल थे। एशियाई व्यापार में रेशमी वस्त्र, चीनी मिट्टी, चंदन और काली मिर्च जैसे वस्त्र महत्वपूर्ण थे, जिन्हें धूप, घोड़े, हाथी दांत, कपास के कपड़े और धातु उत्पादों जैसी वस्तुओं के लिए अदला-बदली किया गया। भारत की समुद्री नेटवर्क चीन और पूर्वी एशिया की ओर उन्मुख थी, जिसमें श्रीलंका भारतीय महासागर व्यापार में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में कार्य करता था।
निर्यात में परिवर्तन
- 11वीं सदी से पहले, भारत मुख्यतः वस्त्र और मसालों जैसे लक्जरी वस्तुओं का निर्यात करता था। 11वीं सदी के बाद, निर्यात में चीनी, कपास के कपड़े, चमड़े के सामान और हथियार भी शामिल हो गए।
पैसे और विनिमय पत्रों का उपयोग
- 7वीं से 12वीं सदी के बीच पश्चिमी भारत में पाए गए गडहिया सिक्के व्यापार में पैसे के उपयोग को दर्शाते हैं। बड़ी लेनदेन को बिना नकद के सुविधा प्रदान करने के लिए हुंडिकास या विनिमय पत्रों का भी उपयोग किया गया।
शुल्क घर और व्यावसायिक कर
- शुल्क घरों (शुल्क-मंडपिकास) का उल्लेख करने वाले शिलालेखों से पता चलता है कि ये राज्य की आय के लिए व्यावसायिक करों के माध्यम से महत्वपूर्ण थे।
चौलुक्य प्रशासन में व्यापारियों की भूमिका
व्यापारी चौलुक्य राजवंश के प्रशासनिक ढांचे में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे, जैसे कि महामात्य (उच्च अधिकारी) और दंडाधिपति (पुलिस प्रमुख) जैसी महत्वपूर्ण नागरिक और सैन्य भूमिकाएँ निभाते थे। इस अवधि में पश्चिमी भारत के कई व्यापारी जैन धर्म के अनुयायी थे। जैन ग्रंथों, जैसे कि 11वीं सदी में जिनेश्वर सूरी द्वारा लिखित शट्स्थानकप्रकरण, ने उन नैतिक दिशानिर्देशों को स्पष्ट किया जिन्हें जैन व्यापारी अपनाने के लिए अपेक्षित थे।
- गुजरात के व्यापारी न केवल ज्ञान के प्रति अपने पोषण के लिए जाने जाते थे, बल्कि कविता, काव्यशास्त्र, दर्शन और व्याकरण जैसे क्षेत्रों में अपनी साहित्यिक योगदान के लिए भी प्रसिद्ध थे। हेमचंद्र, एक प्रमुख व्यक्ति जिन्होंने कई महत्वपूर्ण जैन ग्रंथों के साथ-साथ व्याकरण, छंद और दर्शन पर कार्य किए, एक व्यापारी के पुत्र थे जो धंधुका से थे।
- ये व्यापारी मंदिरों, कुंडों और जलाशयों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण दान देते थे, जिनका उल्लेख माउंट आबू और गिरनार के मंदिरों में देखा जा सकता है।
- क्षेत्र के शिलालेख भी बताते हैं कि व्यापारियों पर लगाए गए शुल्क और कर धार्मिक संस्थाओं के रखरखाव और उत्सवों के उत्सव के लिए पुनः निर्देशित किए जाते थे।
दक्षिण-पूर्व एशिया और चीन के साथ व्यापार
{ "error": { "message": "This model's maximum context length is 128000 tokens. However, your messages resulted in 190914 tokens. Please reduce the length of the messages.", "type": "invalid_request_error", "param": "messages", "code": "context_length_exceeded" } }

- चीन के राजनयिक मिशनों और भिक्षुओं द्वारा भारत में उपहार के रूप में लाए गए महत्वपूर्ण वस्त्रों में रेशम के कपड़े और वस्त्र शामिल थे। हालाँकि, 11वीं शताब्दी तक, चीनी पॉर्सेलिन ने भारत में एक प्रमुख आयात के रूप में रेशम को पार कर लिया।
प्रारंभिक मध्यकालीन काल में चीन और भारत के बीच व्यापार
भारत से चीन के लिए आयात
- 11वीं शताब्दी के दौरान, चीन द्वारा भारत से आयात की गई वस्तुओं की श्रृंखला में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। इनमें विभिन्न प्रकार के सामान शामिल थे, जैसे:
- घोड़े
- धूप
- चंदन का लकड़ी
- घारू (Gharu) लकड़ी
- सापन (Sapan) लकड़ी
- मसाले
- गंधक
- कपूर
- हाथी दांत
- सीनाबार
- गुलाब जल
- गैंडे का सींग
- पचुक (Putchuck)
वस्तुओं का origen
- कुछ वस्तुएँ, जैसे धूप और गुलाब जल, फारसी खाड़ी क्षेत्र से उत्पन्न हुईं और भारतीय बंदरगाहों से पूर्व की ओर भेजी गईं। अन्य वस्तुएँ, जैसे विभिन्न मसाले और लकड़ियाँ, भारत से प्राप्त की गईं।
भारतीय वस्त्र
- 13वीं शताब्दी के अंत तक, भारतीय वस्त्र भारत से चीन के लिए सबसे महत्वपूर्ण निर्यातों में से एक बन गए थे।
व्यापार मार्गों में परिवर्तन
- चीन और भारत के बीच बढ़ते व्यापार ने व्यापार मार्गों के पुनः-निर्देशन का कारण बना। 8वीं शताब्दी से, भारत और चीन के बीच समुद्री मार्गों का उपयोग भूमि मार्गों की तुलना में अधिक बार किया जाने लगा।
समुद्री मार्ग
एक प्रमुख समुद्री मार्ग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से होकर गुजरा। एक अन्य मार्ग बंगाल की खाड़ी के बंदरगाहों से होते हुए सुमात्रा और दक्षिण चीन सागर की ओर गया।
तकनीकी उन्नति
- समुद्री मार्गों की बढ़ती प्राथमिकता आंशिक रूप से समुद्री तकनीक में सुधार के कारण थी।
- सिलाई वाली जहाजों से अधिक टिकाऊ, नायल हुल वाले जहाजों की ओर बदलाव आया, जिससे समुद्री व्यापार की सुरक्षा और दक्षता में वृद्धि हुई।
व्यापार वस्तुओं का विविधीकरण
- प्रारंभिक मध्यकालिक भारत में व्यापार वस्तुओं और लिंक का विविधीकरण देखा गया।
- अय्यावोले गिल्ड की शिलालेखों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि लग्जरी वस्तुओं से बुनियादी सामानों की ओर ध्यान केंद्रित हुआ।
उद्भव व्यापार वस्तुएं
- रेशम, वस्त्र, रंग, प्रसंस्कृत लोहे, काली मिर्च और घोड़ों जैसी वस्तुओं का व्यापार में महत्व बढ़ा।
- 12वीं शताब्दी के मध्य में, शिलालेखों में दक्षिण भारत में पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से बड़ी मात्रा में वस्तुओं के आयात को रिकॉर्ड करना शुरू किया गया।
आयातित वस्तुएं
- कीमती पत्थर
- मोती
- खुशबू
- अरोमेटिक्स
- मायरोबालन
- शहद
- मोम
- वस्त्र, जिसमें रेशम शामिल है
- मसाले
- घोड़े
- हाथी
निर्यातित वस्तुएं
- कपास के वस्त्र
- मसाले, विशेष रूप से काली मिर्च
- लोहे
- रंग
- हाथी दांत
- पान
- पुटचुक
व्यापार गतिशीलता में बदलाव
- 13वीं शताब्दी के बाद, भारत का पश्चिमी तट व्यापार के लिए अधिक महत्वपूर्ण हो गया।
- क्विलोन (कोल्लम) जैसे बंदरगाहों ने महत्व प्राप्त किया, जहाँ चीनी युआन सम्राटों ने इस बंदरगाह पर मिशन भेजे।
व्यापार लिंक का विस्तार
- दक्षिण भारत और श्रीलंका में पश्चिमी बंदरगाहों की ओर बढ़ने से यह संकेत मिलता है कि भारतीय व्यापारिक संबंधों का विस्तार मिस्र और पश्चिम एशिया जैसे क्षेत्रों के साथ हुआ।
बंगाल की खाड़ी के बंदरगाहों की भूमिका
- जबकि प्रारंभिक मध्यकालीन समुद्री व्यापार चर्चाएँ अक्सर गुजरात और दक्षिण भारत पर केंद्रित होती हैं, बंगाल की खाड़ी के बंदरगाहों ने भी भूमिका निभाई, हालाँकि कम तीव्रता के साथ।
- तम्रलिप्ति (मेदिनीपुर जिले में टामलुक) 8वीं शताब्दी तक बंगाल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था।
- 8वीं शताब्दी ईस्वी के बाद, समंदर, जो संभवतः चिटगांग के निकट स्थित था, प्रमुखता में आया और इसे अक्सर अरब खातों में उल्लेखित किया गया।
व्यापार और सांस्कृतिक विनिमय
खलाकापट्ना
- पुरी जिले में कुशभद्र नदी पर स्थित, खलाकापट्ना 11वीं से 14वीं शताब्दी के बीच एक प्रमुख बंदरगाह था।
- खुदाई में चीनी सेलडन बर्तन, पारंपरिक चीनी मिट्टी, तांबे के सिक्के, और संभवतः पश्चिम एशिया से आए ग्लेज़ेड बर्तन मिले।
मनिकापट्ना
- चिल्का झील और बंगाल की खाड़ी को जोड़ने वाली नहर पर स्थित मनिकापट्ना ने प्रारंभिक ऐतिहासिक काल से 19वीं शताब्दी ईस्वी तक का सांस्कृतिक अनुक्रम प्रकट किया।
- खुदाई में चीनी मिट्टी के बर्तन, सेलडन बर्तन (दोनों असली और स्थानीय अनुकरण), और चीन के तांबे के सिक्के मिले।
व्यापारिक समुदायों का प्रवासन
- प्रारंभिक मध्यकालीन अवधि में विभिन्न व्यापारिक समुदायों का प्रवासन देखा गया।
- अरब और फारसी व्यापारी उन प्रारंभिक समूहों में से थे जो कोंकण, गुजरात, और मलाबार तटों पर बस गए।
- 875 ईस्वी के एक शिलालेख में मदुरै के राजा द्वारा अरबों के एक समूह को शरण देने का उल्लेख है, जो कोरोमंडल तट पर पहली अरब बस्ती को चिह्नित करता है।
- 13वीं शताब्दी में गुजरात में अरब जहाज मालिकों और व्यापारियों की उपस्थिति को दर्शाने वाले अरबिक शिलालेख कंबे, प्रभासपट्टन (सोमनाथ), जुनागढ़, और अनाहिलवाड़ा में पाए गए।
- इस अवधि में एक यहूदी समुदाय भी मलाबार क्षेत्र में स्थापित हुआ।
पश्चिम एशिया में राजनीतिक विकास का प्रभाव
पश्चिम एशिया में राजनीतिक परिवर्तनों, विशेष रूप से अरब विस्तार के कारण, ईसाइयों और ज़ोरोस्ट्रियन परसियों (पारसी) के केरल तट पर प्रवास को बढ़ावा मिला।
प्रारंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत में ऐतिहासिक प्रक्रियाएँ
दक्षिण भारतीय राज्यों की प्रकृति
- प्रारंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत की इतिहासलेखन विभिन्न विशिष्ट चरणों के माध्यम से विकसित हुआ है। Nilakantha Sastri उन प्रारंभिक विद्वानों में से थे जिन्होंने विभिन्न स्रोतों से बिखरे हुए आंकड़ों को एक समेकित ऐतिहासिक कथा में बुनने का प्रयास किया। हालांकि, उनकी कथा को राष्ट्रीयतावाद के पक्षपात और चोल राज्य की अत्यधिक केंद्रीकृत साम्राज्य के रूप में महिमा मंडित करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा।
- Burton Stein ने 1960 के दशक में पारंपरिक इतिहासलेखन की आलोचना की, जो चोल राज्य के समाज और अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से कृषि व्यवस्था के साथ संबंध पर केंद्रित था। उन्होंने तर्क किया कि पूर्व के विद्वानों ने चोल राज्य की शक्ति और केंद्रीकरण की प्रशंसा की, जबकि उन्होंने मजबूत स्थानीय स्व-शासन संस्थाओं को भी स्वीकार किया।
Stein का वैकल्पिक मॉडल
- पवित्र राजतंत्र: Stein ने प्रस्तावित किया कि दक्षिण भारतीय राजतंत्र पवित्र अधिकार पर आधारित था न कि नौकरशाही या संवैधानिक सिद्धांतों पर। राजाओं का प्रभावी शक्ति मुख्य रूप से उनके राजनीतिक केंद्रों के चारों ओर के क्षेत्रों में थी, जहाँ वे लोगों और संसाधनों पर नियंत्रण रख सकते थे।
- खंडित राज्य: राज्य को खंडित के रूप में देखा गया, जहाँ राजा अपने मुख्य क्षेत्रों के बाहर अनुष्ठानिक व्यक्तियों के रूप में कार्य करते थे। भूमि राजस्व सीमित क्षेत्रों से एकत्रित किया जाता था, और राज्य अपने पोषण के लिए लूट के अभियानों पर निर्भर करते थे।
- किसान समाज और किसान राज्य: Stein ने प्रारंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत के कार्य में किसान समाज और किसान राज्य की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने तर्क किया कि चोल राज्य में कोई नौकरशाही मशीनरी, स्थायी सेना, और महत्वपूर्ण राजस्व संग्रह प्रणाली नहीं थी।
Stein के मॉडल की आलोचना
- स्टाइन की चोल राज्य की आलोचना वैध थी, लेकिन प्रारंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारतीय राजशाही को पूरी तरह से पवित्र के रूप में प्रस्तुत करने की उनकी धारणा को चुनौती दी गई है। आलोचकों का तर्क है कि यह दृष्टिकोण चोलों जैसी राजवंशों की स्थायी शक्ति और सैन्य सफलताओं की अनदेखी करता है।
- चोल शक्ति का बढ़ा-चढ़ाकर वर्णन: पूर्व के विद्वानों ने चोल राज्य की शक्ति का बढ़ा-चढ़ाकर वर्णन किया था, लेकिन स्टाइन का वैकल्पिक दृष्टिकोण अपने ही चुनौतियों का सामना कर रहा था। उदाहरण के लिए, प्राचीन भारतीय राज्यों की नींव के रूप में लूट के अभियानों पर उनके जोर को questioned किया गया।
- विभिन्न राजनीतिक प्रणाली: स्टाइन के समुद्रगुप्त द्वारा सैन्य अभियानों और दक्षिण भारत में छोटे मवेशी लूटने वालों के उदाहरणों को विभिन्न प्रकार की राजनीतिक प्रणालियों का प्रतिनिधित्व करने के रूप में देखा गया। जबकि युद्ध और लूट प्राचीन और प्रारंभिक मध्यकालीन राजनीति के लिए महत्वपूर्ण थे, मौर्य, गुप्त, सतवाहन और चोल राजवंशों जैसी साम्राज्यों के निर्माण और टिकाव ने एक अधिक जटिल राजनीतिक परिदृश्य को दर्शाया।
साउथॉल ने एकात्मक और खंडित राज्य के बीच भेद किया:
- एकात्मक राज्य: एक राजनीतिक प्रणाली जिसमें केंद्रीय शक्ति का एकाधिकार होता है, जिसे परिभाषित भौगोलिक सीमाओं के भीतर एक विशेष प्रशासनिक स्टाफ द्वारा प्रयोग किया जाता है।
- खंडित राज्य: एक राजनीतिक प्रणाली जिसमें विशेषीकृत शक्ति एक पिरामिडीय श्रृंखला के खंडों के भीतर प्रयोग की जाती है। ये खंड उच्च स्तर के खंडों के प्रति उनके विरोध द्वारा एक साथ बंधे होते हैं और अंततः निकटवर्ती असंबंधित समूहों के खिलाफ उनके संयुक्त विरोध द्वारा परिभाषित होते हैं।
1. क्षेत्रीय संप्रभुता
- मान्यता प्राप्त लेकिन सीमित और सापेक्ष।
- राजनीतिक प्राधिकरण केंद्र के निकटतम सबसे मजबूत होता है और परिधि की ओर कमजोर होता है।
- परिधि अक्सर अनुष्ठानिक वर्चस्व में परिवर्तन अनुभव करती है।
2. केंद्रीकृत सरकार
केंद्रीय सरकार का अस्तित्व सीमित नियंत्रण के साथ परिधीय प्रशासनिक क्षेत्रों पर होता है।
3. प्रशासनिक स्टाफ
- केंद्र में विशेषीकृत प्रशासनिक स्टाफ होता है, जो परिधीय प्रशासनिक स्थलों पर छोटे पैमाने पर दोहराया जाता है।
4. बल का एकाधिकार
- केंद्रीय प्राधिकरण बल का एकाधिकार सीमित सीमा और सीमित रेंज के भीतर दावा करता है। परिधीय केंद्रों के पास भी वैध लेकिन सीमित प्रकार के बल होते हैं।
5. शक्ति के अधीनस्थ केंद्र
- कई स्तरों के अधीनस्थ केंद्रों का संगठन केंद्रीय प्राधिकरण के सापेक्ष पिरामिड संरचना में होता है।
- हर स्तर पर समान शक्तियाँ होती हैं, लेकिन दायरा घटता है। परिधीय प्राधिकरण केंद्रीय प्राधिकरण के छोटे संस्करण होते हैं।
6. परिधीय प्राधिकरणों की लचीलापन
- परिधीय प्राधिकरणों के पास विभिन्न शक्ति पिरामिडों के बीच वफादारी बदलने की अधिक लचीलापन होता है। विभाजित राज्य लचीले, परिवर्तनशील, और आपस में जुड़े होते हैं।
7. द्वंद्वात्मक संप्रभुता
- संप्रभुता में वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण और अनुष्ठानात्मक संप्रभुता शामिल होती है।
- कई केंद्र हो सकते हैं, जिनमें से कुछ राजनीतिक नियंत्रण का अभ्यास करते हैं और अन्य अनुष्ठानात्मक संप्रभुता प्रदान करते हैं।
8. विशेषीकृत प्रशासनिक स्टाफ
- केंद्र में विशेषीकृत प्रशासनिक स्टाफ के पास निचले खंडों में समकक्ष हो सकते हैं।
9. पिरामिडीय संगठन
- केंद्र और परिधीय शक्ति केंद्रों के बीच संबंध सभी मामलों में समान होता है।
- राज्य के हिस्सों के बीच और घटकों के भीतर पूरक विरोध होता है।
10. संविधानिक श्रेणी
- सेगमेंटरी राज्य एक वैचारिक श्रेणी है जिसमें शक्ति का विभाजन होता है। इसमें आलूर जनजातीय प्रणाली और मध्यकालीन यूरोपीय सामंतवादी राज्यों जैसे विविध राज्यों को शामिल किया गया है। साउथॉल ने सेगमेंटरी राज्यों की विभिन्न श्रेणियों की पहचान करने का सुझाव दिया।
प्रारंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत में प्रशासनिक संरचनाएँ
दक्षिण भारत के प्रारंभिक मध्यकालीन राज्यों की प्रशासनिक संरचना पहले से अधिक जटिल और सूक्ष्म थी। वे कुछ इतिहासकारों द्वारा सुझाई गई कमजोरी से नहीं थे, न ही अन्य लोगों द्वारा विश्वास की गई ताकत और केंद्रीकरण में थे। शाही दरबार महत्वपूर्ण अधिकारियों से घिरा हुआ था, जिन्होंने प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाईं।
- राजा को सलाहकारों और पुरोहितों, जैसे कि ब्राह्मण पुरोहित और चोल लेखों में राजगुरु द्वारा सहायता प्राप्त थी। पलवों और चेरों के अपने मंत्रियों की परिषद थी, जबकि पांड्यों के पास मंत्रियों (मंत्रियों) का एक समूह था जो संभवतः एक परिषद का गठन करते थे। अन्य उच्च पदस्थ अधिकारियों, जैसे कि अधिकारी, वायल केट्पर, और तिरुमंदिर-ओलाई, की भूमिकाएँ निश्चित नहीं थीं लेकिन वे राजा के साथ निकटता से जुड़े हुए थे।
प्रशासनिक संरचना का विस्तार
- कराशिमा, सुभरायालु, और मत्सुई के शोध से पता चलता है कि चोल लेखों में पलवों, पांड्यों, और चेरों की तुलना में कार्यालयों और अधिकारियों के लिए अधिक शब्द हैं। यह प्रशासनिक संरचना के विस्तार का संकेत देता है, विशेष रूप से राजा राजराजा I (985–1016) के शासनकाल के दौरान। हालाँकि, कुलोत्तुंगा I (1070–1122) के बाद, ऐसे संदर्भों में कमी आई, जो इस विस्तार में उलटफेर का सुझाव देती है।
अधिकारियों के शीर्षक और कार्य
प्रशासनिक कार्यालयों से जुड़े व्यक्तियों के विभिन्न उपाधियाँ थीं, जैसे कि अरैयान, जो महत्वपूर्ण लोगों के लिए एक सम्मानजनक उपाधि थी। कुछ अधिकारियों, जैसे कि उदयियन, वेलन, और मुवेंडवेलन, ज़मीन के मालिक थे और प्रशासन में विशेष भूमिकाएँ निभाते थे।
स्थानीय प्रशासन
- स्थानीय स्तर पर, अधिकारियों जैसे कि नाडु-वगाई, नाडु-काकानी-नायकम, नाडु-कुरु, और कोट्टम-वगाई के कार्य overlapping थे, और आधिकारिक नियुक्तियों में एक विरासती तत्व था।
- चोलों के पास एक भूमि राजस्व विभाग था, जो खातों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार था, जबकि राजस्व का आकलन और संग्रह कॉर्पोरेट निकायों जैसे कि उर, नाडु, सभा, और नगरम द्वारा तथा कभी-कभी स्थानीय मुखियाओं द्वारा किया जाता था।
भूमि सर्वेक्षण और आकलन
- राजराजा I के शासनकाल के दौरान, चोल राज्य ने भूमि सर्वेक्षण और आकलन की एक विशाल परियोजना शुरू की, जिससे साम्राज्य को वालानाडु के रूप में पुनर्गठित किया गया।
- पश्चात, कुलोत्तुंगा I के शासनकाल में सर्वेक्षण किए गए, और राजराजा के बाद के दौर में, राजस्व विभाग को पुरावु-वाड़ी-तिनैक्कलम या श्री-कारणम कहा जाता था।
प्रारंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत में भूमि राजस्व और कर
- दक्षिण भारत के प्रारंभिक मध्यकालीन काल से मिलने वाली लेखाएं राज्य द्वारा कृषकों पर लगाए गए विभिन्न दिव्याओं से संबंधित शर्तें प्रकट करती हैं। ये शर्तें गाँववालों के राज्य अधिकारियों को भोजन और श्रम सेवाएँ प्रदान करने की जिम्मेदारियों को दर्शाती हैं।
- Eccoru जैसे शर्तें गाँववालों की राज्य अधिकारियों के लिए भोजन प्रदान करने की जिम्मेदारी को संदर्भित करती थीं, जबकि Muttaiyal और vetti श्रम सेवाएँ प्रदान करने की जिम्मेदारी को इंगित करती थीं। Kudimai एक अन्य शब्द था जो ऐसी श्रम सेवाओं के लिए प्रयोग किया जाता था।
- प्रारंभिक चोल काल में, कई भूमि राजस्व की शर्तें प्रचलित थीं, जिनमें पुरावु, इरई, कदान/कनिक्कादान, और ओपाती शामिल थीं। हालाँकि, कडामाई बाद के चोल काल में सबसे महत्वपूर्ण भूमि राजस्व शब्द बन गया। इसका सटीक दर अनिश्चित है, लेकिन यह 40 से 50 प्रतिशत उत्पादन तक हो सकता है और संभवतः यह वस्तु के रूप में एकत्रित किया जाता था।
- अंतारयाम एक ग्रामीण कर था जो नकद में प्राप्त किया जाता था। लेखों में राजस्व की शर्तों की संख्या में ध्यान देने योग्य वृद्धि थी, जो राजेंद्र II (1052–63 ईस्वी) के शासनकाल में अपने चरम पर थी और कुलोत्तुंगा I के समय से घटने लगी।
सैन्य संगठन
- प्रारंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत के राजाओं द्वारा किए गए सैन्य अभियान एक प्रभावी सेना संगठन का सुझाव देते हैं, हालांकि इसके बारे में विवरण सीमित हैं।
- राजाओं और प्रमुखों के व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी अपने लार्ड्स के प्रति वफादारी और वंशानुगत संबंधों के माध्यम से जुड़े होते थे, और उन्हें संभवतः भूमि राजस्व कार्य सौंपे जाते थे।
- राज्य द्वारा कुछ प्रकार की स्थायी सेना बनाए रखी जाती थी, जिसमें सेनापति और दंडनायक जैसे महत्वपूर्ण सैन्य अधिकारी महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाते थे।
- चोल शिलालेखों में कई सैन्य टुकड़ियों का उल्लेख है, और जब आवश्यक होता था तो प्रमुखों से सैनिकों के समय-समय पर उठान से स्थायी सेना को मजबूत किया जाता था।
- राजाराजा I के शासनकाल के दौरान श्रीलंका के लिए किए गए अभियान और राजेंद्र I के शासनकाल के दौरान श्री विजय अभियान अक्सर चोल नौसेना के प्रमाण के रूप में उद्धृत किए जाते हैं।
- हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि क्या यह एक नियमित, अलग से भर्ती की गई नौसैनिक बल थी या सशस्त्र बलों को महासागरों के पार ले जाने के उदाहरण थे।
न्याय का प्रशासन
- शोधकर्ताओं ने इस अवधि के दौरान धर्मसना नामक एक केंद्रीय या शाही न्यायालय के अस्तित्व का सुझाव दिया है, जो इस विचार को दर्शाता है कि राजा अंतिम अपील का सर्वोच्च न्यायालय था।
- हालांकि, दिन-प्रतिदिन के न्याय प्रशासन को संभवतः विभिन्न स्थानीय निकायों, जैसे कि सभा, द्वारा संभाला जाता था।
|
183 videos|620 docs|193 tests
|















