वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव | भारतीय समाज (Indian Society) UPSC CSE PDF Download
वैश्वीकरण: एक जुड़े हुए आर्थिक और सामाजिक दुनिया का अर्थ
वैश्वीकरण से तात्पर्य है कि दुनिया भर में आर्थिक और सामाजिक परस्पर निर्भरता और आपसी संबंध बढ़ रहे हैं। यह विभिन्न देशों के एकीकरण को दर्शाता है, इस हद तक कि एक क्षेत्र में होने वाली घटना अन्य क्षेत्रों के लोगों को प्रभावित कर सकती है। यह प्रक्रिया अंतरराष्ट्रीय व्यापार, निवेश और सूचना प्रौद्योगिकी में उन्नति द्वारा संचालित होती है।
सरल शब्दों में, वैश्वीकरण इस बात का संदर्भ है कि विभिन्न देशों के लोग, संगठन और सरकारें एक-दूसरे के साथ कैसे बातचीत और एकीकरण करते हैं। यह देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और जानकारी के लिए बढ़ती निर्भरता को उजागर करता है।
परिचय
वैश्वीकरण एक ऐसा प्रक्रिया है जो बहुत समय से हो रही है, लेकिन इसे 20वीं सदी के दूसरे भाग में ही इस नाम से जाना गया।
वैश्वीकरण का इतिहास:
भारत, दो हजार वर्ष पूर्व, चीन, फारस, मिस्र और रोम जैसी महान सभ्यताओं के साथ सिल्क रूट के माध्यम से जुड़ा हुआ था।
- विभिन्न भागों से लोग भारत आए, व्यापारियों, विजेताओं और प्रवासियों के रूप में।
- दूरदराज के गांवों में लोग अक्सर अपने पूर्वजों को याद करते हैं जो विभिन्न स्थानों से आए और वर्तमान घरों में बस गए।
- यह आदान-प्रदान और संबंध बनाने की प्रक्रिया बहुत लंबे समय से चल रही है।
20वीं सदी में वैश्वीकरण:
20वीं सदी के दूसरे भाग में "वैश्वीकरण" शब्द का उपयोग इस प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किया गया।
- देशों ने निर्यात-उन्मुख विकास रणनीतियों और व्यापार उदारीकरण को अपनाना शुरू किया।
- राष्ट्रीय नीतियों, नीति-निर्माण तकनीकों और कार्यान्वयन रणनीतियों का वैश्वीकरण हुआ।
वैश्वीकरण के नकारात्मक पहलू:
वैश्वीकरण ने जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापमान वृद्धि और ओज़ोन परत के क्षय जैसे नकारात्मक परिणामों को भी जन्म दिया।
वैश्वीकरण के विभिन्न पहलू
- सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू:
वैश्वीकरण ने विभिन्न संस्कृतियों के लोगों को करीब लाया है। इससे लोगों के लिए अपनी संस्कृतियों, परंपराओं और जीवन शैलियों को साझा करना और मिलाना आसान हो गया है। हालांकि, इससे कभी-कभी अद्वितीय स्थानीय संस्कृतियों और परंपराओं का ह्रास भी हो सकता है। - प्रौद्योगिकी और संचार:
प्रौद्योगिकी और संचार में उन्नति ने वैश्वीकरण में बड़ा योगदान दिया है। इंटरनेट, स्मार्टफोन और अन्य तकनीकों ने दुनिया भर में लोगों और व्यवसायों के लिए तेजी से जुड़ने और जानकारी साझा करने को आसान बनाया है। - कॉर्पोरेट दुनिया:
वैश्वीकरण ने कंपनियों के संचालन के तरीके को बदल दिया है। अब कई कंपनियों का कई देशों में अस्तित्व है, जो विभिन्न बाजारों और संसाधनों का लाभ उठाती हैं। इससे बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उदय हुआ है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। - अंतरराष्ट्रीय व्यापार, संबंध, और अर्थव्यवस्था:
वैश्वीकरण ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाया है, जिससे देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं की खरीद-फरोख्त करना आसान हो गया है। यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों को भी प्रभावित करता है, क्योंकि देश एक-दूसरे पर संसाधनों और बाजारों के लिए अधिक निर्भर हो रहे हैं।
वैश्वीकरण के पीछे की प्रेरणाएँ:
- प्रौद्योगिकी:
प्रौद्योगिकी ने संचार की गति को तेजी से बढ़ा दिया है। सोशल मीडिया का उदय भौगोलिक दूरी को लगभग अप्रासंगिक बना देता है। - LPG सुधार:
1991 में भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (LPG) के सुधारों ने देश की आर्थिक खुलापन बढ़ा दिया, जिससे वैश्विक समुदाय के साथ अधिक बातचीत हुई। - तेज परिवहन:
परिवहन में उन्नति, विशेष रूप से हवाई यात्रा की तेजी से वृद्धि, ने वैश्विक यात्रा को आसान और तेज बना दिया है। - WTO और बहुपक्षीय संगठनों का उदय:
1994 में विश्व व्यापार संगठन (WTO) की स्थापना ने वैश्विक स्तर पर टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करने में योगदान दिया। - पूंजी की बेहतर गतिशीलता:
पूंजी बाधाओं में सामान्य कमी आई है, जिससे विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के बीच पूंजी का प्रवाह आसान हुआ है। - बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उदय:
विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में काम कर रही बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रसार किया है।
निष्कर्ष:
ये कारक आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जिससे दुनिया एक "वैश्विक गाँव" में विकसित हो रही है।
वैश्वीकरण में योगदान करने वाले कारक
- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT):
टेलीफोन संचार से केबल और सैटेलाइट डिजिटल संचार में परिवर्तन ने सूचना प्रवाह में वृद्धि की है। समय-स्थान संकुचन उस घटना को दर्शाता है जहाँ दूरस्थ स्थानों पर लोग तात्कालिकता से संचार करने की क्षमता के कारण एक-दूसरे के करीब महसूस करते हैं। - आर्थिक कारक:
वैश्विक अर्थव्यवस्था एक पोस्ट-औद्योगिक चरण में बदल गई है, जिससे यह अधिक "वजनहीन" हो गई है। इसका मतलब है कि उत्पाद अधिकतर सूचना-आधारित या इलेक्ट्रॉनिक हैं, जैसे कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर, फिल्में, संगीत, और सूचना सेवाएँ। - राजनीतिक परिवर्तन:
1990 के दशक में साम्यवाद का पतन विभाजित शीत युद्ध के युग का अंत था। पूर्व साम्यवादी देशों ने तब लोकतंत्र की ओर बढ़ते हुए वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकृत किया।
वैश्वीकरण: भारत पर प्रभाव
- दीर्घकालिक वृद्धि को बढ़ावा:
वैश्वीकरण देश की अर्थव्यवस्था की दीर्घकालिक औसत वृद्धि दर को बढ़ाता है। - विदेशी पूंजी और तकनीक को आकर्षित करना:
यह विदेशी पूंजी और उन्नत तकनीक के प्रवेश को प्रोत्साहित करता है। - उत्पादन और व्यापार का पुनर्गठन:
वैश्वीकरण श्रम-गहन वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार में वृद्धि करता है। - वित्तीय क्षेत्र में सुधार:
यह बैंकों, बीमा और वित्तीय क्षेत्रों की दक्षता में सुधार करता है। - जीवन स्तर को बढ़ाना:
वैश्वीकरण उपभोक्ताओं के लिए बेहतर जीवन स्तर और खरीदारी की शक्ति में योगदान करता है। - कीमतों और गुणवत्ता में सुधार:
विकासशील देशों में घरेलू उद्योग अधिक प्रतिस्पर्धी बन जाते हैं।
वैश्वीकरण: चुनौतियाँ
- वैश्वीकरण 4.0 के मिश्रित परिणाम:
हाल के वैश्वीकरण के चरण में तकनीक और विचारों के आंदोलन ने सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम उत्पन्न किए हैं। - छोटे उद्योगों के लिए खतरा:
यह छोटे और गांवों के उद्योगों के लिए खतरा पैदा करता है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में कठिनाई महसूस करते हैं। - कृषि पर प्रभाव:
विकासशील देशों में, वैश्वीकरण कृषि को खतरे में डालता है। - नौकरी का विस्थापन:
हालांकि वैश्वीकरण रोजगार के अवसर बढ़ाने का दावा करता है, कुछ विकासशील देशों में तकनीकी परिवर्तन के कारण नौकरी में कमी आई है। - आर्थिक शक्ति का पुनर्वितरण:
यह आर्थिक शक्ति का पुनर्वितरण करता है, जिससे अमीर देशों का गरीब देशों पर वर्चस्व बढ़ता है। - संस्कृति का क्षय:
वैश्वीकरण ने आतंकवाद, मानव और मादक पदार्थों की तस्करी, संगठित अपराध, और महामारी जैसी समस्याओं को जन्म दिया है।
संस्कृति की गतिशीलता: समरूपता और ग्लोकलाइजेशन के बीच नेविगेट करना
- समरूपता:
कुछ लोग मानते हैं कि सभी संस्कृतियाँ समान और समान हो रही हैं। - ग्लोकलाइजेशन:
दूसरों का तर्क है कि संस्कृतियाँ वैश्विक तत्वों को स्थानीय परंपराओं के साथ मिश्रित कर रही हैं।
रिट्जर का वैश्वीकरण का सिद्धांत:
सामाजिक विज्ञानी रिट्जर ने "वैश्वीकरण" शब्द का उपयोग उन संगठनों और देशों के लिए किया जो वैश्विक स्तर पर विस्तार करने का प्रयास कर रहे हैं।
ग्लोकलाइजेशन को समझना:
ग्लोकलाइजेशन में वैश्विक और स्थानीय संस्कृतियों का मिश्रण होता है।
भारत में ग्लोकलाइजेशन के उदाहरण:
- विदेशी टीवी चैनल:
चैनलों ने स्थानीय दर्शकों को आकर्षित करने के लिए भारतीय भाषाओं का उपयोग किया। - मैकडॉनल्ड्स:
भारत में शाकाहारी और चिकन उत्पाद पेश किए जाते हैं। - संगीत:
'भंगड़ा पॉप' और 'इंडी पॉप' जैसे संगीत शैलियों का उदय।
संस्कृति का परिवर्तन और वैश्वीकरण:
संस्कृति स्थिर नहीं है; यह सामाजिक परिवर्तनों के साथ विकसित होती है। वैश्वीकरण नए स्थानीय और वैश्विक परंपराओं को उत्पन्न करने की संभावना रखता है।
वैश्वीकरण में भारत का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव:
वैश्वीकरण, तकनीकी, संचार और परिवहन में उन्नति द्वारा सुविधाजनक किया गया है।
भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:
- सकारात्मक:
- आर्थिक विकास और बाजार विस्तार। - नकारात्मक:
- नौकरी और सामाजिक असुरक्षा।
भारतीय समाज पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव:
- तनाव और असुरक्षा:
वैश्वीकरण के कारण प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। - आधुनिकता के प्रभाव:
परंपरागत मूल्यों का ह्रास।
कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव:
- सकारात्मक:
- राष्ट्रीय आय में वृद्धि और नई तकनीकों का उपयोग। - नकारात्मक:
- छोटे उत्पादन क्षेत्रों का दबाव।
अनौपचारिक क्षेत्र पर वैश्वीकरण का प्रभाव:
- श्रम की अनौपचारिकता बढ़ी है।
- महिलाएँ अक्सर निम्नतम आय स्तर पर धकेली जाती हैं।
परिवार पर वैश्वीकरण का प्रभाव:
- संयुक्त परिवार प्रणाली में कमी।
- परिवारों में पारंपरिक प्रथाओं का ह्रास।
शादी पर वैश्वीकरण का प्रभाव:
- प्रेम विवाह की वृद्धि।
- विवाह का महत्व घट रहा है।
खाद्य और त्योहारों पर वैश्वीकरण का प्रभाव:
- फास्ट फूड चेन का उदय।
- परंपरागत त्योहारों के साथ नए अवसरों का उदय।
शिक्षा पर वैश्वीकरण का प्रभाव:
- वैश्वीकरण ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है।
- शिक्षा की लागत बढ़ी है।
जाति प्रणाली पर वैश्वीकरण का प्रभाव:
- जाति प्रणाली में कुछ ढील आई है।
- अन्यथा जाति व्यवस्था अभी भी मौजूद है।
महिलाओं पर वैश्वीकरण का प्रभाव:
- महिलाओं के लिए अवसर बढ़े हैं।
- हालांकि, कई महिलाएँ निम्न-भुगतान वाली नौकरियों में फंसी हुई हैं।
युवाओं पर वैश्वीकरण का प्रभाव:
- युवाओं में पारंपरिक मूल्यों से दूर जाने की प्रवृत्ति।
- शिक्षा और कौशल पर जोर।
वैश्वीकरण की नैतिक चुनौतियाँ:
- असमानता में वृद्धि।
- मानवाधिकार मुद्दे।
वैश्वीकरण के राजनीतिक परिवर्तन:
- अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहयोग में वृद्धि।
- गुणवत्ता शासन की अवधारणा का विकास।
उपसंहार:
वैश्वीकरण ने भारत के सामाजिक, आर्थिक, और सांस्कृतिक ढांचे को गहराई से प्रभावित किया है। यह एक ऐसा प्रक्रिया है जो अवसरों और चुनौतियों दोनों को लेकर आती है।
वैश्वीकरण ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया है, जिससे देशों के लिए एक-दूसरे से सामान और सेवाएँ खरीदना और बेचना आसान हो गया है। यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों को भी प्रभावित करता है, क्योंकि देश संसाधनों और बाजारों के लिए एक-दूसरे पर अधिक निर्भर हो जाते हैं। यह आपसी संबंध दुनिया भर के देशों के लिए अवसरों और चुनौतियों दोनों का कारण बन सकता है।
- वैश्वीकरण ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाया है, जिससे देशों के लिए एक-दूसरे से सामान और सेवाएँ खरीदना और बेचना आसान हो गया है।
- यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों को भी प्रभावित करता है, क्योंकि देश संसाधनों और बाजारों के लिए एक-दूसरे पर अधिक निर्भर हो जाते हैं।
वैश्वीकरण के पीछे के प्रेरक तत्व: एक वैश्विक गाँव का निर्माण करने वाले उत्प्रेरक
तकनीक
तकनीक ने संचार की गति को क्रांतिकारी रूप से बढ़ा दिया है। सोशल मीडिया के उदय ने भौगोलिक दूरी को लगभग अप्रासंगिक बना दिया है।
वैश्वीकरण के पीछे के प्रेरक तत्व: एक वैश्विक गाँव का निर्माण करने वाले उत्प्रेरक
- LPG सुधार - भारत में 1991 में हुए उदारीकरण, निजीकरण, और वैश्वीकरण (LPG) सुधारों ने देश की आर्थिक खुलापन को बढ़ाया, जिससे वैश्विक समुदाय के साथ अधिक बातचीत हुई।
- तेज परिवहन - परिवहन में प्रगति, विशेष रूप से हवाई यात्रा की तीव्र वृद्धि, ने वैश्विक यात्रा को आसान और तेज बना दिया, जिससे लोगों और सामानों का आंदोलन सुगम हुआ।
- WTO और बहुपक्षीय संगठनों की वृद्धि - 1994 में विश्व व्यापार संगठन (WTO) की स्थापना ने वैश्विक स्तर पर शुल्क और गैर-शुल्क बाधाओं को कम करने में योगदान दिया। इसने विभिन्न देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौतों की वृद्धि को भी बढ़ावा दिया।
- पूंजी की बढ़ती गतिशीलता - पूंजी बाधाओं में सामान्य कमी आई है, जिससे विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के बीच पूंजी का प्रवाह आसान हुआ है। इससे कंपनियों की वित्तपोषण तक पहुँच बढ़ी है और वैश्विक वित्तीय बाजारों का आपसी जुड़ाव बढ़ा है।
- बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs) की वृद्धि - विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में काम करने वाली MNCs ने सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं का प्रसार किया है। वे वैश्विक स्तर पर संसाधन प्राप्त करते हैं और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उत्पाद बेचते हैं, जिससे स्थानीय बातचीत बढ़ती है।
वैश्वीकरण में योगदान करने वाले कारक: सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT)
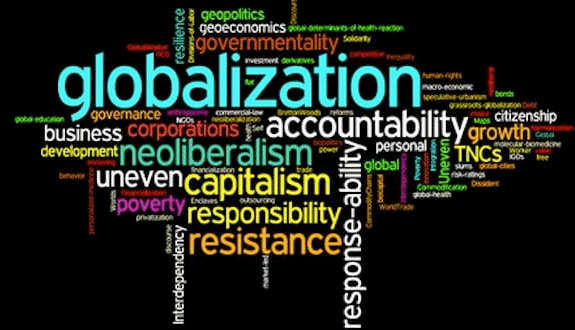
वैश्वीकरण में योगदान देने वाले कारक: सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT)
- टेलीफोन संचार से केबल और उपग्रह डिजिटल संचार में परिवर्तन ने सूचना के प्रवाह में वृद्धि की है।
- समय-स्थान संकुचन उस परिघटना को संदर्भित करता है जहाँ दूरस्थ स्थानों पर लोग तात्कालिक संचार की क्षमता के कारण एक-दूसरे के करीब महसूस करते हैं।
वैश्विक अर्थव्यवस्था एक उत्तर औद्योगिक चरण में स्थानांतरित हो गई है, जिससे यह increasingly "भारहीन" हो गई है। इसका अर्थ है कि उत्पाद अधिकतर सूचना आधारित या इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर, फ़िल्में, संगीत, और सूचना सेवाएँ, न कि ठोस वस्तुएँ जैसे खाद्य, वस्त्र या वाहन। इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण का एक मूलभूत प्रेरक तत्व है। यह बैंकों, कॉर्पोरेशनों, फंड प्रबंधकों, और व्यक्तियों को बड़ी मात्रा में धन को एक क्लिक में सीमा पार तात्कालिक रूप से स्थानांतरित करने की अनुमति देती है।
- वैश्विक अर्थव्यवस्था एक उत्तर औद्योगिक चरण में स्थानांतरित हो गई है, जिससे यह increasingly "भारहीन" हो गई है। इसका अर्थ है कि उत्पाद अधिकतर सूचना आधारित या इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर, फ़िल्में, संगीत, और सूचना सेवाएँ, न कि ठोस वस्तुएँ जैसे खाद्य, वस्त्र या वाहन।
- इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण का एक मूलभूत प्रेरक तत्व है। यह बैंकों, कॉर्पोरेशनों, फंड प्रबंधकों, और व्यक्तियों को बड़ी मात्रा में धन को एक क्लिक में सीमा पार तात्कालिक रूप से स्थानांतरित करने की अनुमति देती है।
1990 के दशक में साम्यवाद का पतन विभाजित शीत युद्ध की दुनिया के अंत को चिह्नित करता है। पूर्व कम्युनिस्ट देशों ने तब से लोकतंत्रों में संक्रमण किया है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकृत हुए हैं। अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय शासन तंत्रों जैसे कि संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ का विस्तार, इन निकायों से उत्पन्न अंतरराष्ट्रीय निर्देशों और कानूनों के द्वारा राष्ट्र-राज्यों पर बढ़ती सीमाओं का कारण बना है।
- 1990 के दशक में साम्यवाद का पतन विभाजित शीत युद्ध की दुनिया के अंत को चिह्नित करता है। पूर्व कम्युनिस्ट देशों ने तब से लोकतंत्रों में संक्रमण किया है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकृत हुए हैं।
वैश्वीकरण 4.0 के मिश्रित परिणाम: प्रौद्योगिकी और विचारों, लोगों और वस्तुओं की गति द्वारा संचालित वैश्वीकरण का नवीनतम चरण सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम लाता है। जबकि देश अधिक जुड़े हुए हैं, राजनीतिक संकट और वैश्विक संघर्ष भी बढ़ गए हैं।
- छोटी उद्योगों के लिए खतरा: वैश्वीकरण छोटे गाँव और लघु उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण खतरा प्रस्तुत करता है, जो संगठित बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs) के साथ प्रतिस्पर्धा करने में संघर्ष करते हैं।
- कृषि पर प्रभाव: विकासशील और अविकसित देशों में, वैश्वीकरण कृषि को खतरे में डालता है। WTO व्यापार प्रावधान कृषि बाजारों को विकसित देशों से सस्ते कृषि उत्पादों से भरने की अनुमति देते हैं, जो स्थानीय किसानों को कमजोर करते हैं।
- रोजगार विस्थापन: हालाँकि वैश्वीकरण यह विचार प्रस्तुत करता है कि प्रौद्योगिकी परिवर्तन और बढ़ी हुई उत्पादकता अधिक नौकरियों और उच्च वेतन का निर्माण करेगी, वास्तव में, कुछ विकासशील देशों ने प्रौद्योगिकी परिवर्तनों के कारण नौकरी के नुकसान का अनुभव किया है, जिससे रोजगार वृद्धि दर में कमी आई है।
- आर्थिक शक्ति का पुनर्वितरण: वैश्वीकरण आर्थिक शक्ति के पुनर्वितरण की ओर ले जाता है, जो अक्सर गरीब देशों पर आर्थिक रूप से शक्तिशाली देशों के प्रभुत्व का परिणाम होता है।
- असभ्य समाज का उदय: वैश्वीकरण ने आतंकवाद, मानव और मादक पदार्थों की तस्करी, संगठित अपराध, समुद्री डकैती, और कोविड-19 जैसे महामारी रोगों जैसे अंतरराष्ट्रीय मुद्दों के उदय को सुविधाजनक बनाया है, जो राज्य संस्थानों और नागरिक समाज को खतरे में डालते हैं।
- मानव तस्करी: वैश्वीकरण का एक सबसे अंधेरा पक्ष मानव तस्करी है, जहाँ व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों, को वस्तुओं के रूप में देखा जाता है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचा जाता है।
वैश्वीकृत युग में सांस्कृतिक पुनरुद्धार: योग, आयुर्वेद, धर्म, और हस्तशिल्प पर प्रभाव
वैश्विक युग में सांस्कृतिक पुनरुत्थान: योग, आयुर्वेद, धर्म और हस्तशिल्प पर प्रभाव
- योग का पुनरुत्थान: भारत और वैश्विक स्तर पर योग में रुचि में वृद्धि हुई है। यह रविशंकर के ‘आर्ट ऑफ लिविंग’ पाठ्यक्रम जैसे कार्यक्रमों की लोकप्रियता और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के वैश्विक उत्सव से स्पष्ट है।
- आयुर्वेद का पुनरुत्थान: आयुर्वेदिक चिकित्सा को बढ़ती मान्यता और मांग मिल रही है, जो भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखी जा रही है।
- धार्मिक पुनरुत्थानवाद: वैश्वीकरण से जुड़े बढ़ते अनिश्चितताओं के बीच, धार्मिक पुनरुत्थानवाद में वृद्धि हो रही है। यह राजनीतिक आंदोलनों और मतदाता आकर्षण के लिए धर्म के उपयोग में देखा जा रहा है।
- स्थानीय हस्तशिल्प की मांग: चिकनकारी और बांधनी जैसे स्थानीय हस्तशिल्प उत्पादों के लिए वैश्विक मांग बढ़ रही है।
- स्थानीय विविधता का संरक्षण: वैश्विक पर्यटन में वृद्धि के साथ, स्थानीय समुदाय अपनी विविध संस्कृतियों को संरक्षित करने और पारंपरिक प्रथाओं को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं।
- सांस्कृतिक मिश्रण: जबकि पश्चिमी संस्कृति भारतीय संस्कृति को प्रभावित कर रही है, यह इसे प्रतिस्थापित नहीं कर रही है। इसके बजाय, दोनों संस्कृतियों का मिश्रण हो रहा है, जो एक अद्वितीय सांस्कृतिक संलयन का निर्माण कर रहा है।
- रोज़गार और सामाजिक असुरक्षा: वैश्वीकरण के कारण रोजगार असुरक्षाएं बढ़ी हैं, और सार्वजनिक क्षेत्र, जो नौकरी की सुरक्षा प्रदान करता है, दबाव में है।
- कृषि की अनदेखी: कृषि क्षेत्र, जो अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए महत्वपूर्ण है, सुधारों के बाद अनदेखा किया गया है, जिससे इसकी अर्थव्यवस्था में योगदान प्रभावित हुआ है।
- बाल श्रम में वृद्धि: सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिकाओं में कमी ने बाल श्रम में वृद्धि का कारण बना है क्योंकि कॉर्पोरेट संस्थाएं लाभ पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं।
- पूंजी-गहन प्रौद्योगिकियाँ: पूंजी-गहन प्रौद्योगिकियों को अपनाने से उच्च बेरोजगारी दर उत्पन्न हुई है, जो एक महत्वपूर्ण चुनौती बन गई है।
- सरकारी नियंत्रण का नुकसान: वैश्वीकरण ने भारतीय सरकार के लिए विदेशी मुद्रा समस्याओं का अस्थायी समाधान किया है, लेकिन इसके साथ ही स्थानीय उद्योग के नियंत्रण और सरकारी निगरानी की कीमत चुकानी पड़ी है।
- फास्ट-फूड श्रृंखलाओं का परिचय: मैकडॉनल्ड्स और केएफसी जैसी फास्ट-फूड श्रृंखलाओं के आगमन ने भारत में खाद्य विकल्पों के समरूपीकरण को बढ़ावा दिया है, जबकि पुराने रेस्तरां को इन नए प्रवेशकों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। पारंपरिक खाद्य विकल्पों को फास्ट फूड और चीनी व्यंजनों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है।
- वैश्वीकरण का त्योहारों पर प्रभाव: वैश्वीकरण ने त्योहारों के उत्सव पर भी प्रभाव डाला है, नए अवसर जैसे वैलेंटाइन डे और फ्रेंडशिप डे पारंपरिक त्योहारों के साथ समान उत्साह के साथ लोकप्रिय हो रहे हैं।
वैश्वीकरण और शिक्षा: शिक्षा भारत की वृद्धि और सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से जब देश वैश्विक ज्ञान अर्थव्यवस्था में अधिक एकीकृत हो रहा है।
वैश्वीकरण और शिक्षा
शिक्षा भारत के विकास और सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, विशेषकर जब देश वैश्विक ज्ञान अर्थव्यवस्था में अधिक एकीकृत हो रहा है।
वैश्वीकरण और जाति प्रणाली
वैश्वीकरण और जाति प्रणाली
- हालांकि बदलाव हुए हैं, जाति प्रणाली अभी भी मजबूत बनी हुई है और यह भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता बनी हुई है।
- वैश्वीकरण ने कमजोर जातियों को अनौपचारिक क्षेत्र की ओर धकेल दिया है, जहाँ उन्हें कौशल की कमी के कारण निम्न श्रेणी के काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
- अछूतपन का प्रचलन, वैश्वीकरण के बावजूद, भारत में अभी भी विद्यमान है।
वैश्वीकरण और युवा के लाभ:
वैश्वीकरण और युवा लाभ:
वैश्वीकरण प्रक्रिया: नैतिक चुनौतियाँ
वैश्वीकरण प्रक्रिया: नैतिक चुनौतियाँ
- ऐसा खाका तैयार करें जो स्थिरता और समावेशिता को प्राथमिकता देता हो, जबकि नए अवसरों का लाभ उठाता हो।
- सभी के लिए परिणामों में सुधार के लिए सार्वभौमिक और लक्षित रणनीतियों को आगे बढ़ाएं, यह सुनिश्चित करते हुए कि कमजोर जनसंख्या पीछे न रह जाए।
- सही शिक्षा, रोजगार और बुनियादी ढांचे के मिश्रण के साथ स्थानीय और क्षेत्रीय प्रणालियों को मजबूत करें ताकि स्थानीय स्तर पर नौकरियों का सृजन और संरक्षण किया जा सके।
भारत में श्रम पर वैश्वीकरण का प्रभाव
1991 के बाद, भारत सरकार (GoI) ने उदारीकरण, निजीकरण, और वैश्वीकरण (LPG) को अपनाने के लिए अपनी औद्योगिक नीति में संशोधन किया। इस बदलाव का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए खोलना और महत्वपूर्ण औद्योगिक परिवर्तन आरंभ करना था।
वैश्वीकरण का भारत में श्रम पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ा है, जो विभिन्न तरीकों से प्रकट हो रहा है:
- आर्थिक विकास: सुधारों ने भारत की GDP विकास दर को लगभग 2-3% से बढ़ाकर लगभग 7-8% कर दिया। इससे एक मजबूत निजी क्षेत्र और लाखों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए।
- नौकरी की गुणवत्ता: नौकरियों की वृद्धि के बावजूद, इन पदों की एक बड़ी संख्या अनौपचारिक है या समय के साथ खो गई है।
- विदेशी प्रतिस्पर्धा: बाजारों के खुलने और शुल्कों में कमी ने विदेशी वस्तुओं के प्रवाह को सुविधाजनक बनाया, जिसने भारतीय श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसरों पर नकारात्मक प्रभाव डाला।
- महिलाओं का रोजगार: वैश्वीकरण ने महिलाओं के लिए कार्य बल में भाग लेने के अवसर खोले हैं। उदार आर्थिक नीतियों को अपनाने वाले देशों में महिला श्रमिकों की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हालांकि, कई महिलाएं अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रही हैं, जो खराब श्रम स्थितियों से ग्रस्त है। जहां महिलाएं प्रमुखता से कार्यरत हैं, वे अक्सर श्रम-गहन, सेवा-उन्मुख, और कम वेतन वाली होती हैं।
- रोजगार में बदलाव: कुछ क्षेत्रों में, उदारीकरण ने नई रोजगार संभावनाओं के बिना नौकरी के नुकसान का कारण बना।
- उपठेकेदारी और नौकरी की असुरक्षा: बड़े कॉर्पोरेट संस्थाएं, जैसे कि ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस (TNCs) और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस (MNCs), ने उपठेकेदारी विक्रेता प्रणाली विकसित की है। यह प्रथा श्रमिकों के लिए नौकरी की असुरक्षा में योगदान करती है और श्रम कल्याण को खराब करती है, क्योंकि उनके हालात को लेकर अक्सर कोई निगरानी नहीं होती।
वैश्वीकरण का आदिवासी समुदायों पर प्रभाव
वैश्वीकरण का जनजातीय समुदायों पर प्रभाव
- वैश्वीकरण ने भारत में जनजातीय समुदायों पर गहरा प्रभाव डाला है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या का लगभग 8.6% बनाते हैं। जबकि वैश्वीकरण को अक्सर प्रगति और विकास से जोड़ा जाता है, कई जनजातीय लोगों के लिए, इसने बढ़ती कीमतों, नौकरी की असुरक्षा और अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल जैसी चुनौतियाँ लाई हैं।
- भूमि पर अधिकार का हनन एक प्रमुख मुद्दा है। भूमि जनजातीय जीवनयापन के लिए महत्वपूर्ण है, और वैश्वीकरण ने कई जनजातीय समुदायों को उनके पूर्वजों की भूमि से विस्थापित कर दिया है। यह प्रवृत्ति विभिन्न विकास परियोजनाओं, जैसे प्रमुख सिंचाई योजनाओं द्वारा संचालित होती है, जहां जनजातीय जनसंख्या अक्सर सबसे अधिक प्रभावित होती है। स्वतंत्रता के बाद, 16 मिलियन से अधिक लोगों को ऐसी परियोजनाओं के कारण विस्थापित किया गया है, जिनमें से एक महत्वपूर्ण संख्या जनजातीय पृष्ठभूमि से हैं।
- इसके अतिरिक्त, जनजातीय समुदायों का विस्थापन एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं, जैसे बाँधों और सड़कों के निर्माण, अक्सर जनजातीय परिवारों के बलात्कारी पुनर्वास की ओर ले जाते हैं, जिससे उनके पारंपरिक जीवन के तरीके और सांस्कृतिक प्रथाएँ बाधित होती हैं।
- वैश्वीकरण ने जनजातीय क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना के क्षय को भी बढ़ावा दिया है। कई क्षेत्र मुख्यधारा के विकास में भाग लेने के लिए आवश्यक संसाधनों और अवसंरचना की कमी का सामना कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप झारखंड, उत्तराखंड और बोडोलैंड जैसे स्थानों पर उप-राष्ट्रीय आंदोलनों का उदय हुआ है। ये आंदोलन अक्सर तेजी से बढ़ते वैश्वीकरण के सामने जनजातीय समुदायों की जरूरतों और अधिकारों की उपेक्षा के प्रति एक प्रतिक्रिया होते हैं।
- अधिकांश जनजातीय समुदायों के लिए बेहतर जीवन स्तर का वादा अक्सर इसके विपरीत परिणाम देता है। विकास के नाम पर बाजार की शक्तियों ने जनजातीय समुदायों की भलाई के मुकाबले लाभ को प्राथमिकता दी है, जिससे आजीविका और सुरक्षा का नुकसान हुआ है। इसने कई युवा जनजातीय महिलाओं को काम की तलाश में शहरी केंद्रों की ओर प्रवास करने पर मजबूर किया है, जहाँ उन्हें खराब जीवन स्थितियों, कम वेतन और बेईमान एजेंटों द्वारा शोषण का सामना करना पड़ता है।
संक्षेप में, जबकि वैश्वीकरण सकारात्मक परिवर्तनों को लाने की क्षमता रखता है, इसने भारत में जनजातीय समुदायों के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियाँ भी उत्पन्न की हैं। भूमि पर अधिकार का हनन, विस्थापन, अपर्याप्त अवसंरचना, और सांस्कृतिक क्षय के मुद्दे विकास के लिए एक अधिक समावेशी और न्यायसंगत दृष्टिकोण की आवश्यकता को उजागर करते हैं, जो जनजातीय लोगों के अधिकारों और आजीविका का सम्मान और संरक्षण करें।
वैश्वीकरण की तीसरी लहर को 1990 के आसपास शुरू होने का विश्वास है।
- वैश्वीकरण की तीसरी लहर को 1990 के आसपास शुरू होने का विश्वास है।
- प्रौद्योगिकी में आगे की प्रगति, विशेष रूप से इंटरनेट का प्रसार, विभिन्न उत्पादन चरणों के विश्वभर में फैलने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है।
- इससे आधुनिक सप्लाई चेन का उदय हुआ, जिससे कंपनियों को सस्ते क्षेत्रों में कार्यों को स्थानांतरित करके उत्पादन और सेवा वितरण की लागत को कम करने का अवसर मिला, जिसे ऑफशोरिंग कहा जाता है।
वैश्वीकरण 4.0, अपने पूर्ववर्तियों की तरह, मिश्रित परिणाम उत्पन्न कर सकता है, जिसमें एक ओर आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन और दूसरी ओर राजनीतिक संकट और आय असमानता में वृद्धि शामिल है।
- वैश्वीकरण 4.0, अपने पूर्ववर्तियों की तरह, मिश्रित परिणाम उत्पन्न कर सकता है, जिसमें एक ओर आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन और दूसरी ओर राजनीतिक संकट और आय असमानता में वृद्धि शामिल है।
- मिलेनियल्स के लिए, आर्थिक संभावनाएं अनिश्चित हैं, और भविष्य में रोजगार के अवसरों के लिए आवश्यक कौशल की कमी के बारे में चिंताएँ हैं।
- वैश्वीकरण 4.0 के लिए जानबूझकर तैयारी के बिना, इन मुद्दों के बिगड़ने का जोखिम है।
- 1990 के दशक में वैश्वीकरण की पिछली लहर ने कुछ देशों को गरीबी से बाहर निकाला।
- हालांकि, उन देशों और संयुक्त राज्य जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में आय असमानता बढ़ रही है।
- कम लागत वाले श्रम वाले देश आगामी वैश्वीकरण की लहर के लाभों की आशा कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा आधार स्थापित करने का जोखिम है जो पीढ़ियों के लिए असमानता को बढ़ावा दे सकता है।
- वैश्वीकरण 4.0 आय असमानता को बढ़ा सकता है जबकि समग्र धन को और अधिक उत्पन्न करते हुए।
नई अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय एकीकरण के रूपों को बढ़ावा देना जो जीवन के कई आयामों के विकास की अनुमति देते हैं जबकि आवश्यक पहलुओं को संरक्षित करते हैं।
- विश्व अर्थव्यवस्था को अधिक पूर्वानुमानित बनाने, कमजोरियों को कम करने, और मुक्त व्यापार प्रणाली को मजबूत करने के लिए सहयोग को बढ़ावा देना।
- ऐसे संगठनों और गठबंधनों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा सहनशील अवसंरचना के लिए गठबंधन, जो वैश्विक सतत विकास में योगदान करते हैं जबकि देशों के बीच समन्वय को बढ़ावा देते हैं।
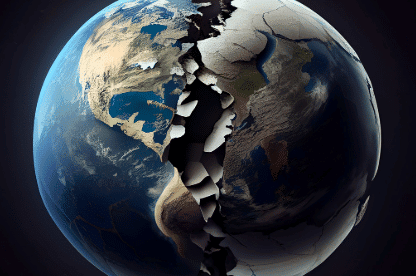
|
35 videos|72 docs
|
















