नैतिकता का सार, स्रोत, निर्धारक और परिणाम | यूपीएससी मेन्स: नैतिकता, सत्यनिष्ठा और योग्यता - UPSC PDF Download
नैतिकता का सार
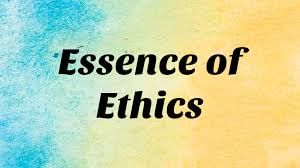
सार का अर्थ है किसी चीज़ की अंतर्निहित गुणवत्ता जो उसके चरित्र को परिभाषित करती है। नैतिकता का सार इसके गुण, महत्व और उन मौलिक गुणों से संबंधित है जो इसे परिभाषित करते हैं। नैतिकता के सार को परिभाषित करने वाले निम्नलिखित गुण/विशेषताएँ हैं:
- अच्छे/बुरे की परिभाषा: नैतिकता हमें विचारों, कार्यों और व्यवहारों की अच्छाई या बुराई का निर्धारण करने में मदद करती है।
- नैतिकता और समाज: नैतिकता एकांत में नहीं रह सकती। कोई व्यक्ति जन्म से नैतिक प्रणाली के साथ नहीं होता। इसके बजाय, समाज और संस्कृति जैसे वातावरण व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना के साथ मिलकर उनकी नैतिक समझ को आकार देते हैं। एक व्यक्ति एकांत में पैदा हो सकता है, लेकिन नैतिकता को समझने के लिए उन्हें समाज में जीना आवश्यक है।
- नैतिकता का आकार देना: जबकि नैतिकता व्यक्तियों को आकार देती है, व्यक्तियों भी नैतिकता को आकार देते हैं। उदाहरण के लिए, दासता और भेदभाव एक समय में सामाजिक रूप से स्वीकार्य थे, लेकिन महान व्यक्तित्वों के प्रभाव के कारण इनमें बदलाव आया।
- संदर्भ-निर्भर नैतिकता: नैतिकता उस संदर्भ से प्रभावित होती है जिसमें वे कार्य करती हैं और समय, स्थान और व्यक्तियों के अनुसार उनके अर्थ और तीव्रता में भिन्नता होती है। उदाहरण के लिए, यूरोप में सार्वजनिक स्थानों पर थूकना, मूत्र विसर्जन करना और कचरा फैलाना अनैतिक माना जाता है, लेकिन भारत में इसे उसी तरह नहीं देखा जा सकता।
- नैतिकता की व्यक्तिपरकता: नैतिकता व्यक्तिपरक होती है और किसी व्यक्ति की भावनाओं और धारणाओं से प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए, एक गुस्से में व्यक्ति अत्यधिक अनैतिक तरीके से कार्य कर सकता है, जैसे दंगे के दौरान। नैतिक विश्वासों पर संघर्ष भी गौ रक्षा और सम्मान हत्या जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है।
- नैतिकता और न्याय: नैतिकता समाज में व्याप्त न्याय की भावना से उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए, जब एक बच्चा दूसरे बच्चे को थप्पड़ मारता है, तो एक तीसरा बच्चा इसे अनैतिक मान सकता है, सामाजिक न्याय और सभी लोगों की समानता में विश्वास करते हुए, जैसा कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार (अनुच्छेद 21) में वर्णित है।
- कानून से परे नैतिकता: नैतिक मानक कानून के विशिष्ट नियमों और विनियमों से परे जा सकते हैं। कुछ कार्य अवैध नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अनैतिक हो सकते हैं, जैसे कि पुलिस का पीड़ितों की मदद करने से इनकार करना केवल इसलिए कि घटना उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर हुई।
- नैतिकता और जिम्मेदारी: नैतिकता एक जिम्मेदारी की भावना से बनाए रखी जाती है, न केवल बाहरी प्राधिकरण के प्रति उत्तरदायित्व के रूप में, बल्कि आंतरिक कर्तव्य की भावना के रूप में भी।
- नैतिकता का निर्दिष्ट स्वभाव: नैतिकता बताती है कि लोगों को कैसे व्यवहार करना चाहिए और हमें उस प्रकार के आचरण के बारे में बताती है जो अपेक्षित है। हालांकि, नैतिकता अक्सर बिना स्पष्टीकरण या कारण के प्रस्तुत की जाती है, जो लोगों के बीच उनके मूल्य और सम्मान को कम कर सकती है। उदाहरण के लिए, पारंपरिक पारिवारिक मूल्य कम हो रहे हैं क्योंकि उनके महत्व और तर्क को युवाओं के सामने ठीक से समझाया नहीं गया है।
- नैतिकता का वर्णात्मक स्वभाव: नैतिकता व्यक्तियों और समुदायों में मौजूदा व्यवहार के मानकों का भी अध्ययन करती है।
- नैतिकता में स्वैच्छिक क्रियाएँ: नैतिकता केवल स्वैच्छिक मानव क्रियाओं से संबंधित है, वे जो तब होती हैं जब व्यक्ति स्वतंत्र इच्छा से कार्य करता है, बिना किसी बल के। उदाहरण के लिए, यदि किसी को बंदूक की नोक पर अनैतिक कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो उन्हें नैतिक या अनैतिक कार्य करने वाला नहीं माना जाएगा, क्योंकि उनके कार्य स्वैच्छिक नहीं थे।
- नैतिकता के स्तर: नैतिकता विभिन्न स्तरों पर कार्य करती है, जिसमें व्यक्तिगत, संगठनात्मक, सामाजिक-सांस्कृतिक, राजनीतिक, और अंतरराष्ट्रीय स्तर शामिल हैं। हालांकि, एक स्तर पर नैतिकता अन्य स्तरों पर नैतिकता को प्रभावित कर सकती है।
- नैतिकता का मूल्यांकन: नैतिकता विभिन्न नैतिक मानदंडों, सिद्धांतों, कानूनों, मूल्यों और मानव आचरण के अन्य पहलुओं की जांच और मूल्यांकन करती है।
नैतिकता को प्रभावित करने वाले स्रोत/कारक
धर्म: धार्मिक ग्रंथ उन सवालों का जवाब देते हैं कि व्यक्तियों को कैसे व्यवहार करना चाहिए और समाज कैसा होना चाहिए। उदाहरण के लिए, जैन धर्म मांसाहारी भोजन को अनैतिक मानता है, जबकि इस्लाम में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है।
परंपराएँ और संस्कृति: विभिन्न संस्कृतियों में मूल्यों में भिन्नता होती है। उदाहरण के लिए, पश्चिमी संस्कृतियाँ व्यक्तिगतता पर जोर देती हैं, जबकि भारतीय संस्कृति परोपकारिता पर बल देती है।
कानून और संविधान: कानून और संविधान अक्सर उन नैतिक मानकों को दर्शाते हैं जिन्हें अधिकांश नागरिक मानते हैं।
नेतृत्व: समाज, संगठन, या राष्ट्र के नेता अपने अनुयायियों या प्रशंसकों के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, लोकतांत्रिक, उदार, धर्मनिरपेक्ष, और सहिष्णुता जैसे मूल्य आधुनिक भारतीय समाज को आकार देते हैं।
दर्शनशास्त्र: विभिन्न दार्शनिक और विचारक विभिन्न नैतिक ढांचे का समर्थन करते हैं।
भूगोल: भूगोल खाने की आदतों को प्रभावित कर सकता है, जैसे कि पश्चिम बंगाल में ब्राह्मण मछली का सेवन करते हैं (जो कि एक मांसाहारी आहार है) क्योंकि भूगोल ने ऐतिहासिक रूप से जीवित रहने के लिए मछली खाने की आवश्यकता को निर्धारित किया है।
आर्थिक कारक: साम्यवादी समाजों में लाभ लेना अनैतिक माना जाता है, जबकि पूंजीवादी समाजों में लाभ को नैतिक माना जाता है।
संस्थान: किसी संगठन के भीतर नैतिक मूल्य वहां काम करने वाले लोगों के व्यवहार को आकार देते हैं। उदाहरण के लिए, ISRO और DRDO के मूल्य उनके कर्मचारियों की नैतिकता को प्रभावित करते हैं।
समय: नैतिक मानक समय के साथ विकसित होते हैं। उदाहरण के लिए, 18वीं सदी की नैतिकता आज के नैतिकता से अलग है।
अनुभव: पिछले अनुभव नैतिकता को आकार देते हैं, जैसे कि कलिंग युद्ध ने अशोक के नैतिक दृष्टिकोण को प्रभावित किया।
लागत-लाभ विश्लेषण: उपयोगितावाद में कार्यों का मूल्यांकन उनके परिणामों के आधार पर किया जाता है, जो सबसे बड़े संख्या के लिए सबसे बड़े भले पर ध्यान केंद्रित करता है।
प्रेरणा: गांधी जैसे व्यक्तित्व नैतिक व्यवहार के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं, विशेष रूप से उनके अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों का पालन करने वालों के लिए।
शक्ति: सही या गलत अक्सर उन लोगों द्वारा निर्धारित होता है जो सत्ता में होते हैं, जैसे कि धार्मिक प्राधिकरण (जैसे, ब्राह्मण), आर्थिक नेता (जैसे, टाटा), और राजनीतिक व्यक्ति (जैसे, मोदी)।
शिक्षा: एक व्यक्ति के विचार और मूल्य उनकी शिक्षा से आकार लेते हैं, हालांकि नैतिकता और शिक्षा के बीच कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता।
मानव क्रियाओं में नैतिकता के निर्धारक
जानबूझकर मानव क्रिया: इसमें ज्ञान, स्वतंत्र इच्छा (चुनाव) और स्वेच्छा/इच्छा शामिल होती है।
- उद्देश्य: क्रिया के पीछे का उद्देश्य व्यक्तिगत, सामाजिक, या संगठनात्मक हो सकता है।
- वस्तु: क्रिया की वस्तु सकारात्मक, नकारात्मक, या तटस्थ हो सकती है, जो क्रिया की प्रकृति पर निर्भर करती है।
- मानव क्रिया की प्रकृति: यह क्रिया की अंतर्निहित विशेषताओं को संदर्भित करती है।
- परिस्थितियाँ: वह संदर्भ जिसमें क्रिया होती है, मांगलिक या सामान्य हो सकता है।
- परिणाम/अंत: क्रिया का परिणाम, जिसे उद्देश्यशास्त्र (उद्देश्य या अंत लक्ष्यों का अध्ययन) के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है।
- साधन: अंत को प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियाँ या दृष्टिकोण, जिन्हें नैतिकता (कर्तव्य और नैतिक सिद्धांतों का अध्ययन) के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है।
वास्तविक जीवन में विभिन्न निर्धारकों के बीच संबंध
- ओवरलैप: जब दो या दो से अधिक निर्धारक एक साथ काम करते हैं, जैसे कि एक कमजोर व्यक्ति के प्रति नागरिक अधिकारियों की सहानुभूति, जहाँ वस्तु की प्रकृति, उद्देश्य, परिणाम, और परिस्थितियाँ शामिल हैं।
- भिन्नता: नैतिक निर्णय संदर्भ के आधार पर भिन्न हो सकते हैं, जैसे कि भूख से मर रहे व्यक्ति को बचाने के लिए खाना चुराना बनाम सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत एक अधिकारी का चोरी करना।
- विरोधाभास: जब उद्देश्य और साधनों के बीच संघर्ष होता है, जैसे कि एक राजा की जान (उद्देश्य) को बचाने के लिए एक भिखारी को मारना (साधन), जो नैतिकता में विरोधाभास पैदा करता है।
मानव क्रियाओं में नैतिकता के परिणाम
- व्यक्तिगत स्तर पर:
- विश्वसनीयता: नैतिकता व्यक्तिगत विश्वास और इमानदारी को बढ़ाती है।
- आत्मविश्वास: नैतिक होना आत्म-विश्वास का निर्माण करता है।
- सामाजिक पूंजी: नैतिकता समुदाय में रिश्तों और विश्वास को मजबूत करती है।
- खुशी: नैतिक जीवन जीने से संतोष और कल्याण का अनुभव होता है।
- समाज के प्रति दृष्टिकोण तय करें: नैतिकता व्यक्ति के समाज के प्रति दृष्टिकोण और उसमें उनकी भूमिका को आकार देती है।
- अपने अस्तित्व की भावना को बढ़ाएँ: नैतिक व्यवहार व्यक्तिगत विकास और उद्देश्य की गहरी भावना को बढ़ावा देता है।
- निर्णय लेना: नैतिकता सही और नैतिक विकल्प बनाने के लिए एक ढांचा प्रदान करती है।
- संगठनात्मक स्तर पर:
- ब्रांड गुणवत्ता: नैतिकता एक ब्रांड की प्रतिष्ठा और गुणवत्ता में योगदान करती है।
- कर्मचारी-नियोक्ता संबंध: नैतिकता नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच विश्वास और सम्मान को बढ़ावा देती है।
- हितधारक संबंध: नैतिक व्यवहार हितधारकों के साथ निष्पक्ष और जिम्मेदार लेन-देन सुनिश्चित करता है।
- सामाजिक स्तर पर:
- लालच का अभाव: नैतिकता निष्पक्षता को बढ़ावा देती है और लालच के हानिकारक प्रभावों को रोकती है।
- सहयोग और शांति: नैतिक मूल्य सहयोग और समाज में सामंजस्यपूर्ण संबंधों को प्रोत्साहित करते हैं।
- समानता और न्याय: नैतिकता न्यायसंगत व्यवहार और अन्याय के उन्मूलन का समर्थन करती है।
- सस्टेनेबिलिटी: नैतिकता समाज को भविष्य के लिए संसाधनों को संरक्षित करने वाले प्रथाओं की ओर मार्गदर्शन करती है।
- प्रगतिशीलता: नैतिकता सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन और आगे की सोच को प्रोत्साहित करती है।
- सही और गलत के मानक निर्धारित करना: नैतिकता यह पहचानती है कि क्या अच्छा या बुरा है, क्या उचित या अन्यायपूर्ण है, और नैतिक कर्तव्यों को परिभाषित करती है। यह अधिकारों, दायित्वों, निष्पक्षता, और सामाजिक लाभों के लिए स्थापित मानकों को निर्धारित करती है।
- विचार, दृष्टिकोण, और निर्णयों में सुधार: नैतिकता व्यक्तियों को उनकी क्रियाओं, चुनावों, और निर्णयों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने के लिए एक ढांचा प्रदान करती है।
- स्व-जागरूकता में सहायता: नैतिकता व्यक्तियों को उनकी वास्तविक प्रकृति को समझने में मदद करती है और उन्हें अपने सर्वोत्तम हितों और कल्याण की ओर निर्णय लेने में मार्गदर्शन करती है।
- हमारी क्रियाओं या निष्क्रियता का निर्धारण: नैतिकता के अभाव में, मानव क्रियाएँ उद्देश्यहीन होंगी। नैतिक मानक व्यक्तियों को उनके कार्यों को व्यवस्थित करने में मार्गदर्शन करते हैं।
- स्वस्थ और शांतिपूर्ण समाज की नींव: मानव कल्याण के लिए स्थापित संस्थाएँ नैतिक सिद्धांतों पर निर्भर करती हैं। नैतिकता एक सामान्य दृष्टिकोण बनाती है, जो सामाजिक स्थिरता और सहमति की ओर ले जाती है।
- समाज को बेहतर बनाने में मदद करती है: नैतिकता समानता, अधिकारों का सम्मान, और सभी व्यक्तियों के साथ निष्पक्ष व्यवहार को बढ़ावा देती है।
- नैतिक दुविधाओं को हल करना: नैतिकता नियमों और सिद्धांतों को प्रदान करती है जो कठिन नैतिक मुद्दों को हल करने में मदद करते हैं।
- विवेक का प्रयोग करने में सहायता: नैतिकता व्यक्तियों को स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करती है जब सामाजिक मानदंड या कानून स्पष्ट दिशा नहीं देते हैं।
- निजी और सार्वजनिक जीवन दोनों के लिए मार्गदर्शिका: नैतिकता व्यक्तिगत और पेशेवर क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है।
- आत्म-प्रकाशन की ओर मार्गदर्शन: नैतिकता व्यक्तियों को अच्छे बनने की इच्छा को पूरा करने में मदद करती है।
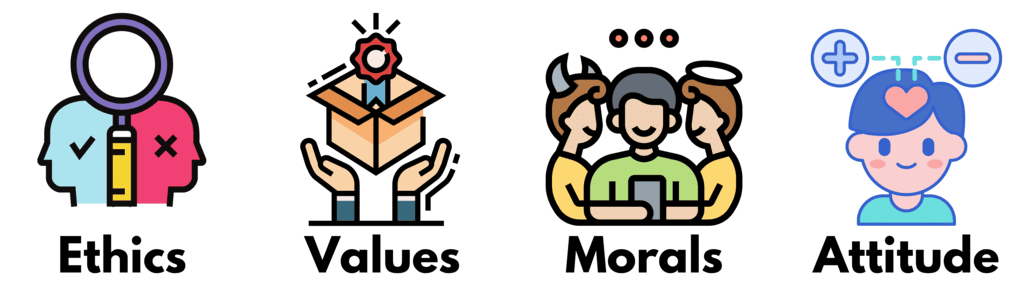
|
46 videos|101 docs
|
















