अरिस्टोटेलियन सद्गुण का सिद्धांत | यूपीएससी मेन्स: नैतिकता, सत्यनिष्ठा और योग्यता - UPSC PDF Download
अरस्तूवादी गुण का सिद्धांत
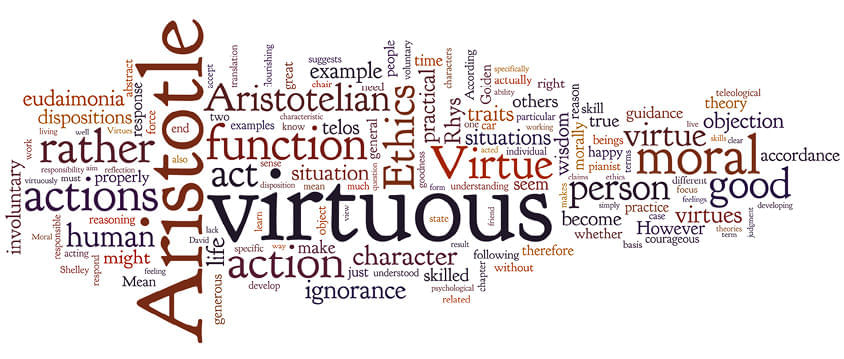
- अरस्तू (384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व) एक प्रमुख ग्रीक दार्शनिक थे और पश्चिमी दुनिया में नैतिकता पर एक पुस्तक लिखने वाले पहले व्यक्ति थे।
- उन्होंने तर्क किया कि ज्ञान, साहस, वीरता, और दृढ़ता जैसे गुण अकेले एक नैतिक रूप से अच्छे चरित्र या व्यक्ति का निर्माण नहीं करते।
- इनका नैतिक मूल्य उन प्रेरणाओं और मूल्यों पर निर्भर करता है जिनसे वे जुड़े होते हैं।
- इसलिए, अरस्तू नैतिक गुणों और बौद्धिक गुणों के बीच भेद करते हैं।
- गुणों के उनके सिद्धांत में एक मुख्य तत्व स्वर्णिम मध्य का सिद्धांत है।
- अरस्तू न्याय के महत्वपूर्ण गुण को विस्तृत करने में भी सही हैं, इसे उच्चतम गुण मानते हैं।
- वे न्याय के दो रूपों की पहचान करते हैं:
- वितरणात्मक न्याय
- उपचारात्मक न्याय
- वितरणात्मक न्याय राज्य के नागरिकों के बीच धन और सम्मान के उचित आवंटन से संबंधित है, जबकि उपचारात्मक न्याय समुदाय के सदस्यों के बीच उचित लेन-देन सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।
- गुणों का विकास गुणकारी कार्यों के आदत के माध्यम से होता है।
- मनुष्यों की विशेषता उनक सोचने और अपनी इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता में है।
- अरस्तू के अनुसार, गुणकारी व्यवहार अत्यधिक या कमज़ोरी के चरम से बचने में है।
- उदाहरण के लिए, अत्यधिक भोग करना उतना ही दोष है जितना इच्छाओं को अधिक दबाना, जिससे आत्म-नियंत्रण एक गुण बन जाता है।
- इसी प्रकार, साहस हठधर्मिता और कायरता के बीच है, जबकि उदारता कंजूसी और फिजूलखर्ची के बीच है।
- इसलिए, गुण का अर्थ है दो दोषों के बीच संतुलन खोजना: एक अत्यधिक और दूसरा कमी।
- इस संतुलन को प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इसमें सही बात, सही व्यक्ति, सही मात्रा, सही इरादा, और सही समय पर करना शामिल है।
- उदाहरण के लिए, उदारता का अभ्यास करना सही मात्रा में, सही व्यक्ति को, सही समय पर, और सही उद्देश्य के साथ देना है।
नैतिक/नैतिक सापेक्षवाद
- नैतिक सापेक्षता एक नैतिक सिद्धांत है जो तर्क करता है कि नैतिकता एक समाज के सांस्कृतिक मानदंडों द्वारा निर्धारित होती है। यह निर्धारित करना कि कोई कार्य सही है या गलत, उस समाज के नैतिक मानकों पर निर्भर करता है जिसमें यह होता है। एक ही कार्य को एक समाज में नैतिक रूप से सही माना जा सकता है, जबकि दूसरे समाज में इसे नैतिक रूप से गलत माना जा सकता है। नैतिक सापेक्षता के अनुसार, सभी लोगों पर सभी समय में लागू होने वाले कोई सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत नहीं होते। नैतिक सापेक्षता सहिष्णुता को अपने केंद्रीय सिद्धांत के रूप में मानती है। नैतिक सापेक्षतावादी इस विचार को अस्वीकार करते हैं कि सभी संस्कृतियों का पालन करने के लिए कोई सार्वभौमिक, वस्तुनिष्ठ "सुपर-नियम" होते हैं। वे मानते हैं कि सापेक्षता मानव समाजों की विविधता का सम्मान करती है और उन विभिन्न संदर्भों का ध्यान रखती है जिनमें मानव क्रियाएँ होती हैं।
नैतिक सापेक्षता और मानक नैतिकता का संबंध
- नैतिक सापेक्षता का कहना है कि कोई वस्तुनिष्ठ या सार्वभौमिक रूप से मान्य नैतिक सिद्धांत नहीं हैं, क्योंकि सभी नैतिक निर्णय केवल मानव राय के अभिव्यक्ति हैं। नैतिक सापेक्षता एक कदम आगे बढ़कर यह तर्क करती है कि किसी संस्कृति के नैतिक सिद्धांत उस विशेष संस्कृति के लिए उपयुक्त होते हैं, जिससे यह एक मानक नैतिकता बन जाती है। इसे विस्तार से समझाने के लिए, विश्व में प्रथाओं की विविधता यह प्रश्न उठाती है कि कौन से नियम सही हैं। सापेक्षतावाद का उत्तर है कि कोई एकल सेट नियम सार्वभौमिक रूप से सही नहीं है—सही और गलत सापेक्ष हैं। एक मानक नैतिकता यह निर्धारित करने का प्रयास करती है कि कौन से कार्य किए जाने चाहिए या नहीं। रूथ बेनेडिक्ट, एक सांस्कृतिक मानवविज्ञानी, इस दृष्टिकोण की मूल प्रवर्तक थीं, जिन्होंने प्रारंभ में सामान्य सांस्कृतिक व्यवहारों का वर्णन करने का लक्ष्य रखा था। उनके निष्कर्षों का सारांश इस विचार में किया जा सकता है कि "जो सामान्य है, वही नैतिक है।"
नैतिक/नैतिक वस्तुनिष्ठता
नैतिक वस्तुवाद यह विश्वास है कि सार्वभौमिक और वस्तुनिष्ठ नैतिक सिद्धांत मौजूद हैं और ये व्यक्तियों या समाजों पर निर्भर नहीं हैं। इस दृष्टिकोण से, नैतिक निर्णयों की सटीकता किसी भी व्यक्ति या समूह के विश्वासों या भावनाओं से स्वतंत्र होती है। यह विचार बताता है कि नैतिक बयानों की तुलना रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, या इतिहास में बयानों से की जा सकती है, क्योंकि ये एक वस्तुनिष्ठ वास्तविकता को चित्रित करने का प्रयास करते हैं। यदि ये बयानों इस नैतिक वास्तविकता का सही प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वे सत्य होते हैं, चाहे किसी के विश्वास, उम्मीदें, इच्छाएं, या भावनाएँ कुछ भी हों। इसके विपरीत, यदि ये इस वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करने में विफल होते हैं, तो वे झूठे होते हैं, चाहे व्यक्तिगत राय या भावनाएं कुछ भी हों।
- इस दृष्टिकोण से, नैतिक निर्णयों की सटीकता किसी भी व्यक्ति या समूह के विश्वासों या भावनाओं से स्वतंत्र होती है। यह विचार बताता है कि नैतिक बयानों की तुलना रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, या इतिहास में बयानों से की जा सकती है, क्योंकि ये एक वस्तुनिष्ठ वास्तविकता को चित्रित करने का प्रयास करते हैं।
नैतिक/नैतिक निरपेक्षता
- यह दृष्टिकोण यह asserts करता है कि कुछ सिद्धांत सार्वभौमिक हैं, इन्हें अधिरोपित नहीं किया जा सकता, और ये सभी परिस्थितियों में सत्य हैं। नैतिक निरपेक्षता यह asserts करती है कि कुछ नैतिक नियम सार्वभौमिक रूप से सत्य हैं, इन्हें खोजा जा सकता है, और ये सभी पर लागू होते हैं। अमोरल क्रियाएँ—जो इन नैतिक नियमों का उल्लंघन करती हैं—स्वाभाविक रूप से गलत होती हैं, चाहे स्थिति या परिणाम कुछ भी हों।
नैतिक/नैतिक यथार्थवाद
नैतिक यथार्थवाद यह मानता है कि ब्रह्मांड में वस्तुनिष्ठ नैतिक तथ्य या सत्य मौजूद हैं और नैतिक बयानों में इन सत्यों के बारे में तथ्यात्मक जानकारी होती है।
नैतिक/आचारिक व्यक्तिवाद
- व्यक्तिवाद यह तर्क करता है कि नैतिक निर्णय केवल एक व्यक्ति की भावनाओं या दृष्टिकोणों को व्यक्त करते हैं और आचारिक कथन अच्छे या बुरे के बारे में तथ्यों को नहीं बताते।
- व्यक्तिवादी बताते हैं कि नैतिक कथन किसी विशेष मुद्दे के संबंध में एक व्यक्ति या समूह की भावनाओं, दृष्टिकोणों और भावनाओं को दर्शाते हैं। जब कोई किसी चीज़ को अच्छा या बुरा बताता है, तो वह इसके प्रति अपनी व्यक्तिगत सकारात्मक या नकारात्मक भावनाओं को व्यक्त कर रहा होता है।
नैतिक/आचारिक भावनावाद
भावनावाद का मानना है कि नैतिक दावे केवल अनुमोदन या असहमति की अभिव्यक्ति हैं। जबकि यह व्यक्तिवाद के समान लग सकता है, भावनावाद इस मायने में भिन्न है कि एक नैतिक कथन वक्ता की भावनाओं के बारे में जानकारी नहीं देता, बल्कि केवल उन्हें व्यक्त करता है।
नैतिक/आचारिक प्रस्तावितवाद
प्रस्तावितवादी मानते हैं कि आचारिक कथन निर्देशों या सुझावों के रूप में कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई कहता है कि कुछ अच्छा है, तो इसका तात्पर्य है कि इसे इस प्रकार कार्य करने की सिफारिश की जा रही है, जबकि यदि कोई कहता है कि कुछ बुरा है, तो इसका मतलब है कि इससे बचने का निर्देश दिया जा रहा है।
नैतिक/आचारिक अधिभौतिकवाद
अधिभौतिकवाद नैतिकता को धर्म से निकटता से जोड़ता है, यह asserting करता है कि नैतिक नियम केवल भगवान से उत्पन्न होते हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार, कुछ अच्छा है क्योंकि भगवान इसे ऐसा घोषित करते हैं, और एक सद्गुणपूर्ण जीवन जीने का मतलब है भगवान की इच्छाओं का पालन करना।
नैतिक/आचारिक अंतर्ज्ञानवाद
- अंतर्ज्ञानवादी मानते हैं कि अच्छा और बुरा वस्तुनिष्ठ, अंतर्निहित गुण हैं जिन्हें सरल तत्वों में विभाजित नहीं किया जा सकता। कुछ चीजें केवल इसलिए अच्छी होती हैं क्योंकि वे हैं, और इसके लिए किसी और तर्क या प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती।
- अंतर्ज्ञानवादी मानते हैं कि वयस्क अपने अंतर्निहित नैतिक संवेदना के माध्यम से अच्छाई या बुराई को पहचान सकते हैं, जो उन्हें वस्तुनिष्ठ नैतिक सत्य को समझने की अनुमति देती है। वे तर्क करते हैं कि मौलिक नैतिक सत्य उन लोगों के लिए स्व-सिद्ध होते हैं जो नैतिक प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और ये तर्कसंगत तर्क के माध्यम से प्राप्त नहीं होते।
हेडोनिज़्म

- हेडोनिज़्म एक दर्शन है जो आनंद को अंतिम अच्छाई और जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मानता है। मूल रूप से, एक हेडोनिस्ट सबसे अधिक समग्र आनंद प्राप्त करने का प्रयास करता है, जिससे दर्द को न्यूनतम किया जा सके।
- आचारिक हेडोनिज़्म यह स्पष्ट करता है कि हर व्यक्ति को अपने लिए सबसे अधिक संभव आनंद की खोज करने का अधिकार है। यह यह भी जोर देता है कि एक व्यक्ति का आनंद उसके दर्द से काफी अधिक होना चाहिए।
- हेडोनिज़्म मानव क्रियाओं का मूल्यांकन उनके परिणामों के आधार पर करता है, विशेष रूप से आनंद और दर्द के संदर्भ में। मानव व्यवहार का मूल्य उस आनंद की मात्रा से मापा जाता है जो यह उत्पन्न करता है। हेडोनिस्टों के लिए, नैतिकता का मानक \"आनंद\" है। ऐसे कार्य जो आनंद उत्पन्न करते हैं, उन्हें सही माना जाता है, जबकि जो दर्द का कारण बनते हैं, उन्हें गलत समझा जाता है।
मनोवैज्ञानिक हेडोनिज़्म और आचारिक हेडोनिज़्म
- हेडोनिज़्म के दो मुख्य रूप हैं: मनोवैज्ञानिक हेडोनिज़्म और नैतिक हेडोनिज़्म। मनोवैज्ञानिक हेडोनिज़्म यह утвержित करता है कि सुख स्वाभाविक रूप से इच्छाओं का वस्तु है, अर्थात् मनुष्य स्वाभाविक रूप से सुख की खोज करता है। इसे तथ्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। दूसरी ओर, नैतिक हेडोनिज़्म यह मानता है कि सुख इच्छाओं का उचित वस्तु है, यह सुझाव देते हुए कि मनुष्यों को सुख की खोज करनी चाहिए। इसे मूल्य के रूप में व्यक्त किया गया है।
- नैतिक हेडोनिज़्म को दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है: स्वार्थी हेडोनिज़्म और सार्वभौमिक हेडोनिज़्म (या उपयोगितावाद)। स्वार्थी हेडोनिज़्म यह मानता है कि एक व्यक्ति का अपना सुख सर्वोच्च अच्छा है, जो व्यक्तिगत संतोष पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके विपरीत, सार्वभौमिक हेडोनिज़्म कई लोगों के सुख को महत्व देता है, व्यक्तिगत सुख के बजाय सामान्य खुशी की ओर प्रयास करता है।
नैतिक हेडोनिज़्म - मोटा और परिष्कृत
नैतिक हेडोनिज़्म, चाहे वह स्वार्थी हो या सार्वभौमिक, को आगे दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है: मोटा हेडोनिज़्म और परिष्कृत हेडोनिज़्म। मोटा हेडोनिज़्म इंद्रिय सुखों पर जोर देता है, सभी सुखों को समान मानते हुए केवल उनकी तीव्रता में भिन्नता को स्वीकार करता है। यह भविष्य के सुखों की तुलना में तात्कालिक सुखों को प्राथमिकता देता है। दूसरी ओर, परिष्कृत हेडोनिज़्म मानसिक और अधिक सूक्ष्म सुखों को महत्व देता है, इन उच्चतर सुखों को प्राप्त करने में तर्क की भूमिका को मान्यता देता है।
|
46 videos|101 docs
|





















