NCERT सारांश: सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ (कक्षा 12) | UPSC CSE (हिंदी) के लिए पुरानी और नई एनसीईआरटी अवश्य पढ़ें PDF Download
परिचय
- संस्कृति के गुण जैसे भाषा, धर्म, संप्रदाय, जाति या नस्ल समुदायों की पहचान में मदद कर सकते हैं।
- समस्याएँ तब उत्पन्न होती हैं जब सांस्कृतिक पहचान की मजबूती से तीव्र भावनाएँ उत्पन्न होती हैं और अक्सर बड़े समूहों को एक साथ लाती हैं।
- यह स्थिति तब और जटिल हो जाती है जब आर्थिक और सामाजिक असमानता सांस्कृतिक विषमताओं के साथ मिलती है।
- एक समुदाय द्वारा अनुभव की गई अन्याय या असमानताओं को संबोधित करने के प्रयासों का विरोध अन्य समुदायों द्वारा किया जा सकता है।
- जब नदी के पानी, नौकरियों, या सरकारी धन जैसी साझा की जाने वाली संसाधनों की कमी होती है, तब स्थिति और खराब हो जाती है।

समुदाय पहचान का महत्व
- समुदाय पहचान किसी भी अर्जित योग्यताओं या उपलब्धियों पर आधारित नहीं होती, बल्कि जन्म और Zugehörigkeit की भावना पर निर्भर करती है।
- यह इस बारे में नहीं है कि हमने क्या हासिल किया है, बल्कि यह इस बारे में है कि हम कौन हैं।
- कोई भी अपने परिवार, समुदाय, या राष्ट्र पर नियंत्रण नहीं रखता, जिस में वह पैदा होता है, इसलिए किसी एक में शामिल होने के लिए कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है।
- आश्रित पहचान और सामुदायिक भावनाएँ सार्वभौमिक हैं, जो हर धर्म और राष्ट्र में मौजूद हैं, मातृभाषा या संस्कृति, मूल्यों, विश्वासों आदि के संदर्भ में।
- इन अवधारणाओं को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि समुदाय पहचान आमतौर पर आवंटित होती है।
- एक व्यक्ति को सभी को अपनाना पड़ता है, और जब एक व्यक्ति इनसे प्यार करता है, तो कोई भी आपत्ति नहीं कर सकता।
- हालांकि, यह मुख्य रूप से एक व्यक्तिगत अनुभव है। जब दो राष्ट्र या समूह संघर्ष में होते हैं, तो यह दुर्लभ है कि कोई भी यह स्वीकार करे कि वे गलत हैं, भले ही एक या दोनों गलत हों।
समुदाय, राष्ट्र, राष्ट्र राज्य
राष्ट्र का अर्थ एक बड़े समूह से है जिनके पास अपना खुद का क्षेत्र, लोग, सरकार और संप्रभुता होती है। एक देश के सभी नागरिकों के बीच एक ही राजनीतिक इकाई से संबंधित होने की इच्छा एक साझा भावना होती है। यह राजनीतिक एकीकरण की आकांक्षा आमतौर पर एक राज्य की स्थापना के माध्यम से प्रकट होती है। देशों में एक सामान्य भाषा, धर्म, जाति या अन्य विशेषताएँ साझा करना आवश्यक नहीं है, जबकि कई अलग-अलग देश विभिन्न जातियों, विश्वासों और भाषाओं को साझा कर सकते हैं।

राज्य एक अमूर्त संस्था है जिसमें कई राजनीतिक और कानूनी संस्थाएँ होती हैं जो एक विशेष भौतिक क्षेत्र और इसके निवासियों पर शक्ति का दावा करती हैं। मैक्स वेबर की परिभाषा के अनुसार, राज्य \"एक ऐसा निकाय है जो एक दिए गए क्षेत्र में वैध शक्ति का एकाधिकार सफलतापूर्वक दावा करता है।\" एक समूह जिसे एक विशेष क्षेत्र में कानूनी शक्ति के रूप में प्रभावी ढंग से प्रमाणित किया जा सकता है, उसे राज्य कहा जाता है।
उपनिवेशी शासन और राष्ट्र-राज्य
- भारत 1947 में अपने विभाजन के बाद एक अलग राष्ट्र-राज्य बन गया।
- बांग्लादेश और पाकिस्तान ने मिलकर पाकिस्तान का राष्ट्र-राज्य बनाया, जो बाद में प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण अलग हो गया।
- एक अन्य समस्या यह थी कि बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा, बांग्ला, ने पाकिस्तान के लिए उर्दू को अपनी राष्ट्रीय भाषा के रूप में चुनना मुश्किल बना दिया।
यूएसएसआर - सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ
- यूएसएसआर एक देश-राज्य था जिसमें कई पड़ोसी राष्ट्र थे, प्रत्येक की अपनी संस्कृति और राज्य-राष्ट्र था, लेकिन सरकार ने शक्ति बनाए रखी, और लोगों का कोई योगदान नहीं था।
- यह 1991 में ढह गया।
अमेरिका में इजरायली नागरिकों की द्वैध नागरिकता
संयुक्त राज्य अमेरिका में, केवल वहीं जन्मे और पले-बढ़े यहूदी नागरिकता प्राप्त करते हैं, और वे ही दोहरी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं।
नीतियाँ (भारत दोनों का पालन करता है)
- असिमिलेशन की नीति: यह नीति सभी को एक ही मानक, संस्कृति, मूल्य और सिद्धांत का पालन करने की आवश्यकता है। बहुमत को अधिक शक्ति होती है, इसलिए पूरा राष्ट्र उनके अनुसार चलता है। उदाहरण के लिए, भारत में, जहाँ हिंदू बहुमत में हैं, वहाँ ईसाइयों या पारसियों की तुलना में बहुत अधिक त्योहार होते हैं।
- एकीकरण की नीति: इस नीति के तहत, लोग अपनी गैर-भौतिक संस्कृति को निजी में बनाए रखते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से राष्ट्रीय संस्कृति या पैटर्न का पालन करते हैं। उदाहरण के लिए, जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है, न कि वन्दे मातरम्। पहले से स्थापित राष्ट्र अल्पसंख्यक पहचानों को संभावित खतरों के रूप में मानते हैं क्योंकि वे देश निर्माण के लिए आधार बन सकते हैं। उदाहरण के लिए, खालिस्तान में सिख अपनी खुद की मातृभूमि की चाह रखते थे।
राज्य एक एकल, समान राष्ट्रीय पहचान को प्राथमिकता देते हैं ताकि एकता और समरसता को बढ़ावा मिल सके, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अल्पसंख्यकों की पहचान को दबाया जाए। ऐसा करने से विद्रोह और विभाजन हो सकता है, एकीकरण नहीं। इसलिए, सरकार लोगों को अपनी सांस्कृतिक भिन्नताएँ बनाए रखने की अनुमति देती है ताकि पूरे देश में शांति और सौहार्द को बढ़ावा मिल सके।
संस्कृतिक विविधता और भारत एक राष्ट्र-राज्य के रूप में
- भारत में सबसे अधिक लोग मुस्लिम हैं, जो इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद हैं।
- भारत धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखता है, जिससे लोगों को अपने धर्म का पालन और प्रचार करने की अनुमति मिलती है, और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण भी दिया जाता है।
भाषा
- भारत में 1632 आधिकारिक भाषाएँ हैं, लेकिन इनमें से 18 आधिकारिक भाषाएँ हैं, जिनमें हिंदी, गुजराती, मराठी, अंग्रेजी, पंजाबी और उर्दू शामिल हैं।
- सरकारी दस्तावेज़ों में हिंदी और अंग्रेजी का उपयोग किया जाता है, सिवाय संविधान के, जो अंग्रेजी में है।
- भाषा ने भारत की एकता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और यह प्रभावी संवाद और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए राज्य बोर्डों को बढ़ावा देने वाला एक एकीकृत कारक है।
- नेहरू के तहत, देश को भाषाई आधार पर विभाजित किया गया, जिससे आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों का निर्माण हुआ।
- हालांकि भाषा एक शक्तिशाली एकीकृत बल हो सकती है, फिर भी क्षेत्रीय असमानताएँ मौजूद रह सकती हैं।
भारतीय संदर्भ में क्षेत्रवाद
- क्षेत्रवाद भारत में विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं, क्षेत्रों, जातियों, और जनजातियों के अस्तित्व की घटना है।
- भाषा ने देश की एकता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद, भारत ने राष्ट्रपति पद के नेतृत्व के लिए ब्रिटिश मॉडल अपनाने का निर्णय लिया।
- बॉम्बे, मद्रास, और कलकत्ता के रियासतों में विभिन्न भाषाएँ बोलने वाले लोग थे, जैसे मलयालम, तमिल, तेलुगु, और कन्नड़।
- भाषा एक एकीकृत कारक है जो प्रभावी संवाद, एकीकरण, राज्य बोर्डों (शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए) को बढ़ावा दे सकती है, और भाषावाद भाषा के प्रति प्रेम को फैलाने में मदद कर सकता है।
- नेहरू के नेतृत्व में, देश को भाषाई आधार पर विभाजित किया गया, जिस पर उन्होंने शुरू में संकोच किया, लेकिन बाद में इसे लाभकारी माना।
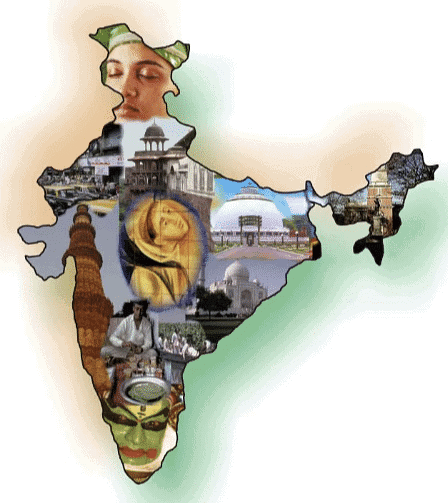
- इसका परिणाम मद्रास राष्ट्रपति के तीन राज्यों में विभाजन हुआ, जिससे तेलुगु लोगों में असंतोष पैदा हुआ।
- उन्होंने एक अलग राज्य की मांग की जब तमिलों को अधिक महत्वपूर्ण पद दिए गए और वे प्रमुख हो गए।
- पॉटी श्रीरामुलु ने तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य की मांग करने के लिए अनशन किया।
- उनकी मृत्यु के बाद, प्रदर्शन जारी रहे, और 1956 में सरकार ने तेलुगु लोगों को आंध्र प्रदेश प्रदान किया, जिन्होंने आंध्र प्रदेश जाने या मद्रास राज्य में रहने का विकल्प चुना।
- हालांकि भाषा एक शक्तिशाली एकीकृत बल के रूप में कार्य कर सकती है, फिर भी क्षेत्रीय असमानताएँ मौजूद रह सकती हैं।
- श्रीलंका में, तमिलों ने मुख्य भाषा सिंहलियों के साथ समान व्यवहार की मांग की और आधिकारिक संसदीय प्रशासन की।
- जनता की मदद के प्रयास में, LTTE की स्थापना की गई, जिसके परिणामस्वरूप राजीव गांधी की हत्या हुई।
धर्म-संबंधी मुद्दे और पहचान
- सामाजिक विज्ञान में, धर्म और बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अल्पसंख्यक उन लोगों को संदर्भित करते हैं जो किसी भी धर्म के बहुसंख्यकों की तुलना में संख्यात्मक रूप से छोटे होते हैं। भारत में, हिंदू 81% जनसंख्या के साथ बहुसंख्यक हैं।
अल्पसंख्यक अधिकार और राष्ट्र निर्माण
समावेशी राष्ट्रवाद
- समावेशी राष्ट्रवाद तब होता है जब सभी धर्म एक साथ मिलकर राष्ट्र के उत्थान के लिए काम करते हैं, जो विविधता में एकता को सृजित करता है। भले ही हम भिन्नताओं और विविधताओं को स्वीकार करते हैं, हम फिर भी सामूहिक भलाई के लिए मिलकर काम करते हैं। हम भेदभाव को समाप्त करने और एक लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना की कोशिश करते हैं।
विशेषाधिकार राष्ट्रवाद
- विशेषाधिकार राष्ट्रवाद तब होता है जब प्रत्येक धर्म अपनी दृष्टि के अनुसार राष्ट्र के लिए सर्वोत्तम का पालन करता है। देश के विकास के लिए सबसे प्रभावी दृष्टिकोण समावेशी सोच को अपनाना है, जहां सभी सामाजिक वर्गों (जिसमें अल्पसंख्यक भी शामिल हैं) की संविधान में देखभाल की जाती है। संविधान के लेखन के दौरान, संविधान सभा ने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय को शामिल करने का प्रयास किया।
अल्पसंख्यक की विशेषताएँ
- सामाजिक दृष्टिकोण से, धर्म और अल्पसंख्यक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और अल्पसंख्यक वे होते हैं जिनकी संख्या बहुसंख्यकों की तुलना में कम होती है। अल्पसंख्यकों की अधूरी आवश्यकताएँ होती हैं और उनकी तुलना में अवसर कम होते हैं। वे अक्सर भेदभाव का सामना करते हैं और अपनी छोटी संख्या के कारण असुरक्षित महसूस करते हैं। अपनी भिन्नताओं के बावजूद, अल्पसंख्यकों में एकता और सामूहिक पहचान की भावना होती है, और वे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एक साथ काम करते हैं। कुछ समुदाय, जैसे जैन और पारसी, की मजबूत अर्थव्यवस्था होती है लेकिन उनके पास सांस्कृतिक और सामाजिक संरचनाओं की कमी होती है। अल्पसंख्यक अपने देश के प्रति वफादारी की भावना महसूस करते हैं।
नीतियाँ और अल्पसंख्यक
 राजनीतिक दलअल्पसंख्यक अनिश्चित और जोखिम में होते हैं, और इसके परिणामस्वरूप एक "अल्पसंख्यक ब्लॉक" का गठन होता है। उन्हें अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए समझौता करना पड़ सकता है। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, और अल्पसंख्यक को अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत सुरक्षा प्रदान की जाती है। अनुच्छेद 30 किसी भी धार्मिक समूह को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने की अनुमति देता है, और अल्पसंख्यकों को अन्य समूहों द्वारा प्रदान की गई सभी सुविधाओं तक पहुंच होनी चाहिए। राष्ट्रीय सामंजस्य के लिए, किसी को भी किसी विशेष विश्वास को स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। यूरोप में, ईसाई बहुसंख्या में हैं, जबकि यहूदी, सिख और अन्य अल्पसंख्यक हिंदू हैं।
राजनीतिक दलअल्पसंख्यक अनिश्चित और जोखिम में होते हैं, और इसके परिणामस्वरूप एक "अल्पसंख्यक ब्लॉक" का गठन होता है। उन्हें अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए समझौता करना पड़ सकता है। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, और अल्पसंख्यक को अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत सुरक्षा प्रदान की जाती है। अनुच्छेद 30 किसी भी धार्मिक समूह को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने की अनुमति देता है, और अल्पसंख्यकों को अन्य समूहों द्वारा प्रदान की गई सभी सुविधाओं तक पहुंच होनी चाहिए। राष्ट्रीय सामंजस्य के लिए, किसी को भी किसी विशेष विश्वास को स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। यूरोप में, ईसाई बहुसंख्या में हैं, जबकि यहूदी, सिख और अन्य अल्पसंख्यक हिंदू हैं।
साम्प्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्र-राज्य
- आपकीधार्मिक भक्ति ने आपको सभी अन्य धर्मों को कम महत्व देने के लिए प्रेरित किया है।
- पश्चिमी देशों में साम्प्रदायिकता को उन व्यक्तियों के एक समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है जो एक साझा उद्देश्य की ओर सहयोग करते हैं।
- भारत में, राजनीतिक नेता धार्मिक संबद्धताओं का उपयोग वोट पाने के लिए करते हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि साम्प्रदायिकता राजनीति से अधिक है।
- भारत की विविधता साम्प्रदायिकता को एक समस्या बनाती है, जहाँ विभिन्न पृष्ठभूमियों वाले बड़े जनसंख्याएँ होती हैं।
- साम्प्रदायिकता एक हिंसक राजनीतिक दर्शन है जो एक विशेष धर्म से जुड़ी होती है, जो अपने धर्म के प्रति अस्वस्थ लगाव को दर्शाती है।
- साम्प्रदायिकतावादी एक आक्रामक राजनीतिक पहचान अपनाते हैं जो अन्य सभी धर्मों को खारिज करती है और अपनी ही समुदाय में दंगे भड़काती है।
- एक समुदाय दूसरे समुदाय के खिलाफ अतीत में किए गए अन्याय का बदला लेने की कोशिश कर सकता है, या अपने क्षेत्र की रक्षा करने के लिए।
- दंगों की विशेषताएँ निरंतर हिंसा, मृत्यु, संपत्ति का विनाश, हमले, लूटपाट, और यौन हमले होती हैं।
- जब भी किसी समुदाय में दंगा होता है, तो सत्ताधारी पार्टी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और पीड़ितों की सुरक्षा करनी चाहिए।
- भारत में, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के किसी भी धर्म का पालन, प्रचार, और उद्घोष करने का अधिकार है, सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाता है।
- इसके विपरीत, पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या यह है कि चर्च को राजनीतिक मुद्दों में शामिल नहीं होना चाहिए, और धर्म सामान्यतः निजी क्षेत्र में सीमित रहता है।
- हालांकि धर्मनिरपेक्षता में प्रगति हुई है, धर्म अभी भी एक निजी मामले के रूप में देखा जाता है।
- आधुनिकता ने धर्मनिरपेक्षता के उदय को बढ़ावा दिया है।
- विभिन्न तार्किक दृष्टिकोणों पर विचार करके और धर्म के बजाय सेवा पर ध्यान केंद्रित करके, एक अधिक खुले दृष्टिकोण को प्राप्त किया जा सकता है।
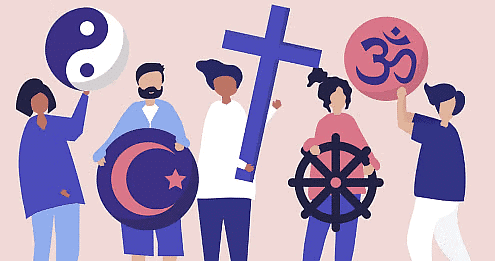
- भारत की धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या, जो सभी धर्मों की समानता पर बल देती है, साम्प्रदायिकता के विपरीत है।
- पश्चिम और भारत में धर्मनिरपेक्षता की विभिन्न व्याख्याएँ हमारे देश के लिए एक चुनौती प्रस्तुत करती हैं।
- सरकार का दावा है कि आरक्षण अन्यायपूर्ण है, जिसे बहुसंख्या द्वारा चुनौती दी जाती है, जबकि अल्पसंख्यक यह तर्क करते हैं कि उन्हें दबा नहीं दिया जाना चाहिए।
- सरकार के अल्पसंख्यकों की रक्षा के प्रयासों के बावजूद, बहुसंख्या की परंपराएँ और छुट्टियाँ अभी भी मनाई जाती हैं, जो धर्मनिरपेक्षता की चुनौतियों को बढ़ाती हैं।
- राजनीतिक दलों से हस्तक्षेप इन चुनौतियों को और बढ़ा रहा है।
- फिर भी, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश बना हुआ है जो बहुसंख्या को परेशान किए बिना अल्पसंख्यकों का ध्यान रखने का प्रयास करता है, जबकि शांति, सहिष्णुता, और समुदाय की सामंजस्य बनाए रखता है।
- भारत की स्वतंत्रता के बाद, नेहरू ने घोषणा की कि देश एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, और स्वतंत्र राष्ट्र है।
राज्य और नागरिक समाज
- लोकतंत्र एक शासन का रूप है जहाँ लोगों की आवाज होती है, वे अपने राजनीतिक नेताओं का चुनाव कर सकते हैं, और अपने मौलिक अधिकारों का आनंद लेते हैं।
- अधिनायकवाद एक शासन का रूप है जहाँ नागरिक स्वतंत्रताओं को सीमित किया जाता है, और नागरिकों के पास सरकार को जिम्मेदार ठहराने के लिए कोई साधन नहीं होता।
- अधिनायकत्व के तहत, संस्थाएँ लोगों की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ हो सकती हैं, जैसे कि बैंक।
- नागरिक समाज उन गैर-व्यवसायिक, गैर-लाभकारी संगठनों को संदर्भित करता है जो सार्वजनिक क्षेत्र के बाहर काम करते हैं, जिसमें स्वैच्छिक सदस्य शामिल होते हैं।
- नागरिक समाज ऐसे समूह हैं जो लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करते हैं, विशेष रूप से दबाए गए समूहों के अधिकारों की, और इनमें राजनीतिक दल, मुख्यधारा के मीडिया, एनजीओ, समाचार पत्र और महिला संगठनों शामिल हो सकते हैं।
- 1975-77 के आपातकाल के दौरान, व्यापक नसबंदी प्रयास हुए जो पुरुषों और महिलाओं दोनों को लक्षित करते हुए बलात vasectomies और tubectomies करने के लिए मजबूर किया गया।
- नागरिक स्वतंत्रताएँ निलंबित कर दी गईं, और व्यक्तियों को बिना मुकदमे के जेल भेज दिया गया।
- जिन लोगों ने इन कार्यों के खिलाफ आवाज उठाई और कुछ निम्न-स्तरीय अपराधियों को भी जेल में डाल दिया गया, जिनमें राजनीतिक व्यक्ति जयप्रकाश नारायण भी शामिल थे।
- आपातकाल के बाद, इंदिरा गांधी चुनाव हार गईं, और देश में एक राष्ट्रीय हलचल मच गई।
- इसके परिणामस्वरूप, नागरिक समाज संगठनों का महत्व बढ़ा।
आदिवासी, स्वास्थ्य देखभाल और पुनर्वास
सरकार की निगरानी में नागरिक समाज की भूमिका:
- नागरिक समाज संगठन यह सुनिश्चित करने के लिए काम करते हैं कि सरकारी धन का सही उपयोग किया जाए।
- वे कानून के अनुप्रयोग की निगरानी भी करते हैं, जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 शामिल है।
- यह अधिनियम व्यक्तियों को सरकारी वित्तीय दस्तावेजों की मांग करने की अनुमति देता है जो धन के वितरण और करों के भुगतान से संबंधित हैं।
- लोगों को सरकार के निर्णयों पर सवाल उठाने का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार केवल सरकारी कार्यों पर लागू होता है, निजी क्षेत्र के कार्यों पर नहीं।
|
389 docs|527 tests
|















