रामेश सिंह का सारांश: भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास | भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) UPSC CSE के लिए PDF Download
स्वतंत्रता के समय भारत की आर्थिक स्थिति
- भारत की स्वतंत्रता के समय, देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से अव्यवस्थित थी।
- भारत एक सामान्य उपनिवेशीय अर्थव्यवस्था के रूप में कार्य कर रहा था, जहाँ इसके संसाधनों का उपयोग एक विदेशी शक्ति, विशेष रूप से यूनाइटेड किंगडम, के लाभ के लिए किया जा रहा था।
- कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों की संरचना बहुत कमजोर थी, और सरकार का अर्थव्यवस्था में न्यूनतम भूमिका थी।
- स्वतंत्रता से पहले के 50 वर्षों में, दुनिया के अन्य हिस्से, जिसमें यूके भी शामिल था, सक्रिय सरकारी भागीदारी के कारण कृषि और उद्योग में तेज़ वृद्धि का अनुभव कर रहे थे।
- इसके विपरीत, भारत ने ब्रिटेन में निवेश पूंजी का एकतरफा हस्तांतरण देखा, जिसे अक्सर \"धन का अपव्यय\" कहा जाता है।
- यह अन्यायपूर्ण व्यापार भारत के वाणिज्य, व्यापार और इसके एक बार समृद्ध हथकरघा उद्योग को गंभीर रूप से नुकसान पहुँचाता था।
- उपनिवेशीय सरकार ने नीतियाँ लागू कीं जो भारत की वृद्धि में बाधक थीं।
- उपनिवेशीय शासन के दौरान, सरकार की आर्थिक दृष्टि भारत की कच्चे माल का निर्यात बढ़ाने और ब्रिटिश निर्मित सामानों का आयात करने पर केंद्रित थी, जिसका उद्देश्य पूंजी अपव्यय और सैन्य खर्चों को कवर करने के लिए धन जुटाना था।
- सामाजिक क्षेत्र को ब्रिटिश शासकों द्वारा बहुत कम ध्यान दिया गया, जिससे अर्थव्यवस्था की उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा।
- ब्रिटिश शासन के तहत, भारत एक अशिक्षित किसान देश बना रहा, जहाँ स्वतंत्रता के समय केवल 17 प्रतिशत साक्षरता थी और जीवन प्रत्याशा केवल 32.5 वर्ष थी।
- ब्रिटिशों ने भारत में औद्योगीकरण की अनदेखी की; अवसंरचना का विकास घरेलू उद्योग के लिए नहीं बल्कि संसाधनों के निष्कर्षण के लिए किया गया।
- इस समय उभरे भारतीय व्यवसायियों ने ब्रिटिश वित्तीय पूंजी पर बहुत अधिक निर्भरता दिखाई, जहाँ कई उद्योगों पर ब्रिटिश कंपनियों का वर्चस्व था, जिसमें शिपिंग, बैंकिंग, बीमा, कोयला, बागान, और जूट शामिल थे।
- स्वतंत्रता से पहले का समय ठहराव का था, जहाँ उत्पादन या उत्पादकता में बहुत कम से कोई सुधार नहीं हुआ।
- 20वीं शताब्दी की शुरुआत में कुल वास्तविक उत्पादन की वृद्धि 2 प्रतिशत प्रति वर्ष से कम थी।
- आर्थिक डेटा दर्शाता है कि 1600 से 1870 के बीच भारत में प्रति व्यक्ति वृद्धि नहीं हुई, और 1870 से 1947 के बीच केवल 0.2 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई, जबकि यूके में 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- प्रति व्यक्ति आय बहुत कम थी, जिसमें 1899 में ₹18 और 1895 में ₹39.5, जो भारतीय लोगों द्वारा सामना की जा रही गंभीर गरीबी को उजागर करता है।
- 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में लगातार सूखा और महामारी ने ब्रिटिश सरकार की अनदेखी और भारतीय जनसंख्या के दुःख को उजागर किया।
- राजनीतिक नेताओं और उद्योगपतियों को स्वतंत्रता के बाद भारत को जिन आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, उसके बारे में अच्छी तरह से पता था।
- आश्चर्यजनक रूप से, इन प्रभावशाली व्यक्तियों ने स्वतंत्रता से पहले कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक समान दृष्टिकोण साझा किया:
- विकास के लिए सीधी जिम्मेदारी: इस पर मजबूत सहमति थी कि सरकार को आर्थिक विकास पर सीधे नजर रखनी चाहिए।
- जन क्षेत्र की भूमिका: अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत जन क्षेत्र को आवश्यक माना गया।
- भारी उद्योगों का विकास: आर्थिक उन्नति के लिए भारी उद्योगों के विकास की आवश्यकता पर साझा विश्वास था।
- विदेशी निवेश: राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए विदेशी निवेश को हतोत्साहित करना महत्वपूर्ण समझा गया।
- आर्थिक योजना: विकास को मार्गदर्शन करने के लिए व्यवस्थित आर्थिक योजना के महत्व को पहचाना गया।
- जब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की, तो सरकार को एक ऐसी अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित करने का कठिन कार्य सौंपा गया जो गंभीर स्थिति में थी और सुधार की कोई उम्मीद नहीं थी।
- राजनीतिक नेताओं और राष्ट्रीय गर्व द्वारा संचालित विकास और प्रगति के लिए एक मजबूत प्रोत्साहन था।
- इन नेताओं द्वारा इस समय किए गए निर्णय भारत के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण थे।
- 1956 तक कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जो भारत के आर्थिक दिशा को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण साबित हुए, जो पूर्व सुधार और बाद के सुधार दोनों अवधियों पर प्रभाव डालते हैं।
- वर्तमान स्थिति और विकास को समझने के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान देने वाले कारकों और घटनाओं पर विचार करना आवश्यक है।
प्रधान गतिशील शक्ति: कृषि बनाम उद्योग
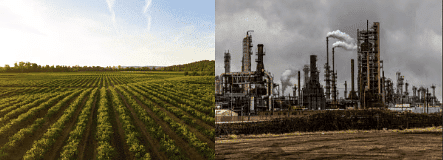
क्या कृषि या उद्योग को भारत की प्रधान गतिशील शक्ति (PMF) होना चाहिए था, इस पर बहस अभी भी विशेषज्ञों के बीच चर्चा का विषय है। सरकार ने शुरू में उद्योग को PMF के रूप में चुना, लेकिन कुछ का तर्क है कि कृषि एक बेहतर विकल्प हो सकता था। हर अर्थव्यवस्था को अपने प्राकृतिक और मानव संसाधनों का उपयोग करके विकसित होना आवश्यक है, लेकिन इस निर्णय को प्रभावित करने वाले सामाजिक और राजनीतिक कारक भी हैं। स्वतंत्रता के समय, भारत के सामने कई चुनौतियाँ थीं, जो औद्योगिकीकरण को कठिन बनाती थीं, जैसे:
- अवसंरचना की कमी: भारत में औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक बिजली, परिवहन और संचार जैसी सुविधाओं की बहुत कमी थी।
- बुनियादी उद्योगों की अनुपस्थिति: लोहे और इस्पात, सीमेंट, कोयला, कच्चा तेल, तेल रिफाइनिंग, और बिजली जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों की उपस्थिति नगण्य थी, जो औद्योगिकीकरण के लिए आधारभूत हैं।
- सीमित पूंजी: सरकार और निजी क्षेत्र दोनों के पास औद्योगिक परियोजनाओं को शुरू करने के लिए आवश्यक निवेश योग्य पूंजी की कमी थी।
- प्रौद्योगिकी की कमी: औद्योगिक गतिविधियों का समर्थन करने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और विकास की कमी थी।
- कौशलयुक्त मानव संसाधन: देश में औद्योगिक नौकरियों के लिए तैयार कौशलयुक्त कार्यबल की कमी थी।
- उद्यमिता की कमी: जनसंख्या में उद्यमिता की भावना और पहल की कमी थी।
- औद्योगिक वस्तुओं के लिए बाजार: औद्योगिक उत्पादों के लिए कोई मौजूदा बाजार नहीं था, जिससे उद्योगों के फलने-फूलने में कठिनाई हुई।
- सामाजिक-मानसिक कारक: विभिन्न सामाजिक और मानसिक कारक उचित औद्योगिकीकरण में बाधा डालते थे।
इन चुनौतियों को देखते हुए, कृषि भारत के लिए एक अधिक उपयुक्त PMF हो सकती थी क्योंकि:
उर्वर भूमि: भारत के पास कृषि के लिए उपयुक्त पर्याप्त उर्वर भूमि थी।
- तैयार कार्यबल: उपलब्ध मानव पूंजी को व्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं थी और इसे न्यूनतम संगठन के साथ कृषि में लगाया जा सकता था।
- कृषि पर ध्यान केंद्रित करके, भारत ने जनसंख्या की बुनियादी आवश्यकताओं जैसे खाद्य, आश्रय, और स्वास्थ्य देखभाल को सुनिश्चित किया होता, जो आगे के विकास की नींव रखता। एक बार जब ये बुनियादी आवश्यकताएँ पूरी हो जातीं, तो जनसंख्या के पास औद्योगिक विकास के लिए खरीद क्षमता होती।
- चीन ने 1949 में इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया, अपने कृषि संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करते हुए औद्योगिककरण की ओर बढ़ा, जिसने अंततः इसे एक वैश्विक औद्योगिक शक्ति बना दिया। यह सवाल उठाता है कि भारत के नेतृत्व ने, विशेषकर पंडित नेहरू के तहत, ऐसा आकलन क्यों नहीं किया और कृषि को प्राथमिकता क्यों नहीं दी।
- गांधीवादी विचारधाराओं के प्रभाव के बावजूद, जो ग्रामीण विकास और कृषि पर जोर देती थीं, उद्योग को प्राथमिकता देने का निर्णय एक अलग रणनीतिक विकल्प को दर्शाता है। नेहरू का दृष्टिकोण, जबकि प्रभावशाली था, भारत की आर्थिक परिस्थितियों की तात्कालिक वास्तविकताओं के साथ मेल नहीं खा सकता।
- कृषि बनाम उद्योग: आगे का रास्ता
- उद्योग को कृषि पर प्राथमिकता देने का विकल्प विशेषज्ञों के बीच एक विवादित विषय बना हुआ है, जिसमें उस समय भारत के आर्थिक इतिहास और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं की विभिन्न व्याख्याएँ हैं।
- नेहरूवादी अर्थशास्त्र, जिसका नाम पंडित नेहरू के नाम पर रखा गया है, आज भी स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों में भारत की आर्थिक नीतियों और प्राथमिकताओं को आकार देने में अपनी भूमिका के लिए पहचाना जाता है।
- भारत के प्राथमिक क्षेत्र के लिए कृषि एक स्पष्ट विकल्प प्रतीत होता था, क्योंकि यहाँ उपजाऊ भूमि और मानव संसाधनों की भरपूरता थी।
- हालांकि, उस समय भारतीय कृषि पारंपरिक उपकरणों और तकनीक पर निर्भर थी।
- कृषि का आधुनिकीकरण और अंततः यांत्रिकीकरण स्वदेशी औद्योगिक समर्थन के बिना कठिन होता।
उद्योग का चयन
- उद्योग को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में चुनकर, भारत ने अर्थव्यवस्था को औद्योगिकीकरण करने और कृषि को आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखा।
- औद्योगिकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन: विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाओं के साथ वैश्विक सहमति ने औद्योगिकीकरण को तेज विकास और प्रगति के रास्ते के रूप में समर्थन दिया।
- जो देश औद्योगिकीकरण का विकल्प चुनते थे, उन्हें समर्थन मिलता था और उन्हें संभावित भविष्य के औद्योगिक निर्यातकों के रूप में देखा जाता था, जबकि जो कृषि पर ध्यान केंद्रित करते थे, उन्हें "पिछड़ा" माना जाता था।
- 1990 के दशक में, यह दृष्टिकोण बदल गया, और कृषि पर जोर देना अब पिछड़ेपन का संकेत नहीं माना गया।
रक्षा और औद्योगिक आधार
- द्वितीय विश्व युद्ध ने रक्षा शक्ति के महत्व को प्रदर्शित किया, जो एक मजबूत औद्योगिक आधार और तकनीकी क्षमता पर निर्भर करती है।
- उद्योग को प्राथमिकता देकर, भारत ने कई लक्ष्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा:
- आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना।
- कृषि को तेजी से आधुनिक बनाना।
- एक मजबूत रक्षा क्षमता का निर्माण करना।
सामाजिक परिवर्तन और आधुनिकीकरण की आवश्यकता
- स्वतंत्रता से पहले भी, समाजशास्त्रियों और राष्ट्रीय नेताओं के बीच यह सहमति थी कि भारत को आधुनिक बनाना चाहिए और पारंपरिक प्रथाओं से आगे बढ़ना चाहिए।
- विज्ञान दृष्टिकोण और सामाजिक परिवर्तन को प्रगति के लिए आवश्यक माना गया, जिसने राजनीतिक नेतृत्व को औद्योगिकीकरण का समर्थन करने के लिए प्रेरित किया।
औद्योगिकीकरण की सिद्ध प्रभावशीलता
- भारत की स्वतंत्रता के समय तक, औद्योगिकीकरण के लाभ स्पष्ट थे, और राष्ट्रीय विकास के लिए इसके प्रभावी होने में कोई संदेह नहीं था।
- परिचय: PMF एक संक्षिप्त रूप है जिसका उपयोग "प्राइम मूवर फैक्टर" के लिए किया जाता है, जो अर्थव्यवस्था को संचालित करने वाले महत्वपूर्ण तत्व या क्षेत्र को संदर्भित करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, पाठ में PMF के संदर्भ में नीति में बदलाव की चर्चा की गई है, जिसमें उद्योग से कृषि की ओर परिवर्तन शामिल है।
- पाठ भारत के राजनीतिक नेतृत्व के ऐतिहासिक दृष्टिकोण पर विचार करता है और उनके औद्योगिकीकरण के प्रति झुकाव को अर्थव्यवस्था के PMF के रूप में प्रस्तुत करता है। यह सुझाव देता है कि भारत की संसाधन-संबंधी और स्वभाविक वास्तविकताएँ शायद विकसित और औद्योगिक राष्ट्र के भविष्य के दृष्टिकोण की खोज में अनदेखी की गई थीं।
- पाठ 1990 के दशक में कृषि के वैश्विक दृष्टिकोण में बदलाव का उल्लेख करता है, जिसमें चीन के सफल अनुभव को उजागर किया गया है, जिसने कृषि का उपयोग PMF के रूप में अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और औद्योगिकीकरण की ओर संक्रमण के लिए किया।
आर्थिक सोच में बदलाव
- 2002 में, भारत में एक महत्वपूर्ण नीति परिवर्तन हुआ जब सरकार ने, जो योजना आयोग द्वारा मार्गदर्शित थी, कृषि को अर्थव्यवस्था के लिए नया PMF घोषित किया, उद्योग को प्रतिस्थापित करते हुए। यह निर्णय दसवें योजना (2002-07) का हिस्सा था और इसका उद्देश्य तीन प्रमुख चुनौतियों का समाधान करना था:
- खाद्य सुरक्षा: कृषि उत्पादन में वृद्धि को खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने और वैश्वीकरण की अर्थव्यवस्था में निर्यात अधिशेष उत्पन्न करने के लिए आवश्यक माना गया, विशेषकर विश्व व्यापार संगठन (WTO) के शासन के तहत।
- गरीबी उन्मूलन: कृषि पर जोर देने से ग्रामीण क्षेत्रों में आय बढ़ाने, अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विकास को उत्तेजित करने की उम्मीद थी।
- पहचान की समयबद्धता: जबकि 1990 के मध्य में कृषि के वैश्विक दृष्टिकोण में बदलाव शुरू हो गया था, भारत ने 2002 में इसके PMF के रूप में महत्व को पहचाना। हालाँकि, अब विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं के बीच कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका को लेकर सहमति बन गई है।
अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका
- कृषि और उससे संबंधित गतिविधियाँ भारतीय जनसंख्या के एक महत्वपूर्ण हिस्से के लिए आजीविका का एक प्रमुख स्रोत बनी हुई हैं, जो रोजगार का 54.5% हिस्सा और अर्थव्यवस्था के कुल मूल्य वर्धन (GVA) में 18.8% का योगदान करती हैं।
औद्योगिक विकास और कृषि सुधारों में देरी
- पाठ में यह नोट किया गया है कि जबकि भारत ने आर्थिक सुधारों के बाद औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति करना शुरू किया, कृषि क्षेत्र में सुधारों की शुरुआत बाद में, लगभग 2000 के प्रारंभ में हुई। कृषि सुधारों में देरी के तीन कारणों की पहचान की गई है:
- निजी क्षेत्र की भागीदारी: कृषि हमेशा निजी क्षेत्र की सहभागिता के लिए खुली रही है, जिससे निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए और अधिक निजीकरण को बढ़ावा देना चुनौतीपूर्ण हो गया।
- कॉर्पोरेट निवेश की आवश्यकता: कृषि में विकास और प्रगति को उत्तेजित करने के लिए कॉर्पोरेट निवेश की आवश्यकता थी।
- फोकस में बदलाव: कृषि को कॉर्पोरेट निवेश और निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए और अधिक आकर्षक बनाने की दिशा में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता थी।
भारतीय कृषि क्षेत्र वर्तमान में सुधार और आधुनिकीकरण के संदर्भ में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा है। राष्ट्रीय कृषि बाजार की अत्यंत आवश्यकता है, फिर भी कई राज्यों में आवश्यक कृषि उत्पाद बाजार समिति (APMC) सुधारों को लागू करने की राजनीतिक इच्छा का अभाव है।
कॉर्पोरेट निवेश और भूमि अधिग्रहण
कर्पोरेट निवेश को कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने में एक प्रभावी और पारदर्शी भूमि अधिग्रहण कानून की अनुपस्थिति बाधा उत्पन्न करती है। मौजूदा श्रम कानूनों की जटिलताएँ भी औद्योगिक खेती और श्रम सुधारों के लिए चुनौती प्रस्तुत करती हैं।
कृषि यांत्रिकीकरण और अनुसंधान
- कृषि यांत्रिकीकरण संबंधित उद्योगों में अपर्याप्त निवेश के कारण बाधित है।
- अनुसंधान और विकास में निजी क्षेत्र के निवेश की अत्यंत आवश्यकता है, लेकिन वर्तमान वातावरण ऐसे निवेश के लिए अनुकूल नहीं है।
आपूर्ति श्रृंखला और वस्तु व्यापार
- कृषि क्षेत्र में उचित डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम आवश्यकताओं का अभाव है, साथ ही कृषि वस्तुओं के लिए प्रभावी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की कमी है।
- कृषि उत्पादों में वस्तु व्यापार के विस्तार की आवश्यकता है।
वैश्विक प्रतिस्पर्धा और कृषि की व्यवहार्यता
- कृषि क्षेत्र को विकसित देशों के कृषि क्षेत्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूत करना महत्वपूर्ण है, विशेषकर वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में सब्सिडी और कीमतों के संदर्भ में।
- कृषि को अधिक लाभकारी बनाना आवश्यक है ताकि समकालीन कृषि संकट का समाधान किया जा सके।
संघीय परिपक्वता और जागरूकता
- विशेषज्ञों का सुझाव है कि कृषि क्षेत्र में उचित नीति कदमों को प्राप्त करने के लिए भारत में संघीय परिपक्वता की उच्च डिग्री की आवश्यकता है।
- किसानों के बीच जागरूकता बढ़ाना, साथ ही कृषि संकट को रोकने के लिए उचित सरकारी समर्थन, सकारात्मक परिवर्तन को आगे बढ़ाने में सहायक होगा।
योजना और मिश्रित अर्थव्यवस्था

स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद, भारत को एक योजनाबद्ध और मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया गया। राजनीतिक नेतृत्व ने स्वतंत्रता से पहले ही राष्ट्रीय योजना की आवश्यकता को पहचाना, यह समझते हुए कि सदियों से बनी क्षेत्रीय और अंतःक्षेत्रीय विषमताओं को संबोधित करना आवश्यक है। जनसामान्य की गंभीर गरीबी एक महत्वपूर्ण कारक थी, जिसने सरकार को योजना बनाने के लिए प्रेरित किया, जिससे यह संसाधनों को समान विकास और वृद्धि के लिए सक्रिय रूप से आवंटित और संगठित कर सके।
- संविधान में राज्यों का संघ होने के बावजूद, योजना प्रक्रिया में संघ सरकार में अधिकार का बढ़ता केंद्रीकरण देखा गया, जो आर्थिक गतिविधियों को निर्देशित और नियंत्रित कर रहा था। यह बदलाव वैश्विक घटनाओं जैसे महान अवसाद और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के पुनर्निर्माण से प्रभावित था, जिसने अर्थव्यवस्था में राज्य हस्तक्षेप की आवश्यकता को उजागर किया।
- इसके अतिरिक्त, 20वीं सदी के मध्य में सोवियत संघ और पूर्वी यूरोपीय देशों की आर्थिक सफलताओं ने बाजार की विफलताओं को संबोधित करने के लिए अर्थव्यवस्था में एक मजबूत राज्य की भूमिका के विचार को और भी मजबूत किया।
- कई नव-स्वतंत्र विकासशील देशों के लिए, जैसे भारत, आर्थिक योजना संसाधनों को संगठित करने और निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राथमिकता वाले उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक व्यवहार्य साधन बन गया।
योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का निर्णय इसके संगठनात्मक स्वरूप पर स्पष्टता की आवश्यकता थी - क्या यह एक राज्य या मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी - क्योंकि योजना एक स्वतंत्र बाजार प्रणाली के साथ असंगत थी। सोवियत योजना से प्रेरित होकर, जो एक आदेशात्मक अर्थव्यवस्था थी, भारतीय मॉडल को इसके लोकतांत्रिक ढांचे और मौजूदा निजी स्वामित्व के अनुसार ढाला जाना था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जो समाजवादी प्रवृत्तियों के लिए जाने जाते थे, स्वतंत्रता के बाद भारत में योजना के पीछे एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरे।
राज्य और निजी क्षेत्र की भूमिका
योजना बनाने वालों ने एक संतुलित दृष्टिकोण में विश्वास किया, जहाँ राज्य और निजी क्षेत्र दोनों की महत्वपूर्ण भूमिकाएँ थीं। उन्होंने पहचाना कि जबकि राज्य को कुछ क्षेत्रों में हस्तक्षेप करना आवश्यक होगा, निजी क्षेत्र को उत्पादन और वितरण में महत्वपूर्ण योगदान देने की अनुमति भी दी जानी चाहिए। यह उस समय दोनों क्षेत्रों की ताकतों और कमजोरियों की व्यावहारिक स्वीकृति थी।
राज्य हस्तक्षेप पर विचारों का विकास
भारत की पहली योजना में प्रस्तुत विचार अपने समय से आगे थे। अगले दशकों में, विशेष रूप से 1950 और 1960 के दशक में, अर्थव्यवस्था में राज्य हस्तक्षेप का वैश्विक रुझान था। हालाँकि, पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के अनुभवों ने, जिन्होंने राज्य और बाजार की भूमिकाओं के विभिन्न संतुलन के साथ उच्च विकास दर प्राप्त की, बाद में आर्थिक योजना को संरचित करने के तरीके को प्रभावित किया।
पूर्वी एशियाई चमत्कार और इसके परिणाम
पूर्वी एशियाई चमत्कार, जिसने तीन दशकों में निरंतर उच्च विकास प्रदर्शित किया, ने आर्थिक विकास में राज्य और बाजार की भूमिकाओं के बारे में नई चर्चाओं को प्रेरित किया। इस अनुभव से निकाले गए निष्कर्ष भारत की पहली योजना में व्यक्त विचारों के समान थे। यह बाद में संरेखण ने भारत में प्रारंभिक योजना विचारों की प्रासंगिकता और पूर्वदृष्टि को प्रदर्शित किया।
लोकतांत्रिक ढांचे में योजना बनाने का दृष्टिकोण
योजनाकारों द्वारा कल्पित लोकतांत्रिक संदर्भ में योजना बनाना उत्पादक शक्तियों को पुनः संरेखित करने के लिए बल या मजबूरी के उपयोग को कम करने का मतलब था। इसका ध्यान नए निवेश के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के संसाधनों का उपयोग करने पर था, न कि मौजूदा उत्पादक क्षमता का अधिग्रहण करने पर। कुछ मामलों में उत्पादन के साधनों का सार्वजनिक स्वामित्व आवश्यक हो सकता है, जबकि अन्य मामलों में सार्वजनिक नियमन और नियंत्रण की आवश्यकता हो सकती है।
निष्कर्ष
भारत की आर्थिक योजना के लिए प्रारंभिक दृष्टि, जो पहली योजना में उल्लिखित थी, राज्य हस्तक्षेप और निजी क्षेत्र की पहल के बीच सही संतुलन खोजने के बारे में थी। यह संतुलन अर्थव्यवस्था को स्थायी विकास की ओर मार्गदर्शित करने के लिए महत्वपूर्ण था, जबकि उस लोकतांत्रिक ढांचे का सम्मान करना आवश्यक था जिसमें योजना को लागू किया जाना था। विकसित वैश्विक दृष्टिकोण, विशेष रूप से सफल पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं से, बाद में इन प्रारंभिक विचारों को मजबूत और परिष्कृत किया, जिससे उनकी स्थायी प्रासंगिकता का पता चलता है।
1951 में, भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था का सही सारांश प्रस्तुत किया गया, लेकिन यह 1950 के दशक में विस्तृत विकास से गुजरा। उस दशक के अंत तक, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विचार लगभग मिट गया, लेकिन 1980 के मध्य में पुनः उभरा और 1990 के प्रारंभ में आर्थिक सुधारों के साथ प्रमुखता प्राप्त की।
सुधार प्रक्रिया के दौरान, सरकार ने योजना और योजना आयोग के कार्यों में संशोधन करना शुरू किया, जिसका लक्ष्य अर्थव्यवस्था में सरकार और निजी क्षेत्र की भूमिकाओं को फिर से परिभाषित करना था। यह बदलाव भारत के विकास और विकास को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र पर बढ़ती निर्भरता का संकेत था।
2015 की शुरुआत में, भारत के योजना ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जब सरकार ने योजना आयोग को नीतिगत आयोग से बदल दिया, जो एक नई आर्थिक विचारक संस्था है। इस परिवर्तन का उद्देश्य देश में योजना प्रक्रिया और विधि को नए सिरे से तैयार करना था, जो भारत के विकास योजना के अनुभव के छह दशकों को दर्शाता है।
नीति आयोग का दृष्टिकोण सहयोगी संघवाद, एक नीचे से ऊपर की रणनीति, समग्र और समावेशी विकास, और विकास का एक भारतीय मॉडल तैयार करने की आवश्यकता पर जोर देता है, जो अर्थव्यवस्था की बदलती जरूरतों के अनुरूप है।
आत्मनिर्भरता की पहल
आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य COVID-19 के बाद भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। यह पांच प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है: अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, प्रणालियाँ, जनसंख्या, और मांग। आलोचक इसे पुराने मेक इन इंडिया योजना के समान मानते हैं, लेकिन विशेषज्ञ इसे महामारी द्वारा उजागर की गई वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की सीमाओं के प्रति एक प्रतिक्रिया के रूप में देखते हैं। यह पहल भारत की आवश्यकता को भी दर्शाती है कि उसे अपने आर्थिक मॉडल, पर्यावरणीय संबंध और आर्थिक कूटनीति पर फिर से विचार करना चाहिए।
सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर
भारत की स्वतंत्रता के बाद, प्रमुख राजनीतिक नेताओं के बीच राज्य की अर्थव्यवस्था में एक मजबूत और सक्रिय भूमिका की आवश्यकता के बारे में स्पष्ट सहमति थी। इसने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) का एक विशाल ढांचा स्थापित करने की ओर अग्रसर किया।
PSUs के पीछे का तर्क
- बुनियादी ढांचे की जरूरतें: प्रत्येक अर्थव्यवस्था को बुनियादी ढांचे की एक मजबूत नींव की आवश्यकता होती है, जिसमें बिजली, परिवहन और संचार शामिल हैं। स्वतंत्रता के समय, भारत में इन आवश्यक तत्वों की कमी थी।
- औद्योगिक आवश्यकताएँ: औद्योगिकीकरण के लिए कुछ प्रमुख उद्योगों की आवश्यकता होती है, जिन्हें बुनियादी या अवसंरचना उद्योग कहा जाता है। इनमें रिफाइनरी उत्पाद और बिजली जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
- सरकार की भूमिका: सरकार को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारी निवेश प्रबंधित करने और इन आवश्यक सेवाओं का वितरण सुनिश्चित करने के लिए एकमात्र इकाई के रूप में देखा गया।
भारत के लिए PSUs के विस्तार को एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के लिए आधार तैयार करने के लिए एक आवश्यक कदम के रूप में देखा गया, जहाँ सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र अंततः फल-फूल सकें।
PSUs की स्थापना के समय कई चुनौतियाँ थीं, जिसमें भारी निवेश की आवश्यकता, सार्वजनिक ऋण और कराधान शामिल थे।
PSUs के लाभ और सामाजिक क्षेत्र विकास के उद्देश्य से सरकार ने PSUs से प्राप्त लाभ और लाभांश का उपयोग सामाजिक वस्तुओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सुरक्षा के लिए करने का लक्ष्य रखा। हालाँकि, कई PSUs ने अपेक्षित लाभ उत्पन्न करने में विफलता प्राप्त की और नियमित बजटीय समर्थन की आवश्यकता पाई।
PSUs ने बुनियादी उद्योगों और बुनियादी ढांचे की नींव रखी और निजी क्षेत्र की उद्योगों के उदय के लिए रास्ता तैयार किया।
विकास में PSUs की भूमिका
भारत सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद विकास के विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका की कल्पना की, जिसमें शामिल हैं:
- स्वावलंबन: यह सुनिश्चित करना कि देश आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन स्वयं कर सके।
- संतुलित क्षेत्रीय विकास: कम विकसित क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना ताकि क्षेत्रीय विषमताएँ कम हो सकें।
- छोटी और सहायक उद्योगों का प्रसार: छोटे उद्योगों की वृद्धि को प्रोत्साहित करना जो बड़े उद्योगों का समर्थन करते हैं।
- सस्ती और स्थिर कीमतें: उपभोक्ताओं के लिए सस्ती कीमतें बनाए रखने में मदद करना।
- भुगतान संतुलन में दीर्घकालिक संतुलन: आर्थिक असंतुलनों से बचने के लिए स्थिर भुगतान संतुलन प्राप्त करना।
PSUs की अक्षमता पर प्रारंभिक सहमति
1980 के मध्य तक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक (WB) सहित वैश्विक सहमति थी कि PSUs अक्षमता और अप्रदर्शन कर रहे थे। इस विश्वास ने वाशिंगटन सहमति से प्रेरित होकर कई देशों, भारत सहित, ने इस अवधि के दौरान PSUs का निजीकरण और अवमूल्यन करना शुरू कर दिया।
1990 के दशक के मध्य में, यह समझने का एक नया सहमति उभरी कि राज्य या सरकार को अर्थव्यवस्था से पूरी तरह से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। यह PSUs के आक्रामक निजीकरण से दूर जाने का संकेत था।
भारत ने पहले एक कम महत्वाकांक्षी अवमूल्यन रणनीति अपनाई, जिसका लक्ष्य अवमूल्यित PSUs में नियंत्रक शेयर बनाए रखना था। 2016-17 के वित्तीय वर्ष से शुरू होकर, भारतीय सरकार ने रणनीतिक अवमूल्यन को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया, जो PSUs के स्वामित्व को निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करने को शामिल कर सकता है।
हाल के अवमूल्यन पर ध्यान को कई महत्वपूर्ण समकालीन वास्तविकताओं के संदर्भ में समझा जाना चाहिए:
- निवेश को बढ़ावा देना: अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ावा देने की अत्यधिक आवश्यकता है। अवमूल्यन निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने और आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने में मदद कर सकता है।
- सरकार की प्राथमिकता: सरकार को अवांछनीय आर्थिक गतिविधियों में अपनी भागीदारी कम करने की आवश्यकता है और उन क्षेत्रों में विस्तार करना चाहिए जहाँ निजी क्षेत्र की भागीदारी कम है, जैसे कल्याणकारी कार्य।
- राजस्व उत्पन्न करना: अवमूल्यन हिस्सेदारी की बिक्री, संपत्तियों का मुद्रीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) से बढ़े हुए लाभ के माध्यम से राजस्व उत्पन्न कर सकता है।
- PSUs से बढ़ा हुआ लाभ: PSUs में बहुमत हिस्सेदारी बेचने के माध्यम से, सरकार अपने स्वामित्व की जिम्मेदारियों से मुक्त हो सकती है, जबकि इन कंपनियों से राजस्व के अपने हिस्से को बढ़ा सकती है।
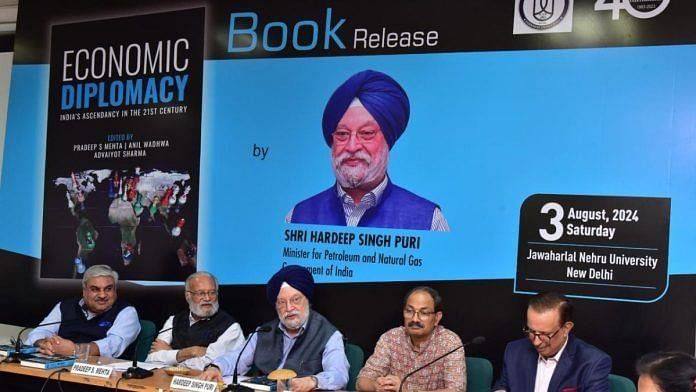

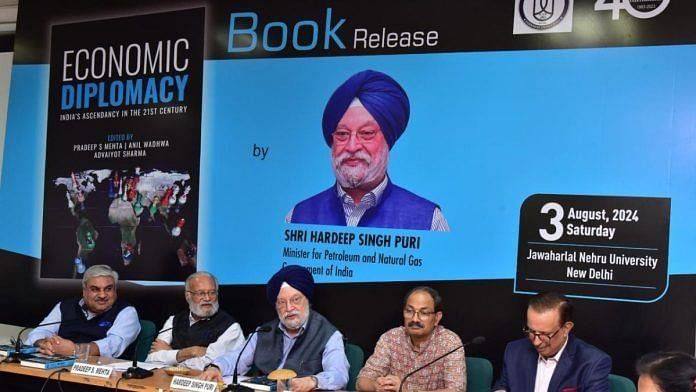

|
289 docs|166 tests
|















