विवेक सिंह का सारांश कृषि - 1 | भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) UPSC CSE के लिए PDF Download
परिचय
कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो सकल मूल्य वर्धन (GVA) में महत्वपूर्ण योगदान करती है। अर्थव्यवस्था की समग्र वृद्धि और विनिर्माण और सेवाओं जैसे अन्य क्षेत्रों के बढ़ते हिस्से के बावजूद, कृषि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है, विशेष रूप से ग्रामीण रोजगार और आजीविका के लिए।
कृषि क्षेत्र में फसल उत्पादन, बागवानी, पशुपालन, मछली पकड़ने, एक्वाकल्चर, और वानिकी जैसे क्रियाकलाप शामिल हैं। ये क्रियाकलाप न केवल भोजन और कच्चे माल प्रदान करते हैं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार में भी योगदान करते हैं।
कृषि का GVA में योगदान अपेक्षाकृत स्थिर रहा है, वर्षों में 18% से 20% के बीच बना हुआ है। यह स्थिरता अन्य क्षेत्रों की तेजी से वृद्धि को देखते हुए उल्लेखनीय है। कुल GVA में कृषि का हिस्सा इसकी खाद्य सुरक्षा प्रदान करने और ग्रामीण आजीविकाओं का समर्थन करने में इसके महत्व को दर्शाता है।
विकास प्रवृत्तियाँ:
कृषि क्षेत्र ने विकास दर में उतार-चढ़ाव का अनुभव किया है, जिसमें मजबूत विकास की अवधि और उसके बाद मंदी आती है। उदाहरण के लिए, 2016-17 में, क्षेत्र की वृद्धि 6.8% थी, जबकि 2018-19 में, वृद्धि दर 2.10% थी।
ऐसे उतार-चढ़ाव अक्सर मानसून के पैटर्न, कीट प्रकोप, और वैश्विक वस्तुओं की कीमतों में बदलाव जैसे कारकों से प्रभावित होते हैं।
संरचनात्मक परिवर्तन:
वर्षों में, कृषि क्षेत्र की संरचना में धीरे-धीरे बदलाव आया है। कुल कृषि उत्पादन में खाद्य अनाज का हिस्सा घटा है, जबकि बागवानी और पशुधन उत्पादों का हिस्सा बढ़ा है।
यह बदलाव उपभोग के पैटर्न में बदलाव और उच्च मूल्य वाले फसलों और पशु उत्पादों के बढ़ते महत्व को दर्शाता है।
नीति समर्थन:
भारतीय सरकार ने कृषि क्षेत्र का समर्थन करने के लिए विभिन्न नीतियों को लागू किया है, जिसमें कुछ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) शामिल हैं, जो किसानों को उनके उत्पादन के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करते हैं।
इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) जैसी योजनाएं किसानों को सीधे आय सहायता प्रदान करती हैं, जिससे उनकी वित्तीय स्थिरता में सुधार होता है।
चुनौतियाँ:
इसके महत्व के बावजूद, कृषि क्षेत्र कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, जैसे जलवायु परिवर्तन, जो वर्षा के पैटर्न और तापमान को प्रभावित करता है, जिससे कृषि अधिक अनिश्चित हो जाती है।
अन्य चुनौतियों में कृषि प्रथाओं का आधुनिकीकरण, किसानों के लिए ऋण तक पहुंच, और सड़क और भंडारण सुविधाओं जैसे बुनियादी ढांचे में सुधार की आवश्यकता शामिल है।
निष्कर्ष:
कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ बनी हुई है, जो भोजन, रोजगार, और कच्चे माल प्रदान करती है। जबकि यह चुनौतियों का सामना करती है, क्षेत्र की मजबूती और विभिन्न योजनाओं और नीतियों के माध्यम से सरकार का समर्थन इसके सतत विकास और अर्थव्यवस्था में योगदान के लिए महत्वपूर्ण है।
कृषि जनगणना 2015-16 के निष्कर्ष
ऑपरेशनल होल्डिंग्स: 2010-11 में 138.35 मिलियन से बढ़कर 2015-16 में 146.45 मिलियन होल्डिंग्स में वृद्धि हुई, जो 5.86% की वृद्धि को दर्शाता है।
ऑपरेटेड एरिया: कुल ऑपरेटेड क्षेत्र 2010-11 में 159.59 मिलियन हेक्टेयर से घटकर 2015-16 में 157.82 मिलियन हेक्टेयर हो गया, जो 1.11% की कमी को दर्शाता है।
औसत आकार: 2015-16 में ऑपरेशनल होल्डिंग्स का औसत आकार 1.08 हेक्टेयर हो गया, जो 2010-11 में 1.15 हेक्टेयर से कम है।
ऑपरेशनल होल्डिंग एक महत्वपूर्ण शब्द है जो विभिन्न कृषि डेटा संदर्भों में उपयोग होता है। इसका अर्थ है एक व्यक्ति द्वारा प्रबंधित या संचालित कृषि भूमि, चाहे वह अकेले हो या अन्य लोगों के साथ, स्वामित्व शीर्षक, आकार, या स्थान की परवाह किए बिना। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति के पास चार अलग-अलग स्थानों पर भूमि है और वह उसे प्रबंधित करता है, तो सभी भूमि को एक ऑपरेशनल होल्डिंग माना जाएगा। इसी तरह, यदि कोई व्यक्ति चार अलग-अलग मालिकों से भूमि किराए पर लेता है लेकिन खेती का प्रबंधन करता है, तो यह भी एक ऑपरेशनल होल्डिंग के रूप में गिना जाएगा।
11वीं कृषि जनगणना (2021-22) जुलाई 2022 में शुरू की गई थी।
भारत में कृषि का संक्षिप्त इतिहास
कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो गरीबी को कम करने, रोजगार सृजन, और राष्ट्रीय GDP में योगदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि 1950-51 में कृषि का GDP में हिस्सा 50% से घटकर 2019-20 में 16% हो गया है, फिर भी इसकी महत्वता बनी हुई है। 1950-51 में, कृषि ने 70% रोजगार का योगदान दिया, लेकिन अब यह लगभग 42% है। इस गिरावट के बावजूद, भारतीय कृषि की वृद्धि 'समावेशी विकास' के लिए आवश्यक है।
विश्व बैंक की रिपोर्ट बताती है कि कृषि से उत्पन्न GDP वृद्धि गरीबी को कम करने में अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम से कम दो गुना अधिक प्रभावी है।
1951 और 1966 के बीच, खाद्य अनाज उत्पादन की दर 2.8% प्रति वर्ष थी, जो बढ़ती जनसंख्या की खपत मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त थी, जो 2% प्रति वर्ष से अधिक बढ़ रही थी। इसके परिणामस्वरूप, भारत ने अपने बढ़ते जनसंख्या को खिलाने के लिए 1950 के दशक के मध्य में खाद्य अनाज आयात पर निर्भर रहना शुरू कर दिया। 1956 में, भारत ने अमेरिका के साथ सार्वजनिक कानून (PL) 480 समझौता किया, जिससे मुख्य रूप से गेहूं के रूप में खाद्य सहायता प्राप्त हुई।
1962 में चीन के साथ युद्ध और 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के कारण, भारत ग्रामीण विकास में निवेश नहीं कर सका, और 1965 और 1966 में लगातार सूखे ने गंभीर खाद्य संकट पैदा किया। खाद्य अनाज उत्पादन और उपज क्रमशः 1966 में 19% और 17% घट गई। सामूहिक अकाल को रोकने के लिए खाद्य अनाज आयात बढ़ा दिया गया। शीत युद्ध के दौरान, खाद्य सहायता को राजनीतिक उपकरण के रूप में उपयोग किया गया, और भारत ने इसका अनुभव किया जब सूखे के दौरान अमेरिकी शिपमेंट अस्थायी रूप से रोक दिए गए। इससे भारतीय नेताओं को विदेशी स्रोतों पर खाद्य सुरक्षा के लिए निर्भरता के राजनीतिक जोखिमों को पहचानने और खाद्य अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित किया।
हरित क्रांति का अवलोकन
हरित क्रांति कृषि विधियों में एक परिवर्तन का प्रतीक है जो 1940 के दशक में मेक्सिको में शुरू हुआ। इस आंदोलन का श्रेय अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को दिया जाता है, जिन्होंने कृषि सुधार के लिए समर्पित थे। 1940 के दशक में, बोरलॉग ने मेक्सिको में शोध किया, जिससे नए, रोग-प्रतिरोधक, उच्च उपज वाले गेहूँ के किस्मों का विकास हुआ। इसकी सफलता के कारण, हरित क्रांति से जुड़े प्रौद्योगिकियाँ 1950 और 1960 के दशक में वैश्विक स्तर पर फैल गईं।
हरित क्रांति में उच्च उपज वाले किस्म (HYV) के बीजों, उर्वरकों, कीटनाशकों, सुधारित सिंचाई, यांत्रिकीकरण, और आधुनिक कृषि तकनीकों का परिचय शामिल है। इसका मूल विचार खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना और अधिक पश्चिमी शैली की खेती के प्रथाओं को अपनाना था। भारत में, M.S. स्वामीनाथन को "हरित क्रांति के पिता" के रूप में सम्मानित किया जाता है।
भारत में हरित क्रांति के चरण
चरण I (1966-72): 1966 में, भारत ने 18,000 टन HYV गेहूँ के बीज आयात किए, जिन्हें पंजाब, हरियाणा, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सिंचित क्षेत्रों में वितरित किया गया।
चरण II (1973-80): HYV की तकनीक गेहूँ से चावल तक विस्तारित की गई, जिसमें निजी और सरकारी दोनों ट्यूबवेलों की वृद्धि हुई। इस चरण ने हरित क्रांति को पूर्वी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, और तमिलनाडु तक फैला दिया।
चरण III (1981-90): इस चरण में, हरित क्रांति ने पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, और ओडिशा के पहले कम विकास वाले क्षेत्रों तक पहुंच बनाई।
हरित क्रांति का प्रभाव
हरित क्रांति ने भारत में खाद्य अनाज उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि की, जो 1966-67 में 74 मिलियन टन (MT) से बढ़कर 1971-72 में 105 MT हो गया। इस समय तक, भारत खाद्य अनाज में आत्मनिर्भर बन गया, आयात पर निर्भरता को लगभग शून्य कर दिया।
वर्तमान कृषि स्थिति
2022-23 तक, भारत में बागवानी उत्पादन लगभग 342 MT तक पहुंच गया, जबकि खाद्य अनाज उत्पादन 324 MT था।
भारत दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है और चावल, गेहूँ, गन्ना, और विभिन्न फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
देश चावल का सबसे बड़ा निर्यातक और गोमांस और कपास का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी है।
2021-22 के वित्तीय वर्ष में, भारत के कृषि निर्यात 50 बिलियन डॉलर थे, जबकि आयात 31 बिलियन डॉलर थे। यह बदलाव उल्लेखनीय है, यह देखते हुए कि भारत ने 1960 के दशक के मध्य में अनाज के लिए अमेरिकी आयात पर निर्भर किया था।
डॉ. वेरघीस कुरियन और श्वेत क्रांति
1949 में, डॉ. वेरघीस कुरियन, जिन्हें "भारत के दूधवाले" के नाम से जाना जाता है, ने आनंद, गुजरात में अपने करियर की शुरुआत की। सरकारी क्रीमरी में काम करते समय, उन्होंने देखा कि गरीब और अनपढ़ किसान दूध वितरकों द्वारा शोषित हो रहे थे। उच्च गुणवत्ता का दूध उत्पादन करने के बावजूद, इन किसानों को उचित भुगतान नहीं किया जा रहा था और उन्हें विक्रेताओं के पास सीधे बेचने से रोका जा रहा था।
त्रिभुवंदास पटेल, सहकारी आंदोलन के एक नेता से प्रेरित होकर, कुरियन और पटेल ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए केडिया जिले में सहकारी मॉडल पर काम करना शुरू किया।
इस प्रयास ने 1949 में "अमूल" की स्थापना की, जिसे आधिकारिक रूप से काइरा जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ लिमिटेड (KDCMPUL) के नाम से जाना जाता है। प्रारंभ में, अमूल के पास केवल दो सहकारी समितियां थीं और दूध की आपूर्ति केवल 247 लीटर थी।
अमूल का सहकारी मॉडल लोकप्रिय हो गया और सरकार का ध्यान आकर्षित किया। 1964 में, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने आनंद का दौरा किया और अमूल के नए पशु चारा संयंत्र का उद्घाटन किया। किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार पर इस मॉडल के प्रभाव से प्रभावित होकर, उन्होंने डॉ. कुरियन को इसे देशभर में दोहराने के लिए प्रेरित किया।
इसके लिए, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) 1965 में स्थापित किया गया, जिसमें डॉ. कुरियन को प्रमुखता दी गई।
इस दौरान, दूध की मांग आपूर्ति से अधिक होने लगी और वित्तपोषण एक महत्वपूर्ण चुनौती बन गया। 1969 में, NDDB ने ऑपरेशन फ्लड शुरू करने के लिए विश्व बैंक से ऋण प्राप्त किया, जिसका उद्देश्य भारत में आनंद मॉडल को दोहराना था।
ऑपरेशन फ्लड के प्राथमिक उद्देश्यों में शामिल हैं:
- दूध उत्पादन बढ़ाना (दूध की "बाढ़"),
- ग्रामीण आय बढ़ाना,
- उपभोक्ताओं के लिए उचित कीमतें सुनिश्चित करना।
ऑपरेशन फ्लड व्यवसाय मॉडल की तीन-स्तरीय संरचना
गाँव की सहकारी समिति:
गाँव स्तर पर, दूध उत्पादक एक गाँव डेयरी सहकारी समिति (DCS) बनाते हैं।
कोई भी उत्पादक एक शेयर खरीदकर और दूध को केवल समिति को बेचने के लिए सहमत होकर इसमें शामिल हो सकता है।
प्रत्येक DCS में एक दूध संग्रह केंद्र होता है जहाँ सदस्य रोजाना अपना दूध देते हैं।
दूध की गुणवत्ता का परीक्षण किया जाता है, और भुगतान वसा और SNF (सॉलिड-नॉट-फैट) सामग्री के आधार पर किया जाता है।
वर्ष के अंत में, DCS के लाभ का एक हिस्सा सदस्यों को उन दूध की मात्रा के आधार पर एक पैट्रोनिज़ बोनस के रूप में वितरित किया जाता है जो उन्होंने उपलब्ध कराया।
जिला संघ:
एक जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ जिले के दूध सहकारी समितियों के स्वामित्व में होता है।
संघ इन समितियों से दूध खरीदता है, इसे प्रोसेस करता है, और तरल दूध और डेयरी उत्पादों का विपणन करता है।
कई संघ DCSs को आवश्यक इनपुट और सेवाएं भी प्रदान करते हैं, जैसे कि चारा, पशु चिकित्सा देखभाल, और दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए कृत्रिम गर्भाधान।
संघ के कर्मचारी DCS नेताओं और कर्मचारियों को प्रशिक्षण और परामर्श सेवाएं प्रदान करते हैं।
राज्य संघ:
एक राज्य में जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ एक राज्य संघ बनाते हैं, जो अपने सदस्यों के संघों के तरल दूध और उत्पादों का विपणन करने के लिए जिम्मेदार होता है।
कुछ संघ चारा का निर्माण भी करते हैं और अन्य संघ गतिविधियों में सहायता करते हैं।
प्रक्रिया अवलोकन
गाँव की सहकारी समिति: दूध उत्पादकों से गाँव स्तर पर संग्रहित किया जाता है।
जिला दूध सहकारी संघ: संग्रहित दूध को जिला स्तर पर प्रोसेस किया जाता है।
राज्य विपणन संघ: प्रोसेस किए गए दूध और उत्पादों का विपणन राज्य स्तर पर किया जाता है।
श्वेत क्रांति की उपलब्धियाँ
भारत में दूध उत्पादन 20 मिलियन MT से बढ़कर 100 मिलियन MT हो गया, जो डेयरी सहकारी आंदोलन के कारण है।
भारत 2020-21 में 210 MT के साथ दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बन गया।
डेयरी सहकारी आंदोलन 22 राज्यों के 180 जिलों में 125,000 से अधिक गाँवों में फैल गया।
गुलाबी क्रांति
गुलाबी क्रांति भारत में मांस और पोल्ट्री प्रसंस्करण क्षेत्र में सुधार पर केंद्रित है, जिसमें प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण, विशेषीकरण, और मानकीकरण शामिल है।
प्रौद्योगिकी उन्नयन और औद्योगिकीकरण भारतीय संस्थाओं के लिए वैश्विक मानकों को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं, और सामूहिक उत्पादन क्षमताओं का विकास उत्पादकता में सुधार करेगा।
आधुनिकीकरण के लिए प्रमुख कदम:
- उन्नत मांस प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करना।
- मांस उत्पादन के लिए नर भैंस बकरियों को उठाने के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास करना।
- कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत भैंस का पालन करने वाले किसानों की संख्या बढ़ाना।
- पशुपालन के लिए रोगमुक्त क्षेत्रों की स्थापना करना।
वर्तमान स्थिति
भारत ने मांस उत्पादन में महत्वपूर्ण प्रगति की है, 2012 में भैंस के मांस का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया।
भारतीय मांस के प्रमुख आयातक मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं।
कृषि फसल वर्ष: 1 जुलाई - 30 जून
खरीफ फसलों का विपणन सत्र: 1 अक्टूबर से शुरू होता है
रबी फसलों का विपणन सत्र: 1 अप्रैल से शुरू होता है
प्रत्येक रबी{ "error": { "message": "This model's maximum context length is 128000 tokens. However, your messages resulted in 355093 tokens. Please reduce the length of the messages.", "type": "invalid_request_error", "param": "messages", "code": "context_length_exceeded" } }
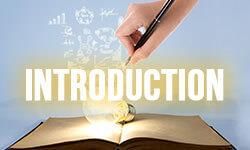




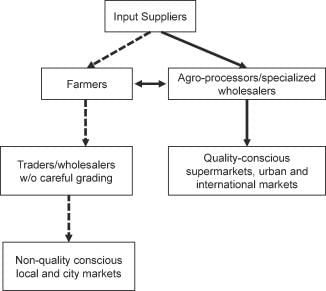


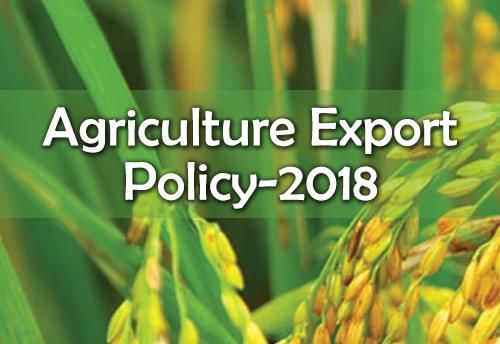
बाजार पहुंच से संबंधित मुद्दों का समाधान अक्सर लंबे समय तक चलता है, कभी-कभी महीनों या यहां तक कि वर्षों तक, इससे पहले कि देश उत्पादों को अपने बाजारों में प्रवेश करने की अनुमति दें। जबकि शुल्क बाधाएं वर्षों से मुक्त व्यापार समझौतों और क्षेत्रीय व्यापार समझौतों के कारण घट रही हैं, गैर-शुल्क बाधाएं (NTBs) और कठोर गुणवत्ता/फाइटो-सैनिटरी मानक बाजार पहुंच को रोकने या प्रतिबंधित करने के लिए अधिक सामान्य होते जा रहे हैं।
- बाजार पहुंच से संबंधित मुद्दों का समाधान अक्सर लंबे समय तक चलता है, कभी-कभी महीनों या यहां तक कि वर्षों तक, इससे पहले कि देश उत्पादों को अपने बाजारों में प्रवेश करने की अनुमति दें।
- जबकि शुल्क बाधाएं वर्षों से मुक्त व्यापार समझौतों और क्षेत्रीय व्यापार समझौतों के कारण घट रही हैं, गैर-शुल्क बाधाएं (NTBs) और कठोर गुणवत्ता/फाइटो-सैनिटरी मानक बाजार पहुंच को रोकने या प्रतिबंधित करने के लिए अधिक सामान्य होते जा रहे हैं।
- इन बाधाओं के बारे में चेतावनियों और अलर्ट का त्वरित उत्तर देना आवश्यक है और यह सुनिश्चित करना कि किसी भी चिंताओं या समस्याओं को उत्पादकों, प्रसंस्करणकर्ताओं और निर्यातकों के साथ साझा किया जाए।
- एक प्रभावी प्रतिक्रिया तंत्र के बिना, अस्थायी प्रतिबंधों या बैन का जोखिम बढ़ जाता है, और ऐसे बैन को हटाने में लंबा समय लग सकता है। उदाहरण के लिए, EU के लिए फलों और सब्जियों पर और सऊदी अरब के लिए हरी मिर्च पर बैन पहले भी लगे हैं।
7. समुद्री प्रोटोकॉल का विकास:
- नाशवान वस्तुओं के लिए समुद्री प्रोटोकॉल का विकास लंबी दूरी के बाजारों के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। नाशवान वस्तुओं का निर्यात विशेष भंडारण, परिवहन, और विशिष्ट तापमान पर संभालने की आवश्यकता होती है। चूंकि समय एक महत्वपूर्ण कारक है और एयर फ्रीट निर्यातकों के लिए महंगा होता है, विभिन्न निर्यात योग्य वस्तुओं के लिए समुद्री प्रोटोकॉल स्थापित करना भारत के ताजे उत्पादों के निर्यात को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है।
- एक समुद्री प्रोटोकॉल उस परिपक्वता स्तर को निर्धारित करेगा जो समुद्री परिवहन के लिए उत्पाद की कटाई के लिए अनुकूल है। यह पहल शिपिंग लाइनों, रीफर सेवा प्रदाताओं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, और कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) के साथ सहयोग में की जानी चाहिए।
- फिलिपींस और इक्वाडोर जैसे देशों ने केले के निर्यात के लिए समुद्री प्रोटोकॉल सफलतापूर्वक विकसित किए हैं, जो क्रमशः 40 और 24 दिनों के समुद्री परिवहन की अनुमति देते हैं। उदाहरण के लिए, फिलिपींस मध्य पूर्व में केले का निर्यात करता है, जिसमें लगभग 18 दिन लगते हैं, जबकि भारत वर्तमान में 2-4 दिन के ट्रांजिट अवधि में उत्पादों को भेजने में सक्षम है। इसलिए, समुद्री प्रोटोकॉल का विकास भारत के लिए व्यापार के अवसरों को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है।
8. अनुपालन मूल्यांकन:
कई आयात करने वाले देश भारत की निर्यात निरीक्षण और नियंत्रण प्रक्रियाओं को मान्यता नहीं देते। भारतीय परीक्षण प्रक्रियाओं और अनुरूपता मानकों की इस मान्यता की कमी निर्यातकों और इसके परिणामस्वरूप किसानों के लिए महंगी साबित हो सकती है। अक्सर,
- देश भर में विभिन्न प्रयोगशालाएँ कई और दोहराए गए परीक्षण कर रही हैं, जिससे मसालों, जैविक खाद्य पदार्थों, और बासमती चावल जैसे उत्पादों के लिए परीक्षण बढ़ रहा है।
- सरकार को इस मुद्दे के समाधान के लिए द्विपक्षीय चर्चाओं के दौरान जातीय और जैविक उत्पादों एवं मानकों की आपसी मान्यता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
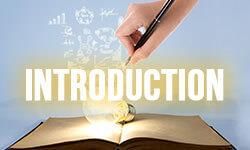




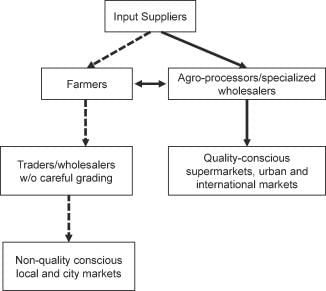


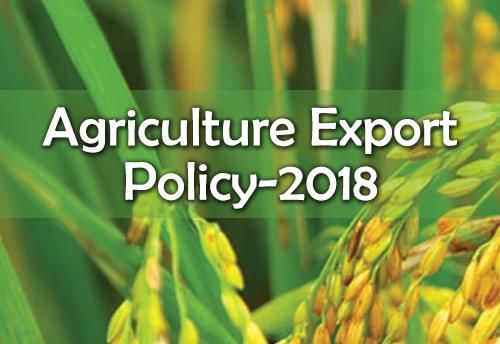
|
289 docs|166 tests
|















