रामेश सिंह सारांश: उद्योग और अवसंरचना - 2 | भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) UPSC CSE के लिए PDF Download
व्यवसाय करने में आसानी
- Doing Business रिपोर्ट, विश्व बैंक समूह की एक वार्षिक प्रकाशन (2004 से) है जो दुनिया के देशों को उन 'नियमों के आधार पर रैंक करती है जो व्यापार गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं और जो इसे रोकते हैं।
- इसे आमतौर पर 'व्यवसाय करने में आसानी रिपोर्ट' के रूप में जाना जाता है, जो निम्नलिखित 12 मानकों पर देशों में व्यापार नियमों की स्थिति को मापता है।
- Doing Business 2020 रिपोर्ट में भारत को 190 देशों में 63वां स्थान दिया गया है। यह पिछले रिपोर्ट के मुकाबले 14 रैंक की छलांग को दर्शाता है।
- हालांकि, केवल दो शहर, दिल्ली और मुंबई इस रिपोर्ट में शामिल हैं, यह देश में व्यापार नियमों के वातावरण के बारे में काफी कुछ बताता है।
- रिपोर्ट ने भारत को उन दस अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में मान्यता दी है जिन्होंने सबसे अधिक सुधार किया है (2014 में 142वें से 2019 में 63वें तक)।
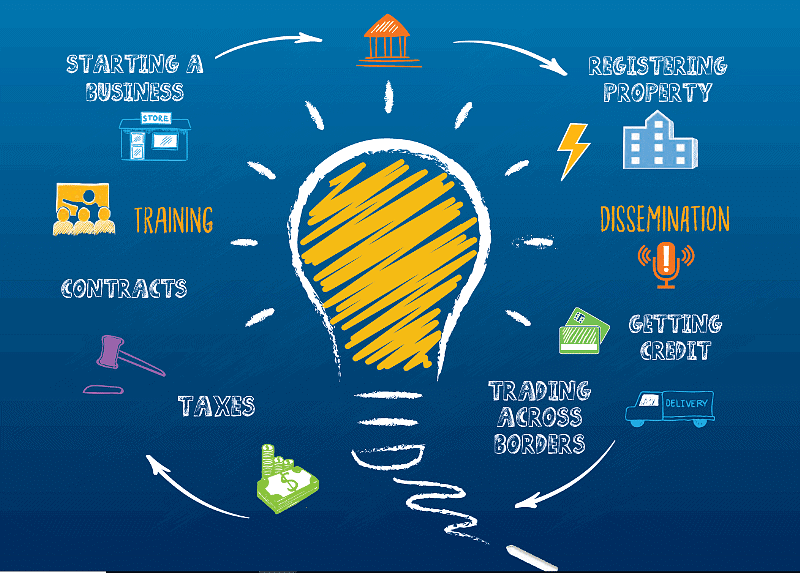
भारत में निर्माण
- Make in India की शुरुआत सितंबर 2014 में भारत सरकार द्वारा की गई थी ताकि बहुराष्ट्रीय और घरेलू कंपनियों को अपने उत्पादों का निर्माण भारत में करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
- यह पहल न केवल निर्माण बल्कि संबंधित अवसंरचना और सेवा क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित की गई है।
मुख्य विशेषताएँ:
- (i) विजन: भारत में पूंजी और तकनीकी निवेश को आकर्षित करना, जिससे यह वैश्विक FDI में शीर्ष पर पहुँच सके, यहां तक कि चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका को भी पीछे छोड़ सके।
- (ii) उद्देश्य: अर्थव्यवस्था के 25 प्रमुख क्षेत्रों में नौकरी सृजन और कौशल संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करना, जिसमें ऑटोमोबाइल, उड्डयन, जीव विज्ञान, रक्षा निर्माण, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, खाद्य प्रसंस्करण, तेल और गैस, और फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं।
- (iii) लोगो: यह अशोक चक्र से प्रेरित है - यह गियर से बना एक चलते हुए सिंह का प्रतीक है, जो निर्माण, शक्ति और राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक है।
- (iv) दुनिया के लिए भारत में असेंबल करें: वर्तमान वातावरण भारत को एक 'अविस्मरणीय' अवसर प्रदान करता है ताकि यह चीन जैसे श्रम-गहन, निर्यात पथ का निर्धारण कर सके और इस प्रकार अद्वितीय नौकरी के अवसर पैदा कर सके। इसके लिए भारत को दुनिया के लिए भारत में असेंबल को भारत में निर्माण में एकीकृत करने की आवश्यकता है।
स्टार्ट-अप इंडिया
- स्टार्ट-अप इंडिया योजना को जनवरी 2016 में भारत सरकार द्वारा एक नारे के साथ लॉन्च किया गया, "स्टार्ट-अप इंडिया और स्टैंड-अप इंडिया"।
- इस मिशन/योजना का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना, स्थायी आर्थिक विकास को प्रेरित करना और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है।
- तकनीकी क्षेत्र के अलावा, स्टार्ट-अप आंदोलन कृषि, विनिर्माण, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसे कई अन्य क्षेत्रों में भी विस्तारित होगा।
- यह योजना मौजूदा टियर 1 शहरों से टियर 2 और टियर 3 शहरों, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी विस्तारित होगी।
- सरकार द्वारा उठाए गए नीतिगत कदमों का देश में नवाचार और उद्यमिता पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
- जिले स्तर पर स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है ताकि आय सृजन का समावेशी प्रभाव基层 स्तर पर महसूस किया जा सके।
- वर्तमान में स्टार्ट-अप्स की स्थिति।
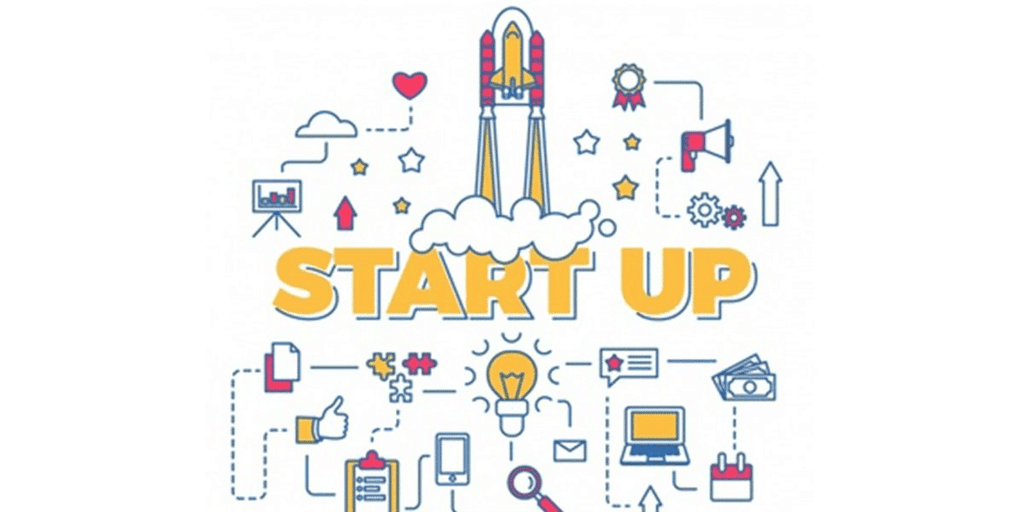
उद्योग 4.0
- उद्योग 4.0, जिसे चौथी औद्योगिक क्रांति के रूप में जाना जाता है, में क्लाउड कंप्यूटिंग, IoT, मशीन लर्निंग, और AI जैसी तकनीकों को उत्पादन में समाहित किया गया है ताकि दक्षता में वृद्धि हो सके।
- भारत धीरे-धीरे इन तकनीकों को उत्पादन में अपनाने की दिशा में बढ़ रहा है, जिसका लक्ष्य व्यापक कार्यान्वयन है।
- मुख्य नीतिगत पहलों में इंटरनेट की पहुंच बढ़ाना, सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता, और उन्नत विनिर्माण के लिए अनुकूल माहौल बनाना शामिल है।
- सरकारी पहलों जैसे SAMARTH और उद्योग भारत 4.0 जागरूकता और प्रदर्शनों के माध्यम से विनिर्माण में तकनीकी समाधानों को बढ़ावा देती हैं।
- 2018 में स्थापित चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र उभरती तकनीकों के लिए नीतिगत ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है।
- नवाचार को बढ़ावा देने के प्रयासों में इनक्यूबेशन, उद्योग-शिक्षा साझेदारी, फंडिंग, और आई.पी. शासन को मजबूत करना शामिल है।
- भारत का आई.पी. आधुनिकीकरण पर ध्यान देने से घरेलू पेटेंट फाइलिंग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, जो ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर एक बदलाव को दर्शाता है।
- ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के अनुसार, भारत ने वैश्विक स्तर पर 40वां स्थान प्राप्त किया और निम्न-मध्यम आय समूह में सबसे नवाचारी राष्ट्र बन गया, वियतनाम को पीछे छोड़ते हुए।
COVID-19 और औद्योगिक सुधार
- COVID-19 के प्रतिक्रिया में, भारत ने मई 2020 में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए भारत अभियान शुरू किया।
- औद्योगिक सुधारों में कुछ रक्षा आयातों पर प्रतिबंध लगाना शामिल था ताकि स्वदेशीकरण को बढ़ावा दिया जा सके और रक्षा निर्माण में 74% FDI को स्वचालित मार्ग के तहत अनुमति दी गई।
- आर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड (OFB) को कॉर्पोरेट बनाने और रक्षा उत्पादन में दक्षता और स्वायत्तता बढ़ाने के लिए सूचीबद्ध किया जाना था।
- अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया, जिसमें निजी कंपनियों को ISRO सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करना और भू-स्थानिक डेटा नीतियों को आसान बनाना शामिल था।
- एविएशन सुधारों में PPP मोड पर 6 हवाईअड्डों की नीलामी, हवाई क्षेत्र की पाबंदियों को आसान बनाना, और MRO कर संरचनाओं का युक्तिकरण शामिल था ताकि भारत को MRO केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके।
- कोयले की वाणिज्यिक खनन को निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ राजस्व-साझाकरण के आधार पर निविदा के माध्यम से पेश किया गया, जिससे सरकारी एकाधिकार समाप्त हुआ।
- शक्ति क्षेत्र के सुधारों का उद्देश्य एक नई tarif नीति के आधार पर संघ शासित क्षेत्रों में बिजली उपयोगिताओं का निजीकरण करना था ताकि परिचालन दक्षता और व्यावसायिकता बढ़ाई जा सके।
भारतीय अवसंरचना
परिचय
- अवसंरचना एक अर्थव्यवस्था की 'जीवन रेखा' है, जैसे कि प्रोटीन मानव शरीर की जीवन रेखा है।
- जिस भी क्षेत्र को अर्थव्यवस्था की प्रमुख प्रेरक शक्ति माना जाता है, वह प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक हो सकता है।
- दुनिया भर में अवसंरचना के रूप में तीन क्षेत्रों को माना जाता है: शक्ति, परिवहन, और संवाद।
- चूंकि अवसंरचना पूरे अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाती है।
आधिकारिक विचारधारा
- भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास की संभावनाओं को पूरा करने के लिए गुणवत्ता और कुशल बुनियादी ढाँचा सेवाओं की स्थापना आवश्यक है। अब यह व्यापक रूप से माना जा रहा है कि सभी बुनियादी ढाँचा सेवाओं के लिए सरकार पर पूरी निर्भरता निवेश के पर्याप्त स्तर, तकनीकी दक्षता, उपयोगकर्ता शुल्क के उचित प्रवर्तन और प्रतिस्पर्धात्मक बाजार संरचना से संबंधित कठिनाइयाँ उत्पन्न करती है। निजी उत्पादन पर पूरी निर्भरता, विशेष रूप से उचित विनियमन के बिना, भी सर्वोत्तम परिणाम उत्पन्न करने की संभावना नहीं है। बुनियादी ढाँचा के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तनकारी बदलाव आया है जब से नई नीति थिंक टैंक Niti Aayog का गठन हुआ है।
UDAY योजना
- DISCOMs के वित्तीय और संचालन में सुधार और समस्या के लिए एक स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए, UDAY (Ujwal DISCOM Assurance Yojana) को भारत सरकार द्वारा नवंबर 2015 में लॉन्च किया गया।
- यह योजना DISCOMs के ब्याज के बोझ, बिजली की लागत और उनके AT&C (Aggregate Transmission & Technical) हानियों को कम करने का भी लक्ष्य रखती है।
- पारंपरिक मुद्दों के कारण, DISCOMs एक दुष्चक्र में फंसे हुए हैं जहाँ संचालन की हानियों को कर्ज द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। 2014-15 तक DISCOMs का बकाया कर्ज ₹4.3 लाख करोड़ था, जिसमें ब्याज दरें 14-15 प्रतिशत तक थीं और AT&C हानियाँ 22 प्रतिशत तक थीं।
- यह योजना क्षेत्र के अतीत और संभावित भविष्य के मुद्दों का स्थायी समाधान प्रदान करके जीवंत और कुशल DISCOMs के उदय की सुनिश्चितता देती है।
- UDAY DISCOMs को अगले 2-3 वर्षों में संतुलन बनाने का अवसर प्रदान करती है।
- UDAY का प्रदर्शन: सरकार के अनुसार, योजना का प्रदर्शन बहुत सकारात्मक नहीं कहा जा सकता। इसे लागू करने वाले 28 राज्यों में से 10 ने 2019-20 (अप्रैल-नवंबर) में न तो हानियाँ कम कीं और न ही लाभ में वृद्धि दिखाई।
- हालांकि, अधिकांश राज्यों ने ACS-ARR अंतर को कम करने और AT&C हानियों को घटाने में सुधार किया है, वे UDAY कार्यक्रम के अनुसार लक्ष्यों को प्राप्त करने में काफी पीछे हैं।
रेलवे
- भारतीय रेलवे (IR) कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। तेज़ी से क्षमता निर्माण के लिए, IR परियोजना निष्पादन क्षमताओं को बढ़ाने के महत्व को मानता है। रेलवे बुनियादी ढांचे में योजना निवेश के लिए आवश्यक संसाधनों की विशालता को देखते हुए, और सार्वजनिक संसाधनों की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, IR इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त आंतरिक अधिशेष उत्पन्न करने और वित्तपोषण के नवाचारी तरीकों का लाभ उठाने के प्रयास कर रहा है। महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि समर्पित माल गलियारे, उच्च गति रेलवे, उच्च क्षमता वाले रोलिंग स्टॉक, अंतिम मील रेलवे लिंक और पोर्ट कनेक्टिविटी में निवेश को प्राथमिकता देने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, और उपलब्ध संसाधनों को पूरा करने के लिए निजी और एफडीआई निवेश को आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है।

उच्च गति ट्रेन परियोजना: जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (JICA) की विस्तृत रिपोर्ट को दिसंबर 2015 में सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया। इस परियोजना को लागू करने के लिए रेलवे मंत्रालय से 50 प्रतिशत इक्विटी भागीदारी और महाराष्ट्र और गुजरात की राज्य सरकारों से 50 प्रतिशत भागीदारी के साथ एक नया विशेष प्रयोजन वाहन स्थापित किया जाएगा।
ट्रेन 18: भारत की पहली इंजन-रहित, अर्ध उच्च गति ट्रेन (160 किमी/घंटा), ट्रेन 18 (जिसका नाम बदलकर वंदे भारत एक्सप्रेस रखा गया) को फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया। यह ट्रेन बेहतरीन सुविधाओं से सुसज्जित है।
सड़कें
लगभग 59.64 लाख किमी की सड़क नेटवर्क के साथ, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं, भारत के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। देश में NH लाख किमी है और यह सड़क यातायात का लगभग 40 प्रतिशत वहन करता है। NHDP का वित्तपोषण।
पेट्रोल और डीजल पर लगाए गए ईंधन सेस का एक हिस्सा NHAI को NHDP के कार्यान्वयन के लिए वित्त पोषण के लिए आवंटित किया जाता है। NHAI इस सेस प्रवाह का उपयोग करके ऋण बाजार से अतिरिक्त धन उधार लेता है। अब तक, ऐसे उधारी केवल 54 EG (पूंजीगत लाभ कर छूट) बांडों के माध्यम से जुटाए गए धन तक सीमित रही हैं और अल्पकालिक ओवरड्राफ्ट सुविधा का उपयोग किया गया है। सरकार ने NHDP के तहत परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए विश्व बैंक (यूएस $ 1,965 मिलियन), एशियाई विकास बैंक (यूएस $ 1,605 मिलियन) और जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक (32,060 मिलियन येन) से भी ऋण लिए हैं, जो NHAI को आंशिक रूप से अनुदान और आंशिक रूप से ऋण के रूप में प्रदान किए जाते हैं। NHAI ने सूरत-मानोर एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए ADB से सीधे यूएस $ 180 मिलियन का ऋण भी लिया है।
प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)
- 500 व्यक्तियों और उससे अधिक की जनसंख्या वाले समतल क्षेत्रों में और 250 व्यक्तियों और उससे अधिक की जनसंख्या वाले पहाड़ी राज्यों, जनजातीय (अनुसूची V) क्षेत्रों, रेगिस्तानी क्षेत्रों, और LWE-प्रभावित जिलों में योग्य अज्ञात बस्तियों को एकल सभी मौसम की सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए शुरू की गई।
- ग्रामीण सड़कों को भारत निर्माण के छह घटकों में से एक के रूप में भी पहचाना गया है, जिसका लक्ष्य सभी गांवों को सभी मौसम की सड़क संपर्क प्रदान करना है, जिनकी जनसंख्या 1,000 है (पहाड़ी या जनजातीय क्षेत्रों में 500 की स्थिति में)।
भारतमाला परियोजना

- 2015-16 में शुरू किया गया, यह एक नया छत्र कार्यक्रम है जो राजमार्ग क्षेत्र पर केंद्रित है, जो देश के भीतर माल और यात्री आंदोलन की दक्षता को अनुकूलित करने पर ध्यान देता है।
- इसका उद्देश्य आर्थिक गलियारों, अंतर गलियारों और फीडर मार्गों, राष्ट्रीय गलियारा दक्षता सुधार, सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क सड़कें, तटीय और बंदरगाह संपर्क सड़कें, और ग्रिन-फील्ड एक्सप्रेसवे के विकास जैसे प्रभावी हस्तक्षेपों के माध्यम से महत्वपूर्ण अवसंरचना अंतराल को पाटना है।
- कार्यक्रम का उद्देश्य समग्र राजमार्ग विकास के लिए संसाधनों का अनुकूल आवंटन प्राप्त करना है।
- कई हवाई अड्डों का उन्नयन, जिसमें नए टर्मिनलों का निर्माण शामिल है, 18 गैर-मेट्रो हवाई अड्डों में सुधार, हवाई नेविगेशन सेवाओं में सुधार के लिए भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (AAI) नए ATS स्वचालन प्रणाली को स्थापित कर रहा है।
- नागरिक उड्डयन क्षेत्र की व्यवहार्यता से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए, विशेष रूप से एयरलाइन उद्योग के लिए, 12 दिसंबर 2011 को नागरिक उड्डयन सचिव की अध्यक्षता में एक कार्य समूह का गठन किया गया था।
MARITIME AGENDA 2010 - 20
- समुद्री एजेंडा 2010-20 का उद्देश्य न केवल अधिक क्षमता बनाना है बल्कि प्रदर्शन के मामले में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय बंदरगाहों के समान बंदरगाह स्थापित करना है:
- (i) वर्ष 2020 के लिए 3,130 MT बंदरगाह क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- (ii) इस क्षमता का 50 प्रतिशत से अधिक गैर-मुख्य बंदरगाहों में निर्माण किया जाना है क्योंकि इन बंदरगाहों द्वारा संभाली जाने वाली यातायात 1,280 MT तक बढ़ने की उम्मीद है।
- (iii) इस विस्तारित संचालन पैमाने से लेन-देन की लागत में काफी कमी आने की उम्मीद है और भारतीय बंदरगाहों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की संभावना है।
- (iv) 2020 तक मुख्य और गैर-मुख्य बंदरगाहों में प्रस्तावित निवेश लगभग ₹2,96,000 करोड़ होने की उम्मीद है।
- (v) अधिकांश निवेश निजी क्षेत्र से आएगा जिसमें FDI (स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक बंदरगाहों के निर्माण और रखरखाव के लिए अनुमति है) शामिल है, और निजी क्षेत्र अधिकांश परियोजनाओं को PPP के माध्यम से या 'निर्माण संचालन हस्तांतरण' (BOT) या 'निर्माण संचालन स्वामित्व हस्तांतरण' (BOOT) के आधार पर वित्त पोषित करेगा।
- (vi) निजी क्षेत्र की भागीदारी न केवल बंदरगाहों की अवसंरचना में निवेश बढ़ाएगी, बल्कि नवीनतम तकनीक और बेहतर प्रबंधन प्रथाओं के माध्यम से बंदरगाहों के संचालन में सुधार की उम्मीद है।
- (vii) सार्वजनिक धन मुख्य रूप से सामान्य उपयोग अवसंरचना सुविधाओं जैसे कि बंदरगाह चैनलों की गहराई, बंदरगाहों से आंतरिक क्षेत्र तक रेलवे और सड़क संपर्क आदि के लिए तैनात किया जाएगा।
SMART CITIES
- गोल ने शहरी विकास के लिए राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के सहयोग से स्मार्ट सिटीज मिशन (SCM) की शुरुआत की है। इस मिशन का उद्देश्य है— स्थानीय क्षेत्र विकास को सक्षम बनाकर और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, विशेष रूप से ऐसी प्रौद्योगिकी जो स्मार्ट परिणाम देती है, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और लोगों की जीवन गुणवत्ता में सुधार करना।
- मिशन का लक्ष्य ऐसे शहरों को बढ़ावा देना है जो मुख्य आधारभूत संरचना प्रदान करते हैं और अपने नागरिकों को एक सम्मानजनक जीवन गुणवत्ता, एक स्वच्छ और सतत वातावरण और 'स्मार्ट' समाधान लागू करते हैं।
- इसका फोकस सतत और समावेशी विकास पर है और विचार यह है कि संकुचित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाए और एक ऐसा मॉडल बनाया जाए जो अन्य आकांक्षी शहरों के लिए एक प्रकाशस्तंभ की तरह कार्य करे।
PPP मॉडल
- इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए उचित मात्रा में फंड प्रबंधित करना हमेशा से भारत के लिए एक चुनौती रहा है। सुधार के युग में, सरकार ने निजी क्षेत्र (घरेलू और विदेशी दोनों) से निवेश आकर्षित करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) का विचार विकसित किया। इस संदर्भ में हमें निजी क्षेत्र से उत्साहजनक योगदान देखने को मिल रहा है।
- महत्वपूर्ण PPP मॉडलों का संक्षिप्त अवलोकन:
- (i) BOT-TOLL : 'बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर-टोल' PPP के प्रारंभिक मॉडलों में से एक था। परियोजना लागत (सरकार के साथ) साझा करने के अलावा, निजी बोलीदाता को सड़क का निर्माण, रखरखाव, संचालन करना और वाहन यातायात पर टोल वसूल करना था।
- BOT-Annuity : यह BOT-TOLL मॉडल का एक सुधार था, जिसका उद्देश्य सड़क परियोजनाओं के प्रति निजी कंपनियों की घटती रुचि को उलटना था, मुख्य रूप से निजी खिलाड़ियों के लिए जोखिम को कम करके।
- EPC मॉडल : यह PPP मॉडल जिसे इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए बेहतर रास्ता माना गया, 2010 तक स्पष्ट रूप से विफल हो गया और सरकार सड़क क्षेत्र में निजी खिलाड़ियों को आकर्षित करने में असमर्थ रही।
- HAM : हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM) EPC और BOT-ANNUITY मॉडलों का एक मिश्रण है। इस मॉडल में परियोजना लागत को सरकार और निजी खिलाड़ी के बीच 40:60 के अनुपात में साझा किया जाता है।
- स्विस चैलेंज मॉडल : भारत सरकार ने पहली बार रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए इस मॉडल का उपयोग करने की घोषणा की। यह अनुबंध देने का एक बहुत लचीला तरीका है (यानी, सार्वजनिक खरीद) जिसे PPP और गैर-PPP परियोजनाओं में उपयोग किया जा सकता है।
- अन्य क्षेत्रों के लिए PPP मॉडल : हालांकि, PPP मॉडल का विचार मूल रूप से इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के लिए विकसित किया गया था, हाल के समय में इसके उपयोग के लिए अन्य क्षेत्रों—जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और यहां तक कि कृषि में प्रस्ताव आए हैं।
- PPPP मॉडल : विशेषज्ञों ने देश के कुछ क्षेत्रों के लिए सार्वजनिक निजी जन भागीदारी (PPPP) मॉडल का सुझाव भी दिया है। हालांकि, ऐसा मॉडल 2000-01 से कृषि क्षेत्र में भागीदार जल विकास को बढ़ावा देने के लिए उपयोग में है—1974 के कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में (जिसे 2004 में कमांड एरिया डेवलपमेंट और वॉटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम का नाम दिया गया)—जिसमें व्यक्तिगत वित्तीय योगदान किसानों से आता है) खेत चैनलों और नालियों के विकास के लिए।
पेट्रोलियम क्षेत्र की चिंताएँ
- पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए, या कम से कम इसके बहिष्कार को संविधान संशोधन विधेयक में नहीं दर्शाना चाहिए।
- cess संग्रह का उपयोग गैस पाइपलाइनों के नेटवर्क के निर्माण के समर्थन के लिए किया जा सकता है, जो देश के परित्यक्त क्षेत्रों को स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- वर्तमान में प्रगति कुछ हद तक उर्वरक इकाइयों के पुनर्जीवन और गैस हाईवे परियोजनाओं के साथ स्थित छोटे उद्योगों के विकास से जुड़ी होने के कारण बाधित है।
- गैस पाइपलाइन नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए, वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) प्रदान की जा सकती है ताकि पाइपलाइन संपत्तियों के निर्माण और कुशल बाजारों के विकास को बढ़ावा दिया जा सके।
- देश भर में पाइपलाइनों के निर्माण के लिए केवल क्रॉस-कंट्री पाइपलाइनों का निर्माण नहीं बल्कि शहर गैस वितरण के लिए भी प्रोत्साहन की आवश्यकता है।
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) द्वारा वर्तमान में बिडिंग प्रणाली पक्षपाती और समय-खपत करने वाली है और इसे सुधारने की आवश्यकता है क्योंकि इसने गैस नेटवर्क के विकास को सीमित कर दिया है।
- PNG/CNG (संकुचित प्राकृतिक गैस) नेटवर्क का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में गैस कनेक्शन प्रदान करने में मदद कर सकता है।
- LPG सब्सिडी का रैशनलाइजेशन आवश्यक है। यह उपयोगी हो सकता है कि प्रत्येक घर के लिए 10 LPG सिलेंडरों की सब्सिडी को सीमित किया जाए (जो सामान्य घरेलू खाना पकाने के लिए अधिकतम उपयोग होता है) जबकि घरेलू और व्यावसायिक LPG उपयोगकर्ताओं पर कर और शुल्क को संरेखित किया जाए।
- शक्ति उद्योग में उपयोग के लिए तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) का आयात कस्टम ड्यूटी से मुक्त है जबकि अन्य सभी उपयोगों के लिए LNG पर 5 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी लगती है। किसी भी क्षेत्र के लिए कोई छूट नहीं होनी चाहिए।
- राष्ट्रीय गैस ग्रिड के लिए उत्पादन और उपभोग करने वाले राज्यों के बीच गैस का स्वैप करने के लिए एक लागत-कुशल और राजस्व-तटस्थ तंत्र विकसित करने के लिए, 1956 के केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत प्राकृतिक गैस की बिक्री के लिए विशेष कर प्रावधान बनाना महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक गैस और LNG को घोषित वस्तुएं माना जा सकता है ताकि कच्चे तेल के साथ कर समानता लाई जा सके और राज्यों में कीमतों को समान बनाया जा सके।
लॉजिस्टिक्स सेक्टर
लॉजिस्टिक्स- लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन का रीढ़ है (यह सामान के प्रवाह का प्रबंधन है, जो उत्पत्ति से लेकर उपभोग तक होता है)। इसमें परिवहन, इन्वेंट्री प्रबंधन, गोदाम, सामग्री हैंडलिंग, पैकेजिंग, और जानकारी का एकीकरण शामिल है। यह क्षेत्र मुख्यतः 'असंगठित' है और भारत में 'अनदेखा' रहा है।
- क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार ने व्यापार मंत्रालय में एक नया लॉजिस्टिक्स डिवीजन बनाया है।
- लंबी अवधि के लिए कम ब्याज दरों पर सस्ते फंड/क्रेडिट को सुगम किया जाएगा।
- बहु-आयामी लॉजिस्टिक्स (पार्क) सुविधाओं के निर्माण के लिए स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा, जिसमें संग्रहण और परिवहन दोनों शामिल हैं।
- नियामक प्राधिकरण के माध्यम से बाजार की जवाबदेही बढ़ाई जाएगी और यह ऋण और पेंशन फंड्स से निवेश को आकर्षित करेगा।
आवास नीति
- आवास आज सरकार की एक प्रमुख नीति प्राथमिकता है। बढ़ती हुई 'तरल' जनसंख्या के साथ, आवास नीति को क्षैतिज या स्थानिक गतिशीलता (यानी, शहरों के भीतर और बीच में आंदोलन) और ऊर्ध्वाधर गतिशीलता (सामाजिक-आर्थिक सीढ़ी चढ़ने के लिए) की अनुमति देनी चाहिए, जैसे-जैसे अवसर उत्पन्न होते हैं।
- आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 ने इस संदर्भ में कुछ कारकों को उजागर किया जब देश एक महत्वाकांक्षी योजना— Housing for All— के लिए जा रहा है।
- क्षेत्र से संबंधित दो बुनियादी मुद्दे हैं: किरायेदार आवास और खाली घर।
PMAY-U

- प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) का शुभारंभ जून 2015 में किया गया था। इसका उद्देश्य 2022 तक सभी पात्र शहरी गरीबों को 70 पक्के मकान प्रदान करना है। यह 'Housing for All' (प्रधान मंत्री आवास योजना) का एक हिस्सा है।
- 2020 की शुरुआत तक, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा मान्य 1.12 करोड़ मकानों की मांग दर्ज की गई थी। यह दुनिया की सबसे बड़ी आवास योजनाओं में से एक है, जो पूरे शहरी भारत को कवर करती है।
- शहरी आवास और शहर आर्थिक विकास के केन्द्र हैं, जो भारत के 60 प्रतिशत GDP में योगदान करते हैं।
- निर्माण क्षेत्र GDP का 8.2 प्रतिशत है और यह लगभग 12 प्रतिशत कार्यबल को रोजगार देता है।
- इसलिए, PMAY-(U) के तहत किए गए निवेश केवल पात्र परिवारों को 'Housing for All' का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पक्के मकान प्रदान नहीं करते हैं, बल्कि यह समग्र अर्थव्यवस्था पर गुणक प्रभाव भी उत्पन्न करते हैं।
- यह योजना निम्नलिखित चार आयामों के माध्यम से लागू की जा रही है:
- (i) इन सिचुए स्लम डेवलपमेंट (ISSR)
- (ii) क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS)
- (iii) अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (AHP)
- (iv) लाभार्थी द्वारा मकान निर्माण/सुधार (BLC)
राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन
- सरकार ने 2024-25 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का GDP लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, भारत को 2020-25 के दौरान अवसंरचना में लगभग 1.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (₹100 लाख करोड़) का निवेश करना होगा।
- 2030 तक विकास को बनाए रखने के लिए, एक और 4.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश आवश्यक है।
- सरकार ने इस क्षेत्र में निवेश के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) परियोजना शुरू की (31 दिसंबर 2019 को)।
- NIP देश के अवसंरचना दृष्टिकोण को 2020-25 की अवधि के लिए संक्षेपित करता है। यह देश में किया गया पहला ऐसा प्रयास है।
|
289 docs|166 tests
|















