UPSC Daily Current Affairs (Hindi)- 28th February 2025 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly PDF Download
जीएस2/राजनीति
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जज के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत पर लोकपाल के आदेश पर रोक लगाई
 चर्चा में क्यों?
चर्चा में क्यों?
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐसे आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें एक अनाम हाई कोर्ट (HC) जज के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत का संज्ञान लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज एएम खानविलकर की अगुआई वाली लोकपाल बेंच ने लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत ऐसे मामलों की सुनवाई करने का अपना अधिकार होने का दावा किया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस स्थिति को चिंताजनक पाया और कार्यवाही रोक दी है, जिसकी अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी।
- सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया है।
- न्यायिक मामलों में लोकपाल की भागीदारी से संभावित कार्यपालिका के अतिक्रमण के संबंध में चिंताएं व्यक्त की गई हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों की जांच के लिए स्थापित प्रक्रियाओं के महत्व को दर्शाता है।
अतिरिक्त विवरण
- न्यायिक स्वतंत्रता: सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक रूप से न्यायाधीशों की आलोचना को न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा की आवश्यकता के साथ संतुलित किया है।
- कार्यपालिका के अतिक्रमण पर चिंताएं: चूंकि लोकपाल एक कार्यकारी वैधानिक निकाय है, इसलिए न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों की सुनवाई करने की इसकी क्षमता न्यायिक स्वायत्तता को कमजोर कर सकती है।
- कानूनी प्रावधान: भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत, न्यायाधीशों पर आधिकारिक कर्तव्यों के दौरान किए गए कार्यों के लिए आरोप नहीं लगाया जा सकता है।
- के. वीरास्वामी बनाम भारत संघ (1991) के ऐतिहासिक मामले ने स्थापित किया कि न्यायाधीश, लोक सेवक होने के नाते, भ्रष्टाचार के लिए जांचे जा सकते हैं, लेकिन ऐसी कार्यवाही के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह के आधार पर राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता होती है।
- न्यायाधीशों के विरुद्ध मामला दायर करने की प्रक्रिया और महाभियोग प्रक्रिया में स्पष्ट अंतर है, क्योंकि महाभियोग प्रक्रिया के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध आरोप: एक निजी कंपनी से संबंधित न्यायिक कार्यवाही को कथित रूप से प्रभावित करने के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध दो शिकायतें दर्ज की गईं, जो पहले न्यायाधीश की मुवक्किल थी।
- लोकपाल के फैसले में मामले के गुण-दोष पर ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर उसके अधिकार क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- लोकपाल अधिनियम लोक सेवकों पर लागू होता है, लेकिन इसमें न्यायाधीशों को स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है, जिससे इसके अधिकार क्षेत्र के संबंध में अस्पष्टता पैदा होती है।
- अधिकार क्षेत्र का दावा करने के बावजूद, लोकपाल ने आगे बढ़ने से पहले मार्गदर्शन के लिए मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया है।
सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से संभावित कार्यकारी अतिक्रमण और न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा की आवश्यकता के बारे में महत्वपूर्ण चिंताएँ उजागर होती हैं। यह मामला न्यायपालिका पर लोकपाल के अधिकार के बारे में चल रही कानूनी अस्पष्टताओं पर और अधिक जोर देता है। सर्वोच्च न्यायालय के आगामी फैसले का भारत में उच्च न्यायपालिका अधिकारियों पर लागू जवाबदेही तंत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।
जीएस3/पर्यावरण
एक नई मेंढक प्रजाति की खोज: मिनर्वरिया घाटीबोरियलिस
चर्चा में क्यों?
पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र के शोधकर्ताओं ने मिनर्वरिया घाटीबोरियलिस नामक मेंढक की एक नई स्थानिक प्रजाति की पहचान की है , जो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला की जैव विविधता पर प्रकाश डालती है।
- इस मेंढक की खोज महाराष्ट्र में सह्याद्री पर्वतमाला के उत्तर-पश्चिमी घाट में स्थित महाबलेश्वर में की गई थी।
- इसका नाम संस्कृत शब्द 'घाटी' , जिसका अर्थ पश्चिमी है, और लैटिन शब्द 'बोरेलिस' , जिसका अर्थ उत्तरी क्षेत्र है, से मिलकर बना है।
- यह प्रजाति मिनर्वरिया वंश का हिस्सा है , जिसे आमतौर पर क्रिकेट मेंढक कहा जाता है ।
अतिरिक्त विवरण
- विशिष्ट विशेषताएं: मिनर्वरिया वंश से संबंधित मेंढकों को उनके पेट पर मौजूद समानांतर रेखाओं से पहचाना जा सकता है।
- घोंसला बनाने की आदतें: वे आमतौर पर स्थिर पानी या छोटे झरनों के पास घोंसला बनाते हैं और बुलबुल जैसी आवाजें निकालते हैं।
- नर मिनर्वरिया घाटीबोरियलिस की प्रजनन ध्वनियाँ उसी वंश की अन्य प्रजातियों से उल्लेखनीय रूप से भिन्न होती हैं।
यह खोज इस क्षेत्र में उभयचर विविधता के बारे में हमारी समझ को समृद्ध करती है तथा ऐसी अनोखी प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने के महत्व को रेखांकित करती है।
जीएस1/इतिहास और संस्कृति
चंद्रशेखर आज़ाद और उनका योगदान
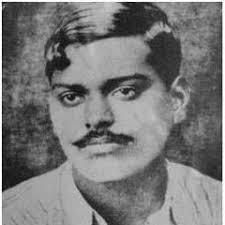 चर्चा में क्यों?
चर्चा में क्यों?
विभिन्न राजनीतिक पृष्ठभूमि के नेताओं ने 27 फरवरी, 1931 को स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद के शहादत दिवस को याद किया।
- चन्द्रशेखर आज़ाद (1906-1931) भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे।
- मध्य प्रदेश के भाभरा में जन्मे वे 15 वर्ष की आयु में गांधीजी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे।
- बाद में असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के बाद वे सशस्त्र क्रांति की ओर मुड़ गये।
- आज़ाद ने भगत सिंह के साथ मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) में पुनर्गठित किया।
- उन्होंने कभी भी जीवित न पकड़े जाने की कसम खाई और अंततः पुलिस के साथ मुठभेड़ में उन्होंने अपनी जान दे दी।
अतिरिक्त विवरण
- असहयोग आंदोलन (1921): आज़ाद को 15 साल की उम्र में गिरफ्तार कर लिया गया और उन्होंने अदालत में अपना नाम "आज़ाद" घोषित किया, जिसके लिए उन्हें सजा के तौर पर 15 कोड़े मारे गए।
- एच.आर.ए. में शामिल होना (1924): वे राम प्रसाद बिस्मिल की एच.आर.ए. के सदस्य बन गए और राजनीतिक गतिविधियों के माध्यम से धन जुटाने में शामिल हो गए।
- काकोरी ट्रेन डकैती (1925): आज़ाद ने खजाने की धनराशि ले जा रही एक ब्रिटिश ट्रेन को लूटने में भूमिका निभाई और भागने में सफल रहे, जबकि अन्य गिरफ्तार कर लिए गए।
- एचएसआरए का पुनर्गठन (1928): उन्होंने एचआरए को एचएसआरए में परिवर्तित कर दिया, संगठन के भीतर समाजवादी विचारधारा पर जोर दिया।
- जॉन सॉन्डर्स की हत्या (1928): लाला लाजपत राय की मौत के जवाब में, आज़ाद ने व्यक्तिगत रूप से प्रतिशोध में एक पुलिस अधिकारी को मार डाला।
- लॉर्ड इरविन की ट्रेन को उड़ाने का प्रयास (1929): आज़ाद ने वायसराय लॉर्ड इरविन की हत्या की योजना बनाई, जो अंततः विफल हो गई।
- फाइनल स्टैंड (1931): एक पुलिस घात के दौरान, आज़ाद ने तीन अधिकारियों को मार डाला, अपने साथी के भागने को सुनिश्चित किया, और अपनी आखिरी गोली से खुद की जान ले ली।
चन्द्रशेखर आज़ाद भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहादुरी और प्रतिबद्धता के प्रतीक हैं तथा अपने समर्पण और बलिदान से भावी पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे।
जीएस3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी
ब्लड मून
 चर्चा में क्यों?
चर्चा में क्यों?
पूर्ण चंद्रग्रहण, जिसे सामान्यतः रक्त चंद्र कहा जाता है, 14 मार्च को आकाश को प्रकाशित करेगा। यह खगोलीय घटना विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में देखी जा सकेगी, हालांकि भारत जैसे कुछ स्थानों पर दिन में होने के कारण यह दिखाई नहीं देगा।
- रक्तिम चन्द्रमा पूर्ण चंद्रग्रहण के दौरान घटित होता है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के ठीक बीच में आ जाती है।
- यह घटना रेले प्रकीर्णन के कारण होती है , जिसके परिणामस्वरूप चंद्रमा का रंग लाल दिखाई देता है।
- पिछला पूर्ण चंद्रग्रहण लगभग तीन वर्ष पहले, 2022 में हुआ था।
अतिरिक्त विवरण
- यह कैसे घटित होता है: रक्तिम चंद्रमा तब घटित होता है जब पृथ्वी अपनी छाया चंद्रमा पर डालती है, जिससे छोटी तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश (नीला) के प्रकीर्णन तथा पृथ्वी के वायुमंडल से लंबी तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश (लाल) के गुजरने के कारण चंद्रमा लाल या नारंगी दिखाई देता है।
- दृश्यमान स्थान: यह रक्त चंद्रमा अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी अफ्रीका और उत्तरी व दक्षिणी अटलांटिक महासागर में दिखाई देगा, लेकिन दिन के उजाले के कारण भारत में नहीं दिखाई देगा।
- पूर्णता के दौरान, पूरा चंद्रमा पृथ्वी की सबसे अंधेरी छाया, जिसे अम्ब्रा के नाम से जाना जाता है, से ढक जाता है , जो उसके लाल-नारंगी रंग को और निखार देता है।
यह आगामी पूर्ण चंद्रग्रहण एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है जो दुनिया भर के आकाशदर्शकों की रुचि को आकर्षित करती है। पर्यवेक्षकों को इस शानदार घटना को देखने के लिए स्थानीय समय और स्थितियों की जांच करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
जीएस2/शासन
भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई)
चर्चा में क्यों?
केंद्र सरकार भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई) के दिशानिर्देशों में सुधार कर रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे समसामयिक मुद्दों के लिए अधिक प्रासंगिक हों तथा पशु क्रूरता को रोकने के लिए उनके प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ाया जा सके।
- एडब्ल्यूबीआई एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 1962 में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत की गई थी।
- इसकी शुरुआत प्रख्यात मानवतावादी स्वर्गीय श्रीमती रुक्मिणी देवी अरुंडेल के नेतृत्व में की गई थी।
- बोर्ड का प्राथमिक दायित्व पशु कल्याण को बढ़ावा देना और पशुओं को अनावश्यक दर्द और पीड़ा से बचाना है।
- इसका मुख्यालय बल्लभगढ़, हरियाणा में स्थित है।
अतिरिक्त विवरण
- सलाहकार भूमिका: AWBI राज्य और केंद्र दोनों सरकारों को पशु कल्याण के मुद्दों पर सलाह देती है, जिसमें पशुओं के प्रति क्रूरता से निपटना भी शामिल है।
- बोर्ड शिकायतों के संबंध में राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ नियमित रूप से संवाद करता है और उनसे अपराधियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह करता है।
- राज्य प्राधिकरण: इन प्राधिकरणों को कानून के अनुसार पशुओं के प्रति क्रूरता के विरुद्ध कार्रवाई शुरू करने का अधिकार है।
- एडब्ल्यूबीआई पशुओं के प्रति मानवीय व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय पशु कल्याण संगठनों को वित्तीय और अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करता है।
- सदस्यता: बोर्ड में 28 सदस्य होते हैं, जिनका कार्यकाल तीन साल का होता है। इसमें विभिन्न सरकारी संगठनों, पशु अधिकार कार्यकर्ताओं और सांसदों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।
पशु अधिकारों का सम्मान और संरक्षण करने वाले समाज को बढ़ावा देने में AWBI के प्रयास महत्वपूर्ण हैं, जो भारत में पशु कल्याण मुद्दों के प्रति बढ़ती जागरूकता को दर्शाता है।
जीएस3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी
चंद्र ट्रेलब्लेज़र अंतरिक्ष यान
 चर्चा में क्यों?
चर्चा में क्यों?
हाल ही में, स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट ने केप कैनावेरल के कैनेडी स्पेस सेंटर से नासा के लूनर ट्रेलब्लेज़र ऑर्बिटर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह मिशन महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर पानी के बारे में हमारी समझ को बढ़ाना है।
- लूनर ट्रेलब्लेज़र नासा की एक पहल है जिसे चंद्रमा पर पानी का पता लगाने और उसका मानचित्र बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- इसका आकार लगभग डिशवॉशर जितना है तथा सौर पैनल लगे होने के कारण इसका वजन लगभग 200 किलोग्राम है।
- यह अंतरिक्ष यान कई महीनों तक चन्द्रमा के कई चक्कर लगाएगा तथा परिक्रमा करेगा।
- अंततः यह लगभग 100 किमी की ऊंचाई पर चंद्रमा की परिक्रमा करेगा।
अतिरिक्त विवरण
- मिशन का उद्देश्य: अंतरिक्ष यान का उद्देश्य विशिष्ट चंद्र क्षेत्रों के उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाले चित्र एकत्र करना है, ताकि पानी के स्वरूप, वितरण और प्रचुरता का विश्लेषण किया जा सके, जिससे चंद्र जल चक्र की समझ में सुधार हो सके।
- जहाज पर उपकरण:
- उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाष्पशील और खनिज चंद्रमा मैपर (एचवीएम 3): यह उपकरण चंद्रमा की सतह पर पानी द्वारा उत्सर्जित प्रकाश पैटर्न का पता लगाएगा।
- लूनर थर्मल मैपर (एलटीएम): इसका कार्य चंद्र सतह का मानचित्रण और तापमान मापना है।
- दोनों उपकरण मिलकर चंद्रमा की सतह पर पानी के विभिन्न रूपों, खनिज संरचना और तापमान की पहचान करेंगे।
- लूनर ट्रेलब्लेज़र अंतरिक्ष यान लॉकहीड मार्टिन के अंतरिक्ष प्रभाग द्वारा विकसित किया गया था।
यह मिशन चंद्र अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा पर पानी के रहस्यों को उजागर करना तथा भविष्य के चंद्र मिशनों पर इसके प्रभाव को जानना है।
जीएस3/अर्थव्यवस्था
भारत के प्रमुख बंदरगाहों के परिचालन को मानकीकृत और सुव्यवस्थित करने के लिए पहल शुरू की गई
 चर्चा में क्यों?
चर्चा में क्यों?
केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के समुद्री बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) के तहत महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। यह पहल बंदरगाह संचालन में स्थिरता को बढ़ावा देते हुए वैश्विक व्यापार में भारत की उपस्थिति बढ़ाने के लिए बनाई गई है।
- बंदरगाह परिचालन को मानकीकृत करने के लिए एक राष्ट्र-एक बंदरगाह प्रक्रिया (ओएनओपी) की शुरूआत।
- बंदरगाह प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए सागर अंकलन - लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉरमेंस इंडेक्स (एलपीपीआई) का शुभारंभ।
- समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत ग्लोबल पोर्ट्स कंसोर्टियम का गठन।
- व्यापार में डिजिटल परिवर्तन के लिए मैत्री पहल का कार्यान्वयन।
- स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए हरित बंदरगाह और शिपिंग में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (एनसीओईजीपीएस) की स्थापना।
- समुद्री विकास को प्रदर्शित करने के लिए भारत समुद्री सप्ताह 2025 की घोषणा।
अतिरिक्त विवरण
- एक राष्ट्र-एक बंदरगाह प्रक्रिया (ONOP): इस पहल का उद्देश्य बंदरगाह दस्तावेज़ीकरण में विसंगतियों को खत्म करना है, जिससे अक्षमताएं और परिचालन लागत कम हो। मंत्रालय ने कंटेनर संचालन दस्तावेजों में 33% और बल्क कार्गो दस्तावेजों में 29% की कमी हासिल की है।
- सागर अंकलन - लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉरमेंस इंडेक्स (एलपीपीआई): यह सूचकांक कार्गो हैंडलिंग और टर्नअराउंड समय जैसे आवश्यक मेट्रिक्स का मूल्यांकन करता है, तथा बंदरगाह संचालन में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देता है।
- भारत ग्लोबल पोर्ट्स कंसोर्टियम: इसका उद्देश्य विभिन्न परिचालनों को एकीकृत करके लॉजिस्टिक्स और व्यापार संपर्क को बढ़ाना है, तथा यह 'मेक इन इंडिया' जैसी पहलों का समर्थन करता है।
- मैत्री: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विनियामक इंटरफेस के लिए मास्टर एप्लीकेशन का ध्यान एआई और ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकियों के माध्यम से व्यापार प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और परिचालन दक्षता को सुविधाजनक बनाने पर केंद्रित है।
- राष्ट्रीय हरित बंदरगाह एवं नौवहन उत्कृष्टता केंद्र (एनसीओईजीपीएस): यह केंद्र समुद्री परिचालन में टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देता है, तथा कार्बन उत्सर्जन को कम करने और स्वच्छ ईंधन को अपनाने पर ध्यान केंद्रित करता है।
केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत की नीली अर्थव्यवस्था रोजगार सृजन, व्यापार विस्तार और आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार 2030 तक भारत को शीर्ष 10 जहाज निर्माण राष्ट्र बनाने और वैश्विक समुद्री शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए विश्व स्तरीय समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
जीएस2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध
भारत-यूरोपीय संघ साझेदारी क्यों महत्वपूर्ण है?
 चर्चा में क्यों?
चर्चा में क्यों?
यूरोपीय आयोग का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल, जिसमें 27 यूरोपीय आयुक्तों में से 22 शामिल हैं और जिसका नेतृत्व राष्ट्रपति उर्सुला वॉन डेर लेयेन कर रही हैं, दो दिवसीय कार्यक्रम के लिए नई दिल्ली का दौरा कर रहा है। यह अभूतपूर्व यात्रा व्यापार, प्रौद्योगिकी, हरित ऊर्जा और रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच मजबूत होते संबंधों को उजागर करती है। भारत-ईयू व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (टीटीसी) की बैठकों के साथ होने वाली इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग और निवेश के अवसरों को बढ़ाना है।
- यह यात्रा भारत-यूरोपीय संघ संबंधों में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में व्यापार, प्रौद्योगिकी, हरित ऊर्जा और रक्षा शामिल हैं।
- 15 वर्ष के अंतराल के बाद मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए बातचीत फिर से शुरू हो गई है।
अतिरिक्त विवरण
- ऐतिहासिक संदर्भ: भारत ने 1962 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ईईसी) के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। मील के पत्थर निम्नलिखित हैं:
- 1993: संयुक्त राजनीतिक वक्तव्य पर हस्ताक्षर।
- 1994: सहयोग समझौते की स्थापना।
- 2000: लिस्बन में प्रथम भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन।
- 2004: सामरिक साझेदारी में उन्नयन।
- 2020: 2025 तक भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी रोडमैप को अपनाना।
- व्यापार और निवेश: यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिसका द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2023-24 में 135 बिलियन डॉलर तक पहुँच जाएगा। FTA का उद्देश्य टैरिफ कम करके और निवेश को बढ़ावा देकर व्यापार संबंधों को बढ़ाना है।
- प्रौद्योगिकी और डिजिटल सहयोग: सहयोग में उभरती प्रौद्योगिकियां, अर्धचालक अनुसंधान एवं विकास, तथा उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग पहल शामिल हैं।
- हरित ऊर्जा सहयोग: हरित हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा में पहल का उद्देश्य 2070 तक भारत के शुद्ध-शून्य लक्ष्यों का समर्थन करना है।
- रक्षा एवं अंतरिक्ष सहयोग: संयुक्त नौसैनिक अभ्यास और अंतरिक्ष मिशन में सहयोग रणनीतिक साझेदारी को उजागर करते हैं।
- लोगों के बीच संबंध: यूरोपीय संघ में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासियों की उपस्थिति से सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान-प्रदान बढ़ता है, जिससे हजारों लोग इरास्मस छात्रवृत्ति से लाभान्वित होते हैं।
यूरोपीय आयोग के आयुक्तों के कॉलेज की यह यात्रा भारत-यूरोपीय संघ संबंधों में एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतीक है। व्यापार, प्रौद्योगिकी, हरित ऊर्जा और रक्षा में सहयोग को तीव्र करके, दोनों पक्षों का लक्ष्य एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी बनाना है। सेमीकंडक्टर और हाइड्रोजन ऊर्जा में चल रही एफटीए वार्ता और सहयोगी परियोजनाएं द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, आपसी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और वैश्विक नेतृत्व स्थापित करने के लिए तैयार हैं। जैसे-जैसे भू-राजनीतिक गतिशीलता विकसित होती है, भारत और यूरोपीय संघ एक साथ एक लचीला, टिकाऊ और सुरक्षित भविष्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
जीएस2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध
हेग सेवा सम्मेलन
चर्चा में क्यों?
अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग ने हाल ही में भारत के केंद्रीय विधि मंत्रालय, जो हेग सेवा संधि के तहत केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है, से गौतम अडानी और उनके सहयोगियों पर सम्मन जारी करने के लिए सहायता मांगी है।
- हेग सेवा कन्वेंशन को 1965 में अपनाया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विदेशी न्यायक्षेत्रों में प्रतिवादियों को कानूनी कार्यवाही की सूचना समय पर मिले।
- भारत और अमेरिका इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले 84 देशों में शामिल हैं, जो सेवा अनुरोधों के प्रसंस्करण के लिए केंद्रीय प्राधिकारियों की नियुक्ति को अनिवार्य बनाता है।
अतिरिक्त विवरण
- हेग सेवा कन्वेंशन का उद्देश्य: यह बहुपक्षीय संधि यह सुनिश्चित करती है कि प्रतिवादियों को उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के बारे में समय पर सूचित किया जाए, जिससे सेवा का प्रमाण प्रस्तुत करने में सुविधा हो।
- सेवा के तरीके: प्राथमिक तरीका निर्दिष्ट केंद्रीय प्राधिकारियों के माध्यम से है, लेकिन अन्य तरीकों में डाक सेवा, राजनयिक चैनल और न्यायिक अधिकारियों के बीच सीधा संचार शामिल हैं।
- भारत में सेवा: भारत ने अनुच्छेद 10 के अंतर्गत वैकल्पिक सेवा पद्धतियों के विरुद्ध आरक्षण के साथ 23 नवम्बर, 2006 को कन्वेंशन को स्वीकार किया।
- सभी सेवा अनुरोध अंग्रेजी में होने चाहिए या उनके साथ अंग्रेजी अनुवाद होना चाहिए, तथा उनका निष्पादन केवल भारत के विधि एवं न्याय मंत्रालय के माध्यम से ही किया जा सकता है।
- मंत्रालय अनुरोधों को अस्वीकार कर सकता है, लेकिन उसे अस्वीकृति के लिए कारण बताना होगा, तथा यह सुनिश्चित करना होगा कि संप्रभुता और सुरक्षा का सम्मान किया जाए।
- एक बार जब केंद्रीय प्राधिकारी अनुरोध पर कार्रवाई कर देता है, तो इस सेवा को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत भारतीय न्यायालय द्वारा जारी समन माना जाता है।
इस प्रक्रिया में आम तौर पर छह से आठ महीने लगते हैं, और अगर कोई विदेशी सरकार समन की तामील में सहयोग करने में विफल रहती है, तो डिफ़ॉल्ट निर्णय जारी किया जा सकता है, बशर्ते अनुच्छेद 15 के तहत विशिष्ट शर्तें पूरी हों। उल्लेखनीय है कि भारत इन परिस्थितियों में अपने न्यायालयों को सीमा पार विवादों में डिफ़ॉल्ट निर्णय जारी करने की अनुमति देता है।
जीएस3/पर्यावरण
इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य (IWL)
चर्चा में क्यों?
हाल ही में, इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य में आयोजित तीन दिवसीय ऑफ-सीजन जीव सर्वेक्षण में 14 पक्षी प्रजातियों, 15 तितली प्रजातियों और 8 ओडोनेट्स प्रजातियों की खोज की गई, जो पहले अभयारण्य में दर्ज नहीं की गई थीं।
- IWL की स्थापना 1976 में हुई थी और यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है।
- यह अभयारण्य इडुक्की आर्क बांध के आसपास 77 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है।
- इसकी ऊंचाई 450 से 1272 मीटर तक है, जिसमें वंजुर मेदु सबसे ऊंची चोटी है।
- प्रमुख नदियों में पेरियार और चेरुथोनियार शामिल हैं।
- यहाँ औसतन 3800 मिमी वर्षा होती है।
अतिरिक्त विवरण
- वनस्पति: प्रमुख प्रकारों में पश्चिमी तट उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, अर्ध सदाबहार वन, नम पर्णपाती वन, पहाड़ी तट और घास के मैदान शामिल हैं।
- वनस्पति: वनों में विविध प्रजातियाँ पाई जाती हैं जैसे सागौन, शीशम, कटहल, आबनूस, दालचीनी और विभिन्न बांस प्रजातियाँ।
- जीव-जंतु: अभयारण्य में हाथी, बाइसन, सांभर हिरण, जंगली कुत्ते, बाघ, जंगली सूअर और कोबरा तथा करैत जैसी विभिन्न सांप प्रजातियों सहित कई वन्यजीव रहते हैं।
- पक्षी प्रजातियाँ: उल्लेखनीय पक्षियों में जंगली मुर्गी, मैना, लाफिंग थ्रश, काली बुलबुल, मोर, कठफोड़वा और किंगफिशर शामिल हैं।
- इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य में लुप्तप्राय नीलगिरि तहर मछली भी पाई जाती है।
इस हालिया सर्वेक्षण में इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक महत्व तथा इसके विविध वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा के लिए सतत संरक्षण प्रयासों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।
जीएस2/राजनीति
गणना के मामले: परिसीमन, संघवाद और जनगणना पर
चर्चा में क्यों?
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने परिसीमन प्रक्रिया पर चर्चा के लिए 5 मार्च को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसका उद्देश्य इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर राष्ट्रीय संवाद शुरू करना है।
- तमिलनाडु कम जनसंख्या वृद्धि के कारण लोकसभा सीटों के संभावित नुकसान से चिंतित है।
- ऐसी आशंका है कि तमिलनाडु में प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण उपायों के कारण राजनीतिक प्रतिनिधित्व में कमी आ सकती है।
अतिरिक्त विवरण
- संसदीय प्रतिनिधित्व में कमी: तमिलनाडु को डर है कि उसकी लोकसभा सीटें घट सकती हैं क्योंकि उत्तरी राज्यों की तुलना में उसकी जनसंख्या वृद्धि दर कम है। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु के मतदाताओं की संख्या में 171% (1971-2024) की वृद्धि हुई जबकि अविभाजित बिहार में 233% की वृद्धि हुई, जिससे तमिलनाडु का राजनीतिक प्रभाव कम हो सकता है।
- जनसंख्या नियंत्रण सफलता के लिए दंड: राज्य का मानना है कि उसके सफल जनसंख्या नियंत्रण उपायों को दंडित किया जाएगा, क्योंकि उच्च प्रजनन दर वाले राज्य, जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार, सीटें हासिल कर सकते हैं, जबकि तमिलनाडु और केरल बेहतर स्वास्थ्य और विकास संकेतकों के बावजूद प्रतिनिधित्व खो सकते हैं।
- परिसीमन के संभावित प्रभाव:
- राजनीतिक शक्ति गतिशीलता में बदलाव: अधिक जनसंख्या वाले राज्यों से प्रतिनिधित्व में वृद्धि से दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों से राजनीतिक प्रभाव स्थानांतरित हो सकता है।
- संघीय असंतुलन और क्षेत्रीय असमानता: केरल जैसे राज्य, जिनकी जनसंख्या नीतियां प्रभावी हैं, राष्ट्रीय विकास में उनके योगदान के बावजूद उनका प्रतिनिधित्व कम हो सकता है।
- संसाधन आवंटन असमानताएं: उत्तरी राज्यों के लिए अधिक सीटें केंद्रीय बजट आवंटन पर प्रभाव बढ़ा सकती हैं, जिससे कम प्रतिनिधियों वाले राज्यों को संभावित रूप से नुकसान हो सकता है।
- राजनीतिक तनाव और क्षेत्रीय असंतोष: उत्तरी राज्यों के प्रति कथित पक्षपात से क्षेत्रीय तनाव बढ़ सकता है, जिससे राजनीतिक आंदोलन और नीति पुनर्मूल्यांकन की मांग बढ़ सकती है।
- परिसीमन स्थगन के कारण:
- विभिन्न जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों के बीच निष्पक्षता सुनिश्चित करना तथा जनसंख्या नियंत्रण नीतियों को सफलतापूर्वक लागू करने वाले राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की रक्षा करना।
- संघीय शासन में शक्ति संतुलन बनाए रखना, कुछ क्षेत्रों के अति-प्रतिनिधित्व को रोकना तथा राष्ट्रीय निर्णय-निर्माण में भौगोलिक संतुलन को बनाए रखना।
- केंद्र सरकार के कदम:
- परिसीमन पर रोक का विस्तार: सरकार ने 42वें संशोधन (1976) के माध्यम से जनसंख्या के आधार पर संसदीय सीट आवंटन पर रोक को 2001 तक बढ़ा दिया, और बाद में 84वें संशोधन (2001) के माध्यम से इसे 2026 तक बढ़ा दिया।
- समान संसाधन आवंटन: 15वें वित्त आयोग (2021-26) ने एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया जिसमें संसाधनों का उचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए जनसंख्या (2011 की जनगणना) और जनसांख्यिकीय प्रदर्शन दोनों को शामिल किया गया।
- परामर्श प्रक्रियाएं: केंद्र सरकार ने निष्पक्ष प्रतिनिधित्व और संसाधन वितरण से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए अंतर-राज्यीय परिषद की बैठकों और वित्त आयोग के परामर्श के माध्यम से दक्षिणी राज्यों के साथ संपर्क स्थापित किया है।
संक्षेप में, परिसीमन की प्रक्रिया तमिलनाडु और अन्य दक्षिणी राज्यों के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करती है, क्योंकि इससे राजनीतिक शक्ति का पुनर्वितरण हो सकता है जो राष्ट्रीय विकास में उनके योगदान को कमजोर कर सकता है। इन चिंताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए निरंतर संवाद और न्यायसंगत दृष्टिकोण आवश्यक हैं।
|
3134 docs|1045 tests
|
FAQs on UPSC Daily Current Affairs (Hindi)- 28th February 2025 - Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly
| 1. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जज के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत पर रोक क्यों लगाई है? |  |
| 2. मिनर्वरिया घाटीबोरियलिस नामक नई मेंढक प्रजाति के बारे में क्या जानकारी है? |  |
| 3. चंद्रशेखर आज़ाद का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान था? |  |
| 4. ब्लड मून क्या है और इसका वैज्ञानिक महत्व क्या है? |  |
| 5. भारत-यूरोपीय संघ साझेदारी क्यों महत्वपूर्ण है? |  |
















