वनस्पति - भूगोल | यूपीएससी सीएसई के लिए भूगोल (Geography) - UPSC PDF Download
उष्णकटिबंधीय सदाबहार या वर्षावन इन वनों में पेड़ पत्तियों को गिराने का कोई विशेष मौसम नहीं रखते हैं, इसीलिए ये सदाबहार होते हैं। ये ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक औसत तापमान लगभग 25°C से 27°C होता है और वर्षा 200 सेमी से अधिक होती है। ये वर्षा के झुकाव वाले ढलानों पर उगते हैं जो मानसून धाराओं का सामना करते हैं। ये क्षेत्र पश्चिमी घाट के पश्चिमी हिस्सों (महाराष्ट्र, कर्नाटका और केरल के भाग); पूर्वी हिमालय (तराई क्षेत्र); उत्तर-पूर्व भारत (जिसमें लुशाई, गारो, खासी, जयंतिया और अन्य पहाड़ शामिल हैं); और अंडमान द्वीप समूह के अधिकांश हिस्सों में होते हैं।
वर्षावन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन घने वृक्षों के साथ होते हैं जिनमें चढ़ने वाले पौधे और एपिफाइट्स, बांस और फ़र्न शामिल होते हैं। पेड़ की ऊँचाई 45 मीटर तक होती है। ये मूल्यवान कठोर लकड़ी जैसे कि गुलाब का लकड़ी, काला लकड़ी और आयरनवुड का उत्पादन करते हैं, जिसका उपयोग फर्नीचर, रेलवे की पटरी और घर बनाने में किया जाता है।
उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन इन्हें मानसून वनों के रूप में भी जाना जाता है, ये भारत के लगभग सभी हिस्सों में प्राकृतिक आवरण बनाते हैं। ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 150 सेमी से 200 सेमी के बीच होती है। अधिकांश पेड़ पतझड़ी होते हैं, अर्थात् ये गर्म मौसम में लगभग 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियाँ गिराते हैं। प्रजातियों के अनुसार, पत्तियों का गिरने का समय आमतौर पर मार्च के प्रारंभ से अप्रैल के अंत तक होता है और इसलिये किसी विशेष समय पर ये वन बिल्कुल खाली नहीं होते।
इन वनों के दो प्रकार होते हैं: (i) गीले पतझड़ी (ii) सूखे पतझड़ी यह देखा गया है कि अधिकांश पतझड़ी वन धीरे-धीरे सूखे पतझड़ी वनों द्वारा प्रतिस्थापित हो रहे हैं। गीले पतझड़ी वन पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों पर होते हैं, (इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रजाति सागवान है) और ये प्रायद्वीप के उत्तर-पूर्वी हिस्से, यानी छोटानागपुर पठार के चारों ओर, पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिण बिहार और पश्चिम ओडिशा में सामान्य होते हैं। ये उत्तर में शिवालिक पहाड़ों के साथ भी सामान्य होते हैं, जिसमें भाभर और तराई शामिल हैं। शेष क्षेत्र जिसमें 100-150 सेमी वर्षा होती है, पहले बताए गए मानकों के भीतर सूखे पतझड़ी वनों का है। सूखे पतझड़ी वन अधिक खुले और बौने होते हैं, पेड़ अधिक बौने और फैले हुए होते हैं, हालांकि प्रजातियाँ ज्यादातर गीले पतझड़ी वनों के समान होती हैं।
पर्णपाती वन
पर्णपाती वन आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वन हैं क्योंकि इनमें कई प्रकार के वाणिज्यिक महत्व के लकड़ी के पेड़ पाए जाते हैं, जो उच्च स्तर की समूहिकता के कारण भी आसानी से उपयोग किए जा सकते हैं। इन वनों के महत्वपूर्ण पेड़ हैं:
- साल: इसका लकड़ी बहुत कठिन और भारी होता है और यह दीमक के हमलों के प्रति प्रतिरोधी होता है। यह मुख्य रूप से उत्तर, मध्य और पूर्वोत्तर भारत (बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, असम) में पाया जाता है। यह बड़े शुद्ध 'स्त्रैंड' में पाया जाता है। इसकी लकड़ी रेलवे स्लीपर और घरों के निर्माण के लिए उपयोगी होती है।
- टीक (Tectona grandis): यह बहुत कठिन और टिकाऊ लकड़ी प्रदान करता है, जो जहाज निर्माण, घर के निर्माण और फर्नीचर के लिए उपयुक्त होती है। अनुभवी टीक की लकड़ी दीमक का सामना कर सकती है। इसके अलावा, यह लोहे की कीलें भी जंग नहीं लगाती हैं। इसे मध्य प्रदेश, असम, ओडिशा, बिहार, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के वनों में पाया जाता है।
- चंदन का पेड़: यह हस्तशिल्प के लिए चंदन की लकड़ी और इत्र में उपयोग होने वाले चंदन के तेल प्रदान करता है। यह मुख्य रूप से कर्नाटक में पाया जाता है।
- सेमुल: यह असम, बिहार और तमिलनाडु में पाया जाता है। इसकी लकड़ी नरम और सफेद होती है और इसका उपयोग पैकिंग केस, माचिस की डिब्बियों और खिलौने बनाने के लिए किया जाता है।
- हरड़: यह चमड़े को टैनिंग करने और कपास, लकड़ी और रेशमी वस्त्रों को रंगने के लिए सामग्री प्रदान करता है।
- महुआ के फूल खाए जाते हैं और शराब बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं और खैर को पान के पत्तों के साथ चबाने के लिए सामग्री प्रदान करता है।
पहाड़ी वन
पहाड़ी क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय से टुंड्रा क्षेत्र तक की प्राकृतिक वनस्पति पट्टियों का एक क्रम पाया जाता है, जो लगभग 6 किमी की ऊँचाई में संकुचित होता है। हालांकि, समान ऊँचाई पर भी, धूप वाले क्षेत्रों की वनस्पति उन क्षेत्रों की वनस्पति से भिन्न होती है जो कम धूप वाले होते हैं। पहाड़ी वनों का अध्ययन दो श्रेणियों में किया जा सकता है:
- पहाड़ी (दक्षिणी): दक्षिण में नीलगिरी और पल्नी पहाड़ियों में 1,070-1,525 मीटर की ऊँचाई पर गीले पहाड़ी वनों का क्षेत्र है; इसके नीचे बौनी प्रकार का वर्षावन होता है और इसके ऊपर, समशीतोष्ण वन शुरू होते हैं। सह्याद्रि, सतपुड़ा और ऐकाल पहाड़ियों के उच्च ढलानों में भी इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। 1,500 मीटर से ऊपर नीलगिरियों, अनामलाई और पल्नी की ढलानों पर पश्चिमी समशीतोष्ण वन पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय रूप से शोला कहा जाता है।
- निम्न स्तरों पर एक समृद्ध घुमावदार सवाना पाया जाता है जिसमें कभी-कभी पीट बोग भी होते हैं। शोला वन घने होते हैं लेकिन छोटे होते हैं, इनमें बहुत अधिक वनस्पति और कई एपिफाइट, काई और फर्न होते हैं। सामान्य प्रजातियाँ हैं: मैग्नोलिया, लॉरेल, रोडोडेंड्रॉन, एल्म और प्रूनस। यूकेलिप्टस, सिनकोना और वाटल को बाहर से लाया गया है।
झाड़ी और कांटेदार वन उन स्थानों पर होते हैं जहाँ वर्षा कम होती है, 100 सेंटीमीटर से कम, जो पेड़ के विकास के लिए अपर्याप्त है। ये वन भारत के उत्तर-पश्चिमी भाग में सौराष्ट्र से लेकर पंजाब के मैदानी क्षेत्रों तक फैले हुए हैं।
पूर्व में यह उत्तरी मध्य प्रदेश (मुख्य रूप से मालवा पठार) और दक्षिण-पश्चिम उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड पठार को कवर करते हुए फैला हुआ है। इन जंगलों में खैर, किकर, बबूल, और खजूर जैसे वृक्ष सामान्य हैं। ये वृक्ष छोटे और बिखरे हुए होते हैं। ये जंगल धीरे-धीरे झाड़ी और कांटेदार झाड़ियों में बदल जाते हैं, जो विशिष्ट रेगिस्तानी वनस्पति की ओर ले जाते हैं।
रेगिस्तान और अर्ध-रेगिस्तानी वनस्पति
यह उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ वर्षा 25 सेमी से कम होती है और जहाँ वार्षिक औसत तापमान 25-27 डिग्री सेल्सियस होता है। वनस्पति मुख्यतः कांटेदार झाड़ियों, एकेशिया, जंगली जामुन, बबूल और किकर पर आधारित होती है। ये वृक्ष केवल छह से 10 मीटर ऊँचे होते हैं लेकिन इनके लंबे जड़ें होती हैं। ये जानवरों से सुरक्षा के लिए कठोर कांटों या तेज काँटों से लैस होते हैं। ये राजस्थान, कच्छ और गुजरात के सौराष्ट्र में, दक्षिण पश्चिम पंजाब और डेक्कन के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं।
मैंग्रोव वन (Tridal या Littoral)
ये ज्वारीय क्षेत्रों में तटों और नदियों के किनारे पाई जाती हैं। ये ताजे और खारे पानी दोनों में जीवित रह सकती हैं, जो ज्वारीय क्षेत्रों की मुख्य विशेषता है। इनमें से कुछ जंगलों का सहारा लेने के लिए कई स्थिर जैसे जड़ों का एक जटिल तंत्र होता है, जो उच्च ज्वार पर पानी के नीचे होती हैं; जबकि निम्न ज्वार पर इन्हें देखा जा सकता है। यह जड़ों का उलझा हुआ तंत्र नरम और बदलते कीचड़ में जीवित रहने के लिए एक अद्भुत अनुकूलन है।
मैंग्रोव वन
ज्वारीय वन पूर्वी तट पर डेल्टाओं के किनारे पर प्रचुर मात्रा में और लगभग निरंतर फैले हुए होते हैं, जैसे गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी की डेल्टाएँ और अंडमान और निकोबार द्वीपों के तटों पर। ये पश्चिमी तट पर भी कुछ स्थानों पर पाए जाते हैं। बंगाल में इन्हें सुंदरबन कहा जाता है (जिसका अर्थ है सुंदरि वृक्षों के जंगल)। अन्य प्रमुख वृक्षों में नागराजन और हिंतल शामिल हैं। ये वन ईंधन का एक मूल्यवान स्रोत हैं।

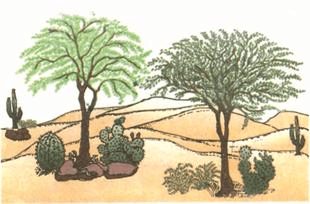
भारत में विभिन्न प्रकार के जंगलों का भौगोलिक वितरण:
- पश्चिम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन: ये जंगल उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 250 सेमी. से अधिक होती है। ये पश्चिमी घाट और असम में पाए जाते हैं। इनमें रबर, महोगनी और आयरनवुड आदि शामिल हैं।
- मानसून वन: ये विशिष्ट मानसूनी पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 150-250 सेमी. होती है। ये जंगल छोटा नागपुर पठार, असम और हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर होते हैं। चाय और साल मुख्य पेड़ हैं।
- शुष्क वन: ये जंगल एक चौड़ी पट्टी में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 100 सेमी. से कम होती है। खैर, शीशम, लकड़ी के लिए उपयोगी होते हैं। ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और डेक्कन पठार में पाए जाते हैं।
- कनिफेरस वन: ये भारत के जंगलों का लगभग 6%占 करते हैं। ये हिमालय में ऊँचाई और वर्षा की मात्रा के अनुसार पाए जाते हैं। देवदार, पाइन, फीर, और स्प्रूस मूल्यवान सॉफ्टवुड पेड़ हैं।
- ज्वारीय वन: ये जंगल गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, और कावेरी के डेल्टाओं में पाए जाते हैं। गंगा डेल्टा के तहत मैनग्रोव जंगल सबसे महत्वपूर्ण हैं।
विदेशी पौधों का हमारे लिए समस्या बनना: भारत में पाए जाने वाले लगभग 40% पौधे प्रजातियाँ बाहर से आई हैं और इन्हें विदेशी पौधे कहा जाता है। ये पौधे सीनो-तिब्बती, अफ्रीकी और इंडो-मलेशियाई क्षेत्रों से लाए गए थे। इन पौधों को भारत में सजावटी बागवानी पौधों के रूप में लाया गया था। ये पौधे गर्म-भीगी उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों में तेजी से बढ़ते हैं। ये तेजी से प्रजनन करते हैं, जिससे इन्हें समाप्त करना कठिन होता है। ये उपयोगी भूमि आवरण को कम करते हैं। ये आर्थिक पौधों की वृद्धि को रोकते हैं। ये बीमारियाँ फैलाते हैं और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा बनते हैं।
लैंटाना और जल हायसिंथ दो ऐसे प्रजातियाँ हैं। जल हायसिंथ को "बंगाल का आतंक" के नाम से जाना जाता है। इसने सभी जल निकायों जैसे नदियों, धाराओं, तालाबों, नहरों आदि को भर दिया है।
- लैंटाना और जल हायसिंथ दो ऐसे प्रजातियाँ हैं। जल हायसिंथ को "बंगाल का आतंक" के नाम से जाना जाता है। इसने सभी जल निकायों जैसे नदियों, धाराओं, तालाबों, नहरों आदि को भर दिया है।
उनकी ऊँचाई की सीमा में, हिमालय उष्णकटिबंधीय से लेकर आल्पाइन तक के वनस्पति क्षेत्रों का एक अनुक्रम प्रस्तुत करता है। हिमालय में विभिन्न प्रकार के वनस्पति क्षेत्र पाए जाते हैं, जो इसके दक्षिणी ढलानों से लेकर उच्च ऊँचाइयों तक फैले हुए हैं। प्राकृतिक वनस्पति समतापृष्ठीय से लेकर टुंड्रा प्रकार तक फैली हुई है। तापमान और वर्षा में ऊँचाई के साथ बदलाव के अनुसार वनस्पति क्षेत्रों की एक श्रृंखला विद्यमान है। वनस्पति में क्रमिक बदलाव ऊँचाई और जलवायु के अनुसार होता है।
- उष्णकटिबंधीय पश्चिमी पर्णपाती वन - ये वन हिमालय के दक्षिणी ढलानों के साथ 1000 मीटर की ऊँचाई तक पाए जाते हैं। उच्च वर्षा के कारण यहाँ साल के घने वन पाए जाते हैं।
- मौसमी वन - घने गीले मौसमी वन 2000 मीटर की ऊँचाई तक पाए जाते हैं। इनमें सदाबहार ओक, चेस्टनट और पाइन के पेड़ शामिल हैं, जो व्यावसायिक रूप से उपयोगी हैं।
- चौड़े पत्तों के सदाबहार वन - ये 2000 मीटर से 3000 मीटर की ऊँचाई के बीच पाए जाते हैं। इनमें ओक, लॉरेल और चेस्टनट के पेड़ शामिल हैं।
- कांटेदार वन - ये 3500 मीटर की ऊँचाई तक पाए जाते हैं। इनमें पाइन, देवदार, सिल्वर फ़िर और स्प्रूस के पेड़ शामिल हैं। देवदार लकड़ी और रेलवे स्लीपर के लिए व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण है।
- आल्पाइन चरागाह - ये 3500 मीटर की ऊँचाई से ऊपर पाए जाते हैं। इनमें छोटी घासें होती हैं, जो गूजर जैसे घुमंतू जनजातियों द्वारा चराई के लिए उपयोग की जाती हैं।
प्रत्येक वनस्पति का अपना विशेष जीवन चक्र होता है, जो इसके पर्यावरण के साथ नाजुक संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है।
- वनस्पति का अपने पर्यावरण के साथ निकट संबंध होता है। प्रत्येक पौधे की प्रजाति अपने पर्यावरण के साथ एक नाजुक संतुलन बनाए रखती है। यह विशेष मिट्टी, जलवायु और तापमान की परिस्थितियों में एक समुदाय के रूप में बढ़ती है। वनस्पति अपने रूप और आकार को पारिस्थितिकीय ढांचे के अनुसार अपनाती है।
- उनका पूर्ण विकास विभिन्न विकास के चरणों का पालन करता है। इस प्रकार, प्रत्येक वनस्पति एक जीवन चक्र से गुजरती है। यह युवा, परिपक्व और वृद्ध अवस्था के विभिन्न चरणों से गुजरती है। प्रत्येक चरण का समय और अवधि पौधे से पौधे में भिन्न होती है। पौधे का जीवन चक्र प्राकृतिक पर्यावरण के तत्वों जैसे जल की आपूर्ति, वर्षा, धूप, मिट्टी और भूमि की ढलान द्वारा नियंत्रित होता है।
उदाहरण के लिए, भारतीय सागौन (Teak) सामूहिक विकास के लिए जाना जाता है। अन्य प्रजातियाँ सागौन के साथ नहीं बढ़ती हैं क्योंकि इसका पर्यावरण विशेष होता है। यह पौधे के विकास का चरम है, जहाँ यह एक समुदाय के रूप में विकसित होता है। इस प्रकार, प्रत्येक वनस्पति एक निश्चित जीवन चक्र से गुजरती है, उनका रूप, अनुकूलन, विकास के चरण और सामूहिक विकास उनके पर्यावरण या पारिस्थितिकीय संतुलन पर निर्भर करते हैं।
बोरेल हिमालय और प्रायद्वीपीय क्षेत्रों का अधिकांश हिस्सा स्वदेशी वनस्पति से ढका हुआ है। लेकिन इंडो-गंगा मैदान और थार रेगिस्तान में ऐसे पौधे होते हैं जो बाहर से आए हैं। इन्हें विदेशी पौधे कहा जाता है। सिनो-तिब्बती क्षेत्रों से आने वाली पौधे की प्रजातियों को 'बोरेल' कहा जाता है।
भारत में वन का क्षय एक देश के पास अपने कुल क्षेत्र का कम से कम एक-तिहाई हिस्सा जंगलों के अधीन होना चाहिए ताकि स्वस्थ पारिस्थितिकीय संतुलन बना रहे। भारत में केवल 23% भूमि जंगलों के अधीन है। वास्तव में अच्छे जंगल निम्नलिखित कारणों से घटित हुए हैं:—
- (i) व्यापक वन क्षेत्र की कटाई।
- (ii) स्थानांतरित कृषि (Shifting Cultivation) का अभ्यास।
- (iii) भारी मिट्टी का अपरदन।
- (iv) चरागाहों का अत्यधिक चराई।
- (v) लकड़ी और ईंधन के लिए पेड़ों की कटाई।
- (vi) भूमि पर मानव निवास।
देश के वन संसाधनों पर जनसंख्या का भारी दबाव है। बढ़ती जनसंख्या को कृषि के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता है। पशुपालन के लिए भी चरागाहों की आवश्यकता होती है। औद्योगिक उपयोग के लिए कई वन उत्पादों की आपूर्ति के लिए जंगलों का तेजी से शोषण किया जा रहा है। इसलिए, वनों की सुरक्षा के लिए विभिन्न तरीकों को अपनाना आवश्यक है। कई क्षेत्रों में वृक्षारोपण और पुनर्वृक्षारोपण का विकास किया जा रहा है। घास के मैदानों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। सिल्वीकल्चर के बेहतर तरीकों का उपयोग किया जा रहा है। तेजी से बढ़ने वाली पौधों की प्रजातियाँ लगाई जा रही हैं। वनों के अंतर्गत क्षेत्र को बढ़ाया जा रहा है।
वन हमारे लिए लाभकारी हैं
जंगलों से प्राप्त अप्रत्यक्ष लाभों में पारिस्थितिकी में सुधार, जलवायु पर प्रभाव और तापमान में संतुलन, मिट्टी का संरक्षण और नमी एवं जलधाराओं का नियंत्रण शामिल हैं। जंगल पहाड़ी धाराओं और नदियों में निरंतर प्रवाह उत्पन्न करते हैं। मैदानों में बाढ़ की तीव्रता कम होती है।
प्रत्यक्ष लाभ
मुख्य वन-आधारित उद्योगों में पल्प पेपर, न्यूजप्रिंट, रेयॉन, सॉ मिलिंग, वुड-पैनल उत्पाद, माचिस, रेजिन, औषधीय जड़ी-बूटियाँ, जंगली जीवन और पर्यटन शामिल हैं। फीर और स्प्रूस रेयान और न्यूजप्रिंट के लिए सबसे अच्छे होते हैं। जंगल विभिन्न प्रकार के छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं जैसे कि टैनिंग सामग्री, शहद, lacquer, रंग, आवश्यक तेल, घास, चारा आदि। टेकी, रोज़वुड, पेपर और पेपर बोर्ड, प्राकृतिक गम, बीज आदि के निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। जंगल आयात प्रतिस्थापन में मदद कर सकते हैं। वन पट्टों पर रॉयल्टी राज्यों के लिए राजस्व उत्पन्न करती है। इसके अलावा, यह कई लोगों को रोजगार भी प्रदान करती है।
भारत की वन नीति भारत उन पहले कुछ देशों में से एक है जिसने वन नीति अपनाई। यह नीति सबसे पहले 1952 में संशोधित की गई थी और फिर 1988 में। 1988 की संशोधित वन नीति के मुख्य उद्देश्य थे:
- (i) पारिस्थितिकी संतुलन का संरक्षण और प्राकृतिक विरासत का संरक्षण
- (ii) मिट्टी की कटाव को नियंत्रित करना, जलग्रहण क्षेत्रों में वनों की कमी और उत्तर-पश्चिम रेगिस्तान क्षेत्र तथा तटों के साथ बालू के टीलों का विस्तार रोकना
- (iii) ग्रामीण और जनजातीय लोगों को वन उत्पादों की उनकी आवश्यकताएं प्रदान करना
- (iv) वनों के उत्पादों का सर्वश्रेष्ठ तरीके से उपयोग करना
- (v) वनों की उत्पादकता और वन आवरण को वृक्षारोपण कार्यक्रमों के माध्यम से बढ़ाना
- (vi) लोगों को इस उद्देश्य को पूरा करने में शामिल करना।
वृक्षारोपण कार्यक्रम
- वृक्षारोपण को बढ़ाने, संरक्षित करने और बनाए रखने के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई गई हैं।
- पर्वतीय ढलानों, जलग्रहण क्षेत्रों, नहरों के किनारों आदि पर नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए संरक्षण प्रयास किए गए हैं।
- छठी योजना में सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों की शुरुआत की गई और इसमें बिना वन को नष्ट किए ईंधन लकड़ी का उत्पादन करने की योजनाएं शामिल की गईं।
- सातवीं योजना में ब्लॉक वृक्षारोपण, पट्टी वृक्षारोपण और कृषि वानिकी को प्राथमिकता दी गई।
- एक राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड का गठन बंजर भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए किया गया, जिसमें लोगों की भागीदारी थी।
- स्थानीय वृक्षारोपण के लिए पौधों का उत्पादन प्रोत्साहित करने के लिए 1986-87 में विकेंद्रित लोगों की नर्सरी स्थापित की गई।
- पौधारोपण सामग्री और वृक्षों की दक्षता में सुधार के लिए अनुसंधान को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- ग्रामीण और जनजातीय जनसंख्या की ईंधन लकड़ी और चारे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट कार्यक्रमों का विकास किया जा रहा है।
सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों के उद्देश्य
सामाजिक वनीकरण कार्यक्रमों की शुरुआत छठी योजना में की गई थी, जिसमें बिना जंगल को नष्ट किए ईंधन लकड़ी, चारा, फल, फाइबर और उर्वरक (5F) उत्पादन के लिए योजनाएँ शामिल थीं। भारत की राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 1976 में सामाजिक वनीकरण कार्यक्रम के उद्देश्य को इस प्रकार स्पष्ट किया:
- (i) ईंधन प्रदान करना और इस प्रकार गोबर के उपयोग को उर्वरक के रूप में मुक्त करना।
- (ii) फलों का उत्पादन बढ़ाना और इस प्रकार देश के लिए खाद्य संसाधनों की क्षमता में वृद्धि करना।
- (iii) मिट्टी का संरक्षण करना और मिट्टी की उर्वरता के आगे के deteriorate को रोकना।
- (iv) कृषि क्षेत्रों के चारों ओर आश्रय बेल्ट बनाने में मदद करना ताकि उनकी उत्पादकता बढ़ सके।
- (v) मवेशियों के लिए पत्तियों का चारा प्रदान करना और इस प्रकार संरक्षित वन क्षेत्रों में चराई की तीव्रता को कम करना।
- (vi) परिदृश्य के लिए छाया और सजावटी पेड़ प्रदान करना।
- (vii) कृषि उपकरणों, घर निर्माण और बाड़ लगाने के लिए छोटे भूखंड और लकड़ी प्रदान करना।
- (viii) लोगों के बीच पेड़ के प्रति जागरूकता और पेड़ों के प्रति प्रेम को बढ़ाना।
- (ix) खेतों, गांवों, नगर निगम और सार्वजनिक भूमि में पेड़ लगाने और उनकी देखभाल को लोकप्रिय बनाना, उनके सौंदर्यात्मक, आर्थिक और संरक्षण मूल्य के लिए।
सामाजिक वनीकरण और पर्यावरण के बीच संबंध
सामाजिक वनीकरण पर्यावरणीय सुधार और सामाजिक-आर्थिक उत्थान से निकटता से जुड़ा हुआ है, जो ग्रामीण और शहरी निवास के जीवन के गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार की ओर ले जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र, सामाजिक वनीकरण और पर्यावरण के बीच संबंध इतने निकटता से जुड़े हुए हैं कि इसे सरलता से समझना कठिन है। इसके अलावा, सामाजिक वनीकरण के प्रमुख उद्देश्य आर्थिक और पर्यावरणीय दोनों होने के कारण जटिलता और भी बढ़ जाती है।
पर्यावरण को अकेले लेते हुए, सामाजिक वानिकी (social forestry) जब व्यापक और सफलतापूर्वक लागू की जाती है, तो यह कई सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव उत्पन्न कर सकती है जैसे कि जल संतुलन में सुधार, जलाशयों से जल उत्पादन, भूमि की भौतिक विशेषताओं में सुधार जो बेहतर जल अवशोषण, संरक्षण क्षमता और गहराई में रिसाव के लिए अनुकूल हैं, भूजल स्तर की कमी, सतही प्रवाह जल और जलाशयों, नदियों, धाराओं आदि में अवसादन में कमी, कार्बन का पुनर्चक्रण, उच्च खाद्य उत्पादन के लिए अनुकूल सूक्ष्मजलवायु स्थितियों का निर्माण, पारदर्शिता के माध्यम से वर्षा में वृद्धि, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडलीय तापमान और सापेक्ष आर्द्रता और ओजोन परत में संतुलन बनाए रखना।
- सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के पर्यावरणीय पुनर्जनन से संबंधित विभिन्न घटक हैं:
- (i) निवास स्थान के निकट अवनत वन का संरक्षण और वृक्षारोपण।
- (ii) सामुदायिक भूमि और सरकारी जल भूमि पर गांव के वन क्षेत्रों का निर्माण।
- (iii) टैंक बिस्तरों और तटभूमि में ब्लॉक वृक्षारोपण।
- (iv) सीमांत और उप-सीमांत कृषि भूमि पर कृषि-वृक्षारोपण।
- (v) गृहस्थानों के साथ, खेतों की सीमाओं पर वृक्षारोपण, विशेष रूप से शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में।
- (vi) चरागाह और सिल्विपैस्टर विकास।
- (vii) शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में सौंदर्य के लिए वृक्षारोपण, प्रदूषित हवा की शुद्धि और ध्वनि प्रदूषण का नियंत्रण।
- (viii) वृक्ष और झाड़ी रोपण के द्वारा जल और वायु कटाव को नियंत्रित करना, आश्रय बेल्ट, हरे बेल्ट और ध्वनि सुरक्षा बेल्ट का रोपण।
- (ix) सड़क किनारे, नहर तटों और रेल लाइनों के साथ पट्टी वृक्षारोपण।
ये कार्यक्रम यदि प्रभावी रूप से लोगों की सक्रिय भागीदारी के साथ किए जाएं, तो यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि ग्रामीण लोगों की बुनियादी आवश्यकताएँ जैसे कि ईंधन, चारा, फाइबर, छोटे लकड़ी और कुटीर उद्योग के कच्चे माल आदि की पूर्ति हो सके, और दूसरी ओर पारिस्थितिकी सुरक्षा जैसे कि वायु और जल कटाव, प्रदूषित जल और हवा से सुरक्षा, और स्वच्छ हवा की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
सामाजिक वानिकी के समस्याग्रस्त क्षेत्र सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में कई क्षेत्र शामिल हैं जो लोगों की भागीदारी के लिए नए रास्ते खोलते हैं। निम्नलिखित समस्याएँ मुख्य क्षेत्र हैं जहाँ लोगों की भागीदारी एक महत्वपूर्ण कारक हो सकती है:
- (i) अवैध कटाई को रोकना।
- (ii) चराई को नियंत्रित करना।
- (iii) उत्पादक वनों का प्रबंधन।
- (iv) वन्यजीवों की सुरक्षा।
- (v) अवनत वनों का पुनर्वास।
- (vi) मिट्टी और जल संरक्षण।
- (vii) सरकार के वृक्षारोपण कार्यक्रम।
|
93 videos|435 docs|208 tests
|




















