NCERT संक्षेप: विषय-5 यात्रियों की दृष्टि से (कक्षा 12) | UPSC CSE के लिए इतिहास (History) PDF Download
परिचय
यात्री नए देशों में विभिन्न परिदृश्यों, रीति-रिवाजों, भाषाओं, विश्वासों और प्रथाओं का सामना करते हैं। महिला यात्री मौजूद थीं, लेकिन उनके खाते कम हैं। यात्रा के जीवित खाते विषयवस्तु में भिन्न होते हैं, जिसमें दरबार के मामलों, धार्मिक मुद्दों, वास्तुकला आदि का समावेश होता है। कुछ यात्रियों ने अपने ही देशों में प्रचलित रीति-रिवाजों और परंपराओं पर ध्यान केंद्रित किया। यात्रियों द्वारा प्रदान की गई सामाजिक जीवन का वर्णन अतीत के ज्ञान को समृद्ध कर सकता है। तीन प्रमुख यात्री अल-बिरूनी, इब्न बतूता, और फ्रैंकोइस बर्नियर हैं, जो विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से आए थे। यात्रियों के दृष्टिकोण उनके खातों को रोचक बनाते हैं। इन खातों के लिए लक्षित दर्शक भिन्न थे।
अल-बिरूनी और किताब-उल-हिंद
ख्वारिज्म से पंजाब तक
पृष्ठभूमि और शिक्षा
- अल-बिरूनी, जिनका जन्म 973 में ख्वारिज्म (वर्तमान उज्बेकिस्तान) में हुआ, एक ऐसे क्षेत्र से आए जो अपने जीवंत बौद्धिक माहौल के लिए जाना जाता है।
- उन्होंने व्यापक शिक्षा प्राप्त की, जिसमें उन्होंने सीरियक, अरबी, फारसी, हिब्रू, और संस्कृत जैसी कई भाषाओं में महारत हासिल की।
- हालांकि उन्हें ग्रीक नहीं आती थी, उन्होंने अरबी अनुवादों के माध्यम से प्लेटो जैसे ग्रीक दार्शनिकों के कार्यों से परिचितता प्राप्त की।
गज़नी में स्थानांतरण
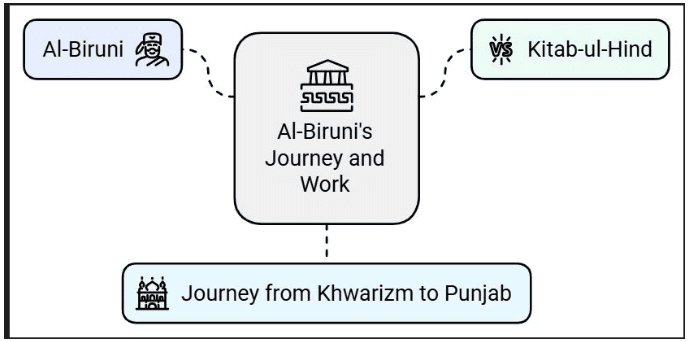
1017 में, सुलतान महमूद के ख्वारिज़्म पर आक्रमण के दौरान, अल-बिरूनी, अन्य विद्वानों और कवियों के साथ, गज़नी ले जाया गया।
- आरंभ में एक बंधक के रूप में, उसने अंततः इस शहर के प्रति रुचि विकसित की और अपना शेष जीवन वहीं बिताया।
गज़नी एक सांस्कृतिक आदान-प्रदान का केंद्र बन गया, जहाँ अल-बिरूनी की बौद्धिक गतिविधियाँ फलने-फूलने लगीं।
भारत में रुचि
- अल-बिरूनी की भारत के प्रति रुचि गज़नी में अपने ठहराव के दौरान बढ़ी।
- गज़नवी साम्राज्य का पंजाब में विस्तार सांस्कृतिक इंटरैक्शन को बढ़ावा देता था, जिससे अरब विद्वानों और स्थानीय जनसंख्या के बीच विश्वास और समझ विकसित हुई।
- अल-बिरूनी ने संस्कृत, भारतीय धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथों का अध्ययन किया, और ब्राह्मण पुजारियों के साथ समय बिताया।
- पंजाब और उत्तरी भारत में उनके व्यापक प्रवास ने क्षेत्र की उनकी समझ में योगदान दिया।
यात्रा साहित्य में योगदान
अल-बिरूनी के समय में, यात्रा साहित्य अरबी साहित्य में एक स्थापित शैली थी।
- उनके अनुभवों ने भारत में इस शैली में एक नया आयाम जोड़ा, जो भारतीय संस्कृति, धर्म और दर्शन पर अंतर्दृष्टियाँ प्रदान करता है।
- हालांकि अल-बिरूनी की रचनाएँ 1500 से पहले भारत में व्यापक रूप से पढ़ी नहीं गई थीं, लेकिन उन्होंने भारत के बाहर लोकप्रियता हासिल की, जिससे उपमहाद्वीप की व्यापक समझ में योगदान मिला।
अल-बिरूनी

किताब-ul-हिंद
संरचना और सामग्री
- अल-बिरूनी की किताब-ul-हिंद, जो अरबी में लिखी गई है, एक व्यापक काम है जो 80 अध्यायों में विभाजित है।
- यह धर्म, दर्शन, त्योहारों, खगोलशास्त्र, रसायन विज्ञान, रीति-रिवाजों, सामाजिक जीवन, वजन और माप, चित्रण, कानून, और मेट्रोलॉजी जैसे विभिन्न विषयों को शामिल करती है।
- प्रत्येक अध्याय की संरचना उल्लेखनीय है, जो आमतौर पर एक प्रश्न से शुरू होती है, उसके बाद संस्कृत परंपराओं के आधार पर एक विवरण होता है, और अन्य संस्कृतियों के साथ तुलना के साथ समाप्त होती है।
गणितीय अभिविन्यास
शोधकर्ताओं ने अल-बिरूनी के काम में एक विशिष्ट ज्यामितीय संरचना का अवलोकन किया है, जो सटीकता और पूर्वानुमानिता द्वारा विशेषता प्राप्त करती है। यह संरचना उनके गणितीय उन्मुखीकरण को दर्शाती है, जो जानकारी प्रस्तुत करने के लिए एक सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करती है।
- शोधकर्ताओं ने अल-बिरूनी के काम में एक विशिष्ट ज्यामितीय संरचना का अवलोकन किया है, जो सटीकता और पूर्वानुमानिता द्वारा विशेषता प्राप्त करती है।
लक्ष्य दर्शक
- अल-बिरूनी ने संभवतः अपने काम को भारतीय उपमहाद्वीप की सीमाओं पर रहने वाले लोगों के लिए लिखा।
- संस्कृत ग्रंथों के अरबी में अनुवादों और अनुकूलनों के प्रति उनकी परिचितता यह दर्शाती है कि वे विद्यमान ज्ञान के भंडार से अवगत थे।
- हालांकि, अल-बिरूनी ने इन ग्रंथों के लेखन के तरीके की आलोचना की, जिससे उनके सुधारने की इच्छा का पता चलता है।
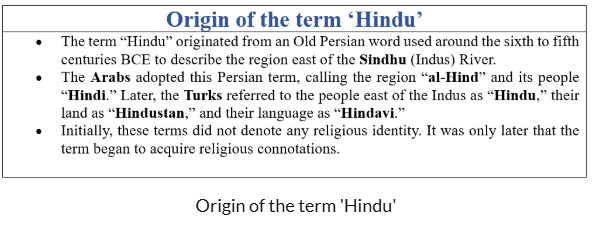
इब्न बतूता का रिहला
एक प्रारंभिक विश्व-यात्री
- इब्न बतूता, जो चौदहवीं शताब्दी में टंगियर, मोरक्को में जन्मे, एक अत्यधिक सम्मानित और शिक्षित परिवार से आए, जो इस्लामी धार्मिक कानून या शरीआ में विशेषज्ञता के लिए जाने जाते थे।
- अपने परिवार की परंपरा के अनुसार, उन्होंने युवा उम्र से ही साहित्यिक और शैक्षणिक शिक्षा प्राप्त की।
यात्रा का प्रेम
अपने समकालीनों से अलग, इब्न बतूता ने यात्रा के माध्यम से प्राप्त अनुभव को पारंपरिक पुस्तक ज्ञान से अधिक महत्व दिया। उनकी यात्रा के प्रति असंतोषजनक प्रेम ने उन्हें दूर-दूर के स्थानों और विविध संस्कृतियों की खोज करने के लिए प्रेरित किया। भारत की यात्रा से पहले, जो 1332-33 में हुई, उन्होंने पहले ही मक्का की तीर्थयात्रा की और सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान और पूर्वी अफ्रीका के कुछ व्यापारिक बंदरगाहों जैसे क्षेत्रों में व्यापक यात्रा की।
- अपने समकालीनों से अलग, इब्न बतूता ने यात्रा के माध्यम से प्राप्त अनुभव को पारंपरिक पुस्तक ज्ञान से अधिक महत्व दिया।
- उनकी यात्रा के प्रति असंतोषजनक प्रेम ने उन्हें दूर-दूर के स्थानों और विविध संस्कृतियों की खोज करने के लिए प्रेरित किया।
भारत की यात्रा
- केंद्र एशिया के माध्यम से भूमि के रास्ते यात्रा करते हुए, इब्न बतूता 1333 में सिंध पहुँचे।
- दिल्ली के सुलतान मुहम्मद बिन तुगलक की प्रसिद्धि से प्रभावित होकर, वे दिल्ली के लिए निकल पड़े, मुल्तान और उच से गुजरते हुए।
- उनकी विद्या से प्रभावित होकर, सुलतान ने उन्हें काज़ी या न्यायाधीश के रूप में दिल्ली में नियुक्त किया।
- कुछ वर्षों बाद, एक गलतफहमी के कारण इब्न बतूता को जेल में डाल दिया गया, लेकिन स्पष्टता के बाद, उन्हें सम्राटी सेवा में बहाल कर दिया गया।
- 1342 में, उन्हें सुलतान का प्रतिनिधि चीन के मंगोल शासक के पास नियुक्त किया गया।
व्यापक यात्राएँ
इब्न बतूता की यात्राएँ मलबार तट से लेकर मालदीव तक फैली हुई थीं, जहाँ उन्होंने अठारह महीनों तक काजी के रूप में सेवा की। इसके बाद वे श्रीलंका गए, फिर से मलबार तट और मालदीव का दौरा किया, और फिर बंगाल और असम का अन्वेषण किया। उनकी यात्रा सुमात्रा और अंततः चीनी बंदरगाह शहर ज़ैतुन (क्वांझोउ) की ओर बढ़ी। चीन में, उन्होंने व्यापक रूप से यात्रा की, बीजिंग तक पहुँचे और 1347 में घर लौटने का निर्णय लिया।
- इब्न बतूता की यात्राएँ मलबार तट से लेकर मालदीव तक फैली हुई थीं, जहाँ उन्होंने अठारह महीनों तक काजी के रूप में सेवा की।
- इसके बाद वे श्रीलंका गए, फिर से मलबार तट और मालदीव का दौरा किया, और फिर बंगाल और असम का अन्वेषण किया।
- उनकी यात्रा सुमात्रा और अंततः चीनी बंदरगाह शहर ज़ैतुन (क्वांझोउ) की ओर बढ़ी।
मार्को पोलो के साथ तुलना
- इब्न बतूता की यात्रा की कहानी अक्सर मार्को पोलो की यात्रा की कहानी के साथ तुलना की जाती है, जिन्होंने तेरहवीं शताब्दी के अंत में चीन और भारत का अन्वेषण किया।
14वीं शताब्दी की यात्रा की चुनौतियाँ
- यह महत्वपूर्ण है कि इब्न बतूता ने चौदहवीं शताब्दी में यात्रा की, जिसमें आधुनिक समय की तुलना में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
- यात्रा की कठिन और खतरनाक प्रकृति को इब्न बतूता के विवरणों से स्पष्ट किया गया है, जो दर्शाते हैं कि इसमें काफी समय लगता था और जोखिम भी होता था।
- उदाहरण के लिए, multan से दिल्ली की यात्रा में चालीस दिन लगे, और सिंध से दिल्ली जाने का मार्ग लगभग पचास दिन लेता था।
“अजीब चीजों का आनंद”
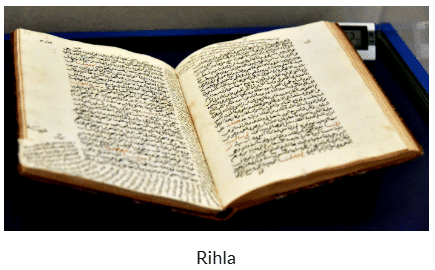
- इब्न बतूता एक अनवरत यात्री थे जिन्होंने मोरक्को लौटने से पहले उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, भारतीय उपमहाद्वीप और चीन की कई वर्षों तक खोजबीन की।
- उनकी वापसी पर, स्थानीय शासक ने इब्न बतूता की कहानियों को रिकॉर्ड करने के निर्देश जारी किए, जो इस अद्वितीय globe-trotter की कथाओं के प्रति आकर्षण और महत्व को दर्शाता है।
फ्रांकोइस बर्नियर: एक अलग डॉक्टर
फ्रांकोइस बर्नियर: एक अलग डॉक्टर
पुर्तगाली आगमन और डुआर्ते बारबोसा
- 1500 के आसपास भारत में पुर्तगालियों के आगमन के बाद, भारतीय सामाजिक रीति-रिवाजों और धार्मिक प्रथाओं के बारे में विस्तृत विवरणों की एक लहर उत्पन्न हुई।
- विशेष रूप से, जीसुइट रोबर्टो नोबिली ने भारतीय ग्रंथों का यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद करने का कार्य किया।
- प्रमुख पुर्तगाली लेखकों में डुआर्ते बारबोसा शामिल थे, जिन्होंने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज का व्यापक विवरण प्रदान किया।
1600 के बाद: डच, अंग्रेजी और फ्रांसीसी यात्री
- 1600 के बाद, डच, अंग्रेजी और फ्रांसीसी यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी।
- जीन-बैप्टिस्ट टेवर्नियर, एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी जौहरी, उनमें से एक हैं, जिन्होंने भारत में कम से कम छह बार यात्रा की।
- टेवर्नियर, व्यापारिक स्थितियों से प्रभावित होकर, भारत, ईरान और ओटोमन साम्राज्य के बीच तुलना की।
- कुछ यात्री, जैसे कि इतालवी डॉक्टर माणुची, ने यूरोप वापस लौटने का विकल्प नहीं चुना और भारत में बस गए।
फ्रांकोइस बर्नियर और मुग़ल साम्राज्य
- फ्रांकोइस बर्नियर, एक फ्रांसीसी, ने भारत में अपने बारह वर्षों (1656 से 1668) के दौरान एक डॉक्टर, राजनीतिक दार्शनिक और इतिहासकार के रूप में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला।
- वह मुग़ल दरबार से निकटता से जुड़े थे, जहां उन्होंने सम्राट शाहजहाँ के बड़े बेटे प्रिंस दारा शुकोह के चिकित्सक के रूप में कार्य किया।
- बाद में, उन्होंने मुग़ल दरबार के आर्मेनियाई नoble डेनिशमंद खान के साथ एक विद्वान और वैज्ञानिक के रूप में काम किया।
“पूर्व” और “पश्चिम” की तुलना
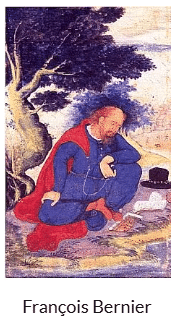
- बर्नियर की भारत में व्यापक यात्रा ने उनकी रचनाओं को प्रेरित किया, जहां उन्होंने अक्सर भारतीय स्थिति की तुलना यूरोप में होने वाले विकासों से की।
- उनका प्रमुख कार्य, जो फ्रांस के राजा लुई XIV को समर्पित था, और अन्य रचनाएँ प्रभावशाली अधिकारियों और मंत्रियों को लिखे गए पत्रों के रूप में, अक्सर भारत को यूरोप की तुलना में एक निराशाजनक रोशनी में प्रस्तुत करते थे।
प्रकाशन और स्वीकृति
- बर्नियर के कार्य 1670-71 में फ्रांस में प्रकाशित हुए और अगले पांच वर्षों में तेजी से अंग्रेजी, डच, जर्मन और इतालवी में अनुवादित किए गए।
- उनकी रचनाओं की लोकप्रियता कई पुनर्मुद्रणों से स्पष्ट है, जिसमें फ्रांसीसी संस्करण 1670 से 1725 के बीच आठ बार पुनर्मुद्रित हुआ और अंग्रेजी संस्करण 1684 तक तीन बार।
एक विदेशी दुनिया को समझना: अल-बिरूनी और संस्कृत परंपरा
समझने में बाधाओं को पार करना
- उपमहाद्वीप में यात्रियों को ऐसी प्रथाओं की व्याख्या करने की चुनौती का सामना करना पड़ा जो उनके लिए अपरिचित थीं।
- प्रत्येक यात्री ने अपने अवलोकनों को समझने के लिए विशिष्ट रणनीतियों का उपयोग किया। उदाहरण के लिए, अल-बिरूनी ने अपने कार्य में अंतर्निहित कठिनाइयों को स्वीकार किया।
- उन्होंने समझने में कई "बाधाओं" की पहचान की, जिसमें भाषा पहली थी। उनके अनुसार, संस्कृत अरबी और फारसी से काफी भिन्न थी, जिससे विचारों और अवधारणाओं का अनुवाद करना चुनौतीपूर्ण हो गया।
- दूसरी बाधा जो उन्होंने पहचानी, वह धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं में भिन्नता थी, और तीसरी स्थानीय जनसंख्या की आत्मकेंद्रितता और अलगाव था।
- दिलचस्प बात यह है कि इन चुनौतियों के बावजूद, अल-बिरूनी ने ब्राह्मणों के कामों पर भारी निर्भरता दिखाई, अक्सर वेदों, पुराणों, भागवत गीता, पतंजलि के ग्रंथों, मनुस्मृति आदि के उद्धरण देते थे ताकि भारतीय समाज की समझ प्राप्त कर सकें।
अल-बिरूनी का जाति व्यवस्था का वर्णन
- जाति व्यवस्था की व्याख्या करने के प्रयास में, अल-बिरूनी ने अन्य समाजों में समानताएँ खोजीं।
- उन्होंने देखा कि प्राचीन फारस ने चार सामाजिक श्रेणियों को मान्यता दी: योद्धा और राजकुमार; साधु, अग्नि-पुरोहित और वकील; चिकित्सक, खगोलज्ञ और अन्य वैज्ञानिक; और किसान और कारीगर।
- ब्राह्मणीय जाति व्यवस्था के वर्णन को स्वीकार करने के बावजूद, अल-बिरूनी ने इस प्रणाली में निहित प्रदूषण की धारणा का विरोध किया।
- उन्होंने तर्क किया कि सब कुछ अशुद्ध स्वाभाविक रूप से शुद्धता को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करता है, जैसे सूर्य हवा को शुद्ध करता है और समुद्र में नमक पानी के प्रदूषण को रोकता है।
- अल-बिरूनी की जाति व्यवस्था की समझ उनके द्वारा मानक संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से गहराई से प्रभावित थी, जो ब्राह्मणों के दृष्टिकोण से प्रणाली के नियमों को स्पष्ट करती है।
- हालांकि, उन्होंने पहचाना कि वास्तविक जीवन में आवेदन अक्सर भिन्न होता है, यह देखते हुए कि "अंत्यजा" (प्रणाली के बाहर जन्मे) श्रेणियों ने किसानों और ज़मींदारों को सस्ती श्रम प्रदान की। सामाजिक उत्पीड़न के बावजूद, वे आर्थिक नेटवर्क में समाहित थे।
इब्न बत्तूता और अपरिचित की उत्तेजना
- जब इब्न बट्टूता चौदहवीं सदी में दिल्ली पहुंचे, तब उपमहाद्वीप एक वैश्विक संचार नेटवर्क का हिस्सा था जो पूर्व में चीन से लेकर पश्चिम में उत्तर-पश्चिम अफ्रीका और यूरोप तक फैला हुआ था।
- इब्न बट्टूता ने स्वयं इन क्षेत्रों का व्यापक रूप से दौरा किया, पवित्र तीर्थ स्थलों का दौरा किया, विद्वानों और शासकों के साथ समय बिताया, अक्सर काज़ी के रूप में कार्य किया, और शहरी केंद्रों की बहुसांस्कृतिक संस्कृति में डूब गए, जहाँ लोग अरबी, फारसी, तुर्की और अन्य भाषाओं में संवाद करते थे, विचार, जानकारी, और किस्से साझा करते थे।
नारियल और पान
- इब्न बट्टूता ने प्रतिनिधित्व की अनूठी रणनीतियों का उपयोग किया, जो विशेष रूप से नारियल और पान के उनके वर्णनों में स्पष्ट हैं। ये पौधों से प्राप्त वस्तुएं उनके दर्शकों के लिए पूरी तरह से अपरिचित थीं, जो उनके विदेशी और अज्ञात पर ध्यान केंद्रित करने को दर्शाती हैं।
इब्न बट्टूता और भारतीय शहर
- इब्न बतूता ने पाया कि उपमहाद्वीप के शहरों में उत्साही, संसाधनों और कौशल वाले लोगों के लिए रोमांचक अवसर थे।
- घनी जनसंख्या और समृद्धि वाले ये शहर, युद्धों और आक्रमणों के कारण कभी-कभी होने वाली रुकावटों के बावजूद, भीड़भाड़ वाली सड़कों और विविध वस्तुओं से भरे जीवंत बाजारों से भरे हुए थे।
- दिल्ली को भारत का सबसे बड़ा शहर बताया गया, और दौलताबाद (महाराष्ट्र) आकार में दिल्ली के बराबर था।
- हालांकि इब्न बतूता ने शहरों की समृद्धि के बारे में विस्तार से नहीं बताया, इतिहासकारों ने उनके विवरणों का उपयोग यह सुझाव देने के लिए किया कि शहरों ने गांवों से अधिशेष का अधिग्रहण करके अपनी संपत्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्राप्त किया।
- भारतीय कृषि की उत्पादकता, जो दो फसलों के लिए उपजाऊ मिट्टी से संचालित होती है, ने इस समृद्धि में योगदान दिया।
- उपमहाद्वीप अंतर-एशियाई व्यापार और वाणिज्य के नेटवर्क में अच्छी तरह से एकीकृत था, जहाँ भारतीय उत्पादों की पश्चिम एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया में उच्च मांग थी।
कपड़े, विशेष रूप से सूती कपड़ा, बारीक मुसलिन, रेशम, ब्रोकेड और साटन अत्यधिक मांग में थे, कुछ प्रकार के बारीक मुसलिन इतने महंगे थे कि केवल nobles और बहुत अमीर लोग ही उन्हें खरीद सकते थे।
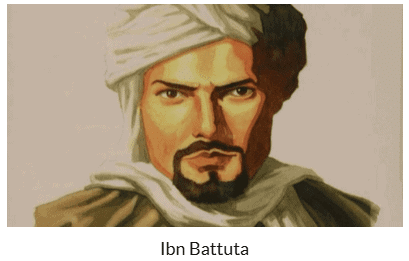
राज्य ने व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष उपाय किए, व्यापार मार्गों के साथ अच्छी तरह से सुसज्जित सराय और अतिथि गृह प्रदान किए।
- राज्य ने व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष उपाय किए, व्यापार मार्गों के साथ अच्छी तरह से सुसज्जित सराय और अतिथि गृह प्रदान किए।
- इब्न बट्टूता ने डाक प्रणाली की दक्षता से प्रभावित होकर देखा, जिससे व्यापारियों को जानकारी भेजने, ऋण भेजने और लंबी दूरी पर सामान भेजने की अनुमति मिली।
- यह प्रणाली इतनी प्रभावी थी कि दिल्ली से सिंध जाने में पचास दिन लगते थे, जबकि जासूसों की खबरें पांच दिन में सुल्तान तक पहुँच जाती थीं।
बर्नियर और नाशवान पूर्व
फ्रांस्वा बर्नियर का दृष्टिकोण
- फ्रांस्वा बर्नियर, एक फ्रांसीसी चिकित्सक और यात्री, का दृष्टिकोण अन्य अन्वेषकों, जैसे इब्न बट्टूता, की तुलना में अलग था।
- जहाँ इब्न बट्टूता ने नवाचार और रोमांच पर ध्यान केंद्रित किया, वहीं बर्नियर ने भारत की तुलना यूरोप, विशेषकर फ्रांस, से एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण से करने पर अधिक ध्यान दिया।
- उनका उद्देश्य नीति निर्माताओं और बुद्धिजीवियों को ऐसे निर्णय लेने के लिए प्रभावित करना था, जिन्हें उन्होंने \"सही\" माना।
मुगल साम्राज्य में यात्राएँ
- बर्नियर की "मुगल साम्राज्य में यात्रा" में विस्तृत अवलोकन, महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टियाँ और चिंतन शामिल हैं।
- उन्होंने मुगल इतिहास को एक सार्वभौमिक ढांचे में रखने का प्रयास किया है, जिसे वे लगातार समकालीन यूरोप से तुलना करते हैं।
भूमि स्वामित्व का प्रश्न
बर्नियर ने यह नोट किया कि मुगल भारत और यूरोप के बीच एक प्रमुख अंतर यह था कि पूर्व में निजी भूमि स्वामित्व का अभाव था। उनका दृष्टिकोण निजी संपत्ति के प्रति उनके मजबूत समर्थन और यह विश्वास से प्रभावित था कि मुगल साम्राज्य की ताज भूमि स्वामित्व प्रणाली का आर्थिक और सामाजिक पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा।
ताज स्वामित्व और इसके परिणाम
- बर्नियर का तर्क है कि मुगल साम्राज्य में सम्राट के पास सभी भूमि थी, जिसे उन्होंने नबाबों के बीच वितरित किया।
- उनके अनुसार, इसके परिणामस्वरूप भूमि धारकों के लिए अपनी भूमि को अपने बच्चों को सौंपने की असमर्थता हुई, जिसने कृषि में दीर्घकालिक निवेश को हतोत्साहित किया।
बर्नियर की आलोचना और इसका प्रभाव
बर्नियर के अनुसार, निजी संपत्ति का अभाव कृषि के विनाश, किसान वर्ग के उत्पीड़न, और जीवन स्तर में निरंतर गिरावट का कारण बना, सिवाय शासक कुलीनता के।
बर्नियर की भारत में भूमि अधिकारों की आलोचना केवल उनके लिए अद्वितीय नहीं थी, बल्कि यह सोलहवीं और सत्रहवीं शताब्दी के अन्य यात्रियों के खातों में पाए गए भावनाओं की गूंज थी।
- बर्नियर की भारत में भूमि अधिकारों की आलोचना केवल उनके लिए अद्वितीय नहीं थी, बल्कि यह सोलहवीं और सत्रहवीं शताब्दी के अन्य यात्रियों के खातों में पाए गए भावनाओं की गूंज थी।
पश्चिमी सिद्धांतकारों पर प्रभाव
- बर्नियर के वर्णन, विशेष रूप से उनके भूमि अधिकारों पर विचार, ने पश्चिमी सिद्धांतकारों पर स्थायी प्रभाव डाला।
- मोंटेस्क्यू ने बर्नियर की रिपोर्ट का उपयोग करके पूर्वी तानाशाही की अवधारणा का विकास किया, यह सिद्धांत को मजबूत करते हुए कि एशिया में शासकों के पास पूर्ण अधिकार होता है और निजी संपत्ति का अस्तित्व नहीं होता।
- कार्ल मार्क्स ने बाद में इस पर निर्माण करते हुए एशियाई उत्पादन मोड का विचार प्रस्तुत किया, यह तर्क करते हुए कि उपनिवेश से पहले के भारत में, अधिशेष का अधिग्रहण राज्य द्वारा किया गया, जिससे एक ऐसा समाज बना जो अधीनता और गरीबी से भरा था।
मुगल भारत में सामाजिक और आर्थिक वास्तविकताएं
जबकि बर्नियर का मुग़ल भारत का दृष्टिकोण बिना भेदभाव के जन masses और अत्याचारी शासकों का कड़ा चित्र प्रस्तुत करता है, ऐतिहासिक दस्तावेज, जैसे अबुल फ़ज़ल की रिपोर्ट, एक अलग परिप्रेक्ष्य का सुझाव देते हैं।
- जबकि बर्नियर का मुग़ल भारत का दृष्टिकोण बिना भेदभाव के जन masses और अत्याचारी शासकों का कड़ा चित्र प्रस्तुत करता है, ऐतिहासिक दस्तावेज, जैसे अबुल फ़ज़ल की रिपोर्ट, एक अलग परिप्रेक्ष्य का सुझाव देते हैं।
- यूरोपीय यात्रियों की धारणाओं और मुग़ल आधिकारिक रिकॉर्ड के बीच का अंतर इन चित्रणों की सटीकता पर प्रश्न उठाता है।
- इसके अतिरिक्त, सोलहवीं और सत्रहवीं शताब्दी के दौरान ग्रामीण समाज की जटिलता बर्नियर द्वारा प्रस्तुत सरल दृष्टिकोण को चुनौती देती है।
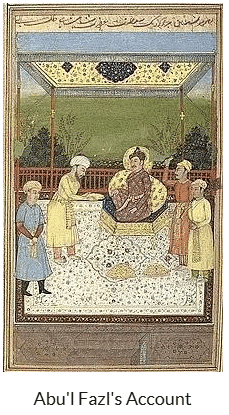
एक अधिक जटिल सामाजिक वास्तविकता
जबकि बर्नियर का मुख्य ध्यान मुग़ल राज्य को अत्याचारी के रूप में प्रस्तुत करने पर था, उसके वर्णन कभी-कभी एक अधिक सूक्ष्म सामाजिक वास्तविकता का सुझाव देते हैं।
कारीगरों और राज्य का अधिग्रहण
- राज्य नियंत्रण की अपनी व्यापक कथा के बावजूद, बर्नियर ने कारीगरों के लिए अपने उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रोत्साहन की कमी को स्वीकार किया क्योंकि राज्य लाभ को अधिग्रहित करता था।
- इससे उत्पादों में गिरावट आई।
- हालांकि, उसने यह भी उल्लेख किया कि भारत ने उत्पादों के निर्यात के माध्यम से कीमती धातुओं की विशाल मात्रा को आकर्षित किया, जो एक समृद्ध व्यापार पहलू को दर्शाता है।
समृद्ध व्यापारी समुदाय
- एकमात्र उत्पीड़ित समाज के चित्र के विपरीत, बर्नियर ने लंबी दूरी के व्यापार में लगे एक समृद्ध व्यापारी समुदाय के अस्तित्व को स्वीकार किया।
लगभग 15 प्रतिशत जनसंख्या सत्रहवीं शताब्दी में शहरों में रहती थी, जो उसी अवधि में पश्चिमी यूरोप की शहरी जनसंख्या से अधिक थी।
मुग़ल शहर: \"कैम्प टाउन\" से परे
बर्नियर ने मुग़ल शहरों का वर्णन \"कैम्प टाउन\" के रूप में किया, यह सुझाव देते हुए कि ये शहर अपने अस्तित्व और जीवित रहने के लिए सम्राट के कैम्प पर निर्भर थे।
- बर्नियर ने मुग़ल शहरों का वर्णन \"कैम्प टाउन\" के रूप में किया, यह सुझाव देते हुए कि ये शहर अपने अस्तित्व और जीवित रहने के लिए सम्राट के कैम्प पर निर्भर थे।
- उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन शहरों में व्यावहारिक सामाजिक और आर्थिक आधारों की कमी थी, और ये केवल सम्राट की सहायता के साथ ही पनपते थे।
- हालाँकि, यह चित्रण मुग़ल साम्राज्य में शहरों की विविधता को अत्यधिक सरल बनाता है।
विविध शहर
- मुग़ल साम्राज्य में शहरों ने विभिन्न उद्देश्यों की सेवा की, जिसमें निर्माण, व्यापार, बंदरगाह, पवित्र केंद्र, और तीर्थ स्थल शामिल थे।
- इनका अस्तित्व व्यापारी समुदायों और पेशेवर वर्गों की समृद्धि को दर्शाता है।
व्यापारी समुदाय और पेशेवर वर्ग
- व्यापारी मुग़ल अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे।
- वे अक्सर मजबूत सामुदायिक या कुल संबंध रखते थे और जाति-व्यवसायिक संगठनों में संगठित होते थे।
- पश्चिमी भारत में, इन समूहों को महाजनों के रूप में जाना जाता था, जिनका नेतृत्व शेठ करते थे।
- शहरी केंद्र जैसे अहमदाबाद में व्यापारियों का एक सामूहिक प्रतिनिधित्व नगरशेठ के माध्यम से होता था।
शहरी समूहों की विविधता
- व्यापारियों के अलावा, शहरी समूहों में विभिन्न पेशेवर वर्ग शामिल थे जैसे कि चिकित्सक (हाकिम या वैद्य), शिक्षक (पंडित या मुल्ला), वकील (वकील), चित्रकार, वास्तुकार, संगीतकार, और कलीग्राफर।
महिलाएं दास, सती और श्रमिक
भारत के उपमहाद्वीप में अपने अनुभवों का दस्तावेजीकरण करने वाले यात्रियों में ज्यादातर पुरुष थे, और उनके खाते महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डालते हैं। ये यात्री अक्सर सामाजिक असमानताओं को एक "प्राकृतिक" स्थिति के रूप में देखते थे और कभी-कभी स्वीकार करते थे।
दासों का उपचार
इब्न बतूता का विवरण
- यात्री इब्न बतूता ने देखा कि दासों को बाजारों में खुलेआम खरीदा और बेचा जाता था, उन्हें वस्तुओं के रूप में देखा जाता था, और उपहार के रूप में आदान-प्रदान किया जाता था। उदाहरण के लिए, उन्होंने सुलतान मुहम्मद बिन तुगलक के लिए उपहार के रूप में घोड़ों और ऊंटों के साथ दास खरीदे। सुलतान ने बदले में उपदेशकों को सिक्के और दास दिए। इब्न बतूता का विवरण यह सुझाव देता है कि दासों के बीच महत्वपूर्ण विभाजन था, कुछ महिला दास सुलतान की सेवा में संगीत और नृत्य की विशेषज्ञ थीं।
दासों का उपयोग
- दासों का मुख्य रूप से घरेलू श्रम के लिए उपयोग किया जाता था, और इब्न बतूता ने पाया कि पालकी या डोला पर व्यक्तियों को ले जाने के लिए उनकी सेवाएं आवश्यक थीं।
- दासों की लागत, खासकर घरेलू श्रम के लिए महिला दासों की, बेहद कम थी। कई परिवार, यदि आर्थिक रूप से सक्षम थे, तो कम से कम एक या दो दास रखते थे।
महिलाओं पर यूरोपीय दृष्टिकोण
महिलाएँ सांस्कृतिक भिन्नता का एक संकेतक
- आधुनिक यूरोपीय यात्रा करने वालों और लेखकों ने अक्सर महिलाओं के प्रति व्यवहार को पश्चिमी और पूर्वी समाजों के बीच एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में रेखांकित किया।
- इस संदर्भ में, फ्रैंकोइस बर्नियर ने सती के प्रचलन पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें उन्होंने इसका विस्तृत विवरण दिया।
- उन्होंने इस प्रथा के प्रति महिलाओं के विभिन्न दृष्टिकोणों को नोट किया, जिसमें कुछ ने स्वेच्छा से मृत्यु को स्वीकार किया और अन्य को मजबूर किया गया।
सती और आगे
- हालांकि बर्नियर ने सती का विस्तार से वर्णन किया, उन्होंने स्वीकार किया कि महिलाओं का जीवन इस प्रथा से परे फैला हुआ था।
- महिलाएँ कृषि और गैर-कृषि उत्पादन दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं।
- व्यापारी परिवारों से आने वाली महिलाएँ व्यापारिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेती थीं, और कुछ मामलों में, उन्होंने व्यापारिक विवादों को अदालत में भी लाया।
- यह इस धारणा को चुनौती देता है कि महिलाएँ केवल अपने घरों के निजी स्थानों तक सीमित थीं।
सारांश
ऐतिहासिक भारत की समृद्ध परंपरा की खोज करते समय विविध यात्रा करने वालों जैसे कि अल-बिरुनी, इब्न बट्टूता, और फ्रैंकोइस बर्नियर के दृष्टिकोण से एक बहुआयामी कथा प्रदर्शित होती है। अल-बिरुनी, जो बौद्धिक जिज्ञासा से प्रेरित थे, भाषाई और सांस्कृतिक बाधाओं को पार करते हुए, अपनी महत्वपूर्ण रचना किताब-उल-हिंद के माध्यम से भारत का एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। इब्न बट्टूता, एक निर्भीक यात्री, ने भारतीय शहरों की जीवंतता को जीवंत किया, 14वीं सदी में व्यापार, संचार, और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के महत्व को उजागर किया। फ्रैंकोइस बर्नियर, एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण के साथ, ने भारत की तुलना यूरोप से की, विशेष रूप से भूमि स्वामित्व पर ध्यान केंद्रित करते हुए, जो स्थायी पश्चिमी धारणाओं में योगदान देता है।
महिलाओं, दासों और सामाजिक जटिलताओं का चित्रण कथा में गहराई जोड़ता है। जबकि यात्रियों ने सामाजिक असमानताओं का अवलोकन किया, उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा निभाई गई सक्रिय भूमिकाओं को भी उजागर किया।
इन अलग-अलग दृष्टिकोणों को एक साथ देखकर हम भारत के अतीत को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यह दिखाता है कि ऐतिहासिक समाजों की जटिलताओं को पूरी तरह से समझने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करना क्यों महत्वपूर्ण है। यह दृष्टिकोण साधारण व्याख्याओं को चुनौती देता है और हमें भारत के समृद्ध और निरंतर बदलते इतिहास की गहराई से सराहना करने में मदद करता है।
|
183 videos|620 docs|193 tests
|















