स्वायत्त राज्यों की नींव | UPSC CSE के लिए इतिहास (History) PDF Download
स्वायत्त राज्यों की नींव: हैदराबाद और कर्नाटिक
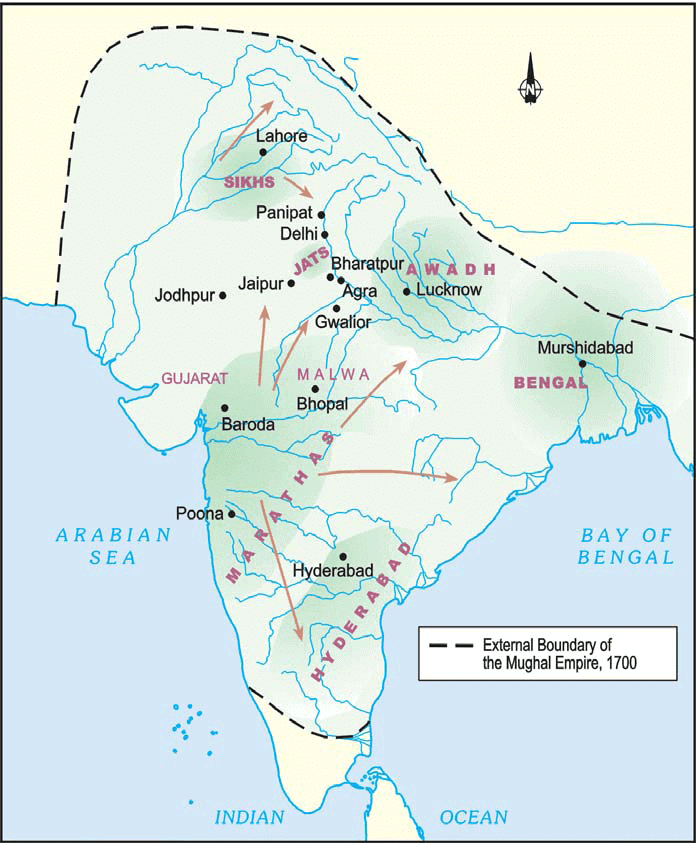
- हैदराबाद राज्य की स्थापना निजाम-उल-मुल्क आसफ जहां (चिन किलिच खान) ने 1724 में की थी।
- वे सम्राट मुहम्मद शाह के वजीर थे।
- निजाम ने सम्राट की लापरवाही से नाराज़ होकर, सरकार को ठीक करने की कोई संभावना न देखकर, डेक्कन में स्वतंत्रता प्राप्त की और हैदराबाद राज्य की स्थापना की।
- कर्नाटिक मुग़ल डेक्कन के एक सूबे में से एक था और इस प्रकार यह हैदराबाद के निजाम के अधीन आया।
- लेकिन कर्नाटिक के उप-राज्यपाल, जिसे नवाब ऑफ कर्नाटिक के रूप में जाना जाता था, ने डेक्कन के वायसराय के नियंत्रण से स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी और अपने पद को वंशानुगत बना लिया।
- इस प्रकार कर्नाटिक के नवाब सआदतुल्ला खान ने अपने भतीजे दोस्त अली को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया, बिना अपने अधीनस्थ निजाम की अनुमति के।
आवध की स्वतंत्रता
- सआदत खान, जो खोरासन से एक फारसी परिवार से आए थे, नवाब-वाईज़िर की लाइन के संस्थापक थे।
- सफदर जंग: “अवध के chiefs एक पल में विघटन उत्पन्न करने में सक्षम थे और डेक्कन के मराठों से अधिक खतरनाक थे।”
- टिपू सुलतान: “मैं उनकी ज़मीन के संसाधनों को बर्बाद कर सकता हूँ, लेकिन मैं समुद्र को सूखा नहीं सकता।”
- टिपू सुलतान: “एक सैनिक की तरह मरना बेहतर है, बजाय इसके कि मैं नास्तिकों पर निर्भरता में जीऊं, उनके पेंशन प्राप्त रजाओं और नवाबों की सूची में।”
- ब्रिटिश निवासी कर्नल पाल्मर: “1800 में नाना फड़नवीस की मृत्यु पर, पूना में remarked: “उनके साथ, मराठा सरकार की सभी बुद्धिमत्ता और संयम विदा हो गए।”
- सिडनी ओवेन: “बासीन की संधि ने कंपनी को भारत का साम्राज्य दिया।”
- पाल्मर: “मैं इसे हर ब्रिटिश नागरिक का कर्तव्य मानता हूँ कि वह अपनी शक्ति के अनुसार सामान्य जानकारी का आकलन करने में योगदान करे।”
- नेपियर: “हमें सिंध पर अधिकार करने का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी हम ऐसा करेंगे, और यह एक बहुत ही लाभकारी, उपयोगी मानव चालाकी होगी। यह मेरे लिए विचार करने का विषय नहीं है कि हम सिंध पर कैसे कब्जा करते हैं, बल्कि इसे अब जो स्थिति है, उसे विचार करना चाहिए।”
- सर व. बटलर: “इस आदमी ने युद्ध के लिए जितनी शिद्दत से लालसा की, उतनी किसी ने नहीं की।”
- कर्नल स्लिमन: “अवध के अधिग्रहण में ब्रिटिश शक्ति को इसके दस राजाओं के मूल्य से अधिक खर्च करना पड़ेगा और यह अनिवार्य रूप से सिपाहियों के विद्रोह का कारण बनेगा।”
- देवेन्द्रनाथ ठाकुर: “अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के कारण हम मूर्ख लोगों की तरह लकड़ी या पत्थर की पूजा नहीं कर सकते, यह सोचकर कि वे भगवान हैं।”
- उन्हें मूल रूप से बियाना का फौजदार नियुक्त किया गया था, लेकिन उन्होंने मुहम्मद शाह के दरबार के कुछ प्रिय राजाओं के साथ झगड़ा किया।
- उन्हें 1722 ई. में अवध के गवर्नर के रूप में भेजा गया।
- 1739 ई. में मृत्यु से पहले, वे वास्तव में स्वतंत्र हो गए थे और प्रांत को एक वंशानुगत संपत्ति बना दिया था।
- उनके बाद उनके भतीजे सफदर जंग ने उनका स्थान लिया, जिन्हें 1748 ई. में साम्राज्य का वजीर नियुक्त किया गया और इसके अतिरिक्त इलाहाबाद का प्रांत भी दिया गया।
- सफदर जंग ने 1754 ई. में अपनी मृत्यु से पहले अवध और इलाहाबाद के लोगों को लंबे समय तक शांति दी।
- सफदर जंग ने लिखा: “अवध के chiefs एक पल में विघटन उत्पन्न करने में सक्षम थे और डेक्कन के मराठों से अधिक खतरनाक थे।”
बंगाल
- औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद, मुरशिद क़ुली ख़ान और अलीवर्दी ख़ान ने बंगाल को वास्तव में स्वतंत्र बना दिया।
- हालाँकि मुरशिद क़ुली ख़ान को 1717 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर बनाया गया था, वह 1700 ईस्वी से इसका प्रभावी शासक रहे थे, जब उन्हें इसका दीवान नियुक्त किया गया था।
- उन्होंने बंगाल को आंतरिक और बाहरी खतरों से मुक्त करके शांति स्थापित की।
- अब बंगाल ज़मींदारों द्वारा विद्रोहों से भी अपेक्षाकृत मुक्त था।
याद रखने योग्य तथ्य
- भील विद्रोह (पश्चिमी घाट): 1817-19, 1825, 1831, 1846 में कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया।
- कोली विद्रोह (भीलों के पड़ोस में): 1829, 1839 और 1844-48 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ।
- कच्छ विद्रोह: 1819 और 1831 में कच्छ के शासक भरमल की बहाली की मांग की।
- वाघेरा विद्रोह (ओखा मंडल का): 1818-19 में विदेशी शासन के खिलाफ।
- सूरत नमक आंदोलन: नमक शुल्क बढ़ाने के खिलाफ। सरकार को इसे वापस लेना पड़ा।
- रामोसी विद्रोह (पश्चिमी घाट की जनजातियाँ): 1822, 1825-28, 1829 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ।
- वहाबी आंदोलन: इस्लाम का एक पुनरुत्थानवादी आंदोलन, जिसका केंद्र पटना था, और जिसका नेतृत्व सैयद अहमद राए बरेली (1786-1831) कर रहे थे।
- उस समय के केवल तीन प्रमुख विद्रोह थे; पहले सिताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मुहम्मद द्वारा, फिर शुजात ख़ान द्वारा और अंत में नजहत ख़ान द्वारा।
- उन्हें पराजित करने के बाद, मुरशिद क़ुली ख़ान ने उनकी ज़मींदारी अपने प्रिय रामजीवन को सौंप दी।
- मुरशिद क़ुली ख़ान का निधन 1727 ईस्वी में हुआ।
- शुजा-उद-दीन, मुरशिद क़ुली का दामाद, ने 1727 में गद्दी पर काबिज होकर 1739 ईस्वी तक बंगाल पर शासन किया।
- 1733 ईस्वी में सम्राट मुहम्मद शाह द्वारा बिहार को बंगाल सुभा में शामिल करने के बाद, शुजा-उद-दीन एक विशाल प्रशासनिक इकाई के सूबेदार बन गए जिसमें बिहार, बंगाल और उड़ीसा शामिल थे।
- 1739 ईस्वी में शुजा-उद-दीन के निधन के बाद, उनके पुत्र सरफराज ने शांति से बंगाल के मसंद पर चढ़ाई की।
- उसी वर्ष, अलीवर्दी ख़ान ने शुजा-उद-दीन के पुत्र सरफराज ख़ान को अपदस्थ और हत्या कर स्वयं नवाब बन गए।
- 1742 से 1751 ईस्वी तक, मराठों ने लगातार आक्रमण किए और अलीवर्दी ख़ान की ज़मीनों को बर्बाद किया।
- अलीवर्दी ख़ान ने मराठों को 12 लाख रुपये की वार्षिक चौथ देने पर सहमति जताई, इस शर्त पर कि वे कभी भी सुवर्णरेखा नदी को पार नहीं करेंगे।
- अलीवर्दी ख़ान ने अंग्रेज़ों और फ़्रांसीसियों को कलकत्ता और चंद्रनगर में अपने कारखाने को मजबूत करने की अनुमति नहीं दी।
- हालाँकि, बंगाल के नवाब एक दृष्टिहीन और लापरवाह तरीके से एक मामले में रहे। उन्होंने 1707 ईस्वी के बाद अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती सैन्य ताकत को दृढ़ता से दबाने का प्रयास नहीं किया।
- अलीवर्दी ख़ान की मृत्यु अप्रैल 1756 में हुई, और उनके पोते मिर्ज़ा मुहम्मद, जिन्हें सराज-उद-दौला के नाम से जाना जाता है, ने गद्दी संभाली।
मैसूर
मैसूर का राज्य अपने अस्थिर स्वतंत्रता को बनाए रखने में सफल रहा, जब से विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में दो मंत्रियों नंजाराज और देवराज ने मैसूर में सत्ता पर कब्जा कर लिया। हैदर अली ने मैसूर सेना में एक छोटे अधिकारी के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उसने मौके का सही उपयोग करते हुए धीरे-धीरे मैसूर सेना में ऊंची पदवी हासिल की। उसने जल्द ही पश्चिमी सैन्य प्रशिक्षण के लाभों को पहचाना और इसे अपनी कमान के तहत सैनिकों पर लागू किया।
- मैसूर का राज्य अपने अस्थिर स्वतंत्रता को बनाए रखने में सफल रहा, जब से विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ।
- 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में दो मंत्रियों नंजाराज और देवराज ने मैसूर में सत्ता पर कब्जा कर लिया।
- हैदर अली ने मैसूर सेना में एक छोटे अधिकारी के रूप में अपने करियर की शुरुआत की।
- उसने मौके का सही उपयोग करते हुए धीरे-धीरे मैसूर सेना में ऊंची पदवी हासिल की।
- उसने जल्द ही पश्चिमी सैन्य प्रशिक्षण के लाभों को पहचाना और इसे अपनी कमान के तहत सैनिकों पर लागू किया।
याद रखने योग्य तथ्य
- मीर जाफर को कुष्ठ रोग था।
- बंगाल के बाद, अंग्रेजों ने अवध के नवाब के क्षेत्र में बिना शुल्क के व्यापार के अधिकारों को सुरक्षित किया।
- वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल सरकार के पहले गवर्नर-जनरल थे।
- बक्सर की लड़ाई की पूर्व संध्या पर, शुजा-उद-दौला ने नवाब मीर कासिम को गिरफ्तार किया क्योंकि कासिम ने अवध की सेना के रखरखाव के लिए भुगतान से बचा लिया।
- बक्सर की लड़ाई में, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला ने मीर कासिम के साथ उस शर्त पर शामिल हुए कि मीर कासिम शुजा की सेना के खर्चों को वहन करेगा और दूसरे, वह अपनी बहाली के बाद बिहार प्रांत को अवध को सौंप देगा।
- शाह आलम II द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का सम्राटीय अनुदान कंपनी के बंगाल पर नियंत्रण को वैध करता है।
- क्लाइव की सेवाओं की सहेजने के लिए मीर जाफर ने शाह आलम II से उन्हें ओमरा का शीर्षक और 24 परगना की ज़मींदारी प्राप्त की।
- 1760 में बंगाल की क्रांति का अर्थ मीर जाफर का अपदस्थ होना और मीर कासिम का बंगाल के नवाब के रूप में आसीन होना है।
- हैदराबाद के निजाम ने 1763 में अंग्रेजों द्वारा पराजित होने के बाद मीर कासिम द्वारा बनाए गए गठबंधन में भाग नहीं लिया।
- मीर कासिम ने कंपनी के सेवकों द्वारा 1717 के फार्मान के दुरुपयोग को रोकने का प्रयास किया।
- मीर जाफर ने चिनसुरा में डच के साथ एक साजिश रची।
- मीर जाफर को 'कर्नल क्लाइव का गीदड़' के नाम से जाना जाता है।
- मीर जाफर को बंगाल के सिंहासन पर स्थापित करने के लिए एक साजिश तैयार की गई।
- अमिचंद को चुप कराने के लिए क्लाइव ने उनके मांगों को स्वीकार करने वाले समझौते की एक नकल तैयार की।
याद रखने योग्य तथ्य
- बक्सर की लड़ाई की पूर्व संध्या पर, शुजा-उद-दौला ने नवाब मीर कासिम को गिरफ्तार किया क्योंकि कासिम ने अवध की सेना के रखरखाव के लिए भुगतान से बचा लिया।
- उन्होंने 1755 में डिंडिगल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया।
- 1761 में उन्होंने नंजाराज को अपदस्थ कर दिया और मैसूर राज्य पर अपनी सत्ता स्थापित की।
- अपनी शक्ति की स्थापना के आरंभ से ही, वह मराठा सरदारों, निजाम और ब्रिटिशों के साथ युद्ध में लगे रहे।
- 1769 में, उन्होंने बार-बार ब्रिटिश बलों को हराया और मद्रास के निकटवर्ती क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया।
- वह 1782 ईस्वी में दूसरे एंग्लो-मिसोर युद्ध के दौरान मृत हो गए।
- उनके बाद टिपू सुलतान ने शासन किया, जो 1799 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक मैसूर का शासन करते रहे।
- वह एक सक्षम प्रशासक और एक सैन्य प्रतिभा थे।
- उनकी पैदल सेना यूरोपीय शैली में मस्कट और बायोनट से सुसज्जित थी।
- उन्होंने 1796 के बाद एक नौसेना बनाने का प्रयास भी किया।
- इस उद्देश्य के लिए उन्होंने दो डॉकीयार्ड स्थापित किए, जिनके मॉडल के जहाज सुलतान द्वारा स्वयं प्रदान किए गए।
- समय के साथ बदलने की उनकी इच्छा नए कैलेंडर, नए मुद्रा प्रणाली, और नए वजन और माप के पैमाने की शुरुआत में प्रतीकित हुई।
- उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति में गहरी रुचि दिखाई।
- उन्होंने सृंगपत्नम में एक स्वतंत्रता का पेड़ लगाया और एक जैकोबियन क्लब के सदस्य बने।
- उन्होंने जमींदारी देने की परंपरा को समाप्त करने की कोशिश की।
- उन्होंने पोलिगारों की पारंपरिक संपत्तियों को कम करने का प्रयास भी किया।
- उनका भूमि राजस्व कुल उत्पादन का 1/3 तक बढ़ गया।
पंजाब
- सिख धर्म का जन्म उसी समय हुआ जब भारत में मुग़ल शासन स्थापित हुआ। इसे समाज के रोगों को दूर करने, भक्ति संप्रदाय को बढ़ावा देने और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एकता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संगठित किया गया।
- अपने प्रारंभिक चरण में, सिख धर्म एक शांतिपूर्ण भक्ति और सेवा का विश्वास बना रहा। यह गुरु अर्जन देव के मार्गदर्शन में परिवर्तन के दौर से गुज़रा, जिन्होंने अपने अनुयायियों को मुग़ल साम्राज्य के भीतर आत्म-शासन की स्थापना का विचार दिया।
- गुरु अर्जन देव के शहीदी के बाद सिखों पर हुए अत्याचारों की धारा ने सिखों के दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल दिया।
- उन्होंने गुरु के मार्गदर्शन में मुग़ल अधिकारियों के अत्याचार का सक्रिय रूप से विरोध किया।
याद रखने योग्य तथ्य
- सन्यासी विद्रोह: अंग्रेज़ कंपनी द्वारा पवित्र स्थलों पर जाने पर लगाए गए प्रतिबंधों के खिलाफ सन्यासियों का विद्रोह।
- कोल विद्रोह: छोटानागपुर के कोल बाहरी लोगों को ज़मीन के हस्तांतरण के खिलाफ थे और 1831 में लगभग एक हजार बाहरी लोगों को मार दिया या जला दिया।
- संथाल विद्रोह: संथालों ने, सिद्धू और कन्हू के नेतृत्व में, 1855 में राजस्व अधिकारियों, पुलिस, जमींदारों और साहूकारों के बुरे व्यवहार के खिलाफ विद्रोह किया।
- आहोम का विद्रोह: आहोमों ने गोमधार कोंवर के तहत 1928 में असम में आहोम क्षेत्र को शामिल करने के अंग्रेज़ों के प्रयास के खिलाफ विद्रोह किया।
- खासी विद्रोह: नंक्लो का शासक कंपनी द्वारा जैंतिया और गारो के अधिग्रहण के खिलाफ था। इसे 1833 में दबा दिया गया।
- पागल पंथियों और फराजियों का विद्रोह: ज़मींदारों के अत्याचारों के खिलाफ टिपू (बंगाल) के तहत, केरण सिंह के पुत्र। फराजियों, एक मुस्लिम संप्रदाय के अनुयायी, ने किरायेदारों के अधिकारों का समर्थन किया।
गोबिंद सिंह और बांदा बहादुर
- बांदा बहादुर के बाद, उन्होंने कई लूटमार समूहों में विभाजित हो गए और गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई।
- 1745 में, उन्होंने 65 घूमते हुए समूहों में संगठित किया।
- बाद में 1748 में, नवाब कपूर सिंह के अनुरोध पर, समूहों का विलय दाल खालसा में किया गया।
- दाल खालसा की कमान जस्सा सिंह अहलुवालिया के अधीन थी।
- दाल खालसा को 12 विभागों में विभाजित किया गया, जो लोकतांत्रिक स्वभाव के थे।
- कुछ समय बाद, उन्हें मिस्ल के रूप में जाना जाने लगा। 'मिस्ल' एक अरबी शब्द है। इसका अर्थ है 'समान' या 'एक जैसा'।
बारह मिस्ल इस प्रकार हैं:
मिस्ल का नाम | संस्थापक नेता का नाम
- सिंहपुरिया मिस्ल: नवाब कपूर सिंह
- अहलुवालिया मिस्ल: जस्सा सिंह अहलुवालिया
- रामगढ़िया जस्सा सिंह मिस्ल: रामगढ़िया
- फुलकिया फुल सिंह मिस्ल:
- कन्हैया मिस्ल: जय सिंह
- भागी मिस्ल: हरि सिंह
- सुखर्चकिया मिस्ल: चरात सिंह
- निशानवालिया मिस्ल: सरदार संगत सिंह
- करोर सिंगिया भागेल सिंह मिस्ल:
- दल्लेवालिया गुलाब सिंह मिस्ल:
- नकई मिस्ल: हीरा सिंह
- शहीदी मिस्ल: बाबा दीप सिंह
प्रत्येक मिस्ल का अपना प्रमुख होता था, जो अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से शासन करता था। जब मिस्लदार एक साथ कार्य करते थे, तो वे लूट का बंटवारा करते थे।
- रिटेनर को अपने मिस्ल के प्रमुख या किसी अन्य प्रमुख की सेवा करने में पूरी स्वतंत्रता थी।
- रिटेनर को कोई वेतन नहीं मिलता था। वे सैन्य सेवा देने की शर्त पर भूमि रखते थे।
पंचायत प्रणाली
गाँव ने प्रशासनिक इकाई का गठन किया। इसके पास अपनी स्वयं की पंचायत थी जो अपने मामलों का प्रबंधन करती थी, विवादों का निपटारा करती थी और आपात स्थिति में सुरक्षा की व्यवस्था करती थी। गाँव के कार्यकारी थे: मुखिया, लेखाकार और चौकीदार।
राजस्व
आय के स्रोत थे:
- भूमि राजस्व
- लूट
- व्यापार पर कर
- भारी जुर्माना
भूमि राजस्व के उद्देश्यों के लिए, गाँवों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया:
- (i) मुखिया के क्षेत्र में गाँव।
- (ii) राखी प्रणाली के अंतर्गत गाँव।
भूमि राजस्व को कृत्रिम रूप से सिंचित भूमि के उत्पादन का 1/5 और वर्षा की भूमि के उत्पादन का 1/4 के दर से एकत्र किया गया। इसे दो छह-महीने की किस्तों में वस्तु और नकद में एकत्र किया गया। राखी प्रणाली के अंतर्गत गाँवों ने किराए या सरकारी हिस्से का 1/5 से 1/2 तक का भुगतान किया। यह कर मराठों के चतुर्थक के समान था।
दान
- अतिथियों और अधिकारियों के मनोरंजन से संबंधित खर्चों को वहन करने के लिए 'आया गया' नामक एक कर लगाया गया।
न्याय
- न्याय वितरित करने के लिए कोई विस्तृत न्यायिक प्रणाली नहीं थी। नागरिक मामले स्थानीय पंचायतों द्वारा निपटाए जाते थे, हालांकि उन्हें मुखिया के पास भी ले जाया जा सकता था।
- अपराध के मामले मुखिया और उनके अधिकारियों द्वारा तय किए जाते थे। दंड कड़े थे और यह अपराध की प्रकृति के अनुसार भिन्न होते थे। अंग-भंग और मृत्युदंड दुर्लभ मामलों में दिए जाते थे। 'शुक्राना' और 'जुर्माना' भी वसूल किए जाते थे।
भूमि संबंध
- भूमि संबंध की निम्नलिखित चार प्रणालियाँ प्रचलित थीं:
(i) पट्टेदारी, (ii) मिस्लदारी, (iii) तबेदारी, और (iv) जागीरदारी।
- ‘सरदार’ की रैंक से नीचे के सभी सदस्यों ने भूमि को ‘पाटीदार’ के रूप में रखा। वे अपनी भूमि के प्रबंधन में स्वतंत्र थे।
- कुछ छोटे सरदार जिन्होंने मिस्ल की मदद की, उन्हें मिस्लदारी प्रणाली के तहत भूमि मिली। यदि किसी मिस्लदार को मिस्ल के प्रमुख द्वारा दी गई सेवा से संतोष नहीं था, तो वह समान अधिकारों के साथ किसी और प्रमुख के क्षेत्र में जा सकता था।
- इस प्रणाली के तहत, रिटेनर्स ने भूमि को धारण किया, जिसे वापस लिया जा सकता था यदि प्रमुख उनके कार्य या आचरण से संतुष्ट नहीं था।
- इसने जमींदारों को वंशानुगत अधिकार दिया। जमींदार आमतौर पर सरदारों के निकट संबंधी और आश्रित होते थे। उन्हें प्रमुख के लिए सैन्य सेवा प्रदान करनी होती थी।
|
198 videos|620 docs|193 tests
|















