स्पेक्ट्रम सारांश: विश्व युद्ध II के बाद राष्ट्रीयवादी प्रतिक्रिया | UPSC CSE के लिए इतिहास (History) PDF Download
➢ कांग्रेस संघर्ष के तरीके पर संकट
- कांग्रेस में जाली सदस्यता और कांग्रेस समितियों में प्रवेश पाने के लिए अनैतिक साधनों का उपयोग करने के मुद्दे थे।
- गांधी का दृढ़ विश्वास था कि कांग्रेस को आंदोलन फिर से शुरू करने से पहले अपना कामकाज ठीक करना चाहिए; इसके अलावा, उन्होंने यह भी महसूस किया कि जनता संघर्ष के लिए तैयार नहीं है।
- कुछ अन्य लोग थे जो मानते थे कि संघर्ष जारी रहना चाहिए।
➢ हरिपुरा और त्रिपुरी सत्र: सुभाष चंद्र बोस के विचार
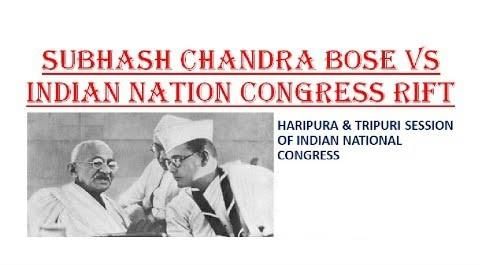
- सुभाष चंद्र बोस बंगाल प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष थे। उनके मुख्य कार्य का क्षेत्र युवा संगठन और व्यापार संघ आंदोलन को बढ़ावा देना था।
- सुभाष बोस ने स्वतंत्रता के संघर्ष के कई पहलुओं पर गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं से असहमत थे।
- उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया, जिसमें भारत के लिए डोमिनियन स्थिति की बात की गई थी।
- बोस पूर्ण स्वतंत्रता के पक्ष में थे; उन्होंने स्वतंत्रता लीग के गठन की भी घोषणा की।
- जब लाहौर कांग्रेस सत्र ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह संकल्प पारित किया कि कांग्रेस का लक्ष्य 'पूर्ण स्वराज' होगा, तो बोस ने इस निर्णय का पूर्ण समर्थन किया।
- फरवरी 1938 में हरिपुरा, गुजरात में कांग्रेस की बैठक में, बोस को सत्र का अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुना गया।
- उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि प्रांतों में कांग्रेस मंत्रालयों में विशाल क्रांतिकारी क्षमता है।
- बोस ने योजना के माध्यम से देश के आर्थिक विकास की बात की और बाद में एक राष्ट्रीय योजना समिति के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- सत्र ने एक संकल्प पारित किया कि कांग्रेस उन लोगों को नैतिक समर्थन देगी जो राजकीय राज्यों में शासन के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे।
➢ 1939: सुभाष जीतते हैं लेकिन कांग्रेस आंतरिक संघर्ष का सामना करती है
➢ जनवरी 1939 में, सुभाष बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए फिर से खड़े होने का निर्णय लिया। गांधी बोस की उम्मीदवारी से खुश नहीं थे। सुभाष बोस ने चुनाव 1580 वोटों के साथ 1377 के मुकाबले जीता, उन्हें कांग्रेस का पूरा समर्थन मिला।
➢ त्रिपुरी
- मार्च 1939 में कांग्रेस का सत्र त्रिपुरी, मध्य प्रांत (वर्तमान मध्य प्रदेश में जबलपुर के निकट) में हुआ। कार्यकारी समिति, जो कांग्रेस का शासकीय निकाय है, का चुनाव नहीं होता, बल्कि इसे अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है; इस प्रकार अध्यक्ष का चुनाव एक संवैधानिक अवसर होता है जिसके माध्यम से सदस्य कांग्रेस के नेतृत्व की प्रकृति को व्यक्त करते हैं।
- गोविंद बल्लभ पंत द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसमें गांधीवादी नीतियों पर विश्वास व्यक्त करते हुए बोस से कहा गया कि वे कार्यकारी समिति का गठन गांधीजी की इच्छाओं के अनुसार करें, और यह प्रस्ताव समाजवादियों या कम्युनिस्टों के विरोध के बिना पारित हुआ।
- गांधी एक ऐसे कांग्रेस संघर्ष का नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं थे जो बोस द्वारा पसंद किए गए कट्टरपंथी रुख पर आधारित था, जबकि बोस अपने विचारों पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने गांधी के नेतृत्व में एक एकीकृत कांग्रेस को प्राथमिकता दी, क्योंकि राष्ट्रीय संघर्ष अत्यधिक महत्वपूर्ण था।
- सुभाष बोस ने अप्रैल 1939 में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया।
➢ गांधी और बोस: वैचारिक मतभेद
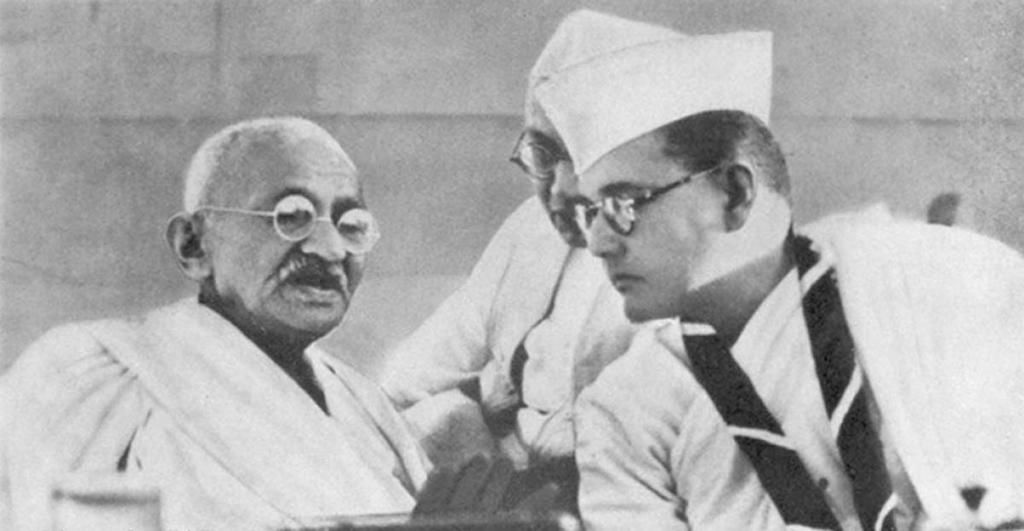
- अहिंसा बनाम सैन्यवादी दृष्टिकोण: गांधी अहिंसा और सत्याग्रह में दृढ़ विश्वास रखते थे, जो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का गैर-violent तरीका है। बोस का मानना था कि गांधी की अहिंसा आधारित रणनीति भारत की स्वतंत्रता के लिए अपर्याप्त होगी।
- उद्देश्य और साधन: बोस क्रिया के परिणाम पर ध्यान केंद्रित करते थे। गांधी का मानना था कि उनकी प्रायोजित गैर-violent विरोध की विधि तभी लागू हो सकती है जब साधन और उद्देश्य समान रूप से अच्छे हों।
- शासन का स्वरूप: बोस ने विचार किया कि प्रारंभ में, एक लोकतांत्रिक प्रणाली राष्ट्र पुनर्निर्माण और गरीबी तथा सामाजिक असमानता के उन्मूलन के लिए अपर्याप्त होगी। गांधी के शासन पर विचार "हिंद स्वराज" (1909) में मिलते हैं, जो "राजनीतिक सिद्धांत का एक स्थायी कार्य" प्रस्तुत करने का उनका निकटतम प्रयास था।
- सैन्यीकरण: सुभाष बोस सैन्य अनुशासन की ओर गहराई से आकर्षित थे और भारतीय रक्षा बल की विश्वविद्यालय इकाई में मिले मूल प्रशिक्षण के लिए आभारी थे।
- आर्थिक विचार: गांधी का "स्वराज" का अर्थव्यवस्था के अपने विशेष दृष्टिकोण के साथ था। वे राज्य नियंत्रण के बिना एक विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था चाहते थे। बोस ने आर्थिक स्वतंत्रता को सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का सार माना।
- धर्म: गांधी मुख्यतः एक धार्मिक व्यक्ति थे। सत्य और अहिंसा वे दो सिद्धांत थे जिन्होंने उन्हें धर्म का एक व्यापक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद की। सुभाष बोस उपनिशदों की शिक्षाओं पर विश्वास करते थे।
- जाति और अछूतत्व: गांधी के समाज के लिए मुख्य लक्ष्य तीन थे: अछूतत्व का उन्मूलन, जाति व्यवस्था के वर्ण भेदों को बनाए रखना, और भारत में सहिष्णुता, विनम्रता, और धार्मिकता को मजबूत करना। बोस ने एक समाज की कल्पना की जो सामाजिक पदानुक्रम को समाप्त कर देगी।
- महिलाएं: गांधी के शब्दों में, "महिलाओं को कमजोर लिंग कहना एक कलंक है; यह पुरुषों का महिलाओं के प्रति अन्याय है।" सुभाष बोस का महिलाओं के प्रति एक मजबूत दृष्टिकोण था। उन्होंने महिलाओं को पुरुषों के समान माना और उन्हें भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने और बलिदान देने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। 1943 में, उन्होंने महिलाओं से भारतीय राष्ट्रीय सेना में सैनिक के रूप में सेवा देने का आग्रह किया।
- शिक्षा: गांधी अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के खिलाफ थे और अंग्रेजी को शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयोग करने के खिलाफ थे। वे चाहते थे कि शिक्षा स्थानीय भाषा में हो। उन्होंने 7 से 14 वर्ष के सभी लड़कों और लड़कियों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की वकालत की।
➢ द्वितीय विश्व युद्ध और राष्ट्रीय प्रतिक्रिया

1 सितंबर, 1939 को, जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया - यह क्रिया दूसरे विश्व युद्ध का कारण बनी। 3 सितंबर, 1939 को, ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की।
➢ कांग्रेस का वायसराय को प्रस्ताव
- भारत का युद्ध प्रयास में सहयोग देने का प्रस्ताव दो मुख्य शर्तों पर आधारित था:
- युद्ध के बाद, एक संविधान सभा का आयोजन किया जाना चाहिए जो स्वतंत्र भारत की राजनीतिक संरचना को निर्धारित करे।
- तत्काल, केंद्र में एक वास्तविक जिम्मेदार सरकार का गठन किया जाना चाहिए।
- यह प्रस्ताव वायसराय लिनलिथगो द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया।
➢ वार्धा में CWC की बैठक
- कांग्रेस की आधिकारिक स्थिति का पालन वार्धा सत्र में कांग्रेस कार्य समिति (CWC) द्वारा किया गया।
- गांधी, जिन्होंने इस युद्ध में ब्रिटेन के प्रति पूरी सहानुभूति रखी, क्योंकि उन्हें फासीवादी विचारधारा से नफरत थी, ने सहयोगी शक्तियों का बिना शर्त समर्थन करने की वकालत की।
- सुभाष बोस और अन्य समाजवादियों के अनुसार, युद्ध दोनों पक्षों द्वारा साम्राज्यवादियों द्वारा लड़ा जा रहा था; प्रत्येक पक्ष अपने उपनिवेशीय संपत्तियों की रक्षा करना चाहता था और अधिक क्षेत्रों पर कब्जा करना चाहता था, इसलिए राष्ट्रीयतावादियों को किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करना चाहिए।
- जवाहरलाल नेहरू गांधी या समाजवादियों की राय स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे।
- CWC प्रस्ताव ने फासीवादी आक्रमण की निंदा की। इसमें कहा गया कि भारत एक ऐसे युद्ध का पक्ष नहीं ले सकता, जो लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के लिए लड़ा जा रहा है, जबकि वह स्वतंत्रता भारत को अस्वीकृत की जा रही है;
- यदि ब्रिटेन लोकतंत्र और स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है, तो इसे अपने उपनिवेशों में साम्राज्यवाद समाप्त करके और भारत में पूर्ण लोकतंत्र स्थापित करके साबित करना चाहिए;
- सरकार को जल्द से जल्द अपने युद्ध के उद्देश्यों की घोषणा करनी चाहिए और यह भी बताना चाहिए कि युद्ध के बाद भारत में लोकतंत्र के सिद्धांतों को कैसे लागू किया जाएगा।
➢ सरकार का रुख और कांग्रेस मंत्रियों का इस्तीफा
- वायसराय लिंलिथगो ने 17 अक्टूबर, 1939 को दिए गए अपने बयान में कांग्रेस के खिलाफ मुस्लिम लीग और राजाओं का उपयोग करने का प्रयास किया। सरकार ने (i) ब्रिटिश युद्ध के लक्ष्यों को परिभाषित करने से इनकार कर दिया, केवल यह कहकर कि ब्रिटेन आक्रमण का प्रतिरोध कर रहा है; (ii) कहा कि वह भविष्य की व्यवस्था के तहत \"भारत में कई समुदायों, पार्टियों और हितों के प्रतिनिधियों, और भारतीय राजाओं\" से परामर्श करेगी कि 1935 का अधिनियम कैसे संशोधित किया जा सकता है; (iii) कहा कि वह तुरंत एक \"सलाहकार समिति\" स्थापित करेगी, जिसकी सलाह आवश्यक होने पर ली जा सकेगी।
- सरकार का छिपा हुआ एजेंडा: लिंलिथगो का बयान कोई अपवाद नहीं था, बल्कि सामान्य ब्रिटिश नीति का एक हिस्सा था—\"युद्ध का लाभ उठाकर कांग्रेस से खोया हुआ मैदान वापस पाना।\" मई 1940 में, एक शीर्ष-गुप्त क्रांतिकारी आंदोलन अध्यादेश तैयार किया गया था, जिसका उद्देश्य कांग्रेस पर प्रहार करना था।
- कांग्रेस मंत्रालयों का इस्तीफा देने का निर्णय: 23 अक्टूबर, 1939 को CWC की बैठक में (i) वायसराय के बयान को पुराने साम्राज्यवादी नीति का पुनरुत्थान मानकर अस्वीकार किया; (ii) युद्ध का समर्थन न करने का निर्णय लिया; और (iii) प्रांतों में कांग्रेस मंत्रालयों से इस्तीफा देने का आह्वान किया।
- तत्काल जन सत्याग्रह पर बहस: गांधी और उनके समर्थक तत्काल संघर्ष के पक्ष में नहीं थे क्योंकि उन्हें लगा कि (i) मित्र देशों का कारण न्यायपूर्ण था; साम्प्रदायिक संवेदनशीलता और हिंदू-मुस्लिम एकता की कमी साम्प्रदायिक दंगों का कारण बन सकती है; (ii) कांग्रेस संगठन बिखराव में था और वातावरण जन संघर्ष के लिए अनुकूल नहीं था; और (iii) masses संघर्ष के लिए तैयार नहीं थे। कांग्रेस का रामगढ़ सत्र मार्च 1940 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हुआ। सभी ने सहमति जताई कि एक लड़ाई लड़ी जानी चाहिए, लेकिन रूप पर असहमति थी।
- पाकिस्तान प्रस्ताव: लाहौर (मार्च 1940) - मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि \"भौगोलिक रूप से सटे क्षेत्रों में जहाँ मुसलमानों की संख्या अधिक है (उत्तर पश्चिम, पूर्व) को स्वतंत्र राज्यों में समूहित किया जाए।\"
➢ अगस्त प्रस्ताव

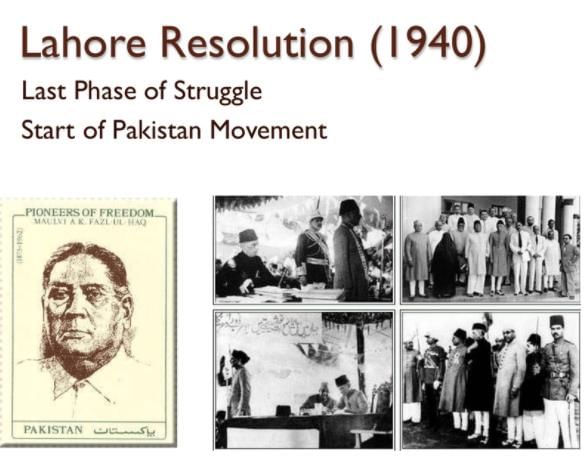
- लिनलिथगो ने अगस्त ऑफर (अगस्त 1940) की घोषणा की, जिसमें प्रस्तावित था:
- (i) भारत के लिए डोमिनियन स्थिति को उद्देश्य के रूप में रखना;
- (ii) वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार, जिसमें भारतीयों की बहुमत होगी;
- (iii) युद्ध के बाद एक संविधान सभा का गठन करना, जहाँ मुख्य रूप से भारतीय संविधान को उनके सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक धारणाओं के अनुसार निर्धारित करेंगे, जब कि सरकार की रक्षा, अल्पसंख्यक अधिकार, राज्यों के साथ संधियाँ, सभी भारतीय सेवाओं के संबंध में दायित्वों की पूर्ति की शर्तों के अधीन;
- (iv) भविष्य का कोई भी संविधान अल्पसंख्यकों की सहमति के बिना अपनाया नहीं जाएगा।
- प्रतिक्रियाएँ: कांग्रेस ने अगस्त ऑफर को अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने लीग को दिए गए वीटो आश्वासन का स्वागत किया।
- मूल्यांकन: जुलाई 1941 में, वायसराय की कार्यकारी परिषद को इस बार भारतीयों को 12 में से 8 की बहुमत देने के लिए विस्तारित किया गया, लेकिन ब्रिटिश रक्षा, वित्त, और गृह के प्रभारी बने रहे।
➢ व्यक्तिगत सत्याग्रह
- सरकार ने अडिग स्थिति अपनाई कि जब तक कांग्रेस मुस्लिम नेताओं के साथ एक समझौते पर नहीं पहुँचती, तब तक कोई संवैधानिक प्रगति नहीं की जा सकती। इसने बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठनों के अधिकार को छीनने वाले आदेश जारी किए।
- व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने के उद्देश्य थे—
- (i) यह दिखाना कि राष्ट्रीयता की धैर्यता कमजोरी के कारण नहीं थी;
- (ii) लोगों की भावना व्यक्त करना कि वे युद्ध में रुचि नहीं रखते और नाज़ीवाद और भारत को शासित करने वाली दोहरी तानाशाही के बीच कोई भेद नहीं करते;
- (iii) सरकार को कांग्रेस की मांगों को शांति से स्वीकार करने का एक और अवसर देना।
- यदि सरकार सत्याग्रहियों को गिरफ्तार नहीं करती, तो वे न केवल इसे दोहराएंगे, बल्कि गांवों में जाकर दिल्ली की ओर मार्च शुरू करेंगे, जिससे \"दिल्ली चलो आंदोलन\" शुरू होगा।
- विनोबा भावे ने सत्याग्रह की पेशकश की और नेहरू दूसरे थे। मई 1941 तक, 25,000 लोगों को व्यक्तिगत नागरिक अवज्ञा के लिए दोषी ठहराया जा चुका था।
➢ गांधी ने नेहरू को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया
- सीडब्ल्यूसी ने गांधी और नेहरू के आपत्तियों को दरकिनार करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि भारत की रक्षा में सरकार के साथ सहयोग करने की पेशकश की जाए, यदि (i) युद्ध के बाद पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है, और (ii) शक्ति का सार तुरंत स्थानांतरित किया जाता है।
- नेहरू और गांधी के स्वभाव और आधुनिकता, धर्म, भगवान, राज्य और औद्योगिकीकरण के प्रति दृष्टिकोण में मतभेद थे। इतने सारे मतभेदों के बावजूद, नेहरू ने गांधी की पूजा की, और गांधी ने नेहरू पर अपने स्वयं के बेटों से अधिक विश्वास किया।
➢ शिक्षक और शिष्य में मौलिक समानताएँ थीं
स्वदेशभक्ति का एक समावेशी अर्थ है, अर्थात्, उन्होंने भारत को एक संपूर्ण देश के रूप में पहचाना, न कि किसी विशेष जाति, भाषा, क्षेत्र, या धर्म के रूप में। दोनों ने अहिंसा और एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में विश्वास किया। राजमोहन गांधी अपनी पुस्तक द गुड बोटमैन में लिखते हैं कि गांधी ने नेहरू को अन्य विकल्पों पर प्राथमिकता दी क्योंकि उन्होंने महात्मा द्वारा प्रस्तुत भारत के बहुवादी, समावेशी विचार को सबसे विश्वसनीय रूप से व्यक्त किया।
➢ क्रिप्स मिशन
- मार्च 1942 में, स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत भेजा गया, जिसका उद्देश्य भारत से युद्ध के लिए सहयोग प्राप्त करने हेतु संवैधानिक प्रस्ताव प्रस्तुत करना था।
➢ क्रिप्स मिशन क्यों भेजा गया
- दक्षिण-पूर्व एशिया में ब्रिटेन को हुई हार के कारण, भारत पर जापानी आक्रमण का खतरा अब वास्तविक प्रतीत हो रहा था, और भारतीय समर्थन महत्वपूर्ण हो गया।
- सहयोगी (USA, USSR, चीन) देशों ने भारत से सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटेन पर दबाव डाला।
- भारतीय राष्ट्रवादियों ने सहमति व्यक्त की थी कि यदि महत्वपूर्ण शक्ति तुरंत स्थानांतरित की जाती है और युद्ध के बाद पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है तो वे सहयोगी कारण का समर्थन करेंगे।
➢ मुख्य प्रस्ताव: मिशन के मुख्य प्रस्ताव इस प्रकार थे।
- एक भारतीय संघ डोमिनियन स्थिति के साथ स्थापित किया जाएगा; इसे कॉमनवेल्थ के साथ अपने संबंधों का निर्णय लेने और संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों में भाग लेने की स्वतंत्रता होगी।
- युद्ध के अंत के बाद, एक संविधान सभा बुलाई जाएगी जो नया संविधान बनाएगी। इस सभा के सदस्य आंशिक रूप से प्रांतीयassemblies द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से चुने जाएंगे और आंशिक रूप से राजाओं द्वारा नामित किए जाएंगे।
- ब्रिटिश सरकार नए संविधान को दो शर्तों के अधीन स्वीकार करेगी: कोई भी प्रांत जो संघ में शामिल होने के लिए इच्छुक नहीं है, उसके पास एक अलग संविधान और एक अलग संघ बनाने का विकल्प होगा, और नया संविधान निर्माण निकाय और ब्रिटिश सरकार शक्ति हस्तांतरण और जातीय एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए एक संधि पर बातचीत करेंगे।
- इस बीच, भारत की रक्षा ब्रिटिश हाथों में बनी रहेगी, और गवर्नर-जनरल की शक्तियाँ बनी रहेंगी।
➢ भूतकाल से प्रस्थान और परिणाम
- प्रस्तावों में कई दृष्टिकोणों से पहले के प्रस्तावों से भिन्नता थी—संविधान का निर्माण अब केवल भारतीयों के हाथ में होना था और न कि 'मुख्यतः' भारतीयों के हाथ में (जैसा कि अगस्त प्रस्ताव में कहा गया था)।
- संविधान सभा के लिए एक ठोस योजना प्रस्तुत की गई थी।
- किसी भी प्रांत को अलग संविधान बनाने का विकल्प उपलब्ध था, जो भारत के विभाजन के लिए एक खाका था।
- स्वतंत्र भारत ने कॉमनवेल्थ से बाहर निकलने का अधिकार रखा।
- भारतीयों को अंतरिम अवधि में प्रशासन में एक बड़ा हिस्सा लेने की अनुमति दी गई।
क्रिप्स मिशन के विफल होने के कारण
विभिन्न पार्टियों और समूहों ने विभिन्न बिंदुओं पर प्रस्तावों पर आपत्ति जताई।
➢ कांग्रेस ने निम्नलिखित पर आपत्ति जताई:
- पूर्ण स्वतंत्रता के प्रावधान के बजाय डोमिनियन स्थिति का प्रस्ताव;
- राज्य के प्रतिनिधित्व के लिए नामांकित व्यक्तियों द्वारा और न कि निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा;
- प्रांतों को अलग होने का अधिकार, क्योंकि यह राष्ट्रीय एकता के सिद्धांत के खिलाफ था;
- शक्ति के तत्काल हस्तांतरण के लिए किसी योजना का अभाव और रक्षा में वास्तविक हिस्सेदारी का अभाव;
- गवर्नर-जनरल की सर्वोच्चता को बनाए रखा गया था, और यह मांग कि गवर्नर-जनरल केवल संवैधानिक प्रमुख हैं, को स्वीकार नहीं किया गया।
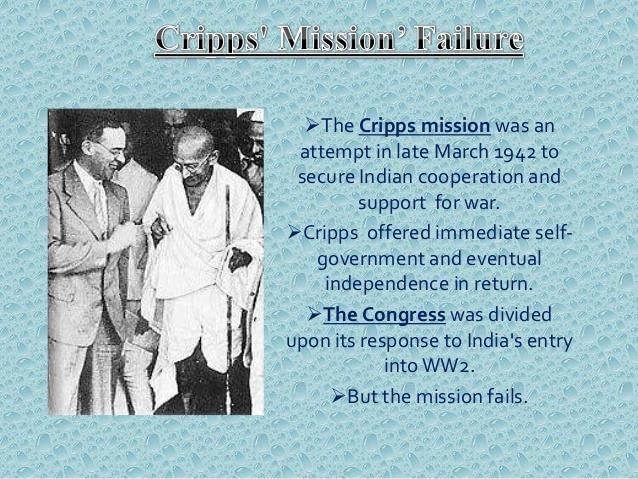
➢ मुस्लिम लीग
- भारतीय संघ के एकल विचार की आलोचना की;
- संविधान सभा की स्थापना के लिए यंत्रणा और संघ में प्रांतों के विलय के निर्णय की प्रक्रिया पसंद नहीं आई, और
- सोचा कि प्रस्तावों ने मुसलमानों को स्व-निर्णय और पाकिस्तान के निर्माण का अधिकार से वंचित किया।
|
198 videos|620 docs|193 tests
|




















