The Hindi Editorial Analysis- 28th May 2025 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC PDF Download
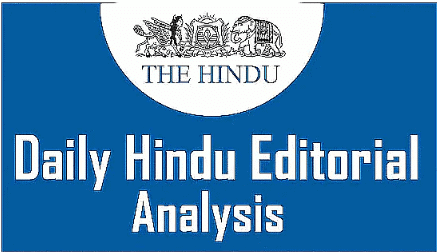
ऊर्जा और दक्षता
चर्चा में क्यों?
भारत को ऊर्जा दक्षता में सुधार करके अपनी बिजली खपत कम करनी होगी।
परिचय
भारत के बिजली क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, खासकर हाल के वर्षों में अक्षय ऊर्जा में तेजी से वृद्धि के साथ। हालांकि, बिजली आपूर्ति और अधिकतम मांग के बीच का अंतर बढ़ता जा रहा है, जो आपूर्ति संबंधी मौजूदा समस्याओं का संकेत देता है। चूंकि देश शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ती ऊर्जा जरूरतों का सामना कर रहा है, इसलिए ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास सुनिश्चित करने का सबसे व्यावहारिक और लागत प्रभावी तरीका बन गया है।
भारत का विद्युत विरोधाभास: बढ़ती आपूर्ति लेकिन बढ़ती मांग का अंतर
बिजली उत्पादन में वृद्धि बनाम अधिकतम मांग में कमी
- भारत ने पिछले बीस वर्षों में बिजली उत्पादन में मजबूत वृद्धि का अनुभव किया है, तथा पिछले पांच वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- इस वृद्धि के बावजूद, भारत को अपनी अधिकतम बिजली मांग को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें अधिकतम बिजली घाटा वित्त वर्ष 2020 में 0.69% से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में अनुमानित 5% हो गया है।
- यह बढ़ता घाटा प्रणालीगत आपूर्ति बाधाओं को उजागर करता है, जिनमें शामिल हैं:
- नये विद्युत उत्पादन, विशेषकर जीवाश्म ईंधन आधारित संयंत्रों की स्थापना के लिए लंबा समय चाहिए।
- मौजूदा ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करने में चुनौतियाँ।
ऊर्जा दक्षता की आवश्यकता: सबसे तेज़ और सस्ता समाधान
ऊर्जा दक्षता सबसे तीव्र और सबसे अधिक लागत प्रभावी समाधान है:
- बिजली की मांग कम करें.
- जलवायु परिवर्तन से निपटें।
आपूर्ति और अधिकतम मांग के बीच के अंतर को पाटने के लिए व्यापक ऊर्जा दक्षता उपायों को लागू करना महत्वपूर्ण है।
उजाला का एक दशक: भारत की एलईडी क्रांति
उजाला (सभी के लिए किफायती एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति)
- लॉन्च: 2015
- प्रभाव: एलईडी बल्बों की कीमत ₹500 से घटाकर ₹70 कर दी गई, जिससे पूरे भारत में घरों में इनका व्यापक उपयोग होने लगा।
- आंकड़े (जनवरी 2025 तक):
- सरकार द्वारा वितरित एलईडी बल्ब: 37 करोड़
- अतिरिक्त एलईडी बल्ब बेचे गए: ~407 करोड़
- अनुमानित लागत बचत: 10 बिलियन डॉलर से अधिक
- बचाई गई उत्पादन क्षमता: ~9,500 मेगावाट (लगभग 19 कोयला संयंत्रों के बराबर)
स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम (एसएलएनपी)
- उजाला के साथ-साथ कार्यान्वित, शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) और ग्राम पंचायतों में एलईडी स्ट्रीट लाइट स्थापना पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- प्रभाव: अधिकतम मांग में 1,500 मेगावाट से अधिक की कमी।
एलईडी क्यों महत्वपूर्ण हैं: दक्षता तुलना
| बल्ब का प्रकार | बिजली की खपत (एलईडी की तुलना में) |
|---|---|
| नेतृत्व किया | 1x (आधार रेखा) |
| कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप (सीएफएल) | 2x |
| तापदीप्त बल्ब | 9x |
एलईडी बल्बों की ओर बदलाव से घरों की लागत में महत्वपूर्ण बचत होती है, साथ ही बिजली की खपत और कार्बन उत्सर्जन में भी बड़ी कमी आती है।
व्यापक ऊर्जा दक्षता उपाय और उनका प्रभाव
विधायी आधार: ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता संबंधी विभिन्न पहलों का प्रमुख समर्थक रहा है।
ऊर्जा दक्षता से लाभ (2000-2018):
- ऊर्जा मांग में कमी: ऊर्जा मांग में 15% की कमी हासिल की गई।
- CO2 उत्सर्जन से बचाव: इस अवधि के दौरान लगभग 300 मिलियन टन CO2 उत्सर्जन से बचाव किया गया।
स्रोत: अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी
बढ़ती चुनौती: बढ़ती ऊर्जा मांग
ऊर्जा मांग को बढ़ाने वाले कारक:
- तेजी से बढ़ते शहरीकरण और बढ़ते तापमान के कारण शीतलन समाधानों की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है।
- 2024 में अधिकतम बिजली की मांग 250 गीगावाट तक पहुंच गई है, जो बढ़ी हुई ऊर्जा आवश्यकताओं को दर्शाती है।
- भारत अब चीन और अमेरिका के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बिजली उपभोक्ता बन गया है।
ऊर्जा मिश्रण एवं भविष्य में कोयले पर निर्भरता:
वर्तमान ऊर्जा स्रोत: कोयला ऊर्जा का प्रमुख स्रोत बना हुआ है, जो ऊर्जा उत्पादन का लगभग 70% हिस्सा है।
नियोजित वृद्धि: 2032 तक कोयला आधारित विद्युत उत्पादन में लगभग 90 गीगावाट की वृद्धि की योजना है, जो निकट भविष्य में कोयले पर निर्भरता जारी रहने का संकेत है।
आगे की राह: क्षेत्रवार ऊर्जा दक्षता अधिदेश
क्षेत्रीय दक्षता अधिदेशों की तत्काल आवश्यकता:
- भवन: ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए डिजाइन और इन्सुलेशन में सुधार पर ध्यान दें।
- घरेलू उपकरण: शीतलन, प्रकाश और ताप उपकरणों में दक्षता को प्राथमिकता दें।
- लघु एवं मध्यम उद्यम (एसएमई): एसएमई में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के उपायों को लागू करना।
लक्ष्य:
- विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता में सुधार लाना।
- ऊर्जा उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भरता कम करना।
- बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिकतम मांग को स्थायी रूप से स्थिर बनाए रखना।
निष्कर्ष
- विद्युत उत्पादन के प्रति प्रतिबद्धता: भारत विद्युत उत्पादन क्षमता का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है, तथा कोयला और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों दोनों में महत्वपूर्ण निवेश की योजना बनाई गई है।
- ऊर्जा दक्षता को प्राथमिकता देना: हालांकि, बढ़ती ऊर्जा मांग और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता को प्राथमिकता देने की अत्यंत आवश्यकता है।
- उजाला और एसएलएनपी का प्रभाव: उजाला और स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम (एसएलएनपी) जैसे कार्यक्रमों ने ऊर्जा खपत पैटर्न को बदलने और अधिकतम मांग को प्रभावी ढंग से कम करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है।
- समान पहलों का विस्तार: भवनों, उपकरणों और लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) में समान ऊर्जा दक्षता पहलों का विस्तार और विस्तार निम्नलिखित के लिए महत्वपूर्ण होगा:
- चरम मांग को कम करना.
- कार्बन उत्सर्जन कम करना।
- महंगे बुनियादी ढांचे के निवेश से बचना।
- दक्षता एक आधारशिला: ऊर्जा दक्षता को भारत की ऊर्जा रणनीति का आधार बनाना सतत विकास, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और देश के जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक होगा।
रणनीतिक साझेदारी की रजत जयंती
चर्चा में क्यों?
भारत और जर्मनी एक मजबूत और विविधतापूर्ण रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। यह रिश्ता, जो चार प्रमुख स्तंभों - शांति, समृद्धि, लोग और ग्रह - पर आधारित है, लगातार बढ़ रहा है और आज की दुनिया की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है। जर्मनी की 'भारत पर ध्यान' रणनीति और हाल की कूटनीतिक भागीदारी इस बंधन को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता का संकेत देती है।
एक साझा दृष्टिकोण
शांति और स्थिरता
- साझा दृष्टिकोण: भारत और जर्मनी दोनों ही शांतिपूर्ण, स्थिर और नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- राजनीतिक विश्वास: अंतर-सरकारी परामर्श से सरकार-से-सरकार संबंधों में वृद्धि होती है तथा राजनीतिक विश्वास को बढ़ावा मिलता है।
- रक्षा सहयोग: हाल के वर्षों में भारत और जर्मनी के बीच रक्षा साझेदारी काफी मजबूत हुई है।
- संयुक्त अभ्यास: 2024 में तमिलनाडु के सुलूर में आयोजित होने वाला आगामी तरंग शक्ति अभ्यास भारतीय और जर्मन पायलटों के बीच समन्वय को प्रदर्शित करेगा।
- भविष्य की योजनाएँ: रक्षा उद्योग सहयोग में घनिष्ठ संबंध और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग में वृद्धि की उम्मीद है।
समृद्धि और आर्थिक विकास
- सकल घरेलू उत्पाद से परे: समृद्धि का अर्थ यह सुनिश्चित करना है कि लोगों के पास अच्छी नौकरियां हों, वे अपने परिवारों का भरण-पोषण कर सकें, तथा अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकें।
- भारत में जर्मन निवेश: भारत में लगभग 2,000 जर्मन कंपनियों ने 750,000 से अधिक नौकरियां पैदा की हैं।
- प्रौद्योगिकी और अवसंरचना साझेदारी: डॉयचे बान द्वारा प्रशिक्षित भारतीयों द्वारा संचालित दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल, आधुनिक अवसंरचना में युवा भारतीय प्रतिभा की भूमिका को उजागर करती है।
- जर्मनी में भारतीय कम्पनियां: जर्मनी की उच्च तकनीक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारतीय कम्पनियों की संख्या बढ़ती जा रही है।
- लचीली आपूर्ति शृंखलाएँ: एकीकृत आपूर्ति शृंखलाएँ वैश्विक व्यापार चुनौतियों के बीच भी आपसी विश्वास को प्रदर्शित करती हैं। संभावित यूरोपीय संघ-भारत मुक्त व्यापार समझौता आर्थिक संबंधों को और बढ़ा सकता है।
विज्ञान, प्रौद्योगिकी और स्थिरता
- संयुक्त अनुसंधान: भारतीय शोधकर्ता वास्तविक दुनिया की चुनौतियों से निपटने के लिए शीर्ष जर्मन संस्थानों के साथ सहयोग कर रहे हैं।
- पर्यावरण के लिए तकनीक: प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर पर्यावरणीय चुनौतियों को व्यावसायिक अवसरों में बदला जा सकता है।
लोगों से लोगों के बीच संपर्क
- साझेदारी का हृदय: भारत-जर्मनी सामरिक संबंधों का हृदय लोग हैं।
- जर्मनी में रहने वाले भारतीयों की संख्या बढ़ रही है।
- छात्र: 50,000 से अधिक भारतीय छात्र अब जर्मन विश्वविद्यालयों में सबसे बड़ा विदेशी छात्र समूह हैं।
- जीवन की कहानियाँ और आपसी विकास: जर्मनी में भारतीय छात्र बहुमूल्य अनुभव प्राप्त करते हैं और दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं और समाजों में योगदान देते हैं। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म युवा भारतीयों को अपने अनुभव साझा करने का अवसर देते हैं, जिससे जर्मनी में उनकी अनुकूलनशीलता और सफलता पर प्रकाश डाला जा सके।
- जर्मनी में योगदान: जर्मनी में रहने वाले भारतीय देश की अर्थव्यवस्था और संस्कृति को समृद्ध करते हैं।
भाषा एक सेतु के रूप में
- जर्मन सीखना: जर्मन सीखने वाले भारतीय जर्मनी में अधिक अवसरों का लाभ उठा सकते हैं।
- भारत में जर्मन भाषा: भारत में जर्मन सीखने में रुचि बढ़ रही है, जिसके लिए अधिक प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता है।
- भारतीयों द्वारा जर्मन सीखना: जर्मन सीखने से नौकरी और शिक्षा के अवसर बढ़ते हैं, साथ ही जर्मनी में बेहतर एकीकरण भी होता है।
भारत में जर्मन - अगला कदम
- रिवर्स एक्सचेंज की आवश्यकता: भारत में अध्ययन, कार्य और व्यापार करने के लिए अधिक जर्मन लोगों की आवश्यकता है, साथ ही भारतीय भाषाओं और संस्कृति को समझने पर भी जोर दिया जाना चाहिए।
- भविष्य की दृष्टि: दोनों देशों के युवाओं में निवेश से भविष्य के लिए साझेदारी मजबूत होगी।
हरित विकास
- साझा पारिस्थितिक जीवन रेखा: ग्रह पृथ्वी हमारी भावी आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे पर्यावरणीय चुनौतियों का मिलकर समाधान करना आवश्यक हो जाता है।
- भारत-जर्मनी हरित एवं सतत विकास साझेदारी (जीएसडीपी): 2022 में स्थापित, जर्मनी की 10 वर्षों में 10 बिलियन यूरो की प्रतिबद्धता के साथ, नवीकरणीय ऊर्जा, जैव विविधता संरक्षण और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- निजी क्षेत्र का सहयोग: जर्मन कंपनियां बड़े पैमाने पर सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं, जैसे पवन टर्बाइनों के लिए पुर्जे बनाने, के माध्यम से भारत के हरित विकास में योगदान दे रही हैं।
- उन्नत जर्मन प्रौद्योगिकी: इसका उद्देश्य भारत की ऊर्जा परिवर्तन में सहायता करना है, साथ ही देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था में योगदान देना है।
निष्कर्ष
भारत-जर्मनी की रणनीतिक साझेदारी पिछले 25 वर्षों में मजबूत हुई है, जो शांति, समृद्धि, लोगों और ग्रह के स्तंभों पर आधारित है। साझा लक्ष्यों, मजबूत आर्थिक संबंधों और संयुक्त हरित पहलों के साथ, दोनों देश भविष्य की चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार हैं। युवाओं, नवाचार और स्थिरता में निवेश जारी रखते हुए, भारत और जर्मनी आने वाले वर्षों में वैश्विक प्रगति का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं।
|
7 videos|3457 docs|1081 tests
|
FAQs on The Hindi Editorial Analysis- 28th May 2025 - Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC
| 1. ऊर्जा और दक्षता क्या हैं और इनका महत्व क्या है ? |  |
| 2. रणनीतिक साझेदारी क्या होती है ? |  |
| 3. रणनीतिक साझेदारी की रजत जयंती का क्या अर्थ है ? |  |
| 4. ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं ? |  |
| 5. रणनीतिक साझेदारियों का ऊर्जा क्षेत्र में क्या प्रभाव है ? |  |





















