UPSC Daily Current Affairs(Hindi)- 17th June 2025 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly PDF Download
GS1/इतिहास और संस्कृति
सोवा-रिग्पा पारंपरिक चिकित्सा
स्रोत: PIB
समाचार में क्यों?
आज लेह में स्थित राष्ट्रीय सोवा-रिग्पा संस्थान (NISR) में एक दिवसीय सम्योग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भारत के दस राज्यों के विशेषज्ञ इस प्राचीन चिकित्सा प्रणाली पर चर्चा करने और उसे बढ़ावा देने के लिए एकत्र हुए।
मुख्य बिंदु
- सोवा-रिग्पा आज भी प्रचलित सबसे पुरानी चिकित्सा प्रणालियों में से एक है।
- यह प्रणाली 2,000 से अधिक वर्ष पहले उत्पन्न हुई थी और इसे 8वीं शताब्दी CE में राजा त्रिसोंग देत्सेन के शासनकाल के दौरान संहिताबद्ध किया गया।
- यह आयुर्वेद और चीनी चिकित्सा सहित विभिन्न चिकित्सा परंपराओं के अवधारणाओं को एकीकृत करती है।
अतिरिक्त विवरण
- अवलोकन: सोवा-रिग्पा, जिसे पारंपरिक तिब्बती चिकित्सा या अमची प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है, समग्र स्वास्थ्य और प्रकृति के साथ सामंजस्य पर जोर देती है।
- वैश्विक उपस्थिति: यह प्रणाली न केवल तिब्बत में, बल्कि मंगोलिया, भूटान, नेपाल, और रूस तथा चीन के कुछ हिस्सों में भी प्रचलित है, साथ ही भारत के क्षेत्रों जैसे लेह-लद्दाख और सिक्किम में भी इसका महत्वपूर्ण अस्तित्व है।
- मुख्य विश्वास: यह रोग निवारण पर ध्यान केंद्रित करती है और मन-शरीर कल्याण के समग्र दृष्टिकोण के माध्यम से दीर्घकालिकता को बढ़ावा देती है।
- diagnosis और उपचार: चिकित्सक नाड़ी और मूत्र विश्लेषण जैसी विधियों का उपयोग करते हैं, साथ ही केस इतिहास की समीक्षा करते हैं, और हर्बल औषधियों और आध्यात्मिक उपचारों जैसे उपचारों का उपयोग करते हैं।
- शिक्षा और मान्यता: पारंपरिक ज्ञान मौखिक परंपराओं के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी منتقل किया जाता है, और सोवा-रिग्पा को 2010 से भारत में AYUSH प्रणालियों के तहत आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त है।
हाल ही में, हिमालयी बिच्छू घास (Girardinia diversifolia) के बारे में जागरूकता बढ़ी है, जिसे विभिन्न उत्पादों के लिए एक स्थायी स्रोत के रूप में पहचाना गया है, जिससे इसके उपयोग में रुचि बढ़ी है।
इस विषय से संबंधित एक क्विज़ में, प्रतिभागियों से हिमालयी बिच्छू घास में पाए जाने वाले स्थायी स्रोत के बारे में पूछा गया, जिसमें विकल्प थे: (a) मलेरिया रोधी दवा, (b) जैव-ईंधन, (c) कागज उद्योग के लिए गूदा, और (d) वस्त्र फाइबर।
GS3/पर्यावरण
काली टाइगर रिजर्व के प्रमुख तथ्य
स्रोत:द हिंदू
संरक्षण कार्यकर्ताओं ने काली टाइगर रिजर्व में वन्यजीव सफारी के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देने के संबंध में चिंताओं का इजहार किया है, यह बताते हुए कि इससे रिजर्व के पारिस्थितिकी तंत्र पर संभावित प्रभाव पड़ सकता है।
- काली टाइगर रिजर्व, जिसे पहले दंडेली-आंशी टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता था, कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित है।
- यह 834.16 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें दंडेली वन्यजीव अभयारण्य और आंशी राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं।
- यह रिजर्व पश्चिमी घाट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो जैविक रूप से संवेदनशील क्षेत्र है।
- भौगोलिक स्थिति: काली टाइगर रिजर्व उत्तर में कर्नाटक के भीमगड वन्यजीव अभयारण्य से घिरा हुआ है, जो महाराष्ट्र के राधानगरी और कोयना वन्यजीव अभयारण्य से जुड़ता है।
- जल स्रोत: रिजर्व का नाम काली नदी पर पड़ा है, जो इस क्षेत्र का मुख्य जल स्रोत है।
- वनस्पति: जंगल मुख्यतः आर्द्र पर्णपाती और अर्ध-शाश्वत प्रकार के हैं, जिनमें कुछ क्षेत्रों में शाश्वत वन के महत्वपूर्ण पैच हैं।
- फ्लोरा: रिजर्व में विभिन्न प्रकार की पौधों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें टिक और चांदी का ओक जैसी हार्डवुड पेड़, झाड़ियाँ और घनी झाड़ी शामिल हैं।
- फौना: यह विभिन्न जानवरों का घर है, जिनमें बाघ, तेंदुए, हाथी, बिशन और कई पक्षियों की प्रजातियाँ, विशेष रूप से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल शामिल हैं।
- यह क्षेत्र इसकी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है, जिसमें दुर्लभ काले तेंदुओं की उपस्थिति भी शामिल है।
काली टाइगर रिजर्व जैव विविधता संरक्षण प्रयासों और पश्चिमी घाट में पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर्यटन के प्रभाव पर चल रही चर्चाएँ वन्यजीव प्रबंधन में स्थायी प्रथाओं की आवश्यकता को उजागर करती हैं।
GS3/अर्थव्यवस्था
भारत की वित्तीय समेकन की दिशा - ताकत, कमी और नीतिगत निहितार्थ
स्रोत: PIB
यह लेख भारत सरकार (GoI) के वित्तीय वर्ष 2024-25 (FY25) की वित्तीय प्रदर्शन का विश्लेषण करता है, जिसमें अस्थायी आंकड़ों का उपयोग किया गया है और FY26 के लिए निहितार्थों का आकलन किया गया है। यह घाटा प्रबंधन, पूंजी व्यय (capex) की वृद्धि, राजस्व संग्रह, और आगामी नीतिगत परिवर्तनों में प्रमुख रुझानों पर जोर देता है, जो भारत में मैक्रोइकोनॉमिक प्रबंधन और वित्तीय संघवाद के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- FY25 का वित्तीय घाटा 15.77 लाख करोड़ रुपये पर दर्ज किया गया, जो संशोधित अनुमान (RE) 15.7 लाख करोड़ रुपये से थोड़ा अधिक है।
- जीडीपी के प्रतिशत के रूप में वित्तीय घाटा 4.8% पर नियंत्रित रहा, जो नाममात्र जीडीपी में वृद्धि के कारण लक्ष्य को पूरा करता है।
- राजस्व घाटा 5.7 लाख करोड़ रुपये तक घट गया, जो जीडीपी के 1.7% पर 17 वर्षों में सबसे कम है।
- पूंजी व्यय में तेजी आई, जिसमें अप्रैल 2025 में 61% की वार्षिक वृद्धि हुई, जिससे यह 1.6 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गया।
- राजस्व में 0.6 लाख करोड़ रुपये की कमी आई, जो FY25 के RE की तुलना में है, जिसके लिए FY26 के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 12.5% की वृद्धि आवश्यक है।
- वित्तीय घाटे के रुझान: FY25 के लिए वित्तीय घाटा अपेक्षाओं से थोड़ा अधिक था, जो नाममात्र जीडीपी वृद्धि के अनुमान से अधिक होने के कारण था।
- राजस्व घाटे की मील का पत्थर: राजस्व घाटा जीडीपी के 1.7% पर गिर गया, जो पिछले वर्ष के लक्ष्य की तुलना में एक महत्वपूर्ण सुधार है।
- पूंजी व्यय में वृद्धि: capex में मजबूत वृद्धि अवसंरचना विकास के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
- राजस्व और राजस्व चुनौतियाँ: कर राजस्व में उल्लेखनीय कमी आई, लेकिन RBI के लाभांश से अतिरिक्त संसाधनों ने कुछ राहत प्रदान की।
- FY26 दृष्टिकोण: नाममात्र जीडीपी वृद्धि की कम प्रवृत्ति के बावजूद, पूर्व की उपलब्धियों के कारण वित्तीय घाटे को प्रभावी रूप से प्रबंधित किया जा सकता है।
निष्कर्षतः, भारत की वित्तीय समेकन की दिशा सकारात्मक प्रतीत होती है, जिसे बढ़ते capex और घटते राजस्व घाटे द्वारा समर्थित किया गया है। हालाँकि, मध्य-कालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए राजस्व संधारण में संरचनात्मक सुधार, व्यय की दक्षता को बढ़ाना, और उभरती भू-राजनीतिक और संस्थागत चुनौतियों के संदर्भ में केंद्र-राज्य वित्तीय समन्वय में सुधार की आवश्यकता होगी।
पोर्टुलका भारत की खोज
स्रोत: द हिंदू
एक नई फूलदार पौधे की प्रजाति, जिसे पोर्टुलका भारत (Portulaca bharat) नाम दिया गया है, जयपुर के निकट अरावली पहाड़ियों के चट्टानी और अर्ध-शुष्क इलाके में पहचानी गई है। यह खोज भारतीय अंतीय पौधों की जैव विविधता में योगदान करती है।
- प्रजाति वर्गीकरण: पोर्टुलका भारत भारत में अंतीय प्रजातियों की सूची में जुड़ता है।
- आवास विशिष्टता: यह पौधा वर्तमान में केवल एक स्थान, गाल्ताजी पहाड़ियों से जाना जाता है, जहां केवल 10 व्यक्तियों का पता चला है।
- संवेदनशीलता: इसकी संकीर्ण अंतीयता और विशिष्ट आवास आवश्यकताएं हैं, जो इसे जलवायु परिवर्तन और आवासीय गिरावट के प्रति संवेदनशील बनाती हैं।
- विशेषताएँ: पौधा विपरीत, थोड़े गर्ताकार पत्ते और हल्के पीले फूलों के साथ दिखाई देता है जो शीर्ष की ओर क्रीमिश-श्वेत हो जाते हैं। इसके उल्लेखनीय लक्षणों में कर्णिक बाल (ग्लैंड्युलर हेयर्स) और मोटी जड़ें शामिल हैं।
- जाति अवलोकन: जाति पोर्टुलका में विश्वभर में लगभग 153 प्रजातियाँ हैं, जो मुख्यतः उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ये सुकुलेंट्स उनकी सहनशीलता और पानी संग्रहित करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं, जो चरम वातावरण में पनपते हैं।
- भारतीय वितरण: भारत में पोर्टुलका की 11 ज्ञात प्रजातियाँ हैं, जिनमें से चार अंतीय हैं और मुख्यतः शुष्क तथा अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं।
पोर्टुलका भारत की खोज अद्वितीय पौधा प्रजातियों और उनके आवासों के संरक्षण के महत्व को उजागर करती है, विशेष रूप से पर्यावरणीय चुनौतियों के सामने।
त्रिपुरा में दो नई कीड़े प्रजातियों की खोज
स्रोत: ETV भारत

हाल ही में, त्रिपुरा में दो नई कीड़े प्रजातियाँ, Kanchuria tripuraensis और Kanchuria priyasankari, की पहचान की गई है। यह खोज इस क्षेत्र में मिट्टी की जैव विविधता की हमारी समझ को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाती है।
- नई प्रजातियाँ रबर और अनानास के बागानों में पाई गईं, जो संशोधित कृषि परिदृश्यों में पारिस्थितिकी विविधता को दर्शाती हैं।
- Kanchuria tripuraensis में 7 और 8 खंडों में एक अद्वितीय एकल वेंट्रोमेडियन स्पर्मैथेका है, जो इसे अपने जाति में विशिष्ट बनाता है।
- Kanchuria priyasankari काफी छोटी है और इसका एक अलग स्पर्मैथेकी संरचना है, जो इसे इसके रिश्तेदार K. turaensis से अलग करती है।
- इन खोजों के साथ, जाति Kanchuria अब 10 प्रजातियों में शामिल है, जिससे त्रिपुरा में 38 दस्तावेजीकृत मेगाड्राइल कीड़े प्रजातियों की कुल संख्या होती है।
- यह पूर्वी हिमालय–उत्तर-पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र को कीड़े की विविधता के लिए भारत का दूसरा सबसे समृद्ध क्षेत्र बनाता है।
- Kanchuria tripuraensis: यह प्रजाति अपनी एकल वेंट्रोमेडियन स्पर्मैथेका के लिए अद्वितीय है, जो इसे पहचानने की एक प्रमुख विशेषता के रूप में कार्य करती है।
- Kanchuria priyasankari: प्रियसांकर चौधुरी, जो कीड़े की वर्गीकरण में एक प्रमुख व्यक्ति हैं, के सम्मान में नामित, यह प्रजाति त्रिपुरा की पारिस्थितिकी समृद्धि को उजागर करती है।
- ये खोजें त्रिपुरा के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मिट्टी जैव विविधता अध्ययनों में महत्व को रेखांकित करती हैं।
अंत में, Kanchuria tripuraensis और Kanchuria priyasankari की पहचान न केवल त्रिपुरा की जैव विविधता सूची को समृद्ध करती है, बल्कि परिवर्तित परिदृश्यों में मिट्टी के पारिस्थितिकी तंत्रों के संरक्षण के महत्व को भी रेखांकित करती है।
PRASHAD योजना
स्रोत: द हिंदू
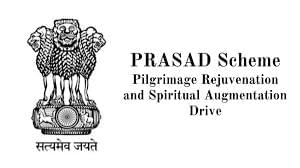
कर्नाटका में लंबे समय से प्रतीक्षित चामुंडी पहाड़ियों विकास परियोजना अंततः तीर्थयात्रा पुनरुद्धार और आध्यात्मिक धरोहर वृद्धि अभियान (PRASHAD) योजना के तहत गति पकड़ रही है।
- PRASHAD योजना भारत भर में तीर्थ स्थलों को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू की गई थी।
- यह आध्यात्मिक पर्यटन अवसंरचना के विकास और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करती है।
- शुरुआत: इस योजना की शुरुआत 2014-15 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा की गई थी।
- मुख्य उद्देश्य: इसका उद्देश्य प्रमुख तीर्थ स्थलों के विकास के माध्यम से आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है।
- सीमा और मिशन: 2017 में, इसे एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में उन्नत किया गया, जिसमें एकीकृत विकास मॉडल के लिए HRIDAY सुविधाओं को शामिल किया गया।
- सांस्कृतिक ध्यान: यह योजना सांस्कृतिक संरक्षण और समुदाय की भागीदारी पर जोर देती है, जबकि देशी और अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देती है।
- कार्यान्वयन:
- कार्यकारी एजेंसियाँ: परियोजनाएँ संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा नियुक्त राज्य स्तरीय एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं।
- वित्तीय मॉडल: योग्य अवसंरचना और विकास घटकों के लिए 100% केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- जन-निजी समर्थन: स्थिरता के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) योगदान और जन-निजी साझेदारियों (PPP) को प्रोत्साहित करती है।
- केंद्र-राज्य सहयोग: स्थानीय संस्कृतियों का सम्मान करते हुए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग के लिए डिज़ाइन की गई है।
- मुख्य विशेषताएँ:
- अवसंरचना विकास: तीर्थ स्थलों पर सड़कों, पीने के पानी, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, और सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार।
- संयोगिता में सुधार: तीर्थयात्रियों के लिए आसान पहुँच के लिए रेल, सड़क, और हवाई लिंक में सुधार।
- तीर्थयात्री सुविधाएँ: सुरक्षित तीर्थयात्राओं को सुनिश्चित करने के लिए आवास, खाद्य कोर्ट, मार्गनिर्देशन प्रणाली, और सुरक्षा उपायों का निर्माण।
- सांस्कृतिक संरक्षण: मंदिरों, स्मारकों, घाटों, और पवित्र झीलों का पुनर्स्थापन, पर्यटन में सांस्कृतिक परंपराओं को एकीकृत करना।
- समुदाय सशक्तिकरण: स्थानीय लोगों के लिए कौशल प्रशिक्षण और हितधारक भागीदारी के माध्यम से पर्यटन से जुड़े रोजगार का विकास।
- सततता पर ध्यान: पारिस्थितिकी के अनुकूल तकनीकों का उपयोग और पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देना।
यह योजना न केवल आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखती है, बल्कि सतत प्रथाओं, समुदाय की भागीदारी और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण पर भी ध्यान केंद्रित करती है।
UPSC 2022
प्रधानमंत्री ने हाल ही में वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सी बातें सही हैं?
- 1. सोमनाथ मंदिर एक ज्योतिर्लिंग तीर्थ है।
- 2. अल-बिरूनी द्वारा सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया गया था।
- 3. सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा (वर्तमान मंदिर की स्थापना) राष्ट्रपति एस. राधाकृष्णन द्वारा की गई थी।
नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3
GS2/राजनीति
न्यायाधीशों की सेवा, लेकिन न्याय नहीं
स्रोत: द हिंदू
क्यों समाचार में?
भारतीय न्यायपालिका, जिसे पारंपरिक रूप से संविधानिक मूल्यों की रक्षा करने वाला माना जाता है, हाल की विवादों के कारण जांच के दायरे में है जो इसकी विश्वसनीयता को चुनौती देती हैं। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का मामला, जिसमें उनके निवास पर नकद की खोज और बाद की अस्पष्ट कार्यवाही शामिल है, न्यायिक जवाबदेही के भीतर महत्वपूर्ण मुद्दों को उजागर करता है।
- न्यायमूर्ति वर्मा के चारों ओर का विवाद न्यायपालिका के भीतर गहरे प्रणालीगत समस्याओं को दर्शाता है।
- न्यायपालिका की 'इन-हाउस प्रक्रिया' में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी है।
- ऐतिहासिक मिसालें गोपनीयता और सार्वजनिक निगरानी की कमी के पैटर्न को दर्शाती हैं।
- न्यायमूर्ति वर्मा विवाद: 14 मार्च को न्यायमूर्ति वर्मा के निवास पर आग लगने से आधे जले हुए बोरों का पता चला, जिनमें नकद होने का संदेह था। उनके त्वरित स्थानांतरण और बाद में महाभियोग की सिफारिश ने जांच प्रक्रिया की इंटीग्रिटी के बारे में चिंताएँ उत्पन्न कीं।
- इन-हाउस प्रक्रिया:न्यायिक दुराचार पूछताछ के लिए यह अनौपचारिक तंत्र सहकर्मी न्यायाधीशों द्वारा संचालित होता है और इसमें सार्वजनिक जवाबदेही की कमी होती है। मुख्य मुद्दे निम्नलिखित हैं:
- पारदर्शिता की कमी: जनता को यह नहीं बताया जाता है कि क्या पूछताछ की जा रही है या उनके परिणाम क्या हैं।
- प्रक्रियागत सुरक्षा का अभाव: औपचारिक पूछताछ के विपरीत, ये प्रक्रियाएँ कानूनी मानकों द्वारा बाध्य नहीं होती हैं।
- कोई सार्वजनिक जवाबदेही नहीं: कोई बाहरी निगरानी या अपील नहीं है, जिससे न्यायपालिका की वैधता कम होती है।
- पारदर्शिता की कमी: जनता को यह नहीं बताया जाता है कि क्या पूछताछ की जा रही है या उनके परिणाम क्या हैं।
- प्रक्रियागत सुरक्षा का अभाव: औपचारिक पूछताछ के विपरीत, ये प्रक्रियाएँ कानूनी मानकों द्वारा बाध्य नहीं होती हैं।
- कोई सार्वजनिक जवाबदेही नहीं: कोई बाहरी निगरानी या अपील नहीं है, जिससे न्यायपालिका की वैधता कम होती है।
- ऐतिहासिक मिसालें: न्यायमूर्ति रामना और CJI रंजन गोगोई के खिलाफ आरोप जैसे पिछले मामलों ने न्यायपालिका के भीतर गोपनीयता और जवाबदेही की कमी के troubling पैटर्न को उजागर किया है।
निष्कर्ष के रूप में, न्यायमूर्ति वर्मा के चारों ओर की स्थिति न्यायपालिका के भीतर सुधार की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है। पारदर्शिता और जवाबदेही को अपनाना सार्वजनिक विश्वास बनाए रखने और न्यायिक प्रक्रियाओं की वैधता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। न्यायिक और स्वतंत्र निगरानी दोनों को शामिल करने वाला एक संशोधित ढांचा भारतीय न्यायपालिका की भविष्य की इंटीग्रिटी के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।
GS2/शासन
भारत की 2027 की जनगणना: क्या नया है और यह कैसे काम करती है
स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस
सरकार ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि भारत की 16वीं जनगणना दो चरणों में आयोजित की जाएगी, जिनकी संदर्भ तिथियाँ 1 अक्टूबर 2026 के लिए बर्फ-धारण क्षेत्रों और 1 मार्च 2027 के लिए देश के बाकी हिस्सों के लिए निर्धारित की गई हैं। यह जनगणना 1931 के बाद से राष्ट्रव्यापी जाति-आधारित गणना की पहली बार होगी और इसे जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 3 के तहत एक गज़ट अधिसूचना के बाद शुरू किया गया है, जो जनसंख्या गणना से पहले घर-लिस्टिंग और आवास सर्वेक्षणों की प्रक्रिया को भी शुरू करता है।
- जनगणना दो मुख्य चरणों में आयोजित की जाएगी: घर-लिस्टिंग और जनसंख्या गणना।
- 2027 भारत की पूरी तरह से डिजिटल जनगणना की दिशा में संक्रमण का संकेत देता है, जिसमें आत्म-गणना विकल्प शामिल हैं।
- दूरस्थ क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता और कनेक्टिविटी जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए ठोस समाधान तैयार किए जा रहे हैं।
- दो-चरणीय संरचना:जनगणना में दो मुख्य चरण शामिल हैं:
- घर-लिस्टिंग और आवास जनगणना: इस चरण में भवनों और घरों से संबंधित विवरण दर्ज किए जाते हैं, जिसमें निर्माण सामग्री और उपयोगिताओं तक पहुँच शामिल है।
- जनसंख्या गणना: इस चरण में व्यक्तिगत जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक डेटा एकत्र किया जाता है, जिसमें नाम, उम्र, लिंग, और वैवाहिक स्थिति जैसे विवरण शामिल हैं।
- घर-लिस्टिंग और आवास जनगणना: इस चरण में भवनों और घरों से संबंधित विवरण दर्ज किए जाते हैं, जिसमें निर्माण सामग्री और उपयोगिताओं तक पहुँच शामिल है।
- जनसंख्या गणना: इस चरण में व्यक्तिगत जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक डेटा एकत्र किया जाता है, जिसमें नाम, उम्र, लिंग, और वैवाहिक स्थिति जैसे विवरण शामिल हैं।
- पहली डिजिटल जनगणना: 2027 की जनगणना मोबाइल ऐप्स और क्लाउड सिस्टम का उपयोग करेगी, जो वास्तविक समय में डेटा की निगरानी और प्रबंधन की अनुमति देती है।
- स्वयं-गणना: पहली बार, घरों को सरकार के पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से स्वयं-गणना करने की अनुमति दी जाएगी, जिसमें सत्यापन के लिए एक अद्वितीय आईडी प्राप्त होगी।
- डेटा गुणवत्ता में सुधार: मानकीकृत डिजिटल कोडिंग सिस्टम और GPS एकीकरण की शुरूआत डेटा की सटीकता बढ़ाने और पिछले जनगणनाओं की तुलना में प्रसंस्करण समय को कम करने के लिए की जा रही है।
- चुनौतियों का समाधान:
- गणनाकर्ताओं के बीच डिजिटल साक्षरता को व्यापक प्रशिक्षण और बहुभाषी इंटरफेस के माध्यम से समर्थन दिया जा रहा है।
- दूरस्थ क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की समस्याओं का समाधान ऑफ़लाइन डेटा संग्रह को सक्षम करके किया जा रहा है, जो ऑनलाइन होने पर समन्वयित होता है।
- गुणवत्ता नियंत्रण के उपायों में स्वचालित त्रुटि पहचान और पर्यवेक्षक समीक्षाएँ शामिल हैं, ताकि डेटा की विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके।
- गणनाकर्ताओं के बीच डिजिटल साक्षरता को व्यापक प्रशिक्षण और बहुभाषी इंटरफेस के माध्यम से समर्थन दिया जा रहा है।
- दूरस्थ क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की समस्याओं का समाधान ऑफ़लाइन डेटा संग्रह को सक्षम करके किया जा रहा है, जो ऑनलाइन होने पर समन्वयित होता है।
- गुणवत्ता नियंत्रण के उपायों में स्वचालित त्रुटि पहचान और पर्यवेक्षक समीक्षाएँ शामिल हैं, ताकि डेटा की विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके।
2027 की जनगणना भारत के लिए इसके गणना प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण छलांग का प्रतिनिधित्व करती है, जो सटीकता, दक्षता, और समावेशिता को बढ़ाती है। ऐतिहासिक चुनौतियों का सामना नवीन डिजिटल समाधानों के माध्यम से करते हुए, सरकार देश की एक व्यापक जनसांख्यिकीय प्रोफ़ाइल बनाने का लक्ष्य रखती है।
GS2/अंतरराष्ट्रीय संबंध
इस वर्ष के G7 शिखर सम्मेलन में ध्यान देने योग्य 5 बातें
स्रोत: भारतीय एक्सप्रेस
2025 का G7 शिखर सम्मेलन अल्बर्टा, कनाडा में होने जा रहा है, जो डोनाल्ड ट्रम्प की राजनीतिक परिदृश्य में वापसी के कारण महत्वपूर्ण वैश्विक ध्यान आकर्षित कर रहा है। यह सम्मेलन वैश्विक तनावों के बीच हो रहा है, विशेष रूप से इज़राइल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष और यूक्रेन में चल रहे युद्ध के संदर्भ में।
- ईरान-इज़राइल संघर्ष और परमाणु वार्ताओं पर ध्यान केंद्रित करना।
- यूक्रेन के लिए सैन्य और वित्तीय सहायता पर चल रही चर्चाएँ।
- वैश्विक व्यापार तनाव, विशेष रूप से अमेरिका द्वारा प्रमुख वस्तुओं पर लगाए गए शुल्क।
- जलवायु कार्रवाई की पहलों और जंगलों की आग के प्रति प्रतिक्रियाएँ।
- कनाडा-भारत तनाव के बीच भारत के निमंत्रण का महत्व।
- बढ़ता ईरान-इज़राइल संघर्ष: ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नियंत्रित करने और इज़राइल की सैन्य कार्रवाई के परिणामों को प्रबंधित करने के लिए वार्ताएँ प्रारंभिक चर्चाओं में प्रमुख रहीं। G7 नेताओं ने एक व्यापक मध्य पूर्व युद्ध से बचने के लिए प्रतिबंधों और कूटनीतिक रणनीतियों पर विचार किया।
- चल रहा रूस-यूक्रेन युद्ध: यूक्रेन के लिए निरंतर सैन्य और वित्तीय सहायता सुनिश्चित करना प्राथमिकता बनी रही। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने नवीनतम जानकारी दी, जबकि कनाडा और यूरोप ने नए सहायता पैकेज का प्रस्ताव रखा, जो ट्रम्प के तहत अमेरिका की सतर्क स्थिति के विपरीत था।
- वैश्विक व्यापार संघर्ष: अमेरिका द्वारा स्टील, एल्यूमीनियम और फेंटेनिल से जुड़े सामानों पर लगाए गए बढ़ते शुल्क ने भागीदारों से प्रतिकृतियों को जन्म दिया। कनाडा ने अमेरिका के साथ द्विपक्षीय चर्चाओं के दौरान स्टील और ऑटोमोबाइल पर शून्य-शुल्क समझौते का समर्थन किया।
- जलवायु कार्रवाई और संसाधन: नेताओं ने जंगलों की आग के प्रति प्रतिक्रियाएँ, कार्बन-मुक्त होने के प्रयास और स्वच्छ प्रौद्योगिकी के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के लिए संक्षिप्त संयुक्त बयान जारी किए, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियों के लिए लिथियम और निकल उत्पादन को बढ़ाने के लिए सहयोग किया।
- ट्रम्प का प्रभाव: ट्रम्प की अप्रत्याशित कूटनीतिक शैली, जैसा कि 2018 के क्यूबेक G7 के दौरान देखा गया था, वार्ताओं को आकार दे सकती है। उनके पिछले कार्य, जिसमें जल्दी प्रस्थान और संयुक्त विज्ञप्ति को समर्थन देने से इनकार करना शामिल है, तनाव पैदा करते हैं। उनके द्वारा लगाए गए शुल्क और ध्रुवीकृत बयानों का मेज़बान देशों की घरेलू राजनीति पर प्रभाव पड़ सकता है।
मध्य पूर्व के संघर्ष और रूस-यूक्रेन स्थिति ने G7 के एजेंडे को सुरक्षा और रक्षा सहयोग की ओर मोड़ दिया है, जिससे सदस्य देशों के बीच एकता की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। भारत को दिया गया निमंत्रण तनावपूर्ण कूटनीतिक संबंधों को सुधारने और वैश्विक शासन में भारत की बढ़ती भूमिका को मान्यता देने के प्रयास को दर्शाता है।
महासागर का अंधकार: एक नई पारिस्थितिकी संकट
स्रोत: भारतीय एक्सप्रेस
प्लायमाउथ विश्वविद्यालय के एक हालिया अध्ययन ने एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी मुद्दे को उजागर किया है: पिछले दो दशकों में वैश्विक महासागर का 21% से अधिक हिस्सा महत्वपूर्ण रूप से अंधकारमय हो गया है।
- महासागर का अंधकार महासागर की ऊपरी परतों में सूर्य के प्रकाश की कमी को संदर्भित करता है, जो समुद्री जीवन के लिए महत्वपूर्ण है।
- फोटिक क्षेत्र, जो 200 मीटर तक फैला होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, जो समुद्री जैव विविधता का समर्थन करता है।
- प्रमुख निष्कर्षों से पता चलता है कि कुछ महासागरीय क्षेत्रों ने महत्वपूर्ण प्रकाश प्रवेश खो दिया है, जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर रहा है।
- महासागर का अंधकार: इस घटना को फैलाव अवशोषण गुणांक (Kd 490) का उपयोग करके मापा जाता है, जो यह आकलन करता है कि समुद्री पानी के माध्यम से यात्रा करते समय प्रकाश कितनी तेजी से कम होता है।
- हालिया निष्कर्ष: "वैश्विक महासागर का अंधकार" (2024) शीर्षक अध्ययन में रिपोर्ट की गई है कि 2003 से 2022 के बीच, महासागर का 9% हिस्सा प्रकाश प्रवेश में 50 मीटर से अधिक की कमी का अनुभव कर चुका है, जिसका क्षेत्र अफ्रीका के बराबर है।
- प्रभावित क्षेत्र: आर्कटिक, अंटार्कटिक, गल्फ स्ट्रीम और उत्तर सागर सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में शामिल हैं।
- कारण: कारकों में पोषक तत्वों के बहाव से होने वाले शैवाल के फूल, गर्म हो रहे समुद्र, प्लवक गतिशीलता में बदलाव, और महासागरीय धाराओं में परिवर्तन शामिल हैं।
- परिणाम: यह अंधकार पारिस्थितिकी तंत्र में विघटन, समुद्री आवासों की हानि, कार्बन अवशोषण में कमी, और वैश्विक मछली पकड़ने को खतरे में डालता है।
शोधकर्ता इस बात पर जोर देते हैं कि यदि इस उभरते संकट को तुरंत संबोधित नहीं किया गया, तो यह समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को मौलिक रूप से बदल सकता है।
UPSC 2025
पृथ्वी ग्रह के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- I. वर्षा वन महासागरों की तुलना में अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं।
- II. समुद्री फाइटोप्लांकटन और प्रकाश संश्लेषण करने वाले बैक्टीरिया दुनिया की लगभग 50% ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं।
- III. अच्छी ऑक्सीजन युक्त सतह का पानी वायुमंडलीय हवा की तुलना में कई गुना अधिक ऑक्सीजन रखता है।
उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
- विकल्प: (a) I और II (b) केवल II * (c) I और III (d) उपरोक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है
प्रधानमंत्री मोदी का साइप्रस गणराज्य का दौरा
स्रोत: पीएम इंडिया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में साइप्रस का राज्य दौरा किया, जो कि पिछले बीस वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का द्वीप पर पहला दौरा है। यह यात्रा महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसने भारत और साइप्रस के बीच रणनीतिक संबंधों और दीर्घकालिक मित्रता को उजागर किया।
- पीएम मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स के साथ चर्चा की।
- भारत ने साइप्रस की संप्रभुता को बाहरी दबावों, विशेष रूप से तुर्की से, समर्थन देने का पुनः आश्वासन दिया।
- प्रधानमंत्री को साइप्रस में सबसे उच्च नागरिक सम्मान, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकैरियोस III, से सम्मानित किया गया।
- दोनों देशों ने स्थायी महासागर शासन पर सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया।
- उन्होंने राजनीतिक संवाद और रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति जताई।
- साइप्रस की संप्रभुता के लिए समर्थन: भारत ने साइप्रस की क्षेत्रीय अखंडता और यूएन के नेतृत्व वाली शांति प्रयासों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, जिसमें बायज़ोनल और बायकम्युनल संघ के लिए समर्थन शामिल है।
- सुरक्षा सहयोग में वृद्धि: भारत और साइप्रस ने आतंकवाद की निंदा की और आतंकवाद-रोधी, साइबर सुरक्षा, और समुद्री सुरक्षा पर सहयोग करने का संकल्प लिया।
- आर्थिक साझेदारियां: साइप्रस-भारत व्यापार मंच की स्थापना और एआई और डिजिटल अवसंरचना जैसे तकनीकी क्षेत्रों में नवाचार की खोज के लिए योजनाओं पर चर्चा की गई।
- आवागमन और पर्यटन: नेताओं ने सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सीधे हवाई संपर्क की आवश्यकता पर जोर दिया।
- कार्य योजना (2025-2029): द्विपक्षीय सहयोग के मार्गदर्शन के लिए एक व्यापक कार्य योजना पर सहमति बनी, जो रणनीतिक क्षेत्रों पर केंद्रित होगी।
अपने दौरे के दौरान, पीएम मोदी की ऐतिहासिक निकोसिया केंद्र में प्रतीकात्मक उपस्थिति, जो तुर्की द्वारा नियंत्रित उत्तरी साइप्रस की ओर देखता है, ने क्षेत्र में चल रही तनावों के बीच साइप्रस के प्रति भारत की एकजुटता को और अधिक प्रदर्शित किया। यह यात्रा उस महत्वपूर्ण समय पर हुई है जब भारत के तुर्की के साथ संबंध तनाव में हैं, विशेष रूप से कश्मीर से संबंधित मुद्दों को लेकर।
|
3144 docs|1049 tests
|
FAQs on UPSC Daily Current Affairs(Hindi)- 17th June 2025 - Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly
| 1. सोवा-रिग्पा चिकित्सा क्या है और इसके प्रमुख तत्व क्या हैं? |  |
| 2. काली टाइगर रिजर्व के बारे में प्रमुख तथ्य क्या हैं? |  |
| 3. भारत की वित्तीय समेकन की दिशा में प्रमुख ताकतें और कमियाँ क्या हैं? |  |
| 4. PRASHAD योजना का उद्देश्य क्या है? |  |
| 5. महासागर के अंधकार से क्या तात्पर्य है और यह पारिस्थितिकी संकट कैसे है? |  |
















