साखियों का प्रतिपाद्य: साखी | Hindi Class 10 PDF Download
‘साखी’ शब्द का अर्थ
‘साखी’ शब्द ‘साक्षी’ शब्द का ही तद्भव रूप है। ‘साक्षी’ शब्द साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है - प्रत्यक्ष ज्ञान। यह ज्ञान गुरु अपने शिष्य को प्रदान करता है। ‘साखी’ वस्तुतः दोहा छंद है जिसका लक्षण है 13 और 11 के विश्राम से 24 मात्रा और अंत में जगण। प्रस्तुत पाठ की साखियाँ प्रमाण हैं कि सत्य की साक्षी देता हुआ ही गुरु शिष्य को जीवन के तत्वज्ञान की शिक्षा देता है। यह शिक्षा जितनी प्रभावपूर्ण होती है उतनी ही याद रह जाने योग्य भी।
साखियों का प्रतिपाद्य
कबीर इस पाठ में संकलित साखियों के माध्यम से कबीरदास जी मनुष्य को नीति का संदेश देते हैं।
पहली साखी के द्वारा कबीरदास जी मीठी वाणी के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। मीठी वाणी बोलने वाले तथा सुनने वाले दोनों को सुख पहुँचाती है।
दूसरी साखी में कबीरदस जी कहते हैं कि ईश्वर तो प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे चारों ओर ढूँढ़ता फिरता है। जिस प्रकार कस्तूरीमृग अपनी कस्तूरी को सारे वन में ढूँढ़ता फिरता है, उसी प्रकार मनुष्य ईश्वर को अन्यत्रा ढूँढ़ता रहता है।
तीसरी साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि अहं के मिटने पर ही ईश्वर की प्राप्ति होती है तथा अज्ञान रूपी अंध्कार मिट जाता है।
चैाथी साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि साध्क ‘विचारक’ ही दुखी और चिंतामग्न है तथा वह ईश्वर के लिए सदा व्याकुल रहता है।
पाँचवीं साखी में कबीरदास जी विरह की व्याकुलता के विषय में बताते हैं कि राम यानी ईश्वर के विरह में व्याकुल व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। अगर वह जीवित रहता भी है तो वह पागल हो जाता है।
छठी साखी में कबीरदास जी निंदक का महत्व स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि निंदक साबुन तथा पानी के बिना ही स्वभाव को निर्मल कर देता है।
सातवीं साखी में कबीरदास जी केवल पुस्तक पढ़-पढ़कर पंडित बने लोगों की निंदा करते हैं तथा सच्चे मन से प्रभु का नाम स्मरण करने को महत्व देते हैं।
आठवीं साखी में कबीरदास जी विषय-वासना रूपी बुराइयों को दूर करने की बात करते हैं।
इस प्रकार सभी साखियाँ मनुष्य को नीति संबंधी संदेश देती हैं।
1.
ऐसी बाँणी बोलिये, मन का आपा खोइ।
अपना तन सीतल करै, औरन कौं सुख होइ।।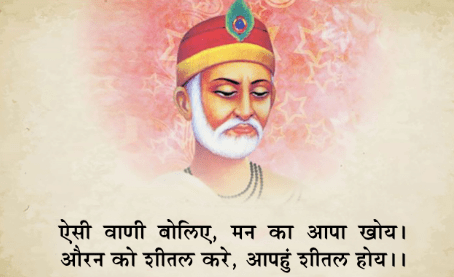
व्याख्या: कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ऐसी बोली बोलनी चाहिए जो हमारे हृदय के अहंकार को मिटा दे अर्थात जिसमें हमारा अहं न झलकता हो, जो हमारे शरीर को भी ठंडक प्रदान करे तथा दूसरों को भी सुख प्रदान करे। तात्पर्य यह है कि हमारे तन को शीतलता प्रदान करे तथा सुनने वाले ‘श्रोता’ को भी मानसिक सुख प्रदान करे।
काव्य-सौंदर्य:
भाव पक्ष:
- वाणी की मधुरता का महत्व बताया गया है।
कला पक्ष:
- सहज एवं सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा भावाभिव्यक्ति में सक्षम है।
- ‘बाँणी बोलिए’ में अनुप्रास अलंकार है।
- सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है।
2.
कस्तूरी कुंडलि बसै, मृग ढूँढै़ बन माँहि।
ऐसैं घटि घटि राँम है, दुनियाँ देखै नाँहि।।
व्याख्या: कबीरदास जी उदाहरण द्वारा ईश्वर की महत्ता स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि कस्तूरी तो हिरन की नाभि में स्थित होती है, परंतु वह उसे वन में ढूँढ़ता पिफरता है अर्थात वह अपने अंदर बसी कस्तूरी को नहीं पहचान पाता है। यही स्थिति मनुष्य की भी है। ईश्वर तो प्रत्येक हृदय में निवास करता है और मनुष्य उसे इध्र-उध्र ढूँढ़ता पिफरता है अर्थात मनुष्य अपने भीतर ईश्वर को न ढूँढ़कर उसे प्राप्त करने के लिए स्थान-स्थान पर यानी मंदिर-मस्जिद में भटकता रहता है।
काव्य-सौंदर्य:
भाव पक्ष:
- कबीर ने ईश्वर का स्थायी निवास मनुष्य के हृदय को ही बताया है।
- मृग का उदाहरण देकर बात को पूर्ण रूप से स्पष्ट किया गया है।
कला पक्ष:
- सरल एवं सहज सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है।
- कस्तूरी-वुंफडलि’, ‘दुनिया-देखै’ में अनुप्रास अलंकार है।
- ‘घटि-घटि’ में पुनरुक्तिप्रकाश अलंकार है।
3.
जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाँहि।
सब अँध्यिारा मिटि गया, जब दीपक देख्या माँहि।।
व्याख्या: कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मेरे अंदर अहंकार था, तब तक मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब जब कि मेरे अंदर का अहं मिट चुका है, तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है। जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक के दर्शन कर लिए, तब अज्ञान रूपी अंध्कार मिट गया अर्थात अहं भाव को त्याग कर ही मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है।
काव्य-सौंदर्य:
भाव पक्ष:
- इसमें ईश्वर-प्राप्ति का उपाय बताया गया है।
- ‘अहं’ भाव को ईश्वर-प्राप्ति में बाध्क बताया गया है।
कला पक्ष:
- ‘मैं’ शब्द अहंभाव के लिए प्रयोग किया गया है।
- ‘हरि है’, ‘दीपक देख्या’ में अनुप्रास अलंकार है।
- ‘अँध्यिारा’ अज्ञान का प्रतीक है और ‘दीपक’ ज्ञान का प्रतीक।
4.
सुखिया सब संसार है, खायै अरू सोवै।
दुखिया दास कबीर है, जागै अरू रोवै।।
व्याख्या: कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार सुखी है क्योंकि यह केवल खाने और सोने का काम करता है अर्थात सब प्रकार की ¯चताओं से परे है। इनमें दुखी केवल कबीरदास हैं क्योंकि वे ही जागते हैं और रोते हैं। आशय यह है कि सांसारिक सुखों में व्यस्त रहने वाले व्यक्ति सुखपूर्वक समय व्यतीत करते हैं और जो प्रभु के वियोग में जागते रहते हैं, उन्हें कहीं भी चैन नहीं मिलता। वे तो केवल संसार की दशा देखकर रोते रहते हैं। चिंतनशील मनुष्य कभी भी चैन की नींद नहीं सो सकता।
काव्य-सौंदर्य:
भाव पक्ष:
- चिंतनशील मनुष्य की व्याकुलता को प्रकाशित किया गया है।
कला पक्ष:
- भाषा सहज-सरल है और भावाभिव्यक्ति में सक्षम है।
- ‘सुखिया सब संसार’, ‘दुखिया दास’ में अनुप्रास अलंकार है।
- सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है।
5.
बिरह भुवंगम तन बसै, मंत्रा न लागै कोइ।
राम बियोगी ना जिवै, जिवै तो बौरा होइ।।
व्याख्या: कबीरदास जी विरही मनुष्य की मनःस्थिति की चर्चा करते हुए कहते हैं कि विरह रूपी सर्प शरीर में निवास करता है। उस पर किसी प्रकार का उपाय या मंत्र भी असर नहीं करता। उसी प्रकार राम यानी ईश्वर के वियोग में मनुष्य भी जीवित नहीं रह सकता। यदि वह जीवित रह भी जाता है तो उसकी स्थिति पागल व्यक्ति जैसी हो जाती है।
काव्य-सौंदर्य:
भाव पक्ष:
- राम-वियोगी मनुष्य की दशा का मार्मिक चित्राण किया गया है।
- विरह की तुलना सर्प से की गई है।
कला पक्ष:
- भाषा सरस-सरल और भावाभिव्यक्ति में सक्षम है।
- ‘बिरह भुवंगम’ में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है।
- सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है।
6.
निंदक नेड़ा राखिये, आँगणि कुटी बँधाइ।
बिन साबण पाँणीं बिना, निरमल करै सुभाइ।।
व्याख्या: कबीरदास जी कहते हैं कि निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने पास रखना ही चाहिए, हो सके तो उसे अपने आँगन में कुटिया ‘झोंपड़ी’ बनाकर रखना चाहिए। वह हमें साबुन और पानी के प्रयोग के बिना ही हमारे स्वभाव को स्वच्छ कर देता है अर्थात अपनी निंदा सुनकर हम अपनी त्राुटियों को सुधर लेते हैं। इससे हमारी स्वभावगत बुराइयाँ दूर हो जाती हैं।
काव्य-सौंदर्य:
भाव पक्ष:
- इसमें निंदक के महत्व को दर्शाया गया है।
- निंदक को अपना परम हितैषी समझना चाहिए।
कला पक्ष:
- भाषा सहज एवं सरल है तथा भावाभिव्यक्ति में सक्षम है।
- ‘निंदक-नेड़ा’ में अनुप्रास अलंकार है।
- सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है।
7.
पोथी पढ़ि पढ़ि जग मुवा, पंडित भया न कोइ।
ऐके अषिर पीव का, पढ़ै सु पंडित होइ।।
शब्दार्थ: पोथी = पुस्तक, ग्रंथ, पढ़ि-पढ़ि = पढ़-पढ़ कर, जग = संसार, मुवा = मर गया, भया = हुआ, बना, ऐके = एक ही,
कोइ = कोई, अषिर = अक्षर, पीव = प्रियतम, ईश्वर।
व्याख्या: कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार पुस्तकें पढ़-पढ़ कर मृत्यु को प्राप्त हो गया, परंतु अभी तक कोई भी पंडित नहीं बन सका। यदि मनुष्य ईश्वर-भक्ति का एक अक्षर भी पढ़ लेता तो वह अवश्य ही पंडित बन जाता अर्थात ईश्वर ही एकमात्र सत्य है, इसे जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी और पंडित होता है।
काव्य-सौंदर्य:
भाव पक्ष:
- ईश्वर-प्रेम तथा ईश्वर-भक्ति से ही ज्ञान-प्राप्ति होती है।
- पुस्तकों को पढ़कर ‘रट कर’ ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है।
कला पक्ष:
- भाषा सहज एवं सरल है तथा भावाभिव्यक्ति में सक्षम है।
- ‘पोथी पढ़ि पढ़ि’ में अनुप्रास अलंकार है।
- सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है।
8.
हम घर जाल्या आपणाँ, लिया मुराड़ा हाथि।
अब घर जालौं तास का, जे चलै हमारे साथि।।
शब्दार्थ: जाल्या = जलाया, आपणाँ = अपना, मुराड़ा = जलती हुई लकड़ी, जालौं = जलाउँ, तास का = उसका, जे = जो।
व्याख्या: कबीरदास जी कहते हैं कि हमने पहले अपना घर जलाया, पिफर जलती हुई लकड़ी को हाथ में ले लिया। अब हम उसका घर जलाएँगे, जो हमारे साथ चलेगा अर्थात पहले हम ने अपने घर की बुराइयाँ नष्ट की और अब हम अपने साथियों की बुराइयाँ दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाने चल पड़े हैं।
काव्य-सौंदर्य:
भाव पक्ष:
- कबीरदास जी समाज को सुधरने का महान कार्य करना चाहते हैं।
- वे चारों ओर ज्ञान की ज्योति प्रज्ज्वलित करना चाहते हैं।
कला पक्ष:
- भाषा सहज एवं सरल है तथा भावाभिव्यक्ति में सक्षम है।
- घर एवं मशाल का प्रतीकात्मक प्रयोग किया गया है।
- सधुक्कड़ी भाषा और प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है।
|
32 videos|436 docs|69 tests
|
FAQs on साखियों का प्रतिपाद्य: साखी - Hindi Class 10
| 1. साखियों का अर्थ क्या है और यह किस प्रकार की कविता होती है? |  |
| 2. साखियों में किस प्रकार के विषयों पर चर्चा की जाती है? |  |
| 3. साखियों का उपयोग किस प्रकार किया जाता है? |  |
| 4. साखियों के प्रमुख रचनाकार कौन हैं? |  |
| 5. साखियों का प्रयोग कक्षा 10 की परीक्षा में किस प्रकार किया जाता है? |  |






















