संयुक्त राष्ट्र संघ और वैश्विक विवाद | इतिहास वैकल्पिक UPSC (नोट्स) PDF Download
संयुक्त राष्ट्र संगठन (UNO) का गठन और उद्देश्य
- संयुक्त राष्ट्र संगठन (UNO) एक अंतरसरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना अक्टूबर 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद की गई। इसका मुख्य उद्देश्य भविष्य में संघर्षों को रोकना और विश्व भर में शांति को बढ़ावा देना है।
- UNO का गठन लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर किया गया था, जो शांति बनाए रखने में असफल सिद्ध हुई थी। UNO के गठन में मुख्य शक्तियों का लक्ष्य उन कमजोरियों को संबोधित करना था, जिन्होंने लीग के प्रयासों को बाधित किया।
- संयुक्त राष्ट्र का चार्टर, जो संगठन के सिद्धांतों और लक्ष्यों को रेखांकित करता है, 1945 में सैन फ्रांसिस्को में तैयार किया गया। यह 1944 में Dumbarton Oaks, अमेरिका में हुई एक पूर्व बैठक में चर्चा किए गए प्रस्तावों पर आधारित था, जिसमें USSR, USA, चीन और ब्रिटेन के प्रतिनिधि शामिल थे।
- संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय 51 सदस्य राज्य थे। आज, संगठन में 193 सदस्य राज्य शामिल हैं, जिसमें दक्षिण सूडान नवीनतम जोड़ है।
- संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय मैनहट्टन, न्यूयॉर्क शहर में स्थित है, जहां इसे एक्स्ट्राटेरिटोरियलिटी का विशेषाधिकार प्राप्त है, अर्थात् यह स्थानीय कानूनों के अधीन नहीं है।
- संयुक्त राष्ट्र के अन्य प्रमुख कार्यालय जिनेवा, नैरोबी और वियना में हैं।
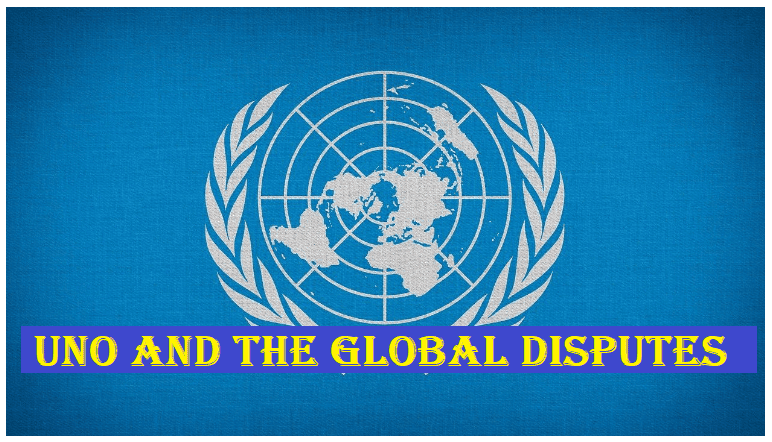
संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य:
- शांति बनाए रखना: UN वैश्विक शांति को बनाए रखने और युद्धों को रोकने का प्रयास करता है।
- संघर्ष के कारणों का समाधान: यह संघर्षों के मूल कारणों को समाप्त करने के लिए आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक प्रगति को बढ़ावा देता है, विशेषकर अविकसित देशों में।
- मानव अधिकारों की रक्षा करना: संगठन व्यक्तिगत मानवों के अधिकारों के साथ-साथ जन और राष्ट्रों के अधिकारों की सुरक्षा के प्रति समर्पित है।
UN प्रणाली के एजेंसियाँ:
- संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में विभिन्न विशेष एजेंसियाँ शामिल हैं, जैसे कि विश्व बैंक समूह, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व खाद्य कार्यक्रम, यूनेस्को, और यूनिसेफ। ये एजेंसियाँ विशिष्ट कार्यों का पालन करती हैं और संयुक्त राष्ट्र के समग्र मिशन में योगदान करती हैं। गैर-सरकारी संगठन (NGOs) भी आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) और अन्य एजेंसियों के साथ सलाहकार स्थिति प्राप्त करके संयुक्त राष्ट्र के कार्यों में भाग ले सकते हैं।
पहचान:
- संयुक्त राष्ट्र को 2001 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो इसके शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के प्रयासों को मान्यता देता है। इसके अतिरिक्त, इसके कई अधिकारियों और एजेंसियों को भी उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र के कार्यों के प्रभाव और महत्व को उजागर करता है।
पृष्ठभूमि और निर्माण
संयुक्त राष्ट्र (UN) की स्थापना से पहले के शताब्दी में, विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संधि संगठनों और सम्मेलनों की शुरुआत की गई। इन प्रारंभिक प्रयासों ने वैश्विक सहयोग की नींव रखी। राज्यों द्वारा विशिष्ट मुद्दों को संबोधित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठनों का गठन किया गया। उदाहरण के लिए:
- अंतरराष्ट्रीय टेलीक्राम यूनियन की स्थापना 1865 में हुई।
- अंतरराष्ट्रीय टेलीग्राफ यूनियन और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना 1874 में हुई, जो अब UN की विशेष एजेंसियां हैं।
1899 में, अंतरराष्ट्रीय शांति सम्मेलन हाग में आयोजित हुआ, जिसका ध्यान शांतिपूर्ण संकट समाधान, युद्ध रोकथाम और युद्ध के नियमों के संहिताकरण पर था। इसके परिणामस्वरूप अंतरराष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संधि को अपनाया गया और स्थायी मध्यस्थता न्यायालय की स्थापना की गई, जो 1902 में क्रियाशील हुआ।
राष्ट्रों के बीच संघर्षों को प्रबंधित करने के लिए, अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति और 1899 तथा 1907 के हाग कन्वेंशन्स बनाए गए।
- प्रथम विश्व युद्ध के बाद, पैरिस शांति सम्मेलन ने वर्साय संधि के तहत राष्ट्रों की लीग की स्थापना की, जिसका उद्देश्य राष्ट्रों के बीच शांति बनाए रखना था।
- लीग ने कुछ क्षेत्रीय विवादों को संबोधित किया और डाक सेवा, विमानन, और अफीम नियंत्रण जैसे क्षेत्रों के लिए अंतरराष्ट्रीय ढांचे की स्थापना की, जिनमें से कुछ बाद में UN में शामिल किए गए।
- हालांकि, लीग को उपनिवेशी जनसंख्या (जो उस समय दुनिया की कुल जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा थी) के लिए प्रतिनिधित्व की कमी और अमेरिका तथा सोवियत संघ जैसे प्रमुख शक्तियों की अनुपस्थिति के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
- लीग ने महत्वपूर्ण घटनाओं, जैसे 1931 में जापानी आक्रमण, 1935 में द्वितीय इतालवी-एथियोपियाई युद्ध, 1937 में चीन पर जापानी आक्रमण, और एडोल्फ हिटलर के तहत आक्रामक विस्तार, का प्रभावी रूप से जवाब देने में संघर्ष किया, जो अंततः द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना।
- लीग केवल उन मुद्दों को संबोधित करने में सफल रही, जहाँ प्रमुख शक्तियों के हित दांव पर नहीं थे। इसका निर्णय लेने की प्रक्रिया सहमति पर आधारित थी, जो समझौतों तक पहुँचने में कठिनाई उत्पन्न करती थी।
अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन भी वर्साय संधि के तहत लीग की एक संबंधित एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया था।
1942 “संयुक्त राष्ट्रों की घोषणा” द्वितीय विश्व युद्ध के सहयोगियों द्वारा
एटलांटिक चार्टर:
- जर्मनी के सफल हमलों के जवाब में ब्रिटेन, ग्रीस, और यूगोस्लाविया पर, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट ने 9-10 अगस्त, 1941 को न्यूफाउंडलैंड के प्लासेंटिया बे में USS प्रिंस ऑफ वेल्स पर बैठक की। इस बैठक में उन्होंने अपने-अपने युद्ध लक्ष्यों पर चर्चा की और युद्ध के बाद के अंतरराष्ट्रीय प्रणाली का खाका तैयार किया। उस समय, जर्मनी ने सोवियत संघ में प्रवेश किया था और मिस्र पर हमले की तैयारी कर रहा था, जबकि दोनों नेताओं को जापान के दक्षिण-पूर्व एशिया में इरादों के बारे में चिंता थी।
- चर्चिल और रूजवेल्ट के अपने-अपने कारण थे एटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर करने की इच्छा के लिए। उन्होंने उम्मीद की कि चार्टर अमेरिकी जनमत को युद्ध में शामिल होने की ओर मोड़ देगा। हालांकि, उन्हें निराशा मिली क्योंकि अमेरिकियों ने पर्ल हार्बर पर जापानी बमबारी के बाद तक युद्ध में शामिल होने का विचार अस्वीकार किया।
- एटलांटिक चार्टर का निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के बीच जर्मन आक्रामकता के खिलाफ एकता प्रदर्शित करने के लिए किया गया था। इसका उद्देश्य मनोबल बढ़ाना था और इसे कब्जे वाले क्षेत्रों में गिराए जाने वाले पर्चों में भी बदला गया था।
इस चार्टर में आठ “सामान्य सिद्धांतों” को शामिल किया गया था, जिनके प्रति संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन ने युद्ध के बाद की दुनिया में समर्थन देने का संकल्प लिया:
- कोई देश क्षेत्रीय या अन्य वृद्धि की खोज नहीं करेगा।
- संबंधित लोगों की स्वतंत्र रूप से व्यक्त इच्छाओं के बिना कोई क्षेत्रीय परिवर्तन नहीं होगा।
- सभी लोगों को अपनी सरकार के रूप को चुनने का अधिकार होगा, और उन लोगों को जिनसे जबरन यह अधिकार छीन लिया गया है, उन्हें संप्रभु अधिकार और आत्म-शासन बहाल किया जाएगा।
- सभी राज्यों के लिए व्यापार और कच्चे माल की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी, चाहे उनका आकार या स्थिति कोई भी हो।
- श्रम मानकों, आर्थिक उन्नति, और सामाजिक सुरक्षा में सुधार के लिए सभी राष्ट्रों के बीच पूर्ण सहयोग की कोशिश की जाएगी।
- सभी देशों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला एक शांतिपूर्ण वातावरण स्थापित किया जाएगा।
- ऐसी शांति समुद्रों और महासागरों में स्वतंत्र पारगमन की अनुमति देनी चाहिए।
- सभी राष्ट्रों को बल प्रयोग को छोड़ देना चाहिए, और एक व्यापक और स्थायी सामान्य सुरक्षा प्रणाली की स्थापना तक निरस्त्रीकरण आवश्यक माना जाएगा।
एटलांटिक चार्टर को चर्चिल और रूजवेल्ट ने 14 अगस्त, 1941 को जारी किया, इससे पहले कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो। यह अमेरिका और ब्रिटेन के युद्ध लक्ष्यों का एक व्यापक बयान प्रदान करता है।
अटलांटिक चार्टर का प्रभाव:
- अटलांटिक चार्टर, जबकि यह विश्व युद्ध II में अमेरिकी भागीदारी को प्रेरित नहीं करता, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम था। यह एक औपचारिक संधि नहीं थी बल्कि साझा नैतिकता और इरादे का एक बयान था, जिसका उद्देश्य कब्जे वाले देशों को आशा देना और अंतरराष्ट्रीय नैतिकता के आधार पर एक विश्व संगठन को बढ़ावा देना था।
चार्टर ने सफलतापूर्वक संयुक्त राष्ट्र बलों को नैतिक समर्थन प्रदान किया और अक्ष शक्तियों को एक शक्तिशाली संदेश भेजा। इसके अतिरिक्त:
- संयुक्त राष्ट्र के देशों ने अटलांटिक चार्टर के सिद्धांतों को अपनाया, जिससे एक सामान्य उद्देश्य स्थापित हुआ।
- अटलांटिक चार्टर ने संयुक्त राष्ट्र के गठन की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक कदम के रूप में कार्य किया।
- इसे अक्ष शक्तियों द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के गठबंधन की शुरुआत के रूप में देखा गया, जिसने जापान में सैन्यवादी सरकार को मजबूत किया।
1 जनवरी 1942 को, अक्ष शक्तियों के साथ युद्ध में 26 देशों के प्रतिनिधियों ने वाशिंगटन में "संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषणा" पर हस्ताक्षर करने के लिए एकत्रित हुए, जिसने अटलांटिक चार्टर का समर्थन किया। इस दस्तावेज़ ने हस्ताक्षरकर्ता सरकारों को अधिकतम युद्ध प्रयासों के लिए प्रतिबद्ध किया और उन्हें एक अलग शांति बनाने से प्रतिबंधित किया।
- “संयुक्त राष्ट्र” नाम, जो राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा गढ़ा गया था, इस घोषणा में पहली बार उपयोग किया गया।
- अटलांटिक चार्टर से एक महत्वपूर्ण बदलाव धार्मिक स्वतंत्रता के प्रावधान का समावेश था, जिसे रूजवेल्ट के आग्रह के बाद स्टालिन ने मंजूरी दी।
- 1 मार्च 1945 तक, 21 अतिरिक्त राज्यों ने इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए।
- युद्ध के दौरान, “संयुक्त राष्ट्र” शब्द संयुक्त बलों के लिए आधिकारिक हो गया।
- शामिल होने के लिए, देशों को घोषणा पर हस्ताक्षर करना पड़ा और अक्ष शक्तियों के खिलाफ युद्ध की घोषणा करनी पड़ी।
संक्षेप में, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की यात्रा अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और संघर्षों का समाधान करने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय प्रयासों और समझौतों की एक श्रृंखला द्वारा अंकित हुई, जो अंततः विश्व युद्ध II के बाद एक नई विश्व व्यवस्था के गठन की ओर ले गई।
अन्य सम्मेलन और घोषणाएँ
क्यूबेक सम्मेलन:
अगस्त 1943 में, क्यूबेक सम्मेलन के दौरान, अमेरिकी विदेश मंत्री और ब्रिटिश विदेश मंत्री ने “सभी देशों की संप्रभु समानता” के सिद्धांत पर आधारित “एक सामान्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन” की घोषणा का मसौदा तैयार करने पर सहमति व्यक्त की। इसके बाद अक्टूबर 1943 में मास्को में एक विदेशी मंत्रियों के सम्मेलन के बाद एक औपचारिक घोषणा जारी की गई।
तेहरान बैठक:
- नवंबर 1943 में, राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट ने तेहरान में सोवियत प्रधानमंत्री जोसेफ स्टालिन के साथ एक बैठक के दौरान एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का प्रस्ताव रखा।
- यह संगठन सभी सदस्य देशों की एक सभा और सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर विचार करने के लिए 10 सदस्यीय कार्यकारी समिति होगी।
- रूजवेल्ट ने यह भी सुझाव दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, सोवियत संघ, और चीन “चार पुलिसकर्मी” के रूप में शांति को लागू करेंगे।
- इस अवधि के दौरान, सहयोगी प्रतिनिधियों ने कई कार्य-उन्मुख संगठनों की स्थापना की, जिनमें शामिल हैं:
- खाद्य और कृषि संगठन—मई 1943
- संयुक्त राष्ट्र राहत और पुनर्वास प्रशासन—नवंबर 1943
- संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक, और सांस्कृतिक संगठन—अप्रैल 1944
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक—जुलाई 1944
- अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन—नवंबर 1944
संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945
- 1945 में, 50 देशों के प्रतिनिधियों ने सैन फ्रांसिस्को में अंतरराष्ट्रीय संगठन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में एकत्र होकर संयुक्त राष्ट्र चार्टर का मसौदा तैयार किया।
- प्रतिनिधियों ने अपने विचारों को 1944 में डम्बार्टन ओक्स सम्मेलन के दौरान चीन, सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम, और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विकसित प्रस्तावों पर आधारित किया।
- चार्टर पर 26 जून 1945 को 50 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। पोलैंड, जो सम्मेलन में उपस्थित नहीं था, बाद में हस्ताक्षरित किया और 51 मूल सदस्य राज्यों में से एक बन गया।
- संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक रूप से 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया, जब चीन, फ्रांस, सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, और अन्य अधिकांश हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा चार्टर की पुष्टि की गई। यह दिन अब संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- सामान्य सभा और सुरक्षा परिषद की पहली बैठकें 6 जनवरी 1946 को लंदन के केंद्रीय हॉल वेस्टमिंस्टर में हुईं।
- सामान्य सभा ने संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय के लिए न्यूयॉर्क शहर को चुना, जो जिनेवा, वियना, और नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय की तरह अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र के रूप में नामित है।
- नॉर्वेजियन विदेश मंत्री Trygve Lie को पहले संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में चुना गया।
सदस्यता
- संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता उन सभी शांति-प्रिय राज्यों के लिए खुली है जो चार्टर के प्रतिबद्धताओं को स्वीकार करते हैं और उन्हें निभाने के लिए तैयार और सक्षम हैं।
- सामान्य सभा, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर, नए सदस्यों के प्रवेश पर निर्णय लेती है।
- संयुक्त राष्ट्र सामान्य सभा में दो गैर-सदस्य पर्यवेक्षक राज्य भी हैं: पवित्र सिंहासन और फिलिस्तीन राज्य।
संयुक्त राष्ट्र संगठन की संरचना
विश्वासिता परिषद:
ट्रस्टशिप काउंसिल, जिसे ट्रस्ट क्षेत्रों की निगरानी और उन्हें आत्म-शासन और स्वतंत्रता के लिए तैयार करने के लिए स्थापित किया गया था, 1994 में पलाऊ की स्वतंत्रता के साथ निष्क्रिय हो गया, जो कि अंतिम शेष यूएन ट्रस्ट क्षेत्र था। 1994 तक, सभी ट्रस्ट क्षेत्र आत्म-शासन या स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके थे।
आर्थिक और सामाजिक परिषद:
- आर्थिक और सामाजिक परिषद, जिसे यूएन चार्टर द्वारा स्थापित किया गया, संयुक्त राष्ट्र और इसके विशेष एजेंसियों के आर्थिक और सामाजिक कार्यों का समन्वय करता है।
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय:
- अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC), जो नीदरलैंड के हेग में स्थित है, एक अंतरसरकारी संगठन और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है जो अंतरराष्ट्रीय अपराधों जैसे कि जातीय सफाई, मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध, और आक्रमण के अपराधों के लिए व्यक्तियों का मुकदमा चलाता है।
- ICC का संचालन 1 जुलाई 2002 से शुरू हुआ, जब रोम संविधि प्रभाव में आई। रोम संविधि एक बहुपक्षीय संधि है जो ICC का मौलिक दस्तावेज है।
यूएन मुख्यालय और प्रमुख एजेंसियाँ:
- संयुक्त राष्ट्र के पांच प्रमुख अंगों में से चार न्यू यॉर्क शहर में मुख्य यूएन मुख्यालय में स्थित हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में है, जबकि अन्य प्रमुख एजेंसियाँ जिनेवा, विएना और नैरोबी में यूएन कार्यालयों में स्थित हैं।
- संयुक्त राष्ट्र की छह आधिकारिक भाषाएँ हैं: अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, और स्पेनिश।
- संयुक्त राष्ट्र के विशेषाधिकारों और छूटों पर कन्वेंशन के आधार पर, यूएन और इसके एजेंसियाँ उन देशों के कानूनों से मुक्त हैं जहां वे कार्यरत हैं, जिससे यूएन की निष्पक्षता सुनिश्चित होती है।
विशेष एजेंसियाँ:
संयुक्त राष्ट्र चार्टर प्रत्येक प्राथमिक अंग को विशेष एजेंसियों की स्थापना की अनुमति देता है ताकि वे अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। इनमें शामिल हैं:
- अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी
- खाद्य और कृषि संगठन
- यूनेस्को
- विश्व बैंक
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)
संयुक्त राष्ट्र अपने मानवीय कार्यों को मुख्य रूप से इन विशेष एजेंसियों के माध्यम से करता है।
नोबेलमेयर सिद्धांत:
- नोबेलमेयर सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय संगठनों, जिनमें संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के संगठन शामिल हैं, को समान कार्य के लिए समान वेतन देने की आवश्यकता करता है, चाहे सदस्य राज्यों के बीच वेतन में अंतर कितना भी क्यों न हो।
- यह सभी सदस्य देशों से कर्मचारियों की भर्ती और बनाए रखने की क्षमता की भी अनिवार्यता करता है।
- हालांकि, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), और उनके संबद्ध संगठन संयुक्त राष्ट्र के सामान्य वेतन और भत्तों के प्रणाली से बाहर हो गए हैं।
संयुक्त राष्ट्र और राष्ट्र संघ के बीच अंतर
- संयुक्त राष्ट्र अधिक सफल रहा है।
कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं जो संयुक्त राष्ट्र को राष्ट्र संघ की तुलना में एक अधिक सफल संगठन बनाने में सहायक रहे हैं।
- संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों पर बहुत अधिक समय और संसाधन खर्च करता है और इसका दायरा राष्ट्र संघ की तुलना में बहुत व्यापक है। सभी विशेष एजेंसियाँ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (जो 1919 में स्थापित हुआ) को छोड़कर, 1945 या उसके बाद स्थापित की गईं।
- संयुक्त राष्ट्र व्यक्तिगत मानव अधिकारों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है, जिसमें राष्ट्र संघ शामिल नहीं था।
- सामान्य सभा और सुरक्षा परिषद की प्रक्रियाओं में परिवर्तन (विशेष रूप से ‘शांति के लिए एकजुट होना’ प्रस्ताव) और महासचिव की बढ़ती शक्ति और प्रतिष्ठा ने संयुक्त राष्ट्र को कभी-कभी अधिक निर्णायक कार्रवाई करने में सक्षम बनाया, जो राष्ट्र संघ कभी नहीं कर सका।
- संयुक्त राष्ट्र का सदस्यता बहुत व्यापक है और इसलिए यह राष्ट्र संघ की तुलना में एक वास्तविक विश्व संगठन है, जिसके साथ यह अतिरिक्त प्रतिष्ठा आती है।
- संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में अमेरिका और सोवियत संघ दोनों शामिल थे, जबकि अमेरिका ने राष्ट्र संघ में कभी शामिल नहीं हुआ।
- 1963 से 1968 के बीच 43 नए सदस्य संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुए, मुख्य रूप से अफ्रीका और एशिया के उभरते राज्यों से। बाद में, कई पूर्व सोवियत संघ के सदस्य राज्यों ने शामिल होकर सदस्यता 193 तक पहुंचा दी; राष्ट्र संघ में कभी 50 से अधिक सदस्य नहीं थे।
राष्ट्र संघ की कुछ कमजोरियाँ अब भी मौजूद हैं:
- सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों में से कोई भी अपने वीटो का उपयोग करके निर्णायक कार्रवाई को रोक सकता है।
- जैसे राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र के पास अपनी स्थायी सेना नहीं है और इसे अपने सदस्य देशों की सेनाओं का उपयोग करना पड़ता है।
संयुक्त राष्ट्र एक शांति बनाए रखने वाले संगठन के रूप में कितना सफल रहा है?
हालांकि इसे मिश्रित सफलता मिली है, यह कहना उचित होगा कि संयुक्त राष्ट्र (UN) ने अपने शांति स्थापना प्रयासों में लीग की तुलना में अधिक सफलता प्राप्त की है, विशेष रूप से उन संकटों में जो महान शक्तियों के हितों से सीधे जुड़े नहीं थे, जैसे कि कांगो में गृहयुद्ध (1960-64) और नीदरलैंड और इंडोनेशिया के बीच पश्चिम न्यू गिनी का विवाद। दूसरी ओर, यह अक्सर लीग की तरह ही निरर्थक रहा है, विशेष परिस्थितियों में - जैसे कि 1956 का हंगेरियन संकट और 1968 का चेक संकट - जहां एक महान शक्ति के हित, इस मामले में सोवियत संघ (USSR), को खतरा महसूस हुआ और जहां महान शक्ति ने संयुक्त राष्ट्र की अनदेखी या उसकी अवहेलना करने का निर्णय लिया। तीसरी दुनिया की बढ़ती उपस्थिति और मध्य पूर्व, वियतनाम और कश्मीर में संघर्षों में संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता की विफलता के कारण, UN ने धीरे-धीरे अपने प्राथमिक लक्ष्यों से ध्यान हटाकर आर्थिक विकास और सांस्कृतिक विनिमय के अपने द्वितीयक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। 1970 के दशक तक, UN का बजट सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए शांति स्थापना बजट से काफी अधिक था।
संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न सफलताओं के स्तर को निम्नलिखित प्रमुख विवादों से देखा जा सकता है जिनमें यह शामिल रहा है।
- पश्चिम न्यू गिनी (1946): 1946 में संयुक्त राष्ट्र ने डच ईस्ट इंडीज, जो बाद में इंडोनेशिया बन गया, के लिए हॉलैंड से स्वतंत्रता की व्यवस्था करने में मदद की। हालांकि, पश्चिम न्यू गिनी (पश्चिम इरियन) के भविष्य के बारे में कोई समझौता नहीं हुआ, जिस पर दोनों देशों का दावा था। 1961 में लड़ाई छिड़ गई; यू थांत (संयुक्त राष्ट्र के महासचिव) ने दोनों पक्षों से बातचीत फिर से शुरू करने का अनुरोध किया, और 1962 में सहमति बनी कि यह क्षेत्र इंडोनेशिया का हिस्सा बनेगा। इस मामले में, संयुक्त राष्ट्र ने वार्ता को आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, हालांकि यह पश्चिम इरियन के भविष्य के बारे में निर्णय नहीं ले सका।
- पालेस्टाइन (1947): फिलिस्तीन में यहूदी और अरबों के बीच विवाद 1947 में संयुक्त राष्ट्र के समक्ष लाया गया। जांच के बाद, संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को विभाजित करने का निर्णय लिया, यहूदी राज्य इज़राइल की स्थापना की। यह संयुक्त राष्ट्र के सबसे विवादास्पद निर्णयों में से एक था, और इसे अधिकांश अरबों ने स्वीकार नहीं किया। संयुक्त राष्ट्र इज़राइल और विभिन्न अरब राज्यों के बीच श्रृंखला में युद्धों को रोकने में असफल रहा (1948-49, 1967 और 1973), हालांकि इसने संघर्ष विराम की व्यवस्था करने और निगरानी बल प्रदान करने में उपयोगी कार्य किया।
- कोरियाई युद्ध (1950-53): यह वह एकमात्र अवसर था जब संयुक्त राष्ट्र ने सीधे एक सुपरपावर के हितों को प्रभावित करने वाली संकट में निर्णायक कार्रवाई करने में सक्षम था। जब दक्षिण कोरिया पर कम्युनिस्ट उत्तर कोरिया ने जून 1950 में आक्रमण किया, तो सुरक्षा परिषद ने तुरंत उत्तर कोरिया की निंदा करने वाला एक प्रस्ताव पारित किया और सदस्य राज्यों से दक्षिण को मदद भेजने का आग्रह किया। हालांकि, यह केवल रूसियों के अस्थायी अनुपस्थिति के कारण संभव था, जो अगर सुरक्षा परिषद की बैठकों का बहिष्कार नहीं कर रहे होते तो इस प्रस्ताव को वीटो कर देते। 16 देशों की सेनाओं ने आक्रमण को रोकने और दोनों कोरियाओं के बीच 38वें समानांतर पर सीमा को बनाए रखने में सफलता प्राप्त की। हालांकि इसे पश्चिम ने एक महान संयुक्त राष्ट्र सफलता के रूप में प्रस्तुत किया, यह वास्तव में एक अमेरिकी ऑपरेशन था।
- सुएज़ संकट (1956): यह तर्क किया जा सकता है कि यह संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को दर्शाता है। जब मिस्र के राष्ट्रपति नासिर ने अचानक सुएज़ नहर का राष्ट्रीयकरण किया, जिसकी कई शेयरें ब्रिटेन और फ्रांस के पास थीं, तो इन दोनों शक्तियों ने बलपूर्वक अपना हितों की रक्षा करने का निर्णय लिया। उसी समय इजरायली सेना ने पूर्व से मिस्र पर आक्रमण किया। एक सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को ब्रिटेन और फ्रांस ने वीटो कर दिया, जिसके बाद सामान्य सभा ने 64 मतों के मुकाबले 5 मतों से आक्रमण की निंदा की और सैनिकों की वापसी की मांग की। संयुक्त राष्ट्र ने एक बल के रूप में 5000 सैनिकों को तैनात किया और ब्रिटिश, फ्रांसीसी और इजराइली घर लौट गए।
- हंगेरियन विद्रोह (1956): यह सुएज़ संकट के साथ-साथ हुआ और संयुक्त राष्ट्र को अपने सबसे निरर्थक रूप में दिखाया। जब हंगेरियन ने रूसी नियंत्रण से स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयास किया, तो सोवियत सैनिकों ने विद्रोह को कुचलने के लिए हंगरी में प्रवेश किया। हंगेरियन सरकार ने संयुक्त राष्ट्र से अपील की, लेकिन रूसियों ने उनके बलों की वापसी के लिए सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को वीटो कर दिया।
- कांगो में गृहयुद्ध (1960-64): यहां संयुक्त राष्ट्र ने अब तक का सबसे जटिल ऑपरेशन किया। जब कांगो (जिसे 1971 से ज़ैरे कहा जाता है) स्वतंत्रता प्राप्त करने के तुरंत बाद अराजकता में चला गया, तो संयुक्त राष्ट्र के 20,000 से अधिक सैनिकों ने किसी तरह स्थिति को सामान्य करने का प्रयास किया। एक विशेष संयुक्त राष्ट्र कांगो कोष स्थापित किया गया।
- किप्रस: 1878 से एक ब्रिटिश उपनिवेश, यह द्वीप 1960 में स्वतंत्रता दी गई। 1963 में ग्रीक और तुर्क के बीच गृहयुद्ध छिड़ गया। मार्च 1964 में संयुक्त राष्ट्र की शांति स्थापना बल तैनात की गई। हालांकि, शांति को बनाए रखने के लिए 3000 संयुक्त राष्ट्र सैनिकों की स्थायी तैनाती की आवश्यकता थी।
- कश्मीर: कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र को किप्रस की तरह ही स्थिति का सामना करना पड़ा। 1947 के बाद, यह बड़ा प्रांत जो भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, दोनों देशों द्वारा दावा किया गया। पहले ही 1948 में संयुक्त राष्ट्र ने संघर्ष विराम की व्यवस्था की। 1965 में पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र पर आक्रमण किया।
- चेक संकट (1968): यह लगभग 12 वर्ष पहले के हंगेरियन विद्रोह का पुनरावृत्ति था। जब चेक ने वह स्वतंत्रता दिखाई जो मास्को को पसंद नहीं आई, तो सोवियत और अन्य वारसॉ संधि के सैनिकों को भेजा गया।
- लेबनान: जबकि लेबनान में गृहयुद्ध चल रहा था (1975-87), स्थिति को और जटिलता में डाल दिया गया। मार्च 1978 में इजरायल ने दक्षिण लेबनान में प्रवेश किया। जून 1978 में इजरायल ने वापसी करने पर सहमति दी, बशर्ते संयुक्त राष्ट्र सीमा क्षेत्र की निगरानी करे।
- ईरान-इराक युद्ध (1980-88): संयुक्त राष्ट्र ने ईरान और इराक के बीच लंबे संघर्ष को समाप्त करने में सफलता प्राप्त की।
शीत युद्ध के अंत के बाद यूएन शांति रक्षा
शीत युद्ध के अंत ने संभावित संघर्षों के अंत को नहीं लाया। कई विवाद जो बहुत पहले उत्पन्न हुए थे, वे जारी रहे, और मध्य पूर्व जैसे क्षेत्रों में अस्थिरता बनी रही, जबकि दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका में समस्याएँ बढ़ीं। इस चल रही अस्थिरता के जवाब में, संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने अपनी शांति रक्षा जिम्मेदारियों को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया, शीत युद्ध के बाद के दशक में पिछले 40 वर्षों की तुलना में अधिक मिशन किए।
1988 से 2000 के बीच:
- अधिप्राप्त सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई।
- शांति रक्षा बजट दस गुना से अधिक बढ़ गया।
1990 से 2003 के बीच, यूएन ने 30 से अधिक शांति रक्षा अभियान चलाए। 1990 के दशक के मध्य में, 77 देशों से 80,000 से अधिक सैनिक शांति रक्षा प्रयासों में सक्रिय रूप से शामिल थे।
- 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक में, यूएन द्वारा अधिकृत अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेपों ने विभिन्न रूप धारण किए। उदाहरण के लिए, सिएरा लियोन के गृहयुद्ध (1991–2002) में यूएन मिशन को ब्रिटिश रॉयल मरीन द्वारा समर्थन मिला, और 2001 में अफगानिस्तान पर आक्रमण पर नाटो ने निगरानी की। यूएन ने सल्वाडोर के गृहयुद्ध के अंत की वार्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, नामीबिया में एक सफल शांति रक्षा मिशन प्रारंभ किया, और उत्तर-अपार्तheid दक्षिण अफ्रीका और उत्तर-खमेर रूज कंबोडिया में लोकतांत्रिक चुनावों की निगरानी की। 1991 में, यूएन ने इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण को रोकने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में एक गठबंधन को अधिकृत किया। हालांकि, ब्रायन उर्कहार्ट, जिन्होंने 1971 से 1985 तक अंडर-सेक्रेटरी-जनरल के रूप में कार्य किया, ने बाद में इन सफलताओं के चारों ओर के उत्साह का वर्णन "झूठे पुनर्जागरण" के रूप में किया, यह देखते हुए कि इसके बाद अधिक चुनौतीपूर्ण मिशन आए।
गुल्फ युद्ध (1991)
- 1991 के गल्फ युद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाई प्रभावशाली थी। जब इराक के सद्दाम हुसैन ने अगस्त 1990 में अपने सैनिकों को कुवैत पर आक्रमण करने और उसे कब्जा करने के लिए भेजा, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उन्हें वापस लौटने की चेतावनी दी या परिणामों का सामना करने को कहा। जब उन्होंने इनकार किया, तो सऊदी अरब में एक μεγάλο संयुक्त राष्ट्र बल भेजा गया। एक संक्षिप्त और निर्णायक अभियान में, इराकी सैनिकों को भारी नुकसान उठाते हुए बाहर निकाल दिया गया, और कुवैत को मुक्त कर दिया गया। हालाँकि, संयुक्त राष्ट्र के आलोचकों ने शिकायत की कि कुवैत को मदद केवल इसलिए मिली क्योंकि पश्चिम को उसके तेल की आपूर्ति की आवश्यकता थी; अन्य छोटे राष्ट्रों, जिनका पश्चिम के लिए कोई मूल्य नहीं था, को तब मदद नहीं मिली जब उन्हें बड़े पड़ोसियों द्वारा आक्रमण किया गया (उदाहरण के लिए, पूर्वी तिमोर, जिसे 1975 में इंडोनेशिया ने अपने कब्जे में ले लिया)।
कंबोडिया में शांति स्थापना कार्य:
- कंबोडिया में समस्याएँ लगभग दो दशकों तक चलती रहीं, लेकिन अंततः, संयुक्त राष्ट्र एक समाधान की व्यवस्था करने में सक्षम था। 1975 में, खमेर रूज, जो पोल पॉट के नेतृत्व में एक कम्युनिस्ट गोरिल्ला बल था, ने प्रिंस सिहानोक की दाएं-झुकाव वाली सरकार से सत्ता छीन ली। अगले तीन वर्षों में, पोल पॉट के क्रूर शासन ने जनसंख्या का लगभग एक तिहाई नष्ट कर दिया, जब तक कि 1978 में एक वियतनामी सेना ने देश पर आक्रमण नहीं किया। वियतनामी बलों ने खमेर रूज को बाहर निकाल दिया और एक नई सरकार स्थापित की।
- प्रारंभ में, संयुक्त राष्ट्र ने, अमेरिका के दबाव में, इस कार्रवाई की निंदा की, हालाँकि कई लोगों का मानना था कि वियतनाम ने क्रूर पोल पॉट शासन को हटाकर कंबोडियाई लोगों के लिए एक बड़ा कार्य किया है। हालाँकि, यह शीत युद्ध की गतिशीलता का हिस्सा था, जहाँ वियतनाम, जो कि यूएसएसआर का सहयोगी था, द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई अमेरिका द्वारा निंदा की जाती थी। शीत युद्ध के अंत ने संयुक्त राष्ट्र को एक समाधान को व्यवस्थित और पुलिस करने में सक्षम बनाया। वियतनामी बलों को सितंबर 1989 में वापस बुला लिया गया, और लंबे समय तक वार्ता और मनाने के बाद, जून 1993 में चुनाव हुए, जिससे देश की स्थिति में क्रमिक स्थिरीकरण हुआ।
मोजाम्बिक में शांति स्थापना कार्य:
- मोज़ाम्बिक, जिसने 1975 में पुर्तगाल से स्वतंत्रता प्राप्त की, कई वर्षों तक गृह युद्ध से प्रभावित रहा।
- 1990 तक, देश खंडहर में तब्दील हो चुका था, और दोनों पक्ष थक चुके थे।
- हालाँकि अक्टूबर 1992 में रोम में एक युद्धविराम समझौता हस्ताक्षरित हुआ था, जिसे रोमन कैथोलिक चर्च और इटालियन सरकार ने सुविधाजनक बनाया, लेकिन यह कायम नहीं रह सका।
- युद्धविराम का कई बार उल्लंघन हुआ, जिससे इस माहौल में चुनाव कराना असंभव हो गया।
- संयुक्त राष्ट्र पूरी तरह से शामिल हो गया, विभिन्न सेनाओं के demobilizing और disarming के लिए एक कार्यक्रम लागू किया, मानवता सहायता वितरित की, और चुनावों की तैयारी की।
- ये चुनाव अक्टूबर 1994 में सफलतापूर्वक हुए, जो देश को स्थिर करने में संयुक्त राष्ट्र की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी।
सोमालिया में शांति रक्षक ऑपरेशन:
- सोमालिया 1991 में गृह युद्ध में टूट गया जब तानाशाह सिआद बैरे को गिराया गया।
- जनरलों ऐडीद और अली मोहम्मद के प्रतिकूल समर्थकों के बीच शक्ति संघर्ष विकसित हुआ, जिससे एक अराजक स्थिति उत्पन्न हुई, जहाँ खाद्य आपूर्ति और संचार ठप हो गए, और हजारों शरणार्थी केन्या में भाग गए।
- आफ्रीकी एकता संगठन (OAU) ने संयुक्त राष्ट्र से सहायता की मांग की, और दिसंबर 1992 में 37,000 संयुक्त राष्ट्र सैनिकों का एक दल, मुख्य रूप से अमेरिकी, सहायता की सुरक्षा और युद्धlords के disarming के लिए आया।
- हालाँकि, युद्धlord, विशेष रूप से ऐडीद, disarmed होने के लिए तैयार नहीं थे, और संयुक्त राष्ट्र सैनिकों को नुकसान उठाना शुरू हो गया।
- अमेरिकियों ने मार्च 1994 में अपने सैनिकों को वापस ले लिया, और शेष संयुक्त राष्ट्र बलों को मार्च 1995 में वापस ले लिया गया, जिससे युद्धlords अपने संघर्ष को जारी रखने के लिए छोड़ दिए गए।
- यह संयुक्त राष्ट्र के लिए एक अपमानजनक पीछे हटना था, जिसने शुरुआत से ही एक असंभव कार्य निर्धारित किया था—दो शक्तिशाली सेनाओं को disarm करना जो लड़ाई जारी रखने के लिए दृढ़ संकल्पित थीं, साथ ही एक मानवीय राहत कार्यक्रम का प्रबंधन करना।
- इस समय के दौरान, संयुक्त राष्ट्र ने 1994 में रवांडा में हो रहे गृह युद्ध और नरसंहार में कोई कार्रवाई नहीं की।
- रवांडा के लिए संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन सुरक्षा परिषद में अनिर्णय के कारण रवांडा नरसंहार में हस्तक्षेप करने में विफल रहा।
- संयुक्त राष्ट्र की सैन्य हस्तक्षेप तब सबसे सफल होने की संभावना थी, जब, जैसे कोरिया (1950-1953) और खाड़ी युद्ध (1991) में, संयुक्त राष्ट्र सैनिकों ने एक पक्ष का सक्रिय रूप से समर्थन किया।
बोस्निया में शांति रक्षक ऑपरेशन:
- बोस्नियाई मुसलमानों और सर्बों के बीच गृहयुद्ध के दौरान, संयुक्त राष्ट्र (UN) कानून और व्यवस्था को लागू करने के लिए पर्याप्त सैनिकों को तैनात करने में असफल रहा। यह कमी आंशिक रूप से इस कारण से थी कि यूरोपीय समुदाय और अमेरिका दोनों ही इसमें भारी रूप से शामिल होने के लिए अनिच्छुक थे। जुलाई 1995 में, जब UN सर्ब बलों को दो शहरों, सरेब्रेनिका और जेपा, को कब्जा करने से रोकने में असमर्थ रहा, तो UN को और भी अपमान का सामना करना पड़ा, जिन्हें सुरक्षा परिषद ने मुसलमानों के लिए सुरक्षित क्षेत्र के रूप में नामित किया था। सरेब्रेनिका में लगभग 8,000 मुस्लिम पुरुषों की हत्या के दौरान UN की बेबसी को स्पष्ट रूप से उजागर किया गया। यह विफलता UN के लिए जटिल और अस्थिर संघर्ष स्थितियों में प्रभावी शांति अभियानों को लागू करने में सामना किए गए चुनौतियों और सीमाओं को उजागर करती है।
इराक में शांति अभियानों:
- मार्च 2003 में, अमेरिका और ब्रिटेन ने इराक पर आक्रमण किया, यह दावा करते हुए कि उनका इरादा वृद्धि करने वाले हथियारों को समाप्त करना और इराकी लोगों को सद्दाम हुसैन के दमनकारी शासन से मुक्त करना था। UN के हथियार निरीक्षक इन हथियारों की खोज कर रहे थे लेकिन उन्हें कुछ महत्वपूर्ण नहीं मिला। इसके बावजूद, आक्रमण UN सुरक्षा परिषद की मंजूरी के बिना आगे बढ़ा। अमेरिका और ब्रिटेन ने सुरक्षा परिषद से सैन्य कार्रवाई की स्वीकृति प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन फ्रांस, रूस, चीन और जर्मनी ने सद्दाम को हथियार निरीक्षकों के साथ सहयोग करने के लिए अधिक समय देने की इच्छा जताई। जब यह स्पष्ट हो गया कि फ्रांस और रूस किसी भी सैन्य कार्रवाई का समर्थन करने वाले प्रस्ताव को वीटो करेंगे, तो अमेरिका और ब्रिटेन ने एकतरफा आगे बढ़ने का निर्णय लिया। उनकी कार्रवाई का औचित्य यह था कि सद्दाम द्वारा पूर्व के UN प्रस्तावों का उल्लंघन सैन्य हस्तक्षेप का औचित्य प्रदान करता है। यह एकतरफा कार्रवाई UN की प्रतिष्ठा के लिए एक गंभीर झटका थी। महासचिव कोफी अन्नान ने कहा कि इस निर्णय ने UN को "एक मोड़ पर ला दिया"। उस बिंदु तक, किसी भी राज्य को आत्म-रक्षा से परे बल का उपयोग करने के लिए सुरक्षा परिषद की मंजूरी आवश्यक थी, जैसा कि UN चार्टर के अनुच्छेद 51 में वर्णित है। बान की-मून, आठवें महासचिव, ने डारफुर (सूडान) युद्ध और किवु संघर्ष (डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो) जैसे संकटों में शांति सैनिकों के साथ UN का नेतृत्व किया। UN ने सीरियाई गृहयुद्ध में पर्यवेक्षकों और रासायनिक हथियार निरीक्षकों को भी भेजा। हालांकि, 2013 में श्रीलंका के गृहयुद्ध के अंतिम लड़ाइयों के दौरान UN की कार्यों की आंतरिक समीक्षा में निष्कर्ष निकाला गया कि संगठन ने "संविधानिक विफलता" का अनुभव किया।
संयुक्त राष्ट्र संगठन का आकलन
संयुक्त राष्ट्र (UN) की प्रभावशीलता का आकलन मिश्रित रहा है। कुछ टिप्पणीकारों का मानना है कि यह संगठन शांति और मानव विकास के लिए एक महत्वपूर्ण बल है, जबकि अन्य इसे अप्रभावी, भ्रष्ट या पक्षपाती मानते हैं। UN लगभग आधी सदी से अस्तित्व में है, लेकिन यह अभी भी अपने मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने के करीब नहीं है। दुनिया अभी भी आर्थिक और सामाजिक समस्याओं से भरी हुई है; आक्रामकता और युद्ध जारी हैं। UN से जुड़े कई एजेंसियों और व्यक्तियों को उनके काम के लिए नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ है। दो महासचिव, डैग हैमरस्कजोल्ड और कोफी अन्नान, को भी यह पुरस्कार मिला है।
स्थायी UN सेना की कमी:
- UN की प्रणाली में कमजोरियाँ हैं जो इसकी विफलताओं में योगदान करती हैं। एक महत्वपूर्ण मुद्दा स्थायी UN सेना का अभाव है, जो निर्णयों को लागू करने में चुनौती उत्पन्न करती है, खासकर उन शक्तिशाली देशों के खिलाफ जो स्वार्थ को प्राथमिकता देते हैं।
- जब प्रेरणा और वैश्विक राय विफल होती है, तो UN सदस्य देशों से सैनिकों को प्रदान करने पर निर्भर करता है।
- ऐतिहासिक उदाहरण जैसे कि 1956 में यूएसएसआर द्वारा हंगरी से सैनिकों की वापसी के लिए UN की मांगों की अनदेखी और 1980 में अफगानिस्तान, इस सीमा को उजागर करते हैं।
- सोमालिया (1992-1995) और बोस्निया (1992-1995) में UN हस्तक्षेप ने यह साबित किया कि संगठन तब संघर्षों को रोकने में असमर्थ है जब संबंधित पक्ष संघर्ष समाप्त करने के लिए तैयार नहीं होते।
- 2003 में अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा UN की अनुमति के बिना इराक पर हमला करना UN की शक्ति की कमी को और अधिक स्पष्ट करता है, खासकर जब अमेरिका उस समय एकमात्र वैश्विक महाशक्ति था।
- यदि संभावित आक्रामक लोगों को पता होता कि उनके बलों का सामना एक UN सशस्त्र बल से होगा जो लड़ाई के लिए सुसज्जित और अधिकृत है, तो यह संघर्षों को रोक सकता था। उदाहरण के लिए, 1990 में कुवैत-इराक सीमा पर या 1991 में क्रोएशिया-सेर्बिया सीमा पर तैनात UN बल ने संघर्षों को रोकने में मदद की हो सकती थी।
UN को कब हस्तक्षेप करना चाहिए?
संघर्षों में यूएन की भागीदारी का सही समय निर्धारित करना एक समस्या है। कई बार, यूएन बहुत अधिक समय लेता है, जिससे समाधान और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है, जैसा कि वियतनाम और अंगोला युद्धों के दौरान देखा गया। इस अनिर्णय ने कुछ राज्यों को शांति बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय संगठनों जैसे नाटो को प्राथमिकता दी, जिससे कई समझौतों का समाधान यूएन की भागीदारी के बिना हुआ। वियतनाम युद्ध के अंत, 1979 में इज़राइल और मिस्र के बीच कैंप डेविड शांति, और 1979 में रोडेशिया/जिम्बाब्वे समझौता जैसे उदाहरण बिना महत्वपूर्ण यूएन योगदान के हुए। आलोचकों का तर्क था कि यूएन अप्रासंगिक होता जा रहा था, केवल प्रचार भाषणों के मंच के रूप में कार्य कर रहा था। यूएन सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यों द्वारा वेटो शक्ति ने निर्णायक कार्रवाई में भी बाधा डाली। हालांकि 'यूनाइटिंग फॉर पीस' प्रस्ताव ने इस स्थिति को कुछ हद तक कम किया, फिर भी वेटो ने कार्रवाई में देरी का कारण बना।
1970 के दशक से यूएन की बढ़ती सदस्यता:
- 1970 के दशक में, यूएन की बढ़ती सदस्यता ने नए चुनौतियों को जन्म दिया।
- 1970 तक, तृतीय विश्व (अफ्रीका और एशिया) के देशों ने स्पष्ट बहुमत बनाया।
- जैसे-जैसे ये देश निकटता से सहयोग करने लगे, उन्होंने अपनी प्रस्तावों के पारित होने को सुनिश्चित किया, जिससे पश्चिमी और कम्युनिस्ट ब्लॉकों के लिए सामान्य सभा में अपने प्रस्तावों को आगे बढ़ाना और भी कठिन हो गया।
- पश्चिमी देशों ने तृतीय विश्व ब्लॉक की आलोचना की कि वे बहुत 'राजनीतिक' हो रहे हैं, जिसका अर्थ था कि वे ऐसे तरीकों से कार्य कर रहे थे जिन्हें पश्चिम ने अस्वीकार किया।
- उदाहरण के लिए, 1974 में, यूनेस्को ने 'उपनिवेशवाद' और 'साम्राज्यवाद' की निंदा करने वाले प्रस्ताव पारित किए।
- 1979 में, जब पश्चिमी ब्लॉक ने आतंकवाद की निंदा करने वाला सामान्य सभा का प्रस्ताव पेश किया, तो इसे अरब देशों और उनके सहयोगियों ने हरा दिया।
- 1983 में, यूनेस्को सामान्य कांग्रेस में तनाव चरम पर था।
- कई पश्चिमी देशों, जिसमें अमेरिका भी शामिल था, ने यूनेस्को को अप्रभावी, बर्बाद करने वाला, और अस्वीकार्य राजनीतिक लक्ष्यों वाला बताया।
- एक महत्वपूर्ण बिंदु तब आया जब कुछ कम्युनिस्ट देशों ने विदेशी पत्रकारों के आंतरिक लाइसेंसिंग का प्रस्ताव रखा। अमेरिका ने तर्क दिया कि इससे सदस्य राज्यों को एक-दूसरे के मीडिया संगठनों को प्रभावी रूप से सेंसर करने की अनुमति मिलेगी।
- इसके परिणामस्वरूप, अमेरिका ने 1 जनवरी 1985 को यूनेस्को से बाहर निकलने की घोषणा की, यह दावा करते हुए कि यह 'एक स्वतंत्र समाज की मूल संस्थाओं, विशेष रूप से एक मुक्त बाजार और स्वतंत्र प्रेस के प्रति शत्रुतापूर्ण हो गया है।'
- ब्रिटेन और सिंगापुर ने 1986 में इसी कारण से ऐसा किया। ब्रिटेन 1997 में फिर से शामिल हुआ, और अमेरिका 2002 में, लेकिन अमेरिका ने 2019 में फिर से बाहर निकलने की घोषणा की, यूनेस्को पर इज़राइल के प्रति पक्षपाती होने का आरोप लगाते हुए।
एजेंसियों के बीच प्रयासों और संसाधनों की बर्बादी:
- कुछ यूएन एजेंसियां एक-दूसरे के काम को दोहराते हुए दिखाई देती हैं, जिससे असक्षम होने की आलोचना होती है। WHO (विश्व स्वास्थ्य संगठन) और FAO (खाद्य और कृषि संगठन) विशेष रूप से ओवरलैपिंग जिम्मेदारियों के लिए आलोचना का सामना कर रहे हैं। FAO को 1984 में प्रशासन पर बहुत खर्च करने और कृषि प्रणालियों में सुधार पर कम खर्च करने के लिए आलोचना मिली। GATT (सामान्य शुल्क और व्यापार समझौता) और UNCTAD (संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन) के बीच स्पष्ट रूप से विरोधाभास दिखाई देता है। GATT शुल्क और अन्य व्यापार प्रतिबंधों को समाप्त करने का लक्ष्य रखता है, जबकि UNCTAD तीसरी दुनिया के देशों के उत्पादों के लिए पसंदीदा उपचार की मांग करता है।
धन की कमी:
- यूएन ने अपने इतिहास में लगातार धन की कमी का सामना किया है। इसके काम के विशाल दायरे के लिए अपने संचालन का समर्थन करने के लिए विशाल वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है।
- यूएन पूरी तरह से सदस्य राज्यों से योगदान पर निर्भर करता है। प्रत्येक राज्य अपनी कुल संपत्ति और भुगतान की क्षमता के आधार पर नियमित वार्षिक योगदान देता है।
- इसके अतिरिक्त, सदस्य राज्य प्रत्येक शांति स्थापना संचालन की लागत का एक अनुपात योगदान करते हैं और विशेष एजेंसियों के खर्चों में मदद करने की अपेक्षा की जाती है।
- कई बार, कई सदस्य राज्यों ने या तो अपनी वित्तीय कठिनाइयों के कारण या कुछ यूएन नीतियों के विरोध में अपने बकाया का भुगतान करने से इनकार कर दिया। उदाहरण के लिए, 1986 में, अमेरिका ने $100 मिलियन से अधिक की राशि रोक दी जब तक कि यूएन ने अपने बजट प्रणाली में सुधार नहीं किया और स्वच्छता को कम नहीं किया।
- अमेरिका ने मुख्य योगदानकर्ताओं को धन के व्यय पर अधिक कहने का लक्ष्य रखा, लेकिन अधिकांश छोटे देशों ने इसे गैर-लोकतांत्रिक के रूप में खारिज कर दिया।
- 1987 में, सुधार लागू किए गए जिससे मुख्य वित्तीय योगदानकर्ताओं को खर्च पर अधिक नियंत्रण मिला, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ।
- हालांकि, 1990 के प्रारंभ में खर्च बढ़ गया जब यूएन विभिन्न नए संकटों में शामिल हो गया, जिसमें मध्य पूर्व (गुल्फ युद्ध), यूगोस्लाविया और सोमालिया शामिल थे।
- अगस्त 1993 में, महासचिव डॉ. बौत्रोस-घाली ने खुलासा किया कि कई राज्य अपने भुगतान के मामले में काफी बकाया थे।
- उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सबसे धनी राज्यों से तत्काल नकद प्रवाह नहीं हुआ, तो सभी यूएन शांति स्थापना संचालन खतरे में होंगे।
- फिर भी, अमेरिकियों और यूरोपियों ने महसूस किया कि वे पहले से ही बहुत योगदान दे रहे थे। अमेरिका, EU, और जापान ने खर्चों का तीन-चौथाई हिस्सा कवर किया, और यह विश्वास था कि कई अन्य धनी राज्यों को अपने योगदान को बढ़ाने में सक्षम होना चाहिए।
अन्य समस्याएं:
- संयुक्त राष्ट्र (UN) की स्थापना के बाद से सुधार के लिए कई बार आवाजें उठाई गई हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए सहमति प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण रहा है।
- कुछ लोग वैश्विक मामलों में एक अधिक शक्तिशाली और प्रभावी UN की भूमिका के पक्षधर हैं, जबकि अन्य मानवीय कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की इच्छा रखते हैं।
- UN सुरक्षा परिषद के सदस्यता का विस्तार, UN महासचिव के चुनाव की विधियों में परिवर्तन, और एक संयुक्त राष्ट्र संसदीय सभा की स्थापना के लिए कई सुझाव दिए गए हैं।
- UN के बारे में विचारों में सबसे लगातार विभाजन उत्तरी-दक्षिणी विभाजन है, जो समृद्ध उत्तरी देशों और विकासशील दक्षिणी देशों के बीच है।
- दक्षिणी देश आमतौर पर एक सशक्त UN और एक सशक्त महासभा का समर्थन करते हैं, जिससे उन्हें वैश्विक मामलों में अधिक प्रभाव मिलता है।
- वही, उत्तरी देश एक अधिक हाथ से दूर रहने वाले UN के पक्षधर हैं, जो आतंकवाद जैसे आंतरराष्ट्रीय मुद्दों को प्राथमिकता देता है।
- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, फ्रांसीसी राष्ट्रीय मुक्ति समिति को प्रारंभ में अमेरिका द्वारा फ्रांस की सरकार के रूप में मान्यता नहीं दी गई और इसे नए संगठन की स्थापना के लिए आयोजित सम्मेलनों से बाहर रखा गया।
- फ्रांस के भविष्य के राष्ट्रपति चार्ल्स डी गॉल ने UN की आलोचना की, इसे एक मशीन कहा और वैश्विक सुरक्षा संधि को विश्व शांति बनाए रखने के लिए प्रभावी नहीं मानते हुए देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा संधियों को प्राथमिकता दी।
- UN पर प्रशासनिक अक्षमता, बर्बादी, और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए गए हैं।
- 1990 के दशक में, अमेरिका ने इन मुद्दों का हवाला देकर योगदान रोक दिया और केवल महत्वपूर्ण सुधार की शर्त पर ही भुगतान फिर से शुरू किया।
- 1994 में, आंतरिक निगरानी सेवाएं (OIOS) की स्थापना की गई ताकि UN के भीतर दक्षता की निगरानी की जा सके।
- 2004 में, UN को तेल-के-लिए-भोजन कार्यक्रम में भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करना पड़ा, जिसमें इराक को बुनियादी जरूरतों के लिए तेल व्यापार करने की अनुमति दी गई थी ताकि प्रतिबंधों के प्रभाव को कम किया जा सके।
- आलोचनाओं के बावजूद, UN को एक विफलता के रूप में खारिज करना गलत होगा। इसके बिना, दुनिया शायद कहीं अधिक खराब स्थान होती।
- UN एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहाँ लगभग 190 देशों के प्रतिनिधि एकत्रित होकर संवाद कर सकते हैं, जिससे छोटे से छोटे देशों को भी वैश्विक चर्चाओं में आवाज मिलती है।
- हालाँकि यह युद्धों को रोकने में सक्षम नहीं रहा है, लेकिन UN ने कुछ संघर्षों के अंत को तेजी से लाने और आगे की विवादों को रोकने में प्रभावी भूमिका निभाई है।
- UN शांति सेना और शरणार्थी एजेंसियों ने महत्वपूर्ण मानव पीड़ा और रक्तपात को टालने में मदद की है।
- 2019 तक, दुनिया भर में लगभग 110,000 UN शांति सैनिक और 14 शांति मिशन सक्रिय रूप से तैनात हैं।
- UN ने दमनकारी शासन के तहत मानवाधिकारों के उल्लंघनों की जांच और प्रकाशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जैसे कि चिली और ज़ायर में।
- इसने धीरे-धीरे सरकारों पर अंतरराष्ट्रीय दबाव डालकर उन्हें प्रभावित किया है।
- संभवतः इसकी सबसे महत्वपूर्ण सफलता आर्थिक, सामाजिक, और तकनीकी मामलों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना रही है।
- विशेष रूप से कम संपन्न देशों में लाखों व्यक्तियों ने UN एजेंसियों के प्रयासों से लाभ उठाया है।
- UN समकालीन मुद्दों में संलग्न है, जैसे UNESCO, ILO (अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन), और WHO (विश्व स्वास्थ्य संगठन) जैसे एजेंसियाँ नशा मुक्ति में सहायता के लिए परियोजनाओं पर सहयोग कर रही हैं और अफ्रीका में इस विनाशकारी महामारी के खिलाफ लड़ाई को समन्वयित करने के लिए AIDS पर सम्मेलन आयोजित कर रही हैं।
UN का भविष्य:
कई लोगों का मानना था कि शीत युद्ध के अंत से अधिकांश वैश्विक मुद्दों का समाधान होगा। हालांकि, ऐसा नहीं हुआ। 1990 के दशक के दौरान, संघर्षों में वृद्धि होती दिखाई दी, और वैश्विक स्थिरता घटती प्रतीत हुई। इसने अंतरराष्ट्रीय शांति रक्षक के रूप में यूएन की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर किया, जिसमें कई लोगों ने संगठन को मजबूत करने के लिए सुधारों की इच्छा व्यक्त की।
कोफी अन्नान, जो दिसंबर 1996 में महासचिव बने, को यूएन शांति अभियानों में उनके नेतृत्व के लिए अत्यधिक सराहा गया। उन्होंने यूएन की कमजोरियों को पहचाना और उन्हें संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध रहे। उन्होंने सभी यूएन शांति अभियानों की एक व्यापक समीक्षा शुरू की, जिसके परिणामस्वरूप 2000 में यूएन को 5,000 सैनिकों की स्थायी ब्रिगेड-आकार की बल बनाए रखने के लिए सिफारिशें मिलीं, जो पेशेवर सैन्य नेतृत्व के तहत तात्कालिक तैनाती के लिए तैयार हों।
सप्टेम्बर 2001 में न्यूयॉर्क में हुए हमलों के बाद, आतंकवाद के उदय ने अन्नान को सितंबर 2002 में आगे के बदलाव के लिए एजेंडा पेश करने के लिए प्रेरित किया। इस योजना का उद्देश्य आतंकवाद से लड़ने में यूएन की भूमिका को मजबूत करना और इसके जटिल बजट प्रणाली को सरल बनाना था।
शीत युद्ध के बाद और अमेरिका के एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरने के बाद से यूएन और अमेरिका के बीच संबंध एक महत्वपूर्ण चुनौती रहे हैं। जब बुश प्रशासन ने 1972 के एंटी-बैलिस्टिक मिसाइलक्योटो प्रोटोकॉल, और यूएन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के लिए रोम संधि जैसे कई अंतरराष्ट्रीय समझौतों को अस्वीकार कर दिया, तो तनाव बढ़ गया।
ये तनाव मार्च 2003 में चरम पर पहुंच गए, जब अमेरिका ने यूके के समर्थन से यूएन की अनुमति के बिना इराक पर आक्रमण करने का निर्णय लिया, जो अधिकांश यूएन सदस्यों की इच्छाओं के खिलाफ था। अमेरिका की भारी शक्ति ने उसे यूएन की अनदेखी करने और स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति दी, जब तक कि यूएन उसके हितों के साथ मेल नहीं खाता। यूएन को प्रभावित करने की एक अमेरिकी रणनीति एक सहानुभूतिपूर्ण महासचिव की नियुक्ति सुनिश्चित करना था।
|
28 videos|739 docs|84 tests
|




















