Environment and Ecology (पर्यावरण और पारिस्थितिकी): January 2025 UPSC Current Affairs | पर्यावरण (Environment) for UPSC CSE in Hindi PDF Download
| Table of contents |

|
| गोल्डन लंगूर |

|
| ब्राज़ीलियाई वेल्वेट एंट |

|
| आईपीबीईएस परिवर्तनकारी परिवर्तन मूल्यांकन |

|
| जनजातीय मंत्रालय का वन अधिकार अधिनियम, 2006 पर निर्देश |

|
गोल्डन लंगूर

समाचार में क्यों?
असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 117 पर एक गोल्डन लंगूर की हालिया मृत्यु ने इस संकटग्रस्त प्रजाति के समक्ष बढ़ते खतरों के बारे में महत्वपूर्ण चिंताएँ उत्पन्न की हैं।
मुख्य बिंदु
- गोल्डन लंगूर एक प्राइमेट प्रजाति है, जो मुख्य रूप से असम, भारत और भूटान के कुछ भागों में पाई जाती है।
- इसे आवास के टुकड़ों में बंटने और विभिन्न मानव गतिविधियों के कारण संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
अतिरिक्त जानकारी
- टैक्सोनॉमी: इस प्रजाति का नाम Trachypithecus geei है, जो परिवार Cercopithecidae (पुराने विश्व के बंदर) और उपपरिवार Colobinae (पत्ते खाने वाले बंदर) से संबंधित है। इसे 1953 में E.P. Gee द्वारा खोजा गया था और 1956 में खजूरिया द्वारा औपचारिक रूप से वर्णित किया गया था।
- भौगोलिक क्षेत्र: गोल्डन लंगूर केवल असम के एक सीमित क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो उत्तर में भूटान के पहाड़ी क्षेत्र, पूर्व में मनास नदी, पश्चिम में संकोश नदी और दक्षिण में ब्रह्मपुत्र नदी से घिरा हुआ है।
- आवास: ये उपोष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले जंगलों में निवास करते हैं, जो समुद्र स्तर से लेकर 3,000 मीटर से अधिक ऊँचाई तक thrive करते हैं।
- शारीरिक विशेषताएँ: इनका पहचान चिन्ह उनका सुनहरे-नारंगी फर है, जो मौसम के साथ रंग बदलता है; गर्मियों में क्रीम और सर्दियों में गहरा सुनहरा। इनके पास काली बेजान चेहरा है, जिसमें हल्की दाढ़ी और सिर पर एक विशिष्ट बालों का घेरा होता है।
- व्यवहार: ये दिन में सक्रिय (डायर्नल) और मुख्यतः वृक्षीय होते हैं, ये लंगूर 3 से 15 व्यक्तियों के समूहों में रहते हैं, आमतौर पर एक नर के साथ कई मादाएँ या कभी-कभी सभी नर समूह होते हैं।
- खतरे: मानव गतिविधियों जैसे सड़क निर्माण और वनों की कटाई के कारण इनके आवासों का टुकड़ों में बंटना इनके अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा प्रस्तुत करता है।
- संरक्षण स्थिति: IUCN रेड लिस्ट में गोल्डन लंगूर को संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और यह CITES की अनुबंध सूची I के तहत तथा 1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (2022 में संशोधित) के तहत संरक्षित है, जो इसे सख्त संरक्षण उपायों में सूचीबद्ध करता है।
- संरक्षण उपाय: रणनीतियों में टुकड़ों में बंटे आवासों को जोड़ने के लिए गलियारे बनाना और सुरक्षित आवागमन के लिए कैनोपी पुलों का निर्माण शामिल हैं, साथ ही मानव प्रभावों को कम करने के लिए दीर्घकालिक संरक्षण प्रयासों की आवश्यकता है।
अंत में, गोल्डन लैंगूर कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, जो कि आवास की हानि और मानव हस्तक्षेप के कारण हैं। इस प्रजाति के संरक्षण के प्रयास जैव विविधता को बनाए रखने और इसे जंगली में जीवित रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
ब्राज़ीलियाई वेल्वेट एंट

हाल ही में बेलस्टाइन जर्नल ऑफ नैनोटेक्नोलॉजी में एक अध्ययन में ब्राज़ीलियाई वेल्वेट एंट (Traumatomutilla bifurca) का उल्लेख किया गया है, जिसमें "अल्ट्रा-ब्लैक" शरीर भाग होते हैं जो 99.5% से अधिक दृश्य प्रकाश को अवशोषित करते हैं, जिससे वे लगभग अदृश्य हो जाते हैं। यह खोज इस प्रजाति में मौजूद अद्वितीय जैविक नैनोस्ट्रक्चर को उजागर करती है, जिसके संभावित तकनीकी अनुप्रयोग हो सकते हैं।
- वर्गीकरण: वेल्वेट एंट असली चींटियाँ नहीं हैं; वे Mutillidae परिवार से संबंधित हैं और Hymenoptera क्रम के अंतर्गत वर्गीकृत हैं, जिसमें मधुमक्खियाँ और ततैया शामिल हैं।
- दृश्य विशेषताएँ: कुछ प्रजातियाँ, जिसमें Traumatomutilla bifurca शामिल है, में काले और सफेद चिह्न होते हैं जो उन्हें उनके प्राकृतिक आवासों, जैसे उष्णकटिबंधीय सवाना और शुष्क झाड़ी वाले रेगिस्तान में दृश्य रूप से आकर्षक बनाते हैं।
- अल्ट्राब्लैक गुण: मादा वेल्वेट एंट्स की पहचान उनके अल्ट्राब्लैक रंग से होती है, जिसे इस प्रजाति में पहली बार देखा गया था। यह रंग विशेष माइक्रो-स्ट्रक्चर्स के कारण लगभग सभी दृश्य प्रकाश को अवशोषित करता है जो उनके एक्सोस्केलेटन में होते हैं और जो प्रकाश को फँसाते हैं। यह अल्ट्राब्लैक रंगाई छिपाव, तापमान नियंत्रण, और साथी को आकर्षित करने में मदद करता है।
- यौन द्विरूपता: केवल मादा वेल्वेट एंट्स इस अल्ट्राब्लैक रंग का प्रदर्शन करती हैं; नर समान काले चिह्न दिखाते हैं लेकिन अधिक प्रकाश को परावर्तित करते हैं, जिससे उनके छिपाव की क्षमता कम होती है।
- पारिस्थितिकी में भूमिका: ये चींटियाँ अपने पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, परागणक के रूप में कार्य कर रही हैं, जो पारिस्थितिक संतुलन में योगदान करती हैं।
- उत्क्रमणीय महत्व: अल्ट्राब्लैक गुण संवहनीय उत्क्रमण का एक उदाहरण है, जहाँ असंबंधित प्रजातियाँ समान गुण विकसित करती हैं। यह अनुकूलन पक्षियों की प्रजातियों और गहरे समुद्री मछलियों में भी देखा गया है, जो उनके छिपाव और अस्तित्व को बढ़ाता है।
- संभावित अनुप्रयोग: अल्ट्राब्लैक गुण जैविक नैनोस्ट्रक्चर्स के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और यह स्टेल्थ प्रौद्योगिकी में प्रगति और सौर पैनल की दक्षता में सुधार के लिए प्रेरणा दे सकता है।
ब्राज़ीलियन वेल्वेट एंट का अध्ययन न केवल इसकी जीवविज्ञान के आकर्षक पहलुओं को उजागर करता है, बल्कि यह तकनीकी नवाचारों के लिए नए रास्ते भी खोलता है, जो प्रकृति और विज्ञान के बीच की परस्पर क्रिया को दर्शाता है।
आईपीबीईएस परिवर्तनकारी परिवर्तन मूल्यांकन
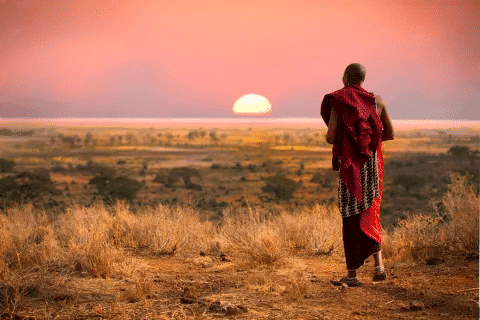
जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतरसरकारी विज्ञान-नीति मंच (IPBES) की एक हालिया रिपोर्ट, जिसका शीर्षक है परिवर्तनकारी परिवर्तन मूल्यांकन, जैव विविधता के नुकसान को संबोधित करने में शासन की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देती है। यह रेखांकित करती है कि प्रभावी शासन, जो समावेशिता और स्थिरता को प्राथमिकता देता है, जैव विविधता को बनाए रखने और दीर्घकालिक प्रणालीगत परिवर्तनों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
- पारिस्थितिकी क्षति को रोकें: जैव विविधता के नुकसान से बचने के लिए प्रकृति के साथ सामाजिक इंटरैक्शन में तात्कालिक बदलाव आवश्यक हैं, क्योंकि निष्क्रियता के परिणामस्वरूप अपरिवर्तनीय पारिस्थितिकी क्षति हो सकती है, जिसमें कोरल रीफ और वर्षावनों का गायब होना शामिल है।
- आर्थिक और रोजगार के अवसर: तात्कालिक कार्रवाई करने से 2030 तक वैश्विक स्तर पर 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यवसाय के अवसर पैदा हो सकते हैं और 395 मिलियन नौकरियों का समर्थन किया जा सकता है, विशेष रूप से प्रकृति पर निर्भर उद्योगों में।
- जैव विविधता के नुकसान के कारण: रिपोर्ट में प्रमुख कारणों की पहचान की गई है जैसे कि मानव और प्रकृति के बीच का डिस्कनेक्ट, प्राकृतिक प्रणालियों पर वर्चस्व, शक्ति और धन का संकेंद्रण, और स्थिरता के मुकाबले तात्कालिक भौतिक लाभ को प्राथमिकता देना।
परिवर्तन के लिए पांच मुख्य रणनीतियाँ
- संरक्षण और पुनर्जीवित करना: ऐसे जैव-सांस्कृतिक विविधता क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करें जो पर्यावरणीय पुनर्स्थापन को सांस्कृतिक मूल्यों के साथ मिलाते हैं, जैसे नेपाल में समुदाय-प्रेरित वन प्रबंधन।
- प्रमुख क्षेत्रों में प्रणालीगत परिवर्तन: कृषि, मत्स्य पालन, और बुनियादी ढाँचे जैसे क्षेत्रों में सतत प्रथाओं को लागू करें जो जैव विविधता को प्रभावित करते हैं।
- आर्थिक प्रणालियों का रूपांतरण: हानिकारक सब्सिडी में सुधार करके और सतत व्यवसाय मॉडल के लिए वकालत करके प्रकृति-हितैषी अर्थव्यवस्थाओं की ओर बढ़ें।
- अनुकूली शासन: शासन प्रणालियों का विकास करें जो विविध हितधारकों, जिसमें स्वदेशी समुदाय भी शामिल हैं, को शामिल करें, जिससे जैव विविधता को बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए एक केंद्रीय नीति का ध्यान केंद्रित किया जा सके।
- दृष्टिकोण और मूल्यों में परिवर्तन: शिक्षा, अनुभवात्मक सीखने, और विभिन्न ज्ञान प्रणालियों के एकीकरण के माध्यम से मानव-प्रकृति के आपसी संबंध की समझ को बढ़ावा दें।
परिवर्तनीय परिवर्तन क्या है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है?
परिवर्तनीय परिवर्तन: यह एक मौलिक, प्रणाली-व्यापी पुनर्गठन को संदर्भित करता है, जो तकनीकी, आर्थिक, और सामाजिक आयामों में, जिसमें मानदंड, लक्ष्य, और मूल्य शामिल हैं, आवश्यक है जैव विविधता संरक्षण, सतत उपयोग, और उच्च गुणवत्ता वाले जीवन और सतत विकास को प्राप्त करने के लिए।
परिवर्तनीय परिवर्तन प्राप्त करने के कदम
- कार्बन-न्यूट्रल क्रियाएँ: व्यक्तियों, व्यवसायों, और सरकारों के लिए कार्बन न्यूट्रैलिटी को मानक के रूप में प्राप्त करना, जबकि विश्वसनीय जलवायु-अनुकूल ऑफसेट का समर्थन करना।
- पृथ्वी-सकारात्मक विकल्प: व्यक्तियों को आपूर्ति श्रृंखलाओं और नीति प्रभावों में बदलाव के माध्यम से पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए सुखद और सुलभ तरीके प्रदान करना।
- सब्सिडियों का सुधार: पर्यावरणीय प्रबंधन को बढ़ावा देने और संसाधन-उत्खनन उद्योगों से सतत प्रथाओं में संक्रमण करने के लिए सब्सिडियों और प्रोत्साहनों का पुनर्निर्देशन करना।
- सावधानीपूर्वक निर्णय लेना: पर्यावरणीय खतरों का सक्रिय रूप से समाधान करने के लिए सावधानीपूर्वक, अनुकूलनशील, समावेशी, और पार-क्षेत्रीय निर्णय लेना, भले ही ठोस सबूत न हों।
- पर्यावरणीय कानूनों को मजबूत करना: मजबूत पर्यावरणीय विधान का समर्थन करना, सुनिश्चित करना कि प्रवर्तन लगातार हो, और प्रकृति संरक्षण और सतत आर्थिक गतिविधियों के लिए वैश्विक पहलों का समर्थन करना।
भारत के परिवर्तनकारी परिवर्तन के लिए पहलकदमियाँ क्या हैं?
- राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना (NBAP)
- स्वच्छ भारत अभियान
- जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना
- हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के तेज़ अपनाने और निर्माण (FAME)
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY)
- मिशन लाइफ (Lifestyle for Environment)
- अटल मिशन फॉर रीजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (AMRUT)
परिवर्तनकारी परिवर्तन के लिए SDGs
सतत विकास लक्ष्य (SDGs) समावेशी विकास के माध्यम से परिवर्तनकारी परिवर्तन का लक्ष्य रखते हैं, जो निम्नलिखित पर केंद्रित हैं:
- पानी के नीचे जीवन
- जलवायु कार्रवाई
- स्वच्छ ऊर्जा
- स्वच्छ पानी
- जिम्मेदार उपभोग
- भूमि पर जीवन
स्मार्ट सिटी मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन, और राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष जैसी पहलकदमियाँ विभिन्न SDGs के साथ मेल खाती हैं। भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा में महत्वपूर्ण निवेश किया है, जिसका लक्ष्य 2030 तक 500 GW की उत्पादन क्षमता प्राप्त करना है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा समर्थन प्राप्त है।
मुख्य प्रश्न
प्रश्न: परिवर्तनकारी परिवर्तन की अवधारणा पर चर्चा करें। जैव विविधता के नुकसान को संबोधित करने और सतत विकास को प्राप्त करने के लिए इसे कैसे लागू किया जा सकता है?
जनजातीय मंत्रालय का वन अधिकार अधिनियम, 2006 पर निर्देश
जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने राज्यों को निर्देशित किया है कि वे बाघ अभयारण्यों में वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत तंत्र स्थापित करें।
जनजातीय मंत्रालय के हालिया निर्देशों की मुख्य बातें क्या हैं?
- FRA अनुपालन सुनिश्चित करना: मंत्रालय ने जोर दिया कि वनवासियों को FRA औरवन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत उनके अधिकारों की कानूनी मान्यता के बिना निष्कासित नहीं किया जा सकता।
- यह कदम वनवासियों के अवैध निष्कासन की शिकायतों के बाद उठाया गया है, विशेष रूप से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और पश्चिम बंगाल में।
- स्थानांतरित करने के लिए सहमति: FRA की धारा 4(2) ऐसी सुरक्षा प्रदान करती है जो स्थानांतरण के लिएग्राम सभाओं की लिखित, मुक्त और सूचित सहमति प्राप्त करना अनिवार्य बनाती है। कानून में उन क्षेत्रों में बस्तियों के अधिकारों की भी व्यवस्था है जहां बस्ती का प्रस्ताव है।
- राज्यों को बाघ अभयारण्यों में जनजातीय गांवों और उनके वन अधिकार दावों की स्थिति का विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा।
- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) ने भी बाघ अभयारण्यों में 591 गांवों के पुनर्वास के लिए समयसीमा मांगी है, जिससे संरक्षण और सामुदायिक अधिकारों के बीच संतुलन पर बहस तेज हो गई है।
- शिकायत निवारण तंत्र: राज्यों को वन क्षेत्रों से निष्कासन से संबंधित शिकायतों और समस्याओं को संभालने के लिए शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने के लिए निर्देशित किया गया है।
वन अधिकार अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ क्या हैं?
- व्यक्तिगत अधिकारों की मान्यता की कमी: वन अधिकार अधिनियम (FRA) के तहत व्यक्तिगत अधिकारों की मान्यता को वन विभाग द्वारा चुनौती के रूप में देखा जाता है, जो इसे अपने वन संसाधनों पर नियंत्रण के लिए खतरा मानते हैं।
- असम में, स्थानांतरण कृषि प्रथाएँ अधिकार मान्यता प्रक्रिया को जटिल बनाती हैं, जबकि महाराष्ट्र के गडचिरोली जिले में, समुदाय के वन भूमि को गैर-वन उद्देश्यों के लिए परिवर्तित करने का खतरा है, भले ही अधिकारों की मान्यता में प्रगति हो रही हो, यह कार्यान्वयन में खामियों को उजागर करता है।
- तकनीकी समस्याएँ: VanMitra जैसे डिजिटल प्लेटफार्मों का कार्यान्वयन खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी और आदिवासी क्षेत्रों में कम साक्षरता दरों के कारण महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करता है, जिससे दावों की सुगम प्रक्रिया में कठिनाई होती है।
- विरोधाभासी विधान: FRA अक्सर भारतीय वन अधिनियम, 1927 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 जैसे कानूनों से टकराता है। ये संघर्ष अस्पष्टताएँ उत्पन्न करते हैं, जिसमें अधिकारी FRA के आदेशों के बजाय पारंपरिक वन शासन को प्राथमिकता देते हैं।
- उच्च अस्वीकृति दरें: कई दावे उचित दस्तावेज़ीकरण या साक्ष्य की कमी के कारण अस्वीकृत होते हैं, अक्सर स्पष्ट स्पष्टीकरण या अपील के अवसर के बिना। इससे वैध दावेदारों के पास कोई उपाय नहीं बचता।
- कमज़ोर ग्राम सभाएँ: ग्राम सभा अक्सर अपनी ज़िम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए क्षमता, संसाधनों और प्रशिक्षण की कमी का सामना करती है।
- वन-आधारित समुदायों में स्थानीय अभिजात वर्ग अक्सर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में प्रभुत्व रखते हैं, लाभों का एकाधिकार करते हैं और हाशिए पर पड़े समूहों को अधिकारों तक पहुँच से वंचित रखते हैं।
- उद्वासन और विकास संघर्ष: FRA की प्रावधानों के बावजूद, खनन, बांधों और राजमार्गों जैसे बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाओं के कारण अक्सर वन-निवासी समुदायों का उद्वासन होता है।
आगे का रास्ता
- प्रतिरोध का समाधान: किसान उत्पादक संगठन (FPOs) जैसे जनजातीय या वनवासियों के निकायों का गठन करना, अधिकारों का सामूहिक रूप सेAssertion करना, वन विभागों के साथ संवाद को बढ़ावा देना, और स्थायी प्रबंधन और सशक्तिकरण के लिए FRA के उद्देश्यों के साथ संरक्षण को संरेखित करना।
- भारतीय वन अधिनियम, 1927 जैसे मौजूदा कानूनों में संशोधन करना ताकि FRA के साथ संघर्षों को कम किया जा सके और स्पष्ट, सहयोगात्मक शासन सुनिश्चित किया जा सके।
- तकनीकी क्षमताओं में सुधार: जनजातीय क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाने और दावों की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए डिजिटल प्लेटफार्मों पर प्रशिक्षण प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना।
- दस्तावेजीकरण प्रक्रियाओं को सरल बनाना ताकि प्रक्रिया अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल हो सके, जबकि व्यापक क्षमता निर्माण के लिए डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना।
- विकास और सामुदायिक अधिकारों का संतुलन: सुनिश्चित करना कि बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाएं सामुदायिक अधिकारों का सम्मान करें और वन समुदायों और जैव विविधता की रक्षा के लिए स्थायी प्रथाओं को एकीकृत करें।
- संरक्षण और सामुदायिक सशक्तिकरण के बीच संघर्षों को संबोधित करने के लिए सह-प्रबंधन मॉडल को बढ़ावा देने वाले ढांचे स्थापित करना।
- समावेशी निर्णय-निर्माण: सुनिश्चित करना कि ग्राम सभाओं में निर्णय-निर्माण समावेशी हो, और हाशिए पर पड़े समूहों जैसे महिलाओं और निम्न जातियों को अधिकारों और लाभों तक समान पहुंच मिले।
- जागरूकता और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना: FRA के तहत अपने अधिकारों के बारे में वनवासियों को शिक्षित करने के लिए व्यापक जागरूकता अभियानों की शुरुआत करना, जिससे वे दावे दाखिल कर सकें।
- ग्राम सभाओं की क्षमता को प्रभावी निर्णय-निर्माण और हाशिए पर पड़े समूहों के समावेश को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संसाधनों और प्रशिक्षण के साथ बढ़ाना।
|
8 videos|267 docs|48 tests
|















