Indian Polity (भारतीय राजव्यवस्था) Part 1: July 2025 UPSC Current Affairs | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly PDF Download
POCSO जमानत निर्णयों में न्यायिक विवेक की कुंजी
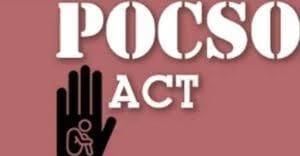
चर्चा में क्यों?
मुंबई की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने हाल ही में एक नाबालिग के यौन उत्पीड़न के आरोपी 40 वर्षीय शिक्षक को सहमति से संबंध बनाने का हवाला देते हुए ज़मानत दे दी है। इस फैसले ने पॉक्सो अधिनियम के तहत ज़मानत से जुड़ी जटिलताओं की ओर फिर से ध्यान आकर्षित किया है, जो मानक आपराधिक कानून की तुलना में ज़्यादा कड़े दिशानिर्देश लागू करता है।
चाबी छीनना
- पोक्सो मामलों में सबूत का भार अभियुक्त पर आ जाता है, जिससे जमानत प्रक्रिया जटिल हो जाती है।
- जमानत संबंधी निर्णय न्यायिक विवेक पर बहुत हद तक निर्भर करते हैं, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पीड़ित संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है।
अतिरिक्त विवरण
- पोक्सो अधिनियम (2012): एक विधायी ढांचा जिसका उद्देश्य बच्चों (18 वर्ष से कम) को यौन अपराधों से बचाना है, जिसमें दुर्व्यवहार, उत्पीड़न और शोषण शामिल है।
- प्रमुख विशेषताऐं:
- लिंग-तटस्थ संरक्षण: यह अधिनियम लड़के और लड़कियों दोनों पर समान रूप से लागू होता है।
- अपराधों की विस्तृत श्रृंखला: इसमें प्रवेशात्मक और गैर-प्रवेशात्मक हमला, यौन उत्पीड़न और बाल पोर्नोग्राफी दोनों शामिल हैं।
- विशेष न्यायालय: त्वरित सुनवाई के लिए बाल-अनुकूल विशेष न्यायालयों की स्थापना।
- अनिवार्य रिपोर्टिंग: बाल यौन शोषण की रिपोर्ट करना व्यक्तियों के लिए कानूनी दायित्व है।
- दोष की धारणा: अभियुक्त को निर्दोषता का प्रदर्शन करना होगा, जो कि "दोषी सिद्ध होने तक निर्दोष" के मानक कानूनी सिद्धांत को उलट देता है।
- गोपनीयता: यह अधिनियम बच्चे की पहचान की रक्षा करता है ताकि उसे आगे कोई आघात न पहुंचे।
- पीड़ितों के लिए सहायता: पीड़ितों के समर्थन और पुनर्वास के लिए रूपरेखा तैयार की गई है।
- बाल-अनुकूल प्रक्रियाएं: बयान दर्ज करने और चिकित्सा परीक्षण करने के लिए उचित प्रक्रियाओं पर जोर दिया जाता है।
- POCSO अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती हैं, इनमें जमानत की कोई गारंटी नहीं होती तथा बिना वारंट के भी गिरफ्तारी हो सकती है।
- जमानत पर निर्णय लेते समय न्यायालय अपराध की गंभीरता, संभावित सजा, भागने का जोखिम, तथा साक्ष्यों से छेड़छाड़ के जोखिम जैसे कारकों पर विचार करते हैं।
- देशराज @ मूसा बनाम राजस्थान राज्य (2024) जैसे हालिया मामले बताते हैं कि न्यायिक विवेक कितना महत्वपूर्ण है, खासकर जब नाबालिगों से जुड़े रिश्तों के संदर्भ का आकलन किया जाता है।
निष्कर्ष
हालाँकि पोक्सो अधिनियम का उद्देश्य नाबालिगों की सुरक्षा करना है, लेकिन सहमति और ज़मानत से संबंधित इसके प्रावधान कानूनी जटिलताएँ पैदा करते हैं। इन चुनौतियों से निपटने में न्यायिक विवेक की अहम भूमिका होती है, खासकर सहमति से बने किशोर संबंधों के मामलों में, जहाँ कानून नाबालिगों के साथ सभी यौन गतिविधियों को अपराध मानता है।
आयुष चिकित्सकों के लिए चिकित्सा सीमाएँ

चर्चा में क्यों?
हाल ही में ट्विटर पर एक हेपेटोलॉजिस्ट और एक भारतीय शतरंज ग्रैंडमास्टर से संबंधित विवाद ने लंबे समय से चली आ रही बहस को फिर से हवा दे दी है कि क्या आयुर्वेद और यूनानी जैसी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के चिकित्सक वैध रूप से "डॉक्टर" की उपाधि का दावा कर सकते हैं और आधुनिक चिकित्सा लिख सकते हैं।
चाबी छीनना
- आयुर्वेदिक चिकित्सकों में वैज्ञानिक प्रशिक्षण की कमी के बारे में चिंता।
- अधिकारों के निर्धारण के संबंध में परस्पर विरोधी राज्य आदेशों के कारण कानूनी अस्पष्टताएं।
- गंभीर देखभाल स्थितियों में रोगी सुरक्षा के लिए जोखिम।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा और पारंपरिक चिकित्सा के एकीकरण पर प्रभाव।
अतिरिक्त विवरण
- वैज्ञानिक प्रशिक्षण का अभाव: आयुर्वेदिक चिकित्सकों के पास अक्सर आधुनिक औषध विज्ञान और निदान विधियों में औपचारिक प्रशिक्षण का अभाव होता है, जिसके कारण अनुचित नुस्खे लिखे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, ऐसे मामले सामने आए हैं जहाँ आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने स्टेरॉयड और एंटीबायोटिक दवाओं के दुष्प्रभावों या उचित खुराक को समझे बिना ही उन्हें लिख दिया।
- कानूनी मानदंडों का उल्लंघन: डॉ. मुख्तियार चंद मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार, गैर-एमबीबीएस चिकित्सकों को एलोपैथिक दवाएं लिखने की अनुमति नहीं है। हालाँकि, कुछ राज्यों ने परस्पर विरोधी कार्यकारी आदेश पारित किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप कानूनी अस्पष्टता बनी हुई है।
- उपभोक्ता धोखाधड़ी: आयुर्वेदिक चिकित्सकों से उपचार प्राप्त करते समय मरीज़ों को यह भ्रम हो सकता है कि वे एमबीबीएस-योग्य चिकित्सक से परामर्श ले रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप गलत जानकारी और संभावित कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
- गंभीर देखभाल में खतरा: आपातकालीन वार्डों में आयुर्वेदिक डॉक्टरों की नियुक्ति से मरीजों की सुरक्षा को खतरा पैदा होता है, क्योंकि उपचार में देरी या गलत हस्तक्षेप की खबरें आती रही हैं।
- औषधियों के तर्कसंगत उपयोग को कमजोर करना: आयुर्वेदिक चिकित्सकों द्वारा एलोपैथिक औषधियों का अनियमित रूप से प्रयोग एंटीबायोटिक प्रतिरोध जैसे मुद्दों को बढ़ावा देता है, जैसा कि उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य ऑडिट में उजागर हुआ है, जिसमें आयुष चिकित्सकों द्वारा उचित निगरानी के बिना आधुनिक औषधियां लिखने के महत्वपूर्ण उदाहरण सामने आए हैं।
- पारंपरिक चिकित्सा विनियमन का विकास: स्वतंत्रता के बाद, भारत ने आयुर्वेद और यूनानी जैसी पारंपरिक प्रणालियों को मान्यता दी, जिसके परिणामस्वरूप 2014 में इन प्रथाओं को बढ़ावा देने और विनियमित करने के लिए आयुष मंत्रालय की स्थापना की गई।
- मुख्यधारा की स्वास्थ्य सेवा के साथ एकीकरण: पारंपरिक चिकित्सा सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों में तेजी से एकीकृत हो गई है, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (2017) और आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों जैसी पहलों में परिलक्षित होती है।
- औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमों का नियम 2(ईई): यह नियम "पंजीकृत चिकित्सा चिकित्सकों" को परिभाषित करता है जो आधुनिक दवाएं लिख सकते हैं, जिससे राज्य सरकारों को गैर-एमबीबीएस चिकित्सकों को भी इसमें शामिल करने का विवेकाधिकार प्राप्त हो जाता है, जिसके कारण कानूनी विवाद चल रहे हैं।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा पर प्रभाव: आयुष पद्धतियों को आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिससे वंचित क्षेत्रों में पारंपरिक उपचारों तक पहुंच को बढ़ावा मिलेगा और रोगियों के लिए लागत कम होगी।
- आगे बढ़ते हुए, पारंपरिक चिकित्सा के साक्ष्य-आधारित एकीकरण को मजबूत करना, स्वास्थ्य प्रशासन को राजनीतिकरण से मुक्त करना, तथा यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आयुष पद्धतियों को वैज्ञानिक रूप से मान्य किया जाए तथा जनता का विश्वास और सुरक्षा बनाए रखने के लिए विनियमित किया जाए।
न्याय ठप्प: भारत की अदालतें ठसाठस भरी हुई हैं

चर्चा में क्यों?
भारत की न्यायिक प्रणाली वर्तमान में लंबित मुकदमों के बोझ तले दबी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है, और विभिन्न अदालतों में 4.5 करोड़ से ज़्यादा मामले लंबित हैं। इस स्थिति ने न्याय व्यवस्था की दक्षता और जनता के विश्वास पर इसके प्रभाव को लेकर चिंताएँ पैदा कर दी हैं।
चाबी छीनना
- न्यायिक विलंब से न्याय व्यवस्था में जनता का विश्वास कम हो रहा है।
- लंबित मामलों के लिए न्यायिक रिक्तियों और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे सहित विभिन्न प्रणालीगत मुद्दों को जिम्मेदार ठहराया गया है।
- लोक अदालतों जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्रों को पारंपरिक अदालतों पर बोझ कम करने के समाधान के रूप में रेखांकित किया जा रहा है।
अतिरिक्त विवरण
- न्यायिक रिक्तियाँ: न्यायाधीशों की भारी कमी के कारण शेष न्यायाधीशों पर कार्यभार बढ़ जाता है, जिससे मामलों की सुनवाई में लंबा समय लगता है। 2024 तक, उच्च न्यायालयों में 30% से ज़्यादा पद रिक्त हैं, जिससे यह समस्या और भी गंभीर हो गई है।
- प्रक्रियागत अक्षमताएँ: पुरानी कानूनी प्रक्रियाएँ और बार-बार स्थगन के कारण मामलों की सुनवाई में अनावश्यक देरी होती है। उदाहरण के लिए, दीवानी मुकदमों में अक्सर नियमित स्थगन देखने को मिलता है जिससे सुनवाई कई सालों तक खिंच सकती है।
- एडीआर का प्रभाव: मध्यस्थता और पंचनिर्णय सहित वैकल्पिक विवाद समाधान विधियाँ, औपचारिक न्यायिक प्रणाली के बाहर विवादों को सुलझाने में मदद करती हैं, जिससे लंबित मामलों की संख्या कम होती है। दिल्ली मध्यस्थता केंद्र ने 2005 में अपनी स्थापना के बाद से 2 लाख से ज़्यादा मामलों का निपटारा किया है।
- लोक अदालतें: ये बड़ी संख्या में मामलों, खासकर समझौता योग्य दीवानी और छोटे-मोटे आपराधिक मामलों को शीघ्रता से निपटाने में कारगर होती हैं। हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत ने केवल एक दिन में 1 करोड़ मामलों का निपटारा करके उनकी दक्षता को दर्शाया।
- भारत की न्यायिक प्रणाली को प्रभावित करने वाले व्यवस्थागत मुद्दों के समाधान हेतु तत्काल सुधार आवश्यक हैं, जिनमें न्यायिक नियुक्तियों में वृद्धि और एडीआर तंत्र को बढ़ावा देना शामिल है। कानूनी साक्षरता में सुधार और डिजिटल समाधानों को एकीकृत करने से न्यायिक प्रक्रिया की समग्र दक्षता में भी वृद्धि हो सकती है।
POSH अधिनियम के अंतर्गत आंतरिक शिकायत समिति (ICC)

चर्चा में क्यों?
ओडिशा में एक दुखद घटना हुई, जिसमें एक छात्रा ने अपने कॉलेज की आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायत खारिज किए जाने के बाद आत्महत्या कर ली। इस घटना ने अधिक प्रभावी शिकायत तंत्र की तत्काल आवश्यकता को उजागर किया है।
चाबी छीनना
- आईसीसी की स्थापना कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पीओएसएच अधिनियम) के तहत की गई है।
- 10 या अधिक कर्मचारियों वाले सभी संगठनों के लिए आईसीसी रखना अनिवार्य है।
- आईसीसी का उद्देश्य उत्पीड़न की शिकायतों का समाधान करके महिलाओं के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल उपलब्ध कराना है।
अतिरिक्त विवरण
- कानूनी आधार: आईसीसी को POSH अधिनियम द्वारा अधिदेशित किया गया था, जो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।
- संरचना: आईसीसी में एक वरिष्ठ महिला कर्मचारी, कम से कम दो आंतरिक सदस्य जो कानूनी या सामाजिक विशेषज्ञता रखते हों, और एक बाहरी सदस्य जो यौन उत्पीड़न के मुद्दों का जानकार हो, शामिल होना चाहिए। कम से कम 50% सदस्य महिलाएँ होनी चाहिए।
- शक्तियाँ और कार्य: आईसीसी घटना के तीन महीने के भीतर शिकायतें स्वीकार कर सकती है, सुलह का प्रस्ताव दे सकती है और औपचारिक जाँच शुरू कर सकती है। इसके पास सिविल कोर्ट के समान शक्तियाँ हैं, जिनमें गवाहों को बुलाना और साक्ष्य एकत्र करना शामिल है। जाँच गोपनीयता बनाए रखते हुए 90 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए।
- जाँच के बाद की कार्रवाई: जाँच के बाद, आईसीसी अनुशासनात्मक कार्रवाई या मामले को बंद करने की सिफारिश करती है, और नियोक्ता को इन सिफारिशों पर 60 दिनों के भीतर कार्रवाई करनी होती है। अगर शिकायतकर्ता आपराधिक कार्रवाई चाहता है, तो आईसीसी एफआईआर दर्ज करने में भी मदद कर सकता है।
- यह समाचार शैक्षणिक संस्थानों और कार्यस्थलों पर महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने हेतु आईसीसी प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन की महत्वपूर्ण आवश्यकता को रेखांकित करता है। पॉश अधिनियम लैंगिक न्याय को बनाए रखने और आवश्यक निवारण तंत्र प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी ढाँचे के रूप में कार्य करता है।
किशोर यौन संबंधों को अपराध घोषित करने से POCSO अधिनियम का उद्देश्य कमज़ोर नहीं होगा

चर्चा में क्यों?
यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित करने के लिए परीक्षणाधीन है कि क्या 16-18 वर्ष की आयु के किशोरों के बीच सहमति से यौन गतिविधियों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाना चाहिए।
चाबी छीनना
- किशोरों के बीच सहमति से बनाए गए संबंधों को अपराध घोषित करने से कानून का दुरुपयोग होता है।
- किशोरों को सहमति से लिए गए निर्णयों के कारण उनकी यौन स्वायत्तता और स्वतंत्रता से वंचित किया जाता है।
- अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों द्वारा मान्यता प्राप्त विकासशील क्षमताओं के आधार पर सहमति से बनाए गए संबंधों के लिए कानूनी अपवाद मौजूद हैं।
अतिरिक्त विवरण
- सहमति से बने संबंधों का अन्यायपूर्ण उत्पीड़न: अपराधीकरण के परिणामस्वरूप स्वैच्छिक संबंधों में रहने वाले युवाओं के विरुद्ध अनावश्यक कानूनी कार्रवाई होती है। अदालतों ने पाया है कि किशोरों को संरक्षण देने के बजाय, उन्हें अपराधी माना जाता है, जो पॉक्सो अधिनियम के सुरक्षात्मक उद्देश्य के विपरीत है।
- यौन स्वायत्तता से इनकार: किशोरों को उनकी सहमति से लिए गए निर्णयों में अधिकारहीन माना जाता है, जिन्हें यौन अपराध माना जाता है। पोक्सो की धारा 2(डी) के अनुसार, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को बच्चों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिससे उनकी सहमति कानूनी रूप से निरर्थक हो जाती है।
- किशोरों की विकासशील क्षमता: संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन (यूएनसीआरसी) मानता है कि किशोरों में विकासशील क्षमताएँ होती हैं और उनमें सहमति से बने संबंधों के बारे में सोच-समझकर निर्णय लेने की परिपक्वता हो सकती है। मद्रास उच्च न्यायालय ने सुझाव दिया है कि किशोरों के बीच सहमति से बने संबंधों को अपराध नहीं माना जाना चाहिए, खासकर जब उम्र का अंतर न्यूनतम हो (5 वर्ष के भीतर)।
- कानूनी सिफारिशें: भारतीय विधि आयोग ने ऐसे मामलों में "निर्देशित न्यायिक विवेक" की वकालत की है, जिससे न्यायाधीशों को दंड निर्धारित करते समय संबंधों की सहमति की प्रकृति पर विचार करने की अनुमति मिल सके, जिससे किशोर साथियों के लिए कठोर सजा से बचा जा सके।
- पॉक्सो अधिनियम और सहमति की उम्र को लेकर चल रही बहस, प्रगतिशील समाज की वास्तविकताओं के अनुरूप कानूनी ढाँचे की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि सामान्य किशोर व्यवहार को अपराध न माना जाए और साथ ही व्यक्तियों को शोषण से भी बचाया जाए।
आंतरिक शिकायत समितियों का कार्य
चर्चा में क्यों?
ओडिशा के बालासोर में हुई एक दुखद घटना ने आंतरिक शिकायत समितियों (ICC) की कार्यप्रणाली पर ध्यान आकर्षित किया है। एक छात्रा ने अपने विभागाध्यक्ष के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत कॉलेज की ICC द्वारा खारिज किए जाने के बाद आत्मदाह कर लिया। उसके परिवार का आरोप है कि समिति पक्षपाती थी और उसे उचित प्रशिक्षण नहीं मिला था, जिससे संस्थागत शिकायत निवारण प्रणालियों की प्रभावशीलता और निष्पक्षता पर गंभीर चिंताएँ पैदा हो रही हैं।
चाबी छीनना
- आईसीसी की स्थापना शैक्षणिक और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों का समाधान करने के लिए की गई थी।
- POSH अधिनियम के तहत 10 से अधिक कर्मचारियों वाले कार्यस्थलों पर ICC के गठन का प्रावधान है।
- आईसीसी का कार्यान्वयन असंगत रहा है, तथा उनके प्रशिक्षण और प्रभावशीलता के संबंध में आलोचनाएं होती रही हैं।
अतिरिक्त विवरण
- आईसीसी के पीछे कानूनी ढाँचा: आईसीसी की नींव सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में विशाखा दिशानिर्देशों के माध्यम से रखी थी। ये दिशानिर्देश राजस्थान में एक सामाजिक कार्यकर्ता भंवरी देवी के साथ हुए सामूहिक बलात्कार के बाद बनाए गए थे और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को परिभाषित करते थे। इनमें निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं के नेतृत्व में और बाहरी पक्षों को शामिल करके शिकायत समितियों के गठन का आदेश दिया गया था।
- पॉश अधिनियम: कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 ने 10 से अधिक कर्मचारियों वाले सभी कार्यस्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग (ICC) की स्थापना अनिवार्य कर दी। इसने छोटे या अनौपचारिक कार्यस्थलों पर कार्यरत महिलाओं को जिला प्राधिकारियों द्वारा गठित स्थानीय समितियों के माध्यम से निवारण प्राप्त करने की भी अनुमति दी।
- आईसीसी की संरचना: प्रत्येक आईसीसी का नेतृत्व एक वरिष्ठ महिला कर्मचारी द्वारा किया जाना चाहिए और इसमें प्रासंगिक अनुभव वाले कम से कम दो आंतरिक सदस्य शामिल होने चाहिए। इसके अतिरिक्त, एक बाहरी सदस्य भी आवश्यक है, जो आमतौर पर किसी गैर-सरकारी संगठन से हो, और कम से कम आधे सदस्य महिलाएँ होनी चाहिए।
- शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया: पीड़ित महिला घटना के तीन महीने के भीतर लिखित शिकायत दर्ज करा सकती है। आईसीसी को 90 दिनों के भीतर अपनी जाँच पूरी करनी होगी और सभी संबंधित पक्षों की पहचान के संबंध में सख्त गोपनीयता बनाए रखनी होगी।
- इस ढाँचे के बावजूद, अंतर्राष्ट्रीय अपराध संहिता (ICC) का कार्यान्वयन अभी भी खराब है, सर्वोच्च न्यायालय ने इसके प्रवर्तन पर चिंता व्यक्त की है और तत्काल अनुपालन का आह्वान किया है। कार्यकर्ताओं ने प्रशिक्षण और गोपनीयता की कमी जैसे मुद्दों को उजागर किया है, जिसके कारण शिकायत निवारण अप्रभावी हो रहा है।
- बालासोर का हालिया मामला उचित रूप से संरचित और लागू आईसीसी की आवश्यकता को रेखांकित करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अनुपालन के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करने के बजाय प्रभावी ढंग से कार्य करें।
कारगिल विजय दिवस
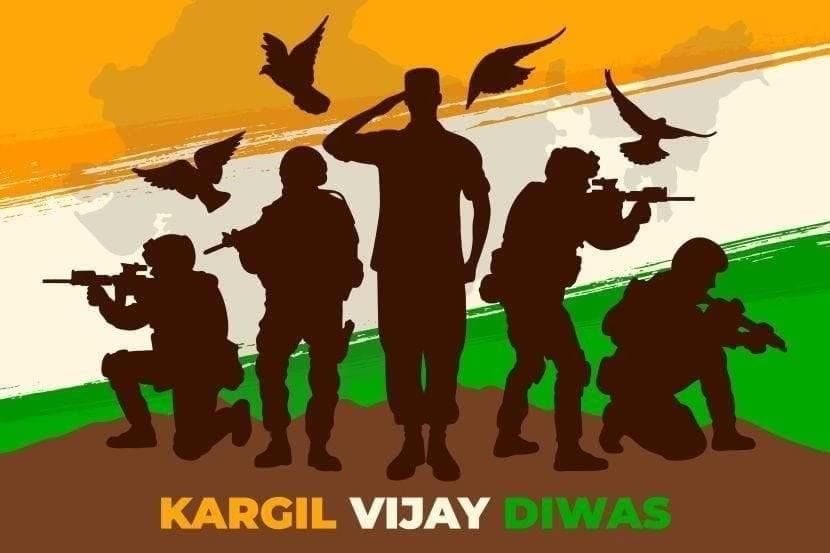
चर्चा में क्यों?
कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ के अवसर पर, भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने कारगिल युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर सैनिकों को सम्मानित करने में राष्ट्र का नेतृत्व किया।
चाबी छीनना
- कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध में भारत की जीत की याद में मनाया जाता है।
- वर्ष 2025 इस महत्वपूर्ण घटना की 26वीं वर्षगांठ होगी।
अतिरिक्त विवरण
- कारगिल युद्ध: यह संघर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच मई से जुलाई 1999 तक कश्मीर के कारगिल जिले में नियंत्रण रेखा (एल.ओ.सी.) पर हुआ था।
- कारण: कश्मीर पर तनाव को हल करने के उद्देश्य से फरवरी 1999 में लाहौर घोषणा के बाद, पाकिस्तानी सेना ने 1998-1999 की सर्दियों के दौरान गुप्त रूप से भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की।
- ऑपरेशन विजय: भारतीय सेना ने प्रसिद्ध 'टाइगर हिल' सहित रणनीतिक ठिकानों को पुनः प्राप्त करने के लिए 'ऑपरेशन विजय' शुरू किया।
- उच्च ऊंचाई वाला युद्ध: यह युद्ध अत्यधिक ऊंचाई पर लड़ा गया था, जिसमें 18,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर लड़ा गया था।
- हताहत: संघर्ष के दौरान लगभग 500 भारतीय सैनिक और लगभग 1,000 पाकिस्तानी सैनिक मारे गये।
- 26 जुलाई, 1999 को कारगिल युद्ध समाप्त हुआ, जो भारत के सैन्य इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। सैनिकों द्वारा दिए गए बलिदानों को प्रतिवर्ष स्मरण किया जाता है, जो राष्ट्र को भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए उनके पराक्रम और समर्पण की याद दिलाता है।
भारत के लोकपाल
चर्चा में क्यों?
भारत का लोकपाल, जो देश के केंद्रीय भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के रूप में कार्य करता है, प्रतिनियुक्ति के आधार पर 81 स्वीकृत पदों को भरने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
चाबी छीनना
- लोकपाल का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1966 में उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार से निपटने के लिए रखा गया था।
- अनेक प्रयासों के बावजूद 1971 से 2008 के बीच प्रस्तुत लोकपाल विधेयक पारित नहीं हो सके।
- 2011 में अन्ना हजारे के नेतृत्व में जन लोकपाल आंदोलन ने एक मजबूत भ्रष्टाचार विरोधी निकाय के लिए जनता का समर्थन जुटाया।
- लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 में अधिनियमित किया गया, जिसके तहत 2014 में औपचारिक रूप से लोकपाल की स्थापना की गई।
- स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए 2024 में एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक पुनर्गठन किया जाएगा।
अतिरिक्त विवरण
- प्रारंभिक प्रस्ताव (1966): लोकपाल की अवधारणा पहली बार प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए पेश की गई थी।
- विधायी विफलताएं (1971-2008): संसद में अनेक लोकपाल विधेयक पेश किए गए, लेकिन कोई भी कानून नहीं बन सका।
- जन लोकपाल आंदोलन (2011): इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन ने एक अधिक स्वतंत्र और शक्तिशाली भ्रष्टाचार विरोधी निकाय की मांग की, जिसने जनमत और राजनीतिक दबाव को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया।
- औपचारिक स्थापना (2014): भारत के लोकपाल को 16 जनवरी, 2014 को लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के तहत आधिकारिक तौर पर अधिसूचित किया गया था।
- हालिया घटनाक्रम (2024): बढ़ती शिकायतों और अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता के मद्देनजर, भविष्य में नियमित भर्ती के लिए 81 प्रतिनियुक्ति पदों को मंजूरी दी गई।
कुल मिलाकर, लोकपाल का विकास भारत में भ्रष्टाचार के विरुद्ध चल रहे संघर्ष को दर्शाता है, जिसमें महत्वपूर्ण सुधार और जन आंदोलन इसके वर्तमान ढांचे को आकार दे रहे हैं।
मानसिक स्वास्थ्य दिशानिर्देश - बढ़ती छात्र आत्महत्याओं पर सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिक्रिया
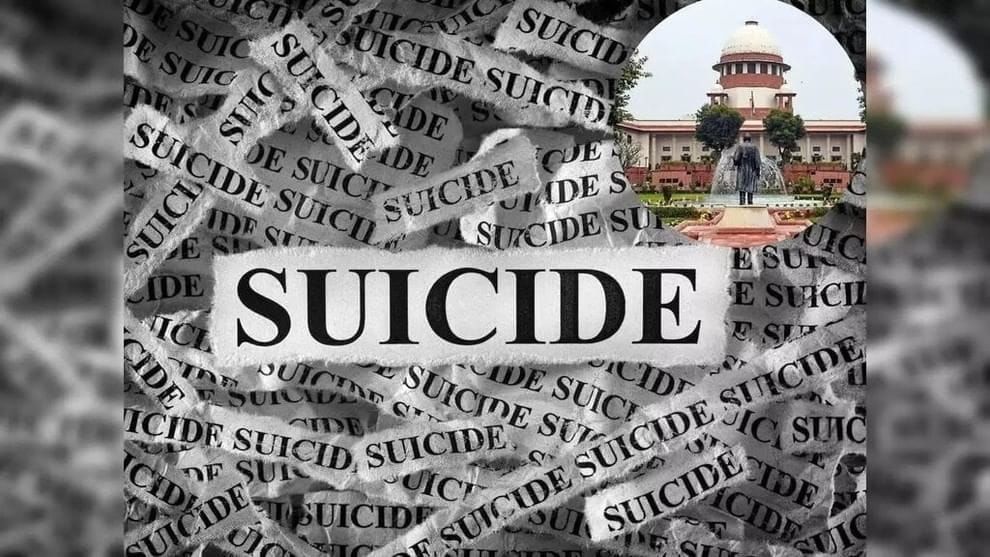
चर्चा में क्यों?
सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में छात्रों की आत्महत्याओं में चिंताजनक वृद्धि के मद्देनजर देश भर के शैक्षणिक संस्थानों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
चाबी छीनना
- सर्वोच्च न्यायालय ने छात्रों के बीच मानसिक स्वास्थ्य संकट को "व्यवस्थागत विफलता" बताया।
- 2022 में 13,044 छात्र आत्महत्याएं दर्ज की गईं, जो भारत में कुल आत्महत्याओं का 7.6% है।
- नये दिशानिर्देशों के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की नियुक्ति अनिवार्य है।
अतिरिक्त विवरण
- परिसरों में आत्महत्याएं: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने छात्र आत्महत्याओं में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है, जो 2001 में 5,425 से बढ़कर 2022 में 13,044 हो गई है, जिसमें एक उल्लेखनीय हिस्सा परीक्षा में असफलता से जुड़ा है।
- सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश: न्यायालय ने सभी शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होने वाले 15 बाध्यकारी दिशानिर्देश जारी किए, तथा उनसे मानसिक स्वास्थ्य नीतियों और सहायता प्रणालियों को लागू करने का आग्रह किया।
- अनिवार्य परामर्शदाता: 100 से अधिक छात्रों वाले संस्थानों को योग्य मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों को नियुक्त करना होगा, जबकि छोटे संस्थानों को रेफरल लिंक स्थापित करना होगा।
- बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के उपाय: आवासीय संस्थानों को भौतिक सुरक्षा उपाय करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि छेड़छाड़-रोधी छत पंखे लगाना।
- भेदभावपूर्ण प्रथाओं को समाप्त करना: संस्थानों से आग्रह किया जाता है कि वे उन प्रथाओं को समाप्त करें जो छात्रों को उनके प्रदर्शन के आधार पर अलग करती हैं तथा सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा होने से बचें।
- जवाबदेही और संरक्षण: शैक्षणिक संस्थानों को उत्पीड़न और भेदभाव की शिकायतों के समाधान के लिए गोपनीय तंत्र स्थापित करना चाहिए।
- नीतिगत ढांचा: संस्थानों को एक वार्षिक मानसिक स्वास्थ्य नीति प्रकाशित करने की आवश्यकता है, जिसमें मनोदर्पण और राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति जैसी सरकारी पहलों का संदर्भ दिया जाए।
- यह ऐतिहासिक फैसला शैक्षिक प्रणालियों में मानसिक स्वास्थ्य सहायता को एकीकृत करने की आवश्यकता पर ज़ोर देता है, जिससे केवल शैक्षणिक प्रदर्शन से हटकर छात्रों के समग्र कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। सफलता इन परिवर्तनों के प्रभावी कार्यान्वयन और सामाजिक स्वीकृति पर निर्भर करेगी।
मणिपुर में सुधार: नाजुक शांति के लिए वास्तविक सुलह की आवश्यकता
चर्चा में क्यों?
हाल ही में, कुकी-ज़ो और मीतेई समुदायों के बीच चल रहे जातीय संघर्षों के बीच, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को 13 अगस्त, 2025 से प्रभावी, अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।
चाबी छीनना
- सर्वोच्च न्यायालय के एसआर बोम्मई निर्णय (1994) ने अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा की शुरुआत की।
- गठबंधन की राजनीति और क्षेत्रीय दलों के उदय ने राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग को कम कर दिया है।
- जन जागरूकता और मीडिया जांच के कारण राष्ट्रपति शासन के राजनीतिक रूप से प्रेरित थोपे जाने के प्रति विरोध बढ़ गया है।
- मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि का विस्तार जारी जातीय संघर्षों और मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद उत्पन्न राजनीतिक शून्यता के कारण किया गया है।
अतिरिक्त विवरण
- न्यायिक समीक्षा: सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि अनुच्छेद 356 लागू करने का राष्ट्रपति का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है, जिससे राज्य सरकारों को मनमाने ढंग से बर्खास्त करने पर रोक लगेगी।
- जातीय संघर्ष: हिंसा में कमी के बावजूद, मेइती बहुसंख्यक और कुकी-ज़ो अल्पसंख्यक के बीच चल रहे जातीय तनाव का समाधान नहीं हो पाया है।
- राजनीतिक शून्यता: मुख्यमंत्री के इस्तीफे से शासन में शून्यता पैदा हो गई, जिससे व्यवस्था बहाल करने के लिए केंद्रीय हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ी।
- ऐतिहासिक तनाव: मणिपुर की जातीय संरचना और ऐतिहासिक शिकायतों ने वर्तमान संकट को बढ़ावा दिया है, विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मेइती की मांग, जिसने मई 2023 में संघर्ष को तीव्र कर दिया।
- मणिपुर की स्थिति सुलह-समझौते की दिशा में एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता को उजागर करती है, जिसमें क्षेत्र में शांति को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक संवाद, कानून के शासन और नागरिक समाज के सशक्तिकरण के महत्व पर बल दिया गया है।
राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति
चर्चा में क्यों?
केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (एनसीएमसी) की स्थापना की है, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव डालने वाली बड़ी आपदाओं से उत्पन्न स्थितियों का प्रभावी ढंग से समाधान किया जा सके।
चाबी छीनना
- एनसीएमसी का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत किया गया है।
- यह प्रमुख आपदा स्थितियों के प्रबंधन के लिए सर्वोच्च निकाय के रूप में कार्य करता है।
अतिरिक्त विवरण
- संरचना: एनसीएमसी की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री करते हैं, तथा इसके सदस्यों में केंद्रीय गृह सचिव, रक्षा सचिव (समन्वय के लिए) तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख शामिल होते हैं।
- भूमिका: आपदा की स्थिति में आवश्यकतानुसार अध्यक्ष केन्द्रीय या राज्य सरकारों या अन्य संगठनों से विशेषज्ञों या अधिकारियों को शामिल कर सकता है।
- समिति संभावित आपदाओं के लिए तैयारियों का मूल्यांकन करती है तथा तत्परता बढ़ाने के लिए निर्देश प्रदान करती है।
- यह आपदा प्रतिक्रिया में शामिल संबंधित मंत्रालयों, राज्य सरकारों और सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठनों की कार्रवाइयों का समन्वय और निगरानी करता है।
- यह देश भर में प्रभावी आपदा प्रतिक्रिया समन्वय के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करता है।
- एनसीएमसी का गठन सरकार की प्रमुख आपदाओं को व्यवस्थित रूप से संबोधित करने और प्रबंधित करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जिससे जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए एक समन्वित प्रतिक्रिया तंत्र सुनिश्चित होता है।
भारत की चुनावी संरचना में खामियाँ स्पष्ट दिखाई दे रही हैं
चर्चा में क्यों?
भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) बिहार में मतदाता सूचियों के अपने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के पहले चरण को 1 अगस्त, 2025 तक पूरा कर रहा है। इस प्रक्रिया ने मताधिकार से वंचित करने के आरोपों पर चर्चाओं को जन्म दिया है, जो विशेष रूप से गरीबों, अल्पसंख्यकों और प्रवासियों को प्रभावित कर रहे हैं। आलोचकों का तर्क है कि ईसीआई के तरीके पक्षपातपूर्ण हैं, जबकि समर्थक मतदाता सूचियों की अखंडता बनाए रखने के महत्व पर ज़ोर देते हैं। हालाँकि, दोनों ही दृष्टिकोण भारत के अत्यधिक गतिशील समाज के संबंध में भारत के चुनावी कानूनों में निहित गहरे मुद्दों की अनदेखी करते हैं।
चाबी छीनना
- ऐतिहासिक चुनावी कानून पुराने हो चुके हैं और उनमें भारत के महत्वपूर्ण आंतरिक प्रवासन को शामिल नहीं किया गया है।
- मताधिकार से वंचित होने से लाखों लोग प्रभावित हैं, संशोधन प्रक्रिया के दौरान अकेले बिहार में 1.2 मिलियन से अधिक नाम हटा दिए गए।
- नागरिकता और निवास का मिश्रण आंतरिक प्रवासियों के लिए मतदाता पंजीकरण को जटिल बना देता है।
- अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण दर्शाते हैं कि चुनावी अखंडता और समावेशिता के बीच संतुलन बनाने के लिए नवीन समाधान मौजूद हैं।
अतिरिक्त विवरण
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950: यह अधिनियम मुख्यतः ग्रामीण आबादी वाले भारत के लिए बनाया गया था, यह मानते हुए कि नागरिक अपने जन्मस्थान पर ही मतदान करेंगे। आज, 45 करोड़ से ज़्यादा आंतरिक प्रवासियों के साथ, यह धारणा व्यवस्थागत रूप से मताधिकार से वंचित करती है।
- मतदाता सूची से नाम हटाना: 2025 में, बिहार के उच्च प्रवास दर वाले जिलों में 5%-7% मतदाता सूची से नाम हटाए गए, जिससे सत्यापन के दौरान अनुपस्थित रहने वाले लोगों को मताधिकार से वंचित कर दिया गया।
- नागरिकता बनाम निवास: ईसीआई का दृष्टिकोण निवास को प्राथमिकता देता है, जिससे लाखों आंतरिक प्रवासियों को चुनावी भागीदारी से वंचित रखा जाता है।
- अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य: संयुक्त राज्य अमेरिका, फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने मतदाता समावेशन सुनिश्चित करने के लिए उपाय लागू किए हैं, जिससे यह प्रदर्शित होता है कि विधायी सुधार संभव है।
- राजनीतिक दल अक्सर मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने के मुद्दे को संबोधित करने के बजाय इसे लामबंदी के उपकरण के रूप में उपयोग करते हैं।
निष्कर्ष
निष्कर्षतः, चुनाव आयोग को दोषमुक्त करना ज़रूरी तो है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। सच्चा चुनावी न्याय पाने के लिए चुनाव आयोग में सुधार और राजनीतिक व नागरिक समाज की सक्रिय भागीदारी, दोनों ज़रूरी हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी नागरिक चुनावी प्रक्रिया में शामिल हों और उनकी आवाज़ सुनी जाए।
मणिपुर में राष्ट्रपति शासन का विस्तार
चर्चा में क्यों?
गृह मंत्री मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को छह महीने के लिए बढ़ाने के उद्देश्य से राज्यसभा में एक वैधानिक प्रस्ताव पेश करने की तैयारी कर रहे हैं।
चाबी छीनना
- राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य किसी राज्य के संवैधानिक ढांचे को निलंबित करके उसे सीधे केंद्र सरकार के अधीन कर देना है।
- राष्ट्रपति शासन का संवैधानिक आधार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355, 356 और 365 में पाया जाता है।
अतिरिक्त विवरण
- राष्ट्रपति शासन क्या है? यह उस स्थिति को दर्शाता है जहाँ राज्य सरकार निलंबित कर दी जाती है, और राष्ट्रपति केंद्र सरकार के माध्यम से नियंत्रण अपने हाथ में ले लेते हैं।
- संवैधानिक आधार:
- अनुच्छेद 355: संघ को यह सुनिश्चित करने का अधिकार देता है कि राज्यों में शासन संविधान के अनुरूप हो।
- अनुच्छेद 356(1): यदि संवैधानिक विफलता की सूचना मिलती है तो राष्ट्रपति को राज्य की कार्यपालिका को अपने नियंत्रण में लेने का अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 365: संघ के निर्देशों का पालन करने में राज्य की विफलता को संवैधानिक तंत्र की विफलता मानता है।
- अवधि और विस्तार:
- प्रारंभिक अवधि घोषणा तिथि से मान्य है।
- संसदीय अनुमोदन से प्रत्येक छह माह में विस्तार संभव है, तथा अधिकतम तीन वर्ष तक हो सकता है।
- निरसन:
- इसे राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 356(2) के तहत संसदीय अनुमोदन के बिना कभी भी रद्द किया जा सकता है।
- सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय:
- एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ (1994): यह स्थापित किया गया कि राष्ट्रपति शासन न्यायिक समीक्षा के अधीन है, और बहुमत साबित करने के लिए शक्ति परीक्षण आवश्यक है।
- सर्बानंद सोनोवाल बनाम भारत संघ (2005): संघ द्वारा निवारक कार्रवाई के दायरे का विस्तार किया गया।
- रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ (2006): बिहार विधानसभा के विघटन को असंवैधानिक घोषित किया गया।
- प्रमुख सुधार/सिफारिशें:
- सरकारिया आयोग (1987): सुझाव दिया कि राष्ट्रपति शासन केवल अंतिम उपाय होना चाहिए।
- पुंछी आयोग (2010): पूरे राज्य के बजाय विशिष्ट क्षेत्रों के लिए स्थानीयकृत आपातकालीन प्रावधानों की सिफारिश की गई।
- संविधान के कार्यकरण की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग (2000): अनुच्छेद 356 के संयमित उपयोग की वकालत की गई तथा चुनाव अव्यवहार्य होने पर राष्ट्रीय आपातकाल के बिना इसके अनुप्रयोग के लिए संशोधन का प्रस्ताव रखा गया।
निष्कर्ष
मणिपुर में राष्ट्रपति शासन का विस्तार एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम है, जो संघ के नियंत्रण वाले राज्यों में शासन और संवैधानिक अनुपालन पर सवाल उठाता है।
क्लीन हाउस: भारत में सेप्टिक टैंकों से कीचड़ निकालने पर
चर्चा में क्यों?
हाल ही में, संसद में प्रस्तुत एक सामाजिक लेखापरीक्षा से पता चला है कि 2022-23 में खतरनाक सफाई के कारण 150 मौतें हुईं। यह चिंताजनक आँकड़ा असुरक्षित आउटसोर्सिंग प्रथाओं, सुरक्षा कानूनों के अपर्याप्त प्रवर्तन और नमस्ते जैसी योजनाओं के लिए अपर्याप्त धन पर प्रकाश डालता है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों और ओडिशा तथा तमिलनाडु जैसे राज्यों में सफल मॉडलों के बावजूद, पूरे देश में स्वच्छता में मशीनीकरण का कार्यान्वयन गंभीर रूप से अपर्याप्त बना हुआ है।
चाबी छीनना
- मौजूदा कानूनों और योजनाओं के बावजूद मैनुअल स्कैवेंजिंग का प्रचलन जारी है।
- कानूनी प्रावधानों का कमजोर प्रवर्तन और स्वच्छता पहलों के लिए अपर्याप्त वित्तपोषण।
- ओडिशा और तमिलनाडु जैसे राज्यों के सफल मॉडल वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।
अतिरिक्त विवरण
- कानूनी प्रावधानों का कमज़ोर प्रवर्तन: मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोज़गार निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 के बावजूद, प्रवर्तन न्यूनतम बना हुआ है। उदाहरण के लिए, 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2022-23 में खतरनाक सफाई के दौरान 150 मज़दूरों की मौत हो गई।
- योजनाओं का खराब क्रियान्वयन और अपर्याप्त वित्त पोषण: अपर्याप्त वित्तीय सहायता और कम पहुँच के कारण नमस्ते जैसी योजनाएँ असफल हो रही हैं। खतरनाक सफाई कार्यों में लगे 57,758 श्रमिकों में से केवल 16,791 को ही पीपीई किट मिले, जो मशीनीकरण के लिए जारी किए गए ₹14 करोड़ की अपर्याप्तता को दर्शाता है।
- नियोक्ता की ज़िम्मेदारी का छिपाया जाना: उप-ठेकेदारी का इस्तेमाल नियोक्ताओं को कर्मचारियों की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी से बचने का मौका देता है। एक सामाजिक ऑडिट से पता चला है कि खतरनाक सफाई से हुई 54 मौतों में से सिर्फ़ पाँच कर्मचारी ही सरकारी वेतन पर थे, जिससे जवाबदेही और भी जटिल हो गई।
- ओडिशा और तमिलनाडु में सफल मॉडल: इन राज्यों ने चिन्हित सफाई कर्मचारियों को मशीनीकृत मल निकासी वाहनों से लैस किया है, जिससे सुरक्षा बढ़ी है और शारीरिक श्रम कम हुआ है। उदाहरण के लिए, अब सीवर की सफाई के लिए वैक्यूम ट्रकों का उपयोग किया जाता है, और हाथ से मैला ढोने की प्रथा को खत्म करने के लिए रोबोटिक हस्तक्षेपों का परीक्षण किया गया है।
- ग्रामीण आंकड़ों का अभाव: ग्रामीण सफाई कर्मचारियों पर विश्वसनीय आंकड़ों का अभाव मशीनीकरण योजनाओं की प्रभावशीलता को सीमित करता है, जिससे कई कर्मचारी अपंजीकृत और लापता रह जाते हैं। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण प्रखंडों में, कोई सुरक्षात्मक उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, जिससे श्रमिकों को खतरनाक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है।
- सरकारी पहल: भारत सरकार ने हाथ से मैला ढोने की प्रथा पर प्रतिबंध लगाने और यंत्रीकृत स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए नमस्ते योजना शुरू करने जैसे कदम उठाए हैं। कल्याणकारी पहलों में आयुष्मान भारत के तहत नकद सहायता और स्वास्थ्य बीमा शामिल हैं।
- मैनुअल स्कैवेंजिंग और श्रमिक सुरक्षा के मुद्दों को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए, सुधारों को अनिवार्य मशीनीकरण, वित्तीय पुनर्वास और सफाई कर्मचारियों के व्यापक दस्तावेजीकरण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि जवाबदेही और समर्थन सुनिश्चित किया जा सके।
राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 - भारत के सहकारी आंदोलन को पुनर्जीवित करना
चर्चा में क्यों?
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में एक नई राष्ट्रीय सहकारी नीति पेश की है, जो पिछले 23 वर्षों से चली आ रही मौजूदा व्यवस्था को बदल देगी। इस पहल का उद्देश्य सहकारी क्षेत्र की संस्थागत क्षमता को बढ़ाना, उसका दायरा व्यापक बनाना और उसे भारत के समग्र विकास उद्देश्यों के साथ जोड़ना है।
चाबी छीनना
- नई नीति सहकार से समृद्धि (सहकारिता के माध्यम से समृद्धि) के दृष्टिकोण से निर्देशित है ।
- इसकी योजना 2034 तक सकल घरेलू उत्पाद में सहकारी क्षेत्र के योगदान को तीन गुना बढ़ाने की है।
- प्रत्येक गांव में कम से कम एक सहकारी समिति स्थापित की जाएगी।
- इस नीति का उद्देश्य 50 करोड़ नागरिकों को सक्रिय सहकारी भागीदारी में शामिल करना है।
अतिरिक्त विवरण
- ऐतिहासिक संदर्भ: राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025, वर्ष 2002 के बाद से पहला अद्यतन है, जो वर्ष 2021 में एक अलग सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के माध्यम से सहकारी क्षेत्र के लिए नए सिरे से सरकारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- मुख्य विशेषताएं:यह नीति छह स्तंभों पर आधारित है:
- आधारभूत प्रणालियों को मजबूत करना
- मौजूदा सहकारी समितियों में जीवंतता को बढ़ावा देना
- डिजिटलीकरण और नवाचार के माध्यम से भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयारी
- समावेशिता और आउटरीच को बढ़ाना
- उभरते क्षेत्रों में विस्तार
- युवाओं को शामिल करना और भावी पीढ़ियों के लिए क्षमता निर्माण करना
- आदर्श सहकारी गांव: प्रत्येक तहसील में पांच सहकारी गांव होंगे, जिनका उद्देश्य डेयरी, मत्स्य पालन और पुष्प कृषि जैसे क्षेत्रों के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं का विकास करना होगा।
- संस्थागत सुदृढ़ीकरण: नीति में PACS परिचालनों के पूर्ण कम्प्यूटरीकरण और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी-संचालित शासन को अनिवार्य बनाया गया है।
- आर्थिक प्रभाव: वर्तमान में, सहकारी क्षेत्र भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जिसमें कृषि ऋण और उत्पादन भी शामिल है, जो आत्मनिर्भरता के लिए सदस्य-केंद्रित मॉडल बनाने के लक्ष्य पर जोर देता है।
- राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 में इस व्यापक दृष्टिकोण से समावेशी विकास को बढ़ावा मिलने, ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने और भविष्य के लिए भारत के सहकारी आंदोलन को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
पालना योजना

चर्चा में क्यों?
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री ने हाल ही में राज्यसभा को पालना योजना के कार्यान्वयन और महत्व के बारे में जानकारी दी।
चाबी छीनना
- पालना योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक केन्द्र प्रायोजित योजना है।
- इसका उद्देश्य 6 महीने से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण क्रेच सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
- क्रेच की सुविधा सभी माताओं के लिए उपलब्ध है, चाहे उनकी रोजगार स्थिति कुछ भी हो।
अतिरिक्त विवरण
- उद्देश्य:पालना योजना का प्राथमिक लक्ष्य बच्चों के लिए सुरक्षित और पोषणकारी वातावरण सुनिश्चित करना है, जिसमें निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा:
- पोषण संबंधी सहायता
- स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक विकास
- विकास निगरानी और टीकाकरण
- पालना योजना के अंतर्गत दो प्रकार के क्रेच हैं :
- स्टैंडअलोन क्रेच
- आंगनवाड़ी-सह-क्रेच (एडब्ल्यूसीसी)
- संचालन में लचीलापन: क्रेच का समय स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर लचीला बनाया गया है, तथा यह महीने में 26 दिन तथा प्रतिदिन 7.5 घंटे संचालित होता है।
- वित्तपोषण संरचना:वित्तपोषण अनुपात क्षेत्र के अनुसार भिन्न होता है:
- सामान्य राज्य: 60:40 (केंद्र:राज्य)
- पूर्वोत्तर एवं विशेष श्रेणी राज्य: 90:10
- विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेश: 60:40
- विधानमंडल रहित केंद्र शासित प्रदेश: केंद्र से 100% सहायता
- प्रदान की जाने वाली सेवाएं:यह योजना सेवाओं का एक व्यापक पैकेज प्रदान करती है, जिसमें शामिल हैं:
- डेकेयर सुविधाएं, जिसमें शयन सुविधाएं भी शामिल हैं
- 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक उत्तेजना
- 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए पूर्व-विद्यालय शिक्षा
- स्थानीय स्तर पर प्राप्त पूरक पोषण
- विकास निगरानी
- स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण
पालना योजना पूरे भारत में बाल देखभाल सेवाओं में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो यह सुनिश्चित करती है कि बच्चों को उनके प्रारंभिक विकास के लिए आवश्यक सहायता मिले।
स्वच्छ सर्वेक्षण से मुख्य बातें
चर्चा में क्यों?
दुनिया के सबसे बड़े स्वच्छता सर्वेक्षण के रूप में मान्यता प्राप्त, स्वच्छ सर्वेक्षण का नौवाँ संस्करण, भारत में शहरी स्वच्छता में हुई उल्लेखनीय प्रगति को उजागर करता है। स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम)-शहरी के अंतर्गत आयोजित यह सर्वेक्षण 2016 में 100 से भी कम शहरों के बीच एक प्रतियोगिता से बढ़कर 2024-25 में 4,500 से अधिक शहरी केंद्रों के व्यापक मूल्यांकन तक पहुँच गया है। हालाँकि रैंकिंग ध्यान आकर्षित करती है, लेकिन इसका असली महत्व शहरी अपशिष्ट प्रबंधन, शासन व्यवस्था और नागरिकों व नीति निर्माताओं के बीच विकसित होते व्यवहार पैटर्न के बारे में दी गई अंतर्दृष्टि में निहित है।
चाबी छीनना
- स्वच्छ सर्वेक्षण शहर प्रबंधकों और नीति निर्माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन उपकरण के रूप में कार्य करता है।
- यह अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता से संबंधित दस मापदंडों के आधार पर शहरों का मूल्यांकन करता है।
- सुपर स्वच्छ लीग की शुरूआत के माध्यम से सार्वजनिक भागीदारी और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया गया है।
- इंदौर और सूरत जैसे शहरों की सर्वोत्तम प्रथाएं अपशिष्ट प्रबंधन में नवाचार की संभावनाओं को उजागर करती हैं।
- अपशिष्ट न्यूनीकरण और पुनर्चक्रण के प्रति सार्वजनिक व्यवहार को बदलने में चुनौतियां बनी हुई हैं।
अतिरिक्त विवरण
- सुपर स्वच्छ लीग: यह नया ढाँचा शहरों को पाँच जनसंख्या वर्गों में वर्गीकृत करता है, जिससे अहमदाबाद और भोपाल जैसे शहरों को अपनी रैंकिंग सुधारने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए, भुवनेश्वर का 34वें स्थान से 9वें स्थान पर पहुँचना इस दृष्टिकोण की प्रभावशीलता को दर्शाता है।
- सर्वोत्तम अभ्यास: उल्लेखनीय नवाचारों में इंदौर का छह-तरफ़ा अपशिष्ट पृथक्करण मॉडल और सूरत का उपचारित सीवेज का मुद्रीकरण शामिल है, जो दर्शाता है कि किस प्रकार रचनात्मकता और सामुदायिक सहभागिता अपशिष्ट को संसाधनों में परिवर्तित कर सकती है।
- आर्थिक निहितार्थ: कम करें, पुनः उपयोग करें, पुनः चक्रित करें (आरआरआर) पर विषयगत फोकस अपशिष्ट प्रबंधन के आर्थिक लाभों पर जोर देता है, जो पर्यटन और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए आवश्यक है।
- चुनौतियाँ: सर्वेक्षण में वर्तमान चुनौतियों का खुलासा हुआ है, जैसे अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं में व्यवहारिक परिवर्तन की आवश्यकता और प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले 1.5 लाख टन ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन।
निष्कर्ष
स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 शहरी स्वच्छता की दिशा में भारत की यात्रा को दर्शाता है, और दर्शाता है कि प्रभावी प्रतिस्पर्धा, डेटा उपयोग और जनभागीदारी से अपशिष्ट प्रबंधन में उल्लेखनीय सुधार संभव है। सूरत जैसे शहर इस बात का उदाहरण हैं कि परिवर्तन न केवल संभव है, बल्कि विभिन्न शहरी परिवेशों में इसे दोहराया भी जा सकता है।
प्रतिभा सेतु पहल
चर्चा में क्यों?
संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने सिविल सेवा के उन अभ्यर्थियों की क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए प्रतिभा सेतु कार्यक्रम शुरू किया है, जो साक्षात्कार चरण तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन अंतिम मेरिट सूची में जगह नहीं बना पाते।
चाबी छीनना
- इस पहल का उद्देश्य उन अभ्यर्थियों को सत्यापित नियोक्ताओं से जोड़ना है जो यूपीएससी साक्षात्कार में उत्तीर्ण तो हुए, लेकिन चयनित नहीं हुए।
- इसे सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) 2023 के परिणामों के साथ लॉन्च किया गया, जो 2018 में स्थापित सार्वजनिक प्रकटीकरण योजना से विकसित हुआ है।
अतिरिक्त विवरण
- उद्देश्य: इस पहल का उद्देश्य उच्च प्रदर्शन करने वाले उम्मीदवारों के लिए वैकल्पिक कैरियर मार्ग प्रदान करना है, जिन्होंने कठोर यूपीएससी चयन प्रक्रिया के माध्यम से अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
- प्रतिभा पूल: इस कार्यक्रम में 10,000 से अधिक उच्च प्रदर्शन करने वाले उम्मीदवारों का प्रतिभा पूल है, जो नियोक्ताओं को संभावित नियुक्तियों के एक अच्छी तरह से मूल्यांकित समूह तक पहुंच प्रदान करता है।
- पात्रता: विभिन्न सेवाओं जैसे सिविल सेवा, भारतीय वन सेवा, इंजीनियरिंग सेवा और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के उम्मीदवार इसमें शामिल हैं, जबकि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी के उम्मीदवार इसमें शामिल नहीं हैं।
- भर्तीकर्ता पहुंच: संगठन अपने कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) का उपयोग करके कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं।
- प्लेटफ़ॉर्म उपकरण: नियोक्ताओं के पास उम्मीदवारों को सूचीबद्ध करने के लिए डैशबोर्ड तक पहुंच होती है और वे उम्मीदवारों की शैक्षिक प्रोफाइल और संपर्क विवरण डिजिटल रूप से देख सकते हैं।
- प्रभाव: यह पहल न केवल यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए नए कैरियर के रास्ते खोलती है, बल्कि नियोक्ताओं के लिए पारदर्शी और कुशल भर्ती प्रक्रियाओं की सुविधा भी प्रदान करती है।
संक्षेप में, प्रतिभा सेतु पहल यूपीएससी चयन प्रक्रिया की प्रासंगिकता को केवल अंतिम नियुक्तियों तक ही सीमित नहीं रखती, बल्कि उसे और भी अधिक प्रासंगिक बनाती है, जिससे भारत में अभ्यर्थियों और नियोक्ताओं दोनों को लाभ मिलता है।
मतदान का अधिकार - भारत में इसकी कानूनी स्थिति और संवैधानिक विकास को समझना
चर्चा में क्यों?
सर्वोच्च न्यायालय वर्तमान में बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से संबंधित मामलों की समीक्षा कर रहा है, जिससे भारत में मतदान के अधिकार के बारे में गंभीर कानूनी प्रश्न उठ रहे हैं।
चाबी छीनना
- लोकतांत्रिक कार्य के लिए मतदान का अधिकार आवश्यक है, लेकिन इसे संवैधानिक या वैधानिक के रूप में वर्गीकृत करने पर बहस होती रही है।
- भारतीय कानूनी ढांचे में अधिकारों की विभिन्न श्रेणियां मौजूद हैं, जो मताधिकार की व्याख्या और प्रवर्तन को प्रभावित करती हैं।
अतिरिक्त विवरण
- अधिकारों का वर्गीकरण:
- प्राकृतिक अधिकार: अंतर्निहित और अविभाज्य अधिकार, जैसे जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, जिनकी व्याख्या मौलिक अधिकारों के माध्यम से की जाती है।
- मौलिक अधिकार: संविधान के भाग III में निहित, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता शामिल है, जो अनुच्छेद 32 के तहत लागू करने योग्य है।
- संवैधानिक अधिकार: भाग III के बाहर स्थित, जैसे संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 226 के माध्यम से प्रवर्तनीय।
- वैधानिक अधिकार: संसद या राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित कानूनों से व्युत्पन्न, जैसे मनरेगा के अंतर्गत अधिकार।
- संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 326 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है, जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को कानूनी योग्यता के आधार पर मतदान करने की अनुमति देता है।
- न्यायिक व्याख्याएं: ऐतिहासिक निर्णयों में मतदान के अधिकार को वैधानिक या संवैधानिक के रूप में देखने के बीच उतार-चढ़ाव रहा है।
मतदान के अधिकार की कानूनी स्थिति के बारे में चल रही बहस का चुनावी अखंडता और नागरिक अधिकारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जिसके लिए उभरते लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आलोक में स्पष्टता और संभावित पुनर्विचार की आवश्यकता है।
धर्मस्थल मंजुनाथेश्वर मंदिर
चर्चा में क्यों?
कर्नाटक सरकार द्वारा एक विशेष जाँच दल (एसआईटी) के गठन के बाद, धर्मस्थल स्थित श्री धर्मस्थल मंजुनाथेश्वर मंदिर हाल ही में जाँच के दायरे में आ गया है। यह जाँच इस महत्वपूर्ण तीर्थस्थल में अज्ञात शवों के सामूहिक गुप्त दफ़न से संबंधित आरोपों की जाँच कर रही है।
चाबी छीनना
- यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जिन्हें यहां भगवान मंजूनाथ के रूप में पूजा जाता है।
- इसका इतिहास बहुत समृद्ध है, जो लगभग 800 वर्ष पुराना है।
- मंदिर का प्रशासन एक वंशानुगत जैन परिवार द्वारा प्रबंधित किया जाता है जिसे हेग्गेड्स के नाम से जाना जाता है।
अतिरिक्त विवरण
- वास्तुकला: यह मंदिर केरल मंदिर वास्तुकला का प्रदर्शन करता है , जो अन्य दक्षिण भारतीय स्थापत्य शैलियों से अलग है। यह विशिष्टता इसकी संरचना और डिज़ाइन में स्पष्ट दिखाई देती है।
- निर्माण सामग्री: मंदिर में लकड़ी, मिट्टी, पत्थर, धातु और लेटराइट सहित विभिन्न सामग्रियों का उपयोग किया गया है। आधार संरचना मुख्यतः ग्रेनाइट और लेटराइट से बनी है।
- मंदिर की योजना वर्गाकार है, जिसमें पिरामिडनुमा ढलान वाली छत है, तथा ढांचे की सुरक्षा के लिए सोने की परत चढ़ी तांबे की प्लेटों से सुसज्जित लकड़ी की छत है।
- लकड़ी के खंभे मंदिर के सामने के मंडप को प्रमुखता से सहारा देते हैं।
यह मंदिर न केवल एक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में कार्य करता है, बल्कि इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्थापत्य कला की भव्यता को भी दर्शाता है। चल रही जाँच-पड़ताल, नैतिक और सामाजिक मुद्दों पर समकालीन चर्चाओं में मंदिर के महत्व को उजागर करती है।
राष्ट्रीय खेल नीति 2025 - विज्ञान, समर्थन और सतत उत्कृष्टता की दिशा में एक आदर्श बदलाव
चर्चा में क्यों?
राष्ट्रीय खेल नीति 2025, भारत की एथलीट विकास रणनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें खेल विज्ञान, चिकित्सा और प्रौद्योगिकी के एकीकरण पर ज़ोर दिया गया है। वैश्विक खेल मंच पर निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन हासिल करने के लिए यह दृष्टिकोण आवश्यक है।
चाबी छीनना
- नीति में केवल सफलता की अपेक्षा करने के बजाय व्यापक प्रणालियों के माध्यम से एथलीट के प्रदर्शन को समर्थन देने के महत्व पर प्रकाश डाला गया है।
- यह खेल विकास के आधारभूत तत्वों के रूप में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और चिकित्सा सहित विभिन्न विषयों को एकीकृत करता है।
अतिरिक्त विवरण
- खेल विज्ञान और चिकित्सा एकीकरण:
- एथलीटों की दीर्घायु बढ़ाने के लिए चोट की निगरानी और शीघ्र हस्तक्षेप पर ध्यान केंद्रित करना ।
- प्रशिक्षण और तकनीकों को परिष्कृत करने के लिए बायोमैकेनिक्स और प्रदर्शन विश्लेषण का उपयोग ।
- पोडियम फिनिश को प्रभावित करने वाले सीमांत लाभों को सुरक्षित करने के लिए पोषण और पुनर्प्राप्ति विज्ञान पर जोर दिया जा सकता है ।
- प्रतियोगिताओं के दौरान मनोवैज्ञानिक दबाव को कम करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक कंडीशनिंग को शामिल करना ।
- बुनियादी ढांचा और संस्थागत विकास:
- राष्ट्रीय खेल विज्ञान एवं अनुसंधान केन्द्र के सहयोग से भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) के क्षेत्रीय केन्द्रों और राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्रों का उन्नयन।
- उदाहरणों में शामिल हैं बेंगलुरु सेंटर, जो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टॉप्स) के तहत एक उन्नत खेल विज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करता है , और दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम, जिसमें एक नया रिटर्न टू स्पोर्ट्स डिवीजन है।
- चिकित्सा टीम सहायता:
- पहली बार, पेरिस ओलंपिक खेलों के दौरान एथलीटों की सहायता के लिए एक समर्पित 10 सदस्यीय भारतीय चिकित्सा टीम का गठन किया गया है।
- प्रौद्योगिकी - नए खेल पारिस्थितिकी तंत्र की रीढ़:
- एथलीट के प्रदर्शन और रिकवरी पर नज़र रखने के लिए एआई-संचालित प्लेटफार्मों और वास्तविक समय डैशबोर्ड का कार्यान्वयन ।
- चोट के जोखिम का आकलन करने और समय पर हस्तक्षेप की सुविधा के लिए पूर्वानुमान उपकरण ।
- डिजिटल उपकरणों के माध्यम से खेल प्रशासन में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाना।
- नवाचार और अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र:
- खेल नवाचार कार्यबल की स्थापना तथा भारत-विशिष्ट प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए अनुसंधान अनुदान का प्रावधान।
- अंतःविषयक अनुसंधान के माध्यम से एथलीट विकास के लिए आत्मनिर्भर पाइपलाइन बनाने पर ध्यान केंद्रित करना।
राष्ट्रीय खेल नीति 2025 भारत के खेल दर्शन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतीक है, जो जुनून पर केंद्रित होने के बजाय व्यवस्थित योजना और निवारक देखभाल के माध्यम से सटीक प्रदर्शन पर केंद्रित है। यह नीतिगत नवाचार, साक्ष्य-आधारित शासन और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के साथ खेलों के एकीकरण में एक महत्वपूर्ण केस स्टडी के रूप में कार्य करती है।
|
3 videos|3445 docs|1079 tests
|
FAQs on Indian Polity (भारतीय राजव्यवस्था) Part 1: July 2025 UPSC Current Affairs - Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly
| 1. POCSO अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? |  |
| 2. आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का कार्य क्या है? |  |
| 3. किशोर यौन संबंधों को अपराध घोषित करने से POCSO अधिनियम का उद्देश्य कैसे प्रभावित होगा? |  |
| 4. भारत की अदालतों में लंबित मामलों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? |  |
| 5. मानसिक स्वास्थ्य दिशानिर्देशों का महत्व क्या है? |  |





















