Indian Polity and Governance (भारतीय राजनीति और शासन): August 2025 UPSC Current Affairs | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly PDF Download
जीएस2/राजनीति
संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025

चर्चा में क्यों?
केंद्रीय गृह मंत्री लोकसभा में तीन महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने की तैयारी कर रहे हैं, जिनका उद्देश्य प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के उन मंत्रियों को पद से हटाने के लिए कानूनी ढांचा स्थापित करना है, जिन्हें गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार किया गया है या हिरासत में लिया गया है।
चाबी छीनना
- तीन विधेयकों में 130वां संविधान संशोधन विधेयक, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक शामिल हैं।
- 130वें संविधान संशोधन विधेयक में विशेष रूप से उन शर्तों का उल्लेख किया गया है जिनके तहत नेताओं को हिरासत में लिए जाने पर इस्तीफा देना होगा।
अतिरिक्त विवरण
- कार्यक्षेत्र: यह विधेयक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों तथा संघ, राज्य और संघ शासित प्रदेश स्तर के मंत्रियों पर लागू होता है।
- निष्कासन का आधार: यदि किसी नेता को पांच वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले आरोपों में गिरफ्तार किया जाता है और लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखा जाता है, तो उसे इस्तीफा देना होगा।
- पुनर्नियुक्ति: नेताओं को हिरासत से रिहा होने के बाद पुनर्नियुक्त किया जा सकता है।
- उद्देश्य: गिरफ्तार नेताओं को लंबे समय तक पद पर बने रहने से रोकना, जिसका उदाहरण दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मामला है।
- अनुच्छेदों में संशोधन:
- अनुच्छेद 75: गंभीर अपराधों के लिए हिरासत में लिए जाने पर केंद्रीय मंत्रियों के स्वतः इस्तीफे का प्रावधान करता है।
- अनुच्छेद 164: मुख्यमंत्रियों और राज्य मंत्रियों के लिए हिरासत में लिए जाने पर स्वतः हटाए जाने के संबंध में समान प्रावधान।
- अनुच्छेद 239एए: नई धारा 5ए में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को गंभीर आरोपों के तहत 30 दिनों तक हिरासत में रखा जाता है तो वे पद छोड़ देंगे।
- इस विधेयक के पीछे तर्क यह सुनिश्चित करना है कि पदाधिकारी जनता का विश्वास बनाए रखें तथा हिरासत की अवधि के दौरान शासन से समझौता न करें।
यह विधेयक मंत्रिस्तरीय पदों को संवैधानिक नैतिकता और जवाबदेही के साथ जोड़कर लोकतंत्र की अखंडता को बढ़ावा देता है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- 1. भारत के संविधान के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो मतदान करने के लिए पात्र है, किसी राज्य में छह महीने तक मंत्री के रूप में कार्य कर सकता है, भले ही वह राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो।
- 2. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार, किसी आपराधिक अपराध में दोषी ठहराए गए और पांच साल के कारावास की सजा पाए व्यक्ति को रिहाई के बाद भी चुनाव लड़ने से स्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है।
विकल्प: (a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2
उत्तर: विकल्प डी
जीएस2/राजनीति
चुनाव अधिकारियों पर नियंत्रण: चुनाव आयोग बनाम राज्य

चर्चा में क्यों?
भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच चुनाव अधिकारियों पर अनुशासनात्मक अधिकार को लेकर विवाद चल रहा है। राज्य सरकार ने मतदाता सूची में छेड़छाड़ के आरोपी चार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया है कि अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है और आदर्श आचार संहिता लागू नहीं है। इस असहमति ने चुनाव ड्यूटी पर तैनात राज्य अधिकारियों पर चुनाव आयोग के नियंत्रण की सीमा को लेकर चल रही बहस को फिर से हवा दे दी है।
चाबी छीनना
- चुनाव अधिकारियों पर भारत निर्वाचन आयोग का अधिकार संवैधानिक रूप से समर्थित है तथा संशोधनों और कानूनी ढाँचों के माध्यम से विकसित हुआ है।
- भारत निर्वाचन आयोग और पश्चिम बंगाल के बीच चल रहा गतिरोध अनुशासनात्मक उपायों के प्रवर्तन पर लगातार तनाव को उजागर करता है।
- ऐतिहासिक संघर्ष, विशेष रूप से टी.एन. शेषन के कार्यकाल के दौरान, निर्वाचन आयोग के समक्ष अपने अधिकार का प्रयोग करने में आने वाली चुनौतियों को रेखांकित करते हैं।
अतिरिक्त विवरण
- ईसीआई के लिए संवैधानिक दृष्टिकोण: संविधान सभा की बहस के दौरान, इस बात पर जोर दिया गया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान सुरक्षा मिलनी चाहिए, जिससे कार्यपालिका शाखा से उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सके।
- 1988 संशोधन: 1950 और 1951 के जनप्रतिनिधित्व अधिनियमों में इन संशोधनों ने औपचारिक रूप से चुनाव अधिकारियों को ईसीआई की निगरानी में रखा, जिससे चुनावों के दौरान उन पर स्पष्ट अधिकार प्राप्त हो गए।
- ऐतिहासिक संदर्भ: 1993 के रानीपेट उपचुनाव के दौरान संघर्ष चरम पर था, जहां टीएन शेषन की केंद्रीय बलों की मांग के कारण मुद्दे के समाधान तक कई चुनावों को अस्थायी रूप से रोकना पड़ा।
- सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप: न्यायिक प्रणाली ने ईसीआई के अधिकार की पुष्टि करने के लिए हस्तक्षेप किया, जिसके परिणामस्वरूप 2000 में एक समझौता हुआ, जिसने ईसीआई की अनुशासनात्मक शक्तियों को स्पष्ट कर दिया।
- भारत निर्वाचन आयोग के लिए वर्तमान विकल्प: पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिरोध को देखते हुए, भारत निर्वाचन आयोग मुख्य सचिव को तलब कर सकता है, केंद्र को शामिल कर सकता है, या अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटा सकता है।
यह वर्तमान स्थिति दर्शाती है कि यद्यपि भारत निर्वाचन आयोग के अधिकार को कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है, फिर भी व्यावहारिक चुनौतियां बनी हुई हैं, क्योंकि राज्य सरकारें कभी-कभी इसके निर्देशों का विरोध करती हैं, जो भारत में चुनावी शासन की जटिलताओं को दर्शाता है।
जीएस2/राजनीति
मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) का कार्यालय
 चर्चा में क्यों?
चर्चा में क्यों?
इंडी गठबंधन गुट द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाने वाला विपक्ष, संसद में मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) को हटाने के लिए एक प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, जिसमें चुनाव प्रबंधन और ईमानदारी पर चिंता जताई गई है।
चाबी छीनना
- भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) एक स्थायी संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, जिसे प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मान्यता दी जाती है।
- भारत निर्वाचन आयोग संविधान के भाग XV के अनुच्छेद 324 से 329 द्वारा शासित है, तथा लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं सहित विभिन्न स्तरों पर चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है।
अतिरिक्त विवरण
- स्थापना: चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और यह भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- संरचना: 1993 से, ईसीआई तीन सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य करता है जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और दो चुनाव आयुक्त शामिल होते हैं।
- मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा: मुख्य चुनाव आयुक्त को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान वेतन, दर्जा और भत्ते प्राप्त होते हैं, जिससे स्वतंत्रता और अधिकार सुनिश्चित होता है।
- नियुक्ति प्रक्रिया: मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है।
- कार्यकाल: मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, होता है।
- निष्कासन प्रक्रिया: मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए प्रक्रिया के समान है, जिसके लिए संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है।
भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग की ईमानदारी और कार्यप्रणाली सर्वोपरि है। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का कोई भी प्रस्ताव देश में निष्पक्ष चुनाव प्रक्रियाओं की महत्वपूर्ण प्रकृति को रेखांकित करता है।
जीएस2/शासन
भारत के चुनावी परिदृश्य में बदलाव

चर्चा में क्यों?
भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने चुनावी प्रक्रिया में सुधार के लिए विभिन्न सुधार लागू किए हैं, जिनमें पारदर्शिता, मतदाता भागीदारी और लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
चुनाव आयोग द्वारा प्रमुख सुधार
1. मतदाता सूची प्रबंधन
- राजनीतिक दल सूची को सटीक रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग 476 निष्क्रिय पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (आरयूपीपी) को सूची से हटाने की योजना बना रहा है।
- चार राज्यों में उपचुनावों के लिए मतदाता सूचियों में संशोधन किया गया, जो 20 वर्षों में पहला विशेष संक्षिप्त संशोधन था।
- बिहार में मतदाता सूची की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण किया गया।
- देश भर में डुप्लीकेट ईपीआईसी (मतदाता) कार्ड समाप्त कर दिए गए, जिससे मतदाताओं को विशिष्ट पहचान संख्या उपलब्ध हो गई।
2. प्रौद्योगिकी-संचालित पारदर्शिता और निगरानी
- ईसीआई ने ईसीआईएनईटी नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लांच किया है, जो निर्वाचकों, मतदाताओं और राजनीतिक दलों के लिए 40 से अधिक अनुप्रयोगों को एकीकृत करता है।
- निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर चुनाव संबंधी आंकड़ों तक बेहतर पहुंच के लिए डिजिटल इंडेक्स कार्ड और रिपोर्ट शुरू की गईं।
- मतदान प्रक्रिया की निगरानी के लिए मतदान केंद्रों की 100% वेबकास्टिंग लागू की गई।
3. बूथ-स्तरीय सुधार
- पारदर्शिता और जनता का विश्वास बढ़ाने के लिए बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) को मानक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए।
- भीड़ कम करने और कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं की संख्या 1,200 तक सीमित कर दी गई।
4. मतदाता सत्यापन और सटीकता
- मतगणना की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए बेमेल स्थिति में वी.वी.पी.ए.टी. पर्चियों की गिनती अनिवार्य कर दी गई।
भारत की चुनावी प्रक्रिया के सामने चुनौतियाँ
1. बढ़ता चुनाव खर्च
- वास्तविक चुनाव व्यय और कानूनी सीमा के बीच का अंतर बढ़ता जा रहा है।
- उम्मीदवार और पार्टियां अक्सर खर्च की सीमा से अधिक खर्च करते हैं, जिसके कारण कम जानकारी दी जाती है और छाया वित्तपोषण होता है, जो भ्रष्टाचार और काले धन को बढ़ावा देता है।
2. राजनीति का अपराधीकरण
- आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार राजनेता-अपराधी गठजोड़ के समर्थन से चुनाव जीत रहे हैं।
- आगामी 2024 के लोकसभा चुनावों में , नवनिर्वाचित सांसदों का एक महत्वपूर्ण प्रतिशत आपराधिक मामलों का सामना कर रहा है।
3. मतदाता मताधिकार से वंचित और मतदान प्रतिशत के मुद्दे
- फर्जी मतदान, मतदाता सूची में नाम गायब होना तथा शहरी क्षेत्रों में कम मतदान जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं।
- आंतरिक प्रवासियों, बुजुर्गों और दिव्यांग नागरिकों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे समावेशिता प्रभावित होती है।
4. मुफ्त की राजनीति और लोकलुभावन वादे
- चुनावों के दौरान असंतुलित मुफ्त उपहार देने की संस्कृति वित्तीय जिम्मेदारी और शासन को कमजोर करती है।
- मतदाता दीर्घकालिक विकास योजनाओं की बजाय अल्पकालिक लाभों से प्रभावित होते हैं।
- स्पष्ट दिशा-निर्देशों के अभाव में कल्याणकारी योजनाओं और राजकोषीय लोकलुभावनवाद के बीच अंतर करना कठिन हो जाता है।
5. चुनावी हिंसा और बूथ स्तर की कमजोरियाँ
- यद्यपि हिंसा, मतदाताओं को डराने-धमकाने तथा बूथ स्तर पर मतदान पैटर्न का खुलासा करने की घटनाएं कम हुई हैं, फिर भी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं।
- संवेदनशील क्षेत्रों में कमजोर बूथ प्रबंधन से चुनाव की शुचिता प्रभावित होती है।
- टोटलाइजर मशीनों की कमी के कारण समुदायों को चुनाव के बाद संभावित प्रतिशोध का सामना करना पड़ सकता है।
6. तकनीकी और साइबर खतरे
- डीपफेक, गलत सूचना और सोशल मीडिया में हेरफेर का बढ़ना चुनावी अखंडता के लिए नए खतरे पैदा कर रहा है।
7. मतदाता सूची में हेरफेर
- मतदाता सूची में हेराफेरी और डुप्लिकेट ईपीआईसी नंबर के आरोप मतदाता सूचियों की विश्वसनीयता और जनता के विश्वास को कमजोर करते हैं।
8. आंतरिक-पार्टी लोकतंत्र का अभाव
- राजनीतिक दल केंद्रीकृत और अपारदर्शी तरीके से काम करते हैं, जिन पर वंशवाद का प्रभुत्व होता है।
- पारदर्शी उम्मीदवार चयन और जवाबदेही का अभाव लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विपरीत है और वास्तविक नेतृत्व के उदय में बाधा डालता है।
भारत के चुनावी ढांचे को और मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाने की आवश्यकता है?
- चुनावी वित्त सुधार:द्वितीय एआरसी के सुझाव के अनुसार आंशिक राज्य वित्तपोषण लागू किया जाए, जिसमें वैध व्ययों की प्रतिपूर्ति शामिल हो तथा एक निश्चित राशि से अधिक के दान का डिजिटल प्रकटीकरण आवश्यक हो।
- गुमनाम कॉर्पोरेट दान को विनियमित करें।
- सीएजी और ईसीआई द्वारा लेखापरीक्षा को बढ़ावा देना।
- वित्तीय प्रभाव को सीमित करने और मतदाताओं के बीच विश्वास पैदा करने के लिए चुनाव खर्च के लिए एक सार्वजनिक पोर्टल बनाएं।
- राजनीतिक दलों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत शामिल करने पर विचार करें।
- आंतरिक पार्टी लोकतंत्र को बढ़ावा देना:राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कई बंद, परिवार द्वारा संचालित व्यवसायों की तरह काम करते हैं।
- कानून में नियमित आंतरिक चुनावों की आवश्यकता होनी चाहिए।
- उम्मीदवारों के चयन के लिए पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करें।
- ऑडिटेड पार्टी संविधान की आवश्यकता है।
- 1999 की विधि आयोग की रिपोर्ट में आंतरिक पार्टी लोकतंत्र को विनियमित करने के लिए एक प्रणाली का सुझाव दिया गया था।
- डिजिटल अभियान और डीपफेक को विनियमित करना:सभी राजनीतिक विज्ञापनों पर स्पष्ट प्रकटीकरण लेबल की आवश्यकता होगी, जिसमें प्रायोजक, वित्तपोषण और लक्षित दर्शकों के बारे में विवरण शामिल हो।
- वास्तविक समय में सोशल मीडिया पर निगरानी रखने के लिए आईआईटी और सीईआरटी-इन के सहयोग से एक राष्ट्रीय डीपफेक डिटेक्शन सेल की स्थापना की जाएगी।
- भ्रामक सामग्री को हटाने के लिए सख्त नियम लागू करें, तथा ऐसा न करने वाले प्लेटफॉर्म पर जुर्माना लगाएं।
- मतदाताओं को एल्गोरिथम संबंधी पूर्वाग्रह, डीपफेक और गलत सूचना के बारे में शिक्षित करने के लिए पहल शुरू करें।
- ईसीआई को मजबूत करना:भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को वित्तीय स्वतंत्रता होनी चाहिए, तथा इसका वित्त पोषण भारत की संचित निधि से होना चाहिए।
- भारत के विविध निर्वाचन क्षेत्रों में बेहतर निगरानी के लिए स्थायी कर्मचारियों के साथ क्षेत्रीय ईसीआई कार्यालय स्थापित करना।
- विश्वसनीयता में सुधार के लिए संसदीय समितियों द्वारा चुनावी प्रक्रियाओं का नियमित मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
- निष्पक्षता सुनिश्चित करने और सरकारी निकायों पर निर्भरता कम करने तथा हितों के टकराव को समाप्त करने के लिए ईसीआई के भीतर अधिकारियों का एक स्थायी, स्वतंत्र समूह बनाएं।
- निर्वाचन प्रक्रिया सुधार:मतदान केंद्रों पर मतों को मिश्रित करने के लिए देश भर में टोटलाइजर मशीनों के उपयोग का विस्तार करना, जिससे विशिष्ट बूथों पर मतदान पैटर्न की पहचान को रोका जा सके।
- सुसंगत मतदाता सूची और आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।
- निष्पक्षता सुनिश्चित करने और मतदाताओं का विश्वास बढ़ाने के लिए अभियान की अवधि सीमित करें।
- एक साथ एवं सतत चुनाव की दिशा में:स्थानीय और राज्य स्तर पर एक राष्ट्र, एक चुनाव की अवधारणा का परीक्षण करें।
- दोहराव को कम करने के लिए एक स्थायी राष्ट्रीय मतदाता सूची और एक समान मतदाता पहचान पत्र लागू करें।
- एक साथ चुनाव से होने वाली बचत का उपयोग शासन में सुधार के लिए करें।
- धीरे-धीरे चुनावों के लिए एक निश्चित कार्यक्रम लागू किया जाना चाहिए ताकि उन्हें अधिक लागत प्रभावी और कुशल बनाया जा सके।
निष्कर्ष
एक सुदृढ़ लोकतंत्र अपनी चुनावी नींव की मज़बूती पर टिका होता है। संस्थाओं की स्वतंत्रता को मज़बूत करना, पारदर्शिता बढ़ाना, मतदाता भागीदारी को व्यापक बनाना, आंतरिक-दलीय लोकतंत्र को मज़बूत करना और तकनीक को अपनाना अनिवार्य है। ऐसे समग्र और निरंतर प्रयासों से ही भारत अपनी चुनावी प्रणाली की अखंडता, विश्वसनीयता और निष्पक्षता की रक्षा कर सकता है और एक जीवंत लोकतंत्र की भावना को सही मायने में कायम रख सकता है।
जीएस2/राजनीति
मतदाता सूची संशोधन में सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप - पिछले निर्णयों के साथ निरंतरता

चर्चा में क्यों?
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) बनाम भारतीय चुनाव आयोग (2025) मामले में सुप्रीम कोर्ट (एससी) का हालिया फैसला बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से संबंधित है, जो लाल बाबू हुसैन बनाम निर्वाचक पंजीयन अधिकारी (1995) मामले में दिए गए उसके पहले के ऐतिहासिक फैसले को दर्शाता है । यह मामला नागरिकता सत्यापन, मतदाता बहिष्करण और मताधिकार के संवैधानिक अधिकार से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डालता है।
चाबी छीनना
- सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि मतदाताओं को उनके विरुद्ध विश्वसनीय साक्ष्य के बिना नागरिकता साबित करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।
- सर्वोच्च न्यायालय ने भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने का निर्देश दिया।
- इस फैसले से सबूत का भार पुनः राज्य पर आ गया है, जिससे नागरिकों के अधिकार मजबूत हुए हैं।
अतिरिक्त विवरण
- ऐतिहासिक समानांतर - लाल बाबू हुसैन मामला (1995): इस मामले में, चुनाव आयोग ने कुछ मतदाताओं को गैर-नागरिक घोषित करने का प्रयास किया। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों को गहन जाँच करनी चाहिए और मतदाताओं द्वारा प्रस्तुत सभी साक्ष्यों पर विचार करना चाहिए।
- वर्तमान मुद्दा - विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर), बिहार: एसआईआर में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए), 1950 और निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के तहत स्पष्ट वैधानिक समर्थन का अभाव है। ईसीआई का उद्देश्य गैर-नागरिकों को हटाना था, लेकिन उसने केवल 2003 की मतदाता सूची और पहचान दस्तावेजों के एक संकीर्ण सेट पर भरोसा किया, जिससे प्रमाण का भार नागरिकों पर आ गया।
- सर्वोच्च न्यायालय का 2025 का आदेश: सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि भारत निर्वाचन आयोग मसौदा मतदाता सूची को सुलभ और खोज योग्य बनाए, मतदाता बहिष्करण के कारण बताए, तथा आधार और चुनावी फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) सहित पहचान दस्तावेजों की एक विस्तृत श्रृंखला को स्वीकार करे।
- लोकतांत्रिक सिद्धांत दांव पर: सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का उद्देश्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांतों को कायम रखना है, तथा एसआईआर द्वारा प्रस्तुत बहिष्कार प्रथाओं के जोखिमों के विपरीत है।
निष्कर्षतः, मतदाता सूची संशोधन में पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सर्वोच्च न्यायालय के ज़ोर से भारत में नागरिक-केंद्रित लोकतंत्र को मज़बूती मिलने की उम्मीद है। जैसे-जैसे राष्ट्र विकसित भारत@2047 की ओर बढ़ रहा है , मतदाता पंजीकरण में सुधार आवश्यक रूप से विकसित होने चाहिए ताकि एक मज़बूत, समावेशी और क़ानूनी रूप से जवाबदेह प्रणाली बनाई जा सके जो सार्वभौमिक मताधिकार को बनाए रखे।
जीएस2/राजनीति
न्यायालय मतों की पुनर्गणना का आदेश कब दे सकता है?

चर्चा में क्यों?
सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में अपने इतिहास में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के मतों की पुनः गणना की, जिसके परिणामस्वरूप हरियाणा में सरपंच के चुनाव परिणाम को पलट दिया गया।
चाबी छीनना
- मतों की पुनर्गणना में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका।
- चुनाव परिणामों को चुनौती देने के लिए कानूनी ढांचा।
- चुनाव याचिका दायर करने के लिए पात्रता और आवश्यकताएं।
- भ्रष्ट आचरण को साबित करने के लिए न्यायिक मानक।
अतिरिक्त विवरण
- चुनाव परिणामों को चुनौती देने के लिए कानूनी ढांचा:
- संसदीय, विधानसभा और राज्य परिषद चुनावों के लिए संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है।
- स्थानीय सरकार के चुनावों के लिए जिला स्तरीय सिविल अदालतों में याचिका दायर करना आवश्यक है।
- केवल चुनाव में शामिल उम्मीदवार या मतदाता ही याचिका दायर कर सकते हैं, जिसे चुनाव परिणाम घोषित होने के 45 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- याचिका की आवश्यकताएं: याचिकाओं में महत्वपूर्ण तथ्यों और भ्रष्ट आचरण के विशिष्ट आरोपों का संक्षिप्त विवरण शामिल होना चाहिए, जिसमें नाम, दिनांक और स्थान का विवरण दिया जाना चाहिए।
- न्यायिक दृष्टिकोण: सर्वोच्च न्यायालय भ्रष्ट आचरण के आरोपों को अर्ध-आपराधिक मानता है, जिसके लिए उच्च स्तर के प्रमाण की आवश्यकता होती है। अस्पष्ट याचिकाएँ आमतौर पर खारिज कर दी जाती हैं।
- चुनाव को अमान्य करने के आधार: न्यायालय रिश्वतखोरी, उम्मीदवारों की अयोग्यता, नामांकन पत्रों की अनुचित स्वीकृति/अस्वीकृति, तथा परिणामों को प्रभावित करने वाले संवैधानिक या चुनाव कानूनों का अनुपालन न करने के आधार पर चुनाव को रद्द कर सकते हैं।
- पुनर्गणना: न्यायालय पुनर्गणना का आदेश तभी दे सकते हैं जब याचिकाकर्ता विशिष्ट तथ्य और संभावित मतगणना त्रुटियों के साक्ष्य प्रस्तुत करे। पुनर्गणना आमतौर पर चुनाव स्थल पर ही की जाती है, पानीपत मामले जैसे अपवादों को छोड़कर, जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने अपने परिसर में पुनर्गणना की थी।
- नए विजेता की घोषणा: हालाँकि यह दुर्लभ है, अदालतें नए विजेता की घोषणा कर सकती हैं यदि साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि याचिकाकर्ता या किसी अन्य उम्मीदवार के पास वैध मतों का बहुमत था या यदि भ्रष्ट आचरण न होता तो वह जीत जाता। इसके लिए दूषित मतों के ठोस प्रमाण की आवश्यकता होती है, जैसा कि फरवरी 2024 के चंडीगढ़ महापौर चुनाव में सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से स्पष्ट होता है।
संक्षेप में, न्यायिक प्रणाली चुनाव परिणामों को चुनौती देने और मतों की पुनर्गणना के लिए एक संरचित प्रक्रिया प्रदान करती है, जो चुनावी प्रक्रिया की अखंडता और विवादों में पारदर्शी साक्ष्य की आवश्यकता पर बल देती है।
जीएस2/राजनीति
रोस्टर का मास्टर - सुप्रीम कोर्ट बनाम हाईकोर्ट, न्यायिक प्राधिकार, और हस्तक्षेप की सीमाएं
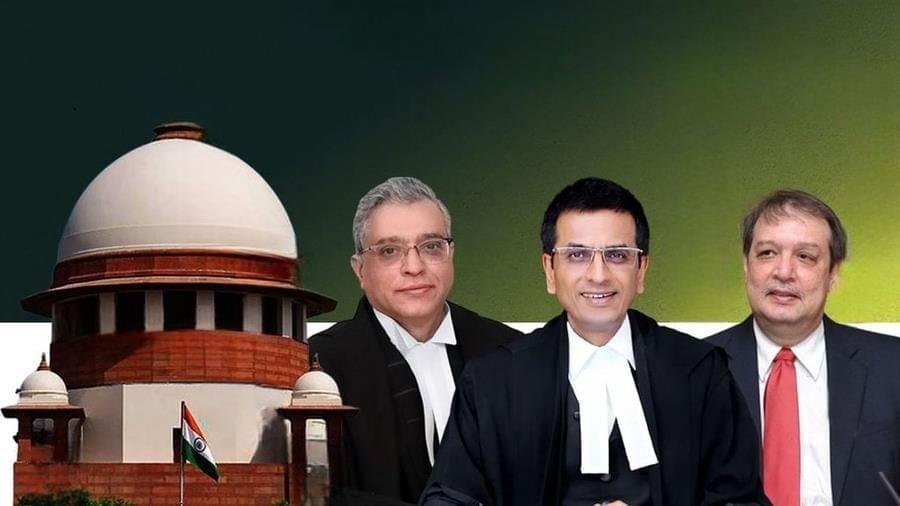
चर्चा में क्यों?
हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय (एचसी) के एक न्यायाधीश को एक "बेतुके" फैसले के लिए सर्वोच्च न्यायालय (एससी) द्वारा लगाई गई फटकार ने उच्च न्यायालयों के आंतरिक कार्यों में, विशेष रूप से राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास मौजूद विशिष्ट 'मास्टर ऑफ रोस्टर' शक्तियों के संबंध में, सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के अधिकार की सीमा पर नए सिरे से चर्चा छेड़ दी है। यह स्थिति न्यायिक स्वतंत्रता, संस्थागत अखंडता और अनुच्छेद 141 और 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न उठाती है।
चाबी छीनना
- सर्वोच्च न्यायालय ने एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आलोचना की, जिसके परिणामस्वरूप न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाओं पर चर्चा शुरू हो गई।
- न्यायिक निगरानी और उच्च न्यायालयों की स्वायत्तता के बीच संतुलन को लेकर चिंताएं व्यक्त की गई हैं।
अतिरिक्त विवरण
- पृष्ठभूमि घटना: न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की एक सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने निर्देश दिया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार को एक वरिष्ठ न्यायाधीश के साथ काम करने के लिए नियुक्त किया जाए और एक "गलत" आदेश के कारण सेवानिवृत्ति तक आपराधिक रोस्टर से हटा दिया जाए।
- चिंताएं व्यक्त की गईं: उच्च न्यायालय और मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली के कानूनी पेशेवरों ने मुख्य न्यायाधीश के प्रशासनिक कर्तव्यों में सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप पर चिंता व्यक्त की।
- आदेश में संशोधन: भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवई के पत्र के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने बाद में अपने आदेश में संशोधन किया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि उसका 'मास्टर ऑफ रोस्टर' प्राधिकरण को चुनौती देने का कोई इरादा नहीं है।
प्रमुख संवैधानिक और न्यायिक सिद्धांत
- रोस्टर के मास्टर सिद्धांत:यह सिद्धांत मुख्य न्यायाधीश (उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय) को पीठों के गठन और मामलों के आवंटन का विशेष अधिकार देता है। कुछ प्रमुख फैसले इसकी पुष्टि करते हैं, जैसे:
- राजस्थान राज्य बनाम प्रकाश चंद (1998): इस बात पर जोर दिया गया कि केवल मुख्य न्यायाधीश ही यह निर्णय ले सकते हैं कि कौन सा न्यायाधीश किस मामले की सुनवाई करेगा।
- राजस्थान राज्य बनाम देवी दयाल (1959): यह स्थापित किया गया कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एकल या खंडपीठ की संरचना निर्धारित करते हैं।
- मायावरम वित्तीय निगम (मद्रास उच्च न्यायालय, 1991): इस बात की पुष्टि की गई कि मुख्य न्यायाधीश के पास न्यायिक कार्य आवंटन के लिए अंतर्निहित शक्तियां हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय की पदानुक्रमिक भूमिका: अनुच्छेद 141 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय का घोषित कानून सभी भारतीय न्यायालयों पर बाध्यकारी है, और अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को मानक प्रक्रियाओं से परे "पूर्ण न्याय" के लिए आवश्यक कोई भी आदेश जारी करने की अनुमति देता है।
- न्यायिक स्वतंत्रता बनाम संस्थागत निगरानी: यद्यपि उच्च न्यायालय स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाओं के रूप में कार्य करते हैं, न्यायपालिका की एकीकृत संरचना कानून के शासन को खतरा पैदा करने वाले असाधारण मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप की अनुमति देती है।
मुद्दों को उठाया
- सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों का दायरा: क्या सर्वोच्च न्यायालय रोस्टर आवंटन के संबंध में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रशासनिक निर्देश जारी कर सकता है?
- न्यायिक अनुशासन: उच्च न्यायालय की स्वायत्तता से समझौता किए बिना निर्णयों की गुणवत्ता कैसे बनाए रखी जाए?
- अनुच्छेद 142 उपयोग: क्या बार-बार होने वाली न्यायिक गलतियों को रोकने के लिए निवारक कार्रवाई का कोई औचित्य है?
- न्यायपालिका के भीतर शक्तियों का पृथक्करण: न्यायिक स्वतंत्रता के साथ पदानुक्रम को संतुलित करना एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बना हुआ है।
आंतरिक तंत्र बनाम सार्वजनिक फटकार
- औपचारिक प्रक्रिया: गंभीर दुर्व्यवहार या अक्षमता के मामले में महाभियोग (संसद के माध्यम से) चलाया जा सकता है, जबकि छोटे मामलों को आंतरिक जांच के माध्यम से निपटाया जाता है।
- सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण: सर्वोच्च न्यायालय ने गोपनीय प्रशासनिक प्रक्रिया का पालन करने के बजाय एक सार्वजनिक निर्देश जारी किया, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल उठते हैं।
- निर्देश की प्रकृति: सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई सुधारात्मक थी, दंडात्मक नहीं, इसका उद्देश्य न्यायाधीश को एक वरिष्ठ सहकर्मी के साथ जोड़कर तथा उसे आपराधिक सूची से हटाकर मार्गदर्शन करना था।
आगे बढ़ने का रास्ता
- इस बारे में स्पष्ट दिशानिर्देश स्थापित करें कि सर्वोच्च न्यायालय कब उच्च न्यायालय के प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है।
- सार्वजनिक विवादों के बिना न्यायिक आचरण को संभालने के लिए आंतरिक तंत्र को मजबूत करना।
- संवेदनशील न्यायिक मामलों में बार-बार होने वाली गलतियों को रोकने के लिए न्यायाधीशों के लिए मार्गदर्शन और प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू करें।
निष्कर्षतः, यद्यपि 'मास्टर ऑफ रोस्टर' सिद्धांत न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, फिर भी यह न्यायिक त्रुटियों से विधि-शासन के लिए खतरा उत्पन्न होने पर सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप को पूरी तरह से नहीं रोकता है। अनुच्छेद 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ असाधारण सुधारात्मक उपायों की अनुमति देती हैं, लेकिन ऐसे हस्तक्षेपों को उच्च न्यायालयों की स्वायत्तता का सम्मान करते हुए सावधानीपूर्वक संतुलित किया जाना चाहिए।
जीएस2/राजनीति
अनुच्छेद 370 - निरस्तीकरण के छह साल बाद जम्मू और कश्मीर

चर्चा में क्यों?
5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) में बदलने का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, विकास और शांति को बढ़ावा देना था। छह साल बाद, एक आलोचनात्मक समीक्षा राजनीति, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और पर्यटन के साथ-साथ मौजूदा संरचनात्मक और प्रशासनिक चुनौतियों में मिले-जुले परिणाम दिखाती है।
चाबी छीनना
- राजनीतिक घटनाक्रम लोकतांत्रिक पुनरुत्थान और सीमित प्राधिकार का मिश्रण दर्शाता है।
- पहलगाम हमले जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं के कारण सुरक्षा सुधार पर ग्रहण लग गया।
- निवेश और राजस्व में वृद्धि के माध्यम से आर्थिक विकास देखा जा रहा है, लेकिन चुनौतियां बनी हुई हैं।
- सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बावजूद पर्यटन का विकास हुआ, जिससे क्षेत्र की नाजुकता उजागर हुई।
अतिरिक्त विवरण
- राजनीतिक घटनाक्रम: नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) एक नई निर्वाचित सरकार का नेतृत्व कर रही है, जो लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की वापसी का संकेत है। हालाँकि, प्रमुख शक्तियाँ उपराज्यपाल के पास बनी हुई हैं, जिससे मुख्यमंत्री के अधिकार सीमित हो गए हैं। सरकार ने पूर्ण राज्य का दर्जा देने और विशेष दर्जे की फिर से पुष्टि करने पर ज़ोर दिया है, जिससे केंद्र के साथ तनाव बढ़ गया है।
- सुरक्षा सुधार: आतंकवाद में उल्लेखनीय गिरावट आई है, 2025 में केवल 28 आतंकवादी मारे जाएंगे जबकि 2024 में 67 आतंकवादी मारे जाएंगे। हालांकि, पहलगाम हमले, जिसमें 26 नागरिक मारे गए, ने पर्यटन क्षेत्रों में सुरक्षा खामियों को उजागर किया है।
- आर्थिक विकास: इस क्षेत्र ने पर्याप्त औद्योगिक निवेश आकर्षित किया है, कुल 1.63 लाख करोड़ रुपये के प्रस्ताव। कर राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 2015-16 के 1.17 लाख करोड़ रुपये से दोगुना होकर 2024-25 में 2.63 लाख करोड़ रुपये हो गया है। हालाँकि, कृषि और उद्योग जैसे प्रमुख क्षेत्रों का प्रदर्शन कमजोर रहा है।
- पर्यटन विकास: 2023 में 2.11 करोड़ पर्यटकों का रिकॉर्ड, पर्यटन क्षेत्र के तेजी से बढ़ते आकार को दर्शाता है, जो सकल घरेलू उत्पाद में 7% का योगदान देगा। फिर भी, सुरक्षा कारणों से कई पर्यटन स्थलों को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा।
निष्कर्षतः, अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के छह साल बाद, जम्मू और कश्मीर एक जटिल परिदृश्य प्रस्तुत करता है, जहाँ सुरक्षा और निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है; हालाँकि, राजनीतिक स्वायत्तता, वित्तीय स्थिरता और निजी क्षेत्र के विश्वास में चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं। हाल ही में पहलगाम में हुए हमले ने स्थायी एकीकरण और समृद्धि प्राप्त करने के लिए सुरक्षा और विकास के बीच संतुलन की आवश्यकता को रेखांकित किया है।
जीएस2/राजनीति और शासन
जम्मू और कश्मीर और उपराज्यपाल विधानसभा सदस्य नामांकन पर
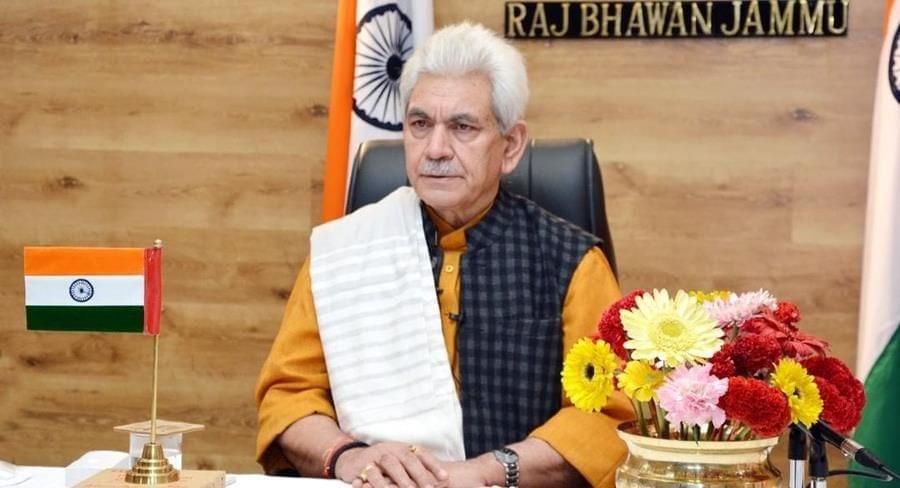
यह समाचार क्यों है?
- केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने जम्मू और कश्मीर (जे एंड के) उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उपराज्यपाल (एलजी) को निर्वाचित सरकार की सहायता और सलाह के बिना पांच विधानसभा सदस्यों को नामित करने का अधिकार है।
- इस बयान ने राजनीतिक रूप से संवेदनशील केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में लोकतांत्रिक जवाबदेही के बारे में संवैधानिक चर्चा शुरू कर दी है।
- उपराज्यपाल द्वारा नामांकन से 119 सदस्यीय विधानसभा में शक्ति संतुलन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, तथा संभवतः जनता द्वारा लिए गए चुनावी निर्णयों को पलट दिया जा सकता है।
- उच्च न्यायालय वर्तमान में इस बात की समीक्षा कर रहा है कि क्या यह प्रथा संविधान के मूल सिद्धांतों को कमजोर करती है।
जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के समक्ष मुख्य मुद्दे
- संवैधानिक प्रश्न: उच्च न्यायालय इस बात की जांच कर रहा है कि क्या जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में 2023 के संशोधन, जो उपराज्यपाल को विधानसभा में पांच सदस्यों को नामित करने की अनुमति देते हैं, संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं।
- संभावित प्रभाव: न्यायालय इस बात पर विचार कर रहा है कि ये मनोनीत सदस्य किस प्रकार विधानसभा की गतिशीलता को बदल सकते हैं, अल्पमत सरकार को बहुमत में बदल सकते हैं, तथा इसके विपरीत, जिससे शासन की स्थिरता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।
- न्यायिक दायरा: यह मुद्दा केवल वैधानिक व्याख्या से आगे बढ़कर लोकतांत्रिक सिद्धांतों और शासन के सार तक जाता है।
2023 के संशोधनों के प्रावधान
- जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धाराएं 15ए और 15बी: ये धाराएं विधानसभा में सदस्यों को नामित करने के मानदंडों को रेखांकित करती हैं, जिसमें विशिष्ट समूहों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के प्रावधान भी शामिल हैं।
- कुल सीटें: संशोधनों में 119 सदस्यीय विधानसभा में पांच मनोनीत सदस्यों के लिए प्रावधान किया गया है, जिसका उद्देश्य प्रतिनिधित्व बढ़ाना और विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना है।
- मतदान का अधिकार: मनोनीत सदस्यों को पूर्ण मतदान का अधिकार होगा, जिससे वे विधानसभा की निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले सकेंगे।
नामांकन के लिए केंद्र का औचित्य
- गृह मंत्रालय ने पुडुचेरी से संबंधित के. लक्ष्मीनारायणन बनाम भारत संघ मामले का हवाला देते हुए तर्क दिया है कि इन नामांकनों को करने की शक्ति निर्वाचित सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
- केंद्र के कानूनी दृष्टिकोण में "स्वीकृत शक्ति" की अवधारणा जैसे तकनीकी पहलू शामिल हैं, जिसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल हैं, और मतदान प्रक्रियाओं के संबंध में 1963 के संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम की धारा 12 का संदर्भ दिया गया है।
- गृह मंत्रालय का दृष्टिकोण ऐसे नामांकनों के व्यापक संवैधानिक और लोकतांत्रिक निहितार्थों के बजाय कानूनी विवरणों पर ध्यान केंद्रित करता प्रतीत होता है।
लोकतांत्रिक निहितार्थों के संबंध में चिंताएँ
- जनादेश के विरूपण का जोखिम: ऐसी चिंता है कि एक कड़े मुकाबले वाली विधानसभा में, मनोनीत सदस्य सरकार की स्थिरता और दिशा निर्धारित करने में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं, जिससे मूल चुनावी जनादेश को संभावित रूप से कमजोर किया जा सकता है।
- पुडुचेरी में मिसाल: पुडुचेरी का अनुभव, जहां मनोनीत सदस्यों और दलबदलुओं ने 2021 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के पतन में योगदान दिया, जम्मू-कश्मीर में इसी तरह के परिदृश्यों के बारे में चिंता पैदा करता है।
- केंद्र शासित प्रदेश का संदर्भ: 2019 में जम्मू-कश्मीर का राज्य से केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तन, जो निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ पर्याप्त परामर्श के बिना हुआ, इस क्षेत्र में जवाबदेही और लोकतांत्रिक मानदंडों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता को बढ़ाता है।
उपराज्यपाल की शक्तियों पर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायशास्त्र
- दिल्ली सेवा मामलों (2018 और 2023 में दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ) जैसे मामलों में, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि एलजी को निर्वाचित सरकार की सलाह पर कार्य करना चाहिए, जिसमें विवेकाधिकार नियम के बजाय अपवाद होगा।
- गृह मंत्रालय का यह कहना कि नामांकन करने की शक्ति निर्वाचित सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इस स्थापित न्यायशास्त्र का खंडन करता है, तथा ऐसे दावों की सुसंगतता और औचित्य पर प्रश्न उठाता है।
निष्कर्ष
- जम्मू-कश्मीर में नामांकन का मुद्दा प्रशासनिक प्राधिकार और लोकतांत्रिक वैधता के बीच नाजुक संतुलन को रेखांकित करता है।
- जम्मू-कश्मीर जैसे क्षेत्रों में, जहां राजनीतिक संवेदनशीलता अधिक है, महत्वपूर्ण निर्णयों में निर्वाचित सरकारों को नजरअंदाज करना, जो विधानसभा के बहुमत को बदल सकता है, जनता के विश्वास और संविधान में निहित प्रतिनिधि शासन के मूलभूत सिद्धांतों के लिए खतरा पैदा करता है।
मूल्य संवर्धन
(क) मूल संरचना सिद्धांत:
- केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) जैसे मामलों के माध्यम से विकसित , जो संसद को संविधान में ऐसे संशोधन करने से रोकता है जो इसकी आवश्यक विशेषताओं को नुकसान पहुंचाते हैं।
- इस मूल संरचना के भाग के रूप में प्रतिनिधि लोकतंत्र और संघवाद को मान्यता दी गई है।
(बी) लक्ष्मीनारायणन केस (2019):
- के. लक्ष्मीनारायणन बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पुडुचेरी में निर्वाचित सरकार से परामर्श किए बिना विधायकों को नामित करने की केंद्र की शक्ति को बरकरार रखा।
- यह मिसाल जम्मू-कश्मीर विवाद के केंद्र में है, क्योंकि उपराज्यपाल द्वारा भी इसी प्रकार की शक्तियों का प्रयोग किया जा रहा है।
(ग) दिल्ली बनाम एलजी न्यायशास्त्र:
- दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ जैसे मामलों के माध्यम से, सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि उपराज्यपाल को विवेक के विशिष्ट मामलों को छोड़कर, निर्वाचित मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना चाहिए।
- यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि प्रशासनिक प्राधिकार को चुनावी जनादेश को दरकिनार नहीं करना चाहिए, जिससे जम्मू-कश्मीर में गृह मंत्रालय का तर्क विकसित हो रहे संवैधानिक मानदंडों के विपरीत प्रतीत होता है।
(घ) केंद्र शासित प्रदेश शासन मॉडल:
- दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर जैसे विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश एक संकर शासन प्रणाली के तहत काम करते हैं, जहां केंद्र के पास महत्वपूर्ण नियंत्रण रहता है, जबकि स्थानीय सरकारों के पास विधायी शक्तियां होती हैं।
- जम्मू-कश्मीर जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील केंद्र शासित प्रदेशों में, केंद्रीय प्राधिकार और स्थानीय लोकतांत्रिक जवाबदेही के बीच तनाव बढ़ जाता है, खासकर तब जब नामांकन जैसी शक्तियां विधायी बहुमत को बदल सकती हैं।
जीएस2/राजनीति
क्रीमी लेयर आय सीमा में संशोधन: समय की मांग
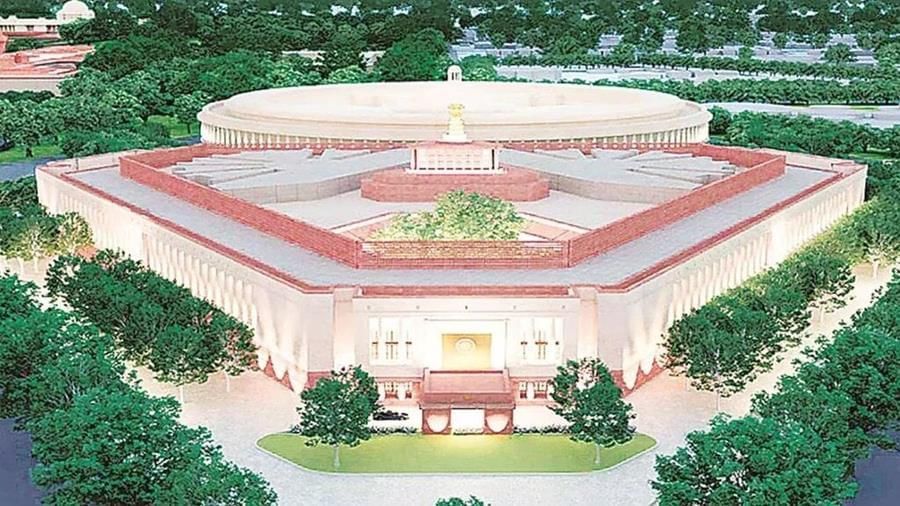
चर्चा में क्यों?
अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के कल्याण संबंधी संसदीय समिति ने ओबीसी आरक्षण लाभों के लिए "क्रीमी लेयर" आय सीमा में संशोधन की आवश्यकता पर बल दिया है। समिति ने इस संशोधन को "समय की आवश्यकता" बताया है और इस बात पर ज़ोर दिया है कि मुद्रास्फीति और बढ़ती आय के स्तर ने ₹8 लाख प्रति वर्ष (2017 में निर्धारित) की वर्तमान सीमा को अपर्याप्त बना दिया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE) ने संकेत दिया है कि वर्तमान में संशोधन के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
चाबी छीनना
- क्रीमी लेयर की अवधारणा इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992) निर्णय के बाद स्थापित की गई थी।
- बदलती आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद 2017 से वर्तमान आय सीमा में संशोधन नहीं किया गया है।
- कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के मानदंडों के अनुसार प्रत्येक तीन वर्ष में आवधिक संशोधन अनिवार्य है।
"क्रीमी लेयर" अवधारणा को समझना
- प्रारंभिक निर्धारण:क्रीमी लेयर की आय सीमा पहली बार 1993 में ₹1 लाख निर्धारित की गई थी और इसे कई बार संशोधित किया गया है:
- 2004 में ₹2.5 लाख
- 2008 में ₹4.5 लाख
- 2013 में ₹6 लाख
- 2014 में ₹6.5 लाख
- 2017 में ₹8 लाख (अंतिम संशोधन)
- बहिष्करण मानदंड: वार्षिक आय सीमा से अधिक आय वाले परिवारों को ओबीसी आरक्षण लाभ प्राप्त करने से बाहर रखा गया है।
भारत में ओबीसी आरक्षण: ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
- संवैधानिक आधार:
- अनुच्छेद 15(4): सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी), अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करता है।
- अनुच्छेद 16(4): राज्य को राज्य सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व वाले किसी भी पिछड़े वर्ग के लिए नियुक्तियों में आरक्षण प्रदान करने का अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 340: राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच करने और उपाय सुझाने के लिए एक आयोग नियुक्त करने का अधिकार देता है।
क्रीमी लेयर सीमा को संशोधित करने का महत्व
- आर्थिक परिवर्तनों के अनुरूप ढलते हुए यह सुनिश्चित किया जाता है कि लाभ उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है।
- इससे अधिकाधिक ओबीसी परिवारों को शिक्षा, नौकरी और सरकारी योजनाओं तक पहुंच बनाने में सहायता मिलेगी, जिससे असमानता कम होगी।
- नीतिगत दिशानिर्देशों का अनुपालन, क्योंकि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 1993 के आदेश में आवधिक संशोधन अनिवार्य किया गया है।
चुनौतियां
- आरक्षण लाभों में संतुलन: अति-विस्तार से बचने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे सबसे अधिक हाशिए पर रहने वाले लोगों को मिलने वाले लाभ कम हो सकते हैं।
- आर्थिक बनाम सामाजिक पिछड़ापन: आय केवल एक संकेतक है; सामाजिक अभाव को मापना अधिक जटिल है।
- राजनीतिक सहमति: आरक्षण नीति में परिवर्तन राजनीतिक रूप से संवेदनशील है और इसके लिए व्यापक सहमति की आवश्यकता है।
वर्तमान ₹8 लाख की सीमा पर समिति की चिंताएँ
- मुद्रास्फीति से क्षरण: बढ़ती आय के स्तर ने वर्तमान सीमा की प्रभावशीलता को कम कर दिया है।
- जरूरतमंद वर्गों का बहिष्कार: आरक्षण लाभ की आवश्यकता वाले कई ओबीसी परिवारों की आय 8 लाख रुपये से अधिक है, लेकिन फिर भी उन्हें आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है।
- सामाजिक-आर्थिक लक्ष्य: व्यापक कवरेज से अधिकाधिक ओबीसी परिवारों की सामाजिक और शैक्षिक स्थिति को ऊपर उठाने में मदद मिलेगी।
आगे बढ़ने का रास्ता
- आवधिक एवं पारदर्शी संशोधन: स्वचालित मुद्रास्फीति-सूचकांकित समायोजन लागू करें।
- व्यापक पिछड़ापन सूचकांक: इसमें आय के साथ-साथ शिक्षा, व्यवसाय और ग्रामीण/शहरी असमानताएं भी शामिल हैं।
- लक्षित छात्रवृत्तियाँ: शैक्षिक पाइपलाइनों को बढ़ाने के लिए निम्न कक्षाओं के लिए प्री-मैट्रिक सहायता का विस्तार करना।
- बेहतर डेटा: साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण के लिए नियमित सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण आयोजित करें।
क्रीमी लेयर प्रावधान यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि आरक्षण का लाभ ओबीसी के वास्तविक वंचित वर्ग तक पहुँचे। वर्तमान मुद्रास्फीति और बढ़ती आय के साथ, मौजूदा ₹8 लाख की सीमा अब प्रभावी नहीं रह सकती। संशोधन के लिए संसदीय समिति की सिफ़ारिश समानता और सामाजिक न्याय के संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप है, हालाँकि समावेशिता, दक्षता और निष्पक्षता के बीच संतुलन बनाने के लिए सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।
मूल्य संवर्धन
- प्रमुख घटनाक्रम:
- प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग (काका कालेलकर आयोग, 1953) - ने जाति-आधारित आरक्षण की सिफारिश की थी, लेकिन मात्रात्मक आंकड़ों की कमी के कारण इसे लागू नहीं किया गया।
- द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग (मंडल आयोग, 1979) - ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की, जिसे 1990 में लागू किया गया।
- इंद्रा साहनी केस (1992) - कुल आरक्षण को 50% तक सीमित कर दिया गया और ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर को बाहर रखा गया।
- हाल के रुझान:
- 102वां संविधान संशोधन (2018) - राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।
- 105वां संविधान संशोधन (2021) - राज्यों को अपने उद्देश्यों के लिए ओबीसी की पहचान करने की शक्ति बहाल की गई।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न:
- “पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण केवल आर्थिक मानदंडों के बजाय सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन पर आधारित होना चाहिए।” चर्चा करें।
- ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर समानता के भीतर समानता सुनिश्चित करने के लिए एक सुरक्षा कवच है।” टिप्पणी करें।
जीएस2/राजनीति
सुप्रीम कोर्ट का सोशल मीडिया विनियमन आदेश: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जवाबदेही

चर्चा में क्यों?
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को सोशल मीडिया को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने का आदेश दिया है, तथा इस बात पर जोर दिया है कि सार्वजनिक सम्मान की कीमत पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए शोषण नहीं किया जाना चाहिए।
चाबी छीनना
- सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को व्यापक सोशल मीडिया विनियमों का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया।
- न्यायालय का यह निर्णय डिजिटल रचनाकारों द्वारा लाभ के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के बारे में बढ़ती चिंताओं के बीच आया है।
- यह निर्णय डिजिटल परिदृश्य में संवैधानिक अधिकारों और जवाबदेही के बीच संतुलन स्थापित करता है।
अतिरिक्त विवरण
- सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश: दो न्यायाधीशों की पीठ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यद्यपि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत एक संवैधानिक अधिकार है, लेकिन इसका उपयोग व्यावसायिक लाभ के लिए इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए जिससे कमजोर समूहों को ठेस पहुंचे।
- यह मामला स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (एसएमए) से पीड़ित व्यक्तियों के लिए वकालत करने वाले एक गैर-लाभकारी संगठन द्वारा दायर याचिका से उत्पन्न हुआ, जिसमें दावा किया गया था कि हास्य कलाकारों की अपमानजनक टिप्पणियों से उनकी गरिमा का हनन होता है।
- न्यायालय ने केंद्र को आदेश दिया कि वह नियमों का मसौदा तैयार करते समय राष्ट्रीय प्रसारक एवं डिजिटल एसोसिएशन (एनबीडीए) से परामर्श करे तथा संबंधित हास्य कलाकारों को अपने सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का निर्देश दिया।
- मुक्त भाषण पर संवैधानिक ढांचा:संविधान का अनुच्छेद 19(2) विशिष्ट आधारों पर मुक्त भाषण पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है, जिनमें शामिल हैं:
- भारत की संप्रभुता और अखंडता
- राज्य की सुरक्षा
- विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध
- सार्वजनिक व्यवस्था
- शालीनता और नैतिकता
- न्यायालय की अवमानना
- मानहानि
- अपराधों के लिए उकसाना
- सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार यह कहा है कि प्रतिबंध इन आधारों से आगे नहीं बढ़ने चाहिए। श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) मामले में, न्यायालय ने आईटी अधिनियम की धारा 66ए को अमान्य करार देते हुए कहा कि "आहत, आघात या विचलित करने वाला" भाषण भी संरक्षित है।
- वाणिज्यिक भाषण पर बहस:भारत में वाणिज्यिक भाषण का विनियमन इस प्रकार विकसित हुआ है:
- हमदर्द दवाखाना बनाम भारत संघ (1959) मामले में न्यायालय ने फैसला दिया कि व्यापार से जुड़े विज्ञापन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में नहीं आते।
- इसके विपरीत, टाटा प्रेस बनाम एमटीएनएल (1995) ने वाणिज्यिक भाषण को संवैधानिक रूप से संरक्षित माना, क्योंकि यह सूचना प्रदान करके सार्वजनिक हित में कार्य करता है।
- ए. सुरेश बनाम तमिलनाडु राज्य (1997) जैसे बाद के मामलों में वाणिज्यिक अभिव्यक्ति को सामाजिक हितों के साथ संतुलित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।
- डिजिटल मीडिया के लिए मौजूदा कानूनी ढाँचा: भारत में सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पहले से ही आईटी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत विनियमित हैं, जो अश्लील और हानिकारक सामग्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश देते हैं। अगर किसी प्रभावशाली व्यक्ति का भाषण मानहानि या उकसावे वाला होता है, तो उसे कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ सकता है।
- विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उल्लंघन से बचने के लिए नए दिशा-निर्देशों को सावधानीपूर्वक तैयार किया जाना चाहिए, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संरक्षण देने का मजबूत इतिहास रहा है।
अदालत का हस्तक्षेप डिजिटल युग में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के भविष्य को लेकर गंभीर प्रश्न उठाता है, खासकर जब लगभग 49.1 करोड़ भारतीय सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। इसका उद्देश्य मनोरंजन या मार्केटिंग के रूप में प्रस्तुत की जाने वाली अपमानजनक या अपमानजनक सामग्री को सीमित करना है, साथ ही यह सरकार पर यह सुनिश्चित करने का दायित्व भी डालता है कि विनियमन सेंसरशिप का रूप न ले ले। कानूनी विद्वानों का सुझाव है कि यह निर्णय संवैधानिक सुरक्षा को कमज़ोर किए बिना जवाबदेही के सिद्धांतों को सुदृढ़ करने का अवसर प्रदान करता है।
जीएस2/राजनीति
भाषा और राज्यों का विभाजन

चर्चा में क्यों?
तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने हाल ही में यह कहकर एक बहस छेड़ दी कि भारतीय राज्यों के भाषाई पुनर्गठन ने आबादी के एक बड़े हिस्से को "द्वितीय श्रेणी के नागरिक" बना दिया है। गांधीनगर में एक कार्यक्रम में उनकी टिप्पणी से पता चलता है कि आज़ादी के तुरंत बाद शुरू किए गए बदलावों ने राष्ट्रीय एकता को खतरे में डाल दिया है।
चाबी छीनना
- भाषाई पुनर्गठन भारत की स्वतंत्रता के एक दशक के भीतर ही शुरू हो गया था और यह राष्ट्रीय एकता के संबंध में विवाद का विषय रहा है।
- भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को भारत के राजनीतिक भूगोल का एक महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है।
अतिरिक्त विवरण
- पुनर्गठन-पूर्व राजनीतिक भूगोल: 1947 में स्वतंत्रता के समय, भारत को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन द्वारा निर्मित एक जटिल प्रशासनिक संरचना विरासत में मिली थी, जिसमें प्रांतों पर प्रत्यक्ष शासन और रियासतों पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण शामिल था।
- 1950 के संविधान के तहत चार-भाग विभाजन:भारत को राज्यों की चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था:
- भाग ए राज्य: इसमें बंबई और मद्रास जैसे निर्वाचित विधानमंडलों वाले नौ पूर्व ब्रिटिश प्रांत शामिल थे।
- भाग बी राज्य: इसमें हैदराबाद और जम्मू एवं कश्मीर सहित आठ पूर्व रियासतें शामिल थीं, जो निर्वाचित विधायिकाओं और एक राजप्रमुख द्वारा शासित थीं।
- भाग सी राज्य: राष्ट्रपति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित दस क्षेत्र, उदाहरणों में दिल्ली और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं।
- भाग डी राज्य: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का प्रशासन एक लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा किया जाता था।
- जेवीपी समिति की चेतावनी: 1949 में, जेवीपी समिति ने चेतावनी दी थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन राष्ट्रीय एकता को बाधित कर सकता है।
- पोट्टी श्रीरामुलु की शहादत: पृथक तेलुगू राज्य के लिए भूख हड़ताल के बाद दिसंबर 1952 में उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जिसके परिणामस्वरूप 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ।
- राज्य पुनर्गठन आयोग (एसआरसी): भाषाई राज्य की मांग का आकलन करने के लिए दिसंबर 1953 में स्थापित, एसआरसी की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अंततः 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना।
- 1956 पुनर्गठन: इस अधिनियम ने भारत के राजनीतिक मानचित्र को मुख्यतः भाषाई आधार पर 14 राज्यों और छह केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया, जिससे भारत के संघीय ढांचे में एक महत्वपूर्ण विकास हुआ।
- संतुलित दृष्टिकोण: एसआरसी ने इस बात पर जोर दिया कि जहां भाषा और संस्कृति महत्वपूर्ण हैं, वहीं राष्ट्रीय एकता और प्रशासनिक व्यवहार्यता भी राज्य पुनर्गठन के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- बहुलवाद बनाम एकभाषावाद: नेहरू ने भाषाई समूहों के बीच सहयोग की वकालत की, तथा भारत के संघवाद की नींव के रूप में एकभाषावाद के विचार के विरुद्ध तर्क दिया।
- अंतर्राष्ट्रीय अवलोकन: कई पश्चिमी पर्यवेक्षकों ने अनुमान लगाया था कि भाषाई विभाजन से विखंडन होगा; हालांकि, भारत के अनुभव ने प्रदर्शित किया कि भाषाई राज्यों ने एकीकरण और दक्षता को बढ़ावा दिया।
निष्कर्षतः, भाषाई पुनर्गठन के प्रति भारत के दृष्टिकोण ने न केवल राष्ट्रीय एकता को बनाए रखा है, बल्कि इसे एक प्रशासनिक सफलता के रूप में भी देखा गया है, जिससे विविध समाज में सामंजस्य बनाए रखने में मदद मिली है। यह अन्य देशों के विपरीत है, जहाँ समान भाषाई मुद्दों के कारण संघर्ष हुए हैं।
जीएस2/राजनीति
न्यायालय से संकेत, आयोग से चुप्पी

चर्चा में क्यों?
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के संबंध में तत्काल प्रश्न उठाए हैं, जिसकी शुरुआत भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने की थी। हालाँकि ईसीआई इसे एक नियमित अद्यतन बता रहा है, लेकिन इसके निहितार्थ एक चिंताजनक बदलाव की ओर इशारा करते हैं जो भारत के लोकतांत्रिक चुनावी ढाँचे को कमज़ोर कर सकता है।
चाबी छीनना
- एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाताओं को नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है, जो निर्वाचन प्रणाली में शामिल होने की पारंपरिक धारणा के विपरीत है।
- कठोर दस्तावेजीकरण आवश्यकताओं के कारण लाखों हाशिए पर पड़े व्यक्तियों को मताधिकार से वंचित होना पड़ सकता है।
- यह नीति भारत के सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के मूलभूत दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण विचलन का प्रतिनिधित्व करती है।
अतिरिक्त विवरण
- मताधिकार से वंचित होने का खतरा: एसआईआर मतदाताओं से जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट जैसे दुर्लभ दस्तावेज एक महीने की सख्त समय सीमा के भीतर प्रस्तुत करने की मांग करता है, जिससे अकेले बिहार में 6.5 मिलियन से अधिक लोगों के मताधिकार से वंचित होने का खतरा है।
- ऐतिहासिक संदर्भ: यह स्थिति संयुक्त राज्य अमेरिका के जिम क्रो युग से मिलती जुलती है, जहां हाशिए पर पड़ी आबादी को दबाने के लिए इसी तरह की नौकरशाही बाधाओं का इस्तेमाल किया गया था।
- अनुमानित समावेशन से अनुमानित बहिष्करण की ओर बदलाव भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में संबद्धता की मौलिक प्रकृति को बदल देता है।
- न्यायिक प्रतिक्रिया: ईसीआई के कार्यों की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच एक सकारात्मक घटनाक्रम है, लेकिन संविधान के मूल मूल्यों को बनाए रखने के लिए अधिक सशक्त हस्तक्षेप आवश्यक है।
यह स्थिति केवल प्रशासनिक मुद्दों से परे है; यह मूलतः लोकतंत्र में सत्ता की गतिशीलता से संबंधित है। यदि मताधिकार से वंचित करना अनियंत्रित रूप से जारी रहा, तो भारत केवल नाममात्र का लोकतंत्र बनकर रह जाने का जोखिम उठाता है। नागरिकों को अपने मताधिकार को एक जन्मजात अधिकार के रूप में पुनः प्राप्त करना होगा, न कि नौकरशाही अनुपालन पर आधारित विशेषाधिकार के रूप में।
जीएस2/राजनीति
भारत में जमानत की मंजूरी

चर्चा में क्यों?
अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा नकदी रहित जमानत के लिए संघीय वित्त पोषण रोकने के हालिया निर्णय से इस प्रणाली की निष्पक्षता, विशेष रूप से आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों पर इसके प्रभाव के संबंध में चर्चाएं शुरू हो गई हैं।
चाबी छीनना
- नकदी रहित जमानत प्रणाली में अग्रिम नकदी की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, तथा इसके स्थान पर निगरानी और अदालत में उपस्थिति के आश्वासन जैसी गैर-वित्तीय शर्तों पर निर्भरता बढ़ जाती है।
- पारंपरिक नकद जमानत प्रणाली गरीबों को असमान रूप से प्रभावित करती है, जिसके कारण अक्सर मामूली अपराधों के आरोपी व्यक्तियों को भुगतान करने में असमर्थता के कारण हिरासत में ले लिया जाता है।
अतिरिक्त विवरण
- भारत में जमानत के प्रावधान: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 के तहत, जमानत एक ऐसे तंत्र के रूप में कार्य करती है जो किसी आरोपी को फरार होने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के खिलाफ आश्वासन के साथ हिरासत से रिहा करता है।
- बीएनएसएस के तहत जमानत के प्रकार:
- नियमित जमानत: जमानतीय अपराधों के लिए जमानत एक अधिकार है (धारा 478); गैर-जमानती अपराधों के लिए यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर है (धारा 480, 483)।
- अग्रिम जमानत (धारा 482): गैर-जमानती अपराधों में गिरफ्तारी से पहले दी जाती है, साथ ही यह शर्त भी लगाई जाती है कि जांच में कोई हस्तक्षेप न हो।
- अंतरिम जमानत: नियमित या अग्रिम जमानत आवेदनों पर निर्णय की प्रतीक्षा करते समय अस्थायी रिहाई।
- वैधानिक/डिफ़ॉल्ट ज़मानत (धारा 187): यदि निर्धारित समय के भीतर आरोपपत्र दाखिल नहीं किया जाता है तो अभियुक्त को ज़मानत का अधिकार है।
- व्यवहार में जमानत तंत्र:
- बांड: अभियुक्त एक बांड पर हस्ताक्षर करता है और गारंटी के रूप में नकदी जमा करता है, जो परीक्षण के बाद वापस कर दी जाती है, जब तक कि शर्तों का उल्लंघन न किया जाए।
- जमानत बांड: किसी मित्र, परिवार के सदस्य या नियोक्ता द्वारा दी गई जमानत, जिसमें उनकी वित्तीय स्थिरता और निवास का सत्यापन आवश्यक होता है।
- व्यक्तिगत पहचान (पीआर) बांड: अभियुक्त को तत्काल नकद जमा के बिना रिहा कर दिया जाता है, लेकिन उसे निर्दिष्ट समय के भीतर धन की व्यवस्था करनी होती है।
- भारत की जमानत प्रणाली में चुनौतियाँ:
- जमानत के पात्र होने के बावजूद कई विचाराधीन कैदी जमानत या छोटी रकम (जैसे, 5,000 रुपये या उससे कम) जमा करने में असमर्थता के कारण जेल में ही रहते हैं।
- जेलों में अत्यधिक भीड़भाड़ एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, महाराष्ट्र की जेलों में जुलाई 2025 तक 12,000 से अधिक अतिरिक्त कैदी होने की सूचना है।
- न्यायिक चिंताएं: 268वीं विधि आयोग रिपोर्ट (2017) ने मौद्रिक जमानत प्रणाली को भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक माना, जो निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन करती है।
- सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देश (2023): यदि कोई अभियुक्त जमानत के बावजूद एक सप्ताह से अधिक समय तक जेल में रहता है, तो जेल अधीक्षक को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को सूचित करना होगा, जो उनकी रिहाई की सुविधा प्रदान कर सकता है।
- बीएनएसएस के अंतर्गत सुधार (2023): जेल प्राधिकारियों को ऐसे विचाराधीन कैदियों के लिए जमानत हेतु आवेदन करना अनिवार्य है, जिन्होंने अपनी अधिकतम सजा का एक निर्दिष्ट भाग पूरा कर लिया है, आजीवन कारावास या मृत्युदंड के मामलों को छोड़कर।
संक्षेप में, भारत में ज़मानत प्रणाली महत्वपूर्ण जाँच और सुधार के दौर से गुज़र रही है क्योंकि यह अभियुक्तों के अधिकारों और न्यायिक प्रक्रिया की अखंडता के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करती है। विचाराधीन कैदियों के सामने आने वाली चुनौतियाँ क़ानूनी और व्यवस्थागत सुधारों की तत्काल आवश्यकता को उजागर करती हैं।
जीएस2/राजनीति
कानूनी पागलपन और न्यायिक कार्यवाहियों में इसके निहितार्थ

चर्चा में क्यों?
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने हाल ही में दोहरे हत्याकांड के एक व्यक्ति को कानूनी पागलपन के आधार पर बरी कर दिया, जिससे आपराधिक मुकदमों में मानसिक स्थिति के मूल्यांकन की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया गया।
चाबी छीनना
- कानूनी पागलपन, आपराधिक कानून में मानसिक अक्षमता पर आधारित बचाव है।
- अभियुक्तों को यह साबित करना होगा कि वे गंभीर मानसिक बीमारी के कारण अपने कार्यों की प्रकृति को समझने में असमर्थ थे।
- कानूनी पागलपन के विभिन्न प्रकार हैं, जिनमें भावनात्मक और अस्थायी पागलपन भी शामिल हैं।
अतिरिक्त विवरण
- कानूनी पागलपन: यह शब्द एक ऐसी मानसिक स्थिति को संदर्भित करता है जो किसी अपराध के लिए कानूनी ज़िम्मेदारी को नकारने के लिए पर्याप्त गंभीर हो। इसमें यह मान लिया जाता है कि प्रतिवादी अपराध के समय अपने कार्यों की प्रकृति को समझ नहीं पा रहा था या सही-गलत में अंतर नहीं कर पा रहा था।
- पागलपन का बचाव एक कानूनी अवधारणा है, न कि केवल एक नैदानिक अवधारणा; पागलपन को साबित करने के लिए केवल मानसिक विकार होने से अधिक की आवश्यकता होती है।
- कानूनी पागलपन का सफलतापूर्वक दावा करने के लिए, अभियुक्त को अक्सर मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के माध्यम से साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा, जिससे पता चले कि घटना के दौरान वे अपनी तर्क क्षमता पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे थे।
- कानूनी पागलपन के विभिन्न रूपों में भावनात्मक पागलपन, जो तीव्र भावनात्मक अशांति से चिह्नित होता है, और अस्थायी पागलपन, जो केवल अपराध के समय ही मौजूद होता है, शामिल हैं।
- सुरेन्द्र मिश्रा बनाम झारखंड राज्य (एआईआर 2011 एससी 627) के सर्वोच्च न्यायालय के मामले में यह स्थापित किया गया कि मानसिक बीमारियों से ग्रस्त सभी व्यक्ति आपराधिक दायित्व से मुक्त नहीं हैं; साक्ष्य का भार अभियुक्त पर है।
निष्कर्षतः, कानूनी पागलपन की अवधारणा यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अपने कार्यों को समझने में असमर्थ व्यक्तियों के साथ कानूनी व्यवस्था में उचित व्यवहार किया जाए। यह आपराधिक उत्तरदायित्व को समझने में मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन के महत्व को उजागर करता है।
जीएस2/राजनीति
परमाणु कानून और विपक्ष की भूमिका

चर्चा में क्यों?
भारत की ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताओं को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार महत्वपूर्ण विधायी मुद्दों, विशेष रूप से परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम (सीएलएनडीए), 2010, और परमाणु ऊर्जा अधिनियम (एईए), 1962 पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार है। प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य दायित्व ढांचे को फिर से परिभाषित करना और परमाणु ऊर्जा में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना है, जिससे विपक्ष की एकता का परीक्षण हो और भारत के परमाणु भविष्य को आकार मिले।
चाबी छीनना
- परमाणु दुर्घटनाओं के लिए उत्तरदायित्व ढांचा स्थापित करने हेतु 2010 में सीएलएनडीए अधिनियमित किया गया था।
- विपक्षी दलों के अनुसार, संशोधनों से जवाबदेही कम हो सकती है तथा विदेशी कॉर्पोरेट हितों को प्राथमिकता मिल सकती है।
- भारत की परमाणु ऊर्जा कुल ऊर्जा मिश्रण में केवल 3% का योगदान देती है, जिससे विकास के लिए संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है।
अतिरिक्त विवरण
- ऐतिहासिक संदर्भ: भारत में परमाणु दायित्व पर बहस पंद्रह वर्ष से अधिक पुरानी है, तथा सीएलएनडीए को भोपाल गैस रिसाव और फुकुशिमा आपदा जैसी बड़ी आपदाओं के बाद लागू किया गया था, जिससे कॉर्पोरेट जवाबदेही की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।
- राजनीतिक गतिशीलता: भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार निवेश आकर्षित करने के लिए मौजूदा कानूनों में संशोधन करना चाहती है, जबकि कांग्रेस इन परिवर्तनों का विरोध करती है, उनका तर्क है कि इससे सुरक्षा और जवाबदेही से समझौता होगा।
- ऊर्जा आकांक्षाएं: सरकार का लक्ष्य 2031-32 तक परमाणु क्षमता को 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 22.48 गीगावाट तथा 2047 तक 100 गीगावाट करना है, जो देयता संबंधी मुद्दों के समाधान तथा नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर निर्भर है।
परमाणु कानूनों पर चल रही चर्चा भारत के ऊर्जा क्षेत्र में जवाबदेही सुनिश्चित करने और विकास को बढ़ावा देने के बीच के नाज़ुक संतुलन को रेखांकित करती है। जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए निवेश आकर्षित करने और परमाणु क्षमता का विस्तार करने के लिए एक व्यावहारिक दायित्व ढाँचा आवश्यक है। अंततः, इन मुद्दों पर द्विदलीय सहयोग और रचनात्मक बहस, ऊर्जा सुरक्षा को जन सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों के साथ संरेखित करने के लिए महत्वपूर्ण होगी।
जीएस2/राजनीति
जन विश्वास विधेयक 2.0
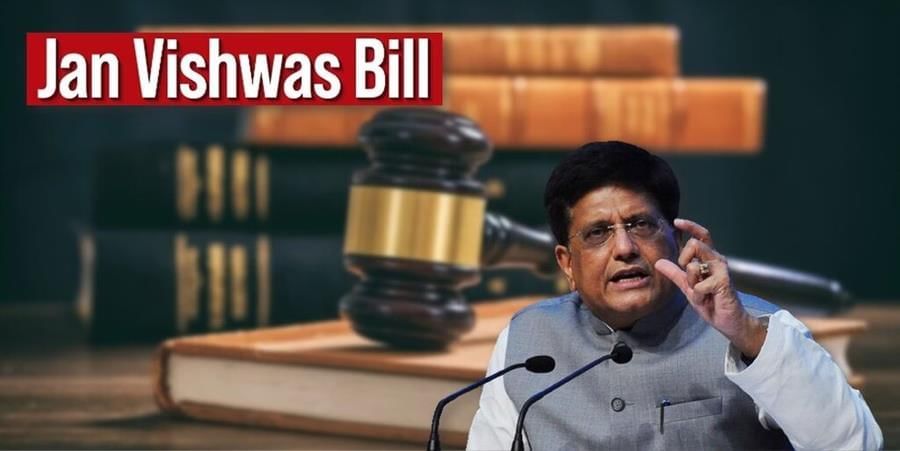
चर्चा में क्यों?
कानूनों को अपराधमुक्त और युक्तिसंगत बनाने के सरकार के प्रयासों की अगली कड़ी के रूप में, जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2025 लोकसभा में पेश किया गया है। यह जन विश्वास विधेयक का दूसरा संस्करण है, इससे पहले 2023 में 42 अधिनियमों के 183 प्रावधानों को अपराधमुक्त करने का लक्ष्य रखा गया था।
चाबी छीनना
- अगस्त 2025 में दूसरे जन विश्वास सुधार के रूप में लोकसभा में पेश किया जाएगा।
- इसका उद्देश्य 10 मंत्रालयों/विभागों से संबंधित 16 केन्द्रीय अधिनियमों में संशोधन करना है।
- यह अधिनियम 2023 के जन विश्वास अधिनियम पर आधारित है, जिसमें 183 प्रावधानों को अपराधमुक्त किया गया है।
- इसका उद्देश्य विश्वास आधारित शासन को बढ़ाना तथा जीवन और व्यापार को आसान बनाना है।
- वर्तमान में यह लोकसभा प्रवर समिति द्वारा समीक्षाधीन है।
अतिरिक्त विवरण
- दायरा: विधेयक में 355 प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव है, जिसमें से 288 को तकनीकी और प्रक्रियागत चूक के कारण अपराधमुक्त कर दिया गया है तथा 67 को बेहतर जीवन-यापन के लिए युक्तिसंगत बनाया गया है।
- इसमें शामिल अधिनियम: इसमें आरबीआई अधिनियम (1934), औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम (1940), मोटर वाहन अधिनियम (1988), विद्युत अधिनियम (2003) और अन्य जैसे महत्वपूर्ण कानून शामिल हैं।
- पहली बार अपराध: मोटर वाहन अधिनियम के छोटे उल्लंघन जैसे 76 अपराधों के लिए "चेतावनी" और "सुधार नोटिस" प्रस्तुत किया गया।
- गैर-अपराधीकरण: मामूली चूक के लिए कारावास की धाराएँ हटाकर उनकी जगह जुर्माना या चेतावनी का प्रावधान किया गया है। उदाहरण के लिए, विद्युत अधिनियम में कारावास की जगह ₹10,000 से ₹10 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
- दंड का युक्तिकरण: दोहराए गए अपराधों के लिए प्रत्येक तीन वर्ष में दंड में 10% की स्वतः वृद्धि की व्यवस्था की गई है, जिससे न्यायपालिका पर अधिक बोझ डाले बिना निवारण सुनिश्चित किया जा सके।
इस विधेयक का प्रस्ताव भारतीय कानूनों के अति-अपराधीकरण को संबोधित करता है, जहाँ 882 केंद्रीय कानूनों में 7,305 से अधिक अपराधों के लिए आपराधिक प्रावधान हैं, जिनमें से कई मामूली या पुराने हैं। इस विधेयक का उद्देश्य अत्यधिक कानूनी परिणामों के कारण उद्यमियों में व्याप्त भय को कम करना है, जिससे व्यावसायिक विकास को बढ़ावा मिले और वर्तमान प्रशासन के शासन सुधार एजेंडे के साथ तालमेल बिठाया जा सके।
जीएस2/राजनीति
ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम 2025 की मुख्य विशेषताएं

समाचार में क्यों?
भारतीय संसद ने ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम 2025 पारित कर दिया है, जिसका उद्देश्य रियल मनी गेम्स (आरएमजी) पर प्रतिबंध लगाकर बढ़ते डिजिटल गेमिंग उद्योग को नियंत्रित करना है और एक संरचित ढाँचे के माध्यम से ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा देना है। यह कानून आरएमजी से जुड़ी लत, धोखाधड़ी और आर्थिक नुकसान से जुड़ी बढ़ती चिंताओं को दूर करता है।
चाबी छीनना
- अधिनियम ऑनलाइन गेम्स को ई-स्पोर्ट्स, सोशल गेमिंग और आरएमजी में वर्गीकृत करता है।
- वास्तविक धन वाले खेलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसमें संबंधित विज्ञापन और समर्थन भी शामिल हैं।
- उल्लंघन के लिए कठोर दंड लगाया जाता है, जिसमें खिलाड़ियों के बजाय ऑपरेटरों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
- इस अधिनियम का उद्देश्य सुरक्षित ऑनलाइन गेमिंग पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना और सरकारी वित्त पोषण के माध्यम से ई-स्पोर्ट्स का समर्थन करना है।
अतिरिक्त विवरण
- ऑनलाइन गेम्स का वर्गीकरण:अधिनियम तीन श्रेणियों में अंतर करता है:
- ई-स्पोर्ट्स: पुरस्कार राशि वाले मान्यता प्राप्त प्रतिस्पर्धी वीडियो गेम, जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी और ग्रैंड थेफ्ट ऑटो।
- सामाजिक गेमिंग: मनोरंजन या शैक्षिक उद्देश्यों के लिए खेले जाने वाले खेल, आमतौर पर बिना किसी मौद्रिक दांव के।
- वास्तविक धन वाले खेल: पोकर और फैंटेसी क्रिकेट जैसे धन, क्रेडिट या टोकन वाले खेलों पर प्रतिबंध है।
- दंड और प्रवर्तन:
- आरएमजी की पेशकश करने पर तीन साल तक की कैद या 1 करोड़ रुपये का जुर्माना हो सकता है।
- गैरकानूनी विज्ञापन पर दो साल की कैद या 50 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है।
- सरकारी निरीक्षण: CERT-IN को गैर-अनुपालन वाले ऐप्स को निष्क्रिय करने का अधिकार दिया गया है, तथा अपतटीय ऑपरेटरों की समस्या से निपटने के लिए इंटरपोल के साथ सहयोग की योजना बनाई गई है।
- कानून का औचित्य: यह अधिनियम नशे की लत, वित्तीय धोखाधड़ी, कर चोरी और आतंकवाद के वित्तपोषण से संभावित संबंध जैसे मुद्दों के प्रति एक सक्रिय प्रतिक्रिया है।
- कानूनी चुनौतियाँ: इस अधिनियम को खेलों के वर्गीकरण और राज्य कानूनों के साथ क्षेत्राधिकार संबंधी ओवरलैप के संबंध में जांच का सामना करना पड़ रहा है।
ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम 2025 भारत के गेमिंग परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण नियामक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका उद्देश्य नवाचार और जन सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करना है। ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा देकर और साथ ही RMG पर नकेल कस कर, सरकार एक सुरक्षित गेमिंग वातावरण बनाने का प्रयास कर रही है।
जीएस2/राजनीति
भारत का ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025
चर्चा में क्यों?
लोकसभा ने हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य एक नए नियामक ढांचे के तहत ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा देते हुए हानिकारक वास्तविक धन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाना है।
चाबी छीनना
- विधेयक में वास्तविक धन से खेले जाने वाले खेलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि इससे सामाजिक, वित्तीय और मनोवैज्ञानिक नुकसान हो सकते हैं।
- इसका उद्देश्य कमजोर समूहों की रक्षा करना, जिम्मेदार गेमिंग को प्रोत्साहित करना और भारत के डिजिटल नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है।
अतिरिक्त विवरण
- मुख्य प्रावधान:विधेयक को तीन मुख्य खंडों में विभाजित किया गया है:
- ई-स्पोर्ट्स: इसे एक रचनात्मक उद्योग के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसमें महत्वपूर्ण विकास की संभावना है, विधेयक इसे मुख्यधारा के क्षेत्र के रूप में विकसित करने का समर्थन करता है।
- ऑनलाइन सामाजिक खेल: इन्हें सुरक्षित मनोरंजन के विकल्प के रूप में प्रचारित किया जाता है, जिसमें वित्तीय जोखिम या जुआ खेलने की लत नहीं होती।
- ऑनलाइन मनी गेम्स: इन पर पूर्णतः प्रतिबंध है, जिनमें फैंटेसी स्पोर्ट्स, पोकर और रम्मी जैसी गतिविधियां शामिल हैं।
- उल्लंघन के लिए दंड: पहली बार अपराध करने वालों को तीन वर्ष तक की कैद और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, तथा बार-बार अपराध करने पर कठोर दंड का प्रावधान है।
- ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण की स्थापना: यह वैधानिक निकाय इस क्षेत्र की देखरेख करेगा, सुरक्षित प्रथाओं को सुनिश्चित करेगा और गेमिंग प्लेटफार्मों को विनियमित करेगा।
कानून के पीछे तर्क
सरकार ने चिंताजनक प्रवृत्तियों के कारण विनियामक कार्रवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला:
- पिछले 31 महीनों में ऑनलाइन मनी गेमिंग की लत से जुड़ी 32 आत्महत्याएं हुईं।
- जुआ खेलने की लत के कारण परिवारों में वित्तीय संकट।
- वास्तविक धन वाले गेमिंग के माध्यम से धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण पर चिंता।
- शोषणकारी गेमिंग एल्गोरिदम से उत्पन्न मनोवैज्ञानिक मुद्दे।
लोकसभा अध्यक्ष ने विधेयक को "राष्ट्रीय हित" का कानून बताया, जिसका उद्देश्य परिवारों में वित्तीय और भावनात्मक संकटों को रोकना है।
उद्योग की प्रतिक्रिया और संभावित चुनौतियाँ
इस विधेयक ने भारत के अरबों डॉलर के रियल मनी गेमिंग क्षेत्र में चिंताएँ पैदा कर दी हैं, जिसने पहले पूर्ण प्रतिबंध के बजाय नियमन की वकालत की थी। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह विधेयक न्यायिक जाँच में खरा उतरने के लिए पर्याप्त मज़बूत है, और जनहित और राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित है।
भारत के डिजिटल भविष्य के लिए महत्व
- युवाओं के लिए: इस विधेयक का उद्देश्य युवा खिलाड़ियों को नशे की लत और वित्तीय बर्बादी से बचाना है।
- उद्योग के लिए: यह ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग स्टार्टअप्स को स्पष्टता और वैधता प्रदान करता है।
- समाज के लिए: यह धोखाधड़ी, धन शोधन और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित चिंताओं को संबोधित करता है।
- शासन के लिए: खंडित गेमिंग क्षेत्र को प्रभावी ढंग से विनियमित करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का ढांचा स्थापित किया गया है।
ई-स्पोर्ट्स को समर्थन देकर, यह विधेयक डिजिटल मनोरंजन में वैश्विक नेता बनने के भारत के लक्ष्य के अनुरूप है, विशेष रूप से प्रस्तावित 2036 ओलंपिक जैसे आगामी आयोजनों के साथ।
जीएस2/शासन
नशा मुक्त भारत की ओर

चर्चा में क्यों?
भारत नशीली दवाओं के दुरुपयोग के बढ़ते संकट का सामना कर रहा है, जिसके कारण सरकार को कदम उठाने के लिए प्रेरित किया गया है। इस समस्या से निपटने के लिए नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया था और यह पिछले पाँच वर्षों से प्रभावी है।
नशा मुक्त भारत अभियान
- नशा मुक्त भारत अभियान के बारे में: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 15 अगस्त 2020 को नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया था।
- उद्देश्य: इस कार्यक्रम का उद्देश्य मादक द्रव्यों के सेवन के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, खासकर शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों और स्कूलों में। यह नशे की लत से ग्रस्त आबादी की पहचान करने और परामर्श एवं उपचार सुविधाओं को मज़बूत करने पर भी केंद्रित है।
- विस्तार: प्रारंभ में इस कार्यक्रम का लक्ष्य 272 संवेदनशील जिले थे, तथा अब इसे भारत के सभी जिलों तक विस्तारित कर दिया गया है।
3-आयामी रणनीति
नशा मुक्त भारत अभियान तीन-आयामी रणनीति का पालन करता है जिसमें शामिल हैं:
- आपूर्ति नियंत्रण: दवाओं की आपूर्ति को नियंत्रित करने के उपाय।
- मांग में कमी: दवाओं की मांग को कम करने के प्रयास।
- चिकित्सा उपचार: व्यसन के लिए चिकित्सा उपचार प्रदान करना।
मुख्य सफलतायें
- जन जागरूकता: 18.10 करोड़ से अधिक लोगों और 4.85 लाख संस्थानों तक पहुंच बनाई गई।
- युवा लामबंदी: प्रतिज्ञाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से 1.67 करोड़ छात्रों को शामिल किया गया।
- डिजिटल एवं तकनीकी एकीकरण: सोशल मीडिया, वेबसाइट, एप और जियो-टैगिंग का उपयोग किया गया।
- स्वयंसेवी नेटवर्क: 20,000 से अधिक मास्टर स्वयंसेवकों का नेटवर्क स्थापित किया गया।
- सामुदायिक आउटरीच: अभियान, निगरानी और जागरूकता अभियान चलाए गए।
- सहयोग: आर्ट ऑफ लिविंग, ब्रह्माकुमारीज, संत निरंकारी मिशन, राम चंद्र मिशन (दाजी), इस्कॉन और अन्य जैसे आध्यात्मिक और सामाजिक संगठनों के साथ साझेदारी बनाई।
भारत में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की व्यापकता
- नशीली दवाओं की लत: भारत में लगभग 10 करोड़ लोग नशीले पदार्थों से प्रभावित हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब जैसे राज्यों में एनडीपीएस अधिनियम (2019-2021) के तहत सबसे अधिक एफआईआर दर्ज की गई हैं।
- प्रमुख उपभोग वाली दवाएं: पदार्थ उपयोग की सीमा और पैटर्न पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण (2019) में पाया गया कि 10-75 आयु वर्ग के लगभग 16 करोड़ लोग (14.6%) शराब का उपयोग करते हैं, जबकि 3.1 करोड़ (2.8%) भांग का उपयोग करते हैं।
दुनिया के 2 प्रमुख दवा उत्पादक क्षेत्र
- गोल्डन क्रिसेंट: इस क्षेत्र में अफ़ग़ानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान शामिल हैं और यह अफ़ीम का एक प्रमुख केंद्र है। यह जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और गुजरात जैसे भारतीय राज्यों को प्रभावित करता है।
- स्वर्णिम त्रिभुज: लाओस, म्यांमार और थाईलैंड से मिलकर बना यह क्षेत्र हेरोइन का एक प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, जहाँ वैश्विक आपूर्ति का लगभग 80% म्यांमार से आता है। इस क्षेत्र से तस्करी के रास्ते भारत से होकर गुजरते हैं, जिससे यह एक संवेदनशील पारगमन और उपभोग क्षेत्र बन जाता है।
भारत में नशीली दवाओं के नियंत्रण में प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?
स्मृति सहायक: डोप
- डी - डार्क नेट और नए पदार्थ: डार्कनेट और क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करके नए मनोवैज्ञानिक पदार्थों और अवैध ऑनलाइन व्यापार का उदय एक महत्वपूर्ण चुनौती है।
- ओ - संगठनात्मक एवं बुनियादी ढांचे में अंतराल: प्रभावी दवा नियंत्रण के लिए आवश्यक प्रशिक्षित कर्मियों, फोरेंसिक प्रयोगशालाओं, पुनर्वास केंद्रों और विशेष सुविधाओं की कमी है।
- पी - अपर्याप्त जागरूकता और रोकथाम: अपर्याप्त शिक्षा और कमजोर सामुदायिक स्तर की जागरूकता, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और युवा आबादी के बीच, रोकथाम के प्रयासों में बाधा डालती है।
- ई - व्यसन उपचार में बहिष्कार और कलंक: सामाजिक कलंक और पुनर्वास सेवाओं की उच्च मांग व्यक्तियों को सहायता लेने से हतोत्साहित करती है, जिससे दवा नियंत्रण उपायों की प्रभावशीलता सीमित हो जाती है।
भारत में नशीली दवाओं के दुरुपयोग को समाप्त करने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए?
स्मृति सहायक: सुरक्षित
- एस - कानून प्रवर्तन को मज़बूत करें: एनडीपीएस अधिनियम, 1985 और स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार निवारण (पीआईटीएनडीपीएस) अधिनियम, 1988 के कार्यान्वयन को बढ़ावा दें। इसमें पर्याप्त संसाधन, प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराना और खुफिया एवं निगरानी क्षमताओं में सुधार करना शामिल है। अंतर-एजेंसी समन्वय को भी मज़बूत किया जाना चाहिए।
- ए - जागरूकता एवं रोकथाम: नशीली दवाओं की माँग में कमी हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) के अनुसार उपचार एवं पुनर्वास सुविधाओं का विस्तार करना। इसमें नशामुक्ति एवं पुनर्वास कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता बढ़ाना शामिल है।
- एफ – आपूर्ति में कमी पर ध्यान: सीमा नियंत्रण में सुधार करें और एआई, बिग डेटा, ड्रोन और उपग्रह जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करें। ऑनलाइन नागरिक रिपोर्टिंग प्रणाली स्थापित करें और अवैध फसल उगाने वाले किसानों के लिए झारखंड पोस्ता योजना जैसे वैकल्पिक आजीविका के साधनों का समर्थन करें। आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करना भी महत्वपूर्ण है।
- ई - अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना: मादक पदार्थों की तस्करी की गतिविधियों पर नज़र रखने और उन्हें रोकने के लिए पड़ोसी देशों, संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (यूएनओडीसी) और इंटरपोल के साथ सहयोग करना।
जीएस2/शासन
अंगदान को जीवन रेखा के रूप में मान्यता देना
चर्चा में क्यों?
अंग प्रत्यारोपण एक महत्वपूर्ण चिकित्सा प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है और टर्मिनल अंग विफलता के लिए सबसे प्रभावी उपाय के रूप में कार्य करता है। हालांकि, भारत दाता अंगों की गंभीर कमी से जूझ रहा है, जिसके परिणामस्वरूप हर साल 500,000 से अधिक रोके जा सकने वाली मौतें होती हैं। हालांकि प्रत्यारोपणों की संख्या 2013 में 4,990 से बढ़कर 2023 में 18,378 हो गई है, इनमें से केवल 1,099 में मृतक दाता शामिल थे। केवल 0.8 प्रति मिलियन लोगों की अंग दान दर के साथ, जो स्पेन और अमेरिका (45 प्रति मिलियन से अधिक) की तुलना में काफी कम है, मांग और आपूर्ति के बीच असमानता चिंताजनक बनी हुई है, जिससे अनगिनत अनावश्यक मौतें होती हैं। यह लेख मिथकों को दूर करके, सार्वजनिक विश्वास को बढ़ाकर और दान दरों को बढ़ाने के लिए प्रभावी नीतियों को लागू करके भारत में अंग की कमी से निपटने की तत्काल आवश्यकता पर जोर देता है।
चाबी छीनना
- भारत में अंगदान की दर बहुत कम है, जिसके कारण मृत्यु दर में भारी वृद्धि हो रही है।
- अंगदान के बारे में मिथक संभावित दाताओं और परिवारों के लिए बाधा बनते हैं।
- अंगदान की दर में सुधार के लिए सार्वजनिक शिक्षा आवश्यक है।
अतिरिक्त विवरण
- मिथकों का खंडन: कई परिवारों का मानना है कि अंग निकालने से शरीर विकृत हो जाता है, जिससे अंतिम संस्कार की रस्में जटिल हो जाती हैं। वास्तव में, अंग निकालने की प्रक्रिया सम्मानपूर्वक की जाती है, ताकि अंतिम संस्कार तक दाता की उपस्थिति बनी रहे। प्रमुख धर्म अंगदान को आध्यात्मिक मूल्यों से जुड़ा एक करुणामय कार्य मानते हैं।
- मस्तिष्क मृत्यु प्रमाणन: यह एक गलत धारणा है कि डॉक्टर अंग प्राप्त करने के लिए मस्तिष्क मृत्यु की घोषणा करने में जल्दबाजी कर सकते हैं। हालाँकि, यह प्रक्रिया मानव अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 द्वारा नियंत्रित होती है, जो नैतिक प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए कई विशेषज्ञों की पुष्टि और विस्तृत दस्तावेज़ीकरण अनिवार्य करता है।
- आयु और स्वास्थ्य संबंधी मिथकों पर ध्यान: एक और गलत धारणा यह है कि केवल युवा दुर्घटना पीड़ित ही अंगदाता हो सकते हैं। वृद्ध व्यक्ति या प्राकृतिक कारणों से मरने वाले व्यक्ति भी गुर्दे, यकृत खंड, फेफड़े, कॉर्निया, हड्डियाँ, त्वचा और हृदय वाल्व सहित विभिन्न अंग और ऊतक दान कर सकते हैं।
- सामुदायिक सहभागिता: मीडिया अभियानों, सामुदायिक कार्यशालाओं और शैक्षिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से निरंतर जागरूकता दान की संस्कृति को बढ़ावा दे सकती है। स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को भी सूचित निर्णय लेने में सहायता के लिए परिवारों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना चाहिए।
निष्कर्षतः, अंगदान चिकित्सा हस्तक्षेप से कहीं आगे जाता है; यह एक गहन मानवीय भाव और करुणा की विरासत का प्रतीक है। विश्व अंगदान दिवस (13 अगस्त) पर, व्यक्तियों को दाता के रूप में पंजीकरण कराने और परिवारों को इस विकल्प का सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मिथकों को दूर करके, नीतियों में सुधार करके और साझा ज़िम्मेदारी की संस्कृति को बढ़ावा देकर, भारत एक ऐसे भविष्य की ओर अग्रसर हो सकता है जहाँ उपलब्ध अंगों की कमी के कारण किसी की जान न जाए।
जीएस2/राजनीति
सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाने का अधिकार दिया
चर्चा में क्यों?
सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में अपने फैसले में कहा है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (पीसीबी) को प्रदूषणकारी संस्थाओं पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाने का अधिकार है। यह फैसला जल अधिनियम और वायु अधिनियम के तहत उनके वैधानिक अधिकार क्षेत्र से जुड़ा है, जो पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिए सक्रिय उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।
चाबी छीनना
- पीसीबी निश्चित मौद्रिक राशि या बैंक गारंटी के माध्यम से क्षतिपूर्ति या प्रतिपूरक क्षतिपूर्ति की मांग कर सकते हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पिछले फैसले को पलट दिया, जिसमें दंड लगाने का अधिकार केवल अदालतों तक सीमित कर दिया गया था।
- मुआवजा केवल तभी लगाया जा सकता है जब वास्तविक पर्यावरणीय क्षति हो चुकी हो या होने वाली हो।
अतिरिक्त विवरण
- मामले की पृष्ठभूमि: दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने 2012 के दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें वैध पर्यावरणीय सहमति के अभाव वाली संपत्तियों से मुआवजे की मांग करने वाले उसके नोटिस को रद्द कर दिया गया था।
- पीसीबी का अधिकार: सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की कि पीसीबी धारा 33ए (जल अधिनियम, 1974) और 31ए (वायु अधिनियम, 1981) के तहत प्रदूषित वायु और जल की बहाली के लिए प्रतिपूरक क्षतिपूर्ति लगा सकते हैं और वसूल सकते हैं।
- न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि मुआवजे का निर्धारण अधीनस्थ कानून के तहत किया जाना चाहिए, जिसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित किया जाए।
- न्यायिक उदाहरण: इस निर्णय में वेल्लोर नागरिक कल्याण फोरम (1996) जैसे ऐतिहासिक मामलों का संदर्भ दिया गया, जिसमें यह स्थापित किया गया कि पर्यावरणीय पुनर्स्थापन एक संवैधानिक दायित्व है।
- प्रदूषक भुगतान सिद्धांत: यह सिद्धांत तब लागू होता है जब पर्यावरणीय सीमाओं का उल्लंघन होता है, और तब भी जब संभावित जोखिमों की पहचान की जाती है।
सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से पीसीबी की शक्तियों का व्यापक विस्तार हुआ है, जिससे वे पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर सकेंगे। यह निर्णय मौजूदा जलवायु संकट के मद्देनजर पर्यावरण संरक्षण के महत्व को रेखांकित करता है, और पीसीबी के कर्तव्यों को राज्य के संवैधानिक दायित्वों से जोड़ता है। न्यायालय ने कहा कि केवल निषेधाज्ञा जारी करना पर्याप्त नहीं है; पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रभावी उपचारात्मक उपाय आवश्यक हैं।
जीएस2/शासन
राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक

चर्चा में क्यों?
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने हाल ही में एक वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक (श्रेष्ठ) का शुभारंभ किया। यह पहल भारत के विभिन्न राज्यों में दवाओं के विनियमन को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
चाबी छीनना
- SHRESTH एक अग्रणी राष्ट्रीय पहल है जिसका उद्देश्य राज्य औषधि नियामक प्रणालियों को मानकीकृत करना और उनमें सुधार करना है।
- यह पहल केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) द्वारा पूरे भारत में दवाओं की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए संचालित की गई है।
- सूचकांक में विनिर्माण राज्यों के लिए 27 तथा प्राथमिक वितरण राज्यों के लिए 23 मापदण्ड शामिल हैं।
- डेटा प्रस्तुतीकरण और स्कोरिंग मासिक आधार पर होगी, जिससे निरंतर मूल्यांकन और सुधार में सुविधा होगी।
अतिरिक्त विवरण
- डेटा प्रस्तुत करना: राज्यों को प्रत्येक माह की 25 तारीख तक पूर्वनिर्धारित मेट्रिक्स के आधार पर अपना प्रदर्शन डेटा सीडीएससीओ को प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिसका मूल्यांकन और साझाकरण अगले माह की पहली तारीख तक किया जाएगा।
- महत्व: यह सूचकांक मानव संसाधन, बुनियादी ढांचे और प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण में सुधार के लिए विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करेगा, जिससे अंततः यह सुनिश्चित होगा कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सभी नागरिकों के लिए दवा सुरक्षा बनाए रखी जाए।
निष्कर्षतः, SHRESTH पहल राज्यों के लिए उनके विनियामक प्रदर्शन का आकलन करने तथा औषधि सुरक्षा और प्रभावकारिता में उच्चतर मानकों को प्राप्त करने की दिशा में काम करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करती है।
जीएस2/राजनीति
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए)

चर्चा में क्यों?
भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) में दो नए सदस्यों को नामित किया है तथा तीन मौजूदा सदस्यों को अतिरिक्त तीन वर्षों के लिए पुनः नामित किया है।
चाबी छीनना
- एनडीएमए भारत में आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च निकाय है।
- इसकी स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत की गई थी।
- प्रधानमंत्री एनडीएमए के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
अतिरिक्त विवरण
- स्थापना: एनडीएमए का गठन आपदा प्रबंधन नीतियों की देखरेख के लिए किया गया था और इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री हैं।
- उद्देश्य: एनडीएमए को प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय नीतियां, योजनाएं और दिशानिर्देश बनाने तथा विभिन्न मंत्रालयों और एजेंसियों में उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है।
- विजन: एनडीएमए का विजन सभी हितधारकों को शामिल करते हुए सक्रिय और टिकाऊ रणनीतियों के माध्यम से एक सुरक्षित और आपदा-प्रतिरोधी भारत का निर्माण करना है।
- संगठनात्मक संरचना: एनडीएमए में कैबिनेट मंत्री स्तर का एक उपाध्यक्ष और राज्य मंत्री स्तर के आठ सदस्य शामिल होते हैं। यह नीति एवं योजना, शमन और संचालन जैसे विशिष्ट प्रभागों के माध्यम से कार्य करता है।
- कार्य और जिम्मेदारियां: एनडीएमए नीतियां बनाने, आपदा प्रबंधन योजनाओं को मंजूरी देने, कार्यान्वयन का समन्वय करने तथा वित्त पोषण और क्षमता निर्माण के लिए सिफारिशें प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।
निष्कर्षतः, एनडीएमए देश की आपदाओं के प्रति तैयारी और प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने तथा राष्ट्रीय और स्थानीय दोनों स्तरों पर लचीलापन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
जीएस2/शासन
भारत की प्रवेश परीक्षा प्रणाली को शुद्ध करना
चर्चा में क्यों?
भारत में प्रवेश परीक्षा प्रणाली अत्यधिक तनाव और प्रतिस्पर्धा का स्रोत बन गई है, जहाँ प्रतिवर्ष लगभग 70 लाख छात्र सीमित स्नातक सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। वर्तमान मॉडल न केवल एक विशाल कोचिंग उद्योग को बढ़ावा देता है, बल्कि वित्तीय शोषण, मानसिक स्वास्थ्य संकट और दुखद छात्र आत्महत्याओं जैसी गंभीर समस्याओं को भी जन्म देता है। यह स्थिति निष्पक्षता और छात्र कल्याण को प्राथमिकता देने के लिए प्रवेश प्रक्रिया की पुनर्व्याख्या की आवश्यकता को बल देती है।
चाबी छीनना
- प्रवेश परीक्षा प्रणाली अति-प्रतिस्पर्धा की संस्कृति को बढ़ावा देती है।
- कोचिंग सेंटर अत्यधिक फीस वसूल कर परिवारों पर वित्तीय बोझ डालते हैं।
- छात्रों पर मानसिक स्वास्थ्य के प्रभाव को लेकर चिंता बढ़ रही है।
- वर्तमान प्रवेश में प्रायः समान रूप से सक्षम ग्रामीण छात्रों की अपेक्षा संपन्न छात्रों को प्राथमिकता दी जाती है।
अतिरिक्त विवरण
- कोचिंग संकट: कोचिंग उद्योग एक गंभीर समस्या बन गया है, जहाँ दो साल की फीस ₹6-7 लाख तक पहुँच जाती है। 14 साल की उम्र के छात्रों पर भी भारी शैक्षणिक दबाव पड़ता है, जिससे तनाव और सामाजिक अलगाव की स्थिति पैदा होती है।
- योग्यतावाद का भ्रम: यह विश्वास कि सफलता केवल व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित है, विशेषाधिकार और संसाधनों के लाभों की अनदेखी करता है, जिससे एक विषम प्रतिस्पर्धी परिदृश्य का निर्माण होता है।
- वैश्विक मॉडल: नीदरलैंड और चीन जैसे देशों ने शिक्षा में पहुंच और समानता को संतुलित करने के लिए भारित लॉटरी और निजी ट्यूशन में कमी जैसे सुधार लागू किए हैं।
- प्रस्तावित सुधार: कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं के आधार पर प्रवेश को सरल बनाना और लॉटरी प्रणाली लागू करना एक अधिक न्यायसंगत दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है। इसके अतिरिक्त, वंचित छात्रों के लिए आरक्षण नीतियों को एकीकृत करने से सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिल सकता है।
अंततः, भारत के सामने एक विकल्प है: अपने युवाओं को नुकसान पहुँचाने वाली ज़हरीली दौड़ जारी रखें या फिर समानता और कल्याण को बढ़ावा देने वाली एक अधिक न्यायसंगत व्यवस्था अपनाएँ। लॉटरी-आधारित प्रवेश प्रक्रिया अपनाने से छात्रों पर दबाव कम हो सकता है, जिससे सभी योग्य उम्मीदवारों के लिए उच्च शिक्षा सुलभ हो सकती है और साथ ही सीखने और विकास के लिए अनुकूल वातावरण भी विकसित हो सकता है।
जीएस2/शासन
शिक्षा प्लस के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (UDISE+)
चर्चा में क्यों?
शिक्षा मंत्रालय ने शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए शिक्षा प्लस के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई+) पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें बताया गया है कि 2024-25 तक भारत में शिक्षकों की कुल संख्या 1 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है।
चाबी छीनना
- यूडीआईएसई+ शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली है।
- यह स्कूलों के लिए आवश्यक डेटा रिकॉर्ड करने और प्रस्तुत करने हेतु एक केंद्रीय मंच के रूप में कार्य करता है।
- भारत भर के सभी मान्यता प्राप्त स्कूल वास्तविक समय डेटा प्रविष्टि में भाग लेते हैं।
अतिरिक्त विवरण
- विशिष्ट यूडीआईएसई कोड: डेटा प्रविष्टि और संशोधन की सुविधा के लिए प्रत्येक स्कूल को एक विशिष्ट 11-अंकीय यूडीआईएसई कोड दिया जाता है।
- स्कूल उपयोगकर्ता निर्देशिका मॉड्यूल: यह मॉड्यूल स्कूलों और नामित उपयोगकर्ताओं की ऑनबोर्डिंग का प्रबंधन करता है जो UDISE+ पर डेटा प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार हैं।
- डेटा रिपोर्टिंग मॉड्यूल:जानकारी को तीन मॉड्यूल में वर्गीकृत किया गया है:
- स्कूल प्रोफ़ाइल और सुविधाएं: यह मॉड्यूल स्कूलों में बुनियादी ढांचे का विवरण और उपलब्ध सेवाओं को रिकॉर्ड करता है।
- छात्र मॉड्यूल: यह प्रत्येक छात्र के लिए एक सामान्य और शैक्षणिक प्रोफ़ाइल बनाए रखता है, जिसमें पाठ्येतर गतिविधियाँ भी शामिल हैं, जिसे स्थायी शिक्षा संख्या का उपयोग करके ट्रैक किया जाता है।
- शिक्षक प्रोफाइल: यह मॉड्यूल सभी शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों का व्यक्तिगत रिकॉर्ड रखता है, तथा उनके सामान्य, शैक्षणिक और नियुक्ति विवरणों का दस्तावेजीकरण करता है।
यूडीआईएसई+ प्रणाली भारत में शैक्षिक डेटा प्रबंधन की दक्षता को बढ़ाती है, तथा यह सुनिश्चित करती है कि स्कूलों, छात्रों और शिक्षकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को सटीक रूप से दर्ज किया जाए और विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर उसकी निगरानी की जाए।
जीएस2/राजनीति
मेरिट योजना
स्रोत: द हिंदू
चर्चा में क्यों?
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में 'तकनीकी शिक्षा में बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान सुधार' (मेरिटे) योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना है।
चाबी छीनना
- मेरिट योजना एक 'केन्द्रीय क्षेत्र योजना' है, जो सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में सरकारी इंजीनियरिंग संस्थानों और पॉलिटेक्निकों को लक्षित करती है।
- इसे तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता, समानता और प्रशासन में सुधार के लिए विश्व बैंक के सहयोग से विकसित किया गया है।
- 2025-26 से 2029-30 की अवधि के लिए कुल 4200 करोड़ रुपये का वित्तपोषण आवंटित किया गया है, जिसमें से 2100 करोड़ रुपये विश्व बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त किए जाएंगे।
- कार्यान्वयन में आईआईटी और आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ-साथ एआईसीटीई और एनबीए जैसी नियामक संस्थाओं की भागीदारी भी शामिल होगी।
अतिरिक्त विवरण
- उद्देश्य: राष्ट्रीय शैक्षिक नीति-2020 (एनईपी-2020) के अनुरूप तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता, समानता और शासन को बढ़ाना।
- वित्तपोषण संरचना: इस योजना में केन्द्रीय नोडल एजेंसी के माध्यम से भाग लेने वाली संस्थाओं को केन्द्र सरकार से धन हस्तांतरण का प्रावधान शामिल है।
- प्रमुख हस्तक्षेप:
- इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना।
- उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम को अद्यतन करना।
- संकाय विकास कार्यक्रमों का आयोजन करना।
- अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना करना।
- इन्क्यूबेशन और नवाचार केंद्रों, कौशल प्रयोगशालाओं और भाषा कार्यशालाओं को समर्थन प्रदान करना।
- अनुमानतः 275 सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त तकनीकी संस्थानों को सहायता के लिए चुना जाएगा, जिनमें राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), राज्य इंजीनियरिंग संस्थान, पॉलिटेक्निक और संबद्ध तकनीकी विश्वविद्यालय (एटीयू) शामिल हैं।
- यह योजना तकनीकी शिक्षा क्षेत्र का प्रबंधन करने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विभागों को भी सहायता प्रदान करेगी।
मेरिट योजना एक व्यापक दृष्टिकोण के माध्यम से छात्रों की रोजगार क्षमता में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो कौशल संवर्धन और उद्योग संरेखण पर केंद्रित है।
जीएस2/राजनीति
एससी/एसटी छात्रवृत्तियों का विस्तार
समाचार में क्यों?
लाभार्थियों की संख्या में गिरावट के बीच, केंद्र सरकार इन महत्वपूर्ण वित्तीय योजनाओं तक पहुंच को व्यापक बनाने के लिए वित्त वर्ष 2026-27 से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति के लिए माता-पिता की आय सीमा में वृद्धि पर विचार कर रही है।
चाबी छीनना
- सरकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति के लिए पात्रता मानदंड में महत्वपूर्ण संशोधन पर विचार कर रही है।
- प्रस्तावित परिवर्तनों में सुगम्यता बढ़ाने के लिए माता-पिता की आय सीमा बढ़ाना शामिल है।
- इन छात्रवृत्ति कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट आई है।
अतिरिक्त विवरण
- एससी/एसटी छात्रवृत्तियों के बारे में: ये छात्रवृत्तियाँ केंद्र प्रायोजित योजनाएँ हैं जिन्हें केंद्र और राज्य सरकारों से 60:40 के अनुपात (पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10) में संयुक्त रूप से वित्त पोषण प्राप्त होता है। इनका उद्देश्य हाशिए पर पड़े समुदायों के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- छात्रवृत्ति के प्रकार:
- प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति: कक्षा IX और X के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है, तथा कक्षा I से X तक के अनुसूचित जातियों के लिए विशेष प्रावधान है, यदि उनके माता-पिता "अस्वच्छ या खतरनाक" व्यवसायों में लगे हुए हैं।
- पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति: दसवीं कक्षा से आगे की शिक्षा को समर्थन देने के लिए डिज़ाइन की गई।
- वर्तमान पात्रता: माता-पिता की वार्षिक आय सीमा 2.5 लाख रुपये है।
- प्रस्तावित संशोधन:
- अनुसूचित जनजातियों के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्तियों के लिए आय सीमा को बढ़ाकर 4.5 लाख रुपये करने पर विचार कर रहा है।
- अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और विमुक्त जनजातियों के लिए भी इसी प्रकार की चर्चा चल रही है, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा को दोगुना करने का सुझाव दिया गया है।
- बजटीय आवंटन:
- वित्त वर्ष 2025-26 के लिए, एससी, ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए छात्रवृत्ति सामाजिक न्याय मंत्रालय के 13,611 करोड़ रुपये के बजट का 66.7% है।
- अनुसूचित जनजातियों के लिए छात्रवृत्ति, जनजातीय मामलों के मंत्रालय के 14,925.81 करोड़ रुपये के आवंटन का 18.6% है।
- लाभार्थियों की घटती प्रवृत्तियाँ:
- 2020-21 से 2024-25 तक अनुसूचित जाति के प्री-मैट्रिक लाभार्थियों की संख्या में 30.63% की कमी आई, जबकि पोस्ट-मैट्रिक लाभार्थियों की संख्या में 4.22% की गिरावट आई।
- ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी में 2021-22 में 58.62 लाख प्री-मैट्रिक लाभार्थियों से 2023-24 में 20.25 लाख तक की गिरावट देखी गई।
- संसदीय समितियों की सिफारिशें:
- ओबीसी कल्याण समिति ने ओबीसी छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा को दोगुना करने तथा प्री-मैट्रिक कवरेज को कक्षा 5 से शुरू करने का सुझाव दिया।
- जनजातीय मामलों पर गठित पैनल ने अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा को संशोधित करने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि अधिक जरूरतमंद परिवारों को इसमें शामिल किया जा सके।
- सामाजिक-आर्थिक प्रभाव:माता-पिता की आय सीमा बढ़ाने से:
- कवरेज का विस्तार करके इसमें निम्न-मध्यम आय वाले परिवारों को शामिल किया जाना चाहिए।
- निरंतर शिक्षा को सक्षम बनाकर स्कूल छोड़ने की दर को कम करना।
- शैक्षिक असमानता को दूर करना तथा प्रतिस्पर्धी करियर तक पहुंच प्रदान करना।
यदि स्वीकृत हो जाती है, तो नई आय सीमाएँ वित्त वर्ष 2026-27 में लागू होंगी, जिससे एक नए पंचवर्षीय वित्तीय नियोजन चक्र की शुरुआत होगी। सरकार के सामने यह सुनिश्चित करने की चुनौती है कि ये छात्रवृत्तियाँ समावेशी और वित्तीय रूप से टिकाऊ हों, साथ ही संसाधनों के दुरुपयोग को भी रोकें।
जीएस2/शासन
आयुर्वेद आहार क्या है?
चर्चा में क्यों?
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) और आयुष मंत्रालय ने हाल ही में आयुर्वेद आहार के अंतर्गत वर्गीकृत खाद्य पदार्थों की एक आधिकारिक सूची प्रकाशित की है, जिसका उद्देश्य प्राचीन भारतीय आहार प्रथाओं को समकालीन पोषण मानकों के साथ सामंजस्य स्थापित करना है।
चाबी छीनना
- आयुर्वेद आहार उन खाद्य उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करता है जो आयुर्वेदिक आहार सिद्धांतों का पालन करते हैं, संतुलन, मौसमी और प्राकृतिक अवयवों को बढ़ावा देते हैं।
- इस पहल का उद्देश्य आयुर्वेदिक खाद्य पद्धतियों को मानकीकृत करना, सुरक्षा सुनिश्चित करना और उपभोक्ता विश्वास को बढ़ावा देना है।
अतिरिक्त विवरण
- परिभाषा: आयुर्वेद आहार से तात्पर्य ऐसे खाद्य उत्पादों से है जो आयुर्वेदिक आहार सिद्धांतों पर आधारित हैं, तथा पोषण के प्रति समग्र दृष्टिकोण पर जोर देते हैं जिसमें संतुलन और ऋतुगतता शामिल है।
- उद्देश्य: प्राथमिक लक्ष्य आयुर्वेदिक आहार प्रथाओं का मानकीकरण, सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है।
- कानूनी ढांचा: इन खाद्य पदार्थों को एफएसएसएआई द्वारा स्थापित आयुर्वेद आहार विनियम (2022) के तहत विनियमित किया जाता है।
- पाठ्य आधार: उत्पाद सूची शास्त्रीय आयुर्वेदिक ग्रंथों से ली गई है और इसमें पारंपरिक व्यंजनों और तैयारी विधियों का पालन किया जाना चाहिए।
- नये उत्पाद का समावेश: खाद्य व्यवसाय संचालक (एफबीओ) आयुर्वेद के आधिकारिक स्रोतों का हवाला देकर नये उत्पादों का प्रस्ताव कर सकते हैं।
- संस्थागत समर्थन: इस पहल को राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का समर्थन प्राप्त है, तथा आयुष आहार संग्रह उद्योग के लिए वैज्ञानिक रूप से मान्य सूत्रीकरण प्रदान करता है।
- महत्व: आयुर्वेद आहार निवारक स्वास्थ्य, पाचन और प्रतिरक्षा का समर्थन करता है, साथ ही प्राचीन खाद्य परंपराओं से जुड़ी भारत की सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करता है।
संक्षेप में, आयुर्वेद आहार पारंपरिक भारतीय आहार को आधुनिक पोषण के साथ एकीकृत करने, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
जीएस2/राजनीति
भारत की स्वदेशी लोकतांत्रिक परंपराएँ - चोल-युग की चुनावी विरासत का पुनरावलोकन

चर्चा में क्यों?
27 जुलाई, 2025 को गंगईकोंडा चोलपुरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में भारत की स्वदेशी लोकतांत्रिक परंपराओं पर ज़ोर दिया गया, जो मैग्ना कार्टा से भी पहले की हैं। यह लेख प्राचीन चुनावी प्रथाओं, विशेष रूप से चोल वंश के अधीन, पर पुनर्विचार करता है और आज के लोकतांत्रिक विमर्श में उनके महत्व पर प्रकाश डालता है।
चाबी छीनना
- भारत की लोकतांत्रिक प्रथाओं की गहरी ऐतिहासिक जड़ें हैं, न कि केवल औपनिवेशिक प्रभाव।
- चोल युग की चुनावी प्रणाली स्वशासन के प्रारंभिक स्वरूप का उदाहरण है।
- कुदावोलाई प्रणाली पारदर्शिता और निष्पक्षता पर जोर देते हुए चुनावों के प्रति एक प्राचीन दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है।
अतिरिक्त विवरण
- वैशाली: 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक प्रारंभिक गणराज्य, जिसमें सहभागी शासन का प्रदर्शन किया गया।
- कौटिल्य का अर्थशास्त्र: स्थानीय शासन संरचनाओं का उल्लेख करता है जिन्हें संघ के रूप में जाना जाता है, जो स्वशासन की दीर्घकालिक परंपरा का संकेत देता है।
- उथिरामेरुर शिलालेख: ये शिलालेख 920 ईस्वी में परांतक चोल के शासनकाल के दौरान स्थापित एक परिष्कृत चुनावी ढांचे का विवरण देते हैं, जिसमें शामिल हैं:
- वार्ड संविधान
- पात्रता और अयोग्यता मानदंड
- समिति का गठन और कार्य
- निर्वाचित सदस्यों को वापस बुलाने का अधिकार
- कुदावोलाई प्रणाली: एक अनोखी चुनावी प्रक्रिया जिसमें उम्मीदवारों के नाम एक बर्तन से निकाले जाते हैं, जिससे निष्पक्षता सुनिश्चित होती है।
- सख्त मानक: चुनावी प्रणाली में उच्च नैतिक और प्रशासनिक मानकों को लागू किया गया, जिनमें शामिल हैं:
- उम्मीदवारों के लिए आयु संबंधी आवश्यकताएं और संपत्ति स्वामित्व
- ऋण चूककर्ताओं और नैतिक रूप से कलंकित व्यक्तियों के लिए अयोग्यता
निष्कर्षतः, भारत की लोकतांत्रिक परंपराएँ उसके सभ्यतागत इतिहास में गहराई से निहित हैं, जैसा कि चोल-युग की प्रथाओं से स्पष्ट है। समकालीन समय में एक अधिक नैतिक, सहभागी और उत्तरदायी राजनीतिक परिदृश्य को बढ़ावा देने के लिए इस विरासत को पहचानना और पुनः प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है।
जीएस2/राजनीति
कार्बन उत्सर्जन व्यापार व्यवस्था को सक्षम करने के लिए राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण (एनडीए)
चर्चा में क्यों?
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में 2015 पेरिस समझौते के प्रावधानों के अनुसार कार्बन उत्सर्जन व्यापार व्यवस्था को लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में एक राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण (एनडीए) की स्थापना की है।
चाबी छीनना
- पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के अंतर्गत एनडीए एक अनिवार्य आवश्यकता है।
- अनुच्छेद 6 कार्बन बाज़ार और उत्सर्जन व्यापार की रूपरेखा को रेखांकित करता है।
- एनडीए में पर्यावरण मंत्रालय के सचिव के नेतृत्व में 21 सदस्यीय समिति शामिल होगी।
- इसमें विदेश मंत्रालय, इस्पात और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल हैं।
- एनडीए की प्रमुख जिम्मेदारियों में उत्सर्जन न्यूनीकरण व्यापार के लिए परियोजनाओं का मूल्यांकन करना शामिल है।
अतिरिक्त विवरण
- अनुच्छेद 6: यह अनुच्छेद, बाकू, अज़रबैजान में COP29 के दौरान पारित किया गया, यह परिभाषित करता है कि देशों के बीच कार्बन बाज़ार कैसे स्थापित और संचालित किए जा सकते हैं।
- एनडीए की जिम्मेदारियां:
- उत्सर्जन में कमी लाने वाली इकाई व्यापार के लिए गतिविधियों की सिफारिश करना।
- इन गतिविधियों को राष्ट्रीय सतत लक्ष्यों के अनुरूप संशोधित करें।
- उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से परियोजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन करना।
- राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी):उत्सर्जन कम करने के लिए भारत की प्रतिबद्धताओं में शामिल हैं:
- 2005 के स्तर से 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी।
- यह सुनिश्चित करना कि 2030 तक 50% विद्युत ऊर्जा क्षमता गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त हो।
- वनरोपण के माध्यम से 2030 तक 2.5-3 बिलियन टन CO2 के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण करना।
एनडीए की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करने और एक संरचित कार्बन व्यापार बाजार को सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
जीएस2/राजनीति
चौराहे पर सहकारी समितियाँ
चर्चा में क्यों?
राष्ट्रीय सहकारी नीति, 2025 ने केंद्र और राज्य के बीच एक गंभीर टकराव को जन्म दिया है, जिसमें केरल सबसे आगे है। यह विवाद केवल नीतिगत असहमति से आगे बढ़कर सहकारी संघवाद के गहरे मुद्दों को उजागर करता है, जिसमें संवैधानिक अधिकार, राजनीतिक निहितार्थ और लगभग ₹3 लाख करोड़ की जमा राशि के बड़े वित्तीय दांव शामिल हैं।
चाबी छीनना
- केरल ने राष्ट्रीय सहकारी नीति को असंवैधानिक करार देते हुए दावा किया है कि यह सहकारी प्रशासन पर राज्य के विशेष अधिकारों का उल्लंघन करती है।
- वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार ने भाजपा पर राजनीतिक लाभ के लिए केरल के सहकारी परिदृश्य पर नियंत्रण पाने का प्रयास करने का आरोप लगाया है।
- केरल में सहकारी समितियां लगभग 2.94 लाख करोड़ रुपये की जमा राशि का प्रबंधन करती हैं , जो स्थानीय अर्थव्यवस्था में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।
अतिरिक्त विवरण
- संघवाद दांव पर: सहकारी समितियों को संविधान में राज्य सूची के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है, फिर भी केंद्र बहु-राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) अधिनियम, 2023 के दौरान उठाए गए मुद्दों की याद दिलाते हुए प्रभाव डालने का प्रयास कर रहा है ।
- ऐतिहासिक संदर्भ: केरल की सहकारी संस्थाएं 20वीं सदी के आरंभ से चली आ रही हैं और केरल सहकारी समिति अधिनियम, 1969 के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक ढांचे का अभिन्न अंग रही हैं ।
- जमीनी स्तर पर महत्व: प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां (पीएसीएस) केरल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए आधारभूत हैं, जो महत्वपूर्ण ऋण स्रोत के रूप में कार्य करती हैं।
- राजनीतिक विरोध: राज्य के सहकारिता मंत्री वी.एन. वासवन ने इस नीति की निंदा करते हुए इसे सहकारी क्षेत्र के लिए हानिकारक बताया है।
- संगठित प्रतिरोध: केरल प्राथमिक कृषि सहकारी समिति एसोसिएशन ने औपचारिक रूप से इस नीति का विरोध किया है, जो व्यापक असंतोष को दर्शाता है।
- श्रमिकों की चिंताएं: केरल सहकारी कर्मचारी संघ (केसीईयू) ने आशंका व्यक्त की है कि केंद्र सरकार सहकारी समितियों का नियंत्रण कॉर्पोरेट संस्थाओं को हस्तांतरित करना चाहती है।
- केरल में सहकारी क्षेत्र विभिन्न गबन घोटालों, विशेष रूप से करुवन्नूर सेवा सहकारी बैंक घोटाले , के कारण विश्वसनीयता के संकट से जूझ रहा है , जिसने जनता का विश्वास हिला दिया है और राज्य सरकार को सवालों के घेरे में ला दिया है। इसके जवाब में, केरल ने इन मुद्दों के समाधान और नियामक सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए 2023 में अपने सहकारी समिति अधिनियम में संशोधन किया है।
- संरचनात्मक सुधार की दिशा में कदम बढ़ाते हुए, केरल ने अपने जिला सहकारी बैंकों को केरल राज्य सहकारी बैंक में समेकित कर दिया है, जिससे पारंपरिक तीन-स्तरीय ऋण संरचना से अधिक सुव्यवस्थित दो-स्तरीय प्रणाली में परिवर्तन हो रहा है, जिसका उद्देश्य दक्षता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करना है।
- भविष्य की ओर देखते हुए, केरल की सहकारी समितियाँ एक नए मोड़ पर खड़ी हैं, जहाँ उन्हें तीव्र शहरीकरण और युवाओं की उभरती आकांक्षाओं के साथ-साथ ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्षेत्रीय बदलावों का सामना करना पड़ रहा है। आने वाले दशकों में आर्थिक लचीलापन बनाए रखने के लिए उनकी अनुकूलन क्षमता अत्यंत महत्वपूर्ण होगी।
- निष्कर्षतः, केरल का सहकारी आंदोलन, जो ग्रामीण ऋण और जमीनी स्तर पर सशक्तिकरण का ऐतिहासिक रूप से अनिवार्य घटक रहा है, एक निर्णायक मोड़ पर है। राष्ट्रीय सहकारी नीति, 2025, जिसे एक सुधारवादी पहल के रूप में तैयार किया गया है, ने भारत के संघीय ढांचे की गंभीर खामियों को उजागर किया है, जिससे केंद्र और राज्य के बीच तनाव और बढ़ गया है। केरल को आधुनिकीकरण और पारदर्शिता को अपनाते हुए अपनी समृद्ध सहकारी विरासत को आगे बढ़ाना होगा, और केंद्र को सहकारी मॉडल में विश्वास बनाए रखने के लिए संवैधानिक सीमाओं का सम्मान करना होगा।
जीएस2/राजनीति
बीसीसीआई के ऐतिहासिक आरटीआई प्रतिरोध के बीच खेल संचालन विधेयक की बाधा दूर
 चर्चा में क्यों?
चर्चा में क्यों?
लोकसभा में पारित होने के बाद, राज्यसभा ने हाल ही में राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025 को पारित कर दिया है। इस विधायी घटनाक्रम ने, विशेष रूप से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के संबंध में, एक महत्वपूर्ण बहस छेड़ दी है, जिसने ऐतिहासिक रूप से सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत पारदर्शिता उपायों का विरोध किया है।
चाबी छीनना
- राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय खेल निकायों को विनियमित करना तथा पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है।
- बीसीसीआई को आरटीआई दायित्वों से छूट प्राप्त है, क्योंकि उसे सरकार से प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता नहीं मिलती है।
- विपक्षी दलों ने इस विधेयक की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें खेल प्रशासन को अत्यधिक केंद्रीकृत किया गया है तथा बीसीसीआई को लाभ पहुंचाया गया है।
अतिरिक्त विवरण
- बीसीसीआई को आरटीआई से छूट: विधेयक आरटीआई अधिनियम के तहत "सार्वजनिक प्राधिकरण" की परिभाषा केवल उन खेल संस्थाओं के लिए करता है जो सरकार से प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्राप्त करती हैं। परिणामस्वरूप, बीसीसीआई, जिसे ऐसी कोई धनराशि नहीं मिलती, आरटीआई आवश्यकताओं से बाहर रखा गया है।
- बीसीसीआई का रुख: बीसीसीआई का कहना है कि वह एक निजी, स्वायत्त संगठन है जो आरटीआई अधिनियम के तहत "सार्वजनिक प्राधिकरण" के रूप में योग्य नहीं है, तथा इसके लिए वह तमिलनाडु सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1975 के तहत अपने पंजीकरण का हवाला देता है।
- न्यायिक सिफारिशें: भारतीय विधि आयोग और सर्वोच्च न्यायालय सहित विभिन्न न्यायिक और अर्ध-न्यायिक निकायों ने, इसके महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्यों का हवाला देते हुए, बीसीसीआई को सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में वर्गीकृत करने की सिफारिश की है।
- आरटीआई समावेशन के निहितार्थ: यदि इसे आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया जाता है, तो नागरिक बीसीसीआई के संचालन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, जैसे कि टीम चयन मानदंड और वित्तीय अनुबंध, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी।
राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक भारत में खेल निकायों को विनियमित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना है, साथ ही बीसीसीआई के संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही के बारे में चल रही चिंताओं का समाधान करना है।
|
5 videos|3453 docs|1080 tests
|
FAQs on Indian Polity and Governance (भारतीय राजनीति और शासन): August 2025 UPSC Current Affairs - Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly
| 1. संविधान (130वां संशोधन) विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है? |  |
| 2. मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) का कार्य क्या होता है? |  |
| 3. मतदाता सूची संशोधन में सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप क्यों महत्वपूर्ण है? |  |
| 4. न्यायालय मतों की पुनर्गणना का आदेश कब दे सकता है? |  |
| 5. अनुच्छेद 370 का निरस्तीकरण जम्मू और कश्मीर में क्या परिवर्तन लाया है? |  |
















