Indian Polity and Governance (भारतीय राजनीति और शासन): September 2025 UPSC Current Affairs | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly PDF Download
शरणार्थियों के लिए राहत: आव्रजन और विदेशी (छूट) आदेश, 2025

चर्चा में क्यों?
आव्रजन एवं विदेशी (छूट) आदेश, 2025 के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी अधिसूचना ने भारत की विकसित होती शरणार्थी नीति, विशेष रूप से श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों के संबंध में, की ओर ध्यान आकर्षित किया है। यह आदेश कुछ समूहों को पासपोर्ट और वीज़ा आवश्यकताओं से छूट देता है, जिससे 1990 के दशक से तमिलनाडु में रह रहे लोगों को जबरन प्रत्यावर्तन से महत्वपूर्ण सुरक्षा मिलती है। हालाँकि, यह उनकी कानूनी स्थिति, नागरिकता अधिकारों और दीर्घकालिक पुनर्वास के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है।
चाबी छीनना
- 2025 का आदेश शरणार्थी नीति के प्रति भारत के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है।
- श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों को अस्थायी राहत तो दी गई है, लेकिन उन्हें नागरिकता मिलने का स्पष्ट रास्ता नहीं मिल पाया है।
- ऐतिहासिक रूप से, इन शरणार्थियों को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के तहत अन्य समूहों को मिलने वाले लाभों से वंचित रखा गया है।
अतिरिक्त विवरण
- छूट प्रदान की गई: यह आदेश नेपाल और भूटान के नागरिकों, तिब्बती शरणार्थियों, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के छह धार्मिक अल्पसंख्यकों और श्रीलंकाई तमिलों को सख्त पासपोर्ट और वीजा नियमों से बचने की अनुमति देता है।
- ऐतिहासिक संदर्भ: अर्हता प्राप्त करने के लिए शरणार्थियों को 9 जनवरी, 2015 से पहले भारत में प्रवेश करना होगा तथा अपना पंजीकरण कराना होगा।
- जबरन वापसी से संरक्षण: यह आदेश विशेष रूप से श्रीलंकाई तमिलों को भारत में दशकों तक रहने के बाद अनैच्छिक प्रत्यावर्तन से बचाता है, जो एक प्रमुख मानवीय चिंता का समाधान है।
- गृहयुद्ध विस्थापन: इनमें से कई शरणार्थी 1990 के दशक में श्रीलंकाई गृहयुद्ध के दौरान तमिलनाडु भाग गए थे और तब से सरकारी सहायता पर निर्भर हैं।
- कानूनी बाधाएं: छूट के बावजूद, शरणार्थियों को "अवैध प्रवासी" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिससे उनकी नागरिकता प्राप्त करने और महत्वपूर्ण सेवाओं तक पहुंच में बाधा उत्पन्न होती है।
- भावी नीतिगत विकल्प: संभावित समाधानों में दीर्घकालिक वीज़ा को उदार बनाना, स्वैच्छिक प्रत्यावर्तन को सुविधाजनक बनाना, तथा वापस लौटने के अनिच्छुक लोगों के लिए स्थानीय एकीकरण की संभावना तलाशना शामिल है।
- 2025 का आव्रजन आदेश एक प्रगतिशील कदम है, फिर भी यह भारत में श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों के भविष्य को लेकर कई गंभीर प्रश्न खड़े करता है। भारत की शरणार्थी नीति में स्थिरता और करुणा को बढ़ावा देने के लिए नागरिकता, सम्मान और दीर्घकालिक समाधानों के मुद्दों पर ध्यान देना आवश्यक है।
आपराधिक मानहानि लोकतांत्रिक बहस के साथ असंगत है
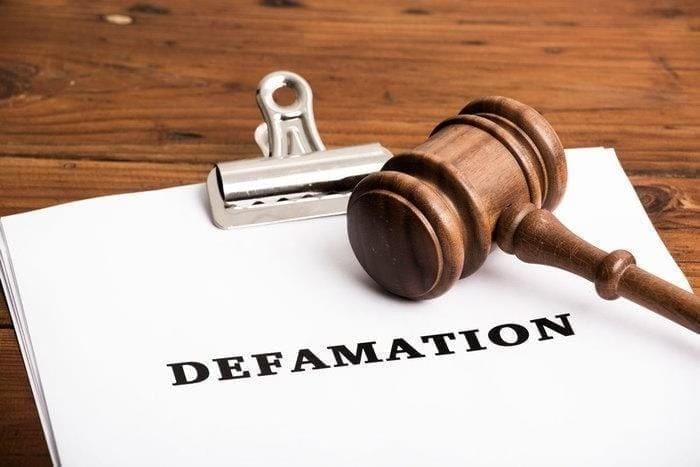
चर्चा में क्यों?
भारत में इसके दुरुपयोग के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के हालिया बयानों के बाद, आपराधिक मानहानि का विषय सार्वजनिक चर्चा में फिर से उभर आया है। शुरुआत में व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए एक सुरक्षात्मक उपाय के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला आपराधिक मानहानि अब धमकी और राजनीतिक प्रतिशोध का एक तंत्र बन गया है, जिससे लोकतांत्रिक संवाद का सार ही खतरे में पड़ गया है।
चाबी छीनना
- आपराधिक मानहानि पर सर्वोच्च न्यायालय के 2016 के फैसले के कारण कानून का दुरुपयोग बढ़ गया है।
- कई राजनीतिक हस्तियां और पत्रकार आपराधिक मानहानि के तहत असंगत मुकदमेबाजी का सामना कर रहे हैं, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा डालता है।
- मानहानि के मामलों में फौजदारी से दीवानी उपचार की ओर संक्रमण हेतु सुधार की मांग बढ़ रही है।
अतिरिक्त विवरण
- वैधानिक परिभाषा: भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के अनुसार, मानहानि में किसी व्यक्ति के बारे में इस आशय या ज्ञान के साथ हानिकारक बयान देना शामिल है कि इससे उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा।
- दंड: धारा 500 के अंतर्गत आपराधिक मानहानि के लिए दंड में दो वर्ष तक का साधारण कारावास, जुर्माना या दोनों शामिल हो सकते हैं।
- दुरुपयोग के मामले: उच्च-स्तरीय उदाहरणों में राजनेताओं द्वारा असहमति को दबाने के लिए मानहानि के दावों का उपयोग करना शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप लंबी कानूनी लड़ाइयां होती हैं जो शासन को प्रभावित करती हैं।
निष्कर्ष
भारत में आपराधिक मानहानि का वर्तमान ढाँचा व्यक्तिगत गरिमा की रक्षा के अपने मूल उद्देश्य से हटकर आलोचनाओं को दबाने का एक साधन बन गया है। इस दुरुपयोग की न्यायिक मान्यता सुधार की तत्काल आवश्यकता को दर्शाती है, और ऐसे नागरिक उपायों को बढ़ावा देती है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए प्रतिष्ठा के अधिकारों की भी रक्षा करें। अब समय आ गया है कि भारत अपनी कानूनी प्रथाओं को वैश्विक लोकतांत्रिक मानकों के अनुरूप ढाले और यह सुनिश्चित करे कि राजनीतिक बहसें मुकदमेबाजी के बजाय खुली और रचनात्मक बनी रहें।
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980
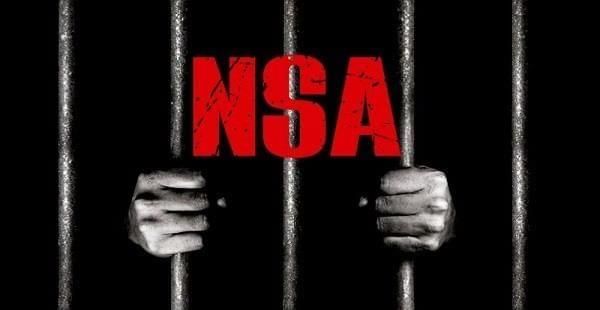
चर्चा में क्यों?
जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को लेह में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत हिरासत में लिया गया है, क्योंकि वह लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा और सुरक्षा की वकालत करते हैं।
चाबी छीनना
- राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 23 सितम्बर 1980 को अधिनियमित किया गया था और यह पूरे भारत में लागू है, पहले यह जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं था।
- यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(3)(बी) और अनुच्छेद 22(4) में निहित है।
अतिरिक्त विवरण
- उद्देश्य: इस अधिनियम का उद्देश्य रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, विदेशी संबंध और आवश्यक आपूर्ति/सेवाओं की रक्षा करना है।
- नजरबंदी के आधार: इसमें भारत की रक्षा के लिए हानिकारक कार्य, विदेशी संबंधों को नुकसान पहुंचाना, सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ना, आवश्यक आपूर्ति को खतरे में डालना और विदेशियों की उपस्थिति को विनियमित करना शामिल है।
- सशक्त प्राधिकारी: केंद्र, राज्य, जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्त (यदि अधिकृत हों) अधिनियम को लागू कर सकते हैं।
- हिरासत की अवधि: किसी व्यक्ति को अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है ; हिरासत के कारणों की सूचना 5 दिनों के भीतर दी जानी चाहिए (जिसे 15 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है)।
- किसी बंदी को आरोपों का खुलासा किये बिना 10 दिनों तक हिरासत में रखा जा सकता है।
- सलाहकार बोर्ड: इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य तीन व्यक्ति होते हैं और यह तीन सप्ताह के भीतर आदेशों की समीक्षा करता है । यदि पर्याप्त कारण नहीं पाया जाता है, तो रिहाई अनिवार्य है।
- ऐतिहासिक संदर्भ: यह औपनिवेशिक युग के कानूनों जैसे बंगाल रेगुलेशन III (1818) , रॉलेट एक्ट (1919) और निवारक निरोध अधिनियम (1950) पर आधारित है , जिसे 1980 में इंदिरा गांधी द्वारा पुनः लागू किया गया था।
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कानूनी प्रतिनिधित्व और न्यायिक उपचार की अनुमति देता है, जिसमें उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिकाएँ दायर करना भी शामिल है। हालाँकि, बंदी सलाहकार बोर्ड के समक्ष कानूनी सलाह नहीं ले सकते, और जन सुरक्षा के हित में बंदी बनाए जाने के आधारों को गुप्त रखा जा सकता है।
सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत हिरासत में लिया गया: कानून के बारे में मुख्य तथ्य

चर्चा में क्यों?
लद्दाख को राज्य का दर्जा दिलाने और छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा प्रदान करने की वकालत करने वाले जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत हिरासत में लेकर जोधपुर जेल भेज दिया गया है। सरकार ने उन पर लेह में हिंसक विरोध प्रदर्शन भड़काने का आरोप लगाया है, जिसके परिणामस्वरूप पुलिस कार्रवाई में चार लोगों की मौत हो गई और 50 अन्य घायल हो गए।
चाबी छीनना
- सोनम वांगचुक की नजरबंदी ने एनएसए और उसके प्रभावों के बारे में चर्चा छेड़ दी है।
- एनएसए भारत के सबसे सख्त निवारक निरोध कानूनों में से एक है, जिसका ऐतिहासिक रूप से विभिन्न समूहों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता रहा है।
अतिरिक्त विवरण
- निवारक निरोध: इस प्रथा में किसी व्यक्ति को पहले से किए गए अपराध के लिए नहीं, बल्कि सार्वजनिक व्यवस्था या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संभावित खतरों को टालने के लिए हिरासत में लिया जाता है। इसका उद्देश्य संभावित नुकसान को घटित होने से पहले ही रोकना है।
- निवारक और दंडात्मक निरोध के बीच अंतर:
- निवारक निरोध: इसका उद्देश्य भविष्य में होने वाली हानिकारक गतिविधियों को रोकना है तथा यह पूर्वानुमानात्मक प्रकृति का है।
- दंडात्मक नजरबंदी: पहले से किए गए अपराध के लिए दोषसिद्धि के बाद, उचित कानूनी प्रक्रिया के बाद सजा के रूप में लागू की जाती है।
- संवैधानिक प्रावधान: भारतीय संविधान अनुच्छेद 22 के तहत निवारक निरोध की अनुमति देता है , जिसके दो भाग हैं। पहला भाग सामान्य कानूनी मामलों से संबंधित है, जबकि दूसरा भाग निवारक निरोध कानूनों से संबंधित है, जो बिना मुकदमे के निरोध की अनुमति देता है।
- सलाहकार बोर्ड की मंज़ूरी के बिना किसी व्यक्ति को तीन महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है, और उससे ज़्यादा समय तक हिरासत में रखने के लिए ऐसी मंज़ूरी ज़रूरी है। हिरासत के कारणों की जानकारी दी जानी चाहिए, हालाँकि जन सुरक्षा के हित में कुछ जानकारियाँ छिपाई जा सकती हैं।
एनएसए की जड़ें औपनिवेशिक काल से जुड़ी हैं और इसे औपचारिक रूप से स्वतंत्रता के बाद 1950 के निवारक निरोध अधिनियम के साथ स्थापित किया गया था। इसे विभिन्न रूपों में संशोधित और अधिनियमित किया गया है, जिसमें 1971 का विवादास्पद आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (मीसा) भी शामिल है, जिसे आपातकाल के बाद निरस्त कर दिया गया था। एनएसए अधिकारियों को भारत की रक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या आवश्यक आपूर्ति के लिए हानिकारक समझी जाने वाली कार्रवाइयों को रोकने के लिए व्यक्तियों को पहले से हिरासत में लेने का अधिकार देता है।
एनएसए क्या प्रदान करता है?
- एनएसए के तहत, हिरासत आदेश गिरफ्तारी वारंट के समान ही कार्य करते हैं, जो प्राधिकारियों को व्यक्तियों को निर्दिष्ट सुविधाओं में रखने और आवश्यकतानुसार उन्हें स्थानांतरित करने की अनुमति देते हैं।
- हिरासत में लिए जाने के कारणों को 5 से 15 दिनों के भीतर साझा किया जाना चाहिए, जिससे बंदियों को सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखने का अवसर मिल सके।
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से गठित एक सलाहकार बोर्ड को तीन हफ़्तों के भीतर मामलों की समीक्षा करनी होगी और अगर हिरासत का कोई पर्याप्त कारण न हो, तो रिहाई का आदेश देना होगा। अधिकतम हिरासत अवधि 12 महीने तक हो सकती है, हालाँकि इसे पहले भी रद्द किया जा सकता है।
- हालाँकि, सुरक्षा उपाय सीमित हैं, क्योंकि सलाहकार बोर्ड के समक्ष बंदियों का कानूनी प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता है, तथा सरकार सार्वजनिक हित का हवाला देते हुए जानकारी को रोक सकती है, जिससे महत्वपूर्ण शक्ति आधिकारिक हाथों में केंद्रित हो जाती है।
- सोनम वांगचुक अपनी एनएसए हिरासत को सरकार को ज्ञापन देकर या सलाहकार बोर्ड की समीक्षा का इंतज़ार करके चुनौती दे सकते हैं। वह अनुच्छेद 226 या 32 के तहत उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का भी सहारा ले सकते हैं। सरकार के पास किसी भी समय हिरासत आदेश को रद्द करने का अधिकार है।
- जब तक कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, एनएसए खुली अदालत में औपचारिक आरोप या साक्ष्य के बिना हिरासत में रखने की अनुमति देता है, जिससे प्राधिकारियों को काफी विवेकाधिकार प्राप्त हो जाता है।
एनएसए के उपयोग का ऐतिहासिक संदर्भ
- एनएसए को उल्लेखनीय मामलों में लागू किया गया है, जिसमें कट्टरपंथी सिख उपदेशक अमृतपाल सिंह की 2023 में हिरासत और 2017 में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद की पिछली हिरासत शामिल है।
- 2020 में सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान, उत्तर प्रदेश में कई व्यक्तियों को इस अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया।
- डॉ. कफील खान जैसे उल्लेखनीय व्यक्तियों की एनएसए के तहत की गई नजरबंदी को न्यायपालिका द्वारा रद्द कर दिया गया है।
- उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने "लव जिहाद", सांप्रदायिक हिंसा, गोहत्या और आदतन अपराध से संबंधित मामलों में एनएसए लागू किया है, जो अक्सर राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा को बढ़ा-चढ़ाकर बताता है।
- आलोचकों का तर्क है कि एनएसए एक कुंद हथियार है जिसका दुरुपयोग होने की संभावना है, जबकि समर्थक राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता पर जोर देते हैं।
- इस कानून के लागू होने पर प्रायः न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ती है, जैसा कि ऐसे मामलों में देखा गया है जहां सर्वोच्च न्यायालय ने अनुचित हिरासत को रद्द कर दिया है।
विदेशी न्यायाधिकरणों की बढ़ी हुई शक्तियाँ

चर्चा में क्यों?
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में आव्रजन और विदेशी अधिनियम, 2025 के तहत नियम, आदेश और छूट आदेश को अधिनियमित किया है। यह व्यापक कानून विभिन्न पुराने कानूनों जैसे पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम, 1939, विदेशी अधिनियम, 1946 और आव्रजन (वाहक दायित्व) अधिनियम, 2000 को प्रतिस्थापित करता है, जिससे विदेशी व्यक्तियों और आव्रजन प्रक्रियाओं के शासन को सुव्यवस्थित किया जाता है।
चाबी छीनना
- नये अधिनियम का उद्देश्य आव्रजन और यात्रा से संबंधित स्वतंत्रता-पूर्व के अनेक कानूनों के कारण उत्पन्न भ्रम को समाप्त करना है।
- यह आव्रजन धोखाधड़ी की जांच करने और एक व्यापक आव्रजन डेटाबेस बनाए रखने के लिए आव्रजन ब्यूरो (बीओआई) के अधिकार को औपचारिक बनाता है।
- विदेशी न्यायाधिकरणों (एफ.टी.) को अब प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेटों के समान न्यायिक शक्तियां प्रदान की गई हैं।
अतिरिक्त विवरण
- जांच शक्तियां: आव्रजन ब्यूरो को आव्रजन धोखाधड़ी की जांच करने और विदेशियों की पहचान करने और उन्हें निर्वासित करने के लिए राज्य प्राधिकारियों के साथ सहयोग करने का अधिकार है।
- बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग: बायोमेट्रिक डेटा संग्रहण अब सभी विदेशियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है, जो पिछली सीमाओं से आगे बढ़ गया है।
- रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ: शैक्षणिक संस्थानों को विदेशी छात्रों की उपस्थिति और आचरण की रिपोर्ट विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) को देनी आवश्यक है।
- परिसर बंद करना: अवैध प्रवासियों द्वारा अक्सर उपयोग किए जाने वाले प्रतिष्ठानों को बंद किया जा सकता है, जिससे अवांछित विदेशियों के विरुद्ध मौजूदा उपायों में वृद्धि होगी।
- विदेशी नागरिक न्यायाधिकरणों की न्यायिक शक्तियां: विदेशी नागरिक न्यायाधिकरण अब गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकते हैं और नागरिकता प्रमाण के बिना व्यक्तियों को हिरासत केंद्रों में भेज सकते हैं, उनके निर्णयों की 30 दिनों के भीतर समीक्षा की जा सकती है।
- विस्तारित प्रवेश अस्वीकृति आधार: राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों, आतंकवाद और मानव तस्करी जैसे मानदंडों के आधार पर प्रवेश से इनकार किया जा सकता है।
- छूट: पंजीकृत श्रीलंकाई तमिल नागरिकों और पड़ोसी देशों के गैर-दस्तावेजी अल्पसंख्यकों सहित कुछ समूहों को विशिष्ट शर्तों के तहत पासपोर्ट और वीज़ा आवश्यकताओं से छूट दी गई है।
इस नए ढांचे का उद्देश्य भारत की आव्रजन नीतियों का आधुनिकीकरण करना, समकालीन चुनौतियों का समाधान करना तथा देश में विदेशी नागरिकों के संबंध में बेहतर विनियमन और प्रवर्तन सुनिश्चित करना है।
ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम, 2025

चर्चा में क्यों?
हाल ही में संसद द्वारा पारित ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन अधिनियम, 2025 का उद्देश्य भारत में ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र के लिए एक व्यापक कानूनी ढाँचा तैयार करना है। यह अधिनियम ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करता है, साथ ही ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं, विज्ञापनों और ऐसी गतिविधियों से संबंधित वित्तीय लेनदेन पर प्रतिबंध लगाता है।
- राष्ट्रपति की अनुशंसा पर, इस अधिनियम को संविधान के अनुच्छेद 117(1) और 117(3) के अंतर्गत वित्त विधेयक के रूप में संसद में पेश किया गया। इसका उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को विनियमित और प्रोत्साहित करते हुए नागरिकों के लिए एक ज़िम्मेदार डिजिटल वातावरण को बढ़ावा देना है।
- इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूर्ण प्रतिबंध है, जिसमें असली पैसे वाले गेम्स की पेशकश, विज्ञापन या वित्तीय लेनदेन की सुविधा शामिल है। बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए भुगतान संसाधित करने से रोक दिया गया है, और आईटी अधिनियम, 2000 के तहत सशक्त अधिकारियों को गैरकानूनी प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने का अधिकार दिया गया है।
अधिनियम के प्रमुख प्रावधान
1. ऑनलाइन गेम्स का वर्गीकरण
ऑनलाइन गेम को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:
- ई-स्पोर्ट्स: एक वैध खेल के रूप में मान्यता प्राप्त ई-स्पोर्ट्स में संगठित टूर्नामेंटों के माध्यम से खेले जाने वाले प्रतिस्पर्धी डिजिटल खेल शामिल हैं, जिनमें कौशल की आवश्यकता होती है।
- ऑनलाइन सामाजिक खेल: ये मुख्य रूप से कौशल-आधारित खेल हैं जो मनोरंजन या सामाजिक संपर्क के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जैसे वर्डले।
- ऑनलाइन मनी गेम्स: इन खेलों में वित्तीय दांव शामिल होते हैं, चाहे वे मौके पर आधारित हों, कौशल पर, या दोनों पर। खिलाड़ी मौद्रिक या अन्य लाभ की उम्मीद में शुल्क का भुगतान करते हैं या पैसा जमा करते हैं, जैसे ड्रीम11, पोकर और रम्मी।
2. अधिनियम की प्रयोज्यता
यह अधिनियम पूरे भारत में लागू होता है और इसमें देश के भीतर दी जाने वाली या बाहर से संचालित लेकिन भारत में सुलभ ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाएं शामिल हैं।
3. सकारात्मक गेमिंग को बढ़ावा देना
यह अधिनियम सकारात्मक गेमिंग पहलों को भी बढ़ावा देता है, जैसे:
- ई-स्पोर्ट्स: युवा मामले और खेल मंत्रालय को ई-स्पोर्ट्स के लिए दिशानिर्देश तैयार करने, प्रशिक्षण अकादमियां स्थापित करने और अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का काम सौंपा गया है।
- सामाजिक/शैक्षणिक खेल: केंद्र सरकार सीखने और मनोरंजन के लिए सुरक्षित, आयु-उपयुक्त प्लेटफार्मों को मान्यता दे सकती है, पंजीकृत कर सकती है और बढ़ावा दे सकती है।
4. नियामक निकाय
अधिनियम में राष्ट्रीय स्तर पर एक नियामक निकाय की स्थापना का प्रावधान है:
- खेलों को वर्गीकृत और पंजीकृत करें।
- निर्धारित करें कि क्या कोई खेल पैसे वाले खेल के रूप में योग्य है।
- शिकायतों और शिकायतों का निपटारा करें।
5. अपराध और दंड
अधिनियम में विभिन्न अपराधों के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया है, जिनमें शामिल हैं:
- ऑनलाइन मनी गेम की पेशकश करना, जिसके लिए 3 साल तक की कैद और ₹1 करोड़ का जुर्माना हो सकता है।
- प्रतिबंधित खेलों का विज्ञापन करने पर 2 वर्ष तक की कैद और 50 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है।
अपराधों को संज्ञेय और गैर-जमानती के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
6. देयता खंड
यह अधिनियम कंपनियों और उनके अधिकारियों को उल्लंघनों के लिए उत्तरदायी ठहराता है। स्वतंत्र और गैर-कार्यकारी निदेशकों को दायित्व से छूट दी जाती है, बशर्ते वे उचित परिश्रम का प्रदर्शन कर सकें।
ऑनलाइन जुआ
ऑनलाइन गेम वे गेम होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल उपकरणों पर खेले जाते हैं और इंटरनेट या अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार तकनीकों का उपयोग करके सॉफ़्टवेयर के माध्यम से संचालित होते हैं। ये खिलाड़ियों के बीच, चाहे वे कहीं भी हों, वास्तविक समय में बातचीत और प्रतिस्पर्धा की सुविधा प्रदान करते हैं।
वर्गीकरण:
- कौशल-आधारित खेल: ये मौके की बजाय कौशल को प्राथमिकता देते हैं और भारत में वैध हैं। उदाहरण के लिए, गेम 24X7, ड्रीम11 और मोबाइल प्रीमियर लीग (एमपीएल)।
- भाग्य के खेल: इनका परिणाम मुख्यतः कौशल के बजाय भाग्य पर निर्भर करता है और भारत में ये अवैध हैं। उदाहरण के लिए, रूलेट, जो खिलाड़ियों को मुख्यतः मौद्रिक पुरस्कारों के लिए आकर्षित करता है।
मार्केट के खरीददार और बेचने वाले:
- 2023 में, भारत 568 मिलियन गेमर्स और 9.5 बिलियन ऐप डाउनलोड के साथ दुनिया का सबसे बड़ा गेमिंग बाजार बन जाएगा।
- 2023 में इस बाजार का मूल्य 2.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर होगा, तथा 2028 तक इसके 8.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।
भारत के गेमिंग उद्योग के प्रमुख विकास चालक क्या हैं?
1. आर्थिक चालक
- स्टार्ट-अप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलों द्वारा समर्थित भारत के जीवंत स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र ने कई गेमिंग कंपनियों और प्लेटफार्मों के विकास को बढ़ावा दिया है।
- ये स्टार्ट-अप नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं और भारतीय उपभोक्ताओं की विविध गेमिंग प्राथमिकताओं को पूरा कर रहे हैं, जिससे उद्योग के विस्तार में योगदान मिल रहा है।
- उल्लेखनीय गेमिंग यूनिकॉर्न में गेम्स24X7, ड्रीम11 और मोबाइल प्रीमियर लीग शामिल हैं।
- हाल के वर्षों में, गेमिंग कंपनियों ने घरेलू और वैश्विक निवेशकों से 2.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए हैं, जो भारत में कुल स्टार्टअप फंडिंग का 3% है।
- एनवीडिया ने नवंबर 2025 में भारत में अपनी क्लाउड गेमिंग सेवा शुरू करने की घोषणा की है।
2. तकनीकी सक्षमकर्ता
- भारतनेट और राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन जैसी पहलों का उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में हाई-स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराना है, जिससे गेमर्स की पहुंच में वृद्धि होगी।
- 5G के आने से इंटरनेट की गति में और सुधार हुआ है तथा विलंबता कम हुई है, जो निर्बाध गेमिंग अनुभव के लिए महत्वपूर्ण है।
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में किए गए सर्वेक्षण से पता चलता है कि 85% से अधिक भारतीय परिवारों के पास स्मार्टफोन हैं, तथा 86.3% परिवारों के पास अपने परिसर में इंटरनेट की सुविधा है।
- भारत में गेमिंग बाजार में मोबाइल फोन का हिस्सा 90% है, जबकि अमेरिका में यह लगभग 37% और चीन में 62% है।
3. नीति और सांस्कृतिक बदलाव
- आईटी नियम 2021, स्व-नियामक निकायों और एवीजीसी टास्क फोर्स ने गेमिंग उद्योग के सुरक्षित विकास के लिए एक रूपरेखा स्थापित की है।
- कंटेंट क्रिएटर्स अवार्ड में गेमर्स को सम्मानित किया जाता है, और क्रिएट इन इंडिया अभियान कंटेंट क्रिएटर्स को बढ़ावा देता है।
- कोविड-19 लॉकडाउन ने उद्योग की वृद्धि को 50% तक बढ़ा दिया, जिससे औसत गेमिंग समय 2.5 घंटे से बढ़कर 4.1 घंटे प्रतिदिन हो गया, जिससे गेमिंग एक वैध करियर पथ बन गया।
भारत में गेमिंग उद्योग का विनियमन कैसे किया जाता है?
1. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 एवं नियम
- अप्रैल 2023 में संशोधित आईटी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्मों के लिए मानक निर्धारित करते हैं।
- मध्यस्थों को गैरकानूनी/अवैध सामग्री के प्रसार को रोकना होगा।
- पैसे वाले खेल की पेशकश करने वाले प्लेटफार्मों को स्व-नियामक निकायों (एसआरबी) के साथ पंजीकरण करना होगा, जो यह निर्धारित करते हैं कि कोई खेल स्वीकार्य है या नहीं।
- धारा 69ए सरकार को अवैध साइटों/ऐप्स को ब्लॉक करने का अधिकार देती है - 1,524 सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफॉर्म ब्लॉक किए गए (2022-जून 2025)।
2. भारतीय न्याय संहिता, 2023
- धारा 111: गैरकानूनी आर्थिक गतिविधियों और साइबर अपराधों को दंडित करती है।
- धारा 112: अनधिकृत सट्टेबाजी/जुआ खेलने पर 1-7 वर्ष की कैद और जुर्माने का प्रावधान है।
3. एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) अधिनियम, 2017
- अवैध/अपतटीय गेमिंग प्लेटफार्मों तक विस्तारित।
- ऑनलाइन मनी गेमिंग आपूर्तिकर्ताओं को सरलीकृत पंजीकरण योजना के तहत पंजीकरण कराना होगा।
- जीएसटी इंटेलिजेंस के महानिदेशक अपंजीकृत/गैर-अनुपालन वाले प्लेटफार्मों को अवरुद्ध करने का निर्देश दे सकते हैं।
- यह सुनिश्चित करता है कि डिजिटल गेमिंग संस्थाएं भौतिक व्यवसायों के समान कराधान मानदंडों का पालन करें।
4. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019
- भ्रामक/छद्म विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाता है।
- सीसीपीए जांच कर सकता है, दंडित कर सकता है और आपराधिक कार्यवाही शुरू कर सकता है।
- मशहूर हस्तियों/प्रभावशाली व्यक्तियों को सट्टेबाजी प्लेटफार्मों का समर्थन करने से प्रतिबंधित करने के लिए परामर्श जारी किए गए।
निषेध की कैंची से ऑनलाइन गेमिंग को खत्म करना

चर्चा में क्यों?
भारत सरकार ने हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025 पारित किया है, जो ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा देते हुए ऑनलाइन असली पैसे वाले खेलों पर प्रतिबंध लगाता है। यह निर्णय बिना किसी पूर्व चर्चा या परामर्श के लिया गया, जिससे निवेश और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभावों को लेकर गंभीर चिंताएँ पैदा हो रही हैं।
चाबी छीनना
- नये विधेयक ने ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र में नौकरियों के नुकसान और राजस्व में गिरावट के बारे में चिंता जताई है।
- आलोचकों का तर्क है कि यह प्रतिबंध विदेशी निवेश को बाधित कर सकता है तथा भारत के डिजिटल उद्योगों में नवाचार को बाधित कर सकता है।
- सरकार द्वारा प्रतिबन्ध लगाने का औचित्य खिलाड़ियों में नशे की लत और वित्तीय बर्बादी की चिंता पर आधारित है।
अतिरिक्त विवरण
- रोजगार पर प्रभाव: ऑनलाइन गेमिंग उद्योग द्वारा वर्ष 2025 तक डिजाइन, प्रोग्रामिंग और ग्राहक सहायता जैसे क्षेत्रों में लगभग 1.5 लाख लोगों को रोजगार दिए जाने का अनुमान था, लेकिन प्रतिबंध से बड़े पैमाने पर नौकरियां जाने का खतरा है।
- राजस्व निहितार्थ: ऑनलाइन गेमिंग से जीएसटी राजस्व में लगभग 17,000 करोड़ रुपये का योगदान होने की उम्मीद थी, एक ऐसा नुकसान जिसका सामना अब सरकार को करना होगा।
- विनियमन पर चिंताएं: आलोचकों का सुझाव है कि बेहतर दृष्टिकोण में पूर्ण प्रतिबंध के बजाय सावधानीपूर्वक विनियमन शामिल होगा, जो उद्योग को नष्ट किए बिना नशे की लत जैसे मुद्दों को हल कर सकता है।
- जिम्मेदार गेमिंग उपाय: प्रतिबंध से पहले, कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने जिम्मेदार गेमिंग को बढ़ावा देने के लिए आयु-सीमा और स्व-बहिष्कार जैसे उपायों को लागू किया था, जिसकी प्रतिबंध में अनदेखी की गई है।
- संवैधानिक मुद्दे: यह प्रतिबंध संवैधानिक अधिकारों, विशेष रूप से अनुच्छेद 19(1)(जी) के बारे में प्रश्न उठाता है, जो किसी भी पेशे या व्यवसाय को करने के अधिकार की गारंटी देता है।
निष्कर्षतः, ऑनलाइन वास्तविक धन गेमिंग पर अचानक प्रतिबंध से नौकरियों, राजस्व और विनियामक परिदृश्य के लिए जोखिम उत्पन्न हो गया है, जिससे यह अनिश्चितता बनी हुई है कि क्या यह नागरिकों की प्रभावी रूप से रक्षा करेगा या गेमिंग क्षेत्र में मौजूदा कमजोरियों को बढ़ाएगा।
विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति पर राष्ट्रपति का संदर्भ

चर्चा में क्यों?
सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत राष्ट्रपति के संदर्भ पर अपनी राय सुरक्षित रख ली है, जो विधेयकों को मंज़ूरी देने में राष्ट्रपति और राज्यपालों की शक्तियों से संबंधित है। यह संदर्भ सर्वोच्च न्यायालय के अप्रैल 2025 के उस फैसले के बाद आया है जिसमें तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि द्वारा 10 विधेयकों को मंज़ूरी देने में की गई देरी को असंवैधानिक माना गया था। न्यायालय ने मंज़ूरी लागू करने के लिए अनुच्छेद 142 का सहारा लिया और ऐसी कार्रवाइयों के लिए समय-सीमा निर्धारित की। यह स्थिति भारत के संवैधानिक ढाँचे के भीतर संघवाद, शक्तियों के पृथक्करण और न्यायिक समीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है।
चाबी छीनना
- राष्ट्रपति के संदर्भ का उद्देश्य राज्यपाल की शक्तियों के बारे में संवैधानिक संदेहों को स्पष्ट करना है।
- राज्यपाल और निर्वाचित सरकार के बीच शक्ति संतुलन को लेकर बहस चल रही है।
- सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में विधेयकों को समय पर मंजूरी देने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
अतिरिक्त विवरण
- संदर्भ की प्रकृति: अनुच्छेद 143(1) के तहत राष्ट्रपति संदर्भ, राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्नों पर सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने का अधिकार देता है। राज्यों का तर्क है कि यह संदर्भ सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक अप्रत्यक्ष अपील के रूप में कार्य करता है, जो स्टेयर डेसिसिस के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।
- राज्यपाल की शक्तियाँ: राज्यों का तर्क है कि राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह (अनुच्छेद 163) के आधार पर कार्य करना चाहिए, जो व्यक्तिगत विवेक के बजाय जनादेश को दर्शाता है। इसके विपरीत, केंद्र का तर्क है कि विवेकाधीन शक्तियाँ असाधारण परिस्थितियों के लिए ही मौजूद हैं।
- राज्यपाल का वीटो और "पॉकेट वीटो": सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि राज्यपाल किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति अनिश्चित काल तक नहीं रोक सकते, क्योंकि ऐसा करने पर विधेयक निरस्त हो जाता है। राज्यपाल द्वारा "पॉकेट वीटो" की अवधारणा को खारिज कर दिया गया है, और भारत सरकार अधिनियम 1935 के संवैधानिक उदाहरण पर ज़ोर दिया गया है।
- समयसीमा का न्यायिक प्रवर्तन: सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में अनावश्यक देरी को रोकने के लिए स्वीकृति के लिए समयसीमा निर्धारित की गई है, हालांकि केंद्र का तर्क है कि यह संविधान में न्यायिक संशोधन के समान है।
- मौलिक अधिकार और रिट क्षेत्राधिकार: केंद्र का कहना है कि राज्य अनुच्छेद 32 का प्रयोग नहीं कर सकते, जो व्यक्तिगत मौलिक अधिकारों के लिए है, जबकि राज्यों का तर्क है कि उन्हें रिट उपचार से वंचित करने से संघीय संतुलन कमजोर होता है।
- व्यापक संवैधानिक और राजनीतिक निहितार्थ: वर्तमान संदर्भ कार्यकारी कार्यों पर न्यायिक समीक्षा की सीमाओं का परीक्षण करता है और भारत में संघवाद की गतिशीलता को प्रभावित करता है।
निष्कर्षतः, राष्ट्रपति का संदर्भ यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण है कि भारत संघवाद, संवैधानिक परंपराओं और न्यायिक निगरानी के बीच नाजुक संतुलन कैसे बनाए रखता है। राज्यपाल की भूमिका को स्पष्ट करना और भविष्य में विवादों को रोकने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को मज़बूत करने हेतु सुधारों पर विचार करना आवश्यक है।
डीएनए साक्ष्य पर सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देश

चर्चा में क्यों?
कट्टावेल्लई @ देवकर बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में , सर्वोच्च न्यायालय ने आपराधिक मामलों में डीएनए साक्ष्यों के संचालन के लिए कड़े प्रोटोकॉल स्थापित करने का आदेश दिया। न्यायालय ने सभी राज्य पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) को निर्देश दिया कि वे सभी जिलों में डीएनए नमूनों की अखंडता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हुए, चेन ऑफ कस्टडी रजिस्टर फॉर्म और संबंधित दस्तावेज तैयार करें।
चाबी छीनना
- सर्वोच्च न्यायालय ने डीएनए साक्ष्य प्रबंधन के लिए एक समान दिशा-निर्देशों की आवश्यकता पर बल दिया।
- संदूषण को रोकने और डीएनए साक्ष्य में विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए सख्त प्रोटोकॉल निर्धारित किए गए थे।
अतिरिक्त विवरण
- एक समान डीएनए हैंडलिंग दिशानिर्देशों की आवश्यकता: न्यायालय ने पिछले मामलों में गंभीर खामियों को उजागर किया, जैसे कि फोरेंसिक प्रयोगशालाओं में नमूने भेजने में देरी और कस्टडी की स्पष्ट श्रृंखला बनाए रखने में विफलता, जिससे संदूषण की चिंताएं बढ़ गईं।
- जारी किए गए प्रमुख दिशानिर्देश:
- डीएनए नमूनों को उचित देखभाल के साथ एकत्रित किया जाना चाहिए, उचित रूप से पैक किया जाना चाहिए तथा उनका दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए।
- नमूनों को संबंधित पुलिस स्टेशन या अस्पताल में ले जाया जाना चाहिए तथा 48 घंटे के भीतर फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला तक पहुंचना चाहिए, तथा किसी भी देरी के बारे में स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए तथा संरक्षण के उपायों का दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए।
- एक बार संग्रहीत होने के बाद, नमूनों को परीक्षण न्यायालय की अनुमति के बिना खोला या परिवर्तित नहीं किया जा सकता।
- हिरासत की एक श्रृंखला वसूली से लेकर दोषसिद्धि या दोषमुक्ति तक बनाए रखी जानी चाहिए, तथा किसी भी चूक के लिए जांच अधिकारी को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।
- सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार इस बात पर जोर दिया है कि यद्यपि डीएनए साक्ष्य शक्तिशाली है, फिर भी इसे एकत्र करने और संभालने के सख्त मानकों का पालन किया जाना चाहिए।
- पिछले फैसलों में, जैसे अनिल बनाम महाराष्ट्र राज्य (2014) और मनोज बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2022) , न्यायालय ने डीएनए प्रोफाइलिंग की वैधता को बरकरार रखा, लेकिन संदूषण के जोखिम और गुणवत्ता नियंत्रण के महत्व पर ध्यान दिया।
निष्कर्षतः, सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का उद्देश्य डीएनए साक्ष्य की विश्वसनीयता बढ़ाना और आपराधिक न्याय प्रणाली को मज़बूत बनाना है। इनकी प्रभावशीलता पुलिस और फोरेंसिक एजेंसियों द्वारा निरंतर अनुपालन पर निर्भर करती है।
निर्णायक कदम: मतदाता सत्यापन के लिए आधार को 12वें दस्तावेज़ के रूप में शामिल करना

चर्चा में क्यों?
लोकतंत्र में मतदान का अधिकार नागरिकता का एक मूलभूत तत्व है। हालाँकि, मतदाता सूची को अद्यतन करने में प्रक्रियागत कठोरता के कारण पात्र मतदाता सूची से बाहर हो गए हैं। बिहार के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान में सर्वोच्च न्यायालय के हालिया हस्तक्षेप ने मतदाता सत्यापन के लिए 12 स्वीकार्य दस्तावेजों में से एक के रूप में आधार को शामिल करना अनिवार्य कर दिया, जिससे 65 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम मसौदा सूची से हटाए जाने के मुद्दे का समाधान हुआ।
चाबी छीनना
- सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय यह सुनिश्चित करता है कि चुनावी प्रक्रिया समावेशी बनी रहे और वास्तविक मतदाताओं को इससे वंचित न रखा जाए।
- सत्यापन दस्तावेज के रूप में आधार को शामिल करने से बड़े पैमाने पर मताधिकार से वंचित होने की समस्या को रोका जा सकेगा, विशेष रूप से हाशिए पर स्थित समूहों के बीच।
अतिरिक्त विवरण
- न्यायिक स्पष्टता: सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के इस तर्क को खारिज कर दिया कि आधार केवल निवास के प्रमाण के रूप में कार्य करता है, तथा कहा कि कई स्वीकृत दस्तावेज निर्णायक रूप से नागरिकता स्थापित नहीं करते हैं।
- बड़े पैमाने पर बहिष्कार को रोकना: बिहार की 90% आबादी के पास आधार है, इसे बाहर करने से कई पात्र मतदाता, विशेष रूप से गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोग, मताधिकार से वंचित हो जाएंगे।
- विसंगतियों को सुधारना: सांख्यिकीय विश्लेषण से पता चला कि महिलाएं और प्रवासी बहिष्करण प्रक्रिया से असमान रूप से प्रभावित हुए।
मतदाताओं के लिए आधार सत्यापन पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला चुनावी समावेशिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह मतदाता सूची में सटीकता और सभी नागरिकों के लिए लोकतांत्रिक भागीदारी सुलभ बनाने की अनिवार्यता के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता को दर्शाता है।
न्यायाधीशों का सुनवाई से अलग होना

चर्चा में क्यों?
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने कथित अवैध खनन मामले से संबंधित याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है, उन्होंने कहा कि एक विधान सभा सदस्य (एमएलए) ने मामले के संबंध में चर्चा के लिए उनसे संपर्क करने का प्रयास किया था।
चाबी छीनना
- किसी मामले से न्यायाधीश का हट जाना, हितों के टकराव या पक्षपात की धारणा के कारण होता है।
- सुनवाई से अलग होने के संबंध में कोई संहिताबद्ध कानून नहीं हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के फैसले मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान करते हैं।
अतिरिक्त विवरण
- अवलोकन: 'अस्वीकृति' से तात्पर्य किसी न्यायाधीश द्वारा हितों के टकराव या पूर्वाग्रह से बचने के लिए किसी मामले से अलग रहने से है।
- कानूनी आधार: हालाँकि कोई स्पष्ट कानून नहीं हैं, फिर भी सर्वोच्च न्यायालय के कई फैसलों के सिद्धांत, सुनवाई से अलग होने की प्रक्रिया का मार्गदर्शन करते हैं। उदाहरण के लिए, रंजीत ठाकुर बनाम भारत संघ (1987) मामले में , पक्षपात की कसौटी प्रभावित पक्ष के मन में आशंकाओं की तार्किकता से निर्धारित होती है।
- सुनवाई से अलग होने के आधार:न्यायाधीश विभिन्न कारणों से सुनवाई से अलग हो सकते हैं, जिनमें शामिल हैं:
- संबंधित पक्ष के साथ पूर्व व्यक्तिगत या व्यावसायिक संबंध।
- मामले में पहले भी एक पक्ष का प्रतिनिधित्व किया है।
- सम्मिलित पक्षों के साथ एकपक्षीय संचार।
- अपने पूर्व निर्णयों की समीक्षा करना।
- वित्तीय या व्यक्तिगत हित, जैसे मामले से संबंधित कंपनी में शेयरधारिता।
- अंतर्निहित सिद्धांत: नेमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ का सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि किसी को भी अपने मामले में न्यायाधीश नहीं होना चाहिए।
- सुनवाई से अलग होने की प्रक्रिया: सुनवाई से अलग होने का निर्णय आमतौर पर न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर करता है। वे पक्षों को मौखिक रूप से सूचित कर सकते हैं, इसे आदेश में दर्ज कर सकते हैं, या बिना किसी स्पष्टीकरण के सुनवाई से अलग होने का विकल्प चुन सकते हैं। सुनवाई से अलग होने का अनुरोध वकील या पक्षकार दोनों द्वारा किया जा सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय न्यायाधीश का होता है।
- अस्वीकृति से संबंधित चिंताएं:
- न्यायिक स्वतंत्रता खतरे में: मुकदमे से अलग होने की प्रक्रिया का दुरुपयोग वादियों द्वारा "बेंच हंटिंग" में शामिल होने के लिए किया जा सकता है, जिससे न्यायिक निष्पक्षता से समझौता हो सकता है।
- एकसमान मानकों का अभाव: औपचारिक नियमों के अभाव के कारण विभिन्न न्यायाधीशों द्वारा अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाए जा सकते हैं।
- दुरुपयोग की संभावना: कार्यवाही से अलग होने के अनुरोध से कार्यवाही में देरी हो सकती है, न्यायाधीशों को डराया जा सकता है, या न्याय में बाधा उत्पन्न हो सकती है, जिससे न्यायालयों की निष्ठा और समय पर न्याय प्रदान करने में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
भारत के संविधान के संदर्भ में, सामान्य कानूनों में निषेध या सीमाएं अनुच्छेद 142 के तहत संवैधानिक शक्तियों को प्रतिबंधित नहीं करती हैं। इसका तात्पर्य यह है कि:
- (क) भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लिए गए निर्णयों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
- (ख) भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा बनाए गए कानूनों से बाध्य नहीं है।
- (ग) गंभीर वित्तीय संकट की स्थिति में, भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से परामर्श किए बिना वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है।
- (घ) राज्य विधानमंडलों को संघीय विधानमंडल की सहमति के बिना विशिष्ट मामलों पर कानून बनाने से प्रतिबंधित किया गया है।
आरटीई और अल्पसंख्यक स्कूल

चर्चा में क्यों?
सर्वोच्च न्यायालय ने प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट के मामले में अपने 2014 के फैसले पर सवाल उठाए हैं, जिसमें अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के प्रावधानों से छूट दी गई थी। दो न्यायाधीशों वाली पीठ अब इस बात पर पुनर्विचार कर रही है कि क्या अल्पसंख्यक स्कूलों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य है, जो सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मौलिक अधिकार के बारे में चिंताओं को उजागर करता है।
चाबी छीनना
- टीईटी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अल्पसंख्यक स्कूलों और सेवारत शिक्षकों से संबंधित है।
- अल्पसंख्यक संस्थानों पर आरटीई अधिनियम की प्रयोज्यता के संबंध में चिंताएं व्यक्त की गईं।
- 2014 के प्रमति फैसले से बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्रभावित हो सकती है।
अतिरिक्त विवरण
- सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय: पीठ ने प्रमति निर्णय द्वारा दी गई पिछली छूट पर सवाल उठाते हुए अल्पसंख्यक स्कूलों पर आरटीई अधिनियम की प्रयोज्यता के मुद्दे को एक बड़ी पीठ को भेज दिया।
- सेवारत शिक्षक: 5 वर्ष से कम सेवा वाले शिक्षक टीईटी उत्तीर्ण किए बिना पद पर बने रह सकते हैं, जबकि 5 वर्ष से अधिक सेवा वाले शिक्षकों को अपने पद के लिए पात्र बने रहने के लिए दो वर्षों के भीतर इसे उत्तीर्ण करना होगा।
- इस फैसले में प्रमति फैसले की आलोचना करते हुए कहा गया कि यह "कानूनी रूप से संदिग्ध" है और इसमें अल्पसंख्यक संस्थानों को आरटीई के आदेशों से असमान रूप से छूट दी गई है, विशेष रूप से वंचित बच्चों के लिए 25% आरक्षण के संबंध में।
- अनुच्छेद 30(1) (अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकार) और अनुच्छेद 21ए (बच्चों के शिक्षा के अधिकार) के बीच संघर्ष को उजागर किया गया तथा इस बात पर बल दिया गया कि दोनों अधिकार सह-अस्तित्व में होने चाहिए।
- न्यायालय ने 86वें संशोधन (2002) और 93वें संशोधन (2005) को बरकरार रखा, शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी और वंचित समूहों के लिए राज्य प्रावधानों की अनुमति दी, जबकि यह माना कि अल्पसंख्यक स्कूलों में आरटीई अधिनियम का लागू होना असंवैधानिक था।
- छूट के औचित्य में यह चिंता शामिल थी कि वंचित बच्चों के लिए सीटें आरक्षित करने से शैक्षणिक संस्थानों का अल्पसंख्यक चरित्र कमजोर हो सकता है।
- विशेषज्ञों का कहना है कि आरटीई अधिनियम संस्थागत स्वायत्तता की तुलना में बच्चों के अधिकारों को प्राथमिकता देता है, जिससे अल्पसंख्यक स्कूलों में छात्र-शिक्षक अनुपात और योग्य शिक्षकों के संबंध में अनुपालन की आवश्यकता का संकेत मिलता है।
सर्वोच्च न्यायालय की पुनः जांच का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अल्पसंख्यक स्कूल भी अन्य स्कूलों के समान शैक्षिक मानकों को बनाए रखें, जिससे सभी बच्चों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मौलिक अधिकारों की रक्षा हो सके।
राज्यपाल द्वारा कुलपतियों की नियुक्ति
चर्चा में क्यों?
केरल में राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों (वीसी) की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर हाल ही में एक विवाद सामने आया है। राज्यपाल, जो पदेन कुलाधिपति के रूप में कार्य करते हैं, ने सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध किया है कि मुख्यमंत्री को इस चयन प्रक्रिया से बाहर रखा जाए।
चाबी छीनना
- कुलपति विश्वविद्यालय के प्रमुख शैक्षणिक एवं कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं।
- कुलपतियों की नियुक्ति यूजीसी विनियम, 2018 के अनुसार, खोज-सह-चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है।
- यूजीसी विनियमों और राज्य कानूनों के बीच विवादों में कानूनी सर्वोच्चता संविधान के अनुच्छेद 254 के तहत यूजीसी मानदंडों के पक्ष में है।
विश्वविद्यालयों में राज्यपाल और राष्ट्रपति की भूमिका के बारे में
- राज्य विश्वविद्यालय: विश्वविद्यालय प्रशासन से संबंधित मामलों में कुलाधिपति राज्य मंत्रिमंडल से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है।
- कुलपति की नियुक्ति: कुलाधिपति, यूजीसी विनियमों के अनुसार खोज-सह-चयन समिति द्वारा प्रस्तुत पैनल में से कुलपतियों की नियुक्ति करते हैं।
- कानूनी सर्वोच्चता: यूजीसी विनियमों और राज्य कानूनों के बीच संघर्ष के मामलों में, संविधान के अनुच्छेद 254 के तहत यूजीसी मानदंड को प्राथमिकता दी जाएगी।
- केन्द्रीय विश्वविद्यालय: भारत के राष्ट्रपति केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के तहत विजिटर के रूप में कार्य करते हैं, तथा औपचारिक प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं।
- राष्ट्रपति, खोज समिति द्वारा सुझाए गए पैनल में से कुलपतियों का चयन करते हैं तथा असंतुष्ट होने पर नए पैनल का अनुरोध कर सकते हैं।
- निरीक्षण शक्तियां: राष्ट्रपति को विश्वविद्यालयों में निरीक्षण और जांच करने का अधिकार है।
यूपीएससी 2014 प्रश्न:
निम्नलिखित में से कौन सी विवेकाधीन शक्तियां किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई हैं?
- 1. राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए भारत के राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना
- 2. मंत्रियों की नियुक्ति
- 3. राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखना
- 4. राज्य सरकार के कामकाज के संचालन के लिए नियम बनाना
नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1 और 3
- (c) केवल 2, 3 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4
यह चर्चा कुलपतियों की नियुक्ति में राज्यपाल की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है तथा भारत में उच्च शिक्षा में प्रशासन के बारे में चल रही बहस पर प्रकाश डालती है।
विदेशी न्यायाधिकरण (एफटी) गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है
 चर्चा में क्यों?
चर्चा में क्यों?
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी न्यायाधिकरणों (एफटी) को, विशेष रूप से असम में, संदिग्ध अवैध प्रवासियों को निर्दिष्ट शिविरों में हिरासत में रखने का अधिकार दिया है। पहले यह अधिकार केवल कार्यकारी आदेशों के माध्यम से ही प्रयोग किया जाता था।
चाबी छीनना
- विदेशी न्यायाधिकरण, विदेशी (न्यायाधिकरण) आदेश, 1964 के तहत स्थापित अर्ध-न्यायिक निकाय हैं।
- वे यह निर्धारित करते हैं कि कोई व्यक्ति विदेशी है या अवैध आप्रवासी, विशेष रूप से असम में सीमा प्रवास के मुद्दों के संबंध में।
- एनआरसी-2019 के बाद हुए विस्तार के बाद, वर्तमान में असम में लगभग 100 एफटी कार्यरत हैं।
- आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम, 2025 के अंतर्गत नए प्रावधान, विदेशी नागरिकों को गिरफ्तारी वारंट जारी करने और व्यक्तियों को हिरासत में लेने का अधिकार देते हैं।
अतिरिक्त विवरण
- प्रकृति: एफटी की स्थापना संदिग्ध विदेशियों से संबंधित मामलों पर निर्णय देने के लिए की जाती है, जो मुख्य रूप से सीमा पुलिस के संदर्भों और चुनाव आयोग द्वारा चिह्नित "डी" (संदिग्ध) मतदाताओं के मामलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- संरचना: प्रत्येक न्यायाधिकरण में अधिकतम तीन सदस्य होते हैं, जिनमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश, अधिवक्ता और न्यायिक अनुभव वाले सिविल सेवक शामिल हो सकते हैं।
- कार्यप्रणाली: FTs के पास सिविल न्यायालय की शक्तियां होती हैं, जिसमें गवाहों को बुलाने और साक्ष्यों की जांच करने की क्षमता शामिल है, तथा मामलों को 60 दिनों के भीतर निपटाना अनिवार्य होता है।
- न्यायिक प्राधिकार: नए प्रावधानों के तहत, FT अब गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकते हैं, हिरासत में लेने का आदेश दे सकते हैं, तथा व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता कर सकते हैं।
- रोजगार पर प्रतिबंध: विदेशियों को केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना रणनीतिक क्षेत्रों में काम करने से रोक दिया गया है।
- छूट: नेपाल, भूटान, तिब्बतियों और श्रीलंकाई तमिलों को 2025 में जारी एक विशेष आदेश के तहत छूट दी गई है।
नए नियम भारत में, विशेष रूप से असम में, जहां प्रवासन का मुद्दा लंबे समय से चिंता का विषय रहा है, अवैध आप्रवासियों की हिरासत और निर्वासन को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देते हैं।
भारत में 50% आरक्षण सीमा पार करने पर बहस
चर्चा में क्यों?
भारत में 50% आरक्षण सीमा से संबंधित चर्चा ने उच्च कोटा और लाभों के उप-वर्गीकरण की वकालत करने वाली विभिन्न याचिकाओं और राजनीतिक आंदोलनों के कारण नए सिरे से ध्यान आकर्षित किया है।
चाबी छीनना
- राजनीतिक और सामाजिक दबाव के बीच 50% की सीमा को पार करने की मांग फिर से उभरी है।
- हाल के वक्तव्यों में आरक्षण में वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है, जैसे कि बिहार में 85% की सीमा।
- जाति जनगणना की मांग का उद्देश्य आरक्षण नीतियों को सूचित करने के लिए विश्वसनीय जनसांख्यिकीय डेटा एकत्र करना है।
अतिरिक्त विवरण
- संवैधानिक ढांचा: अनुच्छेद 15 और 16 कानून के समक्ष समानता और सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर की गारंटी देते हैं, जबकि अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) सहित सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति देते हैं ।
- केंद्रीय स्तर पर वर्तमान आरक्षण प्रतिशत में शामिल हैं:
- ओबीसी: 27%
- एससी: 15%
- एसटी: 7.5%
- ईडब्ल्यूएस: 10%
- प्रमुख न्यायिक घोषणाएँ:
- बालाजी बनाम मैसूर राज्य (1962): आरक्षण को 'उचित सीमा' के रूप में 50% तक सीमित कर दिया गया।
- केरल राज्य बनाम एनएम थॉमस (1975): मौलिक समानता की वकालत की गई, जिसमें कहा गया कि आरक्षण समानता को बढ़ाता है।
- इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992): ओबीसी आरक्षण को मान्यता देते हुए 50% की सीमा को बरकरार रखा।
- जनहित अभियान बनाम भारत संघ (2022): स्पष्ट किया गया कि 50% की सीमा पिछड़े वर्गों पर लागू होती है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों पर नहीं।
- पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (2024): एससी और एसटी के लिए क्रीमी लेयर सिद्धांतों की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
- उभरते मुद्दे: रोहिणी आयोग ने रिपोर्ट दी कि ओबीसी लाभों का अनुपातहीन हिस्सा कुछ ही प्रतिशत जातियों द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिसके कारण उप-वर्गीकरण की मांग उठी।
- रिक्तियों का लंबित भंडार: आरक्षित सीटों का महत्वपूर्ण हिस्सा रिक्त रह गया है, जो प्रणालीगत भर्ती संबंधी समस्याओं को उजागर करता है।
चुनौती समानता के अधिकार और सामाजिक न्याय की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाने की है। आरक्षण को 50% की सीमा से आगे बढ़ाने से योग्यता-आधारित व्यवस्था कमज़ोर हो सकती है, लेकिन आँकड़े बताते हैं कि हाशिए पर पड़े समूहों का प्रतिनिधित्व अभी भी कम है। प्रस्तावित सुधारों में उप-वर्गीकरण और कौशल विकास में निवेश बढ़ाना शामिल है ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के आरक्षण पर निर्भरता कम की जा सके।
न्यायाधीश की असहमति को छिपाना, न्यायपालिका के अधिकार को कमजोर करना
 चर्चा में क्यों?
चर्चा में क्यों?
न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पदोन्नति के संबंध में न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना की असहमति से उत्पन्न हालिया विवाद ने भारत की न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया, विशेष रूप से कॉलेजियम प्रणाली की पारदर्शिता और जवाबदेही के बारे में महत्वपूर्ण चिंताएं उत्पन्न कर दी हैं।
चाबी छीनना
- कॉलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता का अभाव है, तथा नियुक्तियां बंद दरवाजों के पीछे की जाती हैं।
- न्यायमूर्ति नागरत्ना की असहमति न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया में अस्पष्टता और लोकतांत्रिक घाटे को उजागर करती है।
- न्यायिक नियुक्तियों में गोपनीयता न्यायपालिका की वैधता और अधिकार को कमजोर करती है।
अतिरिक्त विवरण
- कॉलेजियम प्रणाली: द्वितीय न्यायाधीश मामले (1993) और तृतीय न्यायाधीश मामले (1998) के माध्यम से स्थापित, यह प्रणाली सर्वोच्च न्यायालय के पाँच वरिष्ठतम न्यायाधीशों को न्यायिक नियुक्तियों का अधिकार देती है। हालाँकि, इसके विचार-विमर्श को सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं किया जाता है, जिससे जवाबदेही का अभाव होता है।
- न्यायपालिका द्वारा उम्मीदवारों की सुरक्षा और राजनीतिक दबाव का हवाला देकर गोपनीयता की रक्षा करने के बावजूद, अन्य लोकतंत्रों ने दिखाया है कि पारदर्शिता और निष्पक्षता साथ-साथ रह सकती है।
- नियुक्तियों के लिए औचित्य का अभाव और छिपी हुई असहमति जनता के विश्वास और न्यायपालिका के नैतिक अधिकार को कमजोर करती है।
अपनी वैधता की रक्षा के लिए, न्यायपालिका को पारदर्शिता को अपनाने के लिए कॉलेजियम प्रणाली में सुधार करना होगा। ऐसा करके, वह जनता का विश्वास मज़बूत कर सकती है और इस लोकतांत्रिक सिद्धांत को कायम रख सकती है कि सभी शक्तियों का औचित्य सिद्ध होना चाहिए।
राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 - भारतीय खेलों में पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में
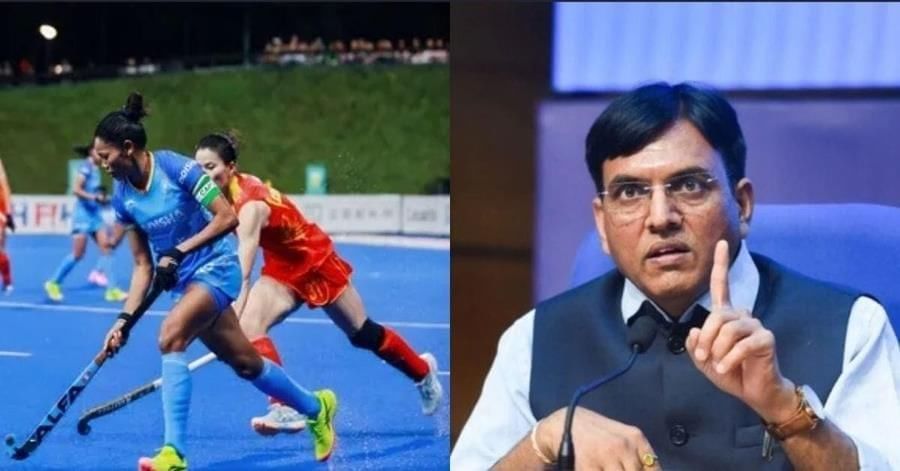
चर्चा में क्यों?
भारत में राष्ट्रीय खेल निकायों को विनियमित और मान्यता देने के लिए संसद के मानसून सत्र के दौरान राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 पारित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य खेल प्रशासन में कुप्रबंधन, राजनीतिक हस्तक्षेप और कानूनी विवादों के दीर्घकालिक मुद्दों को समाप्त करना और पुरानी भारतीय राष्ट्रीय खेल विकास संहिता को एक अधिक व्यापक कानूनी ढाँचे से प्रतिस्थापित करना है।
चाबी छीनना
- इस अधिनियम का उद्देश्य भारत में खेल प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है।
- यह राष्ट्रीय खेल महासंघों को मान्यता देने के लिए एक राष्ट्रीय खेल बोर्ड की स्थापना करता है।
- प्रमुख प्रावधानों में शासन मानदंड, विवाद समाधान और चुनाव निगरानी शामिल हैं।
अतिरिक्त विवरण
- ऐतिहासिक संदर्भ: भारत 1900 में ओलंपिक में भाग लेने वाला पहला एशियाई राष्ट्र था, फिर भी 2025 तक इसके पास एक समर्पित खेल प्रशासन कानून का अभाव था। इस शून्यता ने खेल महासंघों को राजनीतिक हस्तियों द्वारा नियंत्रित करने की अनुमति दी, जिससे चुनावी कदाचार और गैर-खिलाड़ियों के वर्चस्व जैसे मुद्दे पैदा हुए, जैसा कि 2014 की संसदीय स्थायी समिति ने नोट किया था।
- वैश्विक दंड: भारतीय खेल निकायों को कुप्रशासन के लिए प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा, जिसमें भारतीय कुश्ती महासंघ को समय पर चुनाव न कराने के कारण 2023 में निलंबित किया जाना तथा अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ को 2022 में फीफा द्वारा निलंबित किया जाना शामिल है।
- शासन ढाँचा: यह अधिनियम महासंघों को मान्यता प्रदान करने हेतु एक राष्ट्रीय खेल बोर्ड की स्थापना का अधिकार देता है, जिससे वैधता संबंधी विवादों का समाधान हो सके। यह अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप एक आचार संहिता बनाने का भी आदेश देता है।
- विवाद समाधान: विवादों को निपटाने तथा खेल-संबंधी मुकदमेबाजी को सुव्यवस्थित करने के लिए एक राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण की स्थापना की जाएगी।
- चुनाव निगरानी: यह अधिनियम चुनावों की निगरानी, अनुपालन सुनिश्चित करने तथा अनुपालन न करने वाले महासंघों के अयोग्य घोषित होने के जोखिम को कम करने के लिए निर्वाचन अधिकारियों का एक राष्ट्रीय पैनल स्थापित करता है।
राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 भारत में खेल प्रशासन में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जो एक समावेशी और पारदर्शी शासन संरचना को बढ़ावा देता है। इसका प्रभावी कार्यान्वयन खिलाड़ियों को सशक्त बनाने और वैश्विक खेल मंच पर भारत की विश्वसनीयता बहाल करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिससे राष्ट्रमंडल खेलों और ओलंपिक जैसे प्रतिष्ठित आयोजनों की मेजबानी की इसकी संभावनाएँ बढ़ेंगी।
यूजीसी मसौदा यूजी पाठ्यक्रम और राज्यों की आपत्तियाँ

चर्चा में क्यों?
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने हाल ही में जनता की प्रतिक्रिया के लिए स्नातक पाठ्यक्रमों का मसौदा जारी किया है। हालाँकि, विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों, विशेष रूप से कर्नाटक और केरल, ने इस पर गंभीर आपत्तियाँ उठाई हैं। दोनों राज्य अब आधिकारिक प्रतिक्रियाएँ प्रस्तुत करने से पहले मसौदों की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ पैनल गठित कर रहे हैं। हालाँकि यूजीसी ने देश भर से टिप्पणियाँ आमंत्रित की हैं, लेकिन ये आपत्तियाँ पाठ्यक्रम के डिज़ाइन और राज्य की शैक्षिक प्राथमिकताओं के साथ इसके संरेखण को लेकर संघीय चिंताओं को रेखांकित करती हैं।
चाबी छीनना
- यूजीसी ने उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लर्निंग आउटकम्स-आधारित पाठ्यक्रम रूपरेखा (एलओसीएफ) का प्रस्ताव रखा है।
- विपक्षी राज्यों ने मसौदा पाठ्यक्रम की आलोचना करते हुए कहा है कि यह विचारधारा के केन्द्रीय अधिरोपण को दर्शाता है।
- औपचारिक फीडबैक देने से पहले ड्राफ्ट का मूल्यांकन करने के लिए कर्नाटक और केरल में विशेषज्ञ पैनल गठित किए जा रहे हैं।
अतिरिक्त विवरण
- सीखने के परिणाम-आधारित पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एलओसीएफ): यह शैक्षिक मॉडल सीखने के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करता है - छात्रों को क्या जानना, समझना और हासिल करना चाहिए - न कि केवल सामग्री प्रदान करना।
- ज़रूरी भाग:
- स्नातक गुण: बौद्धिक जिज्ञासा, समस्या-समाधान कौशल, नैतिक आचरण और अनुकूलनशीलता जैसे आवश्यक गुण जो अध्ययन के बाद अपेक्षित होते हैं।
- कार्यक्रम परिणाम: संपूर्ण डिग्री कार्यक्रमों के लिए स्पष्ट शिक्षण परिणाम।
- पाठ्यक्रम परिणाम: व्यक्तिगत पाठ्यक्रमों के लिए विशिष्ट, मापन योग्य परिणाम जो यह दर्शाते हैं कि पाठ्यक्रम पूरा होने पर छात्र क्या कर सकते हैं।
- एलओसीएफ के लक्ष्य:
- फोकस में बदलाव: निष्क्रिय स्मरण की तुलना में ज्ञान के सक्रिय निर्माण और अनुप्रयोग पर जोर दिया जाता है।
- छात्र सशक्तिकरण: सक्रिय शिक्षण को प्रोत्साहित करता है, शिक्षकों को मात्र प्रशिक्षक के बजाय सुविधा प्रदाता के रूप में स्थापित करता है।
- कौशल विकास: इसका उद्देश्य विश्लेषणात्मक तर्क और समस्या-समाधान जैसे 21वीं सदी के महत्वपूर्ण कौशल का निर्माण करना है।
- बढ़ी हुई रोजगार क्षमता: छात्रों को कार्यबल के लिए प्रासंगिक ज्ञान और दक्षताओं से लैस करता है।
- समग्र विकास: मूल्यों, नैतिकता और आजीवन सीखने के साथ-साथ शैक्षणिक ज्ञान को बढ़ावा देता है।
यूजीसी ने मानव विज्ञान, रसायन विज्ञान, वाणिज्य और राजनीति विज्ञान सहित नौ विषयों के लिए एलओसीएफ का मसौदा जारी किया है। ये मसौदे राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप हैं और कई विकल्पों के साथ लचीले चार वर्षीय बहु-विषयक स्नातक कार्यक्रमों की परिकल्पना करते हैं। उल्लेखनीय रूप से, इनका उद्देश्य भारतीय ज्ञान प्रणालियों को उच्च शिक्षा में एकीकृत करना है, पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक शिक्षा के साथ मिलाना है।
यूजीसी द्वारा यह स्पष्ट किए जाने के बावजूद कि विश्वविद्यालयों को मॉड्यूल को अनुकूलित या पुनः डिज़ाइन करने की स्वायत्तता बरकरार है, मसौदा पाठ्यक्रम को केंद्र सरकार की विचारधाराओं को थोपने के लिए कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा है। विशेषज्ञों की समीक्षा के साथ, यूजीसी द्वारा प्रस्तावित बदलावों और राज्य शिक्षा प्रणालियों पर उनके प्रभावों को लेकर चर्चाएँ जारी हैं।
नया विदेशी अधिनियम

चर्चा में क्यों?
1 सितंबर से लागू हुए आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम, 2025 ने विदेशी नागरिकों के प्रबंधन हेतु भारत के ढाँचे में व्यापक सुधार किया है। इस महत्वपूर्ण अद्यतन का उद्देश्य मौजूदा कानूनों के समेकन के माध्यम से विदेशी नागरिकों के विनियमन में स्पष्टता, दक्षता और एकरूपता बढ़ाना है।
चाबी छीनना
- यह अधिनियम चार पुराने कानूनों का स्थान लेता है, तथा आव्रजन ढांचे को सुव्यवस्थित करता है।
- यह विदेशी नागरिकों के विनियमन के लिए स्पष्ट, केंद्रीकृत नियम प्रस्तुत करता है।
- नए प्रावधानों में अनिवार्य डिजिटल रिपोर्टिंग और उल्लंघनों के लिए क्रमिक जुर्माना प्रणाली शामिल है।
अतिरिक्त विवरण
- कानूनों का समेकन:यह अधिनियम निम्नलिखित कानूनों का स्थान लेता है:
- पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920
- विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम, 1939
- विदेशी अधिनियम, 1946
- आव्रजन (वाहक दायित्व) अधिनियम, 2000
- आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता क्यों पड़ी: पिछली आव्रजन व्यवस्था खंडित और पुरानी थी, जिसके कारण असंगत प्रवर्तन और प्रशासनिक अंतराल पैदा हो गए थे।
- वैध दस्तावेज़ और प्रवेश बिंदु: सभी प्रवेशार्थियों के पास वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज़ और, जहाँ लागू हो, वीज़ा होना आवश्यक है। प्रवेश और निकास निर्दिष्ट आव्रजन चौकियों तक ही सीमित हैं।
- आव्रजन अधिकारियों की भूमिका: अधिकारियों के पास राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के आधार पर प्रवेश को मान्य या अस्वीकार करने का अधिकार है।
- रिपोर्टिंग दायित्व: आवास प्रदाताओं को विदेशी मेहमानों के आगमन और प्रस्थान के 24 घंटे के भीतर उनका विवरण रिपोर्ट करना होगा।
- छूट प्राप्त श्रेणियाँ: कुछ समूह जैसे सैन्य कार्मिक, नेपाल और भूटान के नागरिक, तथा विशिष्ट शरणार्थी, मानक प्रवेश और वीज़ा आवश्यकताओं से मुक्त हैं।
- डिजिटल रिकॉर्ड: अधिनियम आवास और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ऑनलाइन अधिसूचनाओं को अनिवार्य बनाता है, जिससे निगरानी के लिए एक व्यापक डिजिटल डेटाबेस तैयार होता है।
- उल्लंघन के लिए जुर्माना: उल्लंघन के लिए जुर्माना 10,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक है, तथा विशिष्ट कमजोर समूहों के लिए जुर्माना कम किया गया है।
- शक्तियों का केंद्रीकरण: केंद्र सरकार आव्रजन पर प्राथमिक अधिकार रखती है, लेकिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कार्य सौंप सकती है।
आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम, 2025, आधुनिक प्रणालियों और स्पष्ट नियमों को लागू करके आव्रजन के प्रति भारत के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जो एक प्रभावी नियामक ढांचे के लिए आवश्यक है।
|
1 videos|3438 docs|1076 tests
|
FAQs on Indian Polity and Governance (भारतीय राजनीति और शासन): September 2025 UPSC Current Affairs - Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly
| 1. शरणार्थियों के लिए राहत के संदर्भ में आव्रजन और विदेशी (छूट) आदेश के मुख्य तत्व क्या हैं? |  |
| 2. आपराधिक मानहानि और लोकतांत्रिक बहस के बीच क्या संबंध है? |  |
| 3. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत हिरासत के प्रावधान क्या हैं? |  |
| 4. ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम के तहत कौन-कौन सी गतिविधियाँ शामिल हैं? |  |
| 5. डीएनए साक्ष्य पर सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देश क्या हैं? |  |





















