PIB Summary - 13th August 2025(Hindi) | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC PDF Download
भारत की लुप्तप्राय भाषाओं का दस्तावेजीकरण
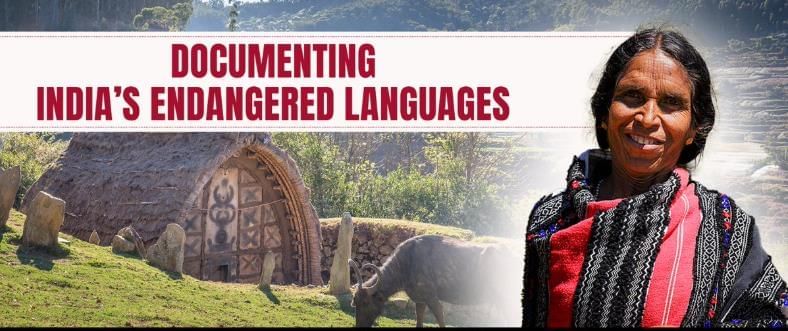
लुप्तप्राय भाषाओं का संदर्भ और महत्व
- भारत में एक विशाल भाषाई विविधता है, जिसमें 2,843 मातृ भाषाएँ 2011 की जनगणना में दर्ज की गई हैं।
- जिन भाषाओं में 10,000 से कम बोलने वाले होते हैं, उन्हें लुप्तप्राय माना जाता है, और वर्तमान में 117 ऐसी भाषाएँ SPPEL द्वारा पहचानी गई हैं।
- लुप्तप्राय भाषाएँ महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे केवल शब्द नहीं, बल्कि संस्कृति, मौखिक परंपराएँ, पारिस्थितिकी ज्ञान, अनुष्ठान और समुदायों की पहचान भी ले जाती हैं।
- उदाहरण के लिए, टोडा भाषा नीलगिरी पहाड़ियों में टोडा जनजाति के अपने पवित्र परिदृश्य और पूर्वजों के ज्ञान से संबंध के लिए महत्वपूर्ण है।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
- भारत की भाषाओं का पहला व्यवस्थित सर्वेक्षण जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1894 से 1928 के बीच किया, जिसमें ब्रिटिश भारत में 179 भाषाओं और 544 बोलियों का दस्तावेजीकरण किया गया।
- इस सर्वेक्षण ने भारत की भाषाई विविधता को समझने की नींव रखी।
- बाद के जनगणनाओं ने भाषाओं के मानचित्रण का विस्तार किया, जिसमें 1961 की जनगणना ने 1,652 मातृ भाषाएँ दर्ज कीं और 2011 की जनगणना ने 2,843 मातृ भाषाएँ दर्ज कीं, जिनमें से 1,369 को मान्यता प्राप्त थी और 1,474 को वर्गीकृत नहीं किया गया।
- SPPEL इस ऐतिहासिक नींव पर आधारित है ताकि कम दस्तावेजीकृत या गंभीर रूप से संकटग्रस्त भाषाओं को संरक्षित किया जा सके।
भारत में संकटग्रस्त भाषाओं का संरक्षण
SPPEL एक योजना है जिसे केंद्रीय भारतीय भाषाएँ संस्थान (CIIL) ने शिक्षा मंत्रालय के तहत लागू किया है। इसके उद्देश्यों में शामिल हैं:
- संकटग्रस्त भाषाओं की व्याकरण, शब्दावली और मौखिक परंपराओं का दस्तावेजीकरण करना,
- ऑडियो-विज़ुअल आर्काइव, चित्रात्मक शब्दकोश और द्विभाषी/त्रिभाषी शब्दकोश बनाना,
- सामग्री को डिजिटल रूप से संग्रहित करना ताकि वैश्विक पहुँच हो सके,
- आदिवासी भाषाओं में प्रारंभिक साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए प्राइमर और शैक्षिक सामग्री तैयार करना।
वर्तमान में, 117 संकटग्रस्त भाषाओं का दस्तावेजीकरण किया गया है, और लक्षित है कि लगभग 500 कम ज्ञात भाषाओं का भी दस्तावेजीकरण किया जाए।
अन्य सरकारी पहलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शामिल है, जो बहुभाषी अध्ययन और तीन-भाषा सूत्र को बढ़ावा देती है, और आदिवासी मामलों का मंत्रालय, जो TRI-ECE योजना के माध्यम से AI-आधारित भाषा संरक्षण को वित्त पोषित कर रहा है।
संस्कृति मंत्रालय और संबद्ध संगठन भी आदिवासी कला, मौखिक परंपराओं, पांडुलिपियों, त्योहारों और साहित्य उत्सवों को बढ़ावा देकर संकटग्रस्त भाषाओं का समर्थन कर रहे हैं।
वैश्विक दृष्टिकोण
- यूनेस्को का अनुमान है कि लगभग 50% वैश्विक 7,000 भाषाएँ संकटग्रस्त हैं।
- 2022 से 2032 का समय आदिवासी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया है, ताकि जागरूकता बढ़े और आदिवासी भाषाओं के संरक्षण को बढ़ावा मिले।
- विश्व के आदिवासी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 अगस्त को आदिवासी लोगों और उनकी भाषाओं के अधिकार, संस्कृति और संरक्षण को उजागर करता है।
एआई और स्वदेशी ज्ञान
- एआई स्वदेशी ज्ञान के लिए जोखिम और अवसर दोनों प्रस्तुत कर सकता है।
- जोखिमों में बिना सहमति के स्वदेशी ज्ञान का संभावित शोषण और उपनिवेशीय पैटर्नों का जारी रहना शामिल है।
- अवसरों में भाषा का पुनर्जीवित करना, अनुवाद उपकरण, और पारिस्थितिकी संरक्षण शामिल हैं।
- सकारात्मक एआई के उपयोग के उदाहरणों में पोलिनेशियन समुदायों द्वारा रीफ संरक्षण के लिए एआई का उपयोग और न्यूजीलैंड में माओरी भाषा का पुनर्जीवन शामिल है।
- भारत में, TRI-ECE योजना जनजातीय भाषाओं के लिए एआई अनुवाद उपकरण विकसित कर रही है, जैसे कि Bhashini, BITS Pilani, और IITs।
भारत में भाषाई विविधता
क्षेत्र के अनुसार
- उत्तर: 25 भाषाएँ (जैसे, स्पीति, जाद, गहरी)
- उत्तर-पूर्व: 43 भाषाएँ (जैसे, ऐमोली, तांगम, शेरदुक्पेन)
- पूर्व-मध्य: 15 भाषाएँ (जैसे, भुंजिया, बोंडो, तोतो)
- पश्चिम-मध्य: भाषाएँ (जैसे, निहाली, बराड़ी, भाला)
- दक्षिण: 20 भाषाएँ (जैसे, टोडा, सोलिगा, जेणुकुरुंबा)
- अंडमान और निकोबार: भाषाएँ (जैसे, सेंटिनलीज़, ओंगे, शोम्पेन)
भाषा परिवार के अनुसार
- इंडो-यूरेशियन: 24 भाषाएँ; 76.89% जनसंख्या
- द्रविड़: 17 भाषाएँ; 20.82% जनसंख्या
- ऑस्ट्रो-एशियाटिक: 14 भाषाएँ; 1.11% जनसंख्या
- तिबेटो-बर्मन: 66 भाषाएँ; 1% जनसंख्या
- सेमिटो-हमिटिक: भाषा; 0.01% जनसंख्या
आदिवासी भाषाओं का वितरण:
- तिबेटो-बर्मन: उत्तर और उत्तर-पूर्व भारत
- ऑस्ट्रो-एशियाटिक: मध्य और पूर्व भारत
- द्रविड़: दक्षिण भारत
- इंडो-यूरेशियन: भारत के अन्य भागों में
बहुभाषावाद और सांस्कृतिक निरंतरता
- भारत में बहुभाषावाद की उच्च डिग्री है, जिसमें 89.59 करोड़ एकभाषी, 22.90 करोड़ द्विभाषी, और 8.60 करोड़ त्रिभाषी हैं, जैसा कि 2011 की जनगणना में दर्शाया गया है।
- मुख्य भाषाओं में हिंदी, बंगाली और मराठी शामिल हैं, लेकिन संकटग्रस्त जनजातीय भाषाएँ इन प्रमुख भाषाओं के दबाव का सामना कर रही हैं।
- संकटग्रस्त जनजातीय भाषाओं को बनाए रखने के लिए संरक्षण प्रयास आवश्यक हैं, और SPPEL, जनजातीय मामलों के मंत्रालय के साथ मिलकर, त्रिभाषी और द्विभाषी पाठ्यपुस्तकों को बढ़ावा देता है ताकि धरोहर को बनाए रखते हुए प्रमुख भाषाओं में शिक्षा संभव हो सके।
दस्तावेज़ीकरण प्रक्रिया (SPPEL मॉडल)
- रिकॉर्डिंग चरण: स्वदेशी वक्ताओं से शब्दों, वाक्यों, गीतों और कहानियों को कैद करना।
- ट्रांसक्रिप्शन & विश्लेषण: मौखिक डेटा को लिखित रूप में परिवर्तित करना और व्याकरण एवं ध्वनिविज्ञान का विश्लेषण करना।
- व्याकरण निर्माण: वाक्यविन्यास और वाक्य निर्माण को व्यवस्थित रूप से दस्तावेज़ित करना।
- संस्कृति दस्तावेज़ीकरण: अनुष्ठानों, त्योहारों, आजीविका प्रथाओं और पवित्र परंपराओं को रिकॉर्ड करना।
- डिजिटल संग्रहण: वैश्विक पहुंच के लिए मेटाडेटा और डिजिटल रिपॉजिटरी बनाना।
- पुनर्जीवन: बच्चों के लिए सामुदायिक-प्रेरित प्रारंभिक पाठ्यक्रम और शैक्षिक सामग्री विकसित करना।
- प्रौद्योगिकी समर्थन: उच्च गुणवत्ता वाली ऑडियो/वीडियो रिकॉर्डिंग, भाषाई सॉफ़्टवेयर, और जुलाई 2025 में शुरू किए गए संचितिका पोर्टल जैसी डिजिटल रिपॉजिटरी का उपयोग करना।
संस्कृति दस्तावेज़ीकरण का उदाहरण:
- “Panuha Not: The Pig Festival Chowra” अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से एक उदाहरण है जहाँ सुअर के त्योहार और इसके महत्व को रिकॉर्ड और संरक्षित किया गया है।
भाषा संरक्षण में चुनौतियाँ
- विशेषकर बुजुर्गों के बीच मूल भाषियों की घटती संख्या, जो अंतर-पीढ़ीगत संचार के नुकसान का कारण बनती है।
- शिक्षा और मीडिया में प्रमुख भाषाओं का प्रभुत्व, संकटग्रस्त भाषाओं के उपयोग और प्रसारण को कम करता है।
- कुछ भाषाओं के लिए मूल लिपि की कमी, जैसे टोडा भाषा, जिसके कारण ट्रांसलिटरेशन और प्रमुख भाषाओं में प्राइमर्स का निर्माण आवश्यक हो जाता है।
- दूरदराज और जनजातीय क्षेत्रों में संसाधनों की कमी, दस्तावेज़ीकरण और संरक्षण प्रयासों में बाधा डालती है।
- स्थानीय ज्ञान के उपयोग में सहमति और स्वदेशी बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हुए नैतिक एआई तैनाती की आवश्यकता।
सामाजिक-संस्कृतिक निहितार्थ
- भाषा का खोना मौखिक इतिहास, अनुष्ठानों, पारिस्थितिकीय ज्ञान और उन विश्वदृष्टियों के खोने के समान है जो प्रत्येक समुदाय के लिए अद्वितीय हैं।
- भाषाओं का संरक्षण मानवाधिकार, सांस्कृतिक पहचान, संज्ञानात्मक विविधता, और स्वदेशी ज्ञान पर आधारित टिकाऊ प्रथाओं का समर्थन करता है।
- भाषा का संरक्षण पीढ़ियों के बीच निरंतरता को मजबूत करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि आधुनिक शिक्षा सांस्कृतिक जड़ों और प्रथाओं को बनाए रखते हुए संलग्न है।
- यह सामुदायिक सहभागिता और संरक्षण प्रयासों में भागीदारी को बढ़ावा देता है, सामाजिक एकता और पहचान को मजबूत करता है।
मुख्य निष्कर्ष
- भारत की भाषाई पारिस्थितिकी प्रणाली समृद्ध लेकिन नाज़ुक है, जिसके लिए खतरे में पड़ी भाषाओं की सुरक्षा और पुनर्जीवन की आवश्यकता है।
- SPPEL खतरे में पड़ी भाषाओं के दस्तावेज़ीकरण और संरक्षण के लिए एक संरचित और तकनीकी रूप से संचालित ढांचा प्रदान करता है।
- AI संरक्षण के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है, लेकिन यदि नैतिकता से उपयोग नहीं किया गया, तो यह शोषण का खतरा भी पैदा कर सकता है।
- बहुभाषावाद, दस्तावेज़ीकरण, सांस्कृतिक मानचित्रण, और साक्षरता कार्यक्रमों को बढ़ावा देने वाली पहलों का सतत भाषा संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण होना आवश्यक है।
- वैश्विक और राष्ट्रीय प्रयास इस बात को सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं कि स्वदेशी भाषाएं न केवल जीवित रहें, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए फल-फूल सकें, जिससे सांस्कृतिक और भाषाई विविधता में योगदान हो।
पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण पर चिंताओं का जवाब

संदर्भ और नीतिगत पृष्ठभूमि
- एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम (EBP): यह एक राष्ट्रीय प्रयास है, जिसमें पेट्रोल के साथ एथेनॉल का मिश्रण किया जाता है ताकि कच्चे तेल पर निर्भरता कम की जा सके और स्वच्छ ईंधनों को बढ़ावा दिया जा सके।
- भारत का ऊर्जा संक्रमण राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान (NDCs) के अनुसार है, जिसका उद्देश्य 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना है।
- जैव ईंधन और प्राकृतिक गैस संक्रमणीय ईंधन के रूप में कार्य करते हैं, जो जलवायु और ऊर्जा लक्ष्यों का समर्थन करते हैं बिना बड़े व्यवधान उत्पन्न किए।
- एथेनॉल मिश्रण के लक्ष्यों में शामिल हैं:
- ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन को कम करना।
- कच्चे तेल के आयात को कम करके ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना।
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना और किसानों की आय में वृद्धि करना।
पर्यावरण और सामाजिक-आर्थिक लाभ
जीएचजी उत्सर्जन में कमी:
- गन्ना आधारित एथेनॉल: पेट्रोल की तुलना में 65% कम उत्सर्जन उत्पन्न करता है।
- मक्का आधारित एथेनॉल: NITI आयोग के अध्ययन के अनुसार, पेट्रोल की तुलना में 50% कम उत्सर्जन का परिणाम देता है।
- CO₂ में कमी: E-20 को अपनाने से लगभग 736 लाख टन CO₂ की बचत होने की उम्मीद है, जो 30 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है।
ऊर्जा सुरक्षा:
- कच्चे तेल का विकल्प: 2014-15 से लगभग 245 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल का विकल्प रखा गया है।
- विदेशी मुद्रा की बचत: 2014-15 से 2024-25 तक 1,44,087 करोड़ रुपये की बचत की गई है।
- अपेक्षित बचत: 2025-26 तक 20% मिश्रण के साथ अनुमानित 43,000 करोड़ रुपये की बचत की उम्मीद है।
किसान कल्याण:
- गन्ना और मक्का उगाने वाले किसानों की आय में वृद्धि।
- किसान distress को कम करने और आत्महत्या की दर को घटाने में योगदान, विशेष रूप से विदर्भ जैसे क्षेत्रों में।
- किसान “उर्जादाता” बन रहे हैं, जो ऊर्जा उत्पादन में योगदान दे रहे हैं, इसके अलावा अपनी पारंपरिक भूमिका “अन्नदाता” के रूप में।
E-20 के तकनीकी लाभ
ईंधन प्रदर्शन:
- उच्च ऑक्टेन रेटिंग: E-20 की ऑक्टेन रेटिंग लगभग 108.5 है, जबकि पेट्रोल की 84.4 है। इससे बेहतर एंटी-नॉकिंग गुण और तेजी में सुधार होता है।
- उच्च वाष्पीकरण ताप: E-20 का उच्च वाष्पीकरण ताप इनटेक मैनिफोल्ड तापमान को कम करता है और एयर-फ्यूल मिश्रण की घनत्व को बढ़ाता है, जिससे वॉल्यूमेट्रिक दक्षता में सुधार होता है।
प्रदूषण में कमी:
- E-20 का उपयोग करने पर कार्बन उत्सर्जन E-10 की तुलना में लगभग 30% कम हो जाता है।
ईंधन मानक:
- BS-VI मानकों के तहत नियमित पेट्रोल का रिसर्च ऑक्टेन नंबर (RON) 88 से बढ़ाकर 91 कर दिया गया है, और E-20 के परिचय के साथ इसे 95 तक बढ़ाया गया है।
वाहन संगतता:
- 2009 के बाद निर्मित कई वाहन पहले से ही E-20 ईंधन के साथ संगत हैं।
- दक्षता: E-10 के लिए डिज़ाइन किए गए वाहनों में दक्षता में न्यूनतम गिरावट होती है, और E-20 संगत वाहनों पर प्रभाव नगण्य होता है।
चिंताओं का समाधान
माइलेज और प्रदर्शन:
- माइलेज और प्रदर्शन कई कारकों से प्रभावित होते हैं, जिनमें ड्राइविंग आदतें, वाहन रखरखाव, टायर दबाव, और एयर कंडीशनर का लोड शामिल हैं।
- E-20 के साथ “गंभीर दक्षता में गिरावट” के दावे गलत हैं।
वाहन जीवन:
- पुराने वाहनों को E-20 का उपयोग करते समय रबर के हिस्सों और गैसकेट्स के occasional प्रतिस्थापन की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन यह वाहन सेवा का एक नियमित और सस्ता हिस्सा है।
बीमा:
- E-20 ईंधन का उपयोग करने से वाहन बीमा पॉलिसियों की वैधता समाप्त नहीं होती है। इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर फैली गलत जानकारी को बीमा कंपनियों ने स्पष्ट किया है।
मूल्य चिंताएँ:
- ईथेनॉल की कीमत वर्षों में बढ़ी है, जिसमें C-heavy मोलासेस ईथेनॉल की कीमत 46.66 रुपये से बढ़कर 57.97 रुपये और मक्का ईथेनॉल की कीमत 52.92 रुपये से बढ़कर 71.86 रुपये हो गई है, जो 2021-22 से 2024-25 के बीच है।
- ब्लेंडेड ईंधन की कीमतें इन लागत परिवर्तनों को दर्शाती हैं, और कार्यक्रम जारी है, भले ही ईथेनॉल की कीमत पेट्रोल से अधिक हो।
वैश्विक मानककरण
- ब्राज़ील: कई वर्षों से E27 ईंधन का सफलतापूर्वक उपयोग कर रहा है बिना किसी महत्वपूर्ण समस्याओं का सामना किए।
- वाहन निर्माता: कंपनियों जैसे टोयोटा, होंडा और हुंडई ऐसे वाहनों का उत्पादन करती हैं जो भारत में E-20 और ब्राज़ील में समान मानकों के साथ संगत हैं।
- मानक: भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) और ऑटोमोटिव उद्योग मानक सुनिश्चित करते हैं कि वाहन ड्राइव करने की क्षमता, प्रारंभ करने की क्षमता और धातु एवं प्लास्टिक भागों की संगतता के लिए आवश्यक मानदंडों को पूरा करते हैं जब E-20 ईंधन का उपयोग किया जाता है।
रणनीतिक और नीति संबंधी अंतर्दृष्टियाँ
क्रमिक कार्यान्वयन:
- E-20 कार्यान्वयन के लिए रोडमैप 2021 में भारतीय मोटर वाहन (IMC) रिपोर्ट में विस्तृत किया गया था, जिससे वाहन प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला समायोजन में समय मिला।
- सरकार ने 31 अक्टूबर 2026 तक E-20 कार्यान्वयन का वचन दिया है।
ऊर्जा परिवर्तन दर्शन:
- पर्यावरण प्रदूषण में कमी और ऊर्जा सुरक्षा के लाभों को बनाए रखने के लिए E-0 पेट्रोल पर वापस न लौटने पर जोर दिया जा रहा है।
एकीकृत हितधारक सहभागिता:
- वाहन निर्माताओं, Oil Marketing Companies (OMCs), एथेनॉल उत्पादकों और अनुसंधान एवं विकास एजेंसियों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ सहयोग E-20 ईंधन में सुचारू संक्रमण के लिए महत्वपूर्ण है।
आर्थिक प्रभाव
- किसानों को ईंधन मिश्रण के लिए इथेनॉल की खरीद के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ मिलते हैं।
- विदेशी कच्चे तेल पर निर्भरता में कमी से महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा की बचत होती है।
- ग्रामीण रोजगार का समर्थन करता है और मक्का और गन्ना की खेती की संभाव्यता सुनिश्चित करता है।
- भारत की ऊर्जा स्वावलंबन को मजबूत करता है और अर्थव्यवस्था में स्थानीय मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देता है।
संवाद और सार्वजनिक धारणा
- सरकार ई-20 ईंधन के उपयोग के संबंध में गलत जानकारी का मुकाबला करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है, विशेष रूप से दक्षता, बीमा, और लागत के मुद्दों पर।
- सोशल मीडिया में उठने वाले भय को आधिकारिक स्पष्टीकरण और डेटा-आधारित प्रतिक्रियाओं के माध्यम से हल किया जाता है।
- ओरिजिनल इकिपमेंट मैन्युफैक्चरर्स (OEMs) उपभोक्ताओं के साथ संवाद करते हैं ताकि वे वाहन की ट्यूनिंग या आवश्यक पार्ट्स के प्रतिस्थापन के लिए समर्थन प्रदान कर सकें, जिससे E-20 ईंधन के साथ संगतता सुनिश्चित हो सके।
सारांश: मुख्य बिंदु
- E-20 ईंधन को सुरक्षित, पर्यावरण के अनुकूल और आर्थिक रूप से लाभकारी माना जाता है।
- यह पहल जलवायु लक्ष्य का समर्थन करती है, किसान की आय बढ़ाती है और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करती है।
- प्रदर्शन और माइलेज के बारे में चिंताएँ अधिकांशतः बढ़ा-चढ़ा कर बताई जाती हैं; उचित वाहन रखरखाव दीर्घकालिकता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
- वैश्विक उदाहरण और वाहन निर्माण मानक E-20 ईंधन के उपयोग की तकनीकी संभावना की पुष्टि करते हैं।
- सरकार ने E-20 ईंधन से आगे बढ़ने से पहले हितधारकों की भागीदारी को प्राथमिकता देते हुए एक सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध कार्यान्वयन रोडमैप का आश्वासन दिया है।
भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2025 पारित: प्रतिस्पर्धात्मक और टिकाऊ भविष्य के लिए समुद्री शासन का आधुनिकीकरण

संक्षिप्त विवरण एवं प्रमुख विशेषताएँ
- बंदरगाह शासन का आधुनिकीकरण: यह विधेयक 1908 के भारतीय बंदरगाह अधिनियम के पुराने नियमों को अपडेट करता है ताकि वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।
- व्यवसाय करने में आसानी (EODB): यह बंदरगाह प्रक्रियाओं को सरल बनाता है और व्यापार और लॉजिस्टिक्स को अधिक कुशल बनाने के लिए संचालन को डिजिटाइज़ करता है।
- स्थिरता और लचीलापन: यह विधेयक हरित पहलों, प्रदूषण नियंत्रण उपायों और आपदा प्रबंधन प्रोटोकॉल को शामिल करता है।
- प्रतिस्पर्धात्मकता और निवेश: यह पारदर्शी टैरिफ मानदंड स्थापित करता है, निवेश ढाँचे में सुधार करता है, और सार्वजनिक-निजी साझेदारियों (PPPs) और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करता है।
- लॉजिस्टिक्स दक्षता: यह कार्गो आंदोलन को तेज करने, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने और कनेक्टिविटी को बढ़ाने का लक्ष्य रखता है, जिससे निर्यातकों और सूक्ष्म, लघु, और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को लाभ होगा।
- रोजगार सृजन: इस विधेयक से बंदरगाह संचालन, लॉजिस्टिक्स, गोदाम, और संबंधित उद्योगों में अधिक नौकरियाँ उत्पन्न होने की उम्मीद है।
संस्थानिक तंत्र
मैरिटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (MSDC):
- संघीय और राज्य स्तर पर एक निकाय, जिसका उद्देश्य बंदरगाह विकास नीतियों को समन्वित करना और सहकारी संघवाद को मजबूत करना है।
राज्य मैरिटाइम बोर्ड:
- ये बोर्ड गैर-मुख्य बंदरगाहों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने के लिए सशक्त हैं, जो विकेंद्रीकृत शासन को बढ़ावा देते हैं।
विवाद समाधान समितियाँ:
- बंदरगाहों, सेवा प्रदाताओं, और उपयोगकर्ताओं के बीच संघर्षों के त्वरित समाधान के लिए स्थापित की गई हैं।
सुरक्षा और पर्यावरण अनुपालन
कचरा प्रबंधन सुविधाएँ:
- पोर्ट्स को अनिवार्य कचरा रिसेप्शन और प्रोसेसिंग के लिए आधारभूत संरचना होनी चाहिए।
प्रदूषण नियंत्रण:
- अंतरराष्ट्रीय संधियों जैसे MARPOL और Ballast Water Management के साथ संरेखित।
आपातकालीन तैयारी:
- सभी पोर्ट्स को आपदा और सुरक्षा तत्परता के लिए योजनाएँ होनी चाहिए।
नवीकरणीय ऊर्जा और तट शक्ति:
- उत्सर्जन कम करने के लिए तट शक्ति का उपयोग करने जैसी पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देना।
रणनीतिक संरेखण
- यह विधेयक मौजूदा सरकारी पहलों जैसे सागरमाला कार्यक्रम और मैरिटाइम इंडिया विज़न 2030 के साथ संरेखित है।
- यह भारत के 2047 तक बंदरगाहों को सतत आर्थिक विकास और वैश्विक व्यापार नेतृत्व के इंजन बनाने के लक्ष्य का समर्थन करता है।
आगे का रास्ता
- भारतीय पोर्ट्स बिल, 2025, भारत के समुद्री ढांचे और शासन को आधुनिक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार का प्रतिनिधित्व करता है।
- संविधान, स्थिरता, और प्रतिस्पर्धात्मकता पर जोर देते हुए, यह विधेयक MSMEs के विकास, क्षेत्रीय विकास, और वैश्विक व्यापार में एकीकरण को बढ़ावा देता है।
- MSDC और राज्य समुद्री बोर्डों जैसे संस्थानों की स्थापना समन्वित योजना सुनिश्चित करती है, जबकि पर्यावरण और सुरक्षा मानकों पर ध्यान जिम्मेदार विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- प्रभावी कार्यान्वयन, सरकारों के बीच सहयोग, क्षमता निर्माण, और निगरानी विधेयक की पूरी संभावनाओं को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण होंगे।
|
3433 docs|1075 tests
|
FAQs on PIB Summary - 13th August 2025(Hindi) - Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC
| 1. भारत की लुप्तप्राय भाषाओं का दस्तावेजीकरण क्यों आवश्यक है? |  |
| 2. लुप्तप्राय भाषाओं के संरक्षण के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं? |  |
| 3. पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण को लेकर क्या चिंताएं हैं? |  |
| 4. भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2025 का उद्देश्य क्या है? |  |
| 5. भारत में लुप्तप्राय भाषाओं की स्थिति क्या है? |  |















