PIB Summary - 30th July 2025(Hindi) | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC PDF Download
बाएं विंग चरमपंथ में कमी

भारत में बाएं विंग चरमपंथ: वर्तमान स्थिति और सरकारी प्रतिक्रिया
भारत में बाएं विंग चरमपंथ (LWE), जो कभी एक महत्वपूर्ण आंतरिक सुरक्षा चुनौती था, अब एक व्यापक सुरक्षा और विकास रणनीति के कारण उल्लेखनीय कमी देख रहा है, जिसे 2015 में राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना के तहत लागू किया गया था।
- LWE हिंसा में कमी: LWE हिंसा की घटनाओं में 80% से अधिक की कमी आई है, और 2013 में प्रभावित जिलों की संख्या 126 से घटकर 2025 में केवल 18 रह गई है।
- समन्वित प्रयास: LWE हिंसा में कमी की सफलता का श्रेय केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच समन्वित प्रयासों को दिया जाता है।
नीति और रणनीतिक ढांचा
राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना (2015) एक बहुआयामी दृष्टिकोण प्रदान करती है जिसमें सुरक्षा, विकास, और सामुदायिक अधिकारों का संरक्षण शामिल है, जिससे LWE (लेफ्ट-विंग एक्स्ट्रीमिज़म) का प्रभावी ढंग से मुकाबला किया जा सके।
हालांकि कानून और व्यवस्था मुख्य रूप से राज्यों की जिम्मेदारी है जैसा कि संविधान के सातवें अनुसूची में उल्लेखित है, केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों का समर्थन और पूरक भूमिका निभाती है।
यह रणनीति कई प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है:
- सुरक्षा को मज़बूत करना: LWE का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए सुरक्षा उपायों को बढ़ाना।
- विकास हस्तक्षेप: उग्रवाद के मूल कारणों को संबोधित करने के लिए विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन।
- सामुदायिक भागीदारी और अधिकार: विकास प्रक्रिया में समुदायों को शामिल करना और उनके अधिकारों और हक का संरक्षण सुनिश्चित करना।
सुरक्षा उपाय
- सुरक्षा संबंधित व्यय (SRE) योजना (2014–2025): इस योजना के तहत कुल ₹3,357 करोड़ जारी किए गए हैं, जिसमें झारखंड के लिए ₹830.75 करोड़ आवंटित किए गए हैं। ये फंड संचालन लागत, अनुग्रह भुगतान और आत्मसमर्पण किए गए कैडरों के पुनर्वास के लिए हैं।
- विशेष अवसंरचना योजना (SIS): इस योजना के तहत ₹1,740 करोड़ के कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें झारखंड के लिए ₹439.45 करोड़ आवंटित किए गए हैं। ये फंड राज्य खुफिया शाखाओं, विशेष बलों, जिला पुलिस और 71 सुदृढ़ पुलिस स्टेशनों (FPS) को मजबूत करने के लिए उपयोग किए जाते हैं।
सुरक्षा परिणाम
- 2010 से LWE से संबंधित हिंसा की घटनाओं में 81% की कमी आई है।
- LWE के कारण नागरिकों और सुरक्षा बलों की मौतों में 2024 तक 85% की कमी आई है।
- LWE से प्रभावित जिलों की संख्या 2013 में 126 से घटकर 2025 में 18 हो गई है।
अवसंरचना विकास
- सड़क संपर्क:
- अनुमोदित: 17,589 किमी (जिसमें 3,168 किमी झारखंड में)
- निर्मित: 14,902 किमी (जिसमें 2,925 किमी झारखंड में)
- टेलीकॉम संपर्क: टावर्स की योजना: 10,644 (जिसमें 1,755 झारखंड में)
- टावर्स चालू: 8,640 (जिसमें 1,589 झारखंड में)
कौशल विकास और शिक्षा
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI): 48 अनुमोदित, 46 कार्यशील (जिसमें 16 कार्यशील ITI झारखंड में)
- कौशल विकास केंद्र (SDC): 61 अनुमोदित, 49 कार्यशील (जिसमें 20 कार्यशील SDC झारखंड में)
- एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS): 258 अनुमोदित, 179 कार्यशील (जिसमें 47 कार्यशील विद्यालय झारखंड में)
वित्तीय समावेशन
- बैंकिंग सेवाओं के साथ डाकघर: कुल 5,899 (जिसमें झारखंड में 1,240)
- एलडब्ल्यूई जिलों में बैंक शाखाएँ: कुल 1,007 (जिसमें झारखंड में 349)
- स्थापित एटीएम: कुल 937 (जिसमें झारखंड में 352)
विशेष केंद्रीय सहायता (SCA)
- 2017 से, SCA योजना के तहत कुल ₹3,769 करोड़ जारी किए गए हैं, जिसमें झारखंड के लिए ₹1,439.33 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इस सहायता का उद्देश्य सबसे अधिक एलडब्ल्यूई-प्रभावित जिलों में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की कमी को पूरा करना है।
समर्पण और पुनर्वास पहलों
- केंद्र सरकार पुनर्वास की लागत को वापस करने और समर्पण के लिए अनुदान प्रदान करके राज्य की नीतियों का समर्थन करती है।
- समर्पण के लिए अनुदान में उच्च LWE कैडरों के लिए ₹5 लाख और निचले कैडरों के लिए ₹2.5 लाख शामिल हैं, साथ ही हथियार समर्पण के लिए प्रोत्साहन भी दिया जाता है। तीन वर्षों के लिए प्रति माह ₹10,000 का व्यावसायिक प्रशिक्षण समर्थन भी प्रदान किया जाता है।
झारखंड से डेटा (जनवरी 2024 – 15 जुलाई 2025):
- हिंसक घटनाएँ: 103
- LWE कैडर तटस्थ किए गए: 25
- गिरफ्तार: 276
- समर्पण किया: 32
झारखंड में गिरावट
- हिंसक घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है, जो 2009 में 742 से घटकर 2024 में 69 हो गई है, जो 92% की गिरावट दर्शाता है।
- झारखंड में LWE (लेफ्ट-विंग एक्सट्रीमिज़्म) से प्रभावित जिलों की संख्या 2013 में 21 से घटकर 2025 में केवल 2 रह गई है। इसके अलावा, 7 जिलों को “लेगेसी और थ्रस्ट” जिलों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें निरंतर ध्यान की आवश्यकता है।
प्रभाव और निष्कर्ष
- LWE की हिंसा और भौगोलिक प्रसार में तीव्र संकुचन हुआ है, जिसमें प्रभावित जिलों और घटनाओं की संख्या में निरंतर गिरावट आई है।
- व्यापक राज्य निर्माण उपायों, जिनमें सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा, कौशल विकास, और समावेश शामिल हैं, ने शासन और विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है।
- झारखंड में लागू किया गया मॉडल, जो हिंसा में महत्वपूर्ण कमी और विकासात्मक निवेश में भारी वृद्धि द्वारा विशेषता है, यह आतंकवाद विरोधी विकास के लिए एक मूल्यवान केस स्टडी के रूप में कार्य करता है।
- केंद्र और राज्यों के बीच सहयोगात्मक ढांचा चरमपंथ को निष्प्रभावी करने में प्रभावी साबित हुआ है, जबकि संस्थानों को मजबूत करके और कमजोर जनसंख्या को उठाने में मदद मिली है।
आत्मनिर्भर तेल बीज अभियान
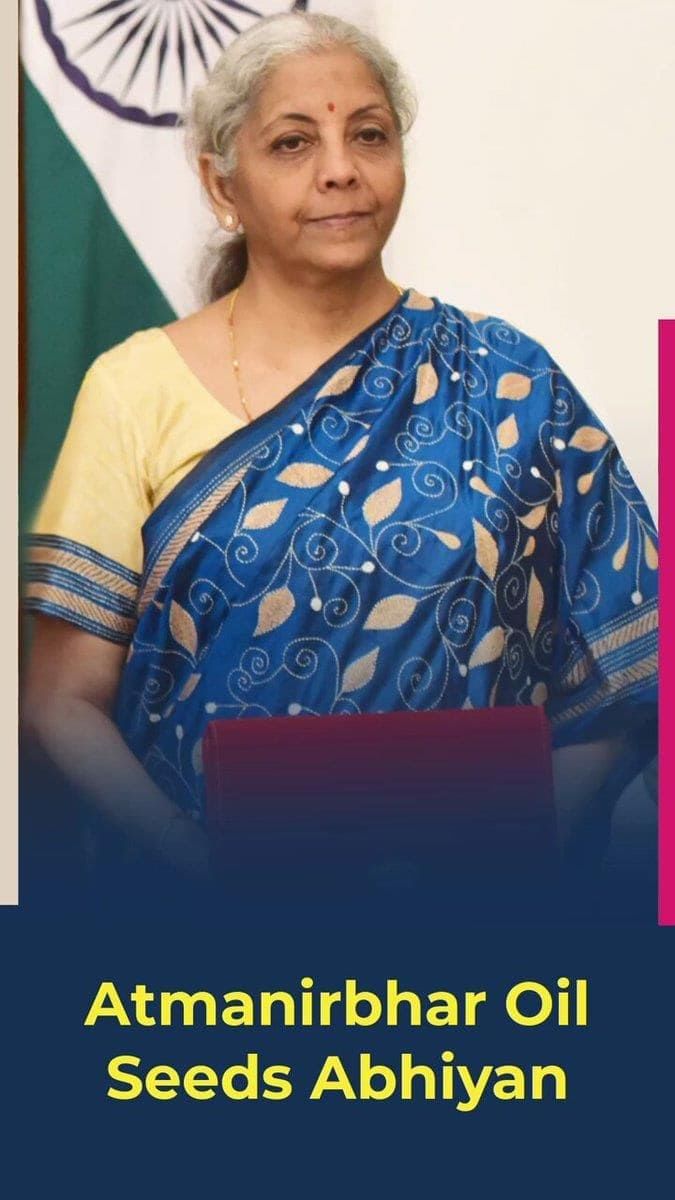
राष्ट्रीय मिशन ऑन एडेबल ऑइल्स – ऑइल पाम (NMEO-OP)
राष्ट्रीय मिशन ऑन एडेबल ऑइल्स – ऑइल पाम (NMEO-OP) का उद्देश्य भारत में ताड़ के तेल का उत्पादन बढ़ाना है, जिससे आयात पर निर्भरता कम हो और खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिले। यह मिशन ताड़ के पौधों की खेती के तहत क्षेत्र को बढ़ाने, बेहतर पौध सामग्री और प्रबंधन प्रथाओं के माध्यम से उपज में सुधार करने, और ताड़ के तेल के प्रसंस्करण और विपणन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की स्थापना सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करता है।
यह पहल घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जो महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत विश्व में खाद्य तेलों का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और अपनी मांग को पूरा करने के लिए भारी मात्रा में आयात पर निर्भर है। ताड़ के पौधों की खेती को बढ़ावा देकर, सरकार इस उच्च-उत्पादक फसल की संभावनाओं का लाभ उठाने की कोशिश कर रही है, जो खाद्य तेलों की घरेलू आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान कर सकती है।
परिचय
- उद्देश्य: घरेलू तेल बीज उत्पादन और प्रसंस्करण दक्षता बढ़ाकर खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना।
- लक्षित फसलें: प्राथमिक तेल बीज फसलों और पेड़ से उत्पन्न तेल बीजों, चावल की भूसी, और कपास के बीज जैसे द्वितीयक स्रोतों पर ध्यान केंद्रित करना।
लक्षित तेल बीज फसलें
प्राथमिक तेल बीज फसलें: प्रमुख फसलें जिनमें शामिल हैं: मूंगफली, सोयाबीन, सरसों, सूरजमुखी, तिल, केनोला, नाइजर, अलसी, और अरंडी।
द्वितीयक स्रोत: कपास के बीज, नारियल, चावल की भूसी, और पेड़ से उत्पन्न तेल बीज (TBOs)।
अनुसंधान और नवाचार (ICAR पहलों)
- अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाएँ (AICRPs): विशेष स्थानों के लिए उपयुक्त उच्च-उत्पादक किस्मों के विकास पर केंद्रित परियोजनाएँ।
- फ्लैगशिप परियोजनाएँ: जलवायु-प्रतिरोधी तेल बीज किस्में बनाने के लिए हाइब्रिड किस्मों के विकास और जीन संपादन प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर केंद्रित प्रमुख पहलों।
- उच्च-उत्पादक किस्में (HYVs) जारी की गईं: विभिन्न तेल बीज फसलों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए कुल 432 नई उच्च-उत्पादक किस्में जारी की गईं।
- किस्मीय प्रतिस्थापन दर (VRR) और बीज प्रतिस्थापन दर (SRR): कुल उत्पादकता बढ़ाने के लिए नए किस्मों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना।
बीज आपूर्ति पारिस्थितिकी तंत्र
- प्रजनक बीज उत्पादन: प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए सार्वजनिक और निजी एजेंसियों को महत्वपूर्ण मात्रा में प्रजनक बीजों का उत्पादन और आपूर्ति।
- जिला स्तर पर बीज हब: किसानों के लिए गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हब की स्थापना।
क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण
- मूल्य श्रृंखला क्लस्टर: भारत भर में 600 से अधिक क्लस्टर स्थापित किए गए हैं, जो वार्षिक 10 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को कवर करते हैं।
- प्रबंधन: क्लस्टर का प्रबंधन किसान उत्पादक संगठनों (FPOs), सहकारी समितियों, और निजी मूल्य श्रृंखला भागीदारों (VCPs) द्वारा किया जाता है।
- किसानों को समर्थन: उच्च गुणवत्ता वाले बीज, अच्छे कृषि प्रथाओं (GAPs) में प्रशिक्षण, मौसम और कीट सलाह सेवाएँ, और तेल निकालने और पुनर्प्राप्ति के लिए पोस्ट-हार्वेस्ट बुनियादी ढांचे का निःशुल्क प्रावधान।
प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और जागरूकता
- प्रदर्शन प्रकार: ICAR, KVKs, और राज्य कृषि विभागों द्वारा सबसे अच्छी प्रथाओं और नई प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- सूचना, शिक्षा, और संचार (IEC) अभियान: स्वस्थ तेल उपभोग पैटर्न को बढ़ावा देने और घरेलू तेल बीज उत्पादन के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान।
बीमा और जोखिम प्रबंधन (PMFBY 2024-25)
- कवरेज: खरीफ और रबी सीजन के दौरान 16 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में तेल बीज फसलों के लिए व्यापक बीमा कवरेज।
- मुख्य बीमित फसलें: सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, सूरजमुखी, अलसी, नाइजर, केनोला, अरंडी।
- वित्तीय सुरक्षा: बीमा योजनाएँ तेल बीज किसानों को फसल विफलताओं के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती हैं और स्थिर आय सुनिश्चित करती हैं।
रणनीतिक महत्व
- आयात पर निर्भरता: भारत वर्तमान में अपने खाद्य तेल की आवश्यकताओं का 60% से अधिक आयात करता है, जिसके साथ एक महत्वपूर्ण आयात बिल है।
- आयात पर निर्भरता में कमी: NMEO-OS का उद्देश्य आयात पर निर्भरता को कम करना, मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करना, और पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देना है।
सामना करने के लिए चुनौतियाँ
- कम उत्पादकता: वैश्विक औसत की तुलना में भारत में तेल बीजों की कम उत्पादकता को संबोधित करना।
- आपूर्ति श्रृंखला का विखंडन: विखंडित आपूर्ति श्रृंखलाओं में सुधार करना और तेल की पुनर्प्राप्ति दरों को बढ़ाना।
- जलवायु संवेदनशीलता: जलवायु संवेदनशीलता के प्रभावों को कम करना जो तेल बीज उपज की स्थिरता पर प्रभाव डालते हैं।
- बुनियादी ढांचे में सुधार: तेल बीजों के प्रसंस्करण और भंडारण के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे का विकास करना।
आगे का रास्ता
- निजी क्षेत्र की भागीदारी: बीज उत्पादन और प्रसंस्करण में निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- कोल्ड-प्रेस्ड तेल निष्कर्षण में निवेश: कोल्ड-प्रेस्ड तेल निष्कर्षण विधियों और जैविक तेल बीज कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देना।
- पोषण कार्यक्रमों के साथ एकीकरण: तेल बीज प्रचार प्रयासों को पोषण-केंद्रित कार्यक्रमों जैसे कि POSHAN Abhiyan से जोड़ना।
- बाजार लिंकिंग: मूल्य श्रृंखला क्लस्टर को इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) और निर्यात बाजारों के साथ जोड़ना ताकि बेहतर मूल्य प्राप्त किया जा सके।
|
7 videos|3454 docs|1081 tests
|
FAQs on PIB Summary - 30th July 2025(Hindi) - Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC
| 1. बाएं विंग चरमपंथ क्या है और यह समाज पर किस प्रकार का प्रभाव डालता है? |  |
| 2. आत्मनिर्भर तेल बीज अभियान का उद्देश्य क्या है? |  |
| 3. बाएं विंग चरमपंथ में कमी लाने के लिए कौन से प्रयास किए गए हैं? |  |
| 4. भारत में तेल बीज उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन से प्रमुख नीतिगत परिवर्तन किए गए हैं? |  |
| 5. बाएं विंग चरमपंथ और आत्मनिर्भरता अभियान के बीच क्या संबंध है? |  |





















