UPSC Exam > UPSC Notes > Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly > The Hindi Editorial Analysis- 12th February 2025
The Hindi Editorial Analysis- 12th February 2025 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC PDF Download
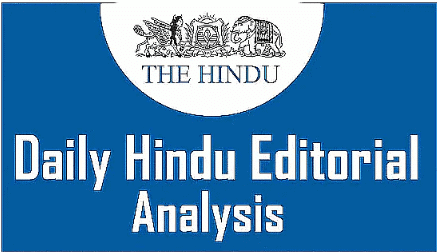
दक्षिण-दक्षिण जलवायु सहयोग में भारत की भूमिका
यह समाचार योग्य क्यों है?
- COP29 का आयोजन बाकू, अज़रबैजान में हुआ, जिसमें जलवायु वित्त और पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जो कार्बन क्रेडिट के व्यापार से संबंधित है।
- भारत, ग्रीनहाउस गैसों का एक प्रमुख उत्सर्जक होने के नाते, जलवायु उद्देश्यों के साथ अपनी विकासात्मक आवश्यकताओं को संतुलित करने का प्रयास करते हुए, वित्तीय और तकनीकी सहायता प्राप्त करने के लिए अनुच्छेद 6.2 का उपयोग करना चाहता है।
सीओपी29 और अनुच्छेद 6.2 का महत्व
- COP29 को 'जलवायु वित्त COP' नाम दिया गया है क्योंकि इसमें पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के प्रमुख घटकों के कार्यान्वयन पर जोर दिया गया है।
- अनुच्छेद 6 बाजार तंत्र स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण है, जो देशों को, विशेष रूप से सीमित संसाधनों वाले देशों को, कार्बन-तटस्थ अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने में सहायता करता है।
- इस लेख का एक महत्वपूर्ण पहलू, अनुच्छेद 6.2 , अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हस्तांतरित शमन परिणामों (आईटीएमओ) की अवधारणा को सुगम बनाता है । यह तंत्र देशों को एक दूसरे के बीच उत्सर्जन में कमी को स्थानांतरित करने की अनुमति देता है।
- यह प्रणाली विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है क्योंकि यह उन्हें विकसित देशों से आवश्यक वित्तीय, तकनीकी और क्षमता निर्माण सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। इन देशों के लिए अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) और सतत विकास लक्ष्यों (SDG) को प्राप्त करने के लिए ऐसा समर्थन महत्वपूर्ण है।
अनुच्छेद 6.2 पर भारत का रुख
- भारत, जो वैश्विक स्तर पर ग्रीनहाउस गैसों का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है , को अपनी विकासात्मक आवश्यकताओं को जलवायु प्रतिबद्धताओं के साथ संतुलित करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, विशेष रूप से इसकी वित्तीय सीमाओं को देखते हुए।
- देश ने 2030 तक अपनी उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करने का संकल्प लिया है , लेकिन इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय और तकनीकी सहायता की आवश्यकता है।
- COP29 से पहले, भारत ने विकसित देशों द्वारा इन प्रयासों के समर्थन हेतु जलवायु वित्त हेतु प्रतिवर्ष कम से कम 1 ट्रिलियन डॉलर जुटाने की आवश्यकता पर बल दिया था ।
भारत का घरेलू कार्बन बाज़ार और पिछला अनुभव
- 2023 में, भारत ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (CCTS) शुरू की , जिसका उद्देश्य कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग के लिए अपनी राष्ट्रीय नीतियों में बाज़ार तंत्र को शामिल करना है।
- यद्यपि सीसीटीएस सीधे तौर पर अनुच्छेद 6.2 से संबद्ध नहीं है, फिर भी यह कार्बन क्रेडिट की पारदर्शी ट्रैकिंग और सत्यापन के लिए भारत की रूपरेखा को बढ़ाता है।
- भारत का विभिन्न कार्बन बाज़ार पहलों में शामिल होने का इतिहास रहा है, जिनमें शामिल हैं:
- स्वच्छ विकास तंत्र (सीडीएम)
- स्वैच्छिक कार्बन बाज़ार (वीसीएम)
- ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र (ESCerts)
- नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी)
- यह पूर्व अनुभव भारत को अनुच्छेद 6.2 के अंतर्गत आईटीएमओ लेनदेन में भाग लेने के लिए अनुकूल स्थिति प्रदान करता है।
अनुच्छेद 6.2 के अंतर्गत भारत के लिए सहयोग के क्षेत्र
- भारत ने अनुच्छेद 6.2 के अंतर्गत संभावित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए 14 प्रमुख गतिविधियों की पहचान की है , जिसका उद्देश्य निम्नलिखित क्षेत्रों में विशेषज्ञता और निवेश आकर्षित करना है:
- नवीकरणीय ऊर्जा (आरई)
- ऊर्जा भंडारण
- कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (सीसीयूएस)
- हरित हाइड्रोजन और टिकाऊ विमानन ईंधन
- इन परियोजनाओं के लिए उन्नत तकनीकी विशेषज्ञता और महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता है, जिसे भारत दक्षिण कोरिया, यूरोपीय संघ और जापान जैसे देशों के साथ साझेदारी के माध्यम से हासिल करना चाहता है ।
- आईटीएमओ लेनदेन में शामिल होने से न केवल भारत को अपने एनडीसी को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी, बल्कि हरित नौकरियों के सृजन को भी बढ़ावा मिलेगा तथा प्रदूषण से संबंधित स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में भी कमी आएगी।
भारत के अवसर
- दक्षिण-दक्षिण सहयोग: भारत विकासशील देशों में जलवायु वित्त पहलों को समर्थन देने में सक्रिय भूमिका निभा सकता है, तथा सहायता के लिए विकसित देशों पर निर्भरता से आगे बढ़ सकता है।
- नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार: भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, जो 2022 में 10 बिलियन डॉलर से अधिक हो जाएगा । आईटीएमओ लेनदेन में न केवल भारत के भीतर बल्कि अन्य विकासशील देशों में भी ऐसे निवेश को और बढ़ाने की क्षमता है।
- भारत-अफ्रीका सहयोग: अफ्रीका में अक्षय ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं और यह जलवायु चुनौतियों का सामना कर रहा है। भारत हरित प्रौद्योगिकी में अपनी विशेषज्ञता का लाभ उठाकर अफ्रीकी देशों को उनके अक्षय संसाधनों का प्रभावी ढंग से दोहन करने में सहायता कर सकता है।
- संतुलित भागीदारी: आईटीएमओ लेन-देन आपसी समझौतों द्वारा संचालित होंगे, जिससे लाभों का निष्पक्ष और न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित होगा। भारत पारदर्शी और न्यायसंगत कार्बन क्रेडिट साझाकरण व्यवस्था को सुविधाजनक बनाने के लिए जापान के संयुक्त ऋण तंत्र (जेसीएम) के समान मॉडल अपनाने पर विचार कर सकता है।
आईटीएमओ लेनदेन में भारत के लिए चुनौतियां
- विकसित देशों द्वारा अत्यधिक निर्भरता का जोखिम: इस बात की चिंता है कि विकसित देश अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए बिना भारत के लागत-प्रभावी उत्सर्जन में कमी का फायदा उठा सकते हैं। इससे अनजाने में भारत पर अधिक बोझ पड़ सकता है।
- अवसर लागत: आईटीएमओ को बेचने से भारत की अपने जलवायु उद्देश्यों के लिए इन क्रेडिटों का उपयोग करने की क्षमता सीमित हो सकती है, जिससे घरेलू लक्ष्यों को पूरा करने में उसकी प्रगति में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
- पारदर्शिता और शासन संबंधी मुद्दे: कमजोर शासन और पारदर्शिता तंत्र ITMO समझौतों में अक्षमता और असमान परिणाम ला सकते हैं। शामिल पक्षों के बीच उचित लाभ-साझाकरण सुनिश्चित करने के लिए मजबूत नियम स्थापित करना महत्वपूर्ण है।
- सुरक्षा उपायों की आवश्यकता: ITMO समझौतों में भारत के हितों की रक्षा के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय शामिल किए जाने चाहिए। इसमें पारदर्शिता, उचित लाभ वितरण और भारत की आर्थिक और जलवायु प्राथमिकताओं के साथ संरेखण सुनिश्चित करना शामिल है।
सारांश
- पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6.2 भारत को जलवायु वित्त सुरक्षित करने, नवीकरणीय ऊर्जा पहल को बढ़ाने और दक्षिण-दक्षिण सहयोग को मजबूत करने की पर्याप्त संभावनाएं प्रदान करता है।
- विकसित और विकासशील दोनों देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी हरित प्रौद्योगिकियों के उपयोग में तेजी ला सकती है तथा आर्थिक स्थिरता में योगदान दे सकती है।
- हालांकि, भारत के लिए इससे जुड़ी चुनौतियों का सावधानीपूर्वक सामना करना ज़रूरी है। इसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि ITMO लेन-देन उसके अपने जलवायु उद्देश्यों को कमज़ोर न करे, जबकि ऐसे समझौतों से प्राप्त वित्तीय और तकनीकी लाभ को अधिकतम किया जा सके।
वनों में आग के बढ़ते खतरे से निपटना
चर्चा में क्यों?
लॉस एंजिल्स में हाल ही में लगी जंगली आग ने बेहतर अग्नि निवारण और प्रबंधन रणनीतियों की महत्वपूर्ण आवश्यकता को रेखांकित किया है।
वनों में आग लगने की घटनाओं पर बढ़ती चिंताएं
- वनों में आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और इसके परिणाम विनाशकारी हो रहे हैं, इसके बावजूद वनों में आग लगने की घटनाएं केवल तभी ध्यान आकर्षित करती हैं जब बड़ी घटनाएं घटित हो जाती हैं।
- ये आग इस बात की स्पष्ट चेतावनी देती हैं कि कोई भी क्षेत्र खतरे से अछूता नहीं है, तथा दीर्घकालिक समाधान की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालती हैं।
भारत में जंगल की आग: बदतर होती स्थिति
- भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार, भारत का 36% से अधिक वन क्षेत्र आग के प्रति संवेदनशील है।
- ऊर्जा, पर्यावरण एवं जल परिषद की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले दो दशकों में वनों में आग लगने की घटनाएं दस गुना बढ़ गई हैं, जबकि कुल वन क्षेत्र में केवल 1.12% की वृद्धि हुई है।
- उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और कर्नाटक जैसे राज्य विशेष रूप से इन आग के प्रति संवेदनशील हैं।
वन आग के प्रमुख कारण
- भारत में लगभग 90% वनों की आग मानवीय गतिविधियों के कारण होती है, जिनमें शामिल हैं:
- भूमि समाशोधन
- कटाई-और-जलाओ कृषि
- बिना देखरेख के कैम्प फायर
- जलवायु परिवर्तन से तापमान में वृद्धि होती है और शुष्क मौसम लंबा हो जाता है, जिससे वनों में आग लगने की संभावना बढ़ जाती है।
जंगल की आग के विनाशकारी परिणाम
पर्यावरणीय प्रभाव:
- जंगल की आग से पेड़, वन्य जीवन और जैव विविधता नष्ट हो जाती है।
- विश्व संसाधन संस्थान के अनुसार, वे कार्बन उत्सर्जन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, तथा भारतीय वनों की आग से प्रत्येक वर्ष 69 मिलियन टन CO₂ उत्सर्जित होता है।
- आग से जल चक्र बाधित होता है और मिट्टी की उर्वरता कम होती है।
आर्थिक प्रभाव:
- लकड़ी और अन्य वन उत्पादों की हानि से वनों पर निर्भर समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2018 में दी गई रिपोर्ट के अनुसार, आग के कारण होने वाले वन क्षरण सहित अन्य कारणों से प्रतिवर्ष 1.74 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान होता है।
सामाजिक प्रभाव:
- आग से वन्यजीव मानव आवासों में आ जाते हैं, जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष बढ़ जाता है।
- वे उन स्थानीय समुदायों की आजीविका को खतरे में डालते हैं जो अपने संसाधनों के लिए वनों पर निर्भर हैं।
मौजूदा नीतियां और पहल
- वन अग्नि पर राष्ट्रीय कार्य योजना और वन अग्नि रोकथाम एवं प्रबंधन योजना (एफएफपीएमएस) वन अग्नि के प्रबंधन में राज्यों को सहायता प्रदान करती है।
- एफएफपीएमएस राज्यों को अग्नि निवारण प्रयासों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
वन अग्नि प्रबंधन में चुनौतियाँ
बजट बाधाएं:
- एफएफपीएमएस के लिए वित्त पोषण पिछले कुछ वर्षों में अलग-अलग रहा है, जिसका आवंटन इस प्रकार है: 2019-20 में ₹46.40 करोड़, 2022-23 में ₹28.25 करोड़, तथा 2023-24 के लिए अनुमानित ₹51 करोड़, जिसे बाद में समायोजित कर ₹40 करोड़ कर दिया गया।
- प्रभावी अग्नि प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए अधिक सुसंगत वित्तीय सहायता की आवश्यकता है।
तकनीकी सीमाएँ:
- मौजूदा वन अग्नि चेतावनी प्रणाली को वन अग्नि और अन्य प्रकार की आग के बीच अंतर करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण प्रतिक्रिया में देरी होती है।
- जलवायु और भौगोलिक डेटा का उपयोग करने वाले उन्नत पूर्वानुमान मॉडलों को लागू करने से उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करने में सहायता मिल सकती है।
- थर्मल इमेजिंग से लैस ड्रोन का उपयोग निगरानी और अग्निशमन क्षमताओं को बढ़ा सकता है।
सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करना
- जंगल की आग की सूचना देने और उसका प्रबंधन करने में स्थानीय समुदाय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- मोबाइल एप्लीकेशन, टोल-फ्री हेल्पलाइन और एसएमएस अलर्ट के माध्यम से पूर्व चेतावनी प्रणालियों में सुधार करके सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाया जा सकता है।
- कुछ राज्यों में सूखी चीड़ की सुइयों को एकत्रित करने वाले महिला स्वयं सहायता समूहों जैसी पहल से आग के खतरे को कम करने में मदद मिलती है।
- नेपाल के सामुदायिक वन उपयोगकर्ता समूहों और इंडोनेशिया के अग्नि-मुक्त ग्राम कार्यक्रम जैसे वैश्विक मॉडलों से सीख लेकर भारत में समुदाय-आधारित वन अग्नि प्रबंधन को मजबूत किया जा सकता है।
आगे का रास्ता
- पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और समाज पर वनों की आग के प्रभाव से निपटने के लिए एक सहयोगात्मक बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
प्रमुख समाधानों में शामिल हैं:
- अग्नि प्रबंधन के लिए निरंतर वित्तपोषण सुनिश्चित करने हेतु नीतिगत समर्थन और बेहतर बजट।
- उन्नत पूर्वानुमान, निगरानी और प्रतिक्रिया क्षमताओं के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाना ।
- स्थानीय समुदायों को वास्तविक समय में आग की सूचना देने और प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने के लिए प्रशिक्षण देना और सशक्त बनाना ।
निष्कर्ष
वनों में आग के बढ़ते खतरे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों, नागरिक समाज संगठनों और स्थानीय समुदायों की ओर से ठोस प्रयास की आवश्यकता है।
The document The Hindi Editorial Analysis- 12th February 2025 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC is a part of the UPSC Course Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly.
All you need of UPSC at this link: UPSC
|
7 videos|3454 docs|1081 tests
|
FAQs on The Hindi Editorial Analysis- 12th February 2025 - Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC
| 1. दक्षिण-दक्षिण जलवायु सहयोग का क्या महत्व है ? |  |
Ans. दक्षिण-दक्षिण जलवायु सहयोग का महत्व इस बात में है कि यह विकासशील देशों के बीच जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अनुभव, तकनीकी और संसाधनों का आदान-प्रदान करता है। यह सहयोग देशों को एकजुट करता है ताकि वे अपनी चुनौतियों का सामना कर सकें और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा दे सकें।
| 2. भारत की दक्षिण-दक्षिण जलवायु सहयोग में क्या भूमिका है ? |  |
Ans. भारत दक्षिण-दक्षिण जलवायु सहयोग में एक प्रमुख भूमिका निभाता है, जहां वह अन्य विकासशील देशों को तकनीकी सहायता, वित्तीय संसाधन और विशेषज्ञता प्रदान करता है। भारत ने अपने अनुभवों को साझा किया है, जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति और जलवायु अनुकूलन के लिए उपाय।
| 3. वनों में आग के बढ़ते खतरे का क्या कारण है ? |  |
Ans. वनों में आग के बढ़ते खतरे के कई कारण हैं, जिनमें जलवायु परिवर्तन, सूखा, मानव गतिविधियाँ और वन प्रबंधन में कमी शामिल हैं। उच्च तापमान और कम वर्षा के कारण जंगलों में आग लगने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान होता है।
| 4. वनों में आग से निपटने के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं ? |  |
Ans. वनों में आग से निपटने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं, जैसे कि बेहतर वन प्रबंधन, आग बुझाने के लिए तकनीकी संसाधनों का उपयोग, समुदायों में जागरूकता बढ़ाना और पूर्वानुमान प्रणाली विकसित करना। इसके अलावा, वन संरक्षण और पुनर्वनीकरण भी महत्वपूर्ण हैं।
| 5. जलवायु परिवर्तन से निपटने में भारत की क्या चुनौतियाँ हैं ? |  |
Ans. जलवायु परिवर्तन से निपटने में भारत की कई चुनौतियाँ हैं, जैसे कि बढ़ती जनसंख्या, आर्थिक विकास की आवश्यकताएँ, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग, और विभिन्न क्षेत्रों में असमानता। इन चुनौतियों के मद्देनजर, भारत को संतुलित और समावेशी नीतियों को लागू करने की आवश्यकता है।
Related Searches
















