The Hindi Editorial Analysis- 14th October 2025 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC PDF Download
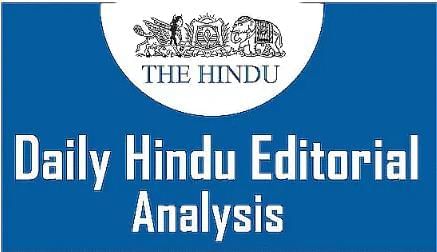
एक हरे संक्रमण की तेजी से बढ़ती प्रक्रिया
समाचार में क्यों?
रेलवे का डिकार्बोनाइजेशन वित्तीय अनुशासन के साथ सुधार को साबित करता है।
परिचय
जुलाई 2025 में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) में भारत की पहली हाइड्रोजन-शक्ति वाली ट्रेन कोच का सफल परीक्षण एक तकनीकी मील का पत्थर होने के साथ-साथ भारतीय रेलवे के हरे परिवर्तन में एक निर्णायक कदम का भी प्रतिनिधित्व करता है।
दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक, भारतीय रेलवे एक ऐसे संक्रमण का अनुसरण कर रहा है जिसकी वैश्विक समानांतरता कम है, जिसका लक्ष्य 2030 तक शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना है, जो भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य से चार दशक पहले है।
यह परिवर्तन केवल स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने तक सीमित नहीं है; यह बुनियादी ढांचे, संचालन और वित्तपोषण मॉडलों का एक संपूर्ण पुनःकल्पना दर्शाता है, जिससे रेलवे को सतत गतिशीलता और जलवायु कार्रवाई में एक नेता के रूप में स्थापित किया जा रहा है।
प्रति दिन 24 मिलियन से अधिक यात्रियों और तीन मिलियन टन माल का परिवहन करते हुए, इस विशाल नेटवर्क का डिकार्बोनाइजेशन भारत की समग्र जलवायु प्रतिबद्धताओं और सतत विकास के उद्देश्यों के लिए गहरे निहितार्थ रखता है।
भारतीय रेलवे के हरित संक्रमण के प्रमुख पहलों (पिछले 10 वर्ष):
- 45,000 किमी का चौड़ा गेज नेटवर्क विद्युत चालित किया गया। अब 98% विद्युत चालित है, जिससे डीजल का उपयोग और उत्सर्जन में तेज कमी आई है।
- नवीकरणीय ऊर्जा का एकीकरण। 553 MW सौर, 103 MW पवन, और 100 MW हाइब्रिड -> कुल 756 MW चालू किया गया।
- 2,000+ स्टेशन और सेवा भवन सौर ऊर्जा से संचालित हैं।
- कई रेलवे कार्यालय, जिसमें उत्तर-पूर्वी सीमा क्षेत्र के कार्यालय शामिल हैं, BEE “शून्य” नेट-जीरो लेबल के साथ प्रमाणित हैं।
- हाइड्रोजन से संचालित ट्रेन “हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज” कार्यक्रम के तहत सफलतापूर्वक परीक्षण की गई - 35 इकाइयों की योजना बनाई गई है।
- भाड़े का रेलवे की ओर स्थानांतरण 2030 तक 45% का लक्ष्य रखने के लिए किया गया है, जिससे सड़क के उत्सर्जन में कमी आएगी।
- जैव ईंधन मिश्रण, हरा भवन, और समर्पित माल गलियारे (DFCs) का संचालन किया गया - 30 वर्षों में 457 मिलियन टन CO₂ को बचाने का अनुमान।
इन पहलों के माध्यम से, भारतीय रेलवे को एक जलवायु-सकारात्मक राष्ट्रीय गतिशीलता आधार के रूप में तकनीकी और प्रणालीगत रूप से पुनः कल्पना किया गया है।
जलवायु वित्त मुख्यधारा में
1. एक हरे वित्त की रीढ़ का निर्माण
उपकरण / संस्था
मुख्य विवरण और योगदान
मुख्य विवरण और योगदान
सर्वभौमिक हरे बांड
- वित्तीय वर्ष 2023 से ₹58,000 करोड़ जारी किए गए; परिवहन क्षेत्र एक प्रमुख लाभार्थी है।
- आवंटन
- ~₹42,000 करोड़ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, मेट्रो और उपनगरीय रेल के लिए निर्धारित।
- संस्थागत एकीकरण
- जलवायु लक्ष्य पूंजी बजटिंग और बुनियादी ढांचे की योजना में समाहित।
- आईआरएफसी (भारतीय रेलवे वित्त निगम)
- 2017 में $500 मिलियन का हरा बांड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वित्तपोषण के लिए जारी किया।
- NTPC ग्रीन एनर्जी को नवीकरणीय क्षमता विकास के लिए ₹7,500 करोड़ का ऋण प्रदान किया।
- विश्व बैंक सहायता
- $245 मिलियन ऋण (जून 2022) रेल लॉजिस्टिक्स परियोजना के लिए, जो माल ढुलाई की दक्षता में सुधार और GHG उत्सर्जन को कम करेगा।
भारतीय रेलवे वित्तीय नवाचार को जलवायु महत्वाकांक्षा के साथ जोड़ रहा है — एक ऐसा वित्तपोषण मॉडल बना रहा है जो हरे पूंजी को रणनीतिक बुनियादी ढांचे के विकास के साथ मिलाता है।
2. वित्त को वास्तविक जलवायु परिणामों के साथ संरेखित करना
- हरे ऊर्जा का स्रोत. विद्युतीकरण को वास्तव में नवीकरणीय ट्रैक्शन पावर के साथ जोड़ना आवश्यक है। सौर और पवन उत्पादकों से सीधी दीर्घकालिक खरीद सच्ची कार्बन कमी सुनिश्चित करती है।
- अंतिम मील स्थिरता. इलेक्ट्रिक बसों, साइकिल साझा करने और चलने योग्य बुनियादी ढांचे को एकीकृत करते हुए बहु-आधारित हरे हब विकसित करें। इलेक्ट्रिक, LNG, या हाइड्रोजन संचालित अंतिम मील वाहनों के माध्यम से स्वच्छ माल ढुलाई को बढ़ावा दें।
- गाड़ी के उपकरण में नवाचार. गैर-विद्युत या विरासत मार्गों पर हाइड्रोजन ईंधन-सेल ट्रेनों का पायलट परीक्षण करें। हल्के कोच, वायुगतिकीय लोकोमोटिव, और AI आधारित ऊर्जा अनुकूलन प्रणाली पेश करें।
- व्यवहार परिवर्तन. ट्रेनों के लिए हरी प्रमाणन और माल सेवाओं के लिए कार्बन लेबलिंग पेश करें। यात्रियों और व्यवसायों को सक्रिय जलवायु भागीदार बनाने के लिए जागरूकता अभियान शुरू करें।
जलवायु वित्त को वास्तविक उत्सर्जन कमी और प्रणालीगत सुधार में बदलना चाहिए। भारतीय रेलवे एक राज्य-नेतृत्व वाले कार्बन कमी मॉडल के रूप में उभर सकता है - जहाँ प्रौद्योगिकी, वित्त, और व्यवहार परिवर्तन एक साथ मिलकर सतत गतिशीलता को परिभाषित करते हैं।
चुनौती का सामना करना
- 2030 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन हासिल करने से भारतीय रेलवे को हर साल 60 मिलियन टन CO₂ से अधिक बचाने में मदद मिल सकती है, जो भारतीय सड़कों से 13 मिलियन कारों को हटाने के बराबर है।
- इलेक्ट्रिफिकेशन और ऊर्जा दक्षता उपायों से दशक के अंत तक ₹1 लाख करोड़ की ईंधन बचत होने की उम्मीद है।
- वास्तविक चुनौती पूंजी को जुटाने और प्रबंधित करने में है, न कि महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को निर्धारित करने में।
- अगर इसे प्रभावी ढंग से लागू किया गया, तो डिकार्बोनाइजेशन योजना एक वैश्विक मॉडल के रूप में काम कर सकती है, इस प्रकार यह दिखा सकती है कि बड़े राज्य-चालित सिस्टम बिना वित्तीय अनुशासन के समझौता किए कम-कार्बन परिवर्तन को अपना सकते हैं।
निष्कर्ष
भारतीय रेलवे का डीकार्बोनाइजेशन यात्रा भारत की बढ़ती क्षमता को दर्शाती है कि वह तकनीकी नवाचार को वित्तीय विवेक के साथ जोड़ सकता है। हरी वित्त, स्वच्छ ऊर्जा, और व्यवहारिक सुधार को संरेखित करके, यह दर्शाता है कि कैसे एक राज्य-प्रबंधित प्रणाली बड़े पैमाने पर सतत परिवर्तन का नेतृत्व कर सकती है। यदि इसे बनाए रखा गया, तो यह तेज़ गति का हरा संक्रमण सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को जलवायु कार्रवाई और आर्थिक लचीलापन के एक स्तंभ के रूप में पुनर्परिभाषित कर सकता है।
शासन का परीक्षण
यह समाचार क्यों है?
- चिनाब नदी पर सावलकोट जलविद्युत परियोजना ने उस समय नई ध्यानाकर्षण प्राप्त किया जब भारत ने सिंध जल संधि को निलंबित किया।
- इस परियोजना को भारत के जल अधिकारों का दावा करने के तरीके के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन यह पर्यावरणीय प्रभाव और नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के भविष्य के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न भी उठाती है।
सावलकोट जलविद्युत परियोजना जम्मू और कश्मीर में चिनाब नदी पर प्रस्तावित 1.8 GW योजना है। इसका पुनरुद्धार भारत द्वारा सिंध जल संधि (IWT) के निलंबन के साथ मेल खाता है, जो नाजुक हिमालयी क्षेत्र में पारिस्थितिकीय स्थिरता और पुनर्वास न्याय के बारे में चिंताओं को जन्म देता है।
सवालकोट जलविद्युत परियोजना को नया impetus
चेनाब नदी पर स्थित सवालकोट जलविद्युत परियोजना (HEP) ने हाल ही में नए ध्यान और गति प्राप्त की है। यह पुनरुद्धार कई कारणों से महत्वपूर्ण है:
- भू-राजनीतिक संदर्भ: परियोजना पर नया ध्यान भारत द्वारा 2025 में पहलगाम हमले के बाद एकतरफा रूप से सिंध जल संधि (IWT) को निलंबित करने के साथ मेल खाता है। यह समय परियोजना को मजबूत भू-राजनीतिक महत्व प्रदान करता है, जो भारत के जल अधिकारों पर रणनीतिक दावे का प्रतीक है।
- पर्यावरणीय और सामाजिक परिणाम: जबकि यह परियोजना जल अधिकारों का एक साहसिक दावा प्रस्तुत करती है, यह पारिस्थितिकीय स्थिरता, पुनर्वास न्याय, और नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की दीर्घकालिक स्थिरता के बारे में महत्वपूर्ण चिंताएँ भी उठाती है। भू-राजनीतिक प्रतीकवाद पर जोर इन महत्वपूर्ण विचारों को छिपा सकता है।
- विशाल जलविद्युत विस्तार के प्रभाव: इस नाजुक और संवेदनशील क्षेत्र में विशाल जलविद्युत परियोजनाओं का विस्तार कई पर्यावरणीय और सामाजिक चुनौतियों के साथ आता है। इनमें स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र में संभावित व्यवधान, जैव विविधता पर प्रभाव, और प्रभावित समुदायों के प्रभावी पुनर्वास और पुनर्वास की आवश्यकता शामिल हैं।
पारिस्थितिकी और भूवैज्ञानिक मुद्दे
- बंपर-टू-बंपर कॉरिडोर: चेनाब बेसिन पहले से ही कई जलविद्युत परियोजनाओं का घर है, जिनमें दुलहस्ती, भागिलहर, और सलाल शामिल हैं, जो जलविद्युत विकास का एक निरंतर कॉरिडोर बनाते हैं।
- संविधानिक प्रभाव: इन परियोजनाओं, जिनमें सावालकोट भी शामिल है, के संचित पर्यावरणीय प्रभावों का अध्ययन अभी तक नहीं किया गया है। प्रमुख चिंताओं में शामिल हैं:
- गाद का बोझ: गाद का बढ़ता बोझ और जलाशयों में कीचड़ जमने की समस्या, जो जलाशयों की दीर्घकालिक उपयोगिता को प्रभावित कर सकती है।
- ढलान अस्थिरता: ढलान अस्थिरता और भूस्खलन का बढ़ता जोखिम, जो बुनियादी ढांचे और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है।
- नदी पारिस्थितिकी तंत्र: नदी पारिस्थितिकी तंत्र का विखंडन और पानी के प्रवाह और आवास में व्यवधान के कारण जल जीवों की विविधता का नुकसान।
- भ्रामक वर्गीकरण: परियोजना को एक रन-ऑफ-रिवर योजना के रूप में वर्गीकृत किया गया है, लेकिन इसका बड़ा जलाशय इसे एक भंडारण बांध की तरह कार्य करने के लिए मजबूर करता है, जिसके विभिन्न पारिस्थितिकी संबंधी निहितार्थ हैं।
सामरिक और भू-राजनीतिक आयाम
- अधिकारों का कार्यान्वयन: सावालकोट परियोजना का समय भारत के इरादे को दर्शाता है कि वह सिंध जल संधि (IWT) के तहत पश्चिमी नदियों पर अपने अधिकारों को पूरी तरह से कार्यान्वित करना चाहता है।
- संधि का निलंबन: संधि को निलंबित करके, भारत उन प्रक्रियात्मक जांचों को हटा देता है जो परियोजना अनुमोदनों में देरी कर सकती हैं, जिससे सावालकोट और वुल्लर बैराज जैसी परियोजनाओं के तेज कार्यान्वयन की अनुमति मिलती है।
- संभावित जोखिम: यह आक्रामक रुख कई जोखिमों को जन्म देता है:
- विश्वसनीयता: यह भारत की विश्वसनीयता को एक नियम-पालक नदी तट राज्य के रूप में कम कर सकता है, जिसका दीर्घकालिक कूटनीतिक प्रभाव हो सकता है।
- तीसरे पक्ष की जांच: भारत भविष्य के विवादों में तीसरे पक्ष की जांच को आमंत्रित कर सकता है, जो एक स्थिति है जिसका उसने ऐतिहासिक रूप से विरोध किया है।
- कानूनी चुनौतियाँ: पाकिस्तान ने पहले ही 1960 के ढांचे के तहत भारत के संधि के निलंबन की वैधता पर सवाल उठाया है, जो संभावित कानूनी और कूटनीतिक चुनौतियों का संकेत देता है।
आगे का रास्ता: रणनीति और स्थिरता का संतुलन
- रणनीतिक अभिव्यक्ति: भारत की जल अधिकारों पर रणनीतिक अभिव्यक्ति को पारिस्थितिकी के प्रति संयम के साथ संतुलित किया जाना चाहिए।
- अनुशंसित उपाय: इस संतुलन को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित उपायों की अनुशंसा की जाती है:
- बेसिन-स्तरीय अध्ययन: कई जलविद्युत परियोजनाओं के समग्र प्रभावों को समझने के लिए बेसिन स्तर पर व्यापक पर्यावरण और तलछट प्रबंधन अध्ययन करें।
- क्षेत्रीय प्रोटोकॉल: बढ़ी हुई जलविद्युत विकास से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए ढलान स्थिरता और समग्र प्रभावों की निगरानी के लिए क्षेत्रीय प्रोटोकॉल विकसित करें।
- हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा करना: हितधारकों के बीच विश्वास बनाने और सुरक्षा जोखिमों को कम करने के लिए क्षेत्रीय या बहुपक्षीय प्लेटफार्मों के माध्यम से हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा करने की प्रक्रिया को संस्थागत बनाएं।
- विश्वास निर्माण तंत्र: हाइड्रोलॉजिकल निगरानी को सुरक्षा चिंता से निकालकर नदी किनारे के राज्यों के बीच विश्वास निर्माण तंत्र में परिवर्तित करें।
- पर्यावरणीय देखभाल: रणनीतिक स्वायत्तता को पर्यावरणीय देखभाल के साथ संरेखित करें ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकताएँ पारिस्थितिकी की स्थिरता को कमजोर न करें।
सवालकोट जलविद्युत परियोजना राष्ट्रीय सुरक्षा और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाने की जटिल चुनौती को उजागर करती है। जैसे-जैसे भारत पश्चिमी नदियों पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है, यह नाजुक पारिस्थितिकी प्रणालियों की रक्षा करना और क्षेत्रीय विश्वास बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। इस परियोजना की विरासत इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या भारत अपनी रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं को एक स्थायी शासन के मॉडल में बदल सकता है, जहां पारिस्थितिकीय देखभाल और राष्ट्रीय शक्ति एक साथ काम करती हैं, न कि एक-दूसरे के खिलाफ।
|
13 videos|3480 docs|1090 tests
|
FAQs on The Hindi Editorial Analysis- 14th October 2025 - Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC
| 1. हरे संक्रमण की प्रक्रिया क्या है और यह किस प्रकार शासन को प्रभावित करती है ? |  |
| 2. हरे संक्रमण के लिए कौन-कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं ? |  |
| 3. शासन के परीक्षण में हरे संक्रमण का क्या महत्व है ? |  |
| 4. हरे संक्रमण को लागू करने में कौन-सी चुनौतियाँ सामने आती हैं ? |  |
| 5. हरे संक्रमण के संदर्भ में भारत की भूमिका क्या है ? |  |





















