UPSC Exam > UPSC Notes > Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly > The Hindi Editorial Analysis- 1st March 2025
The Hindi Editorial Analysis- 1st March 2025 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC PDF Download
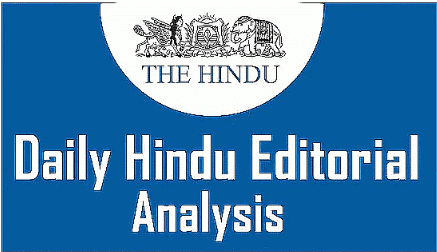
आर्द्रभूमि संरक्षण को मुख्यधारा में लाने की आवश्यकता
चर्चा में क्यों?
- मेघालय में हाल ही में घटित एक मामले ने भारत में आर्द्रभूमि संरक्षण की चुनौतियों की ओर ध्यान आकर्षित किया है, तथा इन क्षेत्रों के पारिस्थितिक महत्व तथा मजबूत सुरक्षात्मक उपायों की आवश्यकता को रेखांकित किया है।
- रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने के बावजूद, भारत में आर्द्रभूमि शहरीकरण, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसे कारकों के कारण क्षरण का सामना कर रही है।
आर्द्रभूमि संरक्षण पर ध्यान केन्द्रित करना
- भारत के एक पूर्वोत्तर राज्य में आर्द्रभूमि के संरक्षण की निगरानी के लिए एक कानूनी पहल शुरू की गई है।
- प्रतिवर्ष 2 फरवरी को 'विश्व आर्द्रभूमि दिवस' 1971 में रामसर कन्वेंशन को अपनाने की याद में मनाया जाता है।
- वर्ष 2023 का विषय 'हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों का संरक्षण', सतत विकास में आर्द्रभूमियों के महत्व पर जोर देता है।
आर्द्रभूमियों के लिए खतरे
- आर्द्रभूमियाँ जैविक रूप से सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्रों में से हैं, जो विश्व स्तर पर 12.1 मिलियन वर्ग किमी क्षेत्र को कवर करती हैं तथा पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का 40.6% प्रदान करती हैं ।
- वे तेजी से हो रहे शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि, औद्योगीकरण और जलवायु परिवर्तन के कारण गंभीर खतरे में हैं ।
- अध्ययनों से पता चलता है कि 1900 के बाद से 50% आर्द्रभूमि नष्ट हो चुकी है , तथा 1970 से 2015 तक आर्द्रभूमि सतही क्षेत्र में 35% की गिरावट आई है ।
- 1970 के बाद से अंतर्देशीय आर्द्रभूमि प्रजातियों की जनसंख्या में 81% की कमी आई है , तथा तटीय/समुद्री प्रजातियों की जनसंख्या में 36% की कमी आई है।
संरक्षण में चुनौतियाँ
- आर्द्रभूमि जल प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन शमन और शहरी बुनियादी ढांचे को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ।
- 2022 रामसर कन्वेंशन में इस बात पर जोर दिया गया कि आर्द्रभूमि संरक्षण को व्यापक वैश्विक पर्यावरणीय पहलों के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए।
- सम्मेलन की रणनीतिक योजना का उद्देश्य आर्द्रभूमि संरक्षण को सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी), वैश्विक जैव विविधता लक्ष्यों और जलवायु समझौतों के साथ संरेखित करना है ।
- जैव विविधता हानि, जलवायु परिवर्तन और कोविड-19 महामारी जैसी वैश्विक चुनौतियों के कारण आर्द्रभूमि संरक्षण की आवश्यकता बढ़ गई है ।
भारत में आर्द्रभूमि संरक्षण
- भारत रामसर कन्वेंशन के प्रति प्रतिबद्ध है और उसने 1.33 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने वाले 75 रामसर स्थलों को नामित किया है, जो देश के कुल 15.98 मिलियन हेक्टेयर आर्द्रभूमि क्षेत्र का लगभग 8% है ।
- 2017-18 राष्ट्रीय वेटलैंड दशकीय परिवर्तन एटलस से पता चलता है कि भारत में 66.6% वेटलैंड प्राकृतिक हैं, जिनमें 43.9% अंतर्देशीय और 22.7% तटीय हैं ।
- प्राकृतिक आर्द्रभूमियों में, विशेष रूप से समुद्र तट पर, उल्लेखनीय गिरावट देखी जा रही है, जबकि मानव निर्मित आर्द्रभूमियों में वृद्धि हो रही है।
- एक अध्ययन में पाया गया कि शहरी विस्तार, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और प्रदूषण के कारण पिछले चार दशकों में भारत की 30% प्राकृतिक आर्द्रभूमि नष्ट हो गई है ।
- शहरी आर्द्रभूमि विशेष रूप से असुरक्षित हैं, प्रमुख शहरों में महत्वपूर्ण नुकसान की सूचना मिली है: मुंबई ने 1970 से 2014 तक अपनी 71% आर्द्रभूमि खो दी , कोलकाता में 1991 और 2021 के बीच 36% की कमी देखी गई और चेन्नई ने अपनी आर्द्रभूमि का 85% नुकसान अनुभव किया ।
आर्द्रभूमि के नुकसान का आर्थिक प्रभाव
- आर्द्रभूमि के क्षरण का पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जो बदले में आर्थिक और सामाजिक कल्याण को प्रभावित करता है।
- कोलंबिया में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि शहरी आर्द्रभूमि के नुकसान से प्रति हेक्टेयर 76,827 डॉलर का वार्षिक आर्थिक प्रभाव हो सकता है ।
- शहरी क्षेत्रों में आर्द्रभूमि क्षरण के कारण प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर 30,354 डॉलर की आर्थिक हानि का अनुमान है ।
समग्र संरक्षण दृष्टिकोण की आवश्यकता
- भारत में वर्तमान आर्द्रभूमि प्रबंधन मुख्य रूप से पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय पहलुओं पर केंद्रित है, तथा आर्द्रभूमि को प्रभावित करने वाले मानव-प्रेरित प्रभावों, भूमि-उपयोग परिवर्तनों और प्रशासनिक मुद्दों पर सीमित शोध किया गया है।
- आर्द्रभूमियाँ पारिस्थितिक, आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिसके लिए एक एकीकृत संरक्षण रणनीति आवश्यक है।
- कार्बन के स्रोत और अवशोषण के रूप में जलवायु परिवर्तन शमन में उनकी भूमिका का मूल्यांकन और निगरानी की आवश्यकता है।
- जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों के कारण बढ़ते दबाव से निपटने के लिए अधिक प्रभावी प्रबंधन रणनीतियों की आवश्यकता है।
- संरक्षण प्रयासों में पारिस्थितिकी तंत्र आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए तथा इसे व्यापक विकास योजनाओं में एकीकृत किया जाना चाहिए, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में अनुशंसित किया गया है।
निष्कर्ष
- आर्द्रभूमियाँ पारिस्थितिक संतुलन, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं।
- आर्द्रभूमि के और अधिक क्षरण को रोकने तथा दीर्घकालिक पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत नीतियों, टिकाऊ प्रबंधन प्रथाओं और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से संरक्षण प्रयासों को मजबूत करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
वे कदम जो भारत की एआई महत्वाकांक्षा को आकार देंगे
चर्चा में क्यों?
भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के क्षेत्र में चीन और अमेरिका के साथ प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में है । हालाँकि, भारत को विनियमन और नवाचार के मामले में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत के लिए एआई को नियंत्रित करने और प्रतिस्पर्धी बने रहने के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है, खासकर इसके आईटी उद्योग के लिए।
भारतीय सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के सामने चुनौतियाँ
- भारत के बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को वैश्विक ग्राहकों के साथ एआई-संचालित परियोजनाओं के लिए अपने चीनी समकक्षों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है ।
- यद्यपि भारत में अत्यधिक कुशल कार्यबल मौजूद है, फिर भी भारतीय कम्पनियां प्रायः अनुबंध खो देती हैं, क्योंकि वे अपने प्रतिद्वंद्वियों की तकनीकी क्षमताओं की बराबरी नहीं कर पातीं।
- मुद्दा स्थानीय या विदेशी एआई प्लेटफॉर्म के चयन से कहीं आगे का है; यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि बाजार विनियमन एआई विकास में भारत की प्रगति में बाधा न बनें।
एआई विकास में भारत की प्रतिस्पर्धा
भारत तीन मोर्चों पर प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में है:
- सिलिकॉन वैली के साथ कदम मिलाते हुए।
- चीन के साथ प्रतिस्पर्धा.
- दक्षिण पूर्व एशिया से उभरती प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है।
- एआई के क्षेत्र में अग्रणी बने रहने के लिए, भारतीय व्यवसायों को अपने परिचालन में एआई प्रौद्योगिकियों को प्रभावी ढंग से एकीकृत करने की आवश्यकता है।
भारत में एआई को अपनाने में बाधा डालने वाले मुद्दे
एआई को अपनाने से निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार हो सकता है, लेकिन यह कई चुनौतियां भी लाता है:
- नौकरी विस्थापन । जैसे-जैसे एआई स्वचालन बढ़ता है, नियमित नौकरियों के खत्म होने का खतरा हो सकता है।
- एआई एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह । एल्गोरिदम में अंतर्निहित पूर्वाग्रहों के कारण एआई निर्णय लेने की प्रक्रिया भेदभावपूर्ण हो सकती है।
- डीपफेक के माध्यम से गलत सूचना । एआई-जनरेटेड डीपफेक में गलत सूचना फैलाने, मीडिया में विश्वास को कम करने और राजनीतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने की क्षमता है।
मध्यस्थ दायित्व
- विदेशी प्रौद्योगिकी कंपनियां अक्सर एआई पारिस्थितिकी तंत्र पर हावी रहती हैं तथा बाजार के नियमों और विनियमों को नियंत्रित करती हैं।
- भारतीय स्टार्टअप्स को विनियामक समर्थन और अनुकूल परिस्थितियों की कमी के कारण प्रतिस्पर्धा में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
विनियामक चुनौतियाँ
- भारतीय ऐप डेवलपर्स ने वैश्विक टेक कंपनियों की एकाधिकारवादी प्रथाओं के बारे में चिंता जताई है और उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई हैं।
- हालाँकि, एआई पर सख्त नियम लागू करने से भारत की तकनीकी प्रगति और अनुकूलन में बाधा आ सकती है, जिससे वैश्विक स्तर पर इसकी प्रतिस्पर्धा कम हो जाएगी।
विनियमन और विकास में संतुलन
- भारत पहले ही एआई मूल्य श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा स्थापित कर चुका है।
- अनुपालन लागत में वृद्धि से भारत को चीन और अमेरिका की तुलना में नुकसान हो सकता है, क्योंकि दोनों ही देश न्यूनतम एआई विनियमन का विकल्प चुन रहे हैं।
- अत्यधिक विनियमन के कारण व्यवसाय अपनी आईटी विकास और अनुसंधान गतिविधियों को अधिक अनुकूल एआई विनियामक वातावरण वाले देशों में स्थानांतरित करने के लिए बाध्य हो सकते हैं।
एआई विनियमन के लिए वैश्विक दृष्टिकोण
विभिन्न देश एआई विनियमन के लिए विभिन्न दृष्टिकोण अपना रहे हैं:
- यूरोपीय संघ (ईयू) - एआई प्रौद्योगिकियों से जुड़े जोखिमों और सामाजिक प्रभावों को दूर करने के लिए कड़े नियमों को लागू करता है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका ने सख्त नियामक उपायों की तुलना में एआई नवाचार और विकास को प्राथमिकता देते हुए अधिक सहज दृष्टिकोण अपनाया है।
- भारत को अपने औद्योगिक और प्रौद्योगिकीय क्षेत्रों की सुरक्षा और वृद्धि सुनिश्चित करते हुए इन दो दृष्टिकोणों के बीच चयन करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।
एआई नीति में भारत के लिए सबक
- यूरोपीय संघ के विपरीत, भारत को विभिन्न राज्यों के बीच विखंडित शासन जैसी संरचनात्मक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है।
- भारत में एआई विनियमन को इस प्रकार से तैयार किया जाना चाहिए कि इसकी निर्यात क्षमताओं में बाधा उत्पन्न न हो, विशेष रूप से एआई-संबंधित हार्डवेयर और क्लाउड प्रौद्योगिकियों में चीन के प्रभुत्व को देखते हुए।
- भारत को पश्चिमी एआई नियामक ढांचे को आँख मूंदकर अपनाने के बजाय आईटी सेवा क्षेत्र में अपनी ताकत का लाभ उठाने वाली नीतियां बनानी चाहिए।
भारत में स्पष्ट एआई नीति की आवश्यकता
- भारत की वर्तमान एआई नीति विभिन्न एजेंसियों के परस्पर विरोधी नियमों के कारण खंडित है।
- नए कानून बनाने के बजाय, भारत को निम्नलिखित विषयों से संबंधित अपने मौजूदा कानूनी ढांचे को मजबूत बनाने और अनुकूलित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए:
- अविश्वास एवं कॉर्पोरेट दायित्व।
- स्वतंत्र भाषण और सार्वजनिक व्यवस्था।
- मौजूदा आईटी अधिनियम पहले से ही एआई प्रशासन के लिए पर्याप्त दिशानिर्देश प्रदान करता है, बिना किसी अलग एआई-विशिष्ट कानून की आवश्यकता के।
आगे का रास्ता
- भारत को अपनी स्वयं की एआई नियामक रणनीति स्थापित करने की आवश्यकता है जो राष्ट्रीय हितों और प्राथमिकताओं के अनुरूप हो।
ध्यान इस पर होना चाहिए:
- व्यापक स्तर पर एआई को अपनाने को प्रोत्साहित करना।
- ओपन-सोर्स एआई पहलों का समर्थन करना।
- भारत के आईटी क्षेत्र में ज्ञान हस्तांतरण और क्षमता निर्माण को सुविधाजनक बनाना।
- यह सुनिश्चित करना कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और साझेदारी के माध्यम से एआई खुला, सुलभ और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बना रहे।
The document The Hindi Editorial Analysis- 1st March 2025 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC is a part of the UPSC Course Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly.
All you need of UPSC at this link: UPSC
|
7 videos|3454 docs|1081 tests
|
FAQs on The Hindi Editorial Analysis- 1st March 2025 - Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC
| 1. आर्द्रभूमि संरक्षण का महत्व क्या है? |  |
Ans. आर्द्रभूमि संरक्षण का महत्व इस तथ्य में निहित है कि यह जैव विविधता, जल प्रबंधन, और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये क्षेत्र प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखते हैं और अनेक वन्यजीवों के लिए निवास स्थल प्रदान करते हैं।
| 2. भारत में आर्द्रभूमियों की स्थिति क्या है? |  |
Ans. भारत में आर्द्रभूमियों की स्थिति चिंताजनक है। कई आर्द्रभूमियाँ Urbanization, औद्योगिकीकरण, और जलवायु परिवर्तन के कारण क्षति का सामना कर रही हैं। यह स्थिति न केवल पारिस्थितिकी पर असर डालती है, बल्कि मानव जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है।
| 3. आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं? |  |
Ans. आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए कुछ उपायों में संरक्षण नीतियों का निर्माण, स्थानीय समुदायों की भागीदारी, और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना शामिल हैं। इसके अलावा, जागरूकता कार्यक्रम और शिक्षा भी महत्वपूर्ण हैं।
| 4. भारत की एआई महत्वाकांक्षाएँ क्या हैं? |  |
Ans. भारत की एआई महत्वाकांक्षाएँ आर्थिक विकास, तकनीकी नवाचार, और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बढ़त हासिल करने पर केंद्रित हैं। सरकार और उद्योग मिलकर एआई को स्वास्थ्य, कृषि, और स्मार्ट शहरों में लागू करने पर काम कर रहे हैं।
| 5. आर्द्रभूमि संरक्षण और एआई का संबंध क्या है? |  |
Ans. आर्द्रभूमि संरक्षण में एआई का उपयोग डेटा विश्लेषण, पर्यावरण निगरानी, और प्रबंधन निर्णय लेने में मदद कर सकता है। एआई तकनीकें आर्द्रभूमियों की स्थिति का मूल्यांकन करने और संरक्षण प्रयासों को अनुकूलित करने में सहायक हो सकती हैं।
Related Searches





















