UPSC Exam > UPSC Notes > Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly > The Hindi Editorial Analysis- 21st January 2025
The Hindi Editorial Analysis- 21st January 2025 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC PDF Download
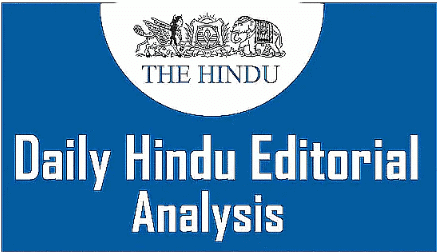
यूजीसी के मसौदा विनियमन में गंभीर संवैधानिक मुद्दे हैं
यह समाचार क्यों है?
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने विश्वविद्यालयों में कुलपतियों (वीसी) के चयन और नियुक्ति के संबंध में एक मसौदा विनियमन प्रस्तुत किया है।
- इस प्रस्ताव को गैर-भाजपा नेतृत्व वाली राज्य सरकारों की ओर से विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जिनका तर्क है कि यह संविधान में निहित संघीय सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।
यूजीसी द्वारा प्रस्तावित संशोधन का विवरण
- यूजीसी के संशोधन का उद्देश्य पात्रता मानदंड का विस्तार करके, कुलपति नियुक्तियों को नियंत्रित करने वाले विनियमन 2010 को अद्यतन करना है।
- पूर्ववर्ती मानदंड: पुराने नियम के तहत, केवल प्रोफेसर के रूप में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले शिक्षाविद ही कुलपति पद के लिए योग्य थे।
- नया प्रस्ताव: संशोधित प्रस्ताव में उद्योग, लोक प्रशासन या सार्वजनिक नीति जैसे विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवरों को शामिल किया गया है, बशर्ते उनके पास 10 या अधिक वर्षों का अनुभव हो।

यूजीसी अधिनियम, 1956 का उद्देश्य
- यूजीसी अधिनियम की स्थापना भारत भर के विश्वविद्यालयों में समन्वय और मानक निर्धारित करने के लिए की गई थी।
- इसका प्राथमिक लक्ष्य विश्वविद्यालय शिक्षा को बढ़ावा देना तथा शिक्षण, अनुसंधान और परीक्षाओं में गुणवत्ता सुनिश्चित करना है।
- अधिनियम के अंतर्गत यूजीसी के कार्य:
- विश्वविद्यालयों के रखरखाव और विकास के लिए धन आवंटित करना।
- शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उपाय सुझाना।
- विश्वविद्यालयों के लिए अनुदान पर सरकारों को सलाह देना।
- विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित जानकारी एकत्रित करना और उसका प्रसार करना।
यूजीसी की भूमिका और सीमाएं
- यूजीसी अधिनियम की धारा 26 यूजीसी को विनियम बनाने का अधिकार देती है, लेकिन ये विनियम अधिनियम के उद्देश्यों के अनुरूप होने चाहिए।
- यह अधिनियम कुलपतियों के चयन या नियुक्ति तक विस्तारित नहीं है, क्योंकि ये संबंधित राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानूनों द्वारा शासित होते हैं।
- कानूनी मिसाल: सुरेश पाटिलखेड़े बनाम महाराष्ट्र विश्वविद्यालय के कुलाधिपति एवं अन्य (2011) के मामले में बंबई उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि कुलपतियों के चयन और नियुक्ति का शैक्षिक मानकों पर सीधा असर नहीं पड़ता है।
- इससे पता चलता है कि कुलपति नियुक्तियों को विनियमित करने का यूजीसी का प्रयास उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो सकता है और इसे अवैध माना जा सकता है।
विनियम बनाम राज्य कानून
- एक महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दा यह है कि क्या यूजीसी के नियम राज्य कानूनों का स्थान ले सकते हैं।
- बॉम्बे उच्च न्यायालय का रुख: न्यायालय ने निर्धारित किया कि यूजीसी नियम अधीनस्थ कानून हैं और वे राज्य कानूनों को दरकिनार नहीं कर सकते।
- सर्वोच्च न्यायालय का रुख: कल्याणी मथिवानन बनाम के.वी. जयराज एवं अन्य (2015) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि यूजीसी के नियम विश्वविद्यालयों पर बाध्यकारी हैं।
- न्यायालय ने संकेत दिया कि इन विनियमों की प्रभावशीलता के लिए संसदीय अनुमोदन आवश्यक है, यद्यपि इस व्याख्या की जांच की गई है।
संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से समाधान
- संविधान का अनुच्छेद 254 राज्य और केन्द्रीय कानूनों के बीच संबंधों से संबंधित है।
- केवल केंद्रीय कानून, जिन्हें संसद द्वारा पारित किया जाता है तथा राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत किया जाता है, को राज्य के कानूनों को रद्द करने का अधिकार है।
- यूजीसी के नियम, अधीनस्थ कानून होने के कारण, अनुच्छेद 254 के अंतर्गत केन्द्रीय कानूनों के मानदंडों को पूरा नहीं करते।
निष्कर्ष
- यूजीसी द्वारा तैयार किया गया मसौदा विनियमन संवैधानिक मुद्दे उठाता है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि यह यूजीसी अधिनियम के तहत आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
- यह स्थिति उच्च शिक्षा के प्रशासन में संघीय सिद्धांतों और राज्य स्वायत्तता के बीच संतुलन बनाए रखने के महत्व को रेखांकित करती है।
IMEC को प्राथमिकता देना अमेरिका के सर्वोत्तम हित में है
चर्चा में क्यों?
भारत -मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (आईएमईसी) एक महत्वपूर्ण बहुपक्षीय पहल है जिसका उद्देश्य भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच व्यापार, संपर्क और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना है।
- आईएमईसी को चीन की बेल्ट एंड रोड पहल (बीआरआई) के जवाब के रूप में देखा जाता है, जिसका उद्देश्य परिवहन और व्यापार मार्गों में सुधार के लिए उन्नत भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करना है।
अमेरिका-भारत संबंधों का विकास 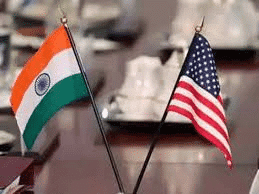
- 1990 के दशक से, विशेषकर राष्ट्रपति क्लिंटन के प्रशासन के दौरान, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच संबंध एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी के रूप में विकसित हुए हैं।
- यह साझेदारी अमेरिका में द्विदलीय आम सहमति द्वारा समर्थित है, जिसमें आर्थिक विकास, क्षेत्रीय सुरक्षा और साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर जोर दिया गया है ।
- जैसे-जैसे वैश्विक गतिशीलता बदलती है, इस साझेदारी का महत्व बढ़ता जाता है, जिससे पारस्परिक लाभ और सहयोग के अवसर उत्पन्न होते हैं।
भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (आईएमईसी)
- 2023 में घोषित, IMEC का उद्देश्य रेलवे, शिपिंग नेटवर्क और डिजिटल संचार प्रणालियों सहित उन्नत बुनियादी ढांचे के माध्यम से भारत, मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ना है ।
- यह पहल व्यापार संपर्क बढ़ाने और परिवहन लागत को कम करने के लिए सीमा पार बिजली ग्रिड, हाइड्रोजन पाइपलाइन और डिजिटल केबल जैसे प्रमुख घटकों को विकसित करने पर केंद्रित है।
- आईएमईसी का उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाना तथा संबंधित क्षेत्रों के बीच गहरे आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना है।
अमेरिकी नेतृत्व के लिए अवसर
- आईएमईसी संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए बहुपक्षीय साझेदारी में अपनी भूमिका को मजबूत करने तथा भारत के सामरिक हितों के साथ तालमेल बिठाने का अवसर प्रस्तुत करता है ।
- IMEC का समर्थन करके, अमेरिका चीन के BRI के लिए एक विकल्प पेश कर सकता है, खुले व्यापार मार्ग सुनिश्चित कर सकता है, ऊर्जा सुरक्षा में सुधार कर सकता है और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा दे सकता है।
- इस संरेखण से अमेरिकी व्यवसायों को लाभ हो सकता है तथा क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव बढ़ सकता है।
IMEC के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ
- आईएमईसी अभी भी वैचारिक चरण में है और इसके सफल कार्यान्वयन के लिए भागीदार देशों के बीच व्यापक योजना और सहयोग की आवश्यकता है।
- महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में निवेश, प्रतिस्पर्धी राष्ट्रीय प्राथमिकताएं और निजी क्षेत्र की भागीदारी इस पहल के लिए गंभीर चुनौतियां पेश करती हैं।
- निजी क्षेत्र की भागीदारी को आकर्षित करने के लिए कॉर्पोरेट निवेशकों को शामिल करना तथा रिटर्न के लिए स्पष्ट मार्ग उपलब्ध कराना आवश्यक है।
भाग लेने वाले देशों की भूमिका
- फ्रांस, ग्रीस, इटली, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब जैसे देश आईएमईसी के विकास में सक्रिय कदम उठा रहे हैं।
- उदाहरण के लिए, फ्रांस ने इस पहल की देखरेख के लिए गेरार्ड मेस्ट्रालेट को नियुक्त किया है, तथा इसकी आर्थिक क्षमता पर जोर दिया है।
- संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब आईएमईसी को पश्चिम के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के साधन के रूप में देखते हैं, जबकि इराक और तुर्की जैसे अन्य देश इस गलियारे के पूरक के रूप में व्यापार समझौते शुरू कर रहे हैं।
भारत के लिए लाभ
- आईएमईसी भारत को महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ प्रदान करता है, जिसमें व्यापार लागत में कमी और समुद्री रसद में सुधार शामिल है ।
- इस गलियारे का उद्देश्य स्वेज नहर जैसे महत्वपूर्ण मार्गों पर निर्भरता कम करना तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आकर्षित करना है।
- स्वयं को BRI के विकल्प के रूप में स्थापित करके भारत पश्चिम एशिया और यूरोप के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर सकता है, तथा अपनी भू-राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को बढ़ा सकता है।
पर्यावरणीय निहितार्थ
- आईएमईसी भारत के हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्यों के अनुरूप है , तथा डीकार्बोनाइजेशन प्रयासों का समर्थन करता है और हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देता है।
- हरित हाइड्रोजन पर जर्मनी और जापान जैसे देशों के साथ सहयोग से उत्सर्जन को कम करने और हरित प्रौद्योगिकी क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिल सकती है।
निष्कर्ष
- आईएमईसी के सफल कार्यान्वयन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत दोनों की ओर से मजबूत नेतृत्व और समन्वय की आवश्यकता है , जो क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को नया रूप देने की इसकी क्षमता को पहचानते हैं।
- ट्रम्प प्रशासन के अब्राहम समझौते जैसे पूर्ववर्ती प्रशासनों द्वारा तैयार किए गए आधारभूत कार्यों ने IMEC के कूटनीतिक और रणनीतिक ढांचे के लिए मंच तैयार किया है।
- भारत और अमेरिका के बीच भावी नेतृत्व और सहयोग, IMEC के आर्थिक और पर्यावरणीय उद्देश्यों को पूरा करने तथा इसकी दीर्घकालिक सफलता और स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण होगा।
हमें न्यायाधीशों के रूप में प्रतिष्ठित न्यायविदों की आवश्यकता है
यह समाचार क्यों है?
भारतीय न्यायपालिका लंबित मामलों और रिक्त पदों के कारण संकट में है। प्रतिष्ठित न्यायविदों की नियुक्ति का प्रस्ताव इस लंबित मामले को कम करने में मदद कर सकता है।
भारतीय न्यायिक प्रणाली में वर्तमान मुद्दे
- भारत की न्यायिक प्रणाली वर्तमान में लंबित मामलों की गंभीर समस्या से जूझ रही है, साथ ही न्यायिक पदों की बड़ी संख्या भी रिक्त है।
- 1 जनवरी 2025 तक उच्च न्यायालयों में स्वीकृत 1,122 पदों में से 371 पद रिक्त हैं। उदाहरण के लिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय अपनी क्षमता के केवल 50% पर काम कर रहा है।
- इस कमी के कारण भारत के सभी उच्च न्यायालयों में लगभग 60 लाख मामले लंबित हैं, जो चिंताजनक बात है।
- न्याय मिलने में देरी के कारण न्याय व्यवस्था में लोगों का भरोसा और आस्था कम हो रही है। इस स्थिति में न्यायपालिका और सरकार दोनों को विश्वास बहाल करने और समय पर न्याय सुनिश्चित करने के लिए तत्काल और प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता है।
समस्या को सुलझाने में कठिनाइयाँ
- कॉलेजियम की सिफारिशों और नियुक्तियों में हाल के सुधारों के बावजूद, ये सेवानिवृत्ति की दर और केस दाखिल करने की बढ़ती संख्या के साथ तालमेल नहीं रख पाए हैं।
- न्यायाधीशों को वर्तमान में अत्यधिक कार्यभार का सामना करना पड़ रहा है, जिससे मामलों की विवेचना की गुणवत्ता और सम्पूर्णता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
- प्रभावी न्याय प्रदान करने के लिए, पूर्ण क्षमता के साथ कार्यरत न्यायपालिका का पर्याप्त स्टाफ होना अत्यंत आवश्यक है।
अनुच्छेद 124(3)(सी) और 217(2)(सी) का महत्व
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124(3)(सी) सर्वोच्च न्यायालय में प्रतिष्ठित न्यायविदों की नियुक्ति की अनुमति देता है। हालाँकि, इस प्रावधान का अभी तक उपयोग नहीं किया गया है।
- अनुच्छेद 217(2)(सी), जो उच्च न्यायालयों में समान नियुक्तियों की अनुमति देता था, को स्पष्ट औचित्य के बिना निरस्त कर दिया गया।
- इन अनुच्छेदों का उपयोग करके प्रतिष्ठित न्यायविदों को शामिल करके वर्तमान संकट को काफी हद तक कम किया जा सकता है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका, पोलैंड और स्पेन जैसे देशों में आम बात है।
न्यायपालिका में शिक्षाविदों की नियुक्ति के लाभ
- न्यायपालिका में प्रतिष्ठित न्यायविदों और शिक्षाविदों की नियुक्ति से जटिल मामलों में विशेषज्ञता, शोध-आधारित अंतर्दृष्टि और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देकर न्यायिक निर्णय लेने की क्षमता में काफी वृद्धि हो सकती है।
- ऐसी नियुक्तियां अकादमिक ज्ञान और व्यावहारिक न्यायिक कार्य के बीच की खाई को प्रभावी ढंग से पाट सकती हैं, तथा कानूनी मुद्दों पर नए और विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकती हैं।
- इसके अलावा, न्यायपालिका में अकादमिक प्रतिभाओं को शामिल करने से कानूनी प्रणाली के भीतर विविध विशेषज्ञता के मूल्य के बारे में सकारात्मक संदेश जाता है, तथा न्याय के प्रति अधिक समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता है।
शिक्षाविदों की नियुक्ति में चुनौतियाँ
- न्यायपालिका में शिक्षाविदों की नियुक्ति में मुख्य चुनौतियों में से एक है, उनमें न्यायालयीन अनुभव, प्रक्रियागत ज्ञान और न्यायिक सीमाओं की समझ का अभाव।
- इसके अतिरिक्त, मौजूदा न्यायपालिका के भीतर इस नवीन दृष्टिकोण को स्वीकार करने में प्रतिरोध हो सकता है, जिससे इसके कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
- हालांकि, उचित प्रशिक्षण और प्रक्रियात्मक पहलुओं की जानकारी से इन चुनौतियों पर काबू पाया जा सकता है, जिससे शिक्षाविदों को न्यायिक वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से अनुकूलन करने में मदद मिलेगी।
समस्या के समाधान के उपाय
- न्यायपालिका में मौजूदा लंबित पदों और रिक्तियों के मुद्दे को हल करने के लिए, सरकार के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह न्यायिक नियुक्तियों के संबंध में कॉलेजियम की सिफारिशों का तुरंत अनुपालन करे।
- अनुच्छेद 217(2)(सी) को पुनः लागू करना तथा उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायविदों की नियुक्ति के लिए अनुच्छेद 124(3)(सी) को लागू करना महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव ला सकता है।
- इसके अतिरिक्त, न्यायपालिका में शिक्षाविदों की विशेषज्ञता का लाभ उठाने से इसकी क्षमता मजबूत हो सकती है, लंबित मामलों में कमी आ सकती है, तथा न्याय प्रदान करने की समग्र गुणवत्ता में वृद्धि हो सकती है।
निष्कर्ष
- न्यायपालिका के लिए संसाधन के रूप में शैक्षणिक समुदाय का उपयोग करने से एक गतिशील और मजबूत न्यायिक प्रणाली सुनिश्चित हो सकती है जो संवैधानिक सिद्धांतों के साथ व्यावहारिक विचारों को प्रभावी ढंग से संतुलित कर सके।
- इस दृष्टिकोण में न्यायिक कार्य में काफी सुधार लाने तथा न्यायपालिका में लंबित मामलों और रिक्त पदों की चुनौतियों का समाधान करने की क्षमता है।
The document The Hindi Editorial Analysis- 21st January 2025 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC is a part of the UPSC Course Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly.
All you need of UPSC at this link: UPSC
|
7 videos|3454 docs|1081 tests
|
Related Searches
















