UPSC Exam > UPSC Notes > Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly > The Hindi Editorial Analysis- 23rd April 2025
The Hindi Editorial Analysis- 23rd April 2025 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC PDF Download
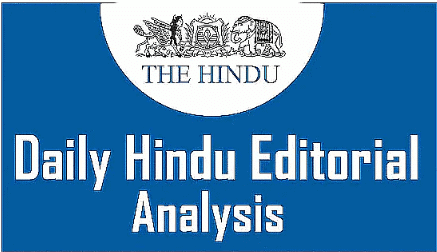
आर्कटिक क्षेत्र में भारत की संभावनाओं का अन्वेषण
चर्चा में क्यों?
आर्कटिक क्षेत्र में आगामी वाणिज्यिक संभावनाओं में भारत की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए तथा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उसके संसाधनों का दुरुपयोग न हो।
परिचय
- वैश्विक व्यापार इस समय तीव्र उतार-चढ़ाव का सामना कर रहा है, जिसमें अमेरिका से उत्पन्न अनिश्चितताएं भी शामिल हैं । यह स्थिति देशों को वैकल्पिक व्यापार रणनीतियों को अधिक सक्रियता से तलाशने के लिए प्रेरित कर रही है।
- इसके साथ ही, क्षेत्रीय गठबंधनों के विघटन और जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव के कारण आपूर्ति श्रृंखलाओं और व्यापार मार्गों से संबंधित साझेदारियों पर जोर बढ़ रहा है ।
- आर्कटिक क्षेत्र , जिसे अक्सर जलवायु परिवर्तन का बैरोमीटर माना जाता है, न केवल अपने पर्यावरणीय महत्व के लिए बल्कि अपनी भू-राजनीतिक क्षमता के लिए भी प्रमुखता प्राप्त कर रहा है ।
- जैसे-जैसे समुद्र का स्तर बढ़ता जा रहा है और नए नौगम्य मार्ग उभर रहे हैं, आर्कटिक नए सामरिक और वाणिज्यिक अवसर प्रदान करने के लिए तैयार है ।
- आने वाले दशकों में, यह वैश्विक दक्षिण के लिए एक महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन बनने की उम्मीद है ।
- यद्यपि आर्कटिक के प्राकृतिक भण्डारों के अंधाधुंध दोहन से बचना आवश्यक है, परन्तु भारत को इस महत्वपूर्ण सीमांत क्षेत्र के भविष्य के वाणिज्यिक परिदृश्य को आकार देने में अपनी रुचि दर्शानी होगी।
आर्कटिक समुद्री बर्फ और सामरिक महत्व
नासा की रिपोर्ट के अनुसार आर्कटिक समुद्री बर्फ 1981-2010 के औसत की तुलना में प्रति दशक 12.2% की दर से घट रही है । यह तेजी से पिघलना उत्तरी समुद्री मार्ग (NSR) तक पहुंच को आसान बना रहा है , जिसमें वैश्विक शिपिंग में क्रांति लाने की क्षमता है। अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ने वाला NSR यूरोप और एशिया के बीच सबसे छोटे मार्ग के रूप में उभर रहा है ।
- एनएसआर पर भारत का परिप्रेक्ष्य भारत एनएसआर को न केवल एक आर्थिक अवसर के रूप में देखता है, बल्कि एक रणनीतिक और भू-राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखता है।
व्यापार मार्ग परिवर्तन: एनएसआर के रणनीतिक निहितार्थ
| पहलू | विवरण |
|---|---|
| समय और लागत दक्षता | एनएसआर से माल ढुलाई का समय काफी कम हो जाएगा तथा माल ढुलाई लागत भी कम हो जाएगी । |
| रणनीतिक लाभ | एनएसआर भारत को वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है जो भू-राजनीतिक तनावों के प्रति कम संवेदनशील है, जिससे भारत की रणनीतिक स्थिति मजबूत होगी। |
| वैश्विक रुचि | आर्कटिक के प्रति गैर-आर्कटिक देशों की रुचि बढ़ रही है, तथा आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षकों की संख्या अब आर्कटिक देशों से अधिक हो गई है। |
| भारत की भागीदारी | भारत 20वीं सदी के प्रारंभ से ही आर्कटिक मामलों में सक्रिय रूप से शामिल रहा है, जिसका प्रमाण स्वालबार्ड संधि (1920) में इसकी भागीदारी और आर्कटिक अनुसंधान बेस हिमाद्रि की स्थापना है । |
भारत के घरेलू उपाय
- 2025-26 के बजट में , भारत सरकार ने समुद्री विकास कोष के लिए 3 बिलियन डॉलर आवंटित किए ।
- इस निधि का फोकस निम्नलिखित पर है:
- जहाज निर्माण क्लस्टर
- आर्कटिक-सक्षम बेड़े का विस्तार
- बर्फ तोड़ने वाले जहाजों में निवेश
- लचीले बुनियादी ढांचे का विकास
कार्रवाई आवश्यक
| उद्देश्य | विवरण |
| जहाज निर्माण क्षमता को मजबूत करना | आर्कटिक परिस्थितियों के लिए उपयुक्त जहाज बनाने की भारत की क्षमता को बढ़ाना। |
| आर्कटिक की कठिन परिस्थितियों में नेविगेट करें | चरम आर्कटिक वातावरण में कार्य करने के लिए विशेषज्ञता और प्रौद्योगिकी विकसित करना। |
| बर्फ श्रेणी के जहाज विकसित करना | बर्फ से ढके पानी में चलने में सक्षम जहाज बनाना। |
| जमे हुए पानी में कुशलतापूर्वक संचालन करें | बर्फीले समुद्री परिस्थितियों में परिचालन प्रभावशीलता सुनिश्चित करना। |
| प्रशिक्षण एवं जनशक्ति को बढ़ावा देना | एनएसआर के लिए आवश्यक परिचालन और सुरक्षा मानकों को पूरा करना। |
वैज्ञानिक एवं जलवायु प्रभाव
- भारत विभिन्न संस्थानों के सहयोग से मानसून और कृषि पर आर्कटिक के प्रभाव पर सक्रिय रूप से शोध कर रहा है , जिनमें शामिल हैं:
- शासन और सतत विकास संस्थान
- राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद
- 2024 में , एनएसआर के माध्यम से परिवहन किया गया माल 37.9 मिलियन टन तक पहुंच गया, जो 2010 में 41,000 टन से उल्लेखनीय वृद्धि है ।
- हालाँकि, यह वृद्धि वैश्विक तापमान के 1.5°C की सीमा को पार करने के साथ हुई , जिससे जलवायु परिवर्तन के बारे में चिंताएँ बढ़ गईं।
कार्रवाई का आह्वान एवं वैश्विक संवाद
- भारत की 2022 आर्कटिक नीति को सैद्धांतिक योजना से व्यावहारिक कार्यान्वयन की ओर ले जाने की आवश्यकता है।
- मई 2025 में नई दिल्ली में आयोजित होने वाला आर्कटिक सर्कल इंडिया फोरम निम्नलिखित के लिए अवसर प्रस्तुत करता है:
- आर्कटिक मुद्दों पर भारत-केंद्रित परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करना ।
- बहुपक्षीय सहयोग , क्षमता निर्माण और हितधारक सहभागिता को उत्प्रेरित करना ।
- इससे आर्कटिक पहलों की देखरेख के लिए एक 'ध्रुवीय राजदूत' की नियुक्ति की संभावना बढ़ गई है ।
प्रमुख नीतिगत दुविधा
भारत के लिए मुख्य प्रश्न यह है: "हमें सूर्य के कितने करीब उड़ना चाहिए?"
- इसमें संतुलन शामिल है:
- आर्कटिक में वाणिज्यिक अवसर, नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा की आवश्यकता।
- इस संतुलन को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है:
- तत्काल नीति स्पष्टता , अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और जलवायु मुद्दों पर मजबूत ध्यान।
बर्फ और आग से खेलना
- अपनी विस्तृत आर्कटिक तटरेखा, आर्कटिक नेविगेशन में मजबूत विशेषज्ञता और अच्छी तरह से प्रशिक्षित कार्मिकों के साथ, रूस उत्तरी समुद्री मार्ग (एनएसआर) की खोज में भारत के लिए एक स्वाभाविक साझेदार है।
- जुलाई 2022 में मास्को में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक के बाद, व्यापार और सहयोग पर भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग के तहत एनएसआर पर एक कार्य समूह की स्थापना की गई थी।
- चेन्नई -व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारे को पेवेक , टिक्सी और सबेट्टा जैसे प्रमुख एनएसआर बंदरगाहों के लिए एक संभावित लिंक के रूप में देखा गया है ।
- हालाँकि, भारत के सामने एक दुविधा है: यदि वह रूस के साथ बहुत अधिक निकटता से जुड़ता है, तो यह माना जा सकता है कि वह अप्रत्यक्ष रूप से चीन के ध्रुवीय रेशम मार्ग का समर्थन कर रहा है , जो चीन की बेल्ट एंड रोड पहल (बीआरआई) का विस्तार है।
- ध्रुवीय रेशम मार्ग का उद्देश्य चीन को आर्कटिक शिपिंग मार्गों पर अधिक नियंत्रण प्रदान करना तथा मलक्का जलडमरूमध्य , जो एक महत्वपूर्ण वैश्विक व्यापार अवरोध है, को पार करना है।
निष्कर्ष
- यदि भारत पश्चिमी देशों के साथ पूरी तरह जुड़ जाता है और अमेरिका के साथ साझेदारी करता है, तो उसे आर्कटिक क्षेत्र में रूस द्वारा नियंत्रित विशाल संसाधनों तक पहुंच खोने का खतरा है ।
- एक अधिक संतुलित दृष्टिकोण, हालांकि चुनौतीपूर्ण है, में अमेरिका और रूस दोनों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखना शामिल होगा ।
- इसके अतिरिक्त, भारत को जापान और दक्षिण कोरिया जैसे अन्य देशों के साथ सहयोग करना चाहिए , जो आर्कटिक में बढ़ती रूस-चीन साझेदारी के बारे में समान चिंताएं साझा करते हैं।
- भारत, जापान और दक्षिण कोरिया मिलकर आर्कटिक परिषद में निष्पक्ष सुधारों की वकालत कर सकते हैं , जिससे अधिक समावेशी और संतुलित शासन संरचना को बढ़ावा मिल सके।
The document The Hindi Editorial Analysis- 23rd April 2025 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC is a part of the UPSC Course Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly.
All you need of UPSC at this link: UPSC
|
7 videos|3454 docs|1081 tests
|
Related Searches
















