The Hindi Editorial Analysis- 27th May 2025 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC PDF Download
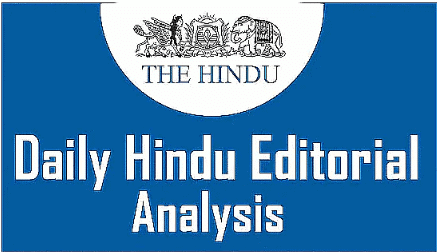
मानसून के बावजूद गर्मी से निपटने पर ध्यान केंद्रित
यह समाचार क्यों है?
- जैसे-जैसे जलवायु संबंधी चरम स्थितियां अधिक गंभीर होती जाएंगी, प्रतिक्रियात्मक आपातकालीन देखभाल से हटकर समानता पर आधारित निवारक सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों पर जोर दिया जाना चाहिए।
परिचय
- जलवायु और स्वास्थ्य पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन 'भारत 2047: जलवायु-लचीले भविष्य का निर्माण' के दौरान , एक ट्रेड यूनियन नेता ने कारखानों में अत्यधिक गर्मी झेलने वाले परिधान श्रमिकों के वास्तविक जीवन के अनुभवों को साझा किया। उसी समय, एक जलवायु मॉडलर ने वेट-बल्ब तापमान की अवधारणा पर चर्चा की। इन दो दृष्टिकोणों, एक विज्ञान पर आधारित और दूसरा वास्तविकता पर, ने विभिन्न क्षेत्रों के बीच सहयोग के महत्व को उजागर किया।
- इस कार्यक्रम में अप्रत्याशित साझेदारी की शक्ति पर जोर दिया गया, जिसमें बाल रोग विशेषज्ञों और वास्तुकारों, मातृ स्वास्थ्य विशेषज्ञों और शहर के इंजीनियरों जैसे विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों के साथ-साथ शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं को एक साथ लाया गया ।
भारत में गर्मी और सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियां
समय से पहले मानसून, लगातार गर्मी
- मानसून के समय से पहले आगमन के बावजूद, भारत अभी भी भीषण गर्मी से जूझ रहा है, यह प्रवृत्ति जारी रहने की संभावना है तथा इससे चुनौतियां भी उत्पन्न होंगी।
अत्यधिक गर्मी का सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रभाव
अत्यधिक गर्मी के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रभाव गंभीर और विविध हैं, जिनमें शामिल हैं:
- निर्जलीकरण
- लू लगना
- दीर्घकालिक बीमारियों का बिगड़ना
- स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे पर दबाव अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच रहा है।
वर्तमान स्वास्थ्य प्रणाली प्रतिक्रिया: अंतराल और आवश्यकताएं
| पहलू | वर्तमान दृष्टिकोण | आवश्यक बदलाव |
|---|---|---|
| केंद्र | आपातकालीन देखभाल (अस्पताल के बिस्तर, IV द्रव, आपातकालीन प्रवेश) | निवारक, सक्रिय स्वास्थ्य देखभाल |
| प्रतिक्रिया की प्रकृति | एकाकी, पृथक | अंतःविषयक और एकीकृत |
| समय | रिएक्टिव | पूर्वानुमानात्मक और निवारक |
| नतीजा | अस्थायी राहत | दीर्घकालिक लचीलापन और सुरक्षा |
भारत की स्वास्थ्य प्रणाली के लिए प्रमुख सिफारिशें
- प्रतिक्रियात्मक से निवारक देखभाल की ओर संक्रमण: गर्मी से उत्पन्न आपात स्थितियों के प्रबंधन से हटकर गर्मी से संबंधित बीमारियों की रोकथाम पर ध्यान केन्द्रित करें।
- अंतःविषयक दृष्टिकोण अपनाएं: सार्वजनिक स्वास्थ्य, शहरी नियोजन, जलवायु विज्ञान और सामुदायिक नेतृत्व में विशेषज्ञता को संयोजित करें।
- स्थानीय क्षमता और नेतृत्व को मजबूत बनाना: समानता-केंद्रित ताप तन्यकता रणनीतियों का नेतृत्व करने के लिए स्थानीय प्रणालियों को सशक्त बनाना।
वर्तमान गर्मी-संबंधी स्वास्थ्य देखभाल प्रथाओं में अंतराल
- हीट एक्सपोजर स्क्रीनिंग का अभाव: कई स्वास्थ्य सेवा प्रदाता नियमित जांच के दौरान हीट एक्सपोजर की जांच नहीं करते हैं। हीट स्ट्रोक का अक्सर गलत निदान किया जाता है या उसे अनदेखा कर दिया जाता है, खासकर व्यस्त आपातकालीन स्थितियों में।
- मानकीकृत नैदानिक प्रोटोकॉल की आवश्यकता: गर्मी से होने वाली बीमारियों के निदान और प्रबंधन के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल आवश्यक हैं। अस्पतालों को तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से गर्मियों में अभ्यास करना चाहिए।
स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग्स में सरल, प्रभावी निवारक कदम
| पहल | विवरण | प्रभाव |
|---|---|---|
| समर्पित 'हीट कॉर्नर' | गर्मी से बीमार मरीजों के लिए आपातकालीन विभागों में विशेष क्षेत्र | तेज़, केंद्रित देखभाल |
| प्री-स्टॉकिंग कूलिंग किट | स्वास्थ्य केन्द्रों पर शीतलन आपूर्ति की तत्काल उपलब्धता | तत्काल उपचार क्षमता |
| डिस्चार्ज के बाद फॉलो-अप | गर्मी से होने वाली बीमारियों से ठीक हो रहे मरीजों की निगरानी | जटिलताओं और पुनः प्रवेश को कम करता है |
| ग्रीष्मकालीन अभ्यास | नियमित आपातकालीन तैयारी अभ्यास | चरम गर्मी के दौरान अस्पताल की तैयारी सुनिश्चित करता है |
गर्मी से होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण
- स्वास्थ्य सेवा से परे: गर्मी से होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए जोखिम को कम करना ज़रूरी है - न कि केवल लक्षणों का उपचार। इसके लिए सभी क्षेत्रों में समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता है:
- शहरी नियोजन गर्मी के जोखिम को कम करने के लिए आवास डिजाइन और सार्वजनिक स्थानों पर पुनर्विचार करें।
- जल आपूर्ति प्रबंधन: गर्मी के चरम महीनों के दौरान विश्वसनीय जल उपलब्धता सुनिश्चित करें।
- श्रम सुरक्षा: विनियमित बाहरी कार्य घंटे और अन्य सुरक्षा उपाय लागू करें।
- जलवायु विज्ञान और स्वास्थ्य सहयोग: जलवायु-स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा निर्देशित डेटा-संचालित, समयबद्ध हस्तक्षेप का उपयोग करें।
जलवायु-स्वास्थ्य लचीलेपन के लिए उत्कृष्टता के नेटवर्क का निर्माण
- उत्कृष्टता के पृथक 'केन्द्रों' से आगे बढ़कर उत्कृष्टता के नेटवर्क की ओर बढ़ें जो:
- सार्वजनिक स्वास्थ्य, जलवायु विज्ञान, शहरी विकास, श्रम अधिकार और सामुदायिक आवाजों के विशेषज्ञों को एक साथ लाना।
- सह-डिजाइन समाधान जीवंत वास्तविकताओं पर आधारित होते हैं, जैसे:
- झुग्गी-झोपड़ियों में आश्रय स्थलों पर धुंध का छिड़काव
- आंगनवाड़ी केन्द्रों में ठंडी छत
अत्यधिक गर्मी: सामाजिक अन्याय को बढ़ाने वाला कारक
- सिर्फ एक मौसमी घटना नहीं: अत्यधिक गर्मी सबसे कमजोर आबादी को असमान रूप से प्रभावित करती है:
- अनौपचारिक विक्रेता फुटपाथ पर काम कर रहे हैं
- तंग कक्षाओं में बच्चे
- खराब हवादार घरों में रहने वाले बुजुर्ग
- जिनके पास कोई विकल्प नहीं है, उन्हें सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है: बिना आश्रय के कचरा बीनने वाले और टिन की छतों के नीचे दिहाड़ी मज़दूर जैसे लोग सबसे ज़्यादा तब पीड़ित होते हैं जब गर्मी का सूचकांक ख़तरे की सीमा को पार कर जाता है। "घर के अंदर रहने" की आम सलाह अक्सर अवास्तविक होती है और गहरी प्रणालीगत असमानताओं को उजागर करती है।
निवारक, समानता-केंद्रित सार्वजनिक स्वास्थ्य की ओर बदलाव
- अत्यधिक गर्मी के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए हमें यह करना होगा:
- प्रतिक्रियात्मक आपातकालीन देखभाल से निवारक, समानता-आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य की ओर बढ़ें।
- मौसम संबंधी आंकड़ों से परे भेद्यता का मानचित्रण करना शुरू करें, जिसमें शामिल हैं:
- लोग कहाँ रहते हैं?
- वे कैसे काम करते हैं
- उनके पास किन संसाधनों का अभाव है?
जीवन रक्षक निवारक उपाय
- रेड अलर्ट अवधि के दौरान प्रातःकाल स्वास्थ्य जांच लागू करें।
- निम्न आय वाले क्षेत्रों में मोबाइल हाइड्रेशन स्टेशन स्थापित करें।
- बेघर लोगों के लिए सब्सिडी वाले ठंडे आश्रय स्थल स्थापित करें।
- बाहरी श्रमिकों के लिए सुरक्षात्मक नीतियां लागू करें।
विज्ञान और नैतिक अनिवार्यता
- इन हस्तक्षेपों का समर्थन करने वाले वैज्ञानिक प्रमाण स्पष्ट हैं।
- नैतिक अनिवार्यता भी उतनी ही मजबूत है: जलवायु लचीलापन तब तक निरर्थक है जब तक कि यह उन लोगों की रक्षा नहीं करता जो सबसे अधिक जोखिम में हैं।
निष्कर्ष
- कार्रवाई के लिए खिड़की कम होती जा रही है, फिर भी आगे का रास्ता साफ है। जैसे-जैसे जलवायु परिवर्तन की चरम स्थितियां बढ़ती जा रही हैं, भारत को इस मौके का दूरदर्शिता और तत्परता के साथ लाभ उठाना चाहिए।
- समानता, विज्ञान और स्थानीय नेतृत्व पर आधारित हमारी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों में ताप प्रतिरोधकता को एकीकृत करके, हम जीवन और आजीविका की रक्षा कर सकते हैं।
- कार्रवाई करने का समय कल या अगले साल नहीं है - यह अभी है। भारत को ऐसा राष्ट्र बनना चाहिए जो तैयारी, सुरक्षा और अग्रणी होने का विकल्प चुनता है।
एक ऐसा ऑपरेशन जो आत्मनिर्भर भारत के बारे में भी था
परिचय
पिछले एक दशक में भारत में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह एक अधिक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र बन गया है। यह परिवर्तन 21वीं सदी में वैश्विक अर्थव्यवस्था , प्रौद्योगिकी और रणनीतिक मामलों में भारत को एक मजबूत खिलाड़ी बनाने की दृष्टि से प्रेरित है। ऑपरेशन सिंदूर की हालिया सफलता एक लचीली आर्थिक और तकनीकी नींव के निर्माण में हुई प्रगति का प्रमाण है।
आइये उन प्रमुख घटनाक्रमों पर नजर डालें जिन्होंने इस परिवर्तन में योगदान दिया है।
औद्योगिक पुनरुत्थान और नवाचार का मार्ग
1. मेक इन इंडिया (2014)
- वर्ष 2014 में "मेक इन इंडिया" की शुरूआत ने वैश्विक विनिर्माण के प्रति भारत के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया।
- नीति का उद्देश्य व्यापार करने में आसानी बढ़ाना , परियोजना अनुमोदन में तेजी लाना तथा घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करना है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स , रक्षा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में गतिविधि और निवेश में वृद्धि हुई।
2. उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं
- वित्तीय प्रोत्साहन देकर विनिर्माताओं को भारत की ओर आकर्षित करने के लिए पीएलआई योजनाएं शुरू की गईं।
- ये योजनाएं विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन को बढ़ावा देने में सहायक रही हैं।
3. Atmanirbhar Bharat Abhiyan (2020)
- 2020 में शुरू किए गए आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना और उन्नत विनिर्माण में वैश्विक नेता बनाना है ।
- इसका फोकस कुशल मूल्य श्रृंखलाओं के निर्माण और रक्षा , इलेक्ट्रॉनिक्स , फार्मास्यूटिकल्स और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में आयात निर्भरता को कम करने पर था ।
- ये क्षेत्र न केवल अर्थव्यवस्था के लिए बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक मजबूती के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।
4. नवाचार और स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र
- भारत नवाचार के केंद्र के रूप में उभरा है और दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप इकोसिस्टम है।
- भारतीय स्टार्ट-अप फिनटेक , एग्रीटेक , हेल्थ टेक और एडटेक जैसे क्षेत्रों में सक्रिय रूप से शामिल हैं , जो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करते हुए स्थानीय चुनौतियों का समाधान कर रहे हैं।
- इसके अतिरिक्त, स्टार्ट-अप रक्षा प्रौद्योगिकी , साइबर सुरक्षा , कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में भी प्रवेश कर रहे हैं ।
5. वैश्विक साझेदारियां
- भारत की आर्थिक उन्नति को अमेरिका-भारत ट्रस्ट पहल और भारत-फ्रांस रोड मैप जैसी वैश्विक साझेदारियों से समर्थन मिल रहा है ।
- ये सहयोग एआई , क्वांटम प्रौद्योगिकी और रक्षा प्रौद्योगिकी जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में संयुक्त प्रयासों को बढ़ावा देते हैं ।
ऑपरेशन सिंदूर: 'मेड इन इंडिया' के लिए एक मील का पत्थर
- ऑपरेशन सिन्दूर एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ, जिसने स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके सटीक हमले करने की भारत की क्षमता को प्रदर्शित किया।
- इस ऑपरेशन ने भारत के एक भरोसेमंद हथियार आयातक से विश्व स्तरीय रक्षा उपकरणों के निर्माता बनने की ओर कदम बढ़ाया ।
- इस ऑपरेशन की सफलता मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत विकसित उपकरणों के कारण संभव हुई, जो आर्थिक और तकनीकी लचीलेपन पर वर्षों के फोकस को दर्शाता है।
रक्षा निर्यात प्रदर्शन
| पहलू | विवरण |
|---|---|
| कुल निर्यात (वित्त वर्ष 25) | ₹23,622 करोड़ |
| पहुँचे हुए देश | लगभग 80 |
| 2029 तक अपेक्षित निर्यात | ₹50,000 करोड़ |
| निजी क्षेत्र का योगदान (वित्त वर्ष 25) | ₹15,233 करोड़ |
रणनीतिक परिसंपत्ति के रूप में प्रौद्योगिकी
- समकालीन विश्व में किसी राष्ट्र की शक्ति, प्रौद्योगिकी में उसके नेतृत्व से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है।
- जो देश कृत्रिम बुद्धिमत्ता , क्वांटम कंप्यूटिंग , जैव प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में पिछड़ रहे हैं, उन्हें दीर्घकालिक कमजोरियों का सामना करना पड़ सकता है।
प्रमुख सरकारी पहल
| पहल | उद्देश्य |
|---|---|
| राष्ट्रीय क्वांटम मिशन | क्वांटम प्रौद्योगिकी में उन्नत अनुसंधान |
| भारत सेमीकंडक्टर मिशन | सेमीकंडक्टर विनिर्माण में क्षमता का विकास करना |
| इसरो मिशन | चंद्रयान और गगनयान अंतरिक्ष क्षमता को दर्शाते हैं |
इन पहलों का उद्देश्य भारत को वैश्विक तकनीकी नेता के रूप में स्थापित करना है, लेकिन पूर्ण सफलता के लिए देशव्यापी भागीदारी की आवश्यकता है।
भारतीय उद्योग की भूमिका
- भारतीय उद्योग प्रमुख क्षेत्रों में सक्रिय रूप से उच्च तकनीक क्षमताओं का निर्माण कर रहा है:
- सेमीकंडक्टर, स्वच्छ प्रौद्योगिकी, अगली पीढ़ी की गतिशीलता, रक्षा और इलेक्ट्रॉनिक्स
- उपग्रह घटकों और प्रक्षेपण प्रणालियों के माध्यम से अंतरिक्ष मिशन में योगदान
- मिसाइलों, ड्रोनों और लड़ाकू प्लेटफार्मों में नवाचारों के साथ रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देना
- एआई के क्षेत्र में उद्योग है:
- 22 भाषाओं में वास्तविक समय अनुवाद के लिए भाषिनी का समर्थन
- कुशल तकनीकी कार्यबल बनाने के लिए फ्यूचरस्किल्स प्राइम के साथ साझेदारी
भविष्य के लिए रणनीतिक प्राथमिकताएँ
- निजी क्षेत्र को:
- अनुसंधान एवं विकास निवेश में तेजी लाएं
- भारत की तकनीकी बढ़त को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियां बनाना
- शैक्षणिक जगत और सार्वजनिक अनुसंधान संस्थानों के साथ मिलकर काम करना
ये सहयोग इस प्रकार होने चाहिए:
- अत्याधुनिक नवाचार को आगे बढ़ाएं
- उद्योग के लिए तैयार इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और तकनीशियनों की एक पाइपलाइन तैयार करें
- वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में भारत की स्थिति को मजबूत करना
निरंतर प्रतिबद्धता के साथ, भारतीय उद्योग उन्नत प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में एक सुरक्षित, आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर सम्मानित भारत को आकार देने में मदद कर सकता है।
भारत की अग्रणी भूमिका
भारत एक ऐसे मोड़ पर है, जिसकी पहचान मजबूत आर्थिक लचीलापन, बढ़ती विनिर्माण क्षमता, नवाचार-संचालित विकास और एक स्पष्ट वैश्विक दृष्टिकोण से है। देश अब दूसरों की बराबरी करने की कोशिश नहीं कर रहा है - यह सक्रिय रूप से भविष्य को आकार दे रहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, इस परिवर्तन के लिए एक मजबूत नींव तैयार की गई है। विकसित भारत की ओर यात्रा के लिए अब उद्योग से सक्रिय और बड़े पैमाने पर भागीदारी की आवश्यकता होगी। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा, "आत्मनिर्भरता न केवल भारत की नीति बन गई है, बल्कि हमारा जुनून भी है।" भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) इस जुनून को बढ़ावा देने और आने वाले वर्षों में भारत के अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचने में सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है।
निष्कर्ष
भारत को अब अपने औद्योगिक, शैक्षणिक और रणनीतिक क्षेत्रों में तकनीकी महत्वाकांक्षा को शामिल करके वैश्विक नवाचार की अगली लहर का नेतृत्व करने का प्रयास करना चाहिए। आगे का रास्ता अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, दूरदर्शी अनुसंधान और एक लचीले नीति पारिस्थितिकी तंत्र के गहन एकीकरण की मांग करता है। व्यापक दृष्टि एक मजबूत, सुरक्षित, आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर सम्मानित भारत की है, जो नवाचार में मानक स्थापित करने और वैश्विक अर्थव्यवस्था के भविष्य को आकार देने में सक्षम है।
|
7 videos|3454 docs|1081 tests
|
FAQs on The Hindi Editorial Analysis- 27th May 2025 - Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC
| 1. मानसून के दौरान गर्मी से निपटने के लिए कौन-कौन सी उपाय किए जा सकते हैं ? |  |
| 2. आत्मनिर्भर भारत योजना क्या है और इसका मानसून से क्या संबंध है ? |  |
| 3. गर्मी के दौरान स्वास्थ्य समस्याएँ क्या हो सकती हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है ? |  |
| 4. मानसून के दौरान किस प्रकार के कृषि उपायों की आवश्यकता होती है ? |  |
| 5. मानसून और गर्मी का जलवायु परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ता है ? |  |
















