The Hindi Editorial Analysis- 29th April 2025 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC PDF Download
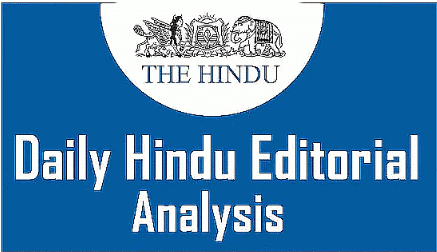
पर्याप्त मजबूत नहीं
चर्चा में क्यों?
पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले की व्यापक निंदा हुई है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भी शामिल है। हालाँकि, 25 अप्रैल, 2025 को यूएनएससी के बयान में संवेदना व्यक्त करते हुए, मुख्य चिंताओं को संबोधित करने में कमी रह गई, विशेष रूप से द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) और लश्कर से उसके संबंधों का उल्लेख न करके। यह प्रतिक्रिया आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में चल रही चुनौतियों को उजागर करती है, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में।
पहलगाम आतंकवादी हमले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का बयान (25 अप्रैल, 2025)
- निंदा: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की।
- संवेदना: भारत और नेपाल के प्रति संवेदना व्यक्त की गई, क्योंकि नेपाल ने इस हमले में अपने एक-एक नागरिक को खो दिया है।
- पाकिस्तान को शामिल करना: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्वाचित अस्थायी सदस्य के रूप में पाकिस्तान को भी वक्तव्य में शामिल किया गया।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वक्तव्य के मुख्य बिंदु:
- अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए आतंकवाद से उत्पन्न खतरे की पुनः पुष्टि।
- अपराधियों और उनके प्रायोजकों को न्याय के दायरे में लाने की आवश्यकता पर बल दिया गया।
अपर्याप्तताएं नोट की गईं:
- विशिष्टता का अभाव: बयान में द रेसिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) का उल्लेख नहीं किया गया, जिस समूह ने हमले की जिम्मेदारी ली है।
- टीआरएफ के संबंधों का उल्लेख नहीं किया गया: लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के साथ टीआरएफ के संबंधों का कोई उल्लेख नहीं किया गया, जिसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है।
- सहयोग के आह्वान का अभाव: वक्तव्य में भारत के साथ सहयोग के लिए विशेष रूप से आह्वान नहीं किया गया, जो कि पिछले उदाहरणों से अलग था।
- सांप्रदायिक तनावों की अनदेखी: बयान में गैर-मुसलमानों को निशाना बनाने के आतंकवादियों के इरादे का जिक्र नहीं किया गया, जिसका उद्देश्य सांप्रदायिक तनावों को भड़काना था।
पिछले वक्तव्यों से तुलना:
- बयान में प्रयुक्त भाषा को "हल्का" माना गया।
- इस परिवर्तन का श्रेय 2025-26 तक परिषद में पाकिस्तान की सदस्यता और चीन के समर्थन को दिया गया, क्योंकि चीन ने पहले भी पाकिस्तान के खिलाफ आलोचनात्मक बयानों पर वीटो लगा दिया था।
बातचीत:
- यह वक्तव्य फ्रांस के दूत, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्तमान अध्यक्ष हैं, द्वारा तैयार किया गया।
- संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और यूनाइटेड किंगडम सहित परिषद के अन्य सदस्यों से सीमित समर्थन मिला।
भारत की प्रतिक्रिया और अगले कदम
- आतंकवाद विरोधी उपाय: भारत जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों के संबंध में निरंतर चर्चा में लगा हुआ है।
- सैन्य विकल्पों पर विचार: खतरे से निपटने के लिए सीमा पार सैन्य विकल्पों पर विचार किया जा रहा है।
संभावित कार्यवाहियाँ:
- भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन और गाजा की स्थिति के जवाब में दिए गए बयान के समान ही एक मजबूत बयान प्रस्तुत कर सकता है।
- भारत पुलवामा हमले के बाद मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करने की तरह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से पहचाने गए आतंकवादियों और टीआरएफ को आतंकवादी घोषित करने की मांग कर सकता है।
- वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) का उपयोग पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों के खिलाफ कार्रवाई बढ़ाने की वकालत करने के लिए किया जा सकता है।
- द्विपक्षीय संबंध: मुंबई, पठानकोट और पुलवामा हमलों जैसी घटनाओं के बाद पाकिस्तानी सहयोग हासिल करने के पिछले प्रयास असफल रहे हैं।
- वर्तमान में तनावपूर्ण संबंधों के कारण पाकिस्तान के साथ राजनयिक संपर्क की संभावना कम ही मानी जा रही है।
- बहुआयामी दृष्टिकोण: भारत को तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के मामले में अपनाए गए दृष्टिकोण के समान वैश्विक रणनीति अपनाने की आवश्यकता हो सकती है।
- अपराधियों को न्याय के दायरे में लाने तथा स्थायी शांति की दिशा में काम करने के लिए धैर्य और निरंतर प्रयास आवश्यक होगा।
भारत के लिए फोकस के प्रमुख क्षेत्र
| फोकस क्षेत्र | संभावित कार्यवाहियाँ |
|---|---|
| यूएनएससी की भागीदारी | संयुक्त राष्ट्र महासभा में सशक्त वक्तव्य |
| आतंकवादी पदनाम | पहचाने गए आतंकवादियों और टीआरएफ को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल करने की मांग |
| एफएटीएफ | पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग |
| द्विपक्षीय संबंध | खराब कूटनीतिक संबंधों के कारण पाकिस्तान से सहयोग की उम्मीद नहीं |
| वैश्विक रणनीति | न्याय के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से जुड़े बहुआयामी प्रयास |
निष्कर्ष
निष्कर्ष के तौर पर, आतंकवाद से निपटने में भारत के सामने कई चुनौतियां हैं, खास तौर पर यूएनएससी की कमजोर प्रतिक्रिया के कारण। आगे बढ़ते हुए, भारत को बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा और एफएटीएफ जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों का लाभ उठाना चाहिए, साथ ही द्विपक्षीय सहयोग की कमी को दूर करना चाहिए। न्याय सुनिश्चित करने और स्थायी शांति प्राप्त करने में धैर्य, कूटनीतिक प्रयास और वैश्विक गठबंधन महत्वपूर्ण होंगे।
उपसभापति का पद प्रतीकात्मक या वैकल्पिक नहीं है
चर्चा में क्यों?
उपसभापति के कार्यालय में चल रही रिक्तता न केवल एक प्रक्रियागत चूक है; यह संविधान का उल्लंघन है तथा लोकतांत्रिक शासन की आधारशिला रखने वाली आम सहमति की राजनीति के सिद्धांतों के प्रति घोर उपेक्षा को दर्शाता है।
परिचय
लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद केवल औपचारिक पद नहीं है; यह एक संवैधानिक आवश्यकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में इस भूमिका को अनिवार्य किया गया है, जो संसद के निचले सदन के सुचारू संचालन के लिए इसके महत्व को उजागर करता है। हालाँकि, हाल के दिनों में, उपाध्यक्ष के पद की उपेक्षा की गई है, जिससे इसके महत्व और संवैधानिक प्रावधानों के पालन को लेकर चिंताएँ पैदा हुई हैं।
उपसभापति कार्यालय
- संविधान का अनुच्छेद 93 उपसभापति के चुनाव की अत्यावश्यकता पर बल देता है, जो दर्शाता है कि यह लोक सभा के कामकाज के लिए अनिवार्य आवश्यकता है।
- जैसा कि अनुच्छेद 94 में उल्लिखित है , उपसभापति सदन की निरंतरता, स्थिरता और संस्थागत संतुलन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
| प्रमुख तत्व | विवरण |
|---|---|
| मूल | भारत में उपसभापति की भूमिका की उत्पत्ति ब्रिटिश शासन के तहत औपनिवेशिक काल के दौरान हुई थी। |
| प्रारंभिक शीर्षक | केन्द्रीय विधान सभा में इस पद को उप राष्ट्रपति कहा जाता था । |
| प्रथम पदाधिकारी (औपनिवेशिक काल) | सच्चिदानंद सिन्हा इस पद पर आसीन होने वाले पहले व्यक्ति थे, जिन्हें 1921 में नियुक्त किया गया था। |
| स्वतंत्रता के बाद का निर्णय | संविधान सभा (विधान) ने संविधान को अपनाने से पहले उपसभापति की भूमिका को बरकरार रखने का निर्णय लिया था। |
| प्रथम लोक सभा उपाध्यक्ष | भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद एम.ए. अयंगर को लोकसभा का पहला उपाध्यक्ष चुना गया। |
| महत्व पर प्रकाश डाला गया | अय्यंगार की भूमिका महत्वपूर्ण थी क्योंकि 1956 में स्पीकर जी.वी. मावलंकर के आकस्मिक निधन के बाद उन्होंने स्पीकर के रूप में कार्य किया, जिससे उप-स्पीकर के पद की महत्ता रेखांकित हुई। |
उपसभापति की भूमिका और महत्व
- अध्यक्ष की सीमाएं: अध्यक्ष प्रत्येक सत्र की लंबी अवधि तक शारीरिक रूप से अध्यक्षता नहीं कर सकते।
- विशेषज्ञ अवलोकन: एससी कश्यप ने कहा कि अध्यक्ष अंतहीन रूप से कार्यवाही की अध्यक्षता नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने एक उपसभापति की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
- उपसभापति की मुख्य भूमिका: उपसभापति, अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान सदन के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करता है।
- विस्तारित जिम्मेदारियां: उपसभापति प्रमुख सत्रों की अध्यक्षता कर सकते हैं, महत्वपूर्ण समितियों का नेतृत्व कर सकते हैं, तथा तटस्थता की आवश्यकता वाली संवेदनशील बहसों को संभाल सकते हैं।
- निष्पक्षता की आवश्यकता: निर्वाचित होने के बाद, उपसभापति को राजनीतिक संबद्धता की परवाह किए बिना निष्पक्ष रूप से कार्य करना चाहिए।
- प्रतीकात्मक महत्व: यह कार्यालय राजनीतिक दलों के बीच द्विदलीय सम्मान और सहयोग को बढ़ावा देने में प्रतीकात्मक महत्व रखता है।
- विपक्षी उम्मीदवार की परंपरा: परंपरागत रूप से, उपसभापति का पद विपक्ष को दिया जाता है, हालांकि यह कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है।
- गैर-पक्षपातपूर्ण लोकाचार को सुदृढ़ बनाना: यह अभ्यास शक्ति को संतुलित करता है, दलों के बीच विश्वास का निर्माण करता है, तथा सदन की तटस्थता को बनाए रखता है।
उपसभापति का पद रिक्त
- लगातार रिक्ति: उपसभापति का पद 17वीं लोकसभा (2019-2024) के पूरे कार्यकाल के दौरान रिक्त रहा और 18वीं लोकसभा में भी यह पद रिक्त है।
- संवैधानिक विसंगति: यह रिक्ति न केवल प्रक्रियागत है, बल्कि एक महत्वपूर्ण संवैधानिक विसंगति है, क्योंकि यह पद संविधान द्वारा अनिवार्य है।
- ऐतिहासिक मिसाल: भारत के संसदीय इतिहास में उपसभापति के पद के लिए इतनी बड़ी रिक्ति कभी नहीं रही, जिससे यह स्थिति अभूतपूर्व बन गई।
- नियुक्ति की तात्कालिकता: हालांकि संविधान में उपसभापति के चुनाव के लिए कोई कठोर समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है, लेकिन "जितनी जल्दी हो सके" वाक्यांश की व्याख्या शीघ्र कार्रवाई के आह्वान के रूप में की जानी चाहिए, न कि सुविधा के रूप में।
- चिंताएं व्यक्त की गईं: लंबे समय से हो रही देरी संवैधानिक आदेशों के पालन और संसदीय मानदंडों के प्रति सम्मान के बारे में गंभीर प्रश्न उठाती है।
रिक्ति का प्रभाव
- संस्थागत सुरक्षा: यह रिक्ति संविधान द्वारा स्थापित संस्थागत सुरक्षा को कमजोर करती है, तथा प्रक्रियात्मक शक्ति को अध्यक्ष और सत्तारूढ़ दल के भीतर केन्द्रीकृत कर देती है।
- प्रतिसंतुलन समाप्त: उपसभापति की अनुपस्थिति एक महत्वपूर्ण प्रतिसंतुलन को समाप्त कर देती है, जिससे सदन की कार्यप्रणाली प्रभावित होती है।
- आपातकालीन तैयारी: किसी आपातकालीन स्थिति में, जहां अध्यक्ष पद पर बने रहने में असमर्थ हों (इस्तीफा, मृत्यु या हटाए जाने के कारण), उपसभापति की अनुपस्थिति से भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है और नेतृत्व शून्य हो सकता है।
- संसदीय परंपराओं की अवहेलना: उपसभापति की नियुक्ति में देरी संसदीय परंपराओं, विशेषकर विपक्ष को यह पद देने के अलिखित नियम की अवहेलना को दर्शाती है।
उपसभापति की भूमिका का महत्व
- संवैधानिक महत्व: संसद में संतुलन और स्थिरता बनाए रखने के लिए उपसभापति का पद आवश्यक है।
- ऐतिहासिक रूप से प्रतीकात्मक: यह भूमिका ऐतिहासिक रूप से संसद के कामकाज में समावेशिता और संयम का प्रतीक रही है।
- संवैधानिक अधिदेश: उपसभापति की अनुपस्थिति संवैधानिक लोकतंत्र और विधायी अखंडता के सिद्धांतों को चुनौती देती है।
- नेतृत्व में अतिरेक: उपसभापति एक महत्वपूर्ण पद है जो आपातकाल के दौरान नेतृत्व में लचीलापन और निरंतरता सुनिश्चित करता है।
आम सहमति की राजनीति को दरकिनार करना
- सक्रिय रूप से दरकिनार करना: उपसभापति की नियुक्ति में विफलता, सर्वसम्मति की राजनीति को सक्रिय रूप से दरकिनार करती है, जो सहयोगी शासन के संवैधानिक लोकाचार के विपरीत है।
- अतिरेक की आवश्यकता: संविधान निर्माताओं ने नेतृत्व की भूमिकाओं में अतिरेक की आवश्यकता का अनुमान लगाया था, तथा उन्होंने उपसभापति के महत्व पर बल दिया था।
- संस्थागत विश्वसनीयता बहाल करना: उपाध्यक्ष की नियुक्ति, अधिमानतः विपक्ष से, से संस्थागत विश्वसनीयता बहाल होगी और लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान होगा।
- विधायी कार्यवाही में संतुलन: विपक्ष के उपसभापति विधायी कार्यवाही में संतुलन लाएंगे, सहयोग को बढ़ावा देंगे और ध्रुवीकरण को कम करेंगे।
विधायी सुधार की आवश्यकता
- जारी रिक्तता: लम्बे समय से रिक्तता के कारण उपसभापति के चुनाव के संबंध में संवैधानिक भाषा को कड़ा करने के लिए विधायी सुधार की आवश्यकता उत्पन्न हो गई है।
- सुझाई गई समय-सीमा: एक विशिष्ट समय-सीमा (जैसे, नई लोकसभा की पहली बैठक के 60 दिनों के भीतर) लागू करने से देरी को रोका जा सकता है तथा अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकता है।
- वैकल्पिक दृष्टिकोण: राष्ट्रपति को एक निश्चित समय सीमा के भीतर उपसभापति के चुनाव की प्रक्रिया आरंभ करने की अनुमति देने वाली वैधानिक व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है।
- वर्तमान अस्पष्टता: प्रक्रिया में विद्यमान अस्पष्टता कार्यशील लोकतंत्र के लिए टिकाऊ नहीं है तथा इसका समाधान किया जाना आवश्यक है।
- संवैधानिक महत्व: विधायी अखंडता, निरंतरता और संवैधानिक लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए उपसभापति का पद महत्वपूर्ण है।
- संविधान का उल्लंघन: उपसभापति के पद की अवहेलना करना संविधान का उल्लंघन है तथा इससे वह लोकतांत्रिक संतुलन कमजोर होता है जिसे बनाए रखने का प्रयास किया जाता है।
निष्कर्ष
संसद के लिए संवैधानिक सिद्धांतों और संस्थागत अखंडता को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए उसे तुरंत उपसभापति नियुक्त करना चाहिए। यह भूमिका सिर्फ़ औपचारिकता नहीं है; यह स्थापित नियमों के अनुसार शासन करने के लिए सदन की प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है। इस नियुक्ति में विफल होने से लोकतांत्रिक शासन और संसदीय कार्यप्रणाली की नींव ही कमज़ोर हो जाती है।
|
7 videos|3454 docs|1081 tests
|
FAQs on The Hindi Editorial Analysis- 29th April 2025 - Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC
| 1. उपसभापति के पद की भूमिका क्या होती है? |  |
| 2. उपसभापति का चुनाव कैसे होता है? |  |
| 3. क्या उपसभापति का पद केवल एक प्रतीकात्मक पद है? |  |
| 4. उपसभापति और सभापति के बीच क्या अंतर है? |  |
| 5. उपसभापति का पद कौन से विशेष अधिकारों के साथ आता है? |  |




















