UPSC Exam > UPSC Notes > Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly > The Hindi Editorial Analysis- 2nd March 2024
The Hindi Editorial Analysis- 2nd March 2024 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC PDF Download
भारत के नए आपराधिक कानूनों में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के निहितार्थ
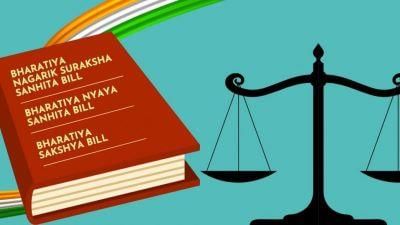
संदर्भ:
भारत सरकार द्वारा भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के आगामी कार्यान्वयन से उसके कानूनी ढांचे में एक ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक है। यह बदलाव 1 जुलाई, 2024 से लागू होने वाला है । गृह मंत्रालय (MHA) और राज्य सरकारों के नेतृत्व में यह बदलाव कानूनी रूपरेखाओं को आधुनिक बनाने और विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को संभालने में कानून प्रवर्तन क्षमताओं को मजबूत करने का लक्ष्य रखता है।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) में मुख्य परिवर्तन:
- वर्ष 1872 के पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम को प्रतिस्थापित करने के लिए लाए जा रहे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कई महत्वपूर्ण सुधारों को शामिल किया गया है, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के संबंध में। हालांकि भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं, फिर भी BSA बुनियादी साक्ष्य सिद्धांतों को बनाए रखते हुए डिजिटल युग के अनुकूल होगा।
इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की परिभाषा और स्पष्टता:
- एक निर्णायक कदम में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 'दस्तावेज़/अभिलेख' को व्यापक रूप से परिभाषित करता है, जिसमें अब स्पष्ट रूप से इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड भी शामिल हैं। यह समावेशी परिभाषा डिजिटल कलाकृतियों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करती है, जिसमें ईमेल, सर्वर लॉग, कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन जैसे विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में संग्रहीत दस्तावेज़, संदेश, वेबसाइट, स्थान संबंधी जानकारी और ध्वनि मेल संदेश आदि सभी शामिल हैं। लेकिन यह इन्हीं साधनों तक सीमित नहीं है, अतः ऐसी स्पष्टता विकसित हो रहे साक्ष्य मानकों के प्रति एक प्रगतिशील रुख को दर्शाती है।
इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता:
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता को संबोधित करती है, जिसमें अधिक विशिष्टता के लिए 'सेमी-कंडक्टर मेमोरी' और 'संचार उपकरण' जैसी शब्दावली का परिचय दिया गया है। इन परिष्करणों के बावजूद, मूल सिद्धांत सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2000 के अनुरूप हैं, जो कंप्यूटर मेमोरी में संग्रहीत और संचार उपकरणों के माध्यम से प्रसारित जानकारी की स्वीकार्यता को संरेखित करते हैं।
कानूनी मिसाल और प्रमाणन आवश्यकताएँ:
- अर्जुन पांडितराव खोटकर बनाम कैलाश कुशनराव गोरंट्याल और अन्य (2020) मामले संबंधी ऐतिहासिक निर्णय में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता से संबंधित मूलभूत सिद्धांतों को निर्धारित किया गया था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63(4) के तहत प्रमाण पत्र के लिए जनादेश, इसके पूर्ववर्ती भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी को दर्शाता है। यह प्रमाणपत्र, प्रमाणीकरण के लिए महत्वपूर्ण है, इसके लिए दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है: प्रासंगिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का संरक्षक और एक विशेषज्ञ।
हैश एल्गोरिथम और डेटा अखंडता:
- प्रमाणन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू विशिष्ट एल्गोरिदम के माध्यम से हैश मानों को सत्यापित करना है। बीएसए, SHA1, SHA 256, MD5, या किसी अन्य कानूनी रूप से स्वीकार्य मानक जैसे हैश एल्गोरिदम के उपयोग को अनिवार्य करता है। जबकि MD5 और SHA1 अन्य कमजोरियां प्रदर्शित करते हैं। इसके विपरीत SHA 256 को इसकी बेहतर सुरक्षा सुविधाओं के लिए जाना जाता है। सुरक्षित हैश एल्गोरिदम को अपनाने से डेटा की अखंडता सुनिश्चित होती है और छेड़छाड़ के जोखिम को कम किया जाता है।
चुनौतियाँ और व्यावहारिक निहितार्थ:
- विशेषज्ञ प्रमाणन की आवश्यकता व्यावहारिक चुनौतियाँ उत्पन्न करती है, विशेष रूप से साइबर प्रयोगशालाओं के कार्यभार के संबंध में। आपराधिक गतिविधियों में स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के सर्वव्यापी उपयोग के साथ, विशेषज्ञ की राय की मांग काफी बढ़ गई है। हालाँकि, राज्यों में कई साइबर लैब गैर-कानूनी रूप से संचालित हैं या आईटी अधिनियम के तहत विधिवत अधिसूचित नहीं हैं, जिसे उपयुक्त संसाधन की कमी के रूप में जाना जाता है।
दक्षता और प्रक्रियाओं के पालन में संतुलन:
- उपर्युक्त के अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण विचार प्रक्रियात्मक पालन और परिचालन दक्षता के बीच संतुलन स्थापित करना है। एक ओर जहां विशेषज्ञ प्रमाणन साक्ष्य मानकों को बढ़ाता है, वहीं दूसरी ओर इसके व्यापक अनुप्रयोग से संसाधनों पर दबाव पड़ सकता है और न्यायिक कार्यवाही में बाधा आ सकती है। इस संदर्भ में एक व्यावहारिक दृष्टिकोण में विशेषज्ञ राय का चयनित रूप से लाभ उठाना शामिल हो सकता है, विशेषतः उन मामलों पर जहां इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की अखंडता विवादित है।
जागरूकता और क्षमता निर्माण:
- नए कानूनों को लागू करने से पहले का संक्रमण काल जागरूकता बढ़ाने और क्षमता निर्माण पहल करने का एक उपयुक्त अवसर प्रस्तुत करता है। सार्वजनिक और निजी संस्थाओं अथवा सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं को एन्क्रिप्शन विधियों और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्रबंधन की बारीकियों के प्रति संवेदनशील बनाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कानून प्रवर्तन एजेंसियों को विकसित हो रही जांच आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने की आवश्यकता है।
भविष्य की रणनीतियां:
- यद्यपि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के भीतर अंतर्निहित सूक्ष्म प्रावधान कानून प्रवर्तन और न्यायिक कार्यवाही में समकालीन चुनौतियों के समाधान के लिए एक प्रगतिशील दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। तथापि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को परिभाषित और स्पष्ट करके, स्वीकार्यता मानदंड को बढ़ाकर, और हैश एल्गोरिदम के माध्यम से डेटा अखंडता पर जोर देकर, कानून डिजिटल युग में साक्ष्य प्रक्रिया को मजबूत करने का प्रयास करता है।
- हालाँकि, इन प्रावधानों के सफल एकीकरण के लिए केवल विधायी अधिनियमन पर्याप्त नहीं है। इसके लिए व्यापक जागरूकता अभियान, क्षमता वृद्धि उपाय और रणनीतिक संसाधन आवंटन की दिशा में समुचित प्रयास की आवश्यकता है। इस हेतु सार्वजनिक और निजी संस्थाओं को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, एन्क्रिप्शन विधियों और साइबर अपराध के उभरते परिदृश्य की जटिलताओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए।
- साथ ही, कानून प्रवर्तन एजेंसियों को डिजिटल जांच की जटिलताओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास और कौशल वृद्धि कार्यक्रमों में निवेश करना चाहिए। साइबर प्रयोगशालाओं को अत्याधुनिक तकनीक से लैस करने और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की बढ़ती मात्रा को संभालने में सक्षम प्रशिक्षित पेशेवरों से लैस करने की आवश्यकता है।
निष्कर्ष:
- भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का आसन्न कार्यान्वयन भारत के कानूनी ढांचे के विकास का प्रतीक है। ये विधायी सुधार एक परिवर्तनकारी चरण का प्रतीक हैं जो आधुनिक दुनिया की जटिलताओं के अनुकूल होने का प्रयास करता है, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के संदर्भ में।
- जैसे-जैसे भारत न्याय की खोज में डिजिटल साक्ष्य के जटिल क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, नवाचार और प्रक्रियात्मक कठोरता के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन अनिवार्य हो जाएगा। पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता के सिद्धांतों को बरकरार रखते हुए, आपराधिक न्याय प्रणाली नागरिकों के बीच विश्वास और विश्वास पैदा कर सकती है, जिससे कानून के शासन को मजबूत किया जा सकता है और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की जा सकती है।
- संक्षेप में, इन विधायी सुधारों का सफल कार्यान्वयन न केवल भारत के कानूनी परिदृश्य को आधुनिक बनाएगा बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि उभरती तकनीकी चुनौतियों के सामने न्याय सुलभ, न्यायसंगत और लचीला बना रहे।
The document The Hindi Editorial Analysis- 2nd March 2024 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC is a part of the UPSC Course Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly.
All you need of UPSC at this link: UPSC
|
3101 docs|1040 tests
|
FAQs on The Hindi Editorial Analysis- 2nd March 2024 - Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC
| 1. नए आपराधिक कानूनों में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य क्या है? |  |
उत्तर: इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का मतलब है किसी आपराधिक काम के सबूत जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में होते हैं, जैसे कि ईमेल, वेबसाइट के डेटा, सोशल मीडिया संदेश आदि।
| 2. भारत में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की महत्वता क्या है? |  |
उत्तर: इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की महत्वता यह है कि यह प्रमाणिक होता है और सीधे और तेजी से आपराधिक मामलों का समाधान करने में मदद करता है।
| 3. क्या इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के नए कानूनों में कोई बदलाव किया गया है? |  |
उत्तर: हां, भारत के नए आपराधिक कानूनों में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं जो इसे और प्रभावी बनाते हैं।
| 4. कैसे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को सुरक्षित रखा जा सकता है? |  |
उत्तर: इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को सुरक्षित रखने के लिए एन्क्रिप्शन तकनीक और सुरक्षित सर्वर उपयोग किया जा सकता है।
| 5. क्या इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के बिना भी अपराधिक मामले हल किए जा सकते हैं? |  |
उत्तर: हां, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के बिना भी अपराधिक मामले हल किए जा सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य स्थायी और प्रमाणित साबित होता है।
Related Searches




















