The Hindi Editorial Analysis- 30th June 2025 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC PDF Download
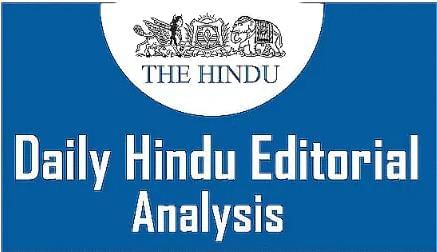
आईटी विधेयक 2025 के तहत डिजिटल खोज शक्तियों पर पुनर्विचार
चर्चा में क्यों?
हाल ही में वित्त मंत्री ने संसद में आयकर अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव रखा, जिससे कर अधिकारियों को तलाशी और जब्ती कार्रवाई के दौरान किसी व्यक्ति के "वर्चुअल डिजिटल स्पेस" तक पहुंच की अनुमति मिल सके। इस प्रस्ताव ने गोपनीयता, सरकारी अतिक्रमण और निरंतर निगरानी के बारे में महत्वपूर्ण चिंताएँ पैदा की हैं।
परिचय
वित्त मंत्री ने हाल ही में आयकर विधेयक, 2025 के भाग के रूप में संसद में प्रस्ताव रखा कि कर अधिकारियों को तलाशी और जब्ती कार्रवाई के दौरान किसी व्यक्ति के "वर्चुअल डिजिटल स्पेस" तक पहुँच प्रदान की जाए। इस प्रस्ताव के पीछे तर्क यह है कि वित्तीय गतिविधियों का ऑनलाइन क्षेत्र में स्थानांतरण हो रहा है, जिसके कारण कर प्रवर्तन के लिए एक समान डिजिटल दृष्टिकोण की आवश्यकता है। हालाँकि, यह दृष्टिकोण ऐसे कदम के गहन निहितार्थों को नज़रअंदाज़ करता है, जिससे गोपनीयता, अत्यधिक अधिकार और निरंतर निगरानी के बारे में गंभीर चिंताएँ पैदा होती हैं।
वर्तमान कानून बनाम प्रस्तावित परिवर्तन
धुंधली होती सीमाएं
पहलू | वर्तमान कानून (आयकर अधिनियम, 1961) | प्रस्तावित परिवर्तन (आयकर विधेयक, 2025) | चिंताएं व्यक्त की गईं |
|---|---|---|---|
खोज का दायरा | धारा 132 के अंतर्गत तलाशी और जब्ती की अनुमति है, लेकिन केवल घरों, कार्यालयों और लॉकरों जैसे भौतिक स्थानों में। | किसी व्यक्ति के "वर्चुअल डिजिटल स्पेस" जैसे ईमेल, क्लाउड स्टोरेज और सोशल मीडिया खातों को कवर करने के लिए शक्तियों का विस्तार करता है। | विशाल और अक्सर असंबंधित डिजिटल सामग्री तक पहुंच के कारण गोपनीयता का जोखिम बढ़ जाता है। |
खोज का आधार | तलाशी को भौतिक स्थानों पर पाई गई संदिग्ध अघोषित आय या परिसंपत्तियों से जोड़ा जाना चाहिए। | यह स्पष्ट संबंध कमजोर हो गया है; डिजिटल क्षेत्र अधिक व्यापक हो गया है और हमेशा वित्तीय गलत कार्यों से संबंधित नहीं होता। | डिजिटल पहुंच में अतिक्रमण और स्पष्ट उद्देश्य की कमी के प्रश्न उठते हैं। |
डिजिटल स्पेस की परिभाषा | लागू नहीं. | इसमें ईमेल, क्लाउड ड्राइव, ऐप्स, सोशल मीडिया और "कोई भी अन्य समान स्थान" शामिल है - जो एक अस्पष्ट और खुला शब्द है। | व्यापक परिभाषा के कारण दुरुपयोग या अपरिभाषित सीमाओं का खतरा उत्पन्न हो सकता है। |
प्रभावित हितधारक | तलाशी केवल जांच के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति को ही प्रभावित करती है। | डिजिटल डेटा में अन्य लोगों की जानकारी शामिल हो सकती है - जैसे मित्र, परिवार, ग्राहक या पेशेवर संपर्क। | इससे असंबद्ध लोगों की निजता का अनायास उल्लंघन हो सकता है। |
प्राधिकरण शक्तियां | पहुंच भौतिक कुंजियों और स्थानों तक सीमित थी। | कर अधिकारी अब डिवाइस या ऑनलाइन खातों में प्रवेश करने के लिए पासवर्ड या एक्सेस कोड को बदल सकते हैं। | यह स्पष्ट नहीं है कि यह कैसे काम करेगा, विशेषकर व्हाट्सएप जैसे एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म पर। |
पेशेवरों पर प्रभाव | पत्रकारों जैसे पेशेवरों को सीधे तौर पर खोजों में लक्षित नहीं किया गया। | अप्रकाशित कहानियां, गोपनीय स्रोत या निजी संचार जैसे संवेदनशील डेटा उजागर हो सकते हैं। | पत्रकारिता की स्वतंत्रता और पेशेवर गोपनीयता को खतरा हो सकता है। |
कानूनी सुरक्षा | न्यायालयों को स्पष्ट साक्ष्य की आवश्यकता होती है, और "विश्वास करने का कारण" शब्द के लिए पर्याप्त सामग्री की आवश्यकता होती है। | विधेयक में डिजिटल खोजों के लिए कोई अतिरिक्त सुरक्षा उपाय प्रदान नहीं किए गए हैं। | यह उस सिद्धांत का उल्लंघन है जिसके अनुसार तलाशी और जब्ती गोपनीयता का गंभीर उल्लंघन है। |
न्यायिक दृष्टिकोण | सर्वोच्च न्यायालय गोपनीयता को मौलिक मानता है तथा तलाशी शक्तियों के सख्त प्रयोग पर जोर देता है। | वर्ष 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल जब्ती पर अंतरिम दिशा-निर्देश जारी किए और सरकार से उचित प्रोटोकॉल बनाने को कहा। | विधेयक इन निर्देशों की अनदेखी कर सकता है, जिससे कानूनी विवाद का खतरा बढ़ सकता है। |
प्रस्तावित प्रावधान में खामियां (आयकर विधेयक, 2025)
- प्रस्तावित कानून में न्यायिक निगरानी, स्पष्ट सीमाओं और सुरक्षात्मक उपायों का अभाव है।
- यह डिजिटल डेटा की गहराई और संवेदनशील प्रकृति के बारे में हमारी खराब समझ को दर्शाता है।
- आज इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व्यक्तिगत, व्यावसायिक और गोपनीय सामग्री संग्रहित करते हैं, जिसका कानून हिसाब नहीं रख पाता।
- यह प्रावधान “विश्वास करने के कारण” के प्रकटीकरण पर रोक लगाता है, जो सीधे पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों के खिलाफ है।
- इससे बिना किसी बाहरी जांच या प्रक्रियात्मक संतुलन के प्राधिकारियों द्वारा अनियंत्रित घुसपैठ हो सकती है।
डिजिटल खोज और गोपनीयता में वैश्विक सर्वोत्तम अभ्यास
कनाडा: अधिकार और स्वतंत्रता चार्टर की धारा 8 “अनुचित तलाशी या जब्ती” से सुरक्षा प्रदान करती है और यह आवश्यक बनाती है:
- पूर्व प्राधिकरण
- तटस्थ न्यायिक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन
- तलाशी के लिए उचित और संभावित आधार
संयुक्त राज्य अमेरिका:
- करदाता अधिकार विधेयक यह सुनिश्चित करता है कि सभी प्रवर्तन कार्रवाइयां वैध हों तथा अत्यधिक हस्तक्षेपकारी न हों।
- रिले बनाम कैलिफोर्निया मामले में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में डिजिटल डेटा की गहन व्यक्तिगत प्रकृति के कारण उस तक पहुंचने से पहले वारंट लेना अनिवार्य कर दिया गया है।
ये मानक वैधानिक सुरक्षा, उचित प्रक्रिया और आनुपातिक प्रवर्तन की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं - जो कि वर्तमान में भारतीय प्रस्ताव में प्रतिबिंबित नहीं है।
भारत के प्रस्तावित आयकर प्रावधान से संबंधित प्रमुख मुद्दे
- प्रस्तावित कानून किसी व्यक्ति के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा तक व्यापक पहुंच की अनुमति देता है।
- इसमें किसी वारंट की आवश्यकता नहीं है, कोई प्रासंगिकता फिल्टर नहीं है, तथा वित्तीय और गैर-वित्तीय डेटा के बीच कोई पृथक्करण नहीं है।
- इस दृष्टिकोण से सभी डिजिटल सामग्री को निष्पक्ष खेल मानकर व्यक्तिगत गोपनीयता के उल्लंघन का खतरा है।
- इसमें न्यायिक जांच का अभाव है तथा दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई सुरक्षात्मक उपाय भी नहीं है।
सर्वोच्च न्यायालय के गोपनीयता मानकों का उल्लंघन
न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ के ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने गोपनीयता प्रतिबंधों के लिए चार-भागीय परीक्षण निर्धारित किया:
- कार्रवाई का उद्देश्य वैध होना चाहिए।
- उस लक्ष्य को प्राप्त करना आवश्यक है।
- इसमें यथासंभव न्यूनतम हस्तक्षेपकारी विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए।
- इसे आनुपातिकता के सिद्धांत को पूरा करना होगा।
नया कर प्रस्ताव इस परीक्षण में विफल हो जाता है, क्योंकि यह न्यायिक निगरानी के बिना व्यक्तिगत डिजिटल डेटा तक बेरोकटोक पहुंच की अनुमति देता है और इसमें न्यूनतम हस्तक्षेपकारी साधनों का उपयोग नहीं किया जाता है।
आगे बढ़ने का रास्ता
आगे बढ़ने का तरीका डिजिटल प्रवर्तन को अस्वीकार करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि यह आनुपातिकता, वैधानिकता और पारदर्शिता के सिद्धांतों पर आधारित हो। जैसे-जैसे भारत अधिक डिजिटल कर ढांचे की ओर बढ़ रहा है, यह आवश्यक है कि नियामक नियंत्रण के नाम पर व्यक्तिगत गोपनीयता का बलिदान न किया जाए। स्पष्ट जाँच और जवाबदेही के बिना निगरानी शासन को मजबूत नहीं करती है - इससे अतिक्रमण और शक्ति के संभावित दुरुपयोग की संभावना होती है।
निष्कर्ष
अभी भी सुधार की गुंजाइश है। वर्तमान में विधेयक की जांच कर रही चयन समिति के पास इन चिंताओं को सार्थक रूप से संबोधित करने का अवसर है। यह 'वर्चुअल डिजिटल स्पेस' की परिभाषा को सीमित करके, यह सुनिश्चित करके कि पहुँच प्रदान करने से पहले न्यायिक वारंट की आवश्यकता है, और इस तरह के डिजिटल घुसपैठ के लिए स्पष्ट कारण बताना अनिवार्य बनाकर ऐसा कर सकता है। उतना ही महत्वपूर्ण यह है कि जिन व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, उनके लिए उचित निवारण प्रणाली होनी चाहिए। लोकतंत्र में, प्रवर्तन को मजबूत करना कभी भी मौलिक स्वतंत्रता की कीमत पर नहीं आना चाहिए।
एक साल बाद - औपनिवेशिक युग के कानून से लेकर नई आपराधिक संहिता तक
चर्चा में क्यों?
प्रौद्योगिकी लाभदायक रही है, लेकिन जांच अधिकारियों (आईओ) से फीडबैक प्राप्त करना महत्वपूर्ण है क्योंकि वे इन उपकरणों का प्रभावी उपयोग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
परिचय
ब्रिटिश काल के पुराने कानूनों की जगह तीन नए आपराधिक कानून लागू हुए करीब एक साल हो चुका है। केंद्र सरकार ने भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह क्रमशः भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) पेश किए हैं।
- पुलिसकर्मी धीरे-धीरे नए कानूनों और उनके प्रावधानों के आदी हो रहे हैं।
- अधिकांश प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) अब अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (सीसीटीएनएस) के माध्यम से पंजीकृत की जा रही हैं, जो अंतर-संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) का एक महत्वपूर्ण घटक है।
- पुराने कानूनों से नए कानूनों में सुचारू परिवर्तन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है, विशेषकर पुलिस स्टेशन स्तर पर।
- अब शून्य एफआईआर को सीसीटीएनएस के माध्यम से उसी राज्य के उपयुक्त पुलिस स्टेशनों को निर्देशित किया जा रहा है, जिसका श्रेय गृह मंत्रालय को जाता है।
- पुलिस व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण प्रगति 'ई-साक्ष्य' मोबाइल ऐप का शुभारंभ है, जिसे वास्तविक समय में साक्ष्य संग्रहण और भंडारण की सुविधा के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) द्वारा गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित यह ऐप आईसीजेएस के प्रबंधन के लिए एनआईसी की व्यापक जिम्मेदारी का हिस्सा है, जो पुलिस, फोरेंसिक प्रयोगशालाओं, अभियोजन, जेलों और अदालतों सहित आपराधिक न्याय प्रणाली के विभिन्न घटकों को जोड़ता है।
- यद्यपि नए कानूनों में परिवर्तन मुख्यतः एक तकनीकी प्रक्रिया है, लेकिन 'ई-साक्ष्य' ऐप दैनिक पुलिस गतिविधियों में ठोस बदलाव ला रहा है।
- जांच अधिकारियों (आईओ) से प्राप्त फीडबैक महत्वपूर्ण है क्योंकि वे नए कानूनों के कार्यान्वयन का नेतृत्व करते हैं और आगे के सुधारों के लिए उनका इनपुट मूल्यवान होता है।
चित्रों और वीडियो की अनिवार्य रिकॉर्डिंग
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के अनुसार जांच अधिकारियों (आईओ) को ऑडियो-वीडियो टूल का उपयोग करके विशिष्ट प्रक्रियाओं को रिकॉर्ड करना आवश्यक है, जिससे कुछ मामलों में यह अनिवार्य हो जाता है जबकि अन्य में वैकल्पिक होता है। 'ई-साक्ष्य' ऐप बीएनएसएस के छह महत्वपूर्ण प्रावधानों के अनुरूप है, जो निम्नलिखित को सुविधाजनक बनाता है:
- धारा 105: ऑडियो-वीडियो माध्यम से तलाशी और जब्ती की रिकॉर्डिंग।
- धारा 185: पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई तलाशी प्रक्रियाओं का दस्तावेजीकरण।
- धारा 176: महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र करने के लिए अपराध स्थलों की वीडियोग्राफी।
- धारा 173: सटीक और विश्वसनीय साक्ष्य के लिए गवाहों के बयान दर्ज करना।
- धारा 180: व्यापक दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करने के लिए गवाहों के बयान दर्ज करने का एक और प्रावधान।
- धारा 497: परीक्षण के दौरान संपत्ति की अभिरक्षा और निपटान का प्रबंधन।
हालाँकि गंभीर अपराधों के लिए नई भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन जांच अधिकारी अपने काम में 'ई-साक्ष्य' ऐप को लाभकारी पा रहे हैं। यह ऐप उन्हें मौके पर ही फोटो और वीडियो कैप्चर करने में सक्षम बनाता है, जिसमें भौगोलिक निर्देशांक और समय-चिह्न भी शामिल होते हैं, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ती है। यह विकास तलाशी और जब्ती अभियानों में शामिल प्रक्रियाओं में अधिक सार्वजनिक विश्वास को बढ़ावा देता है।
- गवाहों की वीडियो रिकॉर्डिंग: अपराध स्थल पर गवाहों की वीडियो रिकॉर्डिंग करने से बाद में उनकी उपस्थिति से इनकार करने की संभावना कम हो जाती है तथा उनके बयानों की सत्यनिष्ठा सुनिश्चित होती है।
- जवाबदेही के लिए सेल्फी फीचर: ऐप का 'सेल्फी' फीचर जांच अधिकारियों को अनौपचारिक रूप से अधीनस्थों को जांच कार्य सौंपने से रोककर जवाबदेही को बढ़ाता है, जिससे जांच की गुणवत्ता बनी रहती है।
- फोरेंसिक विशेषज्ञ की आवश्यकता: बीएनएसएस की धारा 176 अपराध स्थल पर फोरेंसिक विशेषज्ञ की उपस्थिति को अनिवार्य बनाती है, जिससे साक्ष्य संग्रहण के मानकों में सुधार होता है।
- अपराध स्थलों पर पुलिस कुत्तों का उपयोग संदिग्धों का पता लगाने और अतिरिक्त साक्ष्य एकत्र करने में सहायक होता है।
- फोरेंसिक अवसंरचना को मजबूत करना: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा घोषित छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) और एक राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) की स्थापना से पुलिस की फोरेंसिक क्षमताओं को और मजबूती मिलेगी।
कार्यान्वयन में लंबित चुनौतियाँ
- 'ई-साक्ष्य' के उपयोग में सुधार: जांच में 'ई-साक्ष्य' ऐप के बेहतर उपयोग की आवश्यकता है।
- साक्ष्य भण्डारण तक पहुंच: वर्तमान में, ऐप के माध्यम से प्राप्त फोटो और वीडियो को राष्ट्रीय सरकारी क्लाउड (एनजीसी) पर साक्ष्य लॉकर्स में संग्रहीत किया जाता है, लेकिन अदालतों के पास इंटर-ऑपरेबल आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) के माध्यम से इस साक्ष्य तक सीधी पहुंच नहीं है।
- डेटा जमा करने की प्रक्रिया: जांच अधिकारी (आईओ) अक्सर डेटा को सीसीटीएनएस के माध्यम से कॉपी करके और पेन ड्राइव जैसे बाहरी उपकरणों का उपयोग करके अंतिम केस रिपोर्ट के साथ जमा करके डुप्लिकेट करते हैं। इससे अतिरिक्त काम होता है और स्टोरेज डिवाइस की लागत बढ़ जाती है।
डिवाइस और एक्सेस संबंधी समस्याएं
- साक्ष्य संकलन के लिए व्यक्तिगत उपकरण: कई जांच अधिकारी (आईओ) अभी भी साक्ष्य संकलन के लिए अपने निजी मोबाइल फोन का उपयोग कर रहे हैं, जो आधिकारिक कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है।
- नए एंड्रॉयड फोन की आवश्यकता: जिन आईओ के पास संगत एंड्रॉयड फोन (संस्करण 10 या उच्चतर) नहीं थे, उन्हें नए डिवाइस खरीदने पड़े, क्योंकि 'ई-साक्ष्य' ऐप को कम से कम 1 जीबी स्टोरेज स्पेस की आवश्यकता होती है।
- पुलिस स्टेशनों में टैबलेट की कमी: कुछ पुलिस स्टेशनों को उपयोग के लिए केवल एक टैबलेट ही उपलब्ध कराया गया है, जो अपर्याप्त है, क्योंकि प्रत्येक स्टेशन से कई आईओ काम करते हैं।
ऐप में कार्यक्षमता सीमाएँ
- वीडियो की अवधि और मात्रा: प्रत्येक वीडियो को अधिकतम 4 मिनट तक रिकॉर्ड किया जा सकता है, लेकिन कैप्चर किए जाने वाले कुल वीडियो की संख्या पर कोई सीमा नहीं है।
- एफआईआर के साथ मीडिया प्रबंधन: यदि कोई एफआईआर लिंक है, तो खराब गुणवत्ता वाली छवियों या वीडियो को हटाया या फिर से रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। इसके विपरीत, यदि कोई एफआईआर लिंक नहीं है, तो मीडिया को हटाया और फिर से कैप्चर किया जा सकता है, लेकिन केवल पांच साक्ष्य आईडी (एसआईडी) ऑफ़लाइन बनाई जा सकती हैं।
- ऑफलाइन डेटा अपलोड: ऑफलाइन मोड में, डिवाइस के नेटवर्क रेंज में आने पर नए साक्ष्य के लिए स्थान खाली करने हेतु डेटा अपलोड किया जाना चाहिए।
अभियुक्त की अनिच्छा एवं व्यावहारिक कठिनाइयाँ
- आरोपी व्यक्तियों की हिचकिचाहट: आरोपी व्यक्ति अक्सर उन स्थानों का संकेत देते समय दर्ज होने में अनिच्छा दिखाते हैं जहाँ हथियार या ड्रग्स छिपाए गए हैं। यह अनिच्छा जांच के दौरान व्यावहारिक चुनौतियों का सामना करती है।
- 'ई-साक्ष्य' का प्रभाव: आरोपी व्यक्तियों की झिझक के बावजूद, 'ई-साक्ष्य' ऐप जांच की गुणवत्ता बढ़ाने और मजबूत सजा दिलाने में योगदान देने वाला एक परिवर्तनकारी उपकरण साबित हो रहा है। ऐप की विशेषताएं और कार्यक्षमता जांच प्रक्रिया में महत्वपूर्ण अंतर ला रही हैं।
कानूनी सुरक्षा और तकनीकी अंतराल
- हैश मान और प्रमाणपत्र निर्माण: यह ऐप द्वितीयक इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को मान्य करने के लिए SHA256 और प्रमाणपत्र का उपयोग करके हैश मान तैयार करता है, जिससे एकत्रित साक्ष्य की अखंडता सुनिश्चित होती है।
- साइबर अपराध मामलों के लिए विशेषज्ञ की राय: साइबर अपराध मामलों में, इलेक्ट्रॉनिक जब्ती से निपटने के लिए विशेषज्ञ की राय आवश्यक है, जो इन स्थितियों में विशेष ज्ञान की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।
- राज्य फोरेंसिक लैब की अधिसूचना: छत्तीसगढ़ जैसी कुछ राज्य फोरेंसिक लैब को अभी तक आईटी अधिनियम के तहत अधिसूचित नहीं किया गया है, जिससे साइबर फोरेंसिक लैब की स्थापना में देरी हो रही है। इस देरी से साइबर अपराध के मामलों की समय पर प्रक्रिया प्रभावित होती है।
अपराधों के पंजीकरण में अस्पष्टता
- संज्ञेय अपराध और चोरी की सीमा: बीएनएस की धारा 303(1) के तहत, चोरी को संज्ञेय अपराध मानने की सीमा स्पष्ट नहीं है, जिसके कारण पंजीकरण प्रथाओं में असंगतताएं पैदा होती हैं।
- छोटे-मोटे संगठित अपराधों का पंजीकरण: जुआ जैसे छोटे-मोटे संगठित अपराधों को धारा 112 के तहत पंजीकृत किया जा रहा है, जबकि परिभाषा अस्पष्ट और खुली प्रकृति की है, जिससे अपराध पंजीकरण में अस्पष्टता पैदा हो रही है।
साक्ष्य और चिकित्सा रिपोर्ट के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग
- साक्ष्य और गवाहों की जांच के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग: बीएनएसएस की धारा 530 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जांच अधिकारियों (आईओ) सहित साक्ष्य और गवाहों की जांच की अनुमति देती है। हालाँकि, इस प्रथा को अभी तक जांच में व्यापक रूप से नहीं अपनाया गया है।
- बलात्कार पीड़ितों के लिए मेडिकल जांच रिपोर्ट: जांच अधिकारी बीएनएसएस की धारा 184 के तहत बलात्कार पीड़ितों के लिए मेडिकल जांच रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए सात दिन की समय सीमा की सराहना करते हैं। इस समय सीमा को ऐसे संवेदनशील मामलों को समय पर निपटाने के लिए लाभकारी माना जाता है।
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देरी: मेडिकल जांच रिपोर्ट के लिए सात दिन की समय सीमा के सकारात्मक पहलुओं के बावजूद, जांच अधिकारियों को अभी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त करने में देरी का सामना करना पड़ता है, जिससे जांच की प्रगति में बाधा आ सकती है।
- छत्तीसगढ़ में मेडलिएपीआर प्रणाली का परीक्षण: एनआईसी हरियाणा द्वारा विकसित मेडलिएपीआर प्रणाली का वर्तमान में छत्तीसगढ़ में परीक्षण किया जा रहा है। इस प्रणाली का उद्देश्य सीसीटीएनएस के माध्यम से पुलिस को मेडिकल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के तेजी से डिजिटल प्रसारण की सुविधा प्रदान करना है, जिससे रिपोर्ट वितरण की दक्षता में सुधार होगा।
निष्कर्ष
- अब सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश नए कानूनों को लागू कर रहे हैं, इसलिए उनकी उपयोगिता का आकलन करने और जांच अधिकारियों (आईओ) के सामने आने वाली चुनौतियों और अदालतों में कानूनी मुद्दों का समाधान करने के लिए फीडबैक एकत्र करना महत्वपूर्ण है।
- वित्त पोषण और सहायता में वृद्धि: फोरेंसिक और प्रौद्योगिकी के लिए वित्त पोषण और सहायता में वृद्धि की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जांच अधिकारी काम के लिए व्यक्तिगत उपकरणों पर निर्भर न हों और प्रत्येक जिले में अपनी स्वयं की मोबाइल फोरेंसिक प्रयोगशाला इकाई हो।
- निरंतर सुधार: फोरेंसिक और तकनीकी क्षमताओं में चल रहे सुधार नए कानूनों की प्रभावशीलता और आपराधिक न्याय प्रणाली की दक्षता में योगदान देंगे।
|
7 videos|3454 docs|1081 tests
|
FAQs on The Hindi Editorial Analysis- 30th June 2025 - Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC
| 1. आईटी विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? |  |
| 2. डिजिटल खोज शक्तियों में क्या बदलाव अपेक्षित हैं? |  |
| 3. औपनिवेशिक युग के कानूनों का प्रभाव क्या है? |  |
| 4. नई आपराधिक संहिता में क्या विशेषताएँ होगी? |  |
| 5. आईटी विधेयक के अंतर्गत नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी? |  |





















